भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करते हुए गैर-वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया गया। परिणामस्वरूप गैर-वन क्षेत्रों में बांस कटाई और परिवहन के लिये अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। बांस किसानों को बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक व आर्थिक लाभ तथा आजीविका के अवसर प्रदान कराता है। ध्यातव्य है कि वर्गीकरण विज्ञान (Taxonomy) के तहत बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किंतु पूर्ववर्ती अधिनियम में इसे वृक्ष की परिभाषा में शामिल करने से इसके लिये पारगमन परमिट की आवश्यकता होती थी, भले ही यह निजी भूमि पर उगाया जाता हो। वन अधिकार अधिनियम, 2006 में बांस को गैर-इमारती वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि वन अधिनियम में इसे इमारती लकड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम, 2017 से यह विसंगति दूर हुई है।
प्रमुख बिंदु
- यह अधिनियम बांस के पेड़ों को काटने या इसकी ढुलाई के लिये अनुमति हासिल करने से छूट प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा से बांस शब्द को हटा दिया गया है।
- इससे गैर-वन भूमि पर बांस के वृक्षारोपण और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा तथा गांवों और छोटे शहरों में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस प्रकार चीन एवं वियतनाम जैसे देशों से आयात पर निर्भरता भी कम होगी।
- वन क्षेत्रों में उगाए गए बांस को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- सरकार गैर-वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और देश में हरित आवरण (Green Cover) को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है।
- भारत में उपलब्ध खेती योग्य व्यर्थ 12.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में खेती के लिये यह एक व्यवहार्य विकल्प सिद्ध हो सकता है।
कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्त्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसकी हरियाली की स्थिति में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिये आवश्यक तत्त्व नष्ट होते जा रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु व मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिये हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना सड़े-गले हरे पौधे (दलहनी एवं अन्य फसलों अथवा उनके भाग) को जब मृदा की नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिये खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के उपयोग से भूमि में न सिर्फ नाइट्रोजन उपलब्ध होता है बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार होता है। इससे भूमि में न सिर्फ सूक्ष्म तत्त्वों की आपूर्ति होती है बल्कि साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाती है।
हरी खाद के लाभ
- हरी खाद केवल नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों का ही स्रोत नहीं है बल्कि इससे मृदा को कई अन्य आवश्यक पोषक तत्त्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
- हरी खाद के प्रयोग से मृदा भुरभुरी, वायु संचार में अच्छी, जलधारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीयता/क्षारीयता में सुधार एवं मृदा क्षरण में भी कमी होती है।
- हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- हरी खाद से मृदाजनित रोगों में भी कमी आती है।
- इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके भी टिकाऊ खेती कर सकते हैं।
हरी खाद वाली फसलें
हरी खाद के लिये दलहनी फसलों में सनई (सनहेंप) ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि फसलों का उपयोग किया जाता है। इस फसलों की वृद्धि शीघ्र व कम समय में हो जाती है, पत्तियां वज़नदार एवं संख्या में अधिक संख्या में रहती हैं एवं इनको उर्वरक तथा जल की आवश्यकता कम होती है, जिससे कम लागत में अधिक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन को वातावरण से मृदा में स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं।
आदर्श हरी खाद फसल के गुण
हरी खाद के मुख्य चार गुण हैं-
- उगाने में न्यूनतम खर्च।
- न्यूनतम सिंचाई, कम से कम पादप संरक्षण।
- खरपतवारों को दबाते हुए जल्दी बढ़त प्राप्त करने तथा विपरीत परिस्थितियों में उगने की क्षमता।
- कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है।
जलवायु दबाव, जलवायु तंत्र के अंतर्गत वे कारक होते हैं, जिनकी वृद्धि या कमी से जलवायु तंत्र पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु दबाव द्वारा पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ये दबाव प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होते हैं-
प्राकृतिक दबाव
- सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में बदलाव।
- पृथ्वी की कक्षा में बहुत धीमा परिवर्तन।
- ज्वालामुखीय उद्गार।
मानव प्रेरित दबाव
- हरित गृह गैसों का उत्सर्जन।
- जीवाश्म ईंधन के जलने से एरोसॉल का उत्सर्जन।
- भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे- निर्वनीकरण आदि।
जलवायु दबाव के प्रकार
जलवायु दबाव दो प्रकार के होते हैं-
- सकारात्मक दबाव- सकारात्मक दबाव का प्रयास पृथ्वी को गर्म करना होता है। जैसे- सूर्य के प्रकाश में वृद्धि तथा हरित गृह गैसों के कारण पृथ्वी का गर्म होना।
- नकारात्मक दबाव- नकारात्मक दबाव द्वारा पृथ्वी ठंडी होती है। जैसे- अत्यधिक बड़े ज्वालामुखीय उद्गार उत्सर्जन द्वारा वातावरणीय एरोसॉल एवं जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा उत्सर्जित एरोसॉल से पृथ्वी ठंडी होती है।
जलवायु दबाव को प्रभावित करने वाले कारक
- एरोसॉल (Aerosol)- एरोसॉल वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं, जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल या अम्लीय बूँदों आदि से बने होते हैं। वातावरणीय एरोसॉल के अंतर्गत ज्वालामुखीय धूल, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित राख एवं वनों के जलने से निर्मित कण आदि सभी आते हैं। एरोसॉल का सामान्य गुण नकारात्मक दबाव (Negative Forcing) वाला होता है परंतु कुछ भारी प्रकार के एरोसॉल सकारात्मक दबाव (Positive Forcing) भी प्रदर्शित करते हैं।
- प्राकृतिक एरोसॉल- ज्वालामुखीय उद्गार द्वारा प्राकृतिक रूप से एरोसॉल का निर्माण होता है जो कि वातावरण को ठंडा करते हैं। कभी-कभी बड़े ज्वालामुखीय उद्गार द्वारा वातावरण के शीतल होने का प्रभाव (1 वर्ष या उससे अधिक भी) तब तक रहता है जब तक कि वातावरण से सल्फेट कण निकलकर नीचे न बैठ जाएँ।
- मानव जनित हरित गृह गैस- मानव जनित हरित गृह गैसें सकारात्मक जलवायु दबाव के अंतर्गत आती हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड अकेले जलवायु दबाव का सबसे बड़ा कारक है, जो कि पूर्व-औद्योगिक युग से कुल सकारात्मक दबाव के आधे से अधिक हेतु ज़िम्मेदार है।
- मृदामंडल में उपस्थित जल की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता उसमें रहने वाले पौधों तथा जंतुओं को प्रभावित करती है। यह मृदा में स्थित पोषक तत्त्वों को घोलकर मृदा घोल (Soil Solution) बनाने में मदद करता है।
- मृदा में स्थित जल की मात्रा का निर्धारण, जलवर्षा तथा हिमद्रवित जल के मृदा में अंतःसंचरण (Infiltration) की दर तथा मृदा की जलधारण करने की क्षमता (Water Retention Capacity) के आधार पर किया जाता है।
- मृदा के आयतन के संदर्भ में स्थित जल की मात्रा के आधार पर मृदा में ठोस पदार्थों, जल तथा वायु के अनुपातों की तीन दशाओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है-
- संतृप्त अवस्था (Saturated Stage)- इस अवस्था में मृदा में स्थित खाली स्थान जल से भरे होते हैं एवं ऐसी मिट्टी अतिरिक्त जल की मात्रा नहीं सोख पाती है।
- भूमि क्षमता अवस्था (Field Capacity Stage)- जब मृदा में स्थित कुल खाली स्थानों का 50% जल द्वारा तथा शेष 50% भाग वायु द्वारा भरा होता है तो यह भूमि क्षमता अवस्था कहलाती है।
- म्लान अवस्था (Wilting Stage)- जब मृदा में वाष्पीकरण एवं पौधों द्वारा मृदा-जल को ग्रहण करने के बाद जल का अभाव हो जाता है तो यह म्लान अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में पौधे जल के अभाव में मुरझा जाते हैं।
- संयुक्त अवस्था एवं म्लान अवस्था दोनों ही मृदा जीवों तथा पौधों के लिये प्रतिकूल होती हैं। इस प्रकार भूमि क्षमता अवस्था तथा म्लान अवस्था के बीच की स्थिति मृदा स्थित पौधों तथा जंतुओं के लिये सर्वाधिक अनुकूल होती है।
- मृदा में पाया जाने वाला जल निम्नलिखित प्रकार का होता है-
- गुरुत्वीय जल (Gravitational Water)- वर्षा के बाद मृदा के धरातलीय परत के तात्कालिक रूप से संतृप्त होने के पश्चात् यह जल गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी गहराई अथवा भूमि जल स्तर तक पहुँच जाता है, इसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। इस जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते।
- केशिका जल (Capillary Water)- जब धरातलीय जल मृदा की ऊपरी सतह से रिस कर नीचे आता है तब वह पीछे पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में नमी छोड़ आता है, जो केशिका जल कहलाता है। यह पृष्ठ तनाव बलों (Surface Tension Forces) द्वारा बरकरार बने रहता है तथा गुरुत्व खिंचाव से प्रभावित नहीं होता। यह जल पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषण हेतु उपलब्ध होता है।
- आर्द्रता जल (Hygroscopic Water)- मिट्टी कणों के चारों तरफ पतली वाष्पीय परत के रूप में मृदा द्वारा कसकर पकड़े हुए जल को आर्द्रता जल कहते हैं। इस जल को भी पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं करते।
- रसायन युक्त या रवे का जल (Chemically or Crystalline Combined Water)- जो जल मृदा खनिजों की संरचना में रासायनिक रूप से संबद्ध रहता है उसे रसायन युक्त या रवे का जल कहते हैं। यह जल भी पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है।
ये दोनों तरह के कार्बन, कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। काले एवं भूरे कार्बन से अलग ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गृह गैसों के अधिग्रहण (Sequestration) का कार्य करते हैं।
- ग्रीन कार्बन (Green Carbon)- प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संगृहीत हो जाता है, ग्रीन कार्बन कहलाता है। यह वैश्विक कार्बन चक्र का जीवंत भाग है। पौधों एवं फसलों में यह कार्बन लघु जीवन अवधि के कारण थोड़े समय के लिये रहता है एवं कुछ समय बाद वे इस कार्बन को मुक्त कर देते हैं परंतु वन के बायोमास इस कार्बन को कई सदियों तक संचित किये रहते हैं।
- ब्लू कार्बन (Blue Carbon)- वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री पारितंत्रों के मैंग्रोव वन, समुद्री घास बेडों एवं अंतर्ज्वारीय लवण दलदलों में जमा हो जाते हैं तो वह कार्बन, ब्लू कार्बन कहलाने लगता है। ये बहुमूल्य पारितंत्र एक जटिल कार्बन भंडार को एकत्रित किये रहते हैं। वे वातावरणीय CO2 को प्राथमिक उत्पादक के द्वारा अधिग्रहीत कर फिर उन्हें अवसादों में जमा कर देते हैं।
- UNEP द्वारा वर्ष 2009 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 55% वातावरणीय कार्बन को समुद्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसका 50-71% समुद्री वनस्पति द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये समुद्री वनस्पति ही ब्लू कार्बन आवास (Blue Carbon Habitat) कहलाए, जिनमें मैंग्रोव, लवणीय दलदल (Salt Marshes), समुद्री घास (Sea Grass) एवं समुद्री खरपतवार (Sea Weeds) आते हैं, जो कि समुद्र नितल (Sea Bed) का 0.5% से भी कम आच्छादन करते हैं एवं ये विश्व के जलवायु परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। UNEP की इस रिपोर्ट के बाद IUCN, विश्व बैंक जैसे संस्थानों की भी इससे संबंधित रिपोर्ट आई। उसके बाद UNEP की पहल से ब्लू कार्बन पहल (Blue Carbon Initiative) शुरू की गई।
प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का ज़मीन या जल में इकट्ठा होना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। इससे वन्य जंतुओं या मानवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
प्लास्टिक के प्रकार (Types of Plastic)
1. सूक्ष्म प्लास्टिक अथवा माइक्रोबीड्स (Micro Plastic or Microbeads)
- 5 मिमी. या उससे कम आकार की प्लास्टिक के अंश या रेशे सूक्ष्म प्लास्टिक या माइक्रोबीड्स कहलाते हैं।
- इनका निर्माण पॉलिथीन, पॉली प्रोपीलीन, पॉलिथिलीन टेरेफ्थेलेट और नायलॉन से होता है।
- इनका प्रयोग फेशवॉश, बॉडीलोशन, टूथपेस्ट, साबुन, स्क्रब जैसे उत्पादों में होता है। ये अजैवनिम्नीकरणीय होते हैं।
- ये सीवर से बहकर सागरों एवं महासागरों में पहुँच जाते हैं जिससे समुद्री पारितंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाता है।
2. दीर्घ प्लास्टिक (Macro Plastic)
- 5 मिली. से अधिक तथा 20 मिली. से कम आकार की प्लास्टिक के अंश दीर्घ प्लास्टिक कहलाते हैं।
- दीर्घ प्लास्टिक के अंश भी समुद्री पारितंत्र के लिये अत्यधिक हानिकारक हैं।
भारत में प्लास्टिक प्रदूषण (Plastic Pollution in India)
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, “हम प्लास्टिक के बम पर बैठे हुए हैं।” ऐसा उच्चतम न्यायलय ने CPCB (Central Pollution Control Board) की रिपोर्ट के आधार पर कहा, जिसमें बताया गया है कि भारत प्रत्येक वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली अकेले 689.5 टन प्लास्टिक उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार है।
प्लास्टिक के स्रोत (Sources of Plastic)
- Chips & Confectionary Bags- 18.6%
- Bottles/Caps Lids- 11.9%
- PET Beads- 10%
- Supermarket/Retail Bags- 7.4%
- Straws- 7.0%
- Garbage Bags- 6.7%
- Packaging- 6.7%
- Food Bags- 5.2%
- Cling Wrap- 4.0%
- Fruit Juice Bottles- 3.4%
- Water/Soft Drink Bottles- 2.6%
- Cups/Utensils- 2.2%
- Food Containers- 1.7%
- Milk Bottles- 1.6%
- 6 Pack Rings- 1.4%
- Cigarette- 1.2%
प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव
प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव मानव, जलीय जीव, भूमि तथा पर्यावरण पर पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण एक विकत समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण के कारण बहुत से जानवरों की मृत्यु हो रही है तथा बहुत-सी प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो रहा है। प्लास्टिक को जलाने पर हानिकारक गैस वातावरण में फैलती हैं।
- पर्यावरण पर प्रभाव- प्लास्टिक मलबा हवा, समुद्री तरंग, व्यापर मार्ग, शहरी क्षेत्र आदि के कारण अत्यधिक बढ़ रहा है।
- भूमि पर प्रभाव- प्लास्टिक प्रदूषण भूमि पर रासायनिक एवं भौतिक दोनों कारणों से होता है। प्लास्टिक भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी करता है क्योंकि यह खनिज, जल, पोषक तत्त्वों के अवशोषण में अवरोधक का कार्य करता है।
- जल एवं वायु पर प्रभाव- प्लास्टिक के दहन से बहुत सी ज़हरीली गैसें वायुमंडल में पहुँचती हैं, जैसे- कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीन (Dioxin), हाइड्रोजन साइनाइड। प्रदूषित वायु श्वसन, तंत्रिका-तंत्र तथा इम्यून क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। पानी में प्लास्टिक युक्त कचरा डालने पर यह आसानी से मनुष्य के खाद्यजाल में पहुँच जाता है और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है।
- समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव- प्लास्टिक मलबे का प्रभाव समुद्री पारितंत्र पर भी पड़ता है। बहुत से जलीय पक्षी व जंतु प्लास्टिक के अंतर्ग्रहण से मर जाते हैं। पक्षी, कछुए, सील एवं व्हेल आदि द्वारा प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लिया जाता है जिससे यह उनके शरीर में अटक जाता है और विषैला प्रभाव डालता है।
समुद्र पृथ्वी पर विशालतम जलीय निकाय हैं। पिछले कुछ दशकों से मानवीय क्रियाओं के कारण समुद्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। मानव द्वारा समुद्र में हानिकारक पदार्थों, जैसे- प्लास्टिक, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्टों, तेल एवं रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से समुद्र प्रदूषित हुए हैं।
समुद्री प्रदूषण के कारण
- नदियों एवं वर्षा जल द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कूड़ा-करकट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं।
- समुद्र में तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों का विसर्जन एवं रेडियोएक्टिव अपशिष्टों की डंपिंग से भी समुद्री प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- विषाक्त रसायन एवं भारी धातुएँ, जो औद्योगिक अपशिष्टों के साथ आकर समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्री पारिस्थितिकी को नष्ट करती हैं।
- वहां गहरे सागर एवं सागर तल में खनन से भारी धातुओं का जमाव हो जाता है। इसके कारण उस स्थान पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है एवं सागरीय पारिस्थितिक तंत्र के लिये स्थायी एवं गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। यह अम्ल वर्षा समुद्र में हो तो समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागरीय जल का तापमान भी बढ़ रहा है जिससे सागरीय जल की जैव विविधता का ह्रास हो रहा है।
समुद्री प्रदूषण के प्रभाव
- तेल आप्लाव/तेल रिसाव (Oil Spills) सागरीय जीवों के गिल्स (Gills) एवं पंखों पर आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- तेल रिसाव के कारण सागरीय जीव प्रवाल (Coral) के छिद्र बंद हो जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रवाल भित्ति जैव विविधता से संपन्न होती है, अतः प्रवाल की मृत्यु से वहां की जैव विविधता नष्ट होने लगती है।
- समुद्री प्रदूषकों के अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रदूषकों के कारण सागरीय जल में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। जिसके परिणामस्वरूप, सागरीय जीवों की संख्या में कमी आती है।
- कुछ विशेष औद्योगिक एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक एवं उर्वरक सागरीय जल में पहुंचकर सागरीय जीवों के वसा ऊतकों में संगृहीत होकर उनकी जनन क्षमता पर नकारात्मक असर डालते हैं। इससे उनकी संख्या में तीव्रता से कमी आती है।
- ये प्रदूषक सागरीय जीवों के शरीर में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार ये खाद्य शृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इन जीवों के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- विषैली धातु, प्रदूषित जल, अपशिष्ट तथा उर्वरकों का अप्रवाह नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा देता है।
- नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवाल की तीव्र वृद्धि करती है जो कि सूर्या के प्रकाश को रोकती है जिससे उपयोगी समुद्री घास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कार्बन के प्रबंधन का एक नया तरीका कार्बन अधिग्रहण (Carbon Sequestration) है जो काफी प्रचलित एवं सक्षम साबित हो रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) या कार्बन के अन्य रूपों को ग्रहण (Capture) कर उन्हें लंबे समय तक संगृहीत (Store) करके रखना, कार्बन अधिग्रहण कहलाता है। इसे हम CCS (Carbon Capture and Storage) के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भू-अभियांत्रिकी (Geo-Engineering) द्वारा पॉवर स्टेशन, औद्योगिक स्थल एवं यहाँ तक कि सीधे हवा से पकड़कर भूमि के नीचे संगृहीत कर दिया जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को वायुमंडल में मिलने से रोका जाता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिंक में संगृहीत हो जाती है।
कोई भी चीज को कार्बन को छोड़ने से ज़्यादा उसे अवशोषित करे उसे कार्बन सिंक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है-
- प्राकृतिक सिंक (Natural Sink): समुद्र, वन, मृदा।
- कृत्रिम सिंक (Artificial Sink): विघटित तेल भंडार (Depleted Oil Reserves), अखननीय खदान।
कार्बन कैप्चरिंग का कार्य कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। तेल एवं गैस उद्योग, तेल एवं गैस की पुनर्प्राप्ति हेतु कई दशकों से कार्बन कैप्चरिंग का प्रयोग करते आ रहे हैं। आजकल इस कार्बन कैप्चरिंग का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिये किया जा रहा है, इस कारण यह चर्चा का विषय बन गया है। कार्बन अधिग्रहण में मुख्यतः 3 चरण होते हैं-
- पकड़ना एवं अलग करना (Trapping and Separating): इसमें CO2 को दूसरी गैसों से अलग करते हैं।
- परिवहन (Transportation): इसमें पकड़े गए CO2 को संग्रहण स्थल (Storage Location) तक परिवहित करते हैं।
- संग्रहण (Storage): वातावरण से दूर भूमि के नीचे या समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड को संगृहीत कर देते हैं।
पॉवर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के तीन तरीके हैं-
- ईंधन के जलने से पहले (Pre-Combustion)
- यह सबसे जटिल प्रौद्योगिकी है।
- इसमें हाइड्रोजन का उत्पादन, माध्यमिक उत्पाद के तौर पर होता है। इसमें अभी और अधिक विकास की आवश्यकता है।
- ईंधन के जलने के बाद (Post-Combustion)
- यह सबसे महंगी प्रौद्योगिकी है परंतु बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है।
- ऑक्सीफ्यूल (Oxyfuel)
- इसमें ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन में जलाया जाता है एवं परिणामस्वरूप निकली हुई सभी गैसों को जमा किया जाता है।
- यह सबसे सस्ता है।
- प्रतियोगी रूप से काफी अच्छा है एवं कोल के लिये पसंदीदा प्रौद्योगिकी है, परंतु इसमें अभी और विकास की आवश्यकता है।
मौसम में परिवर्तन एवं प्रतिकूल दशाओं (Adverse Condition) के कारण पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कुछ पक्षियों की यह प्रवृत्ति होती है कि प्रतिकूल स्थिति में वे अपना स्थान बदलकर अनुकूल स्थिति वाले क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं और स्थिति के ठीक होने पर मूल स्थान पर लौट आते हैं। ये हज़ारों किमी. दूर तक प्रवास कर जाते हैं। कुछ पक्षी ग्रीष्म ऋतु में तो कुछ शीत ऋतु में प्रवास करते हैं।
प्रवास के कारण (Reasons for Migration)
- प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण।
- भोजन तथा पानी में कमी होने पर उसकी पूर्ति के लिये आवास परिवर्तन।
- प्रजनन तथा स्वास्थ्य दशाओं के लिये।
- घोंसलों को अतिक्रमणकारी जंतुओं से बचाने के लिये।
शीत ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी
साइबेरियन क्रेन (Siberian Crane), ग्रेटर फ्लेमिंगो (Greater Flamingo), यूरेशियन टील (Eurasian Teal), पीली वागटेल (Yellow Wagtail), सफेद वागटेल (White Wagtail), उत्तरी शॉवेलर (Northern Shoveler), रोज़ी पेलिकन (Rosy Pelican), वुड सैंडपाइपर (Wood Sandpiper), चित्तीदार सैंडपाइपर (Spotted Sandpiper), यूरेशियन कबूतर (Eurasian Pigeon)।
ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी
एशियाई कोयल, यूरोपियन सुनहरी ओरियोल, कॉम्ब डक (Comb Duck), कूकूस (Cuckoos), नीली पूँछ वाली मक्खी भक्षी (Blue Tail Bee-eater)।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016) ने वर्ष 2000 में अधिसूचित किये गए म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियम का स्थान लिया है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार स्रोत पर ही सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करना होगा।
- इस नियम का प्रभाव सभी स्थानीय निकायों एवं नगरीय संकुलों (Urban Agglomerations) पर होगा।
- इसके तहत प्रदूषणकर्त्ता को संपूर्ण अपशिष्ट को तीन प्रकारों यथा- जैव निम्नीकरणीय, गैर-जैव निम्नीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत कर इन्हें स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता को ही देना होगा।
- स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित यूज़र्स शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्त्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनियमों से निर्धारित किये जाएँगे।
- इसके अतिरिक्त, इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, ज़िला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्त्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है।
- स्थानीय निकायों के भी कुछ उत्तरदायित्व जैसे- घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण, विनियमन निर्माण, यूज़र्स शुल्क निर्धारण तथा बायोमिथनेशन, माइक्रोबियल कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग जैसी तकनीकों को अपनाना निर्धारित किये गए हैं।
- हाइपरलूप विद्युत चुंबकीय शक्ति पर आधारित परिवहन तकनीक है, जिसके तहत मेट्रो की तर्ज़ पर ही बड़े-बड़े खंभों के ऊपर (एलीवेटेड) पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाती है। इस ट्यूब के भीतर पॉड में सफ़र किया जाता है। इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिये कहा गया क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के माध्यम से होगा जिसकी स्पीड 600-700 मील/घंटा या इससे अधिक होगी। ध्यातव्य है कि इस प्रणाली में प्रयुक्त ट्यूब मोड्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की परिकल्पना पर आधारित है जो लगभग घर्षण से मुक्त होता है।
- परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट एलन मस्क ने दिया। हाइपरलूप प्रणाली परिवहन के पांचवे मोड (भूमि, जल, वायु, पाइपलाइन एवं हाइपरलूप) के रूप में जानी जा रही है।
- हाल ही में रिचर्ड ब्रानसॉन के नेतृत्व वाले लंदन स्थित वर्जिन ग्रुप ने हाइपरलूप परिवहन प्रणाली के विकास के लिये महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इसका मूल उद्देश्य औद्योगिक राजधानी मुंबई और पुणे के बीच यातायात की वर्तमान 3 घंटे की अवधि को कम करना है। इस दिशा में हाइपरलूप परिवहन प्रणाली लगभग 20 मिनट में यह दूरी तय कर लेगी।
लाभ (Advantages)
- हाइपरलूप प्रणाली समय और धन की बचत के लिये अति उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही, उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी।
- इस प्रणाली में पॉड की आवृत्ति बढ़ाने से अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा कराई जा सकती है, जो लगभग वर्ष में 150 मिलियन यात्रियों की संख्या हो सकती है।
- इस प्रणाली का जहाँ प्रबंधन करना सरल है, वहीं यह यातायात प्रणाली यातायात जाम से भी निजात दिलाने में सहायक होगी।
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभिन्न समुद्री जीवों की खोज तथा उनका उपयोग कर मानव उपयोगी उत्पादों को विकसित करना शामिल है। दूसरे शब्दों में, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के तहत वे सभी प्रयास शामिल हैं, जिनमें जैविक समुद्री संसाधनों को जैव प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में मानव लाभ के लिये उपयोग किया जाता है।
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विविधता ने वैज्ञानिकों को समुद्री जीवों के विकास और उनसे जुड़े महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सुविधा प्रदान की है। चूँकि समुद्री जीव समुद्र के भीतर, प्रकाश की अनुपस्थिति, अधिक तापमान और दबाव में विकसित होते हैं, इसलिये वैज्ञानिकों ने इनकी मदद से विशिष्ट प्रकार की दवाओं और एंजाइमों को तैयार करने में सफलता हासिल की है।
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पर बढ़ते शोध ने बहुत-सी दवाओं के विकास को संभव बनाया है। कैरिबियाई समुद्री जीवों की मदद से बनाई गई एंटी-वायरल दवाएं, जैसे- Zovirax (Generic Name- Acyclovir), आदि पहले ही काफी सफल साबित हो चुकी हैं।
समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के कुछ अनुप्रयोग
- समुद्री जीवों (समुद्री शैवालों, अकशेरुकियों अर्थात् बिना रीढ़ वाले जीव) आदि ने बहुत-सी नई दवाओं के विकास को संभव बनाया है। इससे कैंसर के इलाज में भी कुछ सफलता मिली है।
- मछलियों और अन्य समुद्री जीवों से मिलने वाले एंजाइम खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले परंपरागत एंजाइमों से ज्यादा प्रभावी और फायदेमंद होते हैं। मछलियों से मिलने वाले Collagens और Gelatin प्रोटीन अपेक्षाकृत कम तापमान पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं।
- समुद्र में पाए जाने वाले अतिसूक्ष्म शैवालों से ऐसे बायोपॉलिमर्स का निर्माण संभव है, जो तेल निष्कर्षण की प्रक्रिया में मदद करते हैं।
- हिंद महासागर में पाया जाने वाला Dolastatin ब्रेस्ट कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में बहुत उपयोगी साबित हुआ है।
मैंग्रोव वनों के भौगोलिक वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक वहां का तापमान है। विषुवत रेखा के आस-पास के क्षेत्रों में जहाँ जलवायु गर्म और नम होती है, वहां मैंग्रोव वनस्पतियों की लगभग सभी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति विश्व के लगभग 123 देशों में पाई जाती है, जिनमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। विश्व का लगभग 40% मैंग्रोव कवर दक्षिण-पूर्व एशिया व दक्षिण एशिया में मौजूद है। विश्व में पाए जाने वाले 4 मुख्य प्रकार के मैंग्रोव पौधों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-
- लाल मैंग्रोव (Red Mangroves)- लाल मैंग्रोव की श्रेणी में वे पौधे आते हैं जो बहुत अधिक खारे पानी को सहन करने की क्षमता रखते हैं तथा समुद्र के नज़दीक उगते हैं। इनमें भी अन्य मैंग्रोव पौधों की तरह विशेष रूपांतरित जड़ें होती हैं जो तने के निचले भाग से निकलकर धरती तक पहुँचती हैं और पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं। इसलिये इन्हें स्थिर जड़ें कहते हैं। ये जड़ें पौधे को ऐसे स्थान पर उगने की क्षमता प्रदान करती हैं जहाँ भूमि में ऑक्सीजन कम होती है। इन्हीं जड़ों से पौधे वातावरण से हवा का आदान-प्रदान व भूमि से पोषक तत्त्वों को प्राप्त करते हैं।
- काले मैंग्रोव (Black Mangroves)- काले मैंग्रोव वनस्पति (कच्छ वनस्पति) की श्रेणी में वे पौधे आते हैं जिनकी खारे पानी को सहने की क्षमता अधिक होती है। इन पौधों में विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें पाई जाती हैं जो दलदल में उगने वाले पौधों में देखी जाती हैं। इन जड़ों में गैसों के आदान-प्रदान के लिये विशेष प्रकार की संरचनाएँ होती हैं जिन्हें वातरंध्र (लैंटिकल्स) कहते हैं। इनमें हवा का प्रवेश वायवमूलों (न्यूमेटोफोर्स) से होता है।
- सफेद मैंग्रोव (White Mangroves)- सफेद मैंग्रोव का नाम इनकी चिकनी सफेद छाल के कारण पड़ा है। इन पौधों को इनकी जड़ों तथा पत्तियों की विशेष प्रकार की बनावट के कारण अलग से पहचाना जाता है।
- बटनवुड मैंग्रोव (Buttonwood Mangroves)- ये झाड़ी के आकार के पौधे होते हैं तथा इनका यह नाम इनके लाल-भूरे रंग के तिकोने फलों के कारण है। यह सफेद मैंग्रोव के परिवार के ही अंग हैं एवं कुछ वैज्ञानिक इसे वास्तविक मैंग्रोव नहीं मानते।
कुछ तत्त्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है, यही प्रक्रिया रेडियोसक्रियता (Radioactivity) कहलाती है। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम जैसे कुछ तत्त्व हैं, जो इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये किरणें जैविक कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती हैं।
रेडियोएक्टिव प्रदूषण के स्रोत (Sources of Radioactive Pollution)
मुख्यतः इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं-
- प्राकृतिक- सोलर, कॉस्मिक एवं पार्थिव
- मानव निर्मित- नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय हथियार एवं यूरेनियम खनन
रेडियोएक्टिव प्रदूषण के प्रभाव (Effects of Radioactive Pollution)
विकिरण अन्य प्रदूषकों की अपेक्षा जीवों पर अधिक खतरनाक प्रभाव डालते हैं क्योंकि इनके प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलते रहते हैं।
- कायिक प्रभाव (Somatic Effect) : विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुँचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। उच्च तीव्रता के विकिरणी प्रभाव में आने से एनीमिया, रक्तस्राव आदि के कारण प्राणियों की मृत्यु भी हो जाती है।
- आनुवंशिक प्रभाव (Genetic Effect) : विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। उद्योग, अनुसंधान एवं औषधि में रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड का प्रयोग करने वाले लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते हैं। ड्रोसेफिला पर किया गया अध्ययन दर्शाता है कि विकिरणों के प्रभाव से उत्परिवर्तन दर (Mutation Rate) उच्च हो जाती है। उच्चवर्गीय प्राणी (जैसे-मानव) निम्नवर्गीय प्राणियों (जैसे-कीट) की अपेक्षा इन विकिरणों से अधिक प्रभावित होते हैं।
- विकिरण के कारण जंतुओं के बाल उड़ना, खाल में जलन, गाँठ पड़ना, त्वचा का रंग उड़ना आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। ज़्यादा विकिरण कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है तथा मृत्यु का कारण बन सकता है। विकिरण के कारण जंतुओं में उत्परिवर्तन होता है।
- विकिरण का प्रभाव जलीय पारितंत्र, मृदा आदि पर पड़ता है इसके बहुत से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
रेडियोएक्टिव प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (Measures to Control Radioactive Pollution)
- परमाणु बम के भूमिगत, वायुमंडल अथवा जलमंडल में परीक्षण पर रोक लगाई जाए।
- मानव उपयोग वाले यंत्रों को रेडियोधर्मिता से मुक्त करना होगा।
- नाभिकीय तत्त्वों के परिवहन में सावधानी।
- परमाणु अस्त्रों पर रोक एवं निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया।
- चिकित्सीय व अनुसंधान सामान (रेडियोएक्टिव युक्त) का वैज्ञानिक तरीके से निपटान।
- भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।
- भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, तो वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है।
- इन आपात उपबंधों को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक-राजनैतिक व्यवस्था को यथावत् सुरक्षित बनाए रखना है।
- आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसमें आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिये गए हैं, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिये गए हैं।
- भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बांटा गया है-
- राष्ट्रीय आपात – अनुच्छेद 352
- राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन – अनुच्छेद 356
- वित्तीय आपात – अनुच्छेद 360
राष्ट्रीय आपात (National Emergency)
- राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा
- अनुच्छेद 352 में निहित है कि ‘युद्ध’, ‘बाह्य आक्रमण’ या ‘सशस्त्र विद्रोह’ के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है।
- मूल संविधान में ‘सशस्त्र विद्रोह’ की जगह ‘आंतरिक अशांति’ शब्द का उल्लेख था।
- 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ को हटाकर उस स्थान पर ‘सशस्त्र विद्रोह’ को रखा गया है।
- उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि
- अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता, जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दे। यह प्रावधान 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया।
- ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होगा।
- राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा एक महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर प्रवर्तन में नहीं रहता, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर छः माह के लिये प्रवर्तन में बना रह सकता है।
- प्रभाव
- केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव
- कार्यपालिका पर प्रभाव
- विधानमंडल पर प्रभाव
- वित्त पर प्रभाव
- लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव
- जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वतः प्रभावी हो जाते हैं।
- अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 द्वारा दिये गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकार के निलंबन (अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) से संबंधित है।
- उद्घोषणा की समाप्ति
- राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है।
- संसद द्वारा अनुमोदन न किये जाने पर।
- लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है।
प्राकृतिक धरोहर स्थल वे स्थल होते हैं जहाँ जैव विविधता की समृद्धि के साथ वैश्विक महत्त्व के जीव-जंतु, स्थान क्षेत्र, वनस्पति आदि पाए जाते हैं।
प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किये जाने के लिये UNESCO ने विभिन्न मापदंड तय किये हैं-
- पृथ्वी के विशिष्ट जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की उपस्थिति हो एवं आवास क्षेत्रों में दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जंतु तथा पादप प्रजातियों की उपस्थिति हो।
- जहाँ पर पारिस्थितिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के कारण जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों का उद्भव हो रहा हो।
- पृथ्वी के विकास क्रम में महत्त्वपूर्ण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थलाकृति अथवा भू-आकृतिक परिवर्तन हुए हों।
- वे क्षेत्र जहाँ पर अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएँ (Phenomena) हों और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से क्षेत्र अत्यधिक महत्त्व रखते हों।
UNESCO के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में रखा गया है-
- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park)
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladev National Park)
- मानस वन्यजीव अभयारण्य (Manas Wildlife Sanctuary)
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (Sundarban National Park)
- नंदादेवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Nanda Devi and Valley of Flowers National Park)
- पश्चिमी घाट (Western Ghat)
- महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र (Great Himalayan National Park Conservation Area)
एक जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन कोश कहते हैं। वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। ये वे स्थान हैं जहाँ पर फसलों की महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ और स्थानिक जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कृषि पादप प्रजातियों एवं उष्णकटिबंधीय पौधों के जीन या आनुवंशिक पदार्थों को एकत्रित किया जाता है।
जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग है। आनुवंशिक पदार्थों का एकत्रीकरण कर जीन पूल केंद्रों में रखा जाता है, जो भविष्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जीन पूल केंद्र के अंतर्गत विश्व के महत्त्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
विश्व के प्रमुख जीन पूल केंद्र इस प्रकार हैं-
- दक्षिण एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो-चाइना एवं द्वीपीय क्षेत्र जो मलाया द्वीप को शमिल करता है।
- दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र, कॉकेशियन (Caucasian) मध्य-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम भारतीय क्षेत्र
- पूर्वी एशिया, चाइना एवं जापान क्षेत्र
- भूमध्यसागरीय क्षेत्र
- यूरोप क्षेत्र
- दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र
भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के अधिवेशन (रामसर अधिवेशन) के अंतर्गत रक्षित जलकुक्कुट आवास हैं।
हमारे देश में आर्द्रभूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार हैं-
- दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण-पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्रभूमि।
- राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे पानी वाली भूमि।
- गुजरात-राजस्थान से पूर्व (केवलादेव) और मध्य प्रदेश की ताज़े पानी वाली झीलें व जलाशय।
- भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि व लैगून (चिल्का झील आदि)।
- गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र।
- ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर-पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपद के कच्छ एवं मैंग्रोव क्षेत्र।
- कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र।
मैंग्रोव वन लवण, ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़-पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े-तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। ये वन चक्रवातों से तटीय क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
भारत में मैंग्रोव वन 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा तथा गुजरात में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण करना आवश्यक हो गया है।
- मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनदमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्चजल (Backwater), लैगून एवं पंक जमावों में विकसित होते हैं। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द ‘मैग्यू’ तथा अंग्रेज़ी शब्द ‘ग्रोव’ से मिलकर हुई है। ऐसा समझा जाता है कि मैंग्रोव वनों का सर्वप्रथम उद्गम भारत के मलय क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक मैंग्रोव प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- यह धारणा कि मैंग्रोव केवल खारे पानी में उग सकते हैं, सही नहीं है। ये ताज़े पानी वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं लेकिन तब इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है। किसी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की संख्या तथा उनके घनत्व को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता तथा तापमान है।
मैंग्रोव की विशेषताएँ (Features of Mangroves)
- मैंग्रोव प्रजातियाँ बहुत अधिक सहनशील होती हैं और प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती हैं।
- सभी मैंग्रोव पौधे अपनी जड़ों से पानी का अवशोषण करते समय नमक की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं, साथ ही ये पौधे दूसरे पौधों की अपेक्षा नमक की अधिक मात्रा अपने ऊतकों में सहन कर सकते हैं। कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर पाई जाने वाली विशेष कोशिका से अतिरिक्त नमक को बाहर कर देते हैं।
- मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि पर उगते हैं। इनकी विलक्षण जड़ें इन्हें न केवल स्थायित्व प्रदान करती हैं बल्कि धाराओं के तेज़ बहाव और तूफानों में भी मज़बूती से खड़ा रखती हैं और श्वसन में सहायता करती हैं। मैंग्रोव पौधों में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है जिनके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करते हैं। इन जड़ों को ‘न्यूमेटोफोर्स’ कहते हैं।
- इन पौधों में पाई जाने वाली वायवीय जड़ें कई रूप ले सकती हैं। एक तीन मीटर लंबे एवीसीनिया वृक्ष पर लगभग 10,000 श्वसन जड़ें पाई जा सकती हैं।
- बहुत-सी प्रजातियों के नव अंकुरित पौधों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और पानी पर तैरने के लिये विशेष संरचनाएँ पाई जाती हैं जो उन्हें जीवित रखने में सहायक होती हैं।
- जरायुजता (विविपैरी)- मैंग्रोव की कुछ प्रजातियाँ जैसे एवीसीनिया एल्बा (Avicennia Alba) क्रिप्टोविविपैरी (गूढ़जरायुजता) दर्शाता है। क्रिप्टोविविपैरी प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूण विकास की प्रक्रिया पेड़ से फलों से गिरने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है।
- वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के उत्सर्जन को रोकने के लिये इन पौधों में मोटी चिकनी पत्तियां होती हैं।
- मैंग्रोव पौधों में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं और सतह के ऊपर आ जाती हैं।
- जिन स्थानों पर मैंग्रोव उगते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिये मैंग्रोव पौधों में अतिरिक्त जड़ें पाई जाती हैं जो अनुकूलन जड़ें कहलाती हैं।
- मैंग्रोव के बारे में यह सामान्य धारणा है कि ये समुद्री तटों के काले बदबूदार कीचड़ में उगने वाले पौधे हैं। यह धारणा सही नहीं है क्योंकि मैंग्रोव रेतीली भूमि में तथा चट्टानी सतहों पर भी उग सकते हैं।
- यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भारत में कार्यरत एक संवाद समिति है।
- यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के समाचार ब्यूरो भारत के लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में तथा प्रमुख शहरों में विद्यमान हैं।
- U.N.I. का गठन कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत दिसंबर 1959 में हुआ। 21 मार्च, 1961 को इसने विधिवत् काम शुरू किया।
- 1 मई, 1982 को U.N.I. ने हिंदी सेवा ‘यूनीवार्त्ता’ की शुरुआत की तथा दस वर्ष पश्चात् 5 जून, 1992 को U.N.I. उर्दूसेवा तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई।
- U.N.I. की फोटो सेवा में प्रतिदिन लगभग 200 तस्वीरें वितरित की जाती हैं, जिनमें 60 अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें E.P.A., यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी तथा रॉयटर्स से ली जाती हैं। इसकी ग्राफिक्स सेवा प्रतिदिन 5 या 6 ग्राफिक्स वितरित करती है।
- U.N.I. ने ही सर्वप्रथम विश्व में उर्दू समाचारों की आपूर्ति की थी।
- इसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ है।
- U.N.I. संवाददाता वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, मास्को, दुबई, इस्लामाबाद, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, सिंगापुर, टोरंटो, सिडनी, बैंकाक और काबुल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
- U.N.I. ने ख़बरों के आदान-प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों से समझौते कर रखे हैं, जिनमें- चीन की शिन्हुआ, रूस की रिया नोवोस्ती, बांग्लादेश की यू.एन.बी., तुर्की की अनादोलू, संयुक्त अरब अमीरात की वाम, बहरीन की जी.एन.ए. और कुवैत की कुना इत्यादि शामिल हैं।
- वर्ष 1919 में एक छोटे से सेल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में PIB के आठ क्षेत्रीय कार्यालय (चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, कोलकाता और भोपाल) तथा 34 शाखा कार्यालय स्थित हैं।
- पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संप्रेषित करने वाली एक नोडल एजेंसी है।
- पत्र सूचना कार्यालय विभिन्न संचार माध्यमों, जैसे- प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस विवरण, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, PIB की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस, ऑडियो-वीडियो क्लिपिंग्स आदि के ज़रिये सूचनाओं का प्रसार करता है।
- लगभग 8,400 अख़बारों और मीडिया संगठनों के ज़रिये अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना प्रकाशित की जाती है।
- PIB के अधिकारी न सिर्फ अपने संबद्ध मंत्रालयों को लगातार अपनी सेवाएँ देते हैं बल्कि मीडिया के माध्यम से उन मंत्रालयों के कामकाज का प्रचार भी करते हैं।
- PIB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मुखिया प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) हैं, जिनके साथ एक उपमहानिदेशक और आठ अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं।
- एक्स और यूट्यूब पर अपनी सेवा देने के पश्चात् पत्र सूचना कार्यालय ने नए प्लेटफार्म, जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाइन पर अपनी सुविधा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया।
- इस सेवा की मुख्य वेबसाइट हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू, तीनों भाषाओं में उपलब्ध है।
- पत्रकार कल्याणकारी योजना (Journalist Welfare Scheme)- पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ‘पत्रकार कल्याणकारी योजना’ लागू की गई है। इस संशोधित योजना में कहा गया है कि पत्रकार तथा उसके परिवार को जरूरत पड़ने पर एक समय के लिये अनुग्रहपूर्वक राहत देने के प्रावधान के साथ पांच लाख रुपये की धनराशि भी प्रदान की जाएगी। परिवार को राहत बहुत कठिनाई या आफत, जैसे- पत्रकार की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता जैसी स्थिति में ही दी जाएगी। खतरनाक बीमारी, जैसे- कैंसर, ब्रेन हेमरेज इत्यादि तथा दुर्घटना की स्थिति में भी राहत प्रदान की जा सकती है।
- 27 अगस्त, 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) को रजिस्टर्ड किया गया तथा 1 फरवरी, 1949 को इसने कार्य करना शुरू किया। यह भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह अपने इनसेट उपग्रह पर एक ट्रांसपोंडर के ज़रिये समाचार सीधे ग्राहक तक पहुँचाती है और इंटरनेट के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़ी है।
- यह भारत की गैर-मुनाफे वाली सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, जो देश के अख़बारों द्वारा चलाई जाती है। पीटीआई अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी समाचार सेवा भी देती है, जिसे ‘भाषा’ नाम दिया गया है।
- वर्तमान में ज़्यादा-से-ज़्यादा ग्राहक सैटेलाइट के ज़रिये पीटीआई की सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं। देश के कोने-कोने में पीटीआई के लगभग 400 पत्रकार और लगभग 500 स्टिंगर्स प्रत्येक ज़िले एवं छोटे शहर में मौजूद हैं, जो अलग-अलग श्रेणियों में 2000 से ज़्यादा ख़बरें और 200 से ज़्यादा फोटोग्राफ प्रतिदिन प्रदान करते हैं। वर्तमान में भारत में समाचार एजेंसी बाज़ार के 90% हिस्से पर पीटीआई का कब्ज़ा है।
- यह समाचार एजेंसी एशिया के समाचार को पहला स्थान देती है। यह संस्था रॉयटर्स (Reuters), यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल (UPI) और आजांस फ्रांस प्रेस (AFP) के साथ समाचारों का लेन-देन करती है। टेली प्रिंटर सर्विस के अलावा यह एजेंसी कंप्यूटर संगणक की सहायता से भी समाचार देती है।
- पीटीआई ने भारत में समाचार सेवा प्रदान करने के लिये 100 से अधिक देशी एवं विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ करार किया है। एशियाई देशों में आर्थिक विकास और व्यापारिक अवसरों के बारे में ऑनलाइन डाटा बैंक के लिये, सूचनाएँ एकत्र करने के लिये पीटीआई और पांच अन्य एशियाई मीडिया संगठनों ने सिंगापुर में ‘एशिया पल्स इंटरनेशनल’ नाम की कंपनी स्थापित की है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 12 समाचार एजेंसियों ने एक सहकारी व्यवस्था बनाई है, जिसका नाम ‘एशियानेट’ है। पीटीआई एक संस्था में सहभागी अंग है।
|
नाम |
विशेषता |
|
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (मुंबई) |
जैव विविधता पर पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत में सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन, प्रतीक-ग्रेट हार्नबिल। |
|
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (कोलकाता) |
वन्य पादप संसाधनों का वर्गीकरण एवं पुष्प अध्ययन। |
|
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (कोलकाता) |
प्राणिजात संसाधनों का अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रलेखीकरण। |
|
सलीम अली ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (कोयंबटूर) |
पक्षी शोध संस्थान। |
|
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया |
वैश्विक जैविक विविधता संरक्षण। |
|
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून |
वन्यजीव अनुसंधान व प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण व अकादमिक कोर्स। |
|
भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून |
वन संसाधनों का मूल्यांकन करना। |
|
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (बल्लभगढ़) |
पशु कल्याण हेतु भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार। |
|
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (चेन्नई) |
जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु। |
|
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (नई दिल्ली) |
वन्यजीवों (विशेषत: चिड़ियाघरों में) का संरक्षण करना। |
|
भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा |
संकटापन्न प्रजातियों का प्राकृतिक आवास में संरक्षण। |
|
राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड (नई दिल्ली) |
देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी-विकास को बढ़ावा देना। |
|
टेरी (The Energy and Resources Institute) (नई दिल्ली) |
पर्यावरण व ऊर्जा संरक्षण, धारणीय विकास को बढ़ावा देना। |
|
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) |
यह गैर-वन प्रयोग के लिये वन भूमि की हुई क्षति-पूर्ति हेतु पौधरोपण कार्यक्रम है। |
|
सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (CSE) |
1980 में स्थापित भारत का अग्रणी पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसके संस्थापक पर्यावरणविद् अनिल कुमार अग्रवाल थे। यह पर्यावरण पत्रिका ‘डाउन-टू-अर्थ’ का प्रकाशन करता है। |
मानव समाज के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण है। पाषाण काल से ही प्रौद्योगिकी आम जनता को आवश्यक न्यूनतम वस्तुओं को सुलभ कराती रही है, किंतु वर्तमान में प्रौद्योगिकी अधिक खतरनाक व विनाशकारी हो गई है क्योंकि तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ मानव प्रजाति भौतिकवादी प्रवृत्ति तथा उच्च उत्पादन पर अधिक ज़ोर दे रही है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे निजी जीवन से लेकर कृषि, विज्ञान, परिवहन, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में तकनीक का व्यापक उपयोग हो रहा है। निश्चित तौर पर तकनीक ने मानव जीवन को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। किंतु यह भी सत्य है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अधिकांश पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया है।
निम्नलिखित तथ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभिशाप को स्पष्ट करते हैं-
- मनुष्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने हित के लिये मौसम संबंधी दशाओं में परिवर्तन करने में सक्षम हो गया है। मनुष्य आज मेघ बीजन द्वारा वर्षा कराने तथा ओला-वृष्टि (Hailstorm) को रोकने में सक्षम हो गया है। इस तरह मनुष्य वायुमंडलीय प्रक्रमों में परिवर्तन करने लगा है और इन परिवर्तनों से जीवमंडल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य नदियों पर बांध तथा जलाशय बनाने में सक्षम हो गया है। इन क्रियाओं के गंभीर दुष्परिणाम पर्यावरण पर पड़ते हैं, जैसे- बड़े बांधों तथा जलाशयों के भार के कारण चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाता है जिस कारण विनाशकारी भूकंप का आविर्भाव होता है। डेनेवर, मीड झील, करीबा झील तथा कोयना झील मानव द्वारा विकसित एवं प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जनित भूकंपों के कतिपय उदाहरण हैं। इसके अलावा बड़े-बड़े जल भंडारों के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं इस कारण प्रभावित क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाता है। भारत में सरदार सरोवर परियोजना का विरोध इन्हीं आधारों पर हो रहा है।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि के साथ पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से आज मृदा व जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है।
- सिंचाई के साधन, जैसे- पंप, बोरवेल आदि से सिंचाई से कुछ राज्यों यथा- पंजाब व हरियाणा में (अति सिंचाई के कारण संलग्न क्षेत्रों) मृदा लवणता की समस्या देखी जा रही है।
- विलासिता के उत्पादों यथा- रेफ्रीजरेटर, एयरकंडीशनर, स्प्रे, हेयर ड्रायर आदि के संचालन से क्लोरो फ्लोरो कार्बन (CFC) के वायुमंडल में पहुँचने से ओज़ोन क्षरण हो रहा है। जिस कारण सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों के धरातल पर पहुँचने से तापमान में वृद्धि के साथ त्वचा कैंसर की संभावनाएँ बढ़ती जा रही हैं।
- परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास तथा ऊर्जा की पूर्ति के लिये जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग तथा इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) से वायुमंडल के सांद्रण में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्म़िग की समस्या उत्पन्न हो रही है। रासायनिक संयंत्रों से ज़हरीली गैसों के निकलने से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि यह मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। भोपाल गैस त्रासदी, यूक्रेन की चेर्नोबिल तथा थ्री-माइल आइलैंड घटना आधुनिक प्रौद्योगिकी की असफलता से उत्पन्न गंभीर परिणाम हैं।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी के खतरनाक परिणामों में ज़हरीले रसायनों का उत्पादन, कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन तथा जीवों द्वारा विघटित न होने वाले पदार्थों का भारी मात्रा में उत्पादन (जैसे- प्लास्टिक) आदि प्रमुख हैं।
- आज नाभिकीय अपशिष्टों का प्रबंधन मानव समाज के लिये गंभीर खतरा है।
वास्तव में आधुनिक प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन के खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। इसलिये आधुनिक तकनीक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिये कि वह मानव जीवन को खुशहाल व उत्तम बनाने में प्रभावी हो सके।
- अध्येता का सामान्य अर्थ होता है- ‘अध्ययन करने वाला’।
- अध्येता को ‘अधिगमकर्त्ता’, ‘शिक्षार्थी’ या ‘विद्यार्थी’ भी कहते हैं।
- शिक्षण के केंद्रबिंदु में अध्येता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
- अध्येता शिक्षा ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही वह सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों को आत्मसात करता है तो वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है।
- विद्यालयी वातावरण अध्येता के मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव हमें सभी शिक्षक व साथी सहपाठियों के साथ अध्येता के मिलनसार व्यवहार में दिखाई देता है। विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो उसे जीवनपर्यंत बेहतर नागरिक बनने के लिये प्रेरित करता है।
अध्येता की विशेषताएँ (Characteristics of Learner)
एक अध्येता के सद्गुणों व विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख निम्नलिखित अवयवों/बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-
- मूल प्रवृत्तियाँ : प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी-मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं, इन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं।
- संवेग एवं स्थायी भाव : प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुख-दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। इन अनुभवों से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे मानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन भावों को मनोवैज्ञानिक भाषा में ‘संवेग’ कहते हैं। स्थायी भाव एक अर्जित संस्कार है। अर्जित संस्कार धीरे-धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप धारण कर लेते हैं, फलस्वरूप आचरण व व्यवहार नियंत्रित होने लगते हैं।
- अभिवृद्धि एवं विकास : किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को ‘अभिवृद्धि’ कहते हैं और किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है, उसे ‘विकास’ कहते हैं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण : बालक को अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों और पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएँ और गुण प्राप्त होते हैं, उन्हें ‘वंशानुक्रम’ के नाम से जाना जाता है। किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण अथवा घेरे को ही ‘वातावरण’ कहते हैं।
- खेल एवं खेल प्रणाली : अध्येता के विकास में खेलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है।
‘प्रौद्योगिकी विज़न 2035’ का लक्ष्य सुरक्षा, समृद्धि में बढ़ोत्तरी और प्रत्येक भारतीय की अस्मिता को सुनिश्चित करना है। इसका उल्लेख संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के संबंध में दस्तावेज में ‘हमारी आकांक्षा’ या ‘विज़न वक्तव्य’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विज़न दस्तावेज में 12 विशेषाधिकारों (छः वैयक्तिक और छः सामूहिक) का उल्लेख भी किया गया है जो सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होंगे। ये इस प्रकार हैं-
वैयक्तिक विशेषाधिकार
- स्वच्छ वायु और पेयजल
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा और सार्वजनिक स्वच्छता
- 24 x 7 बिजली
- बेहतर आवास
- बेहतर शिक्षा, आजीविका और सर्जनात्मक अवसर
सामूहिक विशेषाधिकार
- सुरक्षित और तेज़ आवागमन
- सार्वजानिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा
- सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता
- पारदर्शी और प्रभावशाली शासन
- आपदा और जलवायु लोच
- प्राकृतिक संसाधनों का पारिस्थितिकीय अनुकूल संरक्षण
विज़न दस्तावेज के अनुसार ये विशेषाधिकार भारत के प्रौद्योगिकी विज़न के केंद्र में हैं। इन विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकियों का निर्धारण किया गया है-
- जिन्हें तेज़ी से तैनात किया जा सके;
- जिन्हें प्रयोगशाला से व्यवहार में लाया जा सके;
- जिनके लिये लक्ष्य अनुसंधान आवश्यक है, और
- जो कि अभी भी कल्पना में हैं।
प्रौद्योगिकियों के इन अंतिम वर्गों के संबंध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बायो प्रिंटिंग और रिजनरेटिव मेडिसिन जैसे उत्कृष्ट ‘ब्लू स्काई’ अनुसंधान उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा सटीक कृषि और रोबोट आधारित खेती, वर्टिकल खेती, इंटरेक्टिव फूड, ऑटोनोमस व्हीकल, बायोलूमिनेसंस, इमारतों की 3D प्रिंटिंग, भूकंप की भविष्यवाणी, मौसम प्रौद्योगिकियाँ, हरित खनन आदि ऐसी अन्य प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनसे मानव की वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी।
- शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है जिसके तीन घटक (शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम) होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते (Teach) हैं, प्रशिक्षित (Trained) करते हैं या उन्हें अनुदेश (Instruct) देते हैं। ये सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों की संज्ञानात्मक संरचना (किसी के मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना) में बदलाव लाने के लिये निष्पादित होती हैं। हालाँकि पढ़ाना, प्रशिक्षण और अनुदेशन अपने अर्थ में काफी भिन्न हैं।
- प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिये तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसे पूरा करने में कई साल लगते हैं। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित करता है जो इसे नहीं जानते हैं।
- अनुदेशन को अक्सर शिक्षण के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसका संबंध शिक्षा की बजाय कौशल के विकास से ज़्यादा होता है।
- प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत, शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति-विशेष के सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने में मदद करता है।
- शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की एक प्रक्रिया है। हालाँकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में भिन्न होते हैं, लेकिन इन सभी के माध्यम से एक केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों में अधिगम संपन्न होता है।
- शिक्षण प्रक्रिया सार्थक तभी होगी जब शिक्षक इस आशय से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो कि विद्यार्थी इसके परिणामस्वरूप कुछ सीखेंगे।
- शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के उद्देश्य से संलग्न करता है, जैसे किसी गद्यांश को पढ़ना, विद्यार्थियों के लिये रचना लिखना आदि।
हाल के वर्षों में शोधार्थियों को बेहतर अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सृजन हुआ है, जिनमें ‘शोधगंगा’, ‘शोधगंगोत्री’ व ‘ई-शोधसिंधु’ के नाम उल्लेखनीय हैं।
शोधगंगा
- ‘शोधगंगा’ एक डिजिटल रिपॉज़िटरी प्लेटफॉर्म है, जो भारत में शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
- यह UGC के एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र ‘सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र’ (INFLIBNET) की एक पहल है। यह पूर्णत: निशुल्क प्लेटफार्म है।
- इस प्लेट्फॉर्म पर शोधार्थी अपने शोध-प्रबंध अन्य शोधार्थियों के साथ साझा करते हैं जिससे वे उनके शोध निष्कर्षों और अध्ययन-प्रक्रिया को देख सकें।
- शोधगंगा एक महत्त्वपूर्ण अकादमिक संसाधन है जो ज्ञान की साझेदारी तथा शोध सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है।
शोधगंगोत्री
- ‘शोधगंगोत्री’ भारत में एक ऑनलाइन मंच और एक राष्ट्रीय रिपॉजिटरी है, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्तर पर चल रहे और हाल ही में पूरे हुए शोध कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये डिजाइन किया गया है।
- यह विभिन्न शैक्षणिक विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान सिनोप्सिस के डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। यह भी ‘INFLIBNET’ की एक पहल है और पूर्णत: निशुल्क प्लेटफार्म है।
- उल्लेखनीय है कि यह प्लेटफार्म ‘शोधगंगा’ से भी कनेक्टेड है। एक बार शोध पूर्ण होने के बाद शोध प्रबंध का लिंक ‘शोधगंगोत्री’ से ‘शोधगंगा’ पर शेयर कर दिया जाता है।
ई-शोधसिंधु
- ‘ई-शोधसिंधु’ की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर की गई थी। यह प्लेटफॉर्म अपने सदस्य संस्थानों को 10,000 से अधिक पीयर-रिव्यूड जर्नल्स, ग्रंथ सूचियों, उद्धरणों व तथ्यात्मक डाटाबेस तक पहुँच उपलब्ध कराता है।
- यह भारत के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों को ई-संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है।
- जब स्वतंत्र भारत में परमाणु ऊर्जा के संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुसंधान कार्य आरंभ करवाया, तब डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ‘परमाणु ऊर्जा आयोग’ (Atomic Energy Commission) के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रारंभ में परमाणु शक्ति के संबंध में ‘शांति के लिये परमाणु’ (Atoms for Peace) सिद्धांत को अपनाया गया अर्थात् केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति के विकास का लक्ष्य रखा गया।
- बांग्लादेश के संकट (वर्ष 1971) के पश्चात् जब यह स्पष्ट होने लगा कि चीन अपने मित्र पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के निर्माण में सहायता कर सकता है, तब भारत को गंभीरता से अपने परमाणु कार्यक्रम पर विचार करना पड़ा। इससे पूर्व ही वर्ष 1964 में चीन अपना प्रथम परमाणु विस्फोट करके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था।
- चीन और अमेरिका के मध्य बढ़ते राजनीतिक संबंधों को देखते हुए भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा : पोखरण-I) किया, परंतु विश्व समुदाय द्वारा इस विषय पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह उसका शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (Peaceful Nuclear Explosion- PNE) था।
- वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) पर हस्ताक्षर करने से भारत सदा इनकार करता रहा है। वास्तव में भारत इस संधि को भेदभाव पर आधारित मानता है क्योंकि इसमें केवल पांच देशों (ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन) को ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र (Nuclear Weapon States) स्वीकार किया गया है।
- वर्ष 1991-96 के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव गंभीरता से विचार करते रहे कि परमाणु परीक्षण किया जाए, परंतु उन्होंने परीक्षण के आदेश नहीं दिये।
- मई 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहसिक कदम उठाकर परमाणु परीक्षण (पोखरण-II) करवाए। परमाणु परीक्षण अत्यंत गोपनीय रूप से किये गए। फलस्वरूप भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र (Nuclear Weapon States) घोषित कर दिया।
- भारत ने न तो ‘परमाणु अप्रसार संधि’ (NPT) पर हस्ताक्षर किये हैं और न ही ‘व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि’ (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty- CTBT) को स्वीकृति दी है।
- भारत ने अपनी परमाणु नीति के तहत मुख्य रूप से तीन तत्त्वों को प्राथमिकता दी है- पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सुदृढ़ता; जो एक लोकतांत्रिक संप्रभु देश की भावना को प्रकट करता है।
भारत की परमाणु नीति के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं-
- विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण एवं रखरखाव।
- परमाणु हथियारों से रहित किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना तथा परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों पर भी पहले आक्रमण नहीं करना।
- परमाणु आक्रमण होने पर जवाबी कार्यवाही इतनी सशक्त होगी कि दुश्मन की प्रतिक्रिया करने की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी।
- जवाबी परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार ‘परमाणु कमान प्राधिकरण’ (Nuclear Command Authority) के माध्यम से केवल राजनीतिक शक्ति होगा।
- भारत विश्व स्तर पर बिना भेदभाव वाले परमाणु नि:शस्त्रीकरण के द्वारा विश्व को परमाण्विक हथियारों से मुक्त कराने के अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहेगा।
- भारतीय सेना पर जैविक या परमाण्विक हथियारों से भारत पर या किसी स्थान पर हमले से नाभिकीय हथियारों के प्रयोग का विकल्प खुला रहेगा।
- भारत अपनी परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर सख्त नियंत्रण बनाए रखेगा।
प्रत्येक वर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना, रोग की जटिलताओं को समझाना और समय पर उपचार की आवश्यकता को उजागर करना है। वर्ष 2025 में यह दिवस 6 मई को मनाया गया। इस वर्ष की थीम “श्वसन उपचार को सभी के लिये सुलभ बनाना” अस्थमा रोगियों के लिये इनहेलर और अन्य श्वसन दवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती है, जिससे रोग प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में राहत सुनिश्चित हो सके।
- अस्थमा: एक दीर्घकालिक श्वसन रोग
अस्थमा एक क्रॉनिक श्वसन विकार है, जिसमें श्वसन नलिकाएँ संकुचित और सूजनग्रस्त हो जाती हैं, जिससे बलगम का निर्माण बढ़ जाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति की श्वशन-प्रणाली पर पड़ता है, जिससे सामान्य रूप से साँस लेना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- मुख्य लक्षण:
- बार-बार होने वाली खाँसी, विशेषकर रात या सुबह के समय
- घरघराहट की आवाज़ (सीटी जैसी साँस)
- साँस फूलना और थकावट
- सीने में जकड़न या दबाव का अनुभव
राष्ट्रीय हृदय, फेफड़े और रक्त संस्थान (NHLBI) के अनुसार, ये लक्षण समय-समय पर उभरते हैं और बिना उपचार के गंभीर रूप ले सकते हैं।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्वभर में 250 मिलियन से अधिक लोग अस्थमा से ग्रस्त हैं।
- वर्ष 2019 में, अस्थमा से लगभग 4,55,000 लोगों की मृत्यु हुई।
- यह आँकड़ा अस्थमा के समुचित प्रबंधन, दवाओं की उपलब्धता और समय पर उपचार की अनिवार्यता को दर्शाता है।
अस्थमा को यदि समय पर नियंत्रित किया जाए, तो इससे जुड़ी जटिलताओं और मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- इतिहास एवं महत्व
- विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 में Global Initiative for Asthma (GINA) द्वारा की गई थी।
- पहला आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था, जिसमें 35 देशों ने भाग लिया।
- तब से यह दिवस एक वैश्विक अभियान का रूप ले चुका है, जो अस्थमा रोग के विषय पर शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।
अस्थमा केवल एक रोग नहीं, बल्कि एक सतत चुनौती है, जिसे जागरूकता, समय पर उपचार और सही देखभाल से नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व अस्थमा दिवस हमें इस दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने की प्रेरणा देता है।
‘रिवाइव अवर ओशन’ एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसे डायनेमिक प्लैनेट नामक गैर-सरकारी संगठन ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) का निर्माण करना और इन क्षेत्रों के माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- प्रमुख विशेषताएँ :
- यह पहल कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचे के 30x30 लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक महासागरों के 30% हिस्से को संरक्षित करना है।
- प्रारंभिक चरण में यह पहल सात देशों – यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्किये, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मैक्सिको – पर केंद्रित है।
- इसमें समुदायों को MPA की स्थापना और प्रबंधन के लिये सक्षम बनाया जाएगा।
- पहल MPA को आर्थिक परिसंपत्तियों के रूप में देखती है। उदाहरण के लिये, मेडिस द्वीप (स्पेन) में मत्स्य निषेध क्षेत्र से पर्यटन के ज़रिए हर वर्ष लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होती है।
- यह पहल 2023 की हाई सीज़ संधि से भी मेल खाती है, जिसे प्रभावी बनाने के लिये 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। भारत इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- MPA की परिभाषा :
समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) ऐसे समुद्री क्षेत्र होते हैं जहाँ पारिस्थितिकीय तंत्र, आवास या प्रजातियों की सुरक्षा हेतु कुछ मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। हालाँकि कुछ बहुउद्देशीय MPA में सीमित मत्स्यन और अनुसंधान की अनुमति दी जा सकती है। - स्थिति और चुनौतियाँ:
- प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, विश्व में 16000 से अधिक MPA मौजूद हैं, जो केवल 8% महासागरों को कवर करते हैं।
- इनमें से केवल 3% क्षेत्र पूर्णतः संरक्षित हैं।
- कई MPAs में कमज़ोर प्रबंधन और विनाशकारी गतिविधियाँ जैसे बॉटम ट्रॉलिंग अब भी जारी हैं, जिससे संरक्षण के उद्देश्य को क्षति पहुँचती है।
पूरी शिक्षण प्रक्रिया आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चरों द्वारा संपादित होती है। आश्रित चर और स्वतंत्र चर के विपरीत, मध्यस्थ चर निष्क्रिय एवं निर्जीव होते हुए भी शिक्षण अधिगम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सक्रिय चर के रूप में आश्रित चर और स्वतंत्र चर के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-
- निदानात्मक कार्य
- शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये कई तरह के निदानात्मक कार्यों का भी संपादन करना पड़ता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के संदर्भ में शिक्षक को शिक्षण वातावरण में परिवर्तन करने होते हैं जिससे विद्यार्थियों का कुशल समायोजन हो सके।
- शिक्षक को शिक्षण अधिगम में प्रयोग किये जा रहे शिक्षण साधनों (पाठ्यवस्तु, अनुदेशन सामग्री, विधि और तकनीक आदि) के साथ-साथ अपनी शिक्षण योग्यताओं एवं शक्तियों का भी निदान करना होता है जिससे शिक्षण अधिगम में अधिकतम लक्ष्यों को पाया जा सके।
- निदानात्मक कार्यों के संदर्भ में विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित होता है। विद्यार्थियों को अपनी कमियाँ, अच्छाई, अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करते हुए शिक्षण प्रकिया में एक सक्रिय भागीदार बनना होता है।
- उपचारात्मक कार्य
- शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिये शिक्षण अधिगम में आ रही बाधाओं की जाँच यानी निदानात्मक क्रिया के उपरांत शिक्षक को उन बाधाओं को दूर करना होता है। ऐसा करने के लिये शिक्षक उपचारात्मक कार्य करते हुए सभी मध्यस्थ चरों को उचित रूप से नियंत्रित करने का प्रयास करता है जिससे शिक्षण अधिगम सुचारु रूप से चलता रहे।
- शिक्षण अधिगम में अपनाए गए उपचारात्मक कार्यों को क्रियात्मक रूप में लाने के लिये विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्हें एक भागीदार के रूप में शिक्षक का सहयोग करना होता है।
- मूल्यांकन कार्य
- शिक्षण अधिगम में शिक्षक द्वारा संपादित निदानात्मक कार्यों एवं उपचारात्मक कार्यों की सफलता की जाँच के लिये मूल्यांकन तकनीक का सहारा लिया जाता है। मूल्यांकन में निदानात्मक कार्यों एवं उपचारात्मक कार्यों के गुण एवं दोष, सफलता और असफलता आदि की जाँच करते हुए पुन: यदि आवश्यक हो तो वांछित संशोधन किये जाते हैं जिससे शिक्षण अधिगम में वांछित सफलता मिल सके।
- मूल्यांकन विधि में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली आदि समेत प्रक्षेपी तकनीकों (Projective techniques) का सहारा लिया जाता है। मूल्यांकन विधियों में शिक्षक एवं विद्यार्थी को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होती है।
- जल निकायों का संरक्षण (Conservation of Water Bodies)- भारत की अधिकतर नदियाँ तथा झीलें प्रदूषण की शिकार हैं तथा इनका जल पीने योग्य नहीं रह गया है। यहाँ की नदियों एवं तालाबों के जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत असंसाधित मल-जल प्रवाह है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय’ का कार्य केंद्र प्रायोजित स्कीमों ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)’ एवं ‘जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना’ (NPCA) के तहत नदियों, झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan–GAP)- देश की प्रमुख नदियों में से एक तथा स्वयं का निर्मलीकरण (गंगा में पाए जाने वाले वायरस जैसे Bacteriophage वगैरह जीवाणुओं को खा जाते हैं।) करने वाली गंगा आज लगभग अपने अपवाह के आधे भाग में प्रदूषित हो गई है। वर्तमान में लगभग 50,000 से अधिक आबादी वाले 100 से अधिक शहरों का असंसाधित मल-अपशिष्ट गंगा में अपवाहित किया जाता है तथा हज़ारों की संख्या में लाशों व जले हुए अवशेषों को इसमें प्रवाहित किया जाता है। गंगा बेसिन में भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ‘केंद्रीय गंगा प्राधिकरण’ (CGA) का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान (GAP) की शुरुआत की गई।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan)- 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण (CGA) का नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण’ (NRCA) कर दिया गया था। गंगा कार्य योजना का विलय NRCP के साथ कर दिया गया।
- नमामि गंगे कार्यक्रम (Namami Gange Project)- केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिये 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को खत्म करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य स्तंभ हैं-
- सीवरेज ट्रीटमेंट
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
- वनीकरण
- जैव विविधता का विकास
- जन-जागरूकता
- गंगा ग्राम योजना
- नदी सतह की सफाई
- औद्योगिक प्रवाह निगरानी
- ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टोकरेंसियों का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल ‘सार्वजनिक बही-खाता’ (Public Ledger) है। ब्लॉकचेन तकनीक में तीन अलग-अलग तकनीकों का समायोजन होता है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल की (निजी कुंजी) की क्रिप्टोग्राफी अर्थात् जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है।
- ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन-देन को दर्ज करने पर इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- ब्लॉकचेन के कारण लेन-देन के लिये एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे- बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े उपकरणों (मुख्यतः कंप्यूटर की शृंखलाओं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है।) के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन-देन के विवरण को बही-खाते में रिकॉर्ड किया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि 2008 में बिटकॉइन का आविष्कार होने के बाद इस क्रिप्टोकरेंसी को समर्थन देने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक की खोज की गई।
- इस तकनीक में सभी ब्लॉक एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी ब्लॉक में बदलाव के लिये अरबों गणनाएँ करने की ज़रूरत होती है, इसलिये एक बार आंकड़े दर्ज हो जाने के बाद इसमें बदलाव करना असंभव होता है, क्योंकि किसी भी एक ब्लॉक में मामूली बदलाव करते ही दूसरे सभी ब्लॉक परस्पर जुड़े होने के कारण बदलाव से असहमति जता देते हैं।
- अतः साइबर क्राइम और हैकिंग को रोकने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक को फुलप्रूफ सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक लागू करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है।
- एक सर्वे के अनुसार, विश्व के 70% से अधिक बैंक अपनी व्यवस्था में ब्लॉकचेन के अनुप्रयोग की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। ध्यातव्य है कि यह तकनीक केवल क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है-
- सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन
- सरकारी योजनाओं का लेखा-जोखा
- सब्सिडी वितरण
- भू-रिकॉर्ड विनियमन
- बैंकिंग और बीमा
- डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण
- स्वास्थ्य आंकड़े
- क्लाउड स्टोरेज
- ई-गवर्नेंस
- शैक्षणिक जानकारी
- ई-वोटिंग आदि।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने अप्रत्याशित फोन कॉल्स तथा मैसेजेज़ को रोकने के लिये ‘टेलिकॉम कमर्शियल कम्यूनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेग्यूलेशन, 2018’ जारी किया है। ट्राई ने इस मसौदे में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को वरीयता दी है।
- मानव सभ्यता के विकास में सूचना तकनीक को चौथी क्रांति माना जा रहा है, जिसका मूल आधार है- डिजिटल तकनीक। इस तकनीक में आंकड़ों को बाइनरी (0, 1) रूप में परिवर्तित कर सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली इसी तकनीक के आधार पर कार्य कर रही है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं-
- आंकड़ों, चित्रों व संदेशों की उच्च गुणवत्ता।
- सूचनाओं की संप्रेषण क्षमता एवं तीव्रता।
- त्रुटियों की संभावना एवं बाह्य हस्तक्षेप का नगण्य होना।
- डिजिटल तकनीक के द्वारा ग्लोबल विलेज (Global Village) की संकल्पना सार्थक होती दिख रही है क्योंकि किसी भी स्थान से किसी अन्य दूरस्थ स्थान को उपग्रहों के माध्यम से जोड़कर त्वरित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत जैसा विकासशील देश इस तकनीक के कारण विकास भी कर रहा है, किंतु इसी क्रम में एक तकनीकी समस्या ने भी जन्म लिया, जिसे ‘डिजिटल डिवाइड’ का नाम दिया गया है।
- यह एक ऐसी समस्या है जिसमें डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर रहे देशों के अंदर तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इसके उपयोग के आधार पर बड़ा आर्थिक अंतर उत्पन्न होता जा रहा है, जो सामाजिक समस्या को भी बढ़ा रहा है। इस प्रकार डिजिटल डिवाइड वह संकल्पना है जो डिजिटल तकनीक के उपयोग के आधार पर बढ़ रही आर्थिक-सामाजिक विषमता को व्याख्यायित करती है। इस समस्या के निवारण हेतु ‘डिजिटल कंवर्जेंस’ की अवधारणा अपनाई जा रही है। भारत सरकार ने इसके लिये दोहरी कार्यवाही को अपनाया है-
अवसंरचनात्मक विकास-
- इसके तहत वैसे क्षेत्रों में भी डिजिटल तकनीक से युक्त संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अभी तक पिछड़े हुए हैं। गुवाहाटी और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर पार्क व IIIT की स्थापना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- देश के पिछड़े क्षेत्रों को VSAT के माध्यम से बड़े सूचना केंद्रों से जोड़ा जा रहा है।
- देश के विभिन्न भागों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण के लिये नए शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
अनुप्रयोगात्मक प्रयास-
- ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे डिजिटल ज्ञान को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिये विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है।
- INSAT-3A द्वारा टेलीमेडिसिन तथा GSAT-3 द्वारा टेली एजुकेशन का प्रावधान कर सुदूर क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- गाँव व शहर के बीच आर्थिक विषमता को कम करने के लिये ‘GRAMSAT’ नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, जिसका उद्देश्य गाँवों के समुचित विकास को प्राप्त करना है। गाँवों में ज़मीन से जुड़े आंकड़ों की जानकारी के लिये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा नेटवर्किंग को विकसित किया जा रहा है, जिसमें SWAN (State Wide Area Network) उल्लेखनीय है।
- वाई-फाई कॉलिंग एक नई तकनीक है जिसके माध्यम से हम बिना करियर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क के किसी से बातचीत कर सकते हैं।
- इसके लिये किसी करियर नेटवर्क की बजाय हमें वाई-फाई कनेक्शन की ही आवश्यकता होती है।
- अभी तक वाई-फाई का प्रयोग तार-रहित इंटरनेट कनेक्शन, डेटा ट्रांसफर, जैसे- SHAREit, Xender आदि के लिये किया जाता था लेकिन अब इसका प्रयोग कॉल करने के लिये भी किया जा रहा है।
- वर्तमान में कुछ मोबाइल ऐप, जैसे- What’s App, Messenger, Skype आदि भी इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा से लैस हैं।
- उक्त सभी मोबाइल ऐप कॉलिंग के लिये पूरी तरह वाई-फाई या डेटा कनेक्शन का प्रयोग करते हैं जिसे Voice Over Internet Protocol- VoIP कहा जाता है।
कार्यप्रणाली
- VoIP की सहायता से कॉलिंग के लिये यूजर को इन एप्लीकेशंस (What’s App, Messenger, Skype आदि) को मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है।
- इसके विपरीत, वाई-फाई कॉलिंग हेतु कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- वाई-फाई कॉलिंग के लिये यूजर इसे डिफ़ॉल्ट मोड में लगा सकता है। इससे मोबाइल में नेटवर्क न होने की स्थिति में यह स्वयं ही वाई-फाई कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने में सक्षम होगा।
- वाई-फाई कॉलिंग के लिये यूजर को अलग से संपर्क सूची (Contact List) नहीं बनानी होगी बल्कि यह फोन की मौजूदा संपर्क सूची को एक्सेस कर लेगा।
- इसके तहत बिना इंटरनेट कनेक्शन और बगैर किसी अन्य ऐप के कॉल भी प्राप्त की जा सकेगी।
- वाई-फाई कॉलिंग हेतु मोबाइल फोन में ‘Wi-Fi Calling’ तथा ‘HD Voice’ की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिये।
महत्त्व
- जब करियर नेटवर्क कमज़ोर हो या उसके प्रयोग से बातचीत करना संभव न हो तब वाई-फाई कॉलिंग की आवश्यकता होती है। उदाहरण- बड़े मकानों के बीच, किसी भूमिगत स्थान में या दूरदराज़ के क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थितियों में वाई-फाई कॉलिंग सहायक साबित हो सकती है।
- वाई-फाई कॉलिंग में किसी करियर नेटवर्क का प्रयोग नहीं होता। अतः इसमें टॉकटाइम या बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- करियर नेटवर्क- करियर या वाहक नेटवर्क एक पंजीकृत नेटवर्क अवसंरचना है जिसका कार्य दूर-संचार सेवाएँ प्रदान करना है। जैसे- Airtel, Vodafone, Jio, BSNL आदि।
अपने वास्तविक रूप में इतिहास अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय, क्रमबद्ध एवं समन्वित विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अध्ययन का मुख्य ध्येय अतीत के बारे में जानना है।
ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय या समाज विशेष के विगत जीवन तथा किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों और नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का अनुसंधान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के उचित नियोजन में भी सहायता करता है।
ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत जिन तथ्यों या सत्यों का अन्वेषण होता है, वे अतीत से जुड़े होने के कारण अमूर्त एवं चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के सारांशों अथवा निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है।
जॉन डब्ल्यू. बेस्ट- ‘‘ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं। जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है।’’
ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्त्व (Importance of Historical Research)
- ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है।
- यह अनुसंधान परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, जैसे- सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, नगरीकरण से संबंधित समस्याओं की प्रकृति से विशेष रूप से परिवर्तन की प्रकृति को समझा जा सकता है।
- अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है।
- इस अनुसंधान का महत्त्व शुद्ध अनुसंधान (Pure Research) और व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research) दोनों ही दृष्टिकोण से है।
- शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिये वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
- अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है।
- अतीत की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करके उसके गुण-दोषों से परिचित कराता है।
- सामाजिक जीवन में इस अनुसंधान की व्यावहारिक उपयोगिता भी है।
ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य (Objectives of Historical Research)
- ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिये सतर्क होना है।
- अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना है।
- अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाक्रमों का अध्ययन कर भविष्य में इनकी सार्थकता को ज्ञात करना है।
- वर्तमान में जो सिद्धांत तथा क्रियाएँ व्यवहार में हैं, उनका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ, इस तथ्य का विश्लेषण करना।
- शिक्षा मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में चिंतन को नई दिशा एवं नवीन ज्ञान के नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना।
सम्मेलन एक औपचारिक बैठक को संदर्भित करता है, जहाँ प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर सूचनाओं एवं विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इसके द्वारा सदस्य या प्रतिभागी अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार करते हैं।
यह एक प्रकार के बड़े समूह की सभा होती है, जहाँ सदस्य आपस में विचारों का आदान-प्रदान एवं अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं। प्रतिभागियों (Participants) के समूह द्वारा सम्मेलन के उद्देश्य व कार्यप्रणाली को समूह के वरिष्ठ व्यक्ति या नेता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। सम्मेलन उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के लिये एक महत्त्वपूर्ण विधि है। शोधकर्त्ता (अनुसंधानकर्त्ता) इसके द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक (ज्ञानात्मक) एवं भावनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। सम्मेलन के द्वारा विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है।
सम्मेलन के प्रकार (Type of Conferences)
सम्मेलन के तीन प्रकार होते हैं-
- क्षेत्रीय सम्मेलन (Regional Conference)- क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में सम्मेलन का आयोजन।
- राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference)- राष्ट्र संबंधी विषयों, जैसे- धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि पर सम्मेलन का आयोजन।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference)- UNESCO या UNO द्वारा किसी मानवीय समस्या पर सम्मेलन।
सम्मेलन के लाभ (Advantage of Conference)
- स्वतंत्र अध्ययन अभिवृत्तियों का विकास होता है।
- विशेषज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद का अवसर प्राप्त होता है।
- कार्य करने के नए तरीकों व कौशल का विकास होता है।
- समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने व बातचीत करने का अवसर मिलता है।
- संयम, धैर्य, कार्य कुशलता तथा सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है।
- अनुसंधान संबंधी समस्याओं के प्रत्येक पक्ष का स्पष्ट निरूपण होता है।
- सहयोगात्मक भावना द्वारा समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होता है।
सम्मेलन की प्रक्रिया (Process of Conference)
सम्मेलन की कार्यवाही को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है-
- प्रारंभ- सम्मेलन का अध्यक्ष सम्मेलन के विषय, समस्या तथा उद्देश्य आदि के बारे में बताता है तथा सम्मेलन की पृठभूमि को भी स्पष्ट करता है।
- विचार विमर्श- मुख्य प्रश्न पूरे समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब समूह के सदस्य उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो परिचर्चा की कार्यवाही शुरू हो जाती है तथा कोई भी सदस्य इसमें प्रतिभाग करके अपने तर्क-वितर्क प्रस्तुत कर सकता है।
- समापन- सम्मेलन के समापन पर अध्यक्ष मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्तीकरण कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है तथा विशेष सुझाव भी देता है।
अनुसंधान (शोध) एक क्रमबद्ध एवं दीर्घ अवधि की प्रक्रिया है, जो विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। अनुसंधान या शोध कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिये, जल्दबाज़ी या शॉर्टकट के द्वारा किया गया शोध कार्य त्रुटियुक्त होता है। कोई भी शोध कार्य पूर्ण होने पर भविष्य हेतु उपयोगी होता है। अनुसंधानकर्त्ता को अनुसंधान में किसी समस्या के समाधान तथा समस्या के संदर्भ में कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य करना चाहिये।
- समस्या के समाधान में मुख्य बातें- गहन अध्ययन + स्वविवेक + बौद्धिक कौशल।
- समस्या के संदर्भ में मुख्य बातें- तथ्यों की गहन व व्यापक खोज करनी चाहिये।
अनुसंधान नैतिकता, अनुसंधान के ज़िम्मेदार आचरण के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है। जब हम नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो हम सही एवं गलत के बीच भेद करने वाले नियमों के बारे में सोचते हैं।
अनुसंधान नैतिकता का विषय अनुसंधान के प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में संगत माना गया है, जैसे- शोध रिपोर्ट्स को रिपोर्ट करना शोध नैतिकता का विषय हो सकता है। अनुसंधान नैतिकता का बहुधा प्रत्यक्ष संबंध समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करने से होता है। अनुसंधान नैतिक तभी होगा जब उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञानता सुनिश्चित होगी। शोध नैतिकता को बेहतर करने हेतु शोधार्थी को ही शोध समस्या सौंपनी चाहिये।
अनुसंधान के नैतिक मूल्य अथवा सिद्धांत (The Ethical Values or Theories of Research)
- अनुसंधान में ईमानदारीपूर्वक आँकड़ों, परिणाम तथा विधियों के साथ प्रकाशन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें।
- अनुसंधान में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह व भ्रांत धारणा से बचना चाहिये।
- शोध नैतिकता में व्यक्तिपरकता को शामिल नहीं करना चाहिये।
- अनुसंधान प्रक्रिया में गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना चाहिये।
- पेटेंट, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकारों का सम्मान करें। अनुमति के बिना प्रकाशित डाटा, विधियों व परिणामों का उपयोग न करें।
- अनुसंधान ‘सर्वजन हिताय’ होता है।
- साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित होता है।
- यह एक स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया है।
- अनुसंधान विश्वसनीय प्रक्रिया है। यह ज्ञान वृद्धि में सहायक है।
- अनुसंधान मानव गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान करता है।
- अनुसंधान एक कलात्मक और सृजनशील प्रक्रिया है।
- अनुसंधान मानवीयता के गुणों से परिपूर्ण होता है।
- अनुसंधान कार्य भविष्य के लिये उपयोगी होता है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विभिन्न विषयों में आधुनिक अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शोधकर्त्ताओं को दक्षता, सहयोग प्रदान करने के साथ डाटा विश्लेषण सरल बनाने और शोध निष्कर्षों के प्रसार को बढ़ाने में सहायता करती है। शोध में ICT के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-
- डाटा संग्रहण और प्रबंधन- ICT ऑनलाइन सर्वेक्षण, सेंसर, मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से बड़ी मात्रा में डाटा एकत्र करने की सुविधा प्रदान करती है। डाटाबेस सिस्टम और डाटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर अनुसंधान डाटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने, संगृहीत करने और पुनर्प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
- डाटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन- उन्नत सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम शोधकर्त्ताओं को जटिल डाटा सेट का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने और सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायता करते हैं। विजुअलाइज़ेशन उपकरण ग्राफ, चार्ट और इंटरैक्टिव विजुअल्स के निर्माण को सक्षम करते हैं, जो शोध निष्कर्षों की व्याख्या और संचार को बढ़ाते हैं।
- सहयोग और संचार- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, प्रोजेक्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म और सहयोगी दस्तावेज संपादन जैसे ICT उपकरण शोधकर्त्ताओं को विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम बनाते हैं। आभासी सहयोग स्थल टीम के सदस्यों के बीच रीयल टाइम संचार और समन्वय को बढ़ाते हैं।
- साहित्य समीक्षा और सूचना पुनर्प्राप्ति- ऑनलाइन डाटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरी और अकादमिक सर्च इंजन शोध लेखों, पुस्तकों और कागजात की एक विशाल शृंखला तक त्वरित पहुँच प्रदान करते हैं तथा साहित्य समीक्षा व पृष्ठभूमि अनुसंधान में सहायता करते हैं। संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर मानकीकृत प्रारूप में संदर्भों को व्यवस्थित और उद्धृत करने में मदद करता है।
- सिमुलेशन और मॉडलिंग- ICT शोधकर्त्ताओं को वास्तविक दुनिया की घटनाओं को दोहराने के लिये जटिल सिमुलेशन और मॉडल बनाने की अनुमति देती है, जिससे परिकल्पना परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण की सुविधा मिलती है। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर परिणामों की भविष्यवाणी करने और सिस्टम व्यवहार को समझने में मदद करता है।
- रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)- ICT उपग्रह इमेजरी और जीपीएस डाटा जैसी रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भौगोलिक डाटा के विश्लेषण का समर्थन करती है। GIS सॉफ्टवेयर शोधकर्त्ताओं को स्थानिक संबंधों एवं पैटर्न का विश्लेषण व परिकल्पना करने में मदद करता है।
- संग्रहण एवं संरक्षण- डिजिटल रिपॉज़िटरी और संग्रह प्रणालियाँ डाटासेट, लेख और रिपोर्ट सहित अनुसंधान आउटपुट के दीर्घकालिक संरक्षण और पहुँच को सुनिश्चित करती हैं।
- ई-लर्निंग और कौशल विकास- ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार और डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म शोधकर्त्ताओं के लिये नए कौशल हासिल करना, प्रगति के साथ अपडेट रहना और अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाना संभव बनाते हैं।
- स्वचालित प्रयोग और रोबोटिक्स- स्वचालन प्रौद्योगिकियाँ और रोबोटिक्स विशेष रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रयोगों को कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से संचालित करने में सहायता कर सकते हैं।
- सोशल मीडिया और सार्वजनिक जुड़ाव- शोधकर्त्ता अपने शोध को साझा करने, जनता के साथ जुड़ने, व्यापक दर्शक वर्ग तक निष्कर्षों का प्रसार करने, ज्ञान के प्रसार और शोध की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं।
- बिग डाटा और मशीन लर्निंग- बिग डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बड़े और जटिल डाटा सेट से मूल्यवान अंतर्दृष्टि निष्कर्षित करने में मदद करते हैं, जिससे शोधकर्त्ताओं को डाटा- संचालित निर्णय और भविष्यवाणियाँ करने में मदद मिलती है।
ताप प्रदूषण तब होता है जब किसी जल निकाय अथवा वायुमंडल की वायु का तापमान बढ़ या घट जाता है। वायु के तापमान की अपेक्षा जल का तापमान सामान्यत: अधिक स्थिर होता है, अत: तापमान में तीव्र और एकाएक परिवर्तन के प्रति जलीय जीवों में अनुकूलन नहीं पाया जाता। तापमान में मात्र 1°C की कमी या वृद्धि जलीय जीवों के लिये घातक हो जाती है।
ताप प्रदूषण के प्रमुख स्रोत (Major Sources of Thermal Pollution)
- ताप प्रदूषण तब होता है जब अपशिष्ट ऊष्मा को जल निकाय के भीतर छोड़ दिया जाता है। वनाग्नि व ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएँ भी ताप प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार हैं। ताप प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत हैं-
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र
- कोयला दहन बिजली संयंत्र
- औद्योगिक कचरा व अपवाह
- तटीय इलाकों में वनोन्मूलन
- मृदा अपरदन
- ताप प्रदूषण के मानवीय कारणों में वनोन्मूलन, वाष्प जेनरेटरों से गर्म जल को बाहर छोड़ा जाना, साथ ही धातु प्रगालक, संसाधन मिलें, पेट्रोलियम शोध कारखाने, पेपर मिलें, रसायन संयंत्रों आदि के शीतलन हेतु जल का प्रयोग किया जाना है।
ताप प्रदूषण के प्रभाव (Effect of Thermal Pollution)
प्रत्येक प्रजाति एक अनुकूलतम तापमान परास में ही जीवित रह सकती है। कुछ जीवों, जैसे कि कुछ मछलियों के लिये यह तापमान परास बहुत कम होता है। उदाहरणत: झीलों की मछलियाँ उस स्थान से दूर हट जाती हैं जहाँ का तापमान सामान्य से 1.5ºC भी अधिक हो जाता है लेकिन नदियों की मछलियाँ 3ºC की तापमान वृद्धि सहन कर सकती हैं। तापमान परिवर्तन से जलीय निकाय के भीतर अन्य जीव स्वरूपों के लिये भी दशाएँ बदल जाती हैं जिनके कारण इन जल निकायों के समस्त बायोम में परिवर्तन आ जाता है। ताप प्रदूषण सुपोषण क्रिया (Eutrophication) को बढ़ावा देता है।
ताप प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (Measures to Control Thermal Pollution)
- नाभिकीय संयंत्रों पर नियंत्रण
- पौधारोपण करना (तटीय क्षेत्रों में)
- मृदा अपरदन को रोकना (इससे जल को पर्याप्त सौर प्रकाश व ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी।)
- कूलिंग टावर (ये वेस्ट ऊर्जा को वायुमंडल में वाष्प के माध्यम से छोड़ते हैं।)
- सह-उत्पादन (Co-generation)- इस प्रक्रिया में औद्योगिक जल अपवाह को ठंडा करके घरेलू उपयोग में लाया जाता है।
- कूलिंग तालाब
- कृत्रिम झील का निर्माण
- विश्व में लगभग 3 अरब लोग खाना बनाने एवं घरों को गर्म रखने में ठोस ईंधन (लकड़ी, चारकोल, कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का प्रयोग करते हैं। इन अवैज्ञानिक और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार घरेलू प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 3.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू वायु प्रदूषण परंपरागत ईंधन, जैसे- जलावन लकड़ी, चारकोल, गोबर आदि द्वारा खाना बनाने के कारण फैलता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रदूषण वायुरुद्ध घरों, वातायन (Ventilation) की कमी, घरों में रासायनिक उत्पादों एवं सिंथेटिक उत्पादों के प्रयोग के कारण फैलता है। ग्रामीण घरों में धूम्र निकासी रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा एवं मिट्टी तेल वाले हीटर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हैं।
- घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं-
- वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ- परफ्यूम, स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, एयर फ्रेशनर जैसे पदार्थ घरेलू प्रदूषण के स्रोत हैं। इनके प्रभाव से आँखों, नाक, त्वचा में जलन, सिरदर्द, मितली आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से ये पदार्थ शरीर में जमा होकर यकृत एवं शरीर के अन्य अंगों को बीमार करते हैं।
- तंबाकू- इसके धुएँ से व्यापक हानिकारक रसायन एवं कैंसरकारक रसायनों की उत्पत्ति होती है। इसके प्रभाव से आँखों, नाक, गले में जलन, कैंसर, अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं।
- जैविक प्रदूषण- इनमें पौधों के परागकण, कीट, परजीवी, कवक एवं जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है। इनके कारण एलर्जी एवं संक्रमणजन्य रोग उत्पन्न होते हैं।
- रेडॉन- यह मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस है। शहरी घरों में कमजोर वातायन (Ventilation) के कारण यह घरों में सांद्रित (Concentrated) होकर फेफड़े के कैंसर का कारण बनती है।
- फॉर्मएल्डिहाइड- यह कार्पेट, तापरोधक फोम आदि से उत्पन्न होता है। यह आँखों एवं नाक में जलन एवं एलर्जी उत्पन्न करता है।
ड्रग्स को उनके स्रोत और उत्पादन विधि के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : प्राकृतिक (नेचुरल), अर्ध-सिंथेटिक (सेमी-सिंथेटिक), और सिंथेटिक ड्रग्स।
1. प्राकृतिक ड्रग्स (Natural Drugs) :
ये सीधे प्राकृतिक स्रोतों, मुख्यतः पौधों, से प्राप्त होते हैं।
उदाहरण :
- अफीम पोस्ता (Papaver somniferum) : इससे मॉर्फिन और कोडीन जैसे अल्कलॉइड प्राप्त होते हैं।
- कैनबिस (Cannabis sativa) : मारिजुआना और हशीश का स्रोत।
- कोका (Erythroxylum coca) : कोकीन का प्राकृतिक स्रोत।
2. अर्ध-सिंथेटिक ड्रग्स (Semi-Synthetic Drugs) :
ये प्राकृतिक ड्रग्स को रासायनिक रूप से संशोधित करके बनाए जाते हैं ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके या दुष्प्रभाव कम किये जा सकें।
उदाहरण :
- हेरोइन : मॉर्फिन का अर्ध-सिंथेटिक व्युत्पन्न।
- ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन : कोडीन से संशोधित दर्द निवारक का निर्माण।
- कोकीन : कोका पत्तियों से प्राप्त, लेकिन प्रसंस्करण के माध्यम से शुद्ध किया जाता है।
3. सिंथेटिक ड्रग्स (Synthetic Drugs) :
ये पूर्णतः प्रयोगशाला में रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं, जिनका प्राकृतिक समकक्ष नहीं होता।
उदाहरण :
- एम्फेटामाइन्स : केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाले।
- फेंटानिल : मॉर्फिन से कई गुना अधिक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड।
- मेथाक्वालोन : शांतिदायक और नींद लाने वाला एजेंट।
यह वर्गीकरण ड्रग्स की उत्पत्ति और उत्पादन विधि के आधार पर उसके विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो उनके उपयोग, प्रभाव, और कानूनी स्थिति को समझने में सहायक होता है।
कर्नाटक के हासन, चिकमंगलूर और कोडागु जिलों में बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, वन अधिकारियों ने एक अभिनव "सॉफ्ट रिलीज़" स्ट्रैटजी का प्रस्ताव रखा है। इस रणनीति का उद्देश्य पकड़े गए हाथियों को धीरे-धीरे भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (BWS) में पुनर्वासित करना है ताकि उनके पर्यावरणीय अनुकूलन में आसानी हो और संघर्ष की संभावना कम हो जाए।
- मुख्य बिंदु :
- रणनीति का उद्देश्य :
- मानव-हाथी संघर्ष को कम करना।
- हाथियों के पुनर्वास के दौरान उनके स्वास्थ्य और अनुकूलन पर विशेष ध्यान देना।
- सॉफ्ट रिलीज़ प्रक्रिया :
- हाथियों को BWS के चार निर्दिष्ट स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा।
- रिलीज़ से पहले, उन्हें 20 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में रखा जाएगा जहाँ उनकी स्वास्थ्य जाँच और अनुकूलन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- स्वास्थ्य और अनुकूलन :
- नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं पर्यावरणीय अनुकूलन के माध्यम से हाथियों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।
- इस चरण के दौरान हाथियों को आवश्यक खाद्य, पानी एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
- पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ :
- धीरे-धीरे रिलीज़ करने से हाथियों में तनाव कम होगा और वे अपने प्राकृतिक आवास के प्रति सहज होंगे।
- मानव समुदाय एवं वन विभाग के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे संघर्ष के मामले में तेजी से समाधान संभव होगा।
- निगरानी एवं मूल्यांकन :
- हाथियों के व्यवहार, स्वास्थ्य एवं आवास में अनुकूलन की नियमित निगरानी की जाएगी।
- वन अधिकारियों एवं जैविक विशेषज्ञों द्वारा जारी फीडबैक के आधार पर रणनीति में आवश्यक सुधार किये जाएँगे।
- संरक्षण के व्यापक उद्देश्य :
- यह स्ट्रैटजी व्यापक वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण प्रयासों का एक हिस्सा है।
- उद्देश्य न केवल हाथियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है, बल्कि क्षेत्रीय जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा भी है।
सॉफ्ट रिलीज़ स्ट्रैटजी एक मानवतावादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाई गई पहल है, जो हाथियों के पुनर्वास के साथ-साथ मानव-हाथी संघर्ष को भी न्यूनतम करने में सहायक सिद्ध होगी। यह रणनीति हाथियों के स्वास्थ्य, अनुकूलन एवं दीर्घकालिक संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिये भी स्थायी समाधान प्रदान करती है।
- रणनीति का उद्देश्य :
सर्वोत्तम वैश्विक और भारतीय कृषि विधियाँ
प्राकृतिक कृषि एक संधारणीय कृषि पद्धति है जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करती है तथा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करके जैव विविधता को बढ़ावा देती है। दुनिया भर में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियाँ पारंपरिक ज्ञान, पारिस्थितिक संतुलन और संसाधन दक्षता पर केंद्रित हैं। नीचे वैश्विक और भारतीय प्राकृतिक कृषि की सर्वोत्तम कृषि विधियों का विवरण दिया गया है ।
- सर्वोत्तम वैश्विक कृषि विधियाँ
- एग्रोइकोलॉजी (लैटिन अमेरिका – ब्राज़ील, मैक्सिको, क्यूबा)
- पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तकनीकों के साथ जोड़ती है।
- जैव विविधता, फसल चक्र और प्राकृतिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा देती है।
- परमाकल्चर (ऑस्ट्रेलिया)
- एक सतत भूमि उपयोग प्रणाली जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का अनुकरण करती है।
- मृदा पुनर्जनन (Regeneration), वर्षा जल संचयन और सहजीवी पौधों की खेती पर केंद्रित है।
- सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन (एसआरआई) (मेडागास्कर और एशिया)
- जल उपयोग और पौधों की दूरी का अनुकूलन करके पैदावार बढ़ाता है।
- रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करता है और पौधों की मज़बूती बढ़ाता है।
- ऑर्गेनिक और बायोडायनामिक फार्मिंग (यूरोप – जर्मनी, स्विट्जरलैंड)
- कम्पोस्टिंग, फसल विविधीकरण और चंद्रमा चक्र (Lunar Cycle) का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है।
- मृदा परिष्करण के लिये सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाता है।
- एग्रोइकोलॉजी (लैटिन अमेरिका – ब्राज़ील, मैक्सिको, क्यूबा)
- सर्वोत्तम भारतीय कृषि विधियाँ
- जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक)
- सुभाष पालेकर द्वारा विकसित, यह जीवामृत, बीजामृत और अंतरफसल विधि का उपयोग कर रासायनिक उर्वरकों को समाप्त करता है।
- ऋषि कृषि और वैदिक खेती (महाराष्ट्र)
- पंचगव्य, अमृतपानी और आयुर्वेदिक सूत्रों का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है।
- पारंपरिक ज्ञान पर आधारित प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करता है।
- सामुदायिक प्राकृतिक खेती (सिक्किम – भारत का पहला जैविक राज्य)
- एक नीति-आधारित पहल जिसने सिक्किम को पूरी तरह जैविक बनाया।
- रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देता है, हालांकि पैदावार में गिरावट को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- वाटरशेड सपोर्ट और आदिवासी कृषि (ओडिशा)
- बहु-स्तरीय फसल प्रणाली, कृषि वानिकी और देशी बीजों को बढ़ावा देता है।
- आदिवासी किसानों को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है।
प्राकृतिक खेती स्थिरता बढ़ाने, रासायनिक निर्भरता कम करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक है। जहाँ वैश्विक पद्धतियाँ आधुनिक तकनीकों के साथ पारिस्थितिक सिद्धांतों को जोड़ती हैं, वहीं भारतीय पारंपरिक विधियाँ स्वदेशी ज्ञान पर आधारित हैं। इन पद्धतियों को बड़े पैमाने पर अपनाने से कृषि का भविष्य अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।
- जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक)
- परिचय
- फ्लाई ऐश (Fly Ash) प्राय: कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक हैं, जिसे दहन कक्ष से निष्कासित गैसों द्वारा ले जाया जाता है।
- इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर या बैग फिल्टर द्वारा निष्कासित गैसों से एकत्र किया जाता है।
- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ESP) को एक फिल्टर उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग प्रवाहित होने वाली गैस से धुएँ और धूल जैसे महीन कणों को हटाने के लिये किया जाता है।
- इस उपकरण को प्रायः वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के लिये प्रयोग किया जाता है।
- चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्यप्रदेश के तीन ताप विद्युत गृहों को फ्लाई ऐश के कुशल व प्रभावी प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।- यह पुरस्कार मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी (MPPGCL) के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी व अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई को प्रदान किया गया।
- यह सम्मान फ्लाई ऐश उपयोगिता-2025 विषय पर गोवा में मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय आवासीय सम्मेलन के दौरान दिया गया।
- यह सम्मेलन मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- संयोजन :
फ्लाई ऐश में विभिन्न रासायनिक तत्त्व होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से :- सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO₂)
- एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃)
- फेरिक ऑक्साइड (Fe₂O₃)
- कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)
ये सभी तत्त्व मिलकर फ्लाई ऐश को विभिन्न उपयोगों के लिये उपयुक्त बनाते हैं।
- अनुप्रयोग :
फ्लाई ऐश का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे :- कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों : फ्लाई ऐश का मिश्रण कंक्रीट में मजबूती और स्थिरता बढ़ाने के लिये किया जाता है।
- रोड बेस : सड़क निर्माण में इसे एक मजबूत और स्थिर आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।
- मेटल रिकवरी : फ्लाई ऐश में कुछ धातुओं का मिश्रण होता है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
- मिनरल फिलर : फ्लाई ऐश का उपयोग विभिन्न प्रकार के मिनरल फिलर के रूप में भी किया जाता है, जो निर्माण सामग्री में सहायक होते हैं।
हालाँकि फ्लाई ऐश के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कण कण विषैले वायु प्रदूषक हैं। ये हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ावा दे सकते हैं।
प्रकाश रासायनिक धुंध (Photochemical Smog) एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, जो तब उत्पन्न होता है जब सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOₓ) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) जैसे प्रदूषकों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में ओजोन (O₃), पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट (PAN) और अन्य विषैले यौगिकों जैसे हानिकारक द्वितीयक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। यह धुंध विशेष रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में गर्म, धूप वाले दिनों में अधिक पाई जाती है।
प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण कैसे होता है?
1. प्राथमिक प्रदूषकों का उत्सर्जन :
- वाहनों, उद्योगों और बिजली संयंत्रों से NOₓ और VOCs जैसे प्रदूषक वातावरण में उत्सर्जित होते हैं।
2. प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया :
- सूर्य के प्रकाश में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) टूटकर नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) और मुक्त ऑक्सीजन परमाणु (O) में परिवर्तित हो जाता है।
- मुक्त ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन अणु (O₂) से प्रतिक्रिया करके ओजोन (O₃) का निर्माण करते हैं।
- VOCs, NO और ओजोन के साथ मिलकर PAN, एल्डिहाइड्स और अन्य विषैले यौगिक बनाते हैं।
प्रकाश रासायनिक धुंध के प्रमुख घटक
- ओजोन (O₃) : एक हानिकारक गैस जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है।
- पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट (PAN) : आँखों में जलन और पौधों को नुकसान पहुँचाता है।
- नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOₓ) : ओजोन के निर्माण और अम्ल वर्षा में योगदान देता है।
- वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) : ईंधन, पेंट और सॉल्वेंट्स से उत्सर्जित होते हैं।
धुंध के निर्माण में सहायक कारक
- उच्च तापमान : रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है।
- तेज धूप : प्रदूषकों के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है।
- स्थिर वायु : प्रदूषकों के फैलाव को रोकती है।
- शहरीकरण : वाहनों और उद्योगों से उत्सर्जन को बढ़ाता है।
प्रकाश रासायनिक धुंध के हानिकारक प्रभाव
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
- श्वसन संबंधी समस्याएँ : दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में जलन का कारण बनता है।
- आँखों में जलन : PAN और ओजोन से आँखों में जलन होती है।
- दीर्घकालिक रोग : लंबे समय तक संपर्क से गंभीर श्वसन रोग हो सकते हैं।
- पर्यावरण पर प्रभाव
- वनस्पति को नुकसान : धुंध प्रकाश संश्लेषण को कम कर देती है, जिससे पौधों की वृद्धि में रुकावट आती है।
- मृदा प्रदूषण : मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर कृषि उत्पादन में कमी लाता है।
- पारिस्थितिकी असंतुलन : संवेदनशील प्रजातियों को नुकसान पहुँचाकर पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता है।
- वस्त्र और संरचनाओं पर प्रभाव
- संरचनाओं का क्षरण : इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुँचाता है।
- रंग-रोगन का क्षरण : वाहनों और अन्य धातु सतहों के रंग को खराब करता है।
प्रकाश रासायनिक धुंध मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और संरचनाओं के लिये एक गंभीर खतरा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिये उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ तकनीकों का उपयोग, और जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इन उपायों से न केवल पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
दृश्य सहायक सामग्री महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण हैं जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक, समझने योग्य और यादगार बनाने में सहायक होते हैं। ये दृश्य उपकरण जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने, शिक्षार्थियों का ध्यान बनाए रखने और जानकारी के बेहतर स्मरण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
- दृश्य सहायक सामग्री के प्रकार
- चार्ट्स और ग्राफ्स
- प्रकार : बार चार्ट, पाई चार्ट, रेखा ग्राफ, हिस्टोग्राम।
- उद्देश्य : सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत करना, विभिन्न चर का तुलनात्मक विश्लेषण करना, और समय के साथ प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करना।
- उदाहरण : विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर को दर्शाने वाला बार ग्राफ।
- आरेख (Diagrams)
- प्रकार : फ्लोचार्ट, प्रक्रिया आरेख, संकल्पना मानचित्र।
- उद्देश्य : प्रक्रियाओं को समझाना, संबंधों का प्रदर्शन करना, और संरचनाओं या प्रणालियों को चित्रित करना।
- उदाहरण : प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाने वाला फ्लोचार्ट।
- मानचित्र (Maps)
- प्रकार : भौतिक, राजनीतिक, थीमैटिक, और टोपोग्राफिक मानचित्र।
- उद्देश्य : भौगोलिक समझ को बढ़ावा देना, स्थानिक संबंधों को प्रदर्शित करना और स्थानों का चित्रण करना।
- उदाहरण : भारत के राज्यों को दर्शाने वाला राजनीतिक मानचित्र।
- पोस्टर (Posters)
- उद्देश्य : प्रमुख अवधारणाओं का दृश्यात्मक सारांश प्रस्तुत करना, प्रेरणादायक संदेश दिखाना और अधिगम उद्देश्यों को सुदृढ़ करना।
- उदाहरण : मानव विकास के चरणों को दिखाने वाला पोस्टर।
- फोटोग्राफ्स और चित्र (Photographs and Pictures)
- उद्देश्य : वास्तविक उदाहरण प्रदान करना, दृश्य स्मृति को सुदृढ़ करना और संदर्भात्मक समझ को स्थापित करना।
- उदाहरण : इतिहास के पाठ में ऐतिहासिक स्मारकों की तस्वीरें।
- फ्लैशकार्ड्स (Flashcards)
- उद्देश्य : शब्दावली और सूत्रों को याद रखने, शीघ्र पुनरावृत्ति, और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करना।
- उदाहरण : गणितीय सूत्रों को दिखाने वाले फ्लैशकार्ड्स।
- मॉडल्स (Models)
- प्रकार : त्रि-आयामी(3-D), डिजिटल या भौतिक मॉडल।
- उद्देश्य : जटिल संरचनाओं को समझने के लिये एक स्पर्शनीय और दृश्य अनुभव प्रदान करना।
- उदाहरण : मानव ह्रदय का त्रि-आयामी मॉडल।
- इन्फोग्राफिक्स (Infographics)
- उद्देश्य : पाठ, चित्रों और चार्ट्स को मिलाकर जटिल डेटा को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना।
- उदाहरण : वैश्विक जलवायु परिवर्तन आँकड़ों का सारांश प्रस्तुत करने वाला इन्फोग्राफिक।
- ब्लैकबोर्ड/व्हाइटबोर्ड चित्रण
- उद्देश्य : व्याख्यान के दौरान तात्कालिक दृश्य स्पष्टीकरण देना और इंटरैक्टिव अधिगम को बढ़ावा देना।
- उदाहरण : जीवविज्ञान व्याख्यान के दौरान तंत्रिका तंत्र का त्वरित चित्रण।
- चार्ट्स और ग्राफ्स
- शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री का महत्व
- स्मृति को सुदृढ़ करना : दृश्य एड्स दीर्घकालिक स्मृति को बढ़ावा देते हैं।
- सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करना : सहभागिता और संवाद को बढ़ावा देना।
- विविध अधिगम शैलियों का समर्थन : दृश्य, श्रवण और संवेदनशील अधिगम विधियों के लिये उपयुक्त।
- समझ विकसित करने में मदद करना : ग्राफिक एड्स से कठिन जानकारी को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया जा सकता है।
मिडिल इनकम ट्रैप एक आर्थिक परिघटना है, जिसे विश्व बैंक ने वर्ष 2007 में परिभाषित किया था। यह उन देशों की स्थिति को दर्शाता है जो तीव्र गति से विकास तो करते हैं लेकिन उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने में असफल रहते हैं। यह ट्रैप मुख्य रूप से उन देशों पर लागू होता है, जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 1,000 से 12,000 अमेरिकी डॉलर (2011 की कीमतों के अनुसार) के बीच होती है।
- मिडिल इनकम ट्रैप के कारण और चुनौतियाँ :
जो देश इस जाल में फंस जाते हैं, उन्हें कई संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं :- बढ़ती श्रम लागत : प्रारंभिक औद्योगीकरण के बाद श्रमिकों की मजदूरी बढ़ने लगती है, जिससे सस्ते श्रम पर आधारित प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।
- नवाचार की कमी : विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिये नवाचार और उच्च मूल्य-वर्धित उद्योगों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई देश इस दिशा में पिछड़ जाते हैं।
- आय असमानता : संपत्ति और आय का असमान वितरण सामाजिक असंतोष को जन्म देता है और आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है।
- जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ : जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, कार्यशील जनसंख्या की घटती भागीदारी और कौशल की कमी विकास को धीमा कर सकती है।
- उद्योगों पर अत्यधिक निर्भरता : कई मध्यम-आय वाले देश विशिष्ट उद्योगों पर अधिक निर्भर होते हैं, जिससे वैश्विक झटकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- क्या भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है?
भारत वर्तमान में तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद इस ट्रैप में फंसने के जोखिम का सामना कर रहा है। इसकी प्रमुख वजहें हैं :- आय असमानता : भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है, जहाँ शीर्ष 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है, जबकि निचले 50% लोगों का हिस्सा घटकर मात्र 13% रह गया है।
- कर नीति का प्रभाव : उच्च GST और कॉर्पोरेट कर कटौती से धनी वर्ग को अधिक लाभ मिलता है, जिससे आय असमानता और गहरी होती है।
- मजदूरी और मुद्रास्फीति : स्थिर या घटती वास्तविक मजदूरी, मुद्रास्फीति, उच्च घरेलू ऋण और कम बचत दरें भारत की आर्थिक स्थिरता को चुनौती दे सकती हैं।
मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिये भारत को समावेशी विकास रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। नवाचार को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और मध्यम वर्ग की आय क्षमता में सुधार लाना महत्वपूर्ण कदम होंगे। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो भारत का उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने का सपना अधूरा रह सकता है।
मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों की सीखने की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करना है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, मूल्यांकन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मुख्य तरीकों से किया जाता है। प्रत्येक पद्धति के अपने लाभ और चुनौतियाँ हैं।
- ऑनलाइन मूल्यांकन
ऑनलाइन मूल्यांकन में कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित परीक्षा शामिल होती है, जहाँ परीक्षार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परीक्षा देते हैं।- लाभ :
- लचीलापन और सुविधा – कहीं से भी परीक्षा देने की सुविधा, जिससे यात्रा की आवश्यकता कम होती है।
- स्वचालित मूल्यांकन – बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुरंत जाँच हो जाती है।
- कम लागत – कागज, प्रिंटिंग और प्रशासनिक खर्चों में बचत होती है।
- तत्काल प्रतिक्रिया – परीक्षार्थियों को तुरंत परिणाम और प्रदर्शन विश्लेषण प्राप्त होता है।
- कुशल डेटा प्रबंधन – डिजिटल रूप से उत्तर संग्रहीत और विश्लेषित किये जाते हैं, जिससे सटीकता बढ़ती है।
- चुनौतियाँ :
- तकनीकी निर्भरता – इंटरनेट और उपयुक्त डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- नकल और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ – परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिये सख्त निगरानी की जरूरत होती है।
- सीमित वर्णनात्मक मूल्यांकन – निबंध और लंबे उत्तरों की जाँच मैन्युअल रूप से करनी पड़ती है।
- डिजिटल विभाजन – सभी परीक्षार्थियों के पास आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं होते।
- लाभ :
- ऑफलाइन मूल्यांकन
ऑफलाइन मूल्यांकन पारंपरिक कागज-आधारित परीक्षा होती है, जिसे परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाता है।- लाभ :
- बेहतर निगरानी – परीक्षक की उपस्थिति से अनुचित तरीकों से परीक्षा देने की संभावना कम हो जाती है।
- सभी परीक्षार्थियों के लिये समावेशी – इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती।
- वर्णनात्मक उत्तरों के लिये प्रभावी – लंबे उत्तरों और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का सटीक मूल्यांकन किया जा सकता है।
- कोई तकनीकी बाधा नहीं – सिस्टम विफलता या कनेक्टिविटी समस्याओं का जोखिम नहीं रहता।
- चुनौतियाँ :
- समय लेने वाली जाँच प्रक्रिया – मैन्युअल मूल्यांकन के कारण परिणाम घोषित होने में अधिक समय लगता है।
- अधिक प्रशासनिक लागत – परीक्षा केंद्र, परीक्षक और प्रिंटिंग जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- सीमित लचीलापन – परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर उपस्थित होना पड़ता है।
- लाभ :
- हाइब्रिड मूल्यांकन दृष्टिकोण
एक हाइब्रिड मॉडल दोनों पद्धतियों की श्रेष्ठ विशेषताओं को मिलाकर मूल्यांकन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है :- वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ऑनलाइन माध्यम से शीघ्रता से मूल्यांकित किया जा सकता है।
- वर्णनात्मक और शोध-आधारित प्रश्नों का ऑफलाइन मूल्यांकन अधिक प्रभावी होता है।
- AI-आधारित ऑनलाइन निगरानी से परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन मूल्यांकन दोनों की अपनी विशेषताएँ और सीमाएँ हैं। जहाँ ऑनलाइन मूल्यांकन सुविधा, गति और स्वचालन प्रदान करता है, वहीं ऑफलाइन मूल्यांकन विश्वसनीयता, समावेशिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। मूल्यांकन का तरीका विषय, मूल्यांकन की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चुना जाना चाहिये। हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाकर एक अधिक संतुलित और प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जा सकती है।
प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक और शोध दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक विधियों और निष्पक्षता पर आधारित होता है। यह समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक व्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान के रूप में देखने पर बल देता है।
- मुख्य विशेषताएँ :
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण :
- प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, जिसे प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाया जाता है।
- यह अनुभवजन्य तथ्यों (empirical facts) और परिक्षणीय डेटा (verifiable data) पर आधारित होता है।
- निष्पक्षता और तटस्थता :
- प्रत्यक्षवाद में निष्पक्षता (objectivity) को प्राथमिकता दी जाती है।
- यह व्यक्तिगत भावनाओं, विश्वासों और मूल्यों को ज्ञान से अलग मानता है।
- ज्ञान और ज्ञाता का विभाजन :
- प्रत्यक्षवाद यह मानता है कि ज्ञान (knowledge) और ज्ञाता (knower) स्वतंत्र होते हैं।
- इसमें आत्मपरकता (subjectivity) को नकारकर तथ्य-आधारित निष्कर्षों पर जोर दिया जाता है।
- समाजशास्त्र और सामान्य बोध का अंतर :
- समाजशास्त्र केवल सामान्य बोध (common sense) पर आधारित नहीं होता, बल्कि व्याख्यात्मक सिद्धांतों (explanatory theories) का अनुसरण करता है।
- यह सार्वभौमिक नियमों (universal laws) के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है।
- संगठित और व्यवस्थित ज्ञान :
- प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शब्दावली के माध्यम से संरचित किया जाता है।
- यह विशेष प्रवीणताओं (expertise) और कौशलों पर आधारित होता है।
- सामान्यीकरण और अमूर्तता :
- प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र को नियमों और सामान्यीकरण (generalization) के माध्यम से समझने का प्रयास करता है।
- यह मानव अनुभवों को विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत तरीके से परिभाषित करता है।
प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। यह निष्पक्षता, तर्क, और अनुभवजन्य तथ्यों के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है, जिससे समाजशास्त्र को एक सुव्यवस्थित विज्ञान के रूप में मान्यता मिलती है।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण :
अनुसंधान एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका मुख्य लक्ष्य नए ज्ञान की खोज, समस्याओं के समाधान और मौजूदा समझ के विस्तार में योगदान देना है। प्रत्येक शोध अध्ययन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है, जो अनुसंधान की दिशा निर्धारित करता है। परिकल्पना (Hypothesis) के निर्माण से लेकर अनुसंधान प्रस्ताव (Research Proposal) के विकास तक, शोध के उद्देश्य मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जिससे शोधकर्ता सार्थक निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं। अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य नवीन निष्कर्षों की खोज, मौजूदा सिद्धांतों की पुष्टि या संशोधन, और वैज्ञानिक एवं बौद्धिक प्रगति में योगदान देना है।
- अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य
- नए ज्ञान की प्राप्ति – अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य अज्ञात तथ्यों, अवधारणाओं या पैटर्न को खोजकर मानवीय ज्ञान को समृद्ध करना है।
- परिस्थितियों का सटीक वर्णन – अनुसंधान का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य किसी विशेष स्थिति, घटना या प्रवृत्ति का विस्तृत, सटीक और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करना है।
- समस्याओं का समाधान – अनुसंधान विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, समाजशास्त्र आदि में प्रासंगिक चुनौतियों की पहचान, विश्लेषण और समाधान करने में सहायक होता है।
- विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान – अनुसंधान तथ्यों और तर्कों पर आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिससे विषय की वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक समझ विकसित होती है।
- कार्य-कारण संबंध (Causal Relationship) की जाँच – अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि कैसे एक तत्व (Factor) दूसरे तत्व को प्रभावित करता है, जिससे कारण और प्रभाव के संबंधों को स्पष्ट किया जा सके।
- सह-संबंध (Correlation) की पहचान – अनुसंधान विभिन्न घटनाओं या चर (Variables) के बीच संबंध या सह-संबंध की खोज करता है, जिससे भविष्यवाणियाँ और निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- सिद्धांतों का विकास – व्यवस्थित अनुसंधान के माध्यम से नए सिद्धांतों (Theories) का निर्माण, पुष्टि या संशोधन किया जाता है, जिससे प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को बेहतर समझा जा सकता है।
- महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजना – अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों, तर्कसंगत सोच और डेटा-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक होता है।
अनुसंधान के उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नवाचार (Innovation) को प्रेरित करने, सामाजिक सुधार लाने और वैज्ञानिक उन्नति को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवस्थित पद्धतियों और जिज्ञासु दृष्टिकोण को अपनाकर अनुसंधान विविध क्षेत्रों में प्रगति और विकास का आधार बना हुआ है।
अनुसंधान में मुख्य तथ्यों (Facts) का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। स्रोत सामग्री के अध्ययन और मूल्यांकन के माध्यम से तथ्यों का व्यवस्थित संग्रह और संयोजन किया जाता है। मानविकी और समाज विज्ञान से जुड़े अनुसंधानों में व्यक्तिगत दृष्टिकोण का कुछ प्रभाव अवश्य रहता है, लेकिन शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक क्षमता उसे वस्तुनिष्ठ (Objective) और तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाती है।
अनुसंधान एक विकसित होती प्रक्रिया है, जिसकी प्रकृति गत्यात्मक (Dynamic), दृष्टिकोण वैज्ञानिक (Scientific), और विकास अभिसंचयी (Cumulative) होता है। यह ज्ञान और विद्वता का मार्गदर्शक भी है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड और क्रॉनबैंक ने अनुसंधान को चार वर्गों में विभाजित किया:
- सर्वेक्षण अनुसंधान (Survey Research)
- यह अनुसंधान दो या अधिक चरों से संबंधित घटनाओं के आँकड़ों के संकलन और वर्गीकरण से जुड़ा होता है।
- इसका उद्देश्य इन चरों के बीच संबंधों (Correlation) को समझना होता है।
- यह अनुसंधान अन्वेषणात्मक (Exploratory) होता है।
- इस विधि का उपयोग कर जनसंख्या अध्ययन (Population Studies) को सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
- प्रविधि अनुसंधान (Technical Research)
- इस अनुसंधान का संबंध अवलोकन (Observation) विधि से जुड़ी समस्याओं के समाधान से होता है।
- जब किसी चर (Variable) के अध्ययन के लिये एक से अधिक अवलोकन विधियाँ उपलब्ध होती हैं, तो यह अनुसंधान उनकी तुलना और मूल्यांकन करके उनकी प्रभावशीलता (Effectiveness) को निर्धारित करता है।
- व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research)
- इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना होता है।
उदाहरण: यदि किसी समस्या को हल करने के लिये कई विधियाँ उपलब्ध हों, और हमें सबसे प्रभावी विधि का चयन करना हो, तो यह अनुसंधान उचित निर्णय लेने में सहायक होता है।
- इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना होता है।
- आलोचनात्मक अनुसंधान (Critical Research)
- यह अनुसंधान पूर्व-निर्धारित धारणाओं (Preconceived Hypothesis) पर आधारित होता है।
- इसमें अनुसंधानकर्ता यह मानकर चलता है कि यदि यह अनुसंधान किया जाए, तो नए ज्ञान की प्राप्ति होगी या कुछ नए तथ्य सामने आएंगे।
एडवर्ड और क्रॉनबैंक द्वारा प्रस्तुत यह वर्गीकरण अनुसंधान पद्धतियों को एक संरचित रूप (Structured Approach) प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ता अपनी अनुसंधान आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त विधि का चयन कर सकते हैं।
अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो नए ज्ञान के प्रकाश में आने और पुराने भ्रमों के सुधार में सहायक होती है। इसमें ज्ञान के प्रसार एवं संवर्धन के लिये प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त निष्पक्ष आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, और इस प्रक्रिया में सांख्यिकी विधियाँ तथा वैज्ञानिक अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित और वस्तुनिष्ठ निरीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों के सत्यापन के लिये विश्वसनीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है, साथ ही नए तथ्यों, विधियों या वस्तुओं की खोज एवं प्राचीन सिद्धांतों में सुधार हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण और सुव्यवस्थित विश्लेषण विधि का पालन किया जाता है।
- अनुसंधान के प्रकार
- प्रत्येक अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या की पहचान से होती है, जिसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं :
- बौद्धिक (Intellectual) : मनुष्य की अंतर्निहित जिज्ञासा एवं ज्ञानार्जन की प्रेरणा से उत्पन्न आत्मसंतुष्टि।
- व्यावहारिक (Practical) : ज्ञान की प्राप्ति और किसी विशेष समस्या का व्यवस्थित विश्लेषण।
इन दो उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है :
- मूलभूत अनुसंधान (Fundamental or Basic Research) : मूलभूत अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य नई प्ररचनाओं (Design) का निर्माण करना और वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक तथा अन्य घटनाओं की बेहतर समझ विकसित करना है।
- विशेषताएँ :
- नए विचारों और सिद्धांतों का सृजन
- प्रगति और विकास के लिये आधार तैयार करना
- जीन पियाजे जैसे वैज्ञानिकों ने मानव विकास के सिद्धांत भी इसी आधार पर प्रतिपादित किये हैं।
- अनुप्रयुक्त अनुसंधान में भूमिका : मूलभूत अनुसंधान के सिद्धांतों और खोजों का उपयोग बाद में व्यावहारिक अनुसंधान में किया जाता है।
- विशेषताएँ :
- व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research) : व्यावहारिक अनुसंधान का लक्ष्य उन क्रियात्मक समस्याओं का समाधान करना है, जिनका सामना दैनिक जीवन में किया जाता है।
- विशेषताएँ :
- वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से व्यावहारिक समस्याओं का विश्लेषण
- नवीन प्रौद्योगिकियों और आधुनिक विधियों के विकास में योगदान
- प्रबंधकीय और संगठनात्मक दृष्टिकोण से अधिक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना
- उदाहरण : किसी उद्योग या संगठन में उत्पन्न समस्या का समाधान खोजने हेतु शोध करना, जिससे की कार्यप्रणाली में सुधार और विकास हो सके।
- विशेषताएँ :
- वर्गीकरण के अन्य आयाम
राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (National Science Foundation) अनुसंधान को निम्नलिखित श्रेणियों में भी वर्गीकृत करता है :- मूलभूत अनुसंधान (Fundamental Research)
- व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research)
- प्रयोगात्मक अनुसंधान (Experimental Research)
इस प्रकार, अनुसंधान की प्रक्रिया न केवल ज्ञान के सृजन और संवर्धन में सहायक है, बल्कि यह समाज में विद्यमान समस्याओं का विश्लेषण और समाधान भी प्रस्तुत करती है। यह एक सुव्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न प्रक्रिया है, जो निरंतर मानव सभ्यता के विकास में योगदान देती रहती है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के त्वरित समाधान के लिये एक विशेष न्यायिक निकाय है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और संसाधनों के सतत् उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- परिचय
- स्थापना : राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत।
- उद्देश्य : पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संबंधी विवादों का 6 माह के भीतर त्वरित समाधान।
- मुख्यालय : नई दिल्ली (मुख्य कार्यालय), और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, तथा चेन्नई।
- संरचना
- संघटन : अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, और विशेषज्ञ सदस्य।
- कार्यकाल : सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)।
- नियुक्ति :
- अध्यक्ष : केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से।
- न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य : चयन समिति के माध्यम से।
- सदस्यों की संख्या : 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य।
- अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
- भारत NGT स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश है।
- शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र
- अधिकार क्षेत्र : पर्यावरणीय अधिकारों और मुद्दों से संबंधित दीवानी मामलों का निपटारा।
- स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers) : 2021 से लागू।
- भूमिकाएँ : न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक।
- सिद्धांत :
- सतत् विकास।
- निवारक सिद्धांत (Precautionary Principle)।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)।
- प्रक्रिया : प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन। CPC, 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं।
- आदेश :
- सिविल कोर्ट के आदेशों की तरह बाध्यकारी।
- राहत और मुआवजे का प्रावधान।
- निर्णयों की समीक्षा और अपील की अनुमति।
- उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान (90 दिनों के भीतर)।
- NGT के तहत प्रमुख कानून :
- जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974।
- वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980।
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग और पर्यावरण संरक्षण में एक प्रभावी उपकरण है। यह प्रदूषण रोकने और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिये एक मजबूत ढाँचा प्रदान करता है।
- इंट्रानेट के लाभ :
- लागत में कमी : इंट्रानेट व्यक्तिगत संचार विधियों जैसे फैक्स या मेल की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके बजाय, संगठन सीधे इंट्रानेट नेटवर्क पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं, जिससे संचार लागत में कमी आती है और समग्र दक्षता में सुधार होता है।
- प्राधिकृत पहुँच : इंट्रानेट का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें प्राधिकृत पहुँच नियंत्रण सेट किये जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल उन व्यक्तियों को ही जानकारी तक पहुँच प्राप्त हो सकती है जिनके पास सही क्रेडेंशियल्स हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुँच को रोका जाता है।
- गोपनीयता : इंट्रानेट प्रणाली संगठनात्मक जानकारी की सुरक्षा के लिये डिजाइन किये गए हैं। डेटा को एक सुरक्षित नेटवर्क में रखने से डेटा उल्लंघनों का जोखिम न्यूनतम होता है, जिससे गोपनीय जानकारी की सुरक्षा बनी रहती है।
- उत्पादकता में वृद्धि : चूँकि कर्मचारी आसानी से इंट्रानेट के माध्यम से आवश्यक संसाधनों और जानकारी तक पहुँच सकते हैं, कार्य जल्दी और अधिक प्रभावी तरीके से पूरे किये जा सकते हैं। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है।
- इंट्रानेट के नुकसान :
- सुरक्षा चिंताएँ : सुरक्षा सुविधाओं के बावजूद, डेटा चोरी या अनधिकृत पहुँच का हमेशा जोखिम रहता है। हैकर्स निजी नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और संवेदनशील डेटा को जोखिम में डाल सकते हैं, इसलिये मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
- संवाद में कमी : इंट्रानेट आधारित संचार पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कर्मचारियों के बीच आमने-सामने बातचीत कम हो सकती है। यह शारीरिक संचार की कमी टीमवर्क और आपसी समझ को प्रभावित कर सकती है, जो संगठनात्मक रिश्तों को मजबूत बनाने और सहयोगी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये महत्वपूर्ण होते हैं।
इंट्रानेट प्रणाली लागत बचत और सुरक्षा में सुधार जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इसके साथ सुरक्षा जोखिमों और कर्मचारियों के बीच सामाजिक संवाद में कमी जैसी चुनौतियाँ भी हैं। इसलिये इन कारकों का संतुलन बनाए रखना संगठन में इंट्रानेट की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिये महत्वपूर्ण है |
इंट्रानेट एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसका उपयोग किसी संगठन के अंदर सूचना के आदान-प्रदान और नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे संस्था के सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। इंट्रानेट का उद्देश्य केवल एक संगठन के भीतर डेटा और जानकारी का सुरक्षित रूप से साझा करना है, न कि बाहरी उपयोगकर्ताओं से जुड़ा होना।
इंट्रानेट की स्थापना लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) और वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) के माध्यम से की जाती है। इन नेटवर्कों के जरिए एक संगठित वातावरण में डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है, जिससे कार्य स्थल पर कार्यशीलता और सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलता है। इंट्रानेट में आमतौर पर दो मुख्य पोर्टल होते हैं:
- इंट्रानेट पोर्टल: यह पोर्टल आंतरिक सूचना को संयोजित करने और संस्थान के भीतर विभिन्न कंप्यूटरों में साझा करने के लिये होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के बीच संगठनात्मक जानकारी को आसानी से उपलब्ध कराना है।
- एंटरप्राइज पोर्टल: इसे एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल भी कहा जाता है। यह पोर्टल मुख्य रूप से संस्थान से बाहर की दुनिया में सूचना भेजने के लिये होता है। इसमें एक सुरक्षित यूनीसेफ एक्सेस पॉइंट होता है, जो वेब-आधारित यूजर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
साइबर खतरों से बचाव के लिये निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय लागू किये जा सकते हैं:
- एंटीवायरस (Antivirus): एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे वायरस तथा अन्य मालवेयर को रोकने, पहचानने, निर्धारित करने तथा हटाने के लिये डिजाइन किया गया है। जैसे: Avast, McAfee, Kaspersky, Quick Heal, Nortan इत्यादि।
- डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature): यह सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो मैसेज या डॉक्यूमेंट भेजने वाले के प्रमाणीकरण तथा पहचान के लिये उपयोग होता है।
- डिजिटल सर्टिफिकेट (Digital Certificate): यह उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के साथ जोड़ा जाता है, यह संदेश की प्रामाणिकता और पहचान सुनिश्चित करता है।
- फायरवॉल (Firewall): एक सुरक्षा बाधा, जो हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर-आधारित हो सकती है, जिसका उपयोग कंप्यूटरों को अनधिकृत पहुँच और संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिये किया जाता है।
- आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल (IP Security Protocol): यह Security Protocol Suit, इंटरनेट पर गोपनीय तथा प्रमाणीकृत सेवा प्रदान करने में उपयोगी है। IP Security, IP ट्रैफिक पर प्रमाणीकरण, इनक्रिप्शन तथा संक्षिप्तीकरण सेवा की अनुमति प्रदान करता है।
इन उपायों को लागू करने से कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है, जिससे साइबर खतरों से संबंधित जोखिमों को कम किया जा सकता है। नियमित अपडेट और साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाए रखने के महत्वपूर्ण घटक हैं।
मानव गतिविधियों, जिन्हें मानवजनित गतिविधियाँ भी कहा जाता है, ने प्राकृतिक पर्यावरण को काफी हद तक बदल दिया है। जबकि तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास ने जीवन स्तर में सुधार किया है, वे पर्यावरणीय क्षरण का कारण भी बने हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा पैदा करता है। निम्नलिखित अनुभागों में प्रमुख मानवजनित गतिविधियों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा की गई है।
- वनों की कटाई
वनों की कटाई, जो बड़े पैमाने पर कृषि विस्तार, शहरीकरण और लकड़ी की कटाई के कारण होती है, पर्यावरण के लिये एक महत्वपूर्ण खतरा है। वन कार्बन भंडारण, जैव विविधता और जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके विनाश के कारण निम्नलिखित हानियाँ होती हैं :- जैव विविधता का नुकसान होता है क्योंकि निवास स्थान नष्ट हो जाते हैं।
- कम कार्बन भंडारण के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
- मृदा कटाव और उपजाऊ क्षमता में कमी।
- स्थानीय और वैश्विक जल चक्रों का विघटन।
- औद्योगिकीकरण और शहरीकरण
औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों का विस्तार प्रदूषण और संसाधनों की कमी का कारण बनता है। इसके मुख्य प्रभावों में शामिल हैं:- कारखानों और वाहनों से वायु प्रदूषण, जो श्वसन समस्याओं और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
- औद्योगिक अपशिष्टों से जल प्रदूषण, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र और पेयजल स्रोतों को प्रभावित करता है।
- ऊर्जा की खपत में वृद्धि, जो अक्सर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर होती है, वैश्विक तापमान को बढ़ाती है।
- कृषि प्रथाएँ
आधुनिक कृषि, जो करोडों लोगों को भोजन प्रदान करती है, पर्यावरण पर दबाव डालती है। इनमें शामिल हैं:- सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, जो मृदा और जल को प्रदूषित करते हैं।
- अत्यधिक सिंचाई, जिससे जल की कमी और मिट्टी का लवणीकरण होता है।
- एकल फसल कृषि, जो जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य को खराब करती है।
- खनन और संसाधन निष्कर्षण
खनिज, धातु और जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण आधुनिक उद्योगों के लिये आवश्यक है, लेकिन इसके गंभीर परिणाम होते हैं:- निवास स्थान का विनाश और परिदृश्य का परिवर्तन।
- भारी धातुओं जैसे हानिकारक प्रदूषकों का पर्यावरण में उत्सर्जन।
- जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि।
- अपशिष्ट उत्पादन
प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और खतरनाक कचरे सहित अपशिष्ट उत्पादन में तेजी से वृद्धि एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है:- प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन के लिये खतरा है और सदियों तक पर्यावरण में बना रहता है।
- ई-कचरे का अनुचित निपटान सीसा और पारा जैसे विषैले पदार्थों को जारी करता है।
- लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन होता है, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
- जलवायु परिवर्तन
मानव गतिविधियों का सबसे व्यापक प्रभाव जलवायु परिवर्तन है। जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने:- वैश्विक तापमान में वृद्धि, हीटवेव और बदलते मौसम के पैटर्न को जन्म दिया है।
- ध्रुवीय बर्फ के पिघलने और समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों को खतरा उत्पन्न हुआ है।
- इससे प्राकृतिक आपदाओं, जैसे तूफान और बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- समाधान रणनीतियाँ
मानवजनित गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये निम्नलिखित सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं:- सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण।
- स्थायी कृषि और वानिकी प्रथाओं को अपनाना।
- कचरे को कम करने, पुनर्चक्रण और परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
- पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और पर्यावरणीय नियमों को सख्त बनाना।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये व्यक्तिगत कार्यों को प्रोत्साहित करना।
मानवजनित गतिविधियों ने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है, लेकिन पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक है। इन प्रभावों को संबोधित करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई से नुकसान को कम किया जा सकता है और प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध निर्मित किया जा सकता है।
साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा तक अनधिकृत पहुँच या उनको क्षति से बचाने के सुरक्षा उपायों से संबंधित है।
- कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित खतरों की समझ :
- मालवेयर (Malware): मालवेयर दोषपूर्ण (Malicious) सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुँच के लिये किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं :
- वायरस (Virus): ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने के पश्चात उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये स्वयं की कॉपी कर सकते हैं तथा अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर उन्हें क्षति पहुँचा सकते हैं। जैसे Melissa आदि।
- वॉर्म (Worms): यह स्वयं की प्रतिकृति (Self-Replicating) बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है। जैसे: Bagle, Morris, Sasser, Code Red आदि।
- ट्रोजन हॉर्स (Trojan Horse): यह ऐसा प्रोग्राम होता है, जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता पर वास्तव में यह मालवेयर होता है।
- स्पाईवेयर (Spyware): यह प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम (Owner) की गतिविधियों तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिये सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है।
- स्पूफिंग (Spoofing): अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुँच बनाने को Spoofing कहते हैं।
- हैकिंग (Hacking): हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है।
- सलामी तकनीक (Salami Technique): यह कई छोटे कार्यों की शृंखला को संदर्भित करता है, जिसे गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर इन कार्यों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्यत: इसे पहचान पाना कठिन होता है। उदाहरणस्वरूप ऑनलाइन खरीददारी या ATM से लेन-देन करते समय कुछ पैसे (5 या 10 पैसे) अनधिकृत रूप से व्यय हो जाना, वाहनों में डीजल एवं पेट्रोल भरवाते समय प्रतिलीटर कुछ मिलीलीटर कम तेल प्राप्त होना इत्यादि। इस प्रकार के सभी कार्य गैर-कानूनी कार्यों की श्रेणी में आते हैं।
- स्पैम (Spam): e-mail के रूप में जो अनचाहे bulk मैसेज प्राप्त होते हैं, उन्हें ‘Spam’ कहते हैं। इसे कई प्राप्तकर्त्ताओं को तुरंत भेजा गया अयातित ई-मेल भी कहते है।
- रूटकिट (Rootkit): ये ऐसे मालवेयर हैं, जिनका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिये किया जाता है।
- फिशिंग (Phishing): यह अवैध तरीके से संवेदनशील जानकारी, जैसे- पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल आदि प्राप्त करने तथा फर्जी बैंक स्टेटमेंट, ई-पे रसीद आदि भेजने के लिये प्रोग्राम किये गए मालवेयर होते हैं।
- मालवेयर (Malware): मालवेयर दोषपूर्ण (Malicious) सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुँच के लिये किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं :
- एंटीवायरस (Antivirus): एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लिकेशन होते हैं जो वायरस, मालवेयर, स्पायवेयर और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर से आपके सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। यह सॉफ्टवेयर वायरस को पहचानकर उसे हटाता है, और सिस्टम को संभावित खतरों से बचाने के लिये निरंतर निगरानी करता है। एंटीवायरस प्रोग्रामों के उदाहरण में Avast, McAfee, Kaspersky, Quick Heal, Norton, Bitdefender, आदि शामिल हैं। इन सॉफ्टवेयर में रियल-टाइम प्रोटेक्शन, ऑटो-स्कैनिंग, और डेटा रिकवरी जैसी कई विशेषताएँ होती हैं, जो उपयोगकर्ता को साइबर हमलों से बचाती हैं।
- डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature): डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, जो किसी व्यक्ति या संगठन की पहचान को प्रमाणित करने के लिये प्रयोग किया जाता है। यह संदेश या दस्तावेज़ को सुरक्षित रूप से भेजने के लिये उपयोगी होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संदेश को बिना किसी परिवर्तन के प्राप्त किया गया है और वह वास्तविक भेजने वाले द्वारा ही भेजा गया है। यह आमतौर पर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी कुंजी का इस्तेमाल होता है।
- डिजिटल सर्टिफिकेट (Digital Certificate): डिजिटल सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ होता है, जिसे प्रमाणित किया जाता है और यह बताता है कि किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान सत्यापित है। यह डिजिटल सिग्नेचर को विश्वसनीय बनाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट आमतौर पर एक सार्वजनिक कुंजी के साथ जुड़ा होता है और इसे प्रमाणित करने वाली संस्था (Certificate Authority - CA) द्वारा जारी किया जाता है। यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिये उपयोगकर्ता के डेटा की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करता है।
- फायरवॉल (Firewall): फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है, जो नेटवर्क पर होने वाली ट्रैफिक की निगरानी करती है और निर्धारित करती है कि कौन सी जानकारी नेटवर्क के अंदर या बाहर जा सकती है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित हो सकता है और उपयोगकर्ताओं को बाहरी हमलों से बचाने के लिये निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर काम करता है। फायरवॉल न केवल वायरस और हैकर्स को रोकता है, बल्कि यह नेटवर्क पर अनधिकृत प्रवेश और डाटा लीक को भी रोकने में मदद करता है।
- आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल (IP Security Protocol): आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल (IPSec) एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर डेटा के संचार को सुरक्षित बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है। यह इंटरनेट ट्रैफिक पर डेटा को एन्क्रिप्ट और प्रमाणित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा को भेजने और प्राप्त करने के दौरान उसकी गोपनीयता और अखंडता बनी रहती है। IPSec का उपयोग VPN (Virtual Private Network) और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शनों में किया जाता है, और यह डेटा के संरक्षण के लिये प्रमाणीकरण, इनक्रिप्शन और डेटा के बारे में जानकारी को संरक्षित करता है।
इन सुरक्षा उपायों का उपयोग करके, हम साइबर हमलों से अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं और व्यक्तिगत, वित्तीय, और संवेदनशील जानकारी की रक्षा कर सकते हैं।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: सस्टेनेबिलिटी 2025 वैश्विक विश्वविद्यालयों द्वारा पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की प्रगति को मापने वाला एक महत्वपूर्ण मानदंड है। इस रैंकिंग का तीसरा संस्करण विश्वविद्यालयों के योगदान को तीन प्रमुख क्षेत्रों—पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, और शासन—के आधार पर मूल्यांकित करता है।
इस बार, रैंकिंग में 78 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई, जिसमें कई संस्थानों ने वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।
- भारत के शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता
- IIT दिल्ली: भारत में प्रथम और विश्व स्तर पर 171वें स्थान पर।
- IIT खड़गपुर: राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा और वैश्विक स्तर पर 202वाँ स्थान।
- IIT बॉम्बे: भारत में तीसरा और विश्व स्तर पर 234वाँ स्थान।
- IIT कानपुर: चौथे स्थान पर और वैश्विक स्तर पर 245वाँ।
- IIT मद्रास: भारत में पाँचवाँ और वैश्विक स्तर पर 277वाँ स्थान।
- उल्लेखनीय क्षेत्र
- पर्यावरणीय प्रभाव: IIT दिल्ली और IIT कानपुर ने क्रमशः 55वें और 87वें स्थान पर रहते हुए वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया।
- पर्यावरणीय स्थिरता: IIT बॉम्बे भारत में सर्वोच्च स्थान पर रहा, वैश्विक स्तर पर 38वें स्थान पर।
- पर्यावरण शिक्षा: IIT बॉम्बे ने वैश्विक रैंकिंग में 32वाँ स्थान हासिल किया।
- शासन और समानता: मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) इस श्रेणी में भारत में अग्रणी रही और समानता के लिये शीर्ष स्थान पर (वैश्विक स्तर पर 390वाँ)।
- सामाजिक प्रभाव: IIT दिल्ली ने रोजगार और परिणाम के मामले में भारत में शीर्ष प्रदर्शन किया, वैश्विक स्तर पर 116वाँ स्थान।
- ज्ञान का आदान-प्रदान: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) इस क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च स्थान पर रहा, वैश्विक स्तर पर 121वें स्थान पर।
- चुनौतियाँ और सुधार के अवसर
हालाँकि भारतीय विश्वविद्यालयों ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण तथा शिक्षा प्रभाव में सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, इन श्रेणियों में कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 350 में शामिल नहीं है।
QS (Quacquarelli Symonds), एक लंदन स्थित संगठन, उच्च शिक्षा विश्लेषण के लिये जाना जाता है। इसकी रैंकिंग वैश्विक संस्थानों के लिये प्रगति और सुधार का रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा मिलता है।
1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में ‘मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा ज़िला स्तर पर ज़िला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था।
- संविधान लागू होने के बाद की विकास यात्रा
- 2 अक्तूबर, 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
- इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिये बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को ही भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार (शिल्पी) कहा जाता है।
- इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने का मूल कारण जन-सहभागिता की उपेक्षा को माना व सुझाव दिया कि जन-सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज ही हो सकता है, अत: पंचायतों का त्रिस्तरीय ढाँचा बनाया जाना चाहिये।
- सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय स्वशासन संबंधित अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया।
- इसके तुरंत बाद 11 अक्तूबर, 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूबनगर ज़िले के शादनगर विकास खंड में शुरू की गई।
- पंचायती राज पर गठित समितियाँ
|
समिति |
सिफारिश |
|
बलवंत राय मेहता (1957) |
त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव |
|
अशोक मेहता (1977) |
त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव |
|
जी.वी.के. राव (1985) |
ज़िला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्त्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव |
|
लक्ष्मीमल सिंघवी (1986) |
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव |
इन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी, 1989 के लोकसभा चुनाव के पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहते थे लेकिन वह राज्यसभा में अपेक्षित बहुमत हासिल नहीं कर पाए। आगे यही विधेयक 73वें संविधान संशोधन का आधार बना।
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- 24 अप्रैल, 1993 को 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ, इसलिये इस तिथि को ‘राष्ट्रीय पंचायत दिवस’ के रूप में भी मनाया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- इसके तहत संविधान के भाग-9 को पुन: जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद-243 था। भाग-9 का शीर्षक है-‘पंचायतें’ तथा इसमें अनुच्छेद 243 से 243ण (O) तक सम्मिलित हैं।
- इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिये निर्दिष्ट 29 विषयों की सूची दी गई है।
नोट: पंचायती राज राज्य सूची का विषय है।
- मेल मर्ज (Mail Merge): मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड (एम.एस.वर्ड) की एक महत्वपूर्ण सुविधा है। जिसकी सहायता से यूजर एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकता है। जब किसी संदेश को एक ग्रुप को भेजना हो तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। इससे हम डाटाबेस को भी जोड़ सकते है।
- वेब एड्रेस (Web Address): यह वेब पेज की स्थिति को बताता है। वेब पर वेब एड्रेस URL कहलाता है, URL (Uniform Resource Locator) इंटरनेट पर किसी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है।
- डोमेन नाम (Domain Name): डोमेन नाम एक विशिष्ट नाम है, जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्त्ता वेबसाइट तक पहुँच सकता है। जैसे-Google.com, Yahoo.com इत्यादि।
- प्रमुख वेबसाइट डोमेन
- .int - International Organization & Treaty
- .info - Informational Organization
- .com - Commercial
- .gov - Government
- .edu - Education
- .org - Non-Profit Organization
- इंटरनेट प्रोटोकॅाल एड्रेस (आईपी एड्रेस) : जब यूजर अपने फोन या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तो उसके डिवाइस को इंटरनेट पर पहचान के लिये एक खास कोड दिया जाता है, जिससे यूजर की लोकेशन और नेटवर्क का पता चलता है। इस कोड को ही आईपी एड्रेस (Internet Protocol Address) कहते हैं। आईपी एड्रेस चार भागों में विभजित रहता है। प्रत्येक को डॉट यानि दशमलव के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। “184.106.117.64” यह आईपी एड्रेस का उदाहरण है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं :
- इंटरनेट प्रोटोकाल वर्जन 4 (IPv4): यह 32 बिट का होता है।
- इंटरनेट प्रोटोकाल वर्जन 6 (IPv6): यह 128 बिट का होता है।
- सर्च इंजन (Search Engine): सर्च इंजन एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो विशिष्ट की-वर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं या दस्तावेज़ों को ढूंढ़ता है। कुछ सर्च इंजन: Google, Alta Vista, Yahoo, HotBot, Lycos आदि। यह इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम है। यह हाइपरलिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह है, जिन तक वेब ब्राउजर के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
नागरिक अधिकारों की रक्षा और न्याय को बढ़ावा
जनहित याचिका (Public Interest Litigation या PIL) भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कानूनी तंत्र है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और आम जनता के हितों की रक्षा करना है। यह याचिका उन मामलों में दाखिल की जाती है, जहाँ व्यापक जनहित से संबंधित मुद्दों का समाधान आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य न्यायालय को इस तरह के मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करना है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं या जिन पर सरकार या प्रशासनिक तंत्र का ध्यान नहीं जाता। इसका आधार भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की गारंटी देते हैं।
- संबंधित कानून और अनुच्छेद
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 :
- यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। इसे 'संविधान की आत्मा' कहा जाता है क्योंकि यह न्यायिक उपचार की गारंटी प्रदान करता है।
- जनहित याचिका मुख्यतः अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की जाती है जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और न्यायालय से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 :
- अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को विशेष अधिकार देता है कि वे जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर सकें। उच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय दे सके।
- यह अनुच्छेद राज्य स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जिससे राज्य के विषयों पर जनहित याचिकाएँ दाखिल की जा सकती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) : इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। यह जनहित याचिका की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण मामला था।
- एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) : इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के दायरे को व्यापक किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था व्यापक जनहित के मुद्दों पर याचिका दाखिल कर सकता है, भले ही वह सीधे तौर पर प्रभावित न हो।
- जनहित याचिका की विशेषताएँ
- लोक कल्याण पर ध्यान : जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य उन समस्याओं का समाधान करना है जो समाज के व्यापक हिस्से को प्रभावित करती हैं। यह खासकर उन लोगों के लिये होती है जो अपनी आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं।
- विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं : जनहित याचिका दायर करने के लिये याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर प्रभावित होना आवश्यक नहीं है। यह किसी भी नागरिक या संगठन द्वारा दायर की जा सकती है जो मानता है कि किसी मामले में जनहित को नुकसान हो रहा है।
- व्यापक मुद्दों का दायरा : जनहित याचिका के अंतर्गत अनेक मुद्दे आते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों का उल्लंघन, सरकारी नीति में खामियाँ, गरीबों के अधिकार, और भ्रष्टाचार।
- न्यायालय की भूमिका : जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे सकता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएँ और उन मुद्दों पर ध्यान दें जो जनहित से जुड़े हैं।
- जनहित याचिका का महत्व
- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा : यह याचिका आम लोगों को यह अधिकार देती है कि वे न्यायपालिका के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहरा सकें और जनहित के मुद्दों पर उचित कार्रवाई की मांग कर सकें।
- सामाजिक न्याय : जनहित याचिका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है, खासकर उन वर्गों के लिये जो वंचित और शोषित हैं। यह सामाजिक असमानताओं को कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
- पर्यावरण संरक्षण : पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जनहित याचिका एक प्रभावी माध्यम बन गया है। न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण सरकार और औद्योगिक संस्थाएँ पर्यावरण की रक्षा के लिये अधिक सचेत हो जाती हैं।
जनहित याचिका भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है, जो आम जनता के हितों की रक्षा करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायक है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 पर आधारित है, जो नागरिकों को न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। न्यायालयों के दिशा-निर्देश और उनके द्वारा दिए गए फैसले जनहित याचिका को और भी प्रभावी बनाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है।
- वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web): यह इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम है। यह हाइपरलिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह है, जिन तक वेब ब्राउजर के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
- वेब पेज (Web Page): HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती हैं।
- वेबसाइट (Website): सामान्यत: अंतर्संबंधित वेब पेजों के समूह, जो किसी विषय से संबंधित तथा हाइपर लिंक से जुड़े हुए होते हैं। इसके प्रथम पेज को ‘Home Page’ कहा जाता है।
- वेब ब्राउज़र (Web Browser): यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, पुन: प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है। जैसे- इंटरनेट एक्सप्लोरर (IE), गूगल क्रोम (Google Chrome), सफारी (Safari), ओपेरा (Opera) आदि। यह दो प्रकार का होता है-
- Text Web Browser : यह केवल टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को प्रदर्शित करता है।
- Graphical Web Browser : यह टेक्स्ट तथा ग्राफिकल, दोनों सूचनाओं को प्रदर्शित करता है।
- वेबमर्शियल (Webmercials): नेट पर वाणिज्यिक संदेशों के लिये इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं।
- वेब सर्वर (Web Server): वेब सर्वर, सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो वेब पेज के ज़रिये सूचनाएँ प्रदान (Deliver) करते हैं। वेब सर्वर का अपना IP Address तथा Domain Name होता है। जैसे: Apache HTTP Server, Microsoft IIS, Lightpad, Sunjava, Jigsaw इत्यादि।
- वेब (Web) 2.0 : यह एक ऐसा शब्द है जो वर्ल्ड वाइड वेब (www) तकनीक और वेब डिज़ाइन के उपयोग में बदलते रुझान का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य रचनात्मकता, सुरक्षित जानकारी साझा करना, सहयोग बढ़ाना और वेब की कार्यक्षमता में सुधार करना है। वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगो को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान-प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है।
शिक्षण प्रक्रिया तीन चरणों में विभाजित की जाती है :
- पूर्व-सक्रिय चरण : तैयारी और योजना पर केंद्रित।
- सक्रिय चरण : सामग्री प्रस्तुत करने और संवाद पर केंद्रित।
- पश्च-सक्रिय चरण : मूल्यांकन और सुधार पर केंद्रित।
1. पूर्व-सक्रिय चरण (योजना चरण)
यह चरण शिक्षण प्रक्रिया की तैयारी और योजना बनाने पर केंद्रित होता है ताकि प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- मुख्य गतिविधियाँ :
- उद्देश्य निर्धारित करना :
- स्पष्ट और मापने योग्य शिक्षण लक्ष्यों को परिभाषित करना (संज्ञानात्मक, भावनात्मक, और क्रियात्मक)।
- पाठ योजना बनाना :
- सामग्री को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना और गतिविधियों को अनुक्रमित करना।
- शिक्षण विधियाँ चुनना :
- व्याख्यान, चर्चा, प्रदर्शन जैसी उपयुक्त विधियों का चयन करना।
- संसाधनों की तैयारी :
- शिक्षण सामग्री, उपकरण, और सहायक सामग्री तैयार करना।
- चुनौतियों का पूर्वानुमान :
- संभावित कठिनाइयों की पहचान करना और उन्हें हल करने के उपाय तैयार करना।
- उद्देश्य निर्धारित करना :
2. सक्रिय चरण (कार्यांवयन चरण)
यह शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य चरण है, जहाँ शिक्षक और छात्रों के बीच वास्तविक कक्षा संवाद होता है।
- मुख्य गतिविधियाँ :
- सामग्री प्रस्तुत करना :
- योजना के अनुसार पाठ को प्रस्तुत करना और संसाधनों का उपयोग करना।
- परस्पर संवाद को बढ़ावा देना :
- प्रश्नों, चर्चाओं और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग :
- दृश्य, श्रव्य, या व्यवहारिक सामग्री का उपयोग करके समझ को गहन बनाना।
- प्रगति की निगरानी :
- छात्रों के व्यवहार, ध्यान और अवधारणाओं की समझ को देखना।
- कक्षा प्रबंधन :
- अनुशासन बनाए रखना, समावेशिता सुनिश्चित करना, और सहयोगपूर्ण शिक्षण वातावरण बनाना।
- सामग्री प्रस्तुत करना :
3.पश्च-सक्रिय चरण (मूल्यांकन चरण)
यह चरण शिक्षण प्रक्रिया और इसके परिणामों का मूल्यांकन करने और भविष्य की शिक्षा के लिये सुधार करने पर केंद्रित है।
- मुख्य गतिविधियाँ :
- अधिगम का मूल्यांकन :
- परीक्षण, असाइनमेंट, या गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की समझ का आकलन करना।
- प्रतिक्रिया प्राप्त करना :
- छात्रों से उनके शिक्षण अनुभवों के बारे में जानकारी लेना।
- स्वयं-प्रतिबिंबन :
- शिक्षण विधियों और संवाद की प्रभावशीलता पर विचार करना।
- रिकॉर्ड रखना :
- छात्रों की प्रगति का रिकॉर्ड संजोकर रखना।
- पुनः योजना बनाना :
- प्रतिक्रिया और परिणामों का उपयोग करते हुए भविष्य की पाठ योजनाओं और रणनीतियों को समायोजित करना।
- अधिगम का मूल्यांकन :
ये तीन चरण मिलकर एक सतत, संरचित चक्र बनाते हैं, जो प्रभावी शिक्षण और गहन अधिगम सुनिश्चित करता है।
इंटरनेट शब्द, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में Vint Cerf द्वारा की गई थी, जिन्हें इंटरनेट का पिता माना जाता है। यह आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिये किये गए थे। इंटरनेट पर डाटा का पारेषण (Transmission) TCP/IP द्वारा नियंत्रित होता है। TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) डाटा पैकेट बनाने एवं उन्हें एकत्र करने तथा उनके एड्रेस को निर्धारित करने का कार्य करता है।
- इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार
- एनालॉग या डायल-अप (Analog or Dial-up): यह इंटरनेट कनेक्शन के लिये टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन तथा PC के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। SLP–Serial Line Internet Protocol तथा PPP– Point to Point Protocol, डायल-अप कनेक्शन के प्रोटोकॉल हैं। यह सबसे धीमी गति (अधिकतम 56 kbps) वाला इंटरनेट कनेक्शन है।
- ISDN (Integrated Services Digital Network ): यह कॉपर टेलीफोन वायर पर डिजिटल सिग्नल द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। यह एक साथ डाटा एवं वॉयस कम्युनिकेशन सेवा प्रदान करने में सक्षम है। यह डायल-अप कनेक्शन से 2 से 3 गुना ज़्यादा गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है।
- DSL (Digital Subscriber Line): यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार है, जो इंटरनेट सेवा हेतु साधारण टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। ADSL, SDSL, HDSL, VDSL आदि विभिन्न प्रकार की DSL तकनीक हैं, जिनकी डाटा ट्रांसफर रेट, डाउनलोड एवं अपलोड स्पीड अलग-अलग है।
- केबल टीवी (Cable TV): केबल टीवी लाइन का उपयोग कर सेवा प्रदान की जाती है। केबल टीवी लाइन के रूप में को-एक्सियल केबल का उपयोग होता है, जिस पर डाटा ट्रांसफर रेट, टेलीफोन लाइन से बेहतर होता है।
- वायरलैस (Wireless): रेडियो तरंगों के उपयोग द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। सामान्यत: इसका उपयोग LAN के रूप में किया जाता है।
- Wi-Fi (Wireless Fidelity): WiMAX (WorldWide Interoperability for Microwave Access) आदि कुछ वायरलेस तकनीकें हैं।
- सैटेलाइट (Satellite): सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। सैटेलाइट कनेक्शन दो प्रकार का होता है।
- One Way : सैटेलाइट कनेक्शन से केवल डाटा डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि अपलोड के लिये Dial&-up Access का प्रयोग किया जाता है।
- Two Way: डाउनलोड और अपलोड दोनों में सक्षम।
समावेशी और सतत् विकास की ओर
18-19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा। यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था जिसकी मेज़बानी ब्राजील ने की, और साथ ही यह पहला शिखर सम्मेलन था जिसमें अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो अधिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता की प्रमुख उपलब्धियाँ
ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने अध्यक्षता के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियों को प्रस्तुत किया :- सामाजिक समावेश :
G20 सोशल समिट का आयोजन किया गया, जिससे नागरिक समाज को नीतिगत चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। - महिला सशक्तिकरण :
महिलाओं के लिये एक विशेष कार्य समूह की स्थापना की गई, जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देगा। - एसडीजी (SDG 18) :
जातीय-नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिये नया सतत विकास लक्ष्य जोड़ा गया। - बहुपक्षीय विकास बैंक (MDB) :
इनमें सुधार के लिये एक रोडमैप तैयार किया गया, जिससे विकासशील देशों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। - जलवायु परिवर्तन :
जलवायु असमानताओं को कम करने और प्रभावित समुदायों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- सामाजिक समावेश :
- एजेंडा प्राथमिकताएँ
शिखर सम्मेलन की थीम "न्यायपूर्ण विश्व और संधारणीय ग्रह का निर्माण (Building a Just World and a Sustainable Planet)" के तहत तीन प्रमुख एजेंडा तय किये गए :- भूख और गरीबी उन्मूलन :
"ग्लोबल एलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी" की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य 2030 तक भूख और गरीबी को समाप्त करना है। - ऊर्जा संक्रमण :
2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई गई। - वैश्विक संस्थागत सुधार :
वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की गई ताकि ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके।
- भूख और गरीबी उन्मूलन :
- सुरक्षा और आयोजन की तैयारियाँ
ब्राज़ील सरकार ने शिखर सम्मेलन के लिये $60 मिलियन का बजट निर्धारित किया और 15 शहरों में आयोजनों की व्यवस्था की। 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति पर संभावित आतंकी हमले का अभ्यास भी सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा था। - वैश्विक और क्षेत्रीय संवाद
ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को अध्यक्षता सौंपी। उन्होंने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच एकजुटता पर जोर दिया। प्रमुख मुद्दों में रूस-यूक्रेन संघर्ष, इजराइल-हमास संघर्ष, अमेरिका-चीन तनाव, और वैश्विक तापमान वृद्धि पर चर्चा हुई। - G20 का वैश्विक महत्व
- वैश्विक आर्थिक प्रभाव :
G20 राष्ट्र सामूहिक रूप से विश्व के 85% आर्थिक उत्पादन, 75% निर्यात और 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। - समावेशिता :
अफ्रीकी संघ को शामिल करना एक बड़ा कदम है, जो विकासशील देशों के दृष्टिकोण को मजबूती देगा। - जलवायु परिवर्तन :
G20 सदस्य देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 80% के हिस्सेदार हैं। इनकी नीतियाँ जलवायु परिवर्तन की दिशा तय करती हैं।
शिखर सम्मेलन का समापन ब्राजील द्वारा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, संधारणीयता को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन में समावेशिता को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करते हुए हुआ।
- वैश्विक आर्थिक प्रभाव :
यह भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात् ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है।
- नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार (Types of Network Topology)
- बस टोपोलॉजी (Bus Topology): इसमें एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार का कार्य करती है तथा जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करता है।

- बस टोपोलॉजी (Bus Topology): इसमें एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार का कार्य करती है तथा जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करता है।
- स्टार टोपोलॉजी (Star Topology): इसमें प्रत्येक कंप्यूटर तार के माध्यम से सीधे केंद्रीय हब (HUB) से जुड़ा रहता हैं। केंद्रीय हब नेटवर्क को नियंत्रित करने वाला सर्वर कंप्यूटर या साधारण जोड़ने वाला उपकरण हो सकता है। होस्ट कंप्यूटर के ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है।

- मेश टोपोलॉजी (Mesh Topology): इसमें प्रत्येक नोड(कंप्यूटर) एवं सर्वर एक दूसरे से सीधे जुड़े रहते हैं। प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम होता है। इसमें एक नोड का कनेक्शन बाधित होने से अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- ट्री टोपोलॉजी (Tree Topology): ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस टोपोलॉजी दोनों के गुण होते हैं। जिसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कम्प्यूटर होता है तथा बस टोपोलॉजी की तरह सारे कम्प्यूटर एक ही नेटवर्क तार से जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है जिसमें सबसे ऊपर होस्ट कंप्यूटर होता है।
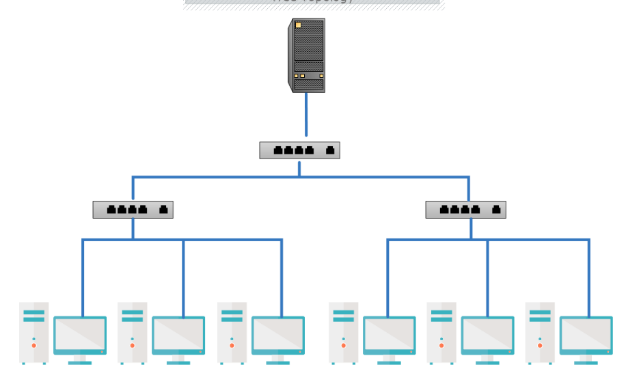
- रिंग टोपोलॉजी (Ring Topology): इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं तथा डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। इसमें एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है तथा सिग्नल के लिये एकल पथ का निर्माण करता है।
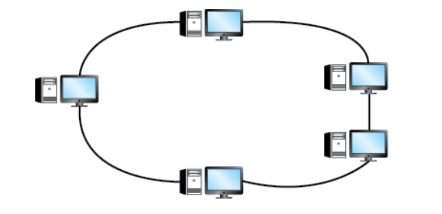
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत ने 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। गणराज्य का अर्थ होता है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इनकी एक संशोधित और संक्षिप्त व्याख्या दी गई है :
- चुनाव और त्यागपत्र :
- राष्ट्रपति का चुनाव गणराज्य की परिभाषा के अनुरूप किया जाता है और वह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं।
- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं।
- उत्तराधिकार :
- राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यभार संभालते हैं।
- राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं।
- कार्यपालिका शक्तियाँ :
- अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
- यह शक्ति संविधान और विधियों के अनुसार ही प्रयोग की जा सकती है।
- राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और यह शक्ति कानूनी सीमाओं के तहत प्रयोग की जाती है।
- क्षमादान और दया याचिका :
- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दंड माफ करने, निलंबित करने, कम करने या समाप्त करने का अधिकार है।
- मृत्युदंड पाए अपराधियों की सजा पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति :
- अनुच्छेद 75 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
- जब किसी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिये स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं।
- राज्यसभा में नामांकन :
- अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिये नामांकित कर सकते हैं।
- आपातकालीन शक्तियाँ :
- अनुच्छेद 352 : युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा।
- अनुच्छेद 356 : राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन।
- अनुच्छेद 360 : वित्तीय आपातकाल की घोषणा।
- अन्य शक्तियाँ :
- अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधिकार हैं, जैसे विधेयक को अपनी सहमति देने से पहले उसे पुनर्विचार के लिये वापस भेजना।
- राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ :
- आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto) : विधेयक को पूरी तरह खारिज करना।
- निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto) : विधेयक पर पुनर्विचार का आग्रह।
- पॉकेट वीटो (Pocket Veto) : विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था।
ये सिग्नल को प्रवर्धित (Amplify) करने तथा डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करते हैं।
प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेज़ (Main Network Devices)
- रिपीटर (Repeater) : रिपीटर का काम वाई-फाई सिग्नल को प्राप्त कर उन्हें फिर से रिजनरेट करना है, ताकि सिग्नल स्ट्रेंथ में वृद्धि की जा सके और वाई-फाई कवरेज एरिया को बढ़ाया जा सके।
- हब (Hub) : कंप्यूटर नेटवर्क में हब एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस है जो नेटवर्क के विभिन्न डिवाइसों को जोड़ने और डेटा सिग्नल को फॉरवर्ड करने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य डेटा पैकेट प्राप्त करना और उन्हें नेटवर्क पर सभी डिवाइसों तक पहुंचाना है।
- गेटवे (Gateway) : एक नेटवर्क गेटवे का उपयोग दो नेटवर्कों के बीच संचार करने के लिये किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल सिस्टम या भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके नेटवर्क को अन्य नेटवर्क या इंटरनेट से डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- स्विच (Switch) : स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग उपकरण है जो की नेटवर्क के विभिन्न उपकरणों(devices) को एक दूसरे के साथ जोड़ता(connect) है, जिससे किसी नेटवर्क के अंदर डाटा का आदान-प्रदान आसानी से किया जा सके।
- ब्रिज (Bridge) : ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग दो "सब-नेटवर्क" को जोड़ने के लिये किया जाता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यह OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर के तहत काम करता है, इसलिये इसे लेयर-2 स्विच कहा जाता है।
- राउटर (Router) : राउटर छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। इसलिये राउटर एक लेयर-3 नेटवर्क गेटवे डिवाइस है
- मॉडेम (Modem) : मॉडेम (modem), modulator-demodulator का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके उसे एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डिमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में प्राप्त करता है।
- इथरनेट कार्ड (Ethernet Card) : इथरनेट कार्ड एक कंप्यूटर को इथरनेट केबल के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है ।
नीति निदेशक तत्त्व राज्य को नैतिक निर्देश हैं, ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। ये तत्त्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही ‘कल्याणकारी राज्य’ का आदर्श भी घोषित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं-
|
अनुच्छेद |
विषय-वस्तु |
|
36 |
नीति निदेशक तत्त्वों के संदर्भ में ‘राज्य’ की परिभाषा। |
|
37 |
विधि निर्माण में नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। |
|
38 |
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना। |
|
39 |
विचारशीलता और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना। इसके अंतर्गत, राज्य को आर्थिक और सामाजिक न्याय की सुनिश्चित करने, गरीबों और असहाय वर्गों के प्रति सामाजिक समर्थन प्रदान करने, और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धि में भागीदार बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिये। |
|
39क |
समान अवसर के आधार पर न्याय देना व नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल) |
|
40 |
ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। |
|
41 |
कुछ दशाओं में विशेषत: बुढ़ापे, बेरोज़गारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। |
|
42 |
कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। |
|
43 |
कर्मकारों को निर्वाह मज़दूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। |
|
43क |
उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिये उपयुक्त विधान बनाना। (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा) |
|
43ख |
सहकारी समितियों का उन्नयन (97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा)। |
|
44 |
नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। |
|
45 |
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल (86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा) |
|
46 |
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। |
|
47 |
लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। |
|
48 |
कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों-बछड़ों व अन्य दुधारु या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये कदम उठाना। |
|
48क |
पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा) |
|
49 |
राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। |
|
50 |
राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। |
|
51 |
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिये प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। (विदेश नीति हेतु आदर्श) |
सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिये आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के आर-पार ट्रांसमिशन के लिये आँकड़ो (Data) को कूटबद्ध करना कोडीकरण (Encryption) कहलाता है।
- कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार (Types of Computer Network)
कंप्यूटर नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार हैं- - LAN (Local Area Network): सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को ‘लोकल एरिया नेटवर्क’ कहते हैं। संस्थानों के अन्तर्गत आंतरिक संचार भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे- घर, स्कूल, ऑफिस आदि तक सीमित नेटवर्क। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक प्रकार है।
- WAN (Wide Area Network): अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को ‘वाइड एरिया नेटवर्क’ कहते हैं। जैसे-संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर स्थापित नेटवर्क। इसमें अनेक संचार माध्यमों, जैसे- टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेब आदि का उपयोग किया जाता है। यह दो या दो से अधिक LAN का संयोजन भी हो सकता है। जैसे:- इंटरनेट (Internet)।
- MAN (Metropolitan Area Network): यह एक मेट्रोपोलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए LAN का नेटवर्क होता है। लेकिन यह WAN की अपेक्षा कम भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है।
- VPN (Virtual Private Network): एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क (जैसे- इंटरनेट) पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इसके लिये टनलिंग प्रोटोकॉल (Tunneling Protocol) का उपयोग होता है।
- 1960 के दशक में US के रक्षा विभाग के लिये प्रथम नेटवर्क अरपानेट ( Advanced Research Projects Agency Network - ARPANET) विकसित किया गया।
जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक संधि
यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है। यह छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों - कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), पर्फ्लोरोकार्बन (PFCs), और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆) पर लागू होती है। यह 1992 में हुए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) का विस्तार है, जो "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" (CBDR) के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें देशों की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा गया है।
- महत्त्वपूर्ण तथ्य
- यह संधि UNFCCC के तीसरे सम्मलेन में 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में इसे स्वीकार किया गया।
- यह क़ानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ।
- इसमें कुल 84 हस्ताक्षरकर्ताऔर 192 पक्ष हैं। हालाँकि, अमेरिका, कनाडा (2012 में वापस) और दक्षिण सूडान जैसे देश इसमें शामिल नहीं हैं।
- प्रतिबद्धता अवधि
- प्रथम प्रतिबद्धता अवधि (2008-2012) :
- 36 विकसित देशों ने अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्यों का पालन किया।
- लचीला तंत्र : नौ देशों ने उत्सर्जन व्यापार और अन्य देशों में कमी पर वित्तीय प्रोत्साहन जैसे तंत्रों का उपयोग किया।
- परिणाम : इन देशों ने उत्सर्जन कम किया, लेकिन कुल वैश्विक उत्सर्जन 1990 से 2010 के बीच 32% तक बढ़ा, जिसमें 2007-08 की वित्तीय मंदी का भी प्रभाव था।
- द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि (2012-2020) :
- दोहा संशोधन (2012) : नए उत्सर्जन लक्ष्य तय किये गए, जिन्हें लागू करने के लिये 144 देशों की स्वीकृति की आवश्यकता थी। 2020 तक इस संख्या को प्राप्त कर लिया गया, जिसमें भारत 80वाँ देश था जिसने संशोधन पर सहमति प्रदान की।
- बाध्यकारी लक्ष्य वाले देश : 37 देश, जिनमें से केवल 7 ने दोहा संशोधन की पुष्टि की है।
- प्रथम प्रतिबद्धता अवधि (2008-2012) :
- संरचना और अनुपालन
- कानूनी रूप से बाध्यकारी : केवल UNFCCC सदस्य ही इसका हिस्सा बन सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग व विमानन से होने वाले उत्सर्जन इसमें शामिल नहीं हैं।
- भूमि उपयोग, भूमि-उपयोग परिवर्तन और वानिकी (LULUCF) : देशों को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिये LULUCF गतिविधियों का उपयोग करने की अनुमति है।
- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)
- क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की औपचारिक बैठक जिसमें प्रगति की समीक्षा की जाती है और कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है।
- भारत की भूमिका और भागीदारी
- क्योटो प्रोटोकॉल : भारत पर बाध्यकारी उत्सर्जन प्रतिबद्धताएँ नहीं थीं, लेकिन उसने विकासशील और विकसित देशों के बीच विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत का समर्थन किया।
- दोहा संशोधन : भारत ने इस संशोधन की पुष्टि की, जोकि 2012-2020 की अवधि के लिये उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने पर केंद्रित है।
क्योटो प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सीमाओं के बावजूद, इसने आगे की संधियों, जैसे पेरिस समझौते, के लिये आधार तैयार किया और वैश्विक जलवायु नीतियों को प्रभावित करना जारी रखा।
- संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में 6 मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग III को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है।
- ‘मैग्नाकार्टा' का तात्पर्य है अधिकारों का वह प्रपत्र जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था।
|
अनुच्छेद |
प्रावधान |
|
|
12. |
|
राज्य की परिभाषा (भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी) |
|
13. |
|
मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ |
|
14. |
समानता का अधिकार |
विधि के समक्ष समानता (विधि का शासन) |
|
15. |
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध |
|
|
16. |
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता |
|
|
17. |
अस्पृश्यता का अंत |
|
|
18. |
उपाधियों का अंत |
|
|
19. |
स्वतंत्रता का अधिकार |
वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताअनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के छह अधिकारों की गारंटी देता है:
|
|
20. |
अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
|
|
21. |
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |
|
|
21क |
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया) |
|
|
22. |
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
|
|
23.
|
शोषण के विरुद्ध अधिकार |
मानव के बलात् श्रम (बेगार) व दुर्व्यापार का प्रतिषेध |
|
24. |
कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध |
|
|
25. |
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार |
अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता |
|
26. |
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता |
|
|
27. |
किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता |
|
|
28. |
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता |
|
|
29. |
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार |
अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार |
|
30. |
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार |
|
|
31. |
निरसित |
संपत्ति का अनिवार्य अर्जन (44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद-300क के तहत अब यह एक कानूनी अधिकार है।) |
|
32. |
संवैधानिक उपचारों का अधिकार |
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये उपचार |
|
33. |
सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। |
|
|
34. |
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। |
|
|
35. |
इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये विधान। |
|
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)
- डॉ. बी.आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है।
- अनुच्छेद-32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये एक प्रत्याभूत (Guaranteed) उपचार प्रदान करता है। यह उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है, क्योंकि यह भाग तीन में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूति दाता बनाया गया है।
- यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा।
भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में उस समय शुरू हुआ, जब 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर ‘क्रे-एक्स’ देने से मना कर दिया। भारत में कई संस्थाओं, जैसे- BARC, DRDO, National Aerospace Lab (NAL), C- DOT (Centre for Development of Telematics), C- DAC (Centre for Development of Advanced Computing) ने सुपर कंप्यूटरों के विकास में महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है। पुणे में वर्ष 1988 में सी-डैक (C-DAC) की स्थापना सुपर कंप्यूटरों के निर्माण हेतु की गई थी। सी-डैक, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना तकनीकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत आने वाला मुख्य अनुसंधान तथा विकास(R & D) संगठन है।
|
वर्ष |
सुपर कंप्यूटर का नाम |
कंप्यूटिंग पॉवर |
|
1991 |
PARAM 8000 |
भारत का पहला गीगा स्तर का सुपर कंप्यूटर |
|
1998 |
PARAM 10000 |
100 गीगाफ्लॉप्स क्षमता का सुपर कंप्यूटर |
|
2002 |
PARAM Padma |
1 टेराफ्लॉप्स क्षमता का भारतीय सुपर कंप्यूटर, जो विश्व के 500 शीर्ष सुपर कंप्यूटरों की सूची में शामिल (जून 2003 में जारी रैंक में 171वाँ स्थान) |
|
2008 |
PARAM Yuva |
54 टेराफ्लॉप्स क्षमता का सुपर कंप्यूटर |
|
2013 |
PARAM Yuva 2 |
529 टेराफ्लॉप्स (कुछ स्रोतों में 524 टेराफ्लॉक्स) की क्षमता |
|
2014 |
PARAM Bio-Blaze |
बायोइंफार्मेटिक्स की चुनौतियों से निपटने के लिये सुपर कंप्यूटर, जिसकी पीक कंम्प्यूटिंग पावर 10.65 TF है। |
|
2016 |
PARAM ISHAN 250 |
250 टेराफ्लॉप्स, IIT गुवाहाटी में शोध कार्यों हेतु |
|
2017 |
SahasraT |
देश का पहला पेटाफ्लॉप्स सुपरकंप्यूटर |
|
2018 |
Pratyush |
देश का प्रथम मल्टीपेटाफ्लॉप्स श्रेणी का कंप्यूटर |
|
2020 |
PARAM Siddhi |
6.5 पेटाफ्लॉप्स (Peak DP) की गति से गणना करने में सक्षम |
|
2023 |
AIRAWAT |
13.17 पेटाफ्लॉप की गति के साथ दुनिया के सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में ऐरावत 75वें नंबर पर है । |
|
2024 |
PARAM Rudra |
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत, 5 पेटाफ्लॉप्स से अधिक की कम्प्यूटिंग गति वाले ये तीन सुपरकंप्यूटर पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किये गए हैं। |
|
विश्व के शीर्ष दस सुपर कंप्यूटर |
||
|
नाम |
गति (पेटाफ्लॉप्स में) |
देश |
|
Frontier |
1194 |
यू.एस.ए. |
|
Fugaku |
442 |
जापान |
|
LUMI |
309.1 |
फिनलैंड |
|
Leonardo |
238.7 |
इटली |
|
Summit |
148.6 |
यू.एस.ए. |
|
Sierra |
94.6 |
यू.एस.ए |
|
Sunway Taihu Light |
93.01 |
चीन |
|
Perlmutter |
70.87 |
यू.एस.ए. |
|
Selene |
63.46 |
यू.एस.ए. |
|
Tianhe-2A |
61.44 |
चीन |
नोट : 2024 की स्थिति के अनुसार
- डाटा संप्रेषण (Data Communication) :
दो या अधिक उपकरणों के मध्य किसी भी संचार माध्यम द्वारा डाटा या सूचना का आदान-प्रदान, ‘डाटा संप्रेषण’ कहलाता है। डाटा संप्रेषण विभिन्न प्रकार के सिग्नल (Digital Signal, Analog Signal, Hybrid Signal) के माध्यम से होता है। - संप्रेषण चैनल (Communication Channel) : यह सिग्नल प्रवाह की दिशा बताता है। ये निम्न हैं :
- Simplex Channel: इसमें सूचना का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है।
- Half Duplex Channel: इसमें सूचना प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन अलग-अलग समय पर।
- Full Duplex Channel: इसमें सूचना का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ एक ही समय पर संभव है।
- संप्रेषण माध्यम (Communication Media) : डाटा या सूचना के आदान-प्रदान का साधन ‘संप्रेषण माध्यम’ कहलाता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है-
- निर्देशित (Guided) : जब संप्रेषण केबल द्वारा होता है तो उसे निर्देशित संप्रेषण कहते हैं। इथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल, को-एक्सियल केबल तथा फाइबर ऑप्टिक केबल आदि इसके प्रमुख साधन हैं।
- अनिर्देशित (Unguided) : जब संप्रेषण तरंगों (Waves) द्वारा होता है तो उसे अनिर्देशित संप्रेषण कहते हैं। रेडियो वेब, माइक्रो वेब, इंप्रारेड वेब संप्रेषण, सैटेलाइट संप्रेषण तथा ब्लूटूथ आदि इसके प्रमुख साधन हैं।
भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। संसद ने सर्वप्रथम 1955 में ‘नागरिकता अधिनियम’ (Citizenship Act) पारित किया, जिसमें (1986, 1992, 2003, 2005, 2015) प्रासंगिक संशोधन किये गए हैं।
- नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद -
- अनुच्छेद 5- संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता
- अनुच्छेद 6- पाकिस्तान से प्रव्रजन (Migration) करके आए व्यक्तियों की नागरिकता
- अनुच्छेद 7- पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार
- अनुच्छेद 8- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता
- अनुच्छेद 9- किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाएगी।
- अनुच्छेद-10- किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है।
- अनुच्छेद-11- नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3-7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के पाँच तरीके हैं-
- जन्म,
- वंश,
- पंजीकरण,
- देशीयकरण (दीर्घावधिक निवास) के माध्यम से।
- किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह विनिर्दिष्ट करेगी कि उस भू-भाग के कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8, 9 तथा 10 में नागरिकता समाप्ति की तीन स्थितियाँ बताई गई हैं-
- नागरिकता का परित्याग करने पर,
- किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर
- भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना।
- विदेशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के लोग -
- अनिवासी भारतीय (NRI): अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं; किंतु ये नौकरी या व्यवसाय के लिये साधारणत: भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएँ मिलती हैं। इन्हें मताधिकार का भी अधिकार है।
- भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO): ये भारत के नागरिक नहीं होते। ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं, किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। भारत में कम-से-कम 7 वर्षों तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हें भी NRI कोटा में शिक्षा का अधिकार है तथा भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में खाता खोलने का अधिकार है।
- ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI): ये विदेशी नागरिक होते हैं तथा साधारणत: इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवनपर्यंत वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्रा की अवधि चाहे जितनी लंबी हो, इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिकता के लिये 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम-से-कम 1 साल से भारत में रह रहा हो। इन्हें NRI कोटा में शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता भी खोल सकते हैं।
- 9 जनवरी, 2015 की अधिसूचना (भारत का राजपत्र) के द्वारा PIO तथा OCI कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है तथा अब सभी PIO कार्डों को OCI कार्डों का दर्जा प्राप्त होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का सेट होता है, जो उपयोगकर्त्ता तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वयकर्त्ता, नियंत्रक तथा निरीक्षक का कार्य करता है। अत: यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है।
- ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार :
- सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम: MS.DOS, Windows 9x, Mac OS, MS Window, Palm OS आदि।
- मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम: UNIX, LINUX, Windows 2000, Solaris आदि।
- मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम: UNIX, LINUX, Windows 95 आदि।
- रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम: LynxOS, RTLinux आदि।
- मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम: एंड्रॉयड (Andriod) (Google – 2007), सिंबियन (Symbian) (Symbian Ltd), IOS (Apple Corporation) आदि।
- ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य :
- प्रोसेस मैनेजमेंट (Process Management)
- मेमोरी मैनेजमेंट (Memory Management)
- फाइल मैनेजमेंट (File Management)
- इनपुट/आउटपुट मैनेजमेंट (Input/Output Management)
- यूज़र इंटरफेस (User Interface):
यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो उपयोगकर्त्ता की विभिन्न एप्लीकेशनों तक पहुँच तथा संप्रेषण(Communication) को संभव बनाता है।- ग्राफिकल यूजर इंटरफेस(Graphical User Interface– GUI) : इसमें संकेत (Symbols) दृश्य रूपकों (Visual Metaphors) तथा प्वाइंटिंग डिवाइस का उपयोग होता है।
- कैरेक्टर यूजर इंटरफेस (Character User Interface– CUI) : इसमें कमांड का उपयोग होता है। डीबग, डिस्कपार्ट, पिंग आदि CUI के अनुप्रयोग हैं।
मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है। हालाँकि भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है, जो निम्नलिखित हैं-
- ब्रिटेन - संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक व्यवस्था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका - मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका का विचार
- कनाडा - एक सशक्त केंद्र के साथ अर्द्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति विभाजन (संघ एवं राज्य के बीच), राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन।
- आयरलैंड - राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाजसेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया
- द. अफ्रीका - संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया
- फ्राँस - स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, गणतंत्रात्मक व्यवस्था
- ऑस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता
- जर्मनी (वाइमर संविधान) - आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन
- जापान - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
- पूर्व सोवियत संघ - मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श
संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम, 1935 से अधिगृहीत है। जैसे न्यायपालिका, कैग, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध आदि।
कंप्यूटर के मुख्यत: दो भाग होते हैं- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर,
- हार्डवेयर (Hardware): कंप्यूटर के लिये आवश्यक एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाले सभी भौतिक हिस्से ‘हार्डवेयर’ कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं-
- इनपुट डिवाइस (Input Device) : ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं। इनके माध्यम से उपयोगकर्त्ता कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकता है तथा उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण- की-बोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टचस्क्रीन, वेब कैम, ज्वॉयस्टीक, ट्रैक बाल, ओसीआर रीडर, बार कोड रीडर, माइकर, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड रीडर एवं बायोमेट्रिक सेंसर आदि।
- आउटपुट डिवाइस (Output Device) : ऐसे पेरिपेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसे प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण- मॉनीटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, एसजीडी (Speech Generating Device), जीपीएस डिवाइस (Global Positioning System), साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर आदि।
- स्टोरेज डिवाइस (Storage Device) : ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो जानकारी या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जैसे- हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, यूएसबी स्टिक, डीवीडी ड्राइव, ब्लू रे ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज़, पेनड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आदि।
- कम्युनिकेशन डिवाइस (Communication Device) : ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं। जैसे:- NIC (Network Interface Card) एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिये कंप्यूटर में लगा होता है।
- WNIC (Wireless Network Interface Controller) : यह वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है।
- मॉडेम (Modem) : एक संचार उपकरण जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है।
- हब (Hub) : यह एक नेटवर्क डिवाइस है, जो लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) को इंटरनेट से जोड़ता है। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है।
- वायरलेस एक्सेस प्वाइंट (Wireless Access Point) : यह भी लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) को इंटरनेट से बिना तार (Wireless) जोड़ता है।
- राउटर (Router) : यह एक डिवाइस है, जो नेटवर्क पर डाटा पैकेटों को अग्रेषित करता है।
- इंफ्रारेड (Infrared-IR) : बेतार संचार उपकरण जो निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटरों को संचार हेतु सक्षम बनाता है
- ब्लूटूथ (Bluetooth) : लघु तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंगों का उपयोग कर यह पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटरों को संचार में सक्षम बनाता है।
- वाई-फाई (Wi-Fi) : यह बेतार संचार द्वारा कंप्यूटरों को इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम बनाता है।
- प्रिंटर(Printer): ये समान्यतः दो प्रकार हैं-
- इंपैक्ट प्रिंटर(Impact Printer): ये हैमर या पिन द्वारा स्याही युक्त रिबन को दबाकर कागज़ पर अक्षरों को प्रिंट करते हैं। जैसे:- डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी-व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर तथा चेन प्रिंटर आदि।
- नॉन-इंपैक्ट प्रिंटर (Non–Impact Printer): ये हैमर या पिन का उपयोग किये बिना अक्षरों/चित्रों को प्रिंट करते हैं। जैसे:- इंक-जेट प्रिंटर: इसमें इलेक्ट्रिक फिल्ड, चार्ज इंक पार्टिकल को कैरेक्टर्स में अरेंज कर देती है। लेजर प्रिंटर: यह लेजर बीम, मिरर तथा ड्रम के माध्यम से प्रिंट करता है। इसकी प्रिटिंग स्पीड अधिक होती है।
- प्रोसेसिंग डिवाइस (Processing Device) : कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग जो इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जैसे:-
- सीपीयू (CPU- Central Processing Unit) : यह कंप्यूटर को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलने वाले निर्देशों का संचालन करता है। इसे कंप्यूटर का ‘मस्तिष्क’ कहते हैं।
- जीपीयू (GPU - Graphics Processing Unit) : यह एक कंप्यूटर चिप है, जो प्रतिकृति प्रतिपादन हेतु तेज़ी से गणितीय गणना करता है।
- मदरबोर्ड (Motherboard) : मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) है, जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। यह सीपीयू, रैम तथा अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार के लिये परिपथ प्रदान करता है। इसके सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते है।
- साउंड कार्ड (Sound Card) : यह एक विस्तार कार्ड (Expansion Card) है, जो कंप्यूटर को ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।
- सॉफ्टवेयर (Software): कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिये जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिये तैयार किये गए इन प्रोग्रामों के समूह को ही ‘सॉफ्टवेयर’ कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं :
- सिस्टम सॉफ्टवेयर (System Software): ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है, जिनका कार्य सिस्टम अर्थात् कंप्यूटर को चलाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि इसके उदाहरण हैं।
- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software): इन्हें किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रोग्राम किया जाता है। भिन्न-भिन्न अनुप्रयोगों के लिये भिन्न-भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एडोब फ़ोटोशॉप,एक्सेल, गूगल क्रोम, व्हाट्सएप आदि इसके उदाहरण हैं।
डाटा निरूपण (Data Representation): कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर (0, 1) को ही समझता है। अत: सभी प्रकार के डाटा(टेक्स्ट, इमेज, गणितीय संख्या या कोई चिन्ह आदि) का 0 एवं 1 के रूप में निरूपण ‘डाटा निरूपण’ कहलाता है। डाटा भंडारण के अधिक्रम में बिट्स, बाइट्स, फील्डस रिकार्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेसेज शामिल रहते हैं।
- नंबर सिस्टम (Number System): अंकों (Values) का समूह जिसका उपयोग संख्याओं को व्यक्त करने के लिये किया जाता है, ‘नंबर सिस्टम’ कहलाता है।
|
Number System |
Base |
Digits |
|
Binary |
2 |
0, 1 |
|
Octal |
8 |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|
Decimal |
10 |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|
Hexadecimal |
16 |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F |
- कैरेक्टर संकेतन तकनीक (Character Encoding Technique): कंप्यूटर में किसी अक्षर (Character), वर्ण, अंक या प्रतीक चिह्नों को 0 या 1 के यूनिक कोड (Unique Code) के स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे ‘कंप्यूटर कोड’ कहते हैं।
- BCD (Binary Coded Decimal) : इसमें चार बिट्, एक डेसीमल डिजिट को निरूपित करता है। इसमें डेसीमल डिज़िट को बाइनरी डिजिट में निरूपित किया जाता है।
- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) : यह कंप्यूटर में और इंटरनेट पर टेक्स्ट फाइलों के लिये सबसे सामान्य प्रारूप है। यह सूचना के अंतर्विनिमय के लिये अमरीकी मानक कोड है।
- एक ASCII फाइल में प्रत्येक अल्फाबेटिक न्यूमेरिक या विशेष कैरेक्टर को 7 बिट् या 8 बिट् के बाइनरी नंबर द्वारा निरूपित किया जाता है। क्रमश: इस प्रकार 128 कैरेक्टर तथा 256 कैरेक्टर परिभाषित किये गए हैं।
- UNIX और DOS, ASCII का उपयोग टेक्स्ट फाइल के लिये करते हैं।
- यूनिकोड (Unicode): यह एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ण संकेतन मानक है जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों, डिवाइसों, एप्लीकेशनों या विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं में किसी अक्षर को निरूपित करने के लिये एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है। यह डाटा निरूपण के लिये 8, 16 या 32 बिट का प्रयोग करता है।
हिंदी भाषा के प्रचार - प्रसार तथा अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से 1 मार्च , 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय (Central Directorate of Hindi) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो चेन्नई , हैदराबाद , गुवाहाटी , कोलकाता में स्थित हैं।
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities) की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी।
- एजुसैट ( शिक्षा उपग्रह ) का प्रक्षेपण 20 सितंबर , 2004 को किया गया।
- ज्ञान गरिमा सिंधु मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित एक त्रैमासिक पत्रिका है।
- केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह ( लद्दाख ) में अवस्थित है।
- इंजीनियरिंग में मूल्य शिक्षा देने हेतु आई . आई . टी . दिल्ली में राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है।
- भारत का प्रथम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा।
- पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल ( मध्य प्रदेश ) में हैं।
- केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- पूर्वी क्षेत्र - भुवनेश्वर ( उड़ीसा )
- पश्चिमी क्षेत्र - पुणे ( महाराष्ट्र )
- उत्तरी क्षेत्र - पटियाला ( पंजाब )
- दक्षिण क्षेत्र - मैसूर ( कर्नाटक )
- उ . पूर्वी क्षेत्र - गुवाहाटी ( असम )
- केंद्रीय हिंदी संस्थान ( आगरा ) के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं - दिल्ली , हैदराबाद , गुवाहाटी , शिलॉन्ग , मैसूर , दीमापुर , भुवनेश्वर , अहमदाबाद।
- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (NITTTR) के देश में चार केंद्र हैं - चेन्नई , भोपाल , कोलकाता और चंडीगढ़ हैं।
- केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी।
|
अनुसंधान संस्थान का नाम |
अनुसंधान कार्य क्षेत्र |
स्थापना वर्ष |
मुख्यालय |
|
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (ICHR) |
ऐतिहासिक शोध कार्यों की समीक्षा करना और इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना |
1972 |
नई दिल्ली |
|
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (ICPR) |
दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा (Promote) देना। |
1977 |
दिल्ली व लखनऊ दोनों स्थानों पर |
|
भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद् (IIAS) |
यह मानविकी, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शोध के लिये आवासीय सुविधायुक्त केंद्र है। |
1965 |
शिमला |
|
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR) |
सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के उन्नयन और समन्वय का कार्य करता है। |
1969 |
नई दिल्ली |
|
राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् (NCRI) |
गांधीवादी दर्शन के अनुसार ग्रामीणों क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना |
1995 |
हैदराबाद
|
- उच्चतर शिक्षा से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण केंद्र
- भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (Indian Institute of Advanced Study) – शिमला
- डॉ. ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज - दिल्ली
- श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ - नई दिल्ली
- राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ - तिरुपति (आंध्र प्रदेश)
- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान - नई दिल्ली
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration- NUEPA) - नई दिल्ली
कंप्यूटर मेमोरी, मानव मस्तिष्क की तरह, प्रोसेसिंग के लिये आवश्यक डाटा, सूचना और निर्देशों के भंडार के रूप में कार्य करती है। यह एक भंडारण इकाई या उपकरण के रूप में कार्य करता है जहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों को अस्थायी रूप से रखा जा सकता है।
विभिन्न प्रकार की मेमोरी मौजूद हैं, सेमीकंडक्टर-आधारित मेमोरी के साथ, विशेष रूप से मेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (एमओएस) ट्रांजिस्टर के साथ एकीकृत सर्किट प्रमुख हैं। कंप्यूटर मेमोरी को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
- प्राथमिक मेमोरी: इसे मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, यह कंप्यूटर संचालन के दौरान डेटा और प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहीत करता है। यह सेमीकंडक्टर तकनीक का उपयोग करता है, जिसे अक्सर सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM) और रीड ओनली मेमोरी (ROM) में विभाजित है।
- रैम (RAM: Random Access Memory):
- यह अस्थायी(Non-volatile) मेमोरी है जो बिजली आपूर्ति के आधार पर जानकारी संग्रहीत करती है।
- स्टेटिक रैम (S RAM) और डायनामिक रैम (D RAM) इसके प्रमुख प्रकार हैं।
- S RAM में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है।
- D RAM में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, तथा इसकी गति S RAM की तुलना में कम है।
- रोम (ROM: Read Only Memory):
- यह स्थायी(volatile) मेमोरी है जिसका उपयोग सिस्टम ऑपरेशन से संबंधित सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिये किया जाता है।
- MROM, PROM, EPROM और EEPROM आदि इसके प्रमुख प्रकार हैं।
- द्वितीयक मेमोरी(Secondary Memory): द्वितीयक मेमोरी को सहायक या बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, यह स्थायी मेमोरी है तथा इसमे बहुत अधिक मात्रा में स्थायी रूप से डेटा संग्रहीत होता है। यह प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमी है तथा सीपीयू इसे अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य मेमोरी के माध्यम से एक्सेस करता है। चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आदि इसके प्रमुख प्रकार हैं।
- कैश मेमोरी(Cache Memory): यह एक हाई-स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यह सीपीयू के तेज संचालन के लिये अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को संग्रहीत करता है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय में एक्सेसबल है । किंतु यह सेमीकंडक्टर के उपयोग के कारण महँगा है तथा इसकी भंडारण क्षमता सीमित है।
संक्षेप में, कंप्यूटर मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग के लिये एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न कार्यात्मकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।
शिक्षा आयोग (1964–66) की अनुशंसा पर वर्ष 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का गठन गैर-वैधानिक संस्था के रूप में किया गया। शुरुआती चरण में इसका मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा से जुडे़ सभी मामलों पर सलाह देना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और कार्य योजना (1992) की अनुशंसा के आधार पर एन.सी.टी.ई. को स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने की बात कही गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक वैधानिक संस्था के रूप में ‘‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993’’ के अनुसरण से 17 अगस्त, 1995 से अस्तित्व में आया।
उद्देश्य :
NCTE का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना और इससे संबंधित मामलों हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण करना है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की चार क्षेत्रीय समिति हैं, जो 6 जनवरी, 1996 से अस्तित्व में हैं-
- पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर (ओडिशा)
- पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल (मध्य प्रदेश)
- उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर (राजस्थान)
- दक्षिण क्षेत्रीय समिति, बंगलूरू (कर्नाटक)
नोट: एन.सी.ई.आर.टी. का अध्यापक शिक्षा विभाग नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) के अकादमिक सचिवालय की तरह कार्य करता है।
कंप्यूटर के मुख्यत: तीन अवयव (Component) होते हैं :
- इनपुट/आउटपुट (I/O) यूनिट: इनपुट यूनिट, कोडेड डाटा को प्रोसेसर को भेजता है तथा आउटपुट यूनिट, प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को उपलब्ध कराता है।
- सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU): यह कंप्यूटर का मस्तिष्क (Brain) होता है, इसे ‘प्रोसेसर’ या ‘माइक्रोप्रोसेसर’ भी कहते हैं। इसका कार्य दिये गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा को प्रोसेस करना है। इस क्रम में यह डाटा पर गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्यों को नियंत्रित भी करता है। इसकी गति को MIPS (Million Instruction Per Second) में मापा जाता है। इसके मुख्यत: तीन भाग होते हैं :
- एएलयू (ALU-Arithmetic Logic Unit): यह गणितीय (Mathematical) तथा तार्किक (Logical) ऑपरेशन संचालित करता है।
- सीयू (CU-Control Unit): यह माइक्रोप्रोसेसर में निहित निर्देश समूहों को लागू करता है। यह मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त कर उन्हें डीकोड करता है तथा निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन एवं ज़रूरत पड़ने पर एएलयू को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भेजता है।
- रजिस्टर्स/मेमोरी यूनिट : ये प्रोसेसर में अस्थायी डाटा स्टोरेज़ एरिया होते हैं, जो प्रोसेस होने वाले डाटा को सँभालने का कार्य करते हैं। यही डाटा कंट्रोल यूनिट द्वारा आगे उपयोग किया जाता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने के साथ ही पुराना डाटा समाप्त होता जाता है।
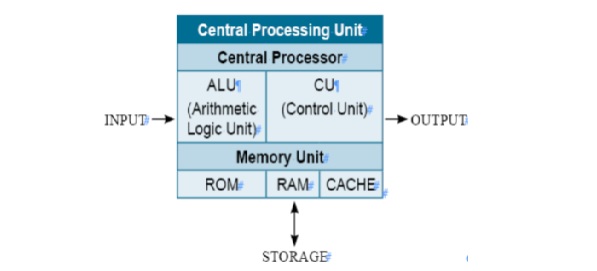
- मेमोरी यूनिट (Memory Unit): मेमोरी, कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज़ एरिया होता है, जो डाटा तथा निर्देशों को स्टोर करता है।
- केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान(Central Institute of Educational Technology)
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना एन.सी.ई.आर.टी. की संवैधानिक इकाई के रूप में वर्ष 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्थान का कार्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी और जनसंचार माध्यमों का विकास करना है। यह संस्थान शैक्षिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों और प्रतिफलों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु शैक्षिक अवसरों का विस्तार करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक तकनीकी को रेडियो, टी.वी फिल्म स्ट्रिप, उपग्रह संचार (INSAT) और साइबर मीडिया के माध्यम से बढ़ावा देना है। टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण INSAT के माध्यम से यही संस्था करती है। - क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान(Regional Institute of Education): यह एन.सी.ई.आर.टी. के अधीन एक संवैधानिक इकाई है। देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कार्यरत हैं-
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (राजस्थान)
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर (ओडिशा)
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर (कनार्टक)
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलॉन्ग (मेघालय)
- पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान: यह संस्थान भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित है। यह संस्थान औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर कार्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान
NCERT द्वारा स्थापित यह एक शोध संगठन है, जो समय-समय पर शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं शिक्षा क्षेत्र के प्रशासकों के लिये प्रशिक्षण व्यवस्था, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। इस संस्थान के विभाग, अनुभाग एवं प्रकोष्ठ निम्नलिखित हैं :
- राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभाग (Departments of National Education Institute)
- कला एवं सौंदर्यबोध शिक्षा विभाग (Department of Education in Arts and Aesthetics- DEAA )
- प्रारंभिक शिक्षा विभाग (Department of Elementary Education-DEE)
- विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (Department of Education of Group with Special Needs- DEGSN)
- शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा आधार विभाग (Department of Educational Psychology and Foundation of Education- DEPFE)
- विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग (Department of Education in Science and Mathematics–DESM)
- सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग (Department of Education in Social Science–DESS)
- भाषा शिक्षा विभाग (Department of Education in Language-DEL)
- जेंडर अध्ययन विभाग (Department of Gender Studies- DGS)
- अध्यापक शिक्षा विभाग (Department of Teacher Education- DTE)
- शिक्षा संस्थान के अनुभाग/प्रभाग (Section/Division of Education Institute)
- प्रकाशन प्रभाग (Publication Divisions)
- पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग (Library and Documentation Division- LDD)
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग (International Relation Division–IRD)
- योजना एवं अनुवीक्षण प्रभाग (Planning and Monitoring Division- PMD)
- शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग (Division of Educational Research–DER)
- शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग (Educational Survey Division–ESD)
- शैक्षिक किट प्रभाग (Division of Educational Kits–DEK)
- राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रकोष्ठ (Cell of National Education Institute)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान परियोजना प्रकोष्ठ (RMSA Project Cell)
- हिंदी प्रकोष्ठ (Hindi Cell)
- जनसंपर्क प्रकोष्ठ (Public Relation Cell)
शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति
यह एन.सी.ई.आर.टी. की एक स्थायी समिति है। यह समिति विद्यालयी और अध्यापक शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा और सहायता देने के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इस समिति के सदस्यों में विश्व विद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के शिक्षा तथा संबद्ध विषयों में कार्यरत प्रसिद्ध अनुसंधानकर्त्ता और एसआईई/एससीईआरटी (SCERT) इत्यादि संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं।
इस समिति के द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :
- शिक्षक और शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना
- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण (कक्षा 1 से 12 तक)
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन
- शैक्षिक सर्वे रिपोर्ट का प्रकाशन
- व्यावसायिक कार्यक्रम
- विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में नवाचार प्रयोग
- राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम
- स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा
- कंप्यूटर शिक्षा
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (NCF), पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री का निर्माण।
- शिक्षा मंत्रालय की स्कूल स्तरीय शैक्षिक नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग एवं परामर्श देना।
- मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ-साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाना।
- राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले प्रक्रम के रूप में कार्य करना।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्(National Council of Educational Research and Training- NCERT) :
शैक्षिक अनुसंधान के विकास तथा उसके प्रचार-प्रसार में सहयोग एवं प्रशिक्षण देने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी) का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860) के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया। वर्तमान में यह परिषद् शिक्षा मंत्रालय की तकनीकी इकाई या संस्था के रूप में कार्य करती है। इस परिषद् का वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
यह परिषद् स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने और उन्हें सुझाव देने के लिये एक शीर्ष संसाधन संगठन है। यह स्कूल शिक्षा में गुणवत्तायुक्त सुधार के लिये शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सूचना के प्रकाशन और प्रसार से संबंधित कार्यक्रम चलाता है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का संचालन एवं शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन एक कार्यकारिणी समिति (Executive Council) के द्वारा किया जाता है। समिति का विवरण निम्नलिखित रूप में है :
एन.सी.ई.आर.टी. की कार्यकारिणी समिति (Executive Council of NCERT)
- केद्रीय शिक्षा मंत्री (अध्यक्ष)
- केंद्रीय शिक्षा सचिव
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष
- एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक
- एन.सी.ई.आर.टी. के संयुक्त निदेशक
- शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
- वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
- दो प्राध्यापक सदस्य
- एन.सी.ई.आर.टी. संकाय के तीन सदस्य
- दो प्रख्यात शिक्षाविद् सदस्य
नोट: कार्यकारिणी समिति (Executive Council) एन.सी.ई.आर.टी के कार्यों से संबंधित मामलों का निर्णय लेती है।
- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘सकल नामांकन अनुपात’ (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम को ‘मल्टीपल एंट्री-एक्जिट’ से लचीला बनाने का प्रयास किया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में विद्यार्थी कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट को अंतिम रूप दिया जा सके।
- उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।
- भारत उच्चतर शिक्षा आयोग : चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्चतर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India-HECI) का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-
- विनियमन हेतु : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council-NHERC)
- मानक निर्धारण : सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council-GEC)
- वित्तपोषण : उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)
- प्रत्यायन : राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC)
महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी।देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के ‘बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय’ (Multidisciplinary Education and Research Universities) की स्थापना की जाएगी।
- अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (All India Council of Secondary Education):
- अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना में माध्यमिक शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। इसके अंतर्गत दो विभाग थे- 1. सलाहकार विभाग, 2. प्रशासकीय विभाग
- वर्ष 1958 में परिषद् का पुनर्गठन करके इसके प्रशासकीय विभाग को एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया आगे चलकर यही स्वतंत्र इकाई माध्यमिक शिक्षा प्रसार निदेशालय में परिवर्तित हो गई।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डेटा (इनपुट) प्राप्त करने, उसे प्रोसेस करने और परिणाम (आउटपुट) उत्पन्न करने के लिये प्रोग्राम किया जा सकता है। जब इसे अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक कंप्यूटर प्रणाली का निर्माण करता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण अध्ययन और उपयोग की सुविधा के लिये किया जाता है, इस आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है-
- तकनीक के आधार पर (On the Basis of Technology)
- डिजिटल कंप्यूटर (Digital Computer): असतत रूप में सूचनाओं के प्रसंस्करण (Processing) द्वारा समस्याओं के समाधान में सक्षम उपकरणों के एक वर्ग को ‘डिजिटल कंप्यूटर’ कहते हैं। ये कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग डिजिटल रूप (0 एवं 1) में करते हैं। जैसे- सामान्य प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि।
- एनालॉग कंप्यूटर (Analog Computer): सतत रूप में सूचनाओं के प्रसंस्करण (Processing) के लिये उपयोग होने वाले कंप्यूटर ‘एनालॉग कंप्यूटर’ कहलाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग तापमान, दाब, भार, वोल्टेज आदि से संबंधित सतत डाटा (Analog Data) की प्रोसेसिंग में होता है। जैसे-वाहनों की गति मापने हेतु प्रयोग में आने वाले एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग घड़ी इत्यादि।
- हाइब्रिड कंप्यूटर (Hybrid Computer): यह डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन होता है अर्थात् इसमें एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड तथा डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी एवं शुद्धता (Accuracy) होती है। जैसे- रडार प्रणाली, स्मार्ट फोन, टैबलेट डिवाइस इत्यादि।
- आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर (On the Basis of Size and Work Capacity)
- सुपर कंप्यूटर (Super Computer): ये प्रदर्शन (Performance) एवं डाटा-प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे शक्तिशाली होते हैं तथा बड़े संस्थानों/संस्थाओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले विशेषीकृत एवं विशेष कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। वर्तमान में 1.1 एक्साफ्लॉप्स की क्षमता के साथ अमेरिकी सुपरकंप्यूटर Frontier दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर है।
- मेनफ्रेम कंप्यूटर (Mainframe Computer): ये आकार में बड़े तथा महँगे कंप्यूटर होते हैं, जो एक साथ हज़ारों उपयोगकर्त्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। सामान्यत: जहाँ सुपर कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम पर बहुत तेज़ गति से कार्य कर सकता है, वहीं मेनफ्रेम कंप्यूटर थोड़ी कम गति से, लेकिन हज़ारों प्रोग्रामों पर एक साथ कार्य कर सकता है। स्टोरेज़ क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग बड़े संगठनों, जैसे- बैंकिंग, बीमा संस्थान, सरकारी संगठन, कंपनियाँ आदि करते हैं।
- मिनी कंप्यूटर (Mini Computer): इनका उपयोग छोटी कंपनियों या फर्मों द्वारा किया जाता है। विशेष उद्देश्यों हेतु बड़ी कंपनियों के अलग-अलग विभागों द्वारा भी इनका उपयोग होता है। सामान्यत: इन्हें ‘मिडरेंज कंप्यूटर’ भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी क्षमता सुपर कंप्यूटर तथा मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम एवं पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि से अधिक होती है।
जैसे- K-202, IBM Midrange Computer आदि। - माइक्रो कंप्यूटर (Micro Computer): माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग हेतु डिज़ाइन किया गया है, जो शिक्षा, मनोरंजन, छोटे ऑफिस के कार्य आदि के लिये उपयोगी हैं।
जैसे-Desktop Computer, Gaming Consoles, Sound and Navigation of Car, Notebooks, Smartphones आदि।
वर्तमान तक कंप्यूटर की पाँच पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। कंप्यूटर विकास का पीढ़ियों में विभाजन कंप्यूटर तकनीकी में हुए व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसने कंप्यूटर को और अधिक छोटा, सस्ता, शक्तिशाली तथा दक्ष बनाया है। कंप्यूटर विकास को निम्नलिखित पाँच पीढ़ियों में बाँटा जा सकता हैं-
- प्रथम पीढ़ी (First Generation) 1940–1956:
- वृहद् आकार, वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tube) का सर्किट के लिये तथा मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिये उपयोग
- अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता तथा ऊष्मा का उत्सर्जन, मशीनी भाषा का उपयोग,इनपुट के लिये पंचकार्ड एवं पेपर टेप तथा आउटपुट के लिये प्रिंटर का उपयोग आदि।
- UNIVAC तथा ENIAC प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं।
- द्वितीय पीढ़ी (Second Generation) 1956–1963:
- इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर (Transistor) ने वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक कोर तकनीकी ने मैग्नेटिक ड्रम का तथा असेंबली (Assembly) भाषा ने मशीनी भाषा का स्थान ले लिया।
- जिसने कंप्यूटर को पहले से छोटा, सस्ता, तेज़ तथा अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया लेकिन अधिक ऊर्जा खपत एक समस्या बनी रही।
- तृतीय पीढ़ी (Third Generation) 1964–1971:
- इंटीग्रेटेड सर्किट (Integrated Circuit) के विकास ने कंप्यूटर की गति तथा क्षमता में अत्यधिक वृद्धि की ।
- की-बोर्ड, मॉनीटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस के उपयोग ने कंप्यूटर को एक साथ कई एप्लीकेशन के उपयोग हेतु सक्षम बनाया।
- आसानी से काम करने योग्य तथा आकार में छोटे होने के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर पहली बार सामान्य जन को सुलभ हुए।
- चौथी पीढ़ी (Fourth Generation) 1971&Present:
- माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessors) जिसमें हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी होती है, का उपयोग आरंभ हुआ।
- इस पीढ़ी के कंप्यूटर, नेटवर्क में जुड़ सकते थे।
- अत: इसने इंटरनेट के उपयोग को संभव बनाया। इसी पीढ़ी में GUI (Graphical User Interface) तथा माउस का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ।
- पाँचवीं पीढ़ी (Fifth Generation) Present and Beyond:
- इस पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि (Artificial Intelligence) पर आधारित हैं तथा विकास के क्रम में हैं। इस पीढ़ी में एक ऐसे कंप्यूटर के विकास का लक्ष्य है, जो प्राकृतिक भाषाओं का उपयोग कर सके।
- कंप्यूटर के मुख्यत: तीन अवयव (Component) होते हैं :
- इनपुट/आउटपुट (I/O) यूनिट: इनपुट यूनिट, कोडेड डाटा को प्रोसेसर को भेजता है तथा आउटपुट यूनिट, प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को उपलब्ध कराता है।
- सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU): यह कंप्यूटर का मस्तिष्क (Brain) होता है, इसे ‘प्रोसेसर’ या ‘माइक्रोप्रोसेसर’ भी कहते हैं। इसका कार्य दिये गए निर्देशों अनुसार इनपुट डाटा को प्रोसेस करना है। इस क्रम में यह डाटा पर गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्यों को नियंत्रित भी करता है। इसकी गति को MIPS (Million Instruction Per Second) में मापा जाता है। इसके मुख्यत: तीन भाग होते हैं :
- एएलयू (ALU-Arithmetic Logic Unit): यह गणितीय (Mathematical) तथा तार्किक (Logical) ऑपरेशन संचालित करता है।
- सीयू (CU-Control Unit) : यह माइक्रोप्रोसेसर में निहित निर्देश समूहों को लागू करता है। यह मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त कर उन्हें डीकोड करता है तथा निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन एवं ज़रूरत पड़ने पर एएलयू को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भेजता है।
- रजिस्टर्स/मेमोरी यूनिट: ये प्रोसेसर में अस्थायी डाटा स्टोरेज़ एरिया होते हैं, जो प्रोसेस होने वाले डाटा को सँभालने का कार्य करते हैं। यही डाटा कंट्रोल यूनिट द्वारा आगे उपयोग किया जाता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने के साथ ही पुराना डाटा समाप्त होता जाता है।
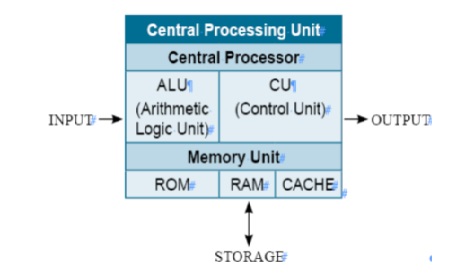
-
- मेमोरी यूनिट (Memory Unit): मेमोरी, कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज़ एरिया होता है, जो डाटा तथा निर्देशों को स्टोर करता है।
संविधान प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मानवता की प्रगति के लिये समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शिक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पहुँचे। इसे पूरा करने के लिये समावेशी शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। इस दृष्टि से हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
- आवश्यकता :
- सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है।
- बच्चों में उनकी सीखने की क्षमता और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भेदभाव मिटाने के लिये समावेशी शिक्षा आवश्यक है।
- बच्चों के शैक्षणिक और सामाजिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये।
- सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा विशेष बच्चों को समाज व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये।
- बच्चों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा स्थापित करने के लिये।
- बच्चों में भय को कम करने, दोस्ती का निर्माण व आत्मविश्वास की क्षमता के लिये।
- समूह में सुरक्षा और सुरक्षित भावना के विकास तथा विविधता के बीच व्यक्तिगत क्षमतानुसार आत्मविश्वास के लिये।
- महत्त्व :
- समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिये उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
- यह अन्य विद्यार्थियों को अपनी उम्र के साथ कक्षा में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिये अभिप्रेरित करती है।
- समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।
- यह सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिये भी अवसर प्रदान करती है।
- समावेशी शिक्षा गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। साथ ही यह बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के साथ रहने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिये स्कूल का माहौल बेहतर हो सकता है।
- यह प्रथा भेदभाव को दूर करने में मदद कर सकती है जो समाज के हर क्षेत्र में व्यापक है।
- यह राष्ट्र के विकास के लिये व्यक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ावा देती है।
कंप्यूटर की भाषाएँ, कंप्यूटर सिस्टम से संप्रेषण (Communication)का मुख्य माध्यम तथा किसी कार्य के संपादन हेतु कंप्यूटर को दिये गए निर्देश हैं। कंप्यूटर के प्रकार तथा कार्य के आधार पर अनेक भाषाओं का विकास किया गया है। कंप्यूटर की भाषाओं को मुख्यत: दो भागों में विभाजित किया गया है-
- निम्न-स्तरीय भाषाएँ (Low Level Languages): ये मशीन कोड हैं, जिनमें कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देश दिये जाते हैं। इसका मुख्य कार्य हार्डवेयर और सिस्टम घटकों का संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना है। इसके निम्नलिखित दो प्रकार हैं-
- मशीनी भाषा (Machine Language): यह प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा है। मशीनी भाषा एकमात्र भाषा है, जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है। यह सामान्यत: हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। यह भाषा बाईनरी नंबर (0, 1) का उपयोग कंप्यूटर को विद्युत सिग्नल भेजने में करती है, जहाँ 0 विद्युत सिग्नल की अनुपस्थिति तथा 1 विद्युत सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। इंटरप्रेटर (Interpreter) एक प्रकार का अनुवादक सॉफ्टवेर है जिसका मुख्य कार्य उच्च-स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा (0,1) में ट्रांसलेट करना हैं। हालाँकि यह एक बार में एक लाइन का ही अनुवाद करता है।
- असेंबली भाषा (Assembly Language): द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, जिसकी संरचना तथा अनुदेशों के सेट, मशीनी भाषा के समान होते हैं, लेकिन इसमें मशीनी भाषा में उपयोग होने वाले अंकों की जगह अंग्रेज़ी के शब्दों, नामों तथा संकेतों का उपयोग होता है।
- उच्च-स्तरीय भाषाएँ (High Level Languages): उच्च-स्तरीय भाषाएँ मूल रूप से प्रतीकात्मक भाषाएँ हैं, जिनमें अंग्रेज़ी शब्दों तथा गणितीय प्रतीकों का उपयोग होता है। उच्च-स्तरीय भाषाओं में दिये जाने वाले निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। कंपाइलर (compiler) एक प्रकार का अनुवादक सॉफ्टवेर है जिसका मुख्य कार्य उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद करता है।
प्रमुख उच्च-स्तरीय भाषा वर्ग का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है-- बीजगणितीय फॉर्मूला प्रसंस्करण भाषाएँ (Algebraic Formula Processing Languages) : ये भाषाएँ गणितीय एवं सांख्यिकीय समस्याओं को सुलझाने में कंप्यूटर के उपयोग हेतु विकसित की गई हैं :
- BASIC (Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code)
- FORTRAN (Formula Translation)
- PL1 (Programming Language, Version 1)
- ALGOL (Algorithmic Language)
- व्यावसायिक डाटा प्रसंस्करण भाषाएँ (Business Data Processing Languages) : ये भाषाएँ कंप्यूटर को डाटा प्रसंस्करण प्रक्रियाओं तथा फाइलों को सँभालने में आने वाली समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाती हैं।
- COBOL (Common Business Oriented Language)
- RPG (Report Programme Generation)
- स्ट्रिंग और लिस्ट प्रोसेसिंग भाषाएँ (String and List Processing Languages) : इन भाषाओं का उपयोग स्ट्रिंग ऑपरेशन में होता है, जिसमें पैटर्न सर्च तथा वर्णों (Characters) को सम्मिलित करना (Insertion) और हटा देना (Deletion) शामिल है। जैसे: LISP (List Processing), Prolog (Programming in Logic) इत्यादि।
- ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएँ (Object Oriented Programming Languages) : यह एक ऐसी भाषा है, जो एक्शन के बजाय ऑब्जेक्ट तथा तर्क (Logic) के बजाय डाटा को ध्यान में रखकर प्रोग्राम की जाती है। जैसे- C++, Java इत्यादि।
- दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाएँ (Visual Programming Languages) : एक प्रोग्रामिंग भाषा, जो प्रोग्राम को विकसित करने के लिये चित्रात्मक तत्त्वों (Graphical Elements) तथा आकृतियों का उपयोग करती है। जैसे: Kodu, MIT app Inventor इत्यादि।
- बीजगणितीय फॉर्मूला प्रसंस्करण भाषाएँ (Algebraic Formula Processing Languages) : ये भाषाएँ गणितीय एवं सांख्यिकीय समस्याओं को सुलझाने में कंप्यूटर के उपयोग हेतु विकसित की गई हैं :
29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ (National Education Policy-2020) को मंज़ूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986’ [National Policy on Education (NPE)-1986] को प्रतिस्थापित करेगी।
- NEP-2020 से संबंधित प्रमुख तथ्य :
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा’ प्रस्तुत किया था।
- ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020’ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।
- NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में वर्तमान 10+2 में सक्रिय शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषायी बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि हेतु तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णयन और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
- NEP-2020 के तहत ‘शिक्षा और सीखने (Education and Learning)’ पर पुन: अधिक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर ‘शिक्षा मंत्रालय’ कर दिया गया है।
नोट: यह NEP-2020 का संक्षिप्त सारांश है। संपूर्ण नीति दस्तावेज़ यहां देखा जा सकता है:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
मूल्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग दूसरों को नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं। मूल्य शिक्षा का अर्थ विद्यार्थियों में मानवीयता का भाव उत्पन्न करने और राष्ट्रहित के प्रति गहरी सोच उत्पन्न करने की व्यवस्था से है। विद्यालयों में मूल्य शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक पक्ष का विकास होता है। वस्तुत: हम कह सकते हैं कि मूल्य हमारे जीवन में सही कार्य करने के लिये पथ-प्रदर्शक होते हैं। मूल्य शिक्षा भारतीय दर्शन परंपराओं और संस्कृति में अंतर्निहित है।
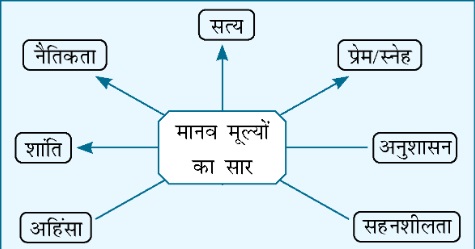
मूल्य शिक्षा आदर्श और यथार्थ के मध्य सेतु की भूमिका का निर्वाह करती है। मूल्यों के अभाव में विद्यार्थियों को दी गई शिक्षा निर्जीव होती है। मूल्य हमारे व्यवहार को निर्देशित तथा नियंत्रित करते हैं। उद्देश्यों के प्राप्ति के साधनों के चयन में निर्णय लेने में निर्णायक का कार्य करते हैं।
- मूल्य शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग के सुझाव
वर्ष 1964 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने मूल्य शिक्षा के संदर्भ में कुछ सुझाव दिये जो निम्नलिखित हैं-- प्राथमिक विद्यालय स्तर पर मूल्यपूरक शिक्षा रोचक कहानियों के द्वारा, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों एवं विद्यालयों के पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा प्रदान की जाए।
- निजी प्रबंधकों (Private Management) द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में भी नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य की शिक्षा दी जाए।
- शिक्षण संस्थानों में साप्ताहिक या मासिक आधार पर नैतिक शिक्षा देने हेतु एक रोस्टर तैयार किया जाए।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए।
- कोठारी आयोग के अनुसार मूल्य शिक्षा दो विधियों के माध्यम से दी जानी चाहिये। ये दो विधियाँ निम्नलिखित हैं-
- प्रत्यक्ष विधियाँ (Direct Methods): इसके तहत मूल्य शिक्षा के लिये समयावधि निर्धारित होनी चाहिये तथा विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं कहानियों तथा महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से मूल्य शिक्षा दी जाए।
- अप्रत्यक्ष विधियाँ (Indirect Methods): इसके तहत विद्यालय का वातावरण, सुझाव व प्रेरणा, सामूहिक कार्य, मौन चिंतन, प्रात:कालीन सभा तथा धार्मिक समारोह आदि| उपर्युक्त दोनों विधियों द्वारा मूल्य शिक्षा प्रदान की जाए।
- राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद (National Value Education Centre)
तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना आईआईटी दिल्ली में की गई है। वर्तमान समय में सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ व्यावसायिक संस्थान भी अपने पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को स्थान दे रहे हैं।
- विश्व के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इग्ंलैंड में 1969 ई. में हुई थी तथा जनवरी 1971 में पहले विद्यार्थी का नामांकन हुआ था।
- भारत में इस समय राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या (State Open Universities) 14 है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसलिये इसे राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है।
राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की सूची
|
विश्वविद्यालय का नाम |
राज्य |
स्थापना वर्ष |
|
डॉ. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
तेलंगाना |
1982 |
|
वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा |
राजस्थान |
1987 |
|
नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना |
बिहार |
1987 |
|
यशवंत राव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक |
महाराष्ट्र |
1989 |
|
मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल |
मध्य प्रदेश |
1991 |
|
डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद |
गुजरात |
1994 |
|
कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर |
कर्नाटक |
1996 |
|
नेता जी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता |
प. बंगाल |
1997 |
|
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
उत्तर प्रदेश |
1999 |
|
तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई |
तमिलनाडु |
2002 |
|
पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर |
छतीसगढ़ |
2005 |
|
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी |
उत्तराखंड |
2005 |
|
कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी |
असम |
2005 |
|
ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय |
ओडिशा |
2015 |
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना संसद अधिनियम 1985 के तहत हुई है। IGNOU ने बहुत तेज़ी के साथ विकास किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त (OPEN) शिक्षा संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना चुका है।
- IGNOU का मुख्य परिसर (Main Campus) दिल्ली में स्थित है।
- विश्वविद्यालय ने शिक्षा प्रदायगी के लिये संचार के माध्यम जैसे प्रिंट मीडियम, ऑडियो-वीडियो विजुअल, ब्रॉडकास्ट, रेडियो, शैक्षिक टीवी चैनलों और अन्य डिजिटल माध्यमों का बखूबी इस्तेमाल किया है।
- IGNOU अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्य देशों: संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, दोहा, श्रीलंका, मॉरीशस, मालदीव, नेपाल, केन्या, फिजी, कैरीबियन द्वीपसमूह आदि देशों में भी अपनी शैक्षिक सेवाएँ प्रदान करता है।
- IGNOU, यूनेस्को और क्षमता निर्माण के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से अफ्रीका, इथोपिया, लाइबेरिया, मेडागास्कर और घाना में भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पहुँच प्रदान करता है।
- समाज से वंचित व्यक्तियों की उच्चतर शिक्षा तक पहुँच बनाने में IGNOU ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये IGNOU का शैक्षिक कार्यक्रम अनवरत जारी है।
नोट : वर्ष 2024 की NIRF रैंकिंग में तीन नई श्रेणियाँ सम्मिलित की गई हैं : ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और स्टेट-फंडेड यूनिवर्सिटी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 में IGNOU ने ओपन यूनिवर्सिटी में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centres)
क्षेत्रीय केंद्र को IGNOU अधिनियम की धारा 2(J) के तहत परिभाषित किया गया है। यह केंद्र मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये विद्यार्थियों की सहायता सेवा के रखरखाव तथा निगरानी का कार्य करता है। इसके अलावा IGNOU अधिनियम की धारा 5(1) (XXVI) के तहत विश्वविद्यालय को कॉलेज या क्षेत्रीय केंद्र पर वैधानिक दर्जा दिया जाता है ताकि विधियों द्वारा निर्धारित तरीके से सम्मानित किया जा सके।- IGNOU के क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या 56 है।
- IGNOU-आर्मी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र 6 हैं।
- IGNOU-नौसेना मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र 4 हैं।
- IGNOU-असम राइफल्स मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र 1 है।
- नोट: IGNOU के समस्त क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या IGNOU के वेबसाइट (12 सितंबर, 2019 तक) के अनुसार है।
- IGNOU द्वारा संचालित प्रमुख रेडियो/टीवी चैनल :
- ज्ञान वाणी: विद्यार्थियों की सुविधा हेतु वर्ष 2001 में इस एफ.एम. रेडियो चैनल की शुरुआत की र्गई।
- ज्ञान दर्शन: विद्यार्थियों की सुविधा हेतु 26 जनवरी, 2000 को इस शैक्षिक टेलीविजन चैनल की शुरुआत की गई। विद्यार्थियों के अध्ययन को यह चैनल सुगम व सहज बनाता है।
- एकलव्य प्रौद्योगिकी/तकनीक चैनल: आई.आई.टी. और IGNOU के मध्य दूरस्थ शिक्षा की एक संयुक्त पहल है। इस चैनल की शुरुआत 26 जनवरी, 2003 को हुई थी।
- व्यास चैनल (Vyas Channel): कॉन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (CEC) ने यूजीसी के साथ मिलकर 24 × 7 उच्चतर शिक्षा चैनल की स्थापना 26 जनवरी, 2004 को की।
नोट: ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन की नोडल एजेंसी IGNOU है तथा ज्ञान दर्शन टीवी चैनल का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है।
जेम्स टेलर ने वर्ष 1995 में दूरस्थ शिक्षा की चार पीढ़ियों का उल्लेख किया है। वर्तमान में शिक्षा का विकास क्रम दिनोदिन आगे बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम के अंतर्गत पाँचवीं पीढ़ी (Fifth Generation) का आविर्भाव हो चुका है।
- प्रथम पीढ़ी (First Generation): इस पीढ़ी के अंतर्गत पत्राचार शिक्षा (Correspondence Education) को रखा गया है। पत्राचार शिक्षा प्रणाली में ‘मुद्रण’ माध्यम (Print Medium) का उपयोग शिक्षण अधिगम के विकास हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी गति व कठोर परिश्रम से सीखता है।
- द्वितीय पीढ़ी (Second Generation): इस पीढ़ी में मुद्रित सामग्री के साथ-साथ कंप्यूटर, सीडी, कैसेट्स जैसी अमुद्रित सामग्री का प्रयोग बढ़ जाता है। इस पीढ़ी में बहु-माध्यम उपागम (Multi Media Approach) तथा स्व अध्ययन सामग्री की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी दृष्टि से इस पीढ़ी ने बहुत अधिक सफलताएँ अर्जित की हैं।
- तृतीय पीढ़ी (Third Generation): इस पीढ़ी को ‘टेली लर्निंग एप्रोच’ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा रेडियो द्वारा पाठ्य वस्तुओं का प्रसारण होता है। विद्यार्थियों व शिक्षकों के मध्य विषय संबंधी मुद्दों पर क्रिया-प्रतिक्रिया का दौर प्रारंभ होता है।
- चतुर्थ पीढ़ी (Fourth Generation): इस पीढ़ी के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकता है। इसमें Computer Conferencing, E–Mail, जैसी सुविधाओं का उपयोग हुआ है।
- पाँचवीं पीढ़ी (Fifth Generation): ऑनलाइन अध्ययन करना, समस्या का समाधान इस पीढ़ी का प्रमुख ध्येय होता है। मल्टीमीडिया का अत्यधिक प्रयोग इस पीढ़ी में होता है। वर्तमान समय में आभासी विश्वविद्यालय (Virtual Universities) की अवधारणा का धीरे-धीरे विकास हो रहा है।
- वर्ष 1642: प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कलाइन (Pascaline)का विकास फ्राँसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया।
- ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने वाष्प चालित गणना करने वाली मशीन एनालिटिकल (Analytical) इंजन का विकास किया।
- चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है।
- चार्ल्स बैबेज द्वारा ही डिफरेंस इंजन (Difference Engine) का विकास किया गया था।
- वर्ष 1890: हरमन हॉलेरिथ द्वारा ‘पंचकार्ड’ बनाया गया, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था।
- वर्ष 1936: एलन ट्यूरिंग द्वारा ‘ट्यूरिंग मशीन’ का विकास किया गया। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इसी पर आधारित है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है।
- वर्ष 1944: स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क-I बनकर तैयार हुआ।
- वर्ष-1945: गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। न्यूमैन ने ही बाईनरी नंबर सिस्टम तथा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी दी थी।
- वर्ष 1946 : इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर (ENIAC) का निर्माण हुआ। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो सामान्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया गया।
- वर्ष 1947 : बेल लेबोरेटरी (Bell Laboratories) द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। इसने कंप्यूटर में लगने वाले वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया।
- वर्ष 1951 : UNIVAC–I (Universal Automatic Computer) का निर्माण पूरा हुआ। इसे Eckert - Mauchly Computer Corporation द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह पहला वाणिज्यिक (Commercial) कंप्यूटर था। इसका उपयोग यू.एस. प्रेसीडेंट इलेक्शन परिणामों के पूर्वानुमान तथा जनगणना में किया गया था।
- वर्ष 1950 : के दशक में FORTRAN भाषा का विकास हुआ।
- वर्ष 1958 : जैक किल्बी (Jack Kilby) तथा रॉबर्ट नॉएस (Robert Noyce) ने इंटीग्रेटेड सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया। इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टरों का समूह होता है।
- मैनुएल केस्टले ने ‘‘नेटवर्क सोसायटी’’ का सर्वप्रथम प्रयोग किया।
- विलियम इंग्लिश ने पहले माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया।
- वर्ष 1964 : सेमर क्रे (Seymour Cray) द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 निर्मित हुआ।
- वर्ष 1968 : माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) से युक्त आधुनिक कंप्यूटर के एक प्रोटोटाइप का डगलस एंजलबर्ट द्वारा प्रदर्शन किया गया। माउस का पेटेंट डगलस एंजलबर्ट के नाम है।
- वर्ष 1969 : बेल लैब (Bell Labs) ने UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया, जिसे बाद में C–Programming Language में लिखा गया।
- वर्ष 1970 : इंटेल (Intel) द्वारा डायनेमिक एक्सेस मेमोरी (DRAM 1103) चिप का निर्माण किया गया।
- वर्ष 1973 : जेरॉक्स (Xerox) टीम के सदस्य रॉबर्ट मेटकॉफ (Robert Metcalfe) द्वारा इथरनेट (Ethernet) का विकास किया गया।
- वर्ष 1975 : पॉल एलन (Paul Allen) तथा बिल गेट्स (Bill Gates) द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई।
- वर्ष 1976 : स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) तथा स्टीव वॉज़्निएक द्वारा (Steve Wozniak) एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की गई।
- वर्ष 1981 : Osborne 1 को विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया था। इसी वर्ष घोषित Epson HX-20 को पहला लैपटॉप कंप्यूटर माना जाता है।
- वर्ष 1983: GUI (Graphical User Interface) से युक्त पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल का लीजा (Lisa) था। Gavilan SC पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था, जिसे ‘लैपटॉप’ नाम से बाज़ार में उतारा गया।
- वर्ष 1985: माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लांच किया।
- Symbolics.com पहला रजिस्टर्ड डोमेन नाम था।
- वर्ष 1990 : टिम बर्नर ली (Tim Berner Lee) ने Hyper Text Markup Language (HTML) का विकास किया।
- वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार ली द्वारा 1989 में ही कर लिया गया था, लेकिन HTML के विकास ने इसे अनुप्रयोगी बनाया।
- टिम बर्नर ली ने पहली बार URL (Uniform Resource Locator) की रचना की।
- वर्ष 1993 : इंटेल ने पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर प्रस्तुत किया।
- सेर्गेई ब्रिन तथा लैरी पेज ने गूगल सर्च इंजन का विकास किया।
- वर्ष 2004 : Mozilla Firefox 1.0 नामक वेब ब्राउजर तथा Facebook नामक सोशल नेटवर्किंग साइट मार्केट में लांच की गईं।
- वर्ष 2005 : You Tube नामक एक Video Sharing Service की शुरुआत की गई।
मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों को खास स्थान पर खास समय के अनुसार एकत्रित होने की बाध्यता नहीं होती है। यह प्रणाली कार्यविधियों एवं शिक्षण समय के संबंध में बहुत लचीली है। साथ ही इसमें दाखिले के लिये किसी मेरिट कसौटी को पूरा करने की बाध्यता नहीं होती है। दूरस्थ शिक्षा को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे दूरवर्ती शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, गृह अध्ययन, परिसर के बाहर अध्ययन (Off Campus Study)तथा इसे ‘बहुमाध्यम उपागम’ (Multi Media Approach) भी कहते हैं।
- दूरस्थ शिक्षा को गैर-सरकारी उपागम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुद्रित एवं अमुद्रित बहु-माध्यमों का प्रयोग शिक्षण तथा विद्यार्थी के मध्य संचार के लिये किया जाता है। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी एक-दूसरे से अलग रहकर आवश्यक कार्यों तथा उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हैं। इसमें स्व अध्ययन (Self Study) को महत्त्व दिया जाता है।
- दूरस्थ शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिये शिक्षा सहायक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण सहायक उपकरणों की सूची में रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो-वीडियो फाइल्स, सी.डी. फिल्म्स, पत्राचार सामग्री तथा विभिन्न डिजिटल माध्यम सम्मिलित हैं।
- दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को जन-शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वंचित क्षेत्रों से जुडे़ युवाओं को, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उन्हें अध्ययन का अवसर प्रदान करना।
- भारत में दूरस्थ (दूरवर्ती) शिक्षा का प्रारंभ वर्ष 1962 में पत्राचार (Correspondence) शिक्षा कार्यक्रम के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया।
- डी.एस. कोठारी- ‘‘अंशकालिक और पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा को पूर्णकालिक शिक्षा के समान दर्जा दिया जाना चाहिये, ताकि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को अवसर मिले, जो खुद को शिक्षित करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पूर्णकालिक आधार पर ऐसा नहीं कर पाते’’।
- यूनेस्को- ‘‘जीवन पर्यंत शिक्षा एक प्रक्रिया है। व्यक्ति औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से सीखता है।’’
- दूरस्थ शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएँ
- दूरस्थ शिक्षा परिषद् (Distance Education Council): राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ तथा मुक्त शिक्षा के मानकों और आपसी समन्वय को बनाये रखने के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड ने इस उत्तरदायी संस्थान की स्थापना वर्ष 1992 में की थी।
- दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (Distance Education Bureau): दूरस्थ शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों का दायित्व यूजीसी ने दूरस्थ शिक्षा परिषद के स्थान पर दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो को सौंपा है। इस ब्यूरो की स्थापना सितंबर 2012 के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो यूजीसी के अधीन एक निकाय है।वर्ष 2013 में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के विघटित होने के बाद अस्तित्व में आई।
इस एजेंसी का गठन देश के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (IIT, NIT और IIM आदि ) के लिये अनुसंधान केंद्रित बुनियादी ढाँचे को विकसित करना तथा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किया गया।
- स्थापना
- HEFA के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2016 को मंजूरी प्रदान की।
- इसे 2017 में शिक्षा मंत्रालय और केनरा बैंक के संयुक्त उद्यम (क्रमशः 91% और 9% निवेश भागीदारी) के रूप में शुरू किया गया।
- मुख्य उद्देश्य
- प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- बाज़ार आधारित उपकरणों का उपयोग करके बाज़ार से धन प्राप्त करना।
- कानूनी स्थिति
- HEFA कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गैर-लाभकारी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
- यह गैर-जमा (Non-deposit) कंपनी के रूप में RBI के साथ NBFC-ND के रूप में पंजीकृत है।
- आर्थिक पक्ष
- HEFA की अधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपये है, जिसमें सरकारी हिस्सेदारी 1000 करोड़ रुपये की है।
- इसे PSU बैंक और सरकारी स्वामित्व वाली NBFC के दायरे में विशेष इकाई के रूप में गठित किया गया है।
EQUIP का तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन और समावेशी कार्यक्रम (Education Quality Upgradation and Inclusion Program) से है। यह प्रोजेक्ट सरकार के साथ नीति आयोग के सीईओ, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और पूर्व राजस्व सचिव सहित कुछ कॉर्पोरेट प्रमुखों के नेतृत्व वाली दस सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया है।
- प्रमुख बिंदु
- भारत में बहुस्तरीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये एक कार्ययोजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसे वर्ष 2019-2024 के बीच लागू किया जाना है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन योजना के रूप में वर्णित है। इसे नीति और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिये लाया जा रहा है।
- उद्देश्य
- उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करना।
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में भौगोलिक रूप से विद्यमान विषमता में सुधार करना।
- देश भर में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को लागू करना।
- शीर्ष वैश्विक संस्थानों में कम-से-कम 20 भारतीय संस्थानों की उपस्थिति दर्ज कराना।
- अनुसंधान/नवाचार के परिवेश को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों के लिये रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता में आवश्यक सुधार करना।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये रूपरेखा तैयार करना।
- बेहतर प्रमाणन प्रणालियों, शिक्षा प्रौद्योगिकी के उपयोग, प्रशासनिक सुधार और निवेश में मात्रात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि करना।
- वित्तपोषण
- इस परियोजना का वित्तपोषण उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency-HEFA) के अलावा बाज़ार में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।
आयु के संदर्भ में लिंग भिन्नताएँ यह दर्शाती हैं कि जैसे-जैसे व्यक्ति बड़े होते हैं, उनकी विकासात्मक प्रक्रियाएँ और अनुभव कैसे भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएँ जीवन के विभिन्न चरणों में अधिक स्पष्ट होती हैं, जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, और सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं।
- आयु के अनुसार विकासात्मक भिन्नताएँ : आयु जीवन के विकासात्मक पथ निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो लिंग के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। बचपन के दौरान, तेजी से शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही तीव्र विकास अनुभव करते हैं। हालाँकि, इस विकास की दर और प्रकार में भिन्नताएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिये, लड़कियाँ आमतौर पर भाषा अधिग्रहण और सूक्ष्म मोटर कौशल जैसे विकासात्मक स्तर को लड़कों की तुलना में थोड़ा पहले प्राप्त करती हैं। दूसरी ओर, लड़के, शुरुआती किशोरावस्था के दौरान अधिक स्पष्ट शारीरिक विकास प्रदर्शित कर सकते हैं।
- संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास : बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ते समय, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास जारी रहता है। अनुसंधान से पता चलता है कि जबकि दोनों लिंग संज्ञानात्मक वृद्धि का अनुभव करते हैं, यह वृद्धि अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है। लड़कियाँ अक्सर शब्दावली और सामाजिक कौशल में पहले विकसित होती हैं, जो उनके शैक्षिक प्रदर्शन और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित कर सकती है। लड़के किशोरावस्था में रीज़निंग और गणितीय कौशल में अधिक सक्षम हो सकते हैं, जो उनके शैक्षिक और कैरियर विकल्पों को प्रभावित कर सकता है।
- शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य : शारीरिक वृद्धि की प्रक्रियाएँ भी लिंग के आधार पर भिन्न होती हैं। किशोरावस्था के दौरान, लड़कियाँ आमतौर पर लड़कों की तुलना में शारीरिक परिवर्तनों का पहले अनुभव करती हैं, जैसे कि तीव्र शारीरिक वृद्धि और हार्मोनल बदलाव। ये प्रारंभिक परिवर्तन आत्म-संवेदनशीलता और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। लड़के आमतौर पर अधिक समय तक वृद्धि और मांसपेशियों के विकास का अनुभव करते हैं, जो उनके शारीरिक क्षमताओं और सामाजिक धारणाओं को प्रभावित कर सकता है।
- अनुभव का संचय : आयु के साथ, जीवन के अनुभवों का संचय लिंग भिन्नताओं को बढ़ाता है। उदाहरण के लिये, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में विभिन्न सामाजिक अपेक्षाएँ और कैरियर चुनौतियाँ का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके अनुभव और अवसरों को प्रभावित कर सकती है। लिंग-विशिष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ व्यक्ति के अनुभव और कौशल के विकास को प्रभावित कर सकती हैं।
- शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव : इन लिंग भिन्नताओं को समझना शिक्षकों और नियोक्ताओं के लिये महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा में, ऐसे शिक्षण तरीकों को अपनाना जो लड़कों और लड़कियों की अलग-अलग विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हों, यह सीखने के परिणामों में सुधार कर सकता है।
- लिंग भिन्नताओं को संबोधित करना : लिंग भिन्नताओं को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिये, ऐसी रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है जो विभिन्न आयु चरणों में प्रत्येक लिंग की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करें। समावेशी शैक्षिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, समान अवसर प्रदान करना, और सामाजिक अपेक्षाओं को संबोधित करना इन भिन्नताओं को कम करने में मदद कर सकता है।
स्पष्ट है कि आयु के संदर्भ में लिंग भिन्नताएँ यह प्रदर्शित करती हैं कि पुरुषों और महिलाओं के बीच विकासात्मक प्रक्रियाएँ कैसे भिन्न होती हैं। इन भिन्नताओं को समझकर और संबोधित करके, हम जीवन के सभी चरणों में अधिक समान अवसर और समर्थन प्रदान कर सकते हैं।
हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल ‘स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकॉनमी’ (STRIDE) की घोषणा की।
- STRIDE के प्रमुख उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है।
- मानविकी और मानव विज्ञान के संदर्भ में विशेष ध्यान देते हुए बहु-संस्थागत नेटवर्क तथा प्रभावी रिसर्च परियोजनाओं को फंड प्रदान करना।
- प्रमुख बिंदु
- STRIDE उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होगें।
- इसे शोध की एक नई संस्कृति को विकसित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
- यह मज़बूत नागरिक समाज के निर्माण हेतु नए विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं तथा विकास को समर्थन प्रदान करेगा।
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च कल्चर को मज़बूत करने में सहयोग हेतु STRIDE के निम्नलिखित तीन घटक दिये गए हैं-
- इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तथा नवाचार को प्रेरित करने के साथ ही युवा प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान हेतु युवा प्रतिभाओं की पहचान व उनका समर्थन करके विविध विषयों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिये 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिये विश्वविद्यालयों, सरकार, स्वैच्छिक संगठनों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान करने के लिये 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
इसके तहत निधिकरण के लिये पात्र शर्तों में शामिल हैं : दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, नृविज्ञान, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा एवं संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य, प्रबंधन, पर्यावरण और सतत विकास। इस घटक के लिये उपलब्ध अनुदान के अंतर्गत एक उच्च शैक्षणिक संस्थान हेतु 1 करोड़ रुपए और बहु संस्थागत नेटवर्क के लिये 5 करोड़ रुपए तक दिये जाने का प्रावधान है।
- उच्चतर आविष्कार योजना : शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 (6 अक्तूबर, 2015) में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य कार्य भारत और भारत के बाहर शिक्षा और उद्योगों के मध्य सहयोग स्थापित करना है।
- ईशान उदय : यूजीसी द्वारा वर्ष 2014 – 15 के शैक्षिक सत्र से पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिये ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है।
- ईशान विकास : पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों में विज्ञान गणित और इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है।
- उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan): ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के लिये उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में आधारभूत ज्ञान के प्रयोग के लिये उन्नत भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत सभी तकनीकी और उच्चतर शिक्षा सस्थाएँ 5 गाँवों को (प्रत्येक अलग-अलग) गोद लेंगे और उनके नवाचार की योजना तैयार करेंगे। आई.आई.टी. दिल्ली को इस अभियान का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ नवंबर 2014 में किया गया था।
- ई-पाठशाला (e-Pathshala): एन.सी.ई.आर.टी (NCERT) द्वारा पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, आवधिक पत्रिकाओं सहित सभी ई-शैक्षिक संसाधनों और अन्य मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्री की प्रदर्शन मंजूषा और विस्तारण के लिये ई-पाठशाला का निर्माण किया गया है।
- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (Rashtriya Avishkar Abhiyan): इस अभियान का शुभारंभ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 9 जुलाई, 2015 को किया गया था। यह 6–18 आयु वर्ग के बच्चों में विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रेरित व प्रोत्साहित करने की एक पहल है।
- उड़ान परियोजना (Udaan Scheme): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 11वीं व 12वीं की बालिकाओं के लिये वर्ष 2014 में यह परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के अंतर्गत जेईई मुख्य एवं एडवांस प्रवेश परीक्षा और साथ ही अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों/संस्थानों में दाखिले की तैयारी हेतु पात्र बालिकाओं के मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन संसाधन उपलब्ध कराना है।
- रिवाइटलाइज़िंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम एजुकेशन (राइज़) (Revitalising Infrastructure and System in Education – RISE): देश के उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में अनुसंधान से जुड़ी अधोसंरचनाओं को सुधारने हेतु वित्तीय वर्ष 2018 में ‘राइज’ अभियान नामक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत अगले चार वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह निवेश उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency) के द्वारा किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना(Prime Ministers Research Fellowship Scheme): विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना (PMRF) को मंजूरी दी गई है।
- इस योजना के तहत देश के शीर्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थाओं से बीटेक उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष के सर्वोत्तम विद्यार्थियों को आईआईटी (IIT), आईआईएससी (IISC) के पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा।
- चयनित रिसर्च फेलों को प्रथम दो वर्षों के लिये 70,000 रुपये प्रतिमाह, तीसरे वर्ष के लिये 75,000 रुपये प्रतिमाह तथा चौथे और पाँचवे वर्ष के लिये 80,000 प्रतिमाह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी।
यह परियोजना शैक्षिक संस्थाओं में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। आईआईटी मुंबई इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। इसके तहत निम्नलिखित सॉफ्टवेर हैं :
- विद्वान (Vidwan): यह एक विशेषज्ञ डाटाबेस है जो भारत और विदेशों में अग्रणी शैक्षिक और शोध संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल को एकत्रित करता है।
- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (NDL): शिक्षा मंत्रालय, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (NMEICT) के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। आईआईटी खड़गपुर को राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के समन्वय और स्थापना का दायित्व दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को एकल खिड़की पहुँच प्रदान करने के लिये शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं निकायों में सभी मौजूदा डिजिटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करना है
- टॉक-टू-ए-टीचर (Talk to a Teacher): आईआईटी मुंबई द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देशभर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस प्रोजेक्ट में अमृता विश्वविद्यालय भी भागीदार है।
- आस्क अ क्वेश्चन (Ask A Question): यह प्रश्नोत्तर आधारित एक प्लेटफार्म है। पूरे भारत के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब आई.आई.टी. मुंबई के संकाय सदस्य (Faculty Member) देते हैं।
- ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडेमिक नेटवर्क(GIAN): GIAN भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। यह 30 नवंबर, 2015 को प्रारंभ हुआ। जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद वैज्ञानिकों और उद्यमियों की टैलेंट पूल बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों को वैश्विक उत्कृष्टता की सहायता मिल सके।
- राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप (National Research Professorship):भारत सरकार ने ज्ञान के किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षाविदों (Academics) और विद्वानों को सम्मानित करने के लिये सन् 1949 से इस योजना की शुरुआत की थी। वे व्यक्ति, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र पार कर ली हो और ज्ञान के किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो और 65 वर्ष के बाद भी उस क्षेत्र में सकारात्मक योगदान दे रहे हो तब उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुकता प्रशिक्षण योजना(National Scheme of Apprenticeship Training):
- प्रशिक्षुकता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुकता योजना का कार्यान्वयन एक सांविधिक आवश्यकता है। इसके तहत लगभग 10000 प्रतिष्ठानों/संगठनों के इंजीनियर, डिप्लोमाधारकों (तकनीशियनों) और 10+2 की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- अधिनियम के तहत प्रशिक्षुकता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षकों को हर महीने 5000 रुपये से कम की राशि का वजीफा भी दिया जाता है।
- मानव-संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णत:, वित्तपोषित चार प्रशिक्षुकता बोर्ड-मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में स्थित है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य नव स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों और 10+2 पास युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वह उद्योगों की आवश्यकतानुसार अपना क्षमता निर्माण कर सकें।
- इस योजना का आदर्श वाक्य ‘सशक्त युवा, समर्थ भारत’ है।
- ई-यंत्र (e-Yantra): ई-यंत्र शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (NMEICT) प्रायोजित कार्यक्रम है। इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थानों में रोबोटिक्स तकनीक के महत्त्व को देखते हुए आईआईटी बॉम्बे ने इस पहल को आगे बढ़ाया है। इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ अंत:स्थापित प्रक्रिया में अभियंताओं (इंजीनियरों) की अगली पीढ़ी को तैयार करना। आई.आई.टी. बॉम्बे (मुंबई) इस पहल का राष्ट्रीय संयोजक (National Coordinator) है।
- इंप्रिंट (IMPacting Research, INnovation and Technology- IMPRINT)
- इंप्रिंट (इंपैक्ट़िग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी) योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मौजूद प्रासंगिक चुनौती को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ज्ञान के अमूर्तिकरण को उत्पाद में बदलकर भारतीय राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें।
- 5 नवंबर, 2015 में शुरू हुई यह योजना पैन आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी. योजना है, जिसका मुख्य काम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध के लिये कार्य करना है।
- आई.आई.टी. कानपुर इस पहल का राष्ट्रीय संयोजक (National Coordinator) है।
- स्वयं(Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds-SWAYAM)
- स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया ई-शिक्षा कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा के तीन आधारभूत सिद्धांतों अर्थात् पहुँच, निष्पक्षता (अर्थात् सभी को शिक्षा) तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
- कक्षा 9 से लेकर परास्नातक (Post Graduate) से संबंधित सारे विषयों को देश के चुनिंदा 1000 शिक्षकों के माध्यम से स्वयं योजना के तहत पढ़ाने की व्यवस्था है।
- स्वयं प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है।
- स्वयं में प्रदान किये जा रहे पाठ्यक्रम निम्न भागों में होंगे– (1) वीडियो व्याख्यान, (2) विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री, जो डाउनलोड/मुद्रित की जा सकेगी, (3) परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा, (4) संकायों के समाधान के ऑनलाइन विचार-विमर्श।
- इस प्रकार SWAYAM एक मूक (Moocs–Massive Open Online Courses) प्लेटफॉर्म है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसे राज्यों के योग्य (Eligible) उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक रूप से विभिन्न सहायता देने के लिये 2013 में शुरू किया गया। इसके तहत समालोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal) के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुँच और उत्कृष्टता से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिये राज्यों की कार्ययोजना में सहायता करती है।
उद्देश्य
- निर्धारित मानकों और मापदंडों को सुनिश्चित करके राज्य की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिये प्रत्यायन (Accreditation) की पद्धति का अनिवार्य रूप से उपयोग करना।
- संबंधन (Affiliation), शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना।
- उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों में पर्याप्त गुणवत्तायुक्त संकाय मुहैया करना और कार्य के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उपयुक्त माहौल प्रदान करना, ताकि वह खुद को शोध और नवाचार के प्रति समर्पित कर सके।
- अल्पविकसित और पिछडे़ क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर उच्चतर शिक्षा में बने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की कोशिश करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, दिव्यांगों, कमजोरों आदि समाज के वंचित समुदाय को उच्चतर शिक्षा में समावेशित करने की कोशिश करना।
मुख्य कार्य
- मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन (Upgradation)
- कॉलेजों को क्लस्टर (Cluster) विश्वविद्यालयों में बदलना।
- विश्वविद्यालय की अवसंरचना के लिये अनुदान।
- मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल कॉलेजों में उन्नयन (Upgradation)
- नए व्यावसायिक (Professional) कॉलेजों की स्थापना।
- शोध, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार।
- संकायों (Faculty) के लिये भर्ती में सहायता।
- संस्थाओं की पुनर्संरचना और उनमें सुधार।
- डाटा एकत्रीकरण (Data Collection) और योजना, ताकि संस्थाओं के क्षमता निर्माण में बेहतर तैयारी की जा सके।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की स्थापना वर्ष 2017 में भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित कराती है।
- उद्देश्य (Objectives)
- इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर करना है।
- अभी तक इन परीक्षाओं का आयोजन CBSE द्वारा किया जाता था। NTA के गठन से CBSE का कार्यभार कम हुआ है।
- कार्य (Functions)
- यह ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाओं को आयोजित कराती है जिसके लिये इसे ऐसे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का चयन करना होता है जहाँ पर सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हों और परीक्षा के आयोजन से उनकी शैक्षणिक दिनचर्या पर कोई प्रभाव न पड़े।
- अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से सभी विषयों के प्रश्न-पत्र तैयार किये जाते हैं, जिससे पेपर लीक की समस्या का समाधान हो सके।
- भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना और सलाहकारी सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज़ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना।
- विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा किसी परीक्षा के आयोजन का दायित्व सौंपे जाने की स्थिति में उसका संचालन करना।
- विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षण संबंधी मानकों की समय-समय पर जाँच करना।
- प्रशासन (Administration)
- NTA का अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद् होता है एवं उसकी नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- महानिदेशक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जिसमें परीक्षा आयोजित करवाने वाले संस्थानों के सदस्य भी शामिल होते हैं।
- तकनीकी शिक्षा(Technical Education): तकनीकी शिक्षा कुशल जनशक्ति का सृजन कर, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन में सुधार कर मानव संसाधन विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में तकनीकी शिक्षा के माहौल की शुरुआत सड़कों, भवनों, बंदरगाहों के निर्माण व रखरखाव में लगे आर्मी, नेवी और सर्वे विभाग के लोगों की सहायता करने की कोशिश से हुई। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार इन कामों के लिये ब्रिटेन से आए तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों को ऊँचे पदों पर बिठाती थी। लेकिन तकनीकी क्षेत्र के निम्न स्तरीय पद स्थानीय लोगों से ही भरे जाते थे। इन स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान करने के लिये कारखाने के इर्द-गिर्द तकनीकी स्कूल खुलना शुरू हुए और भारत के लिये तकनीकी शिक्षा के माहौल का अंकुरण शुरू हो गया।
भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास-- तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, आर्किटेक्चर, नगर नियोजन, प्रयुक्त कला और शिल्प (Applied Arts and Crafts), होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित कौशल निर्माण के हुनर सिखाए जाते हैं।
- भारत में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना उत्तराखंड के रूड़की शहर में सन् 1847 में हुई, जिसने प्रशिक्षण के लिये गंगा कैनल के लिये बने सार्वजनिक भवनों का इस्तेमाल किया।
- मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैटलर्जी (Metallurgy) के क्षेत्र में डिग्री देने की शुरुआत सन् 1917 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई।
- आज़ादी के बाद से भारत के आधुनिक उत्पादकीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कई इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना हो चुकी है।
- व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education): जो शिक्षा विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय या वृत्ति के समन्वय में ज्ञान एवं कुशलता अर्जित करने में सहायक होती है, ‘उसे व्यावसायिक शिक्षा’ कहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्र के शिक्षा संबंधी प्रयास का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। व्यापक रूप में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिये प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का ही अंग है।
व्यावसायिक शिक्षा की विशेषताएँ(Characteristics of Vocational Education)-- यह विद्यार्थियों की रुचि, प्रवृत्ति एवं व्यक्तित्व का ध्यान रखती है।
- यह शिक्षा एक व्यावहारिक शिक्षा है। यह शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान न प्रदान कर जीवन के हर क्षेत्र के लिये उपयोगी होती है।
- यह शिक्षा परिवार, श्रम एवं कार्य से संबंधित होने के साथ-साथ विद्यार्थियों के जीवन से भी संबंधित है।
- इस शिक्षा का स्वरूप स्थिर नहीं रहता है बल्कि गतिशील रहता है। इसमें समय की गति एवं सभ्यता के विकास के साथ इसके रूप में परिवर्तन आता है।
केंद्र सरकार की शैक्षिक सलाहकार समितियाँ शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं। ये समितियाँ शैक्षिक विषयों से संबंधित कार्यों और जिम्मेदारियों का प्रबंधन करती हैं। इनका क्षेत्र कार्यक्षेत्र विस्तृत है, और शिक्षा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न सलाहकार मंडल, परिषद, और समितियों की स्थापना की गई है।
प्रमुख समितियाँ और परिषद्
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
- स्थापना वर्ष : 3 नवंबर, 1962
- मुख्यालय/स्थान : दिल्ली
- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education)
- स्थापना वर्ष : 1920 (सर्वप्रथम), हार्टोग समिति के सुझाव पर 1935 में पुनर्गठित
- मुख्यालय/स्थान : नई दिल्ली
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT)
- स्थापना वर्ष : 1 सितंबर, 1961
- मुख्यालय/स्थान : नई दिल्ली
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (All India Council for Technical Education - AICTE)
- स्थापना वर्ष : नवंबर 1945
- मुख्यालय/स्थान : दिल्ली
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education - NCTE)
- स्थापना वर्ष : 1995
- मुख्यालय/स्थान : दिल्ली
- केंद्रीय सामाजिक-कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board)
- स्थापना वर्ष : 1953
- मुख्यालय/स्थान : दिल्ली
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (Council of Scientific & Industrial Research - CSIR)
- स्थापना वर्ष : 26 सितंबर, 1942
- मुख्यालय/स्थान : दिल्ली
- अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद् (All India Council For Elementary Education)
- स्थापना वर्ष : 1984
- मुख्यालय/स्थान : दिल्ली
- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC)
- स्थापना वर्ष : 1994
- मुख्यालय/स्थान : बंगलूरू (कर्नाटक)
- राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration - NUEPA)
- स्थापना वर्ष : 1962
- मुख्यालय/स्थान : नई दिल्ली
ये संगठन केंद्र सरकार को शिक्षा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ाने के लिये सुझाव प्रदान करते हैं।
भारत में शैक्षिक प्रशासन और नियंत्रण का विकास
मूल संविधान में शिक्षा को राज्य (State) के विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। कुछ समय पश्चात् वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती (Concurrent) सूची का विषय बना दिया गया अथवा अब शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के महत्त्वपूर्ण विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार अपनी-अपनी सुविधानुसार कानून बना सकते हैं। परंतु कुछ राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर नीति-निर्धारण करने एवं अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये राज्य सरकारों को केंद्र से परामर्श लेना पड़ता है।
वर्ष 1985 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resources Development) के नाम से जाना जाने लगा। पुन: वर्ष 2020 में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह मंत्रालय शिक्षा की समस्त इकाइयों से जुडे़ होने के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंत्रालय के अधीन शिक्षा से जुडे़ अनेक प्रभाग कार्यरत हैं, जो निम्नलिखित हैं-
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा)
- उच्चतर शिक्षा विभाग (विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा)
- तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज कल्याण
- शोध एवं प्रकाशन
- यूनेस्को प्रभाग
- विदेशी शैक्षिक संबंध प्रभाग
- विदेशी छात्रवृत्तियाँ प्रभाग
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रभाग
- केंद्रशासित एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग
|
शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ |
||
|
राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान |
स्थापना वर्ष |
मुख्यालय/स्थान |
|
केंद्रीय हिंदी संस्थान |
1960 |
आगरा (उत्तर प्रदेश) |
|
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान |
1969 |
मैसूर (कर्नाटक) |
|
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय |
15 अक्तूबर, 1970 |
नई दिल्ली |
|
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान |
अगस्त 1957 |
ग्वालियर(मध्य प्रदेश) |
|
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान |
7 मई, 1961 |
पटियाला (पंजाब) |
|
भारतीय विज्ञान संस्थान |
27 मई, 1909 |
बंगलूरू (कर्नाटक) |
|
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान |
1951 |
खड़गपुर (कोलकाता) (प्रथम आईआईटी) |
|
भारतीय प्रबंधन संस्थान |
1961 |
कोलकाता (प. बंगाल) (प्रथम IIM–Indian Institute of |
|
क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज |
1960 |
वारगंल (तेलंगाना) (प्रथम क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज) |
|
इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया |
1981 |
हैदराबाद (तेलंगाना) |
- यह फ्रेमवर्क पूरे देश के संस्थानों की रैंकिंग करने के लिये एक पद्धति की रूपरेखा है।
- इस रूपरेखा का निर्माण शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित कोर कमेटी करती है।
- इस रूपरेखा के पैरामीटर मोटे तौर पर ‘टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज’, ‘रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस’, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी (Inclusivity) तथा ‘परसेप्शन’ को कवर करते हैं।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त इस प्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर, 2015 को की गई।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा (National Institutional Ranking Framework – NIRF), 2023 के अंतर्गत कार्य-निष्पादन के आधार पर विभिन्न वर्गों में संस्थानों की रैंकिंग-
- ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ संस्थान - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- मद्रास,चेन्नई (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ कॉलेज - मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ अभियांत्रिकी संस्थान - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- मद्रास, चेन्नई (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान - भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एज्युकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ आयुर्विज्ञान संस्थान - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ विधि संस्थान - नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बंगलूरू (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ दंत चिकित्सीय संस्थान - सवीता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस, चेन्नई (प्रथम स्थान)
- सर्वश्रेष्ठ वास्तुशिल्प संस्थान - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, उत्तराखंड (प्रथम स्थान)
- सन् 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर भारतीय उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर की जाँच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सन् 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बंगलूरू में स्थित है।
- NAAC का मुख्य अधिदेश (Mandate) उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और इनके विभागों (Department), स्कूलों, संस्थाओं, कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना है। शिक्षण संस्थाओं को मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड A, B और C में प्रत्यायित कर दिया जाता है और जिनका प्रत्यायन नहीं होता है, उन्हें ग्रेड D के अंतर्गत रखा जाता है।
- NAAC का प्रतीक चिह्न वाक्य-उत्कृष्टता (Excellence), विश्वसनीयता (Credibility), प्रासंगिकता (Relevance) है।
- NAAC का मुख्य अधिदेश (Mandate) उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और इनके विभागों (Department), स्कूलों, संस्थाओं, कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना है। शिक्षण संस्थाओं को मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड A, B और C में प्रत्यायित कर दिया जाता है और जिनका प्रत्यायन नहीं होता है, उन्हें ग्रेड D के अंतर्गत रखा जाता है।
- उद्देश्य (Mission)
- विशेष अकादमी कार्यक्रम अथवा प्रोजेक्ट और उच्चतर शिक्षण संस्थानों अथवा इनकी इकाइयों का आवधिक मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना।
- उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकीय शिक्षा (Teaching–Learning) और शोध की गुणवत्ता में बढ़ावा देने के लिये अकादमिक माहौल बनाने में सहायता करना।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्व मूल्यांकन, उत्तरदायित्व, स्वायत्तता, नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- गुणवत्ता मूल्यांकन, उन्नयन और धारणीय स्थिति से संबंधित उच्चतर शिक्षा के विषयों पर उच्चतर शिक्षा के अन्य हितधारकों (Stakeholder) से सहायता लेना।
- NAAC का मूल्य ढाँचा (NAAC's Value-Frame Work)
- NAAC द्वारा निम्नलिखित संकेंद्रक मूल्यों (Core Values) को बढ़ावा दिया गया है :
- राष्ट्रीय विकास में योगदान
- विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण
- विद्यार्थियों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना।
- प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- उत्कृष्टता (Excellence) के लिये खोज।
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में शामिल है।
- यह प्रशासकों एवं सदस्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षाविदों को किसी मामले पर एक-दूसरे के विचारों के आदान-प्रदान के लिये मंच मुहैया कराता है।
- यह उच्चतर शिक्षा में सूचना आदान-प्रदान ब्यूरो (Bureau of Information Exchange) के रूप में कार्य करता है।
- ‘यूनिवर्सिटी हैंडबुक’ नाम से शोध पेपर (Research Paper) और ‘यूनिवर्सिटी न्यूज’ नाम से साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। यह कुछ उपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन भी करता है।
- वर्तमान में इस संघ की सदस्यता 931 है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के 17 एसोसिएट सदस्य हैं
- इस संघ का अधिकांश वित्तपोषण सदस्य विश्वविद्यालयों के वार्षिक चंदे से किया जाता है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देखरेख व विकास संबंधी व्यय के एक हिस्से को पूरा करने के लिये अनुदान प्रदान करता है जिन्हें शोध अध्ययन, कार्यशालाएँ, विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रबोधन कार्यक्रम (Orientation Program) और ग्लोबल विश्वविद्यालय के डाटा बैंक बनाने पर खर्च किया जाता है।
- डी.एस. कोठारी आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ को अंतर्विश्वविद्यालय परिषद् कहा है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालय को इसके सदस्य के रूप में नामित करने का सुझाव दिया था।
प्रत्येक विश्वविद्यालय में पदों की व्यवस्था उस अधिनियम के अनुसार होती है, जिनके द्वारा वे स्थापित होते हैं, परंतु अगर सामान्य तौर पर किसी विश्वविद्यालय के शीर्षस्थ स्तर पर कुलपति (Chancellor), उपकुलपति (Vice Chancellor), प्रो. वाइस चांसलर या रेक्टर, कोर्ट, सीनेट, एक्जीक्यूटिव काउंसिल, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, संकाय (Faculty), बोर्ड ऑफ रिसर्च कमेटी जैसे नामों से नामांकित पद और संस्थाएँ होती हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पद कुलाध्यक्ष (The Visitor) का होता है।
- कुलाध्यक्ष (The Visitor) : केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्य विश्वविद्यालय के संदर्भ में राज्य का राज्यपाल कुलाध्यक्ष (The Visitor) होता है। कुलाध्यक्ष के पद को विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। कुलाध्यक्ष सरकार और विश्वविद्यालय के मध्य महत्त्वपूर्ण कड़ी की तरह काम करता है। कुलाध्यक्ष के पास यह शक्ति होती है कि वह विश्वविद्यालयों से संबंधित किसी भी कार्य का औचक निरीक्षण कर सके।
- कुलाधिपति (The Chancellor) : विश्वविद्यालय की प्रशासकीय सूची में सबसे शीर्षस्थ पद कुलाधिपति (Chancellor) का होता है, जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के आंतरिक मामले से संबंधित संस्था जिसे कोर्ट, बोर्ड ऑफ गवर्नर, सीनेट आदि नामों से जाना जाता है, उनके सदस्यों के द्वारा की जाती है। अधिकांश मामले में इस पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा कोई व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश के पद के समान ही सम्माननीय हो, उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के आंतरिक मुद्दे से जुड़ी शीर्षस्थ प्रशासकीय संस्था अथवा भारतीय राज्य के किसी सम्माननीय पद को कुलपति के रूप में नियुक्त करने की परंपरा भी बना सकती है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति परंपरा बन चुकी है।
- कुलपति (The Vice Chancellor) : कार्यात्मक दृष्टि से विश्वविद्यालय का शीर्षस्थ अधिकारी कुलपति (Vice Chancellor) होता है। प्रशासकीय स्तर के साथ-साथ विश्वविद्यालय के कार्यात्मक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाए रखने की ज़िम्मेदारी कुलपति की होती है, ताकि शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थी सही दिशा में सही लगन के साथ काम करते रहे। कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था अपने विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार करती है।
- रेक्टर अथवा प्रो-वाइस-चांसलर (Rector or Pro-Vice-Chancellor) : कुलपति के कामों के सहायक के तौर पर रेक्टर अथवा प्रो-वाइस-चांसलर की नियुक्ति की जाती है। इस पद का चयन भी विश्वविद्यालय की प्रशासकीय संस्था ही करती है। सामान्यत: विश्वविद्यालय के प्रोपेसरों के बीच से ही किसी सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।
- डीन (Dean) : विश्वविद्यालय में संकाय (Faculty) के शीर्षस्थ पद को डीन (Dean /संकायाध्यक्ष) कहा जाता है। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये तीन प्रशासनिक समितियों का गठन किया जाता है, जो विश्वविद्यालय से जुडे़ सभी विषयों पर आपसी सहमति के आधार पर निर्णय लेते हैं।
- सीनेट (Senate) : यह विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति है। इसका अध्यक्ष कुलपति (Vice–Chancellor) होता है।
- कार्यकारी परिषद् (Executive Council) : सीनेट द्वारा निर्धारित नियमों व नीतियों का क्रियान्वयन कार्यकारी परिषद् द्वारा किया जाता है। इस परिषद् में विश्वविद्यालय की कार्यकारी शक्ति निहित होती है।
- शैक्षणिक परिषद् (Academic Council) : यह विश्वविद्यालय का उच्चतम शैक्षणिक निकाय होता है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव का दायित्व इसी परिषद् के पास होता है। सभी शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद् (Executive Council) को सलाह देने का अधिकार होता है। यह परिषद् पाठ्यक्रम और शोध संबंधी नियमों का भी निर्धारण करती है।
भारत में उच्चतर शिक्षा के अभिशासन को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है-
- विश्वविद्यालय
- कॉलेज
विश्वविद्यालय संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित स्वायत्त संस्था होती है और कॉलेजों का अभिशासन विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है, इसलिये इन्हें विश्वविद्यालयों से संबद्ध (Affiliated to Universities) शिक्षण संस्थान कहा जाता है।
|
कॉलेज और विश्वविद्यालय में अंतर |
||
|
अंतर का आधार |
कॉलेज |
विश्वविद्यालय |
|
अर्थ |
विश्वविद्यालयों से जुडे़ अनेक उच्च शिक्षण संस्थान ‘कॉलेज’ कहलाते हैं। अधिकांश कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध (Affiliated to University) होते हैं और कुछ स्वायत्त भी होते हैं। |
एक विश्वविद्यालय प्राधिकृत (Authorized) शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान होता है जो अपने विद्यार्थियों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करता है। |
|
पाठ्यक्रम |
विश्वविद्यालयों से जुडे़ कॉलेज अपना पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुसार निर्धारित करते हैं और इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की डिग्रियाँ भी विश्वविद्यालयों की ही मिलती है। |
विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम खुद निर्धारित करते हैं। |
|
शोध कार्यक्रम |
कॉलेजों के द्वारा शोध कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जाता। |
विश्वविद्यालयों द्वारा शोध कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाता है। |
|
अध्यक्ष |
कॉलेजों का हेड डीन अथवा डायरेक्टर होता है। |
जबकि विश्वविद्यालय प्रमुख अथवा अध्यक्ष का पद (Vice Chancellor) कुलपति का होता है। |
उपशीर्षक: विश्वविद्यालयों/ विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों का विवरण
विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान कॉलेजों के रूप में उच्चतर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आज़ादी के बाद बढे़ स्तर पर वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 में विश्वविद्यालय की कुल संख्या 20 थी। 31 मार्च, 2023 तक तक यह संख्या बढ़कर लगभग 1085 हो गई, मतलब यह है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग कई गुना वृद्धि हुई है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में हुई वृद्धि से विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से बढे़ हैं, जो अध्ययन का सर्वोच्च स्तर है।
उच्चतर शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों की साझा ज़िम्मेदारी है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मानकों का समन्वय और निर्धारण यूजीसी और अन्य सांविधिक निकायों (Statutory Regulatory Bodies) को सौंपा गया है। केंद्र सरकार यूजीसी को अनुदान देती है और देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं की स्थापना करती है। केंद्र सरकार यूजीसी की सिफारिश पर शैक्षिक संस्थाओं को ‘सम विश्वविद्यालय’ (Deemed University) घोषित करने के लिये भी ज़िम्मेदार है।
वर्तमान में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं के मुख्य घटक निम्नवत् हैं-
- केंद्रीय विश्वविद्यालय(Central University): वर्तमान में (1 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार) केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालयों की संख्या 56 है।
- राज्य विश्वविद्यालय(State Universities): प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय को ‘राज्य विश्वविद्यालय’(State University) कहा जाता है। वर्तमान में (1 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार) कुल 482 राज्य विश्वविद्यालय थे, जिनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(b) के तहत शामिल राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 253 है।
- सम विश्वविद्यालय(Deemed Universities): विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा के संस्थान(जो विशेष क्षेत्रों, जैसे कि मेडिकल, शारीरिक, भाषाओं, सामाजिक विज्ञान, वन शोध, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में) जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में ऊँचे मानक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें यूजीसी की सलाह पर केंद्रीय सरकार द्वारा ‘सम विश्वविद्यालय’ संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकता है।वर्तमान में (1 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार) कुल 124 सम (डीम्ड) विश्वविद्यालय थे, जिनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(b) के तहत शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या 44 है।
- राज्य निजी विश्वविद्यालय(State Private Universities): राज्य निजी विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय है, जिसे प्रायोजित निकाय (Sponsored Bodies), जैसे कि कोई सोसाइटी, जिनका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत होता है, कोई पब्लिक ट्रस्ट या कंपनी जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार होता है आदि के माध्यम से केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियमों के अधीन स्थापित किया गया है। राज्य निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी विनियम 2003 द्वारा विनियमित किया गया है। वर्तमान में (1 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार) कुल 475 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(b) के तहत शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या 26 है।
स्रोत : UGC वेबसाइट
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी अधिनियम के खंड 12 (CCC) के तहत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र को स्थापित करता है, जिनके उद्देश्य निम्नवत् हैं :
- उन विश्वविद्यालयों को समान उन्नत केंद्रीय सुविधाएँ व सेवाएँ प्रदान करना, जो अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में समर्थ नहीं है।
- संपूर्ण देश में शिक्षक और अनुसंधानकर्त्ताओं (Researchers) को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- अनुसंधान और शिक्षक समुदाय के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान आधुनिक उपकरणों और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना।
नई दिल्ली में स्थित परमाणु विज्ञान केंद्र अब ‘इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर’ सेंटर कहलाता है। यह 1994 में स्थापित देश का पहला अनुसंधान केंद्र था। विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत देश में 7 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कार्य कर रहे हैं, जो निम्नवत् हैं-
- इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेरेटर सेंटर (पूर्व- न्यूक्लियर साइंस सेंटर), नई दिल्ली
- इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स (IUCAA) पुणे, महाराष्ट्र
- यूजीसी- डी.ए.ई. कॉन्सोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च (UGC-DAECSR)- इंदौर (मध्य प्रदेश)
- सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET)- अहमदाबाद (गुजरात)
- कॅान्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (CEC)- नई दिल्ली
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (NAAC)- बंगलूरू (कर्नाटक)
- अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र (IUTEC)- काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश)
- डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन् 1948 में बने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था में मौजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्था को भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के लिये स्वीकार किया गया, जिसे 1956 में वैधानिक मान्यता मिली।
- 28 दिसंबर, 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 6 है। यह बंगलूरू, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ मुख्यालय नई दिल्ली से कार्य करता है।
- यूजीसी का आदर्श वाक्य ‘ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये’ है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ज़िम्मेदारियाँ
- यूजीसी के पास देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी होने का अनूठा गौरव है, जिसे दो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं :
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उचित निधियों का आवंटन करना।
- विश्वविद्यालय की शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और देख-रेख की ज़िम्मेदारी।
- विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों को निर्धारित करना और बनाए रखना।
- शिक्षा के न्यूनतम स्तर के लिये विनियमों की रूपरेखा तैयार करना।
- कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा पर निगरानी रखना।
- विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक उपायों के लिये केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना तथा सरकार एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच महत्त्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करना
आयोग के सदस्य
- आयोग में सम्मिलित होंगे :
- एक अध्यक्ष
- एक उपाध्यक्ष
- कुल 10 सदस्य (सचिव उच्चतर शिक्षा, सचिव व्यय एवं 8 अन्य सदस्य), इन सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- यूजीसी के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित है।
इसके साथ यह आवश्यक है कि कुल सदस्यों में कम-से-कम आधे सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के द्वारा भारतीय सरकार के कामों को सुविधाजनक बनाने के लिये मंत्रालयों की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से शिक्षा मंत्रालय की भी स्थापना हुई। इस मंत्रालय ने अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिये दो विभाग- स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा को स्थापित किया। इस प्रकार उच्चतर शिक्षा से जुडे़ मसलों की सबसे शीर्ष संस्था शिक्षा मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग बना। नीति और आयोजना के स्तर पर भारत में उच्चतर शिक्षा के लिये आधारभूत संरचना मुहैया कराने हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) जिम्मेदार है। इस तरह विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया कराने के लिये विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कॉलेजों तक भारतीय शिक्षण संस्थानों की पहुँच बनाने की ज़िम्मेदारी भी उच्चतर शिक्षा विभाग के पास है।
- ध्येय (Vision)
- समान और समावेशी रूप से भारत के मानव संसाधन की अभीष्टतम क्षमता को उच्चतर शिक्षा से प्राप्त करना।
- लक्ष्य (Mission)
- सभी पात्र व्यक्तियों को तथा विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों को समानता के साथ उच्चतर शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करना।
- उच्चतर शिक्षा में मौजूद क्षेत्रीय तथा अन्य असंतुलन को दूर करने की कोशिश करना। सभी प्रकार के संगठनों की सहायता में भागीदार बनना।
- अनुसंधान तथा नवप्रवर्तनों को मज़बूत करने के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम आरंभ करना और इस हेतु निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन देना।
- उद्देश्य (Objectives)
- उच्चतर शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) 2011–12 तक 15 प्रतिशत, 2016-17 तक 21 प्रतिशत और 2020 तक 30 प्रतिशत करना।
- उच्चतर संस्थाओं के मौजूदा आधारभूत अवसंरचना में वृद्धि करना।
- सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्चतर शिक्षा का अवसर प्रदान करना।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध सुविधाओं में सुधार कर ज्ञान अर्जन करने की शर्त रखना।
- सर्वसुलभ ज्ञान की उन्नति तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- भारतीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा देना।
- उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता, नवाचार और शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देना।
इस समिति का गठन डॉ. यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में बच्चों पर एकेडेमिक बोझ कम करने हेतु की गयी थी। इसने 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बच्चों और अध्यापकों के अनुपात को कम करने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गृह कार्य की प्रथा समाप्त करने, रटने पर बल समाप्त करने हेतु क्विज टाइप प्रश्नों को प्रचलन में लाने, शैक्षिक नवाचारों हेतु स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम और पर्यवेक्षण का विकेंद्रीकरण करने पर जोर दिया।
डॉ. यशपाल समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ :
- स्कूली बच्चों को स्कूल में भारी किताबें ले जाने की बाध्यता नहीं होनी चाहिये।
- नर्सरी दाखिले के लिये साक्षात्कार प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिये।
- शिक्षक-छात्र अनुपात को कम से कम 1:30 निर्धारित किया जाए।
- ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर शिक्षा समितियों के गठन की सिफारिश की।
- प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाना चाहियेऔर यहां तक कि उच्च कक्षाओं के लिये भी, यह गैर-पाठ्यात्मक होना चाहिये।
- सीबीएसई का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों तक ही सीमित होना चाहिये, और अन्य सभी स्कूल संबंधित राज्य बोर्डों से संबद्ध होने चाहिये।
- पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिये और इसमें अधिक शिक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- व्यावसायीकरण से बचने के लिये निजी स्कूलों को मान्यता देने के नियम और अधिक सख्त होने की जरूरत है।
- समिति ने शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के लिये कई कदमों की भी सिफारिश की।
नोट : अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार बच्चों के कंधे पर उनके कुल वज़न का 10 फ़ीसदी से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिये। देश के चिल्ड्रन्स स्कूल बैग एक्ट, 2006 के तहत भी बच्चों के स्कूल बैग का वज़न उनके शरीर के कुल वज़न का 10 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिये।
परिचय
शैक्षिक पुर्ननिर्माण की दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रथम बड़ा प्रयास प्रो० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता के अन्तर्गत शिक्षा आयोग (1964-66) का गठन किया । शिक्षा आयोग को शिक्षा के राष्ट्रीय अनुक्रम पैटर्न और सभी स्तरों पर और सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिये सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिये आदेश किया गया था। यह भारत में स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा से जुडे महत्वपूर्ण आयोगों में से प्रमुख आयोग था।
शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ :
- आयोग ने कई पथ-प्रदर्शक सिफारिशें कीं, पहले ही वाक्य में आयोग ने माना कि "भारत का भाग्य अब अपने कक्षाओं में आकार ले रहा है" (पाठ. 1, पैरा 1.01), जो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है।
- राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये आयोग ने उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने के लिये सिफारिश की ।
- शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने के लिये आयोग द्वारा कुछ उपायों की सिफारिश की गई थी - विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी घटक के रूप में विज्ञान का परिचय; सभी - प्रकार की शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव की शुरूआत; माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण; और विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर बल ।
- सार्वजनिक शिक्षा की एक समान विद्यालय प्रणाली शुरू की जानी चाहिये।
- आयोग ने सिफारिश की है कि पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, शिल्प शेड, आदि पूरे वर्ष भर खुला होना चाहिये और कम से कम एक दिन के आठ घंटे उपयोग किया जाना चाहिये।
- शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का 6 प्रतिशत खर्च करना ।
- इस अवस्था में प्रतिभाशाली छात्रों के पहचान के लिये उपयुक्त तकनीकों का विकास करना चाहिये।
- आयोग ने शिक्षा, इसकी विषयवस्तु, विकास के विस्तार और योजना आदि की भूमिका में बहुमूल्य योगदान दिया। भारत में मौजूद शिक्षा प्रणाली बहुत सीमा तक, इस रिपोर्ट से अपनी प्रेरणा प्राप्त करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) भी काफी सीमा तक इस पर आधारित है। आयोग ने स्वतंत्र भारत के संविधान में निर्धारित आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के आदर्शों और बहुमूल्य आगे आने वाले शैक्षिक पुनर्निर्माण के पूरे कार्यक्रम पर विचार किया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में महिलाओं की शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में वर्ष 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया था। यह भारत में स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा से संबद्ध महत्वपूर्ण समितियों में प्रमुख थी।
इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी :
- स्वतंत्रता के बाद दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में यह पहली समिति थी। इसने विशेषतः ऐसे विद्यालयों में जहाँ कोई अध्यापिका नहीं थी वहाँ अध्यापिकाओं की नियुक्ति और महिला शिक्षा के पक्ष में जनमत को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों की सिफारिश की।
- पाठ्यक्रम के संबंध में समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिये संपूर्ण शिक्षा के मध्य बिन्दु (मिडिल स्कूल) तक एक जैसे पाठ्यक्रम की सिफारिश की।
- समिति ने माध्यमिक स्तर पर सहशिक्षा की अनुशंसा की।
- इसने जेंडर संबंधी प्रतिरूपी चित्रण की पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करनें की भी सिफारिश की।
- वयस्क महिलाओं के लाभार्थ, सभी राज्यों में सघन पाठ्यक्रम आरंभ किये जाने थे ताकि वे माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में भाग ले सकें।
समग्रतः समिति ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर के संबंध में महिलाओं की आवश्यकता के संदर्भ में विस्तृत दृष्टि प्रदान की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में समानता लाने को उच्च प्राथमिकता दिये जाने की अनुशंसा की। Top of Form
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुधार के लिये सुझाव देने हेतु आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में इस समिति का गठन किया गया। आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित थी :
- समिति ने सुझाव दिया कि महिलाओं की शिक्षा के लिये, सभी स्कूल-आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आंतरिक निगरानी के कार्य की जिम्मेदारी पंचायती राज ढाँचे में स्थित शैक्षिक परिसरों को सौंपने का सुझाव दिया।
- संस्थागत स्तर पर, प्राथमिक / मध्य / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुख को सूक्ष्म स्तर की योजना और लड़कियों की शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये।
- यह भी सिफारिश की गई थी कि सभी स्कूल पाठ्य-पुस्तकें, दोनों NCERT / SCERT और अन्य प्रकाशकों द्वारा, महिलाओं और लैंगिक रूढ़ियों की अयोग्यता को समाप्त करने के लिये समीक्षा की जाए ।
- इसके साथ ही, इस बात पर बल दिया गया कि योजना और प्रबंधन का विकेंद्रीकृत और भागीदारी मोड शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं की चुनौती का जवाब देने के लिये एक प्रभावी आधार प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं की शिक्षा भी सम्मिलित है।
इस समिति ने शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य स्कूल प्रणाली, कार्य हेतु व्यक्तियों का सशक्तीकरण,स्कूली विश्व व कार्य स्थल में संबंध स्थापित करना, परीक्षा सुधार, मातृभाषा को स्थान,स्त्रियों की शिक्षा, धार्मिक अंतरों को कम करना, शैक्षिक उपलब्धि, अवसरों आदि के संदर्भ में बुनियादी सुधार संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे।
मुदलियार आयोग का गठन
- भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पाठ्यक्रम निर्धारण तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु शैक्षिक संरचना में बदलाव की आवश्यकता महसूस की। इसलिये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार ने 23 सितंबर, 1952 को डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं की वर्तमान स्थिति पर जांच करने तथा उसमें सुधार के लिये अनुशंसाओं सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। यह भारत में स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण आयोगों में एक था।
माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी-
- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्रस्तावित किया जिसमें चरित्र निर्माण, लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करना, आर्थिक और व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व को बढ़ावा देना और हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना सम्मिलित था।
- इसमें दिव्यांग और पिछड़े बच्चों के लिये विद्यालय खोलने पर बल दिया गया है।
- आयोग ने उद्योगों के निकट बड़ी संख्या में तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया।
- उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर विषय अनिवार्य रहे, जैसे- गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि।
- 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से जोड़ दिया जाए तथा बहु-उद्देशीय विद्यालय स्थापित किये जाएँ।
- आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के बारे में महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की।
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मूल्यांकन का भी सुझाव दिया।
संसद द्वारा आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णता स्वीकार कर लिया गया। आयोग ने विद्यार्थियों के लिये कृषि शिक्षा पर बल देने, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया। इसने शिक्षा प्रणाली में सुधाार के लिये महत्वपूर्ण उपाय सुझाए, जिनका माध्यमिक शिक्षा पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये शिक्षा की व्यवस्था को फि़र से उन्मुख करने का प्रथम प्रयास भारत सरकार द्वारा डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के माध्यम से किया गया था । यह भारत में स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा से जुडे प्रमुख आयोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोग था।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी-
- ज्ञान को विकसित करके जीवन जीने की जन्मजात योग्यता को जागृत करना।
- सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाना व लोकतंत्र के लिये प्रशिक्षित करना।
- विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिये।
- स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष हो।
- विद्यालयी शिक्षा के 10 से 12 वर्षों के बाद छात्रों को अलग-अलग व्यवसाय में स्थानांतरित करने हेतु बड़ी संख्या में व्यावसायिक संस्थान खोले जा सकते हैं ।
- विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने शिक्षण और परीक्षाओं के उच्चतम मानक को बनाए रखना है।
- देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देख-रेख के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए।
- इस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिये पूर्व के ज्ञान तथा प्रज्ञा एवं पश्चिम के प्राचीन तथा आधुनिक समाज का विश्लेषण किया। तदनुसार अपने पाठ्यक्रम पर अपनी सिफ़ारिशें दीं।
वर्ष 2017 में UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 23वाँ सम्मेलन बॉन, जर्मनी में आयोजित किया गया। इसे COP-23 भी कहते हैं। अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते से अपना नाम वापस लेने के बाद वार्ता का यह प्रथम प्रयास है। यह वार्ता पेरिस समझौते की कार्य योजना को पूर्ण करने पर आधारित थी। इस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य उपलब्धियाँ थीं-
- 2018 तालानोवा वार्ता का शुभारंभ : इसके तहत पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्रगति के संबंध में पार्टियों के सामूहिक प्रयासों की समीक्षा की जाएगी तथा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDC) की तैयारियों के संबंध में सभी को सूचित करना ज़रूरी होगा।
- बिलो 50 इनिशिएटिव : इसे वर्ल्ड बिजनेस कॉउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (WBCSD) द्वारा आरंभ किया गया। इसका लक्ष्य ऐसे ईंधन के लिये मांग और बाज़ार का निर्माण करना है जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में 50% कम CO2 का उत्सर्जन करें।
- जेंडर एक्शन प्लान : देशों ने पहली बार जेंडर एक्शन प्लान को अंतिम रूप प्रदान किया जिसका उद्देश्य सभी UNFCCC प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।
- लोकल कम्युनिटीज एवं इंडीजेनस पीपल्स के लिये मंच की स्थापना : यह मंच स्थानीय समुदायों एवं मूल निवासियों के लिये जलवायु वार्ता में प्रत्यक्ष एवं व्यापक तरीके से मदद पहुँचाकर, भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ताकि वो अपने परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर सकें। यह वर्ष 2018 से कार्य करना प्रारंभ कर देगा।
- कृषि में ऐतिहासिक प्रगति : ‘कृषि पर कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क’ ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार जलवायु वार्ता में देश किसी कृषि पर समझौते पर राजी हुए।
- कोयला संबंधी पूर्व संधियों को सशक्त बनाना : कनाडा एवं यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में एलायंस का निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत 2030 तक कोयले के उपयोग में कमी लानी थी।
वारसा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2013 (COP-19) पोलैंड की राजधानी वारसा में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसमें भाग लेने वाले देशों ने वार्ता के गतिरोध को दूर किया एवं 2015 तक एक सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने हेतु एक रूपरेखा तय की। हालाँकि यह EU की मूल आशाओं पर खरा नहीं उतरा लेकिन अधिकांश विकासशील देशों को यह स्वीकार्य था।
सरकारों ने इंटेन्डेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (INDC-Intended Nationally Determined Contribution) की घरेलू तैयारी करने का निर्णय लिया ताकि दिसंबर 2015 से पहले उसे तैयार कर लिया जाए। इसे एक स्पष्ट एवं पारदर्शी तरीके से संपादित करने को कहा गया। इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लिये गए-
- डरबन प्लेटफार्म को आगे बढ़ाना
- ग्रीन क्लाइमेट फंड
- दीर्घ अवधि वित्त
- REDD+ हेतु वारसा फ्रेमवर्क
- क्षति एवं नुकसान हेतु वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र
वारसा सम्मेलन के अन्य परिणाम
- 2020 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर को गतिशील करने हेतु प्रयासों को मज़बूती प्रदान करना : विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को सार्वजनिक एवं निज़ी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले हेतु 2020 तक 100 बिलियन डॉलर देने के प्रयास पर सहमति बनी, जो 2014 से 2020 की अवधि में प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाना निर्धारित किया गया।
- हरित जलवायु निधि (Green Climate Fund) : इस निधि को व्यवसाय हेतु खोल दिया गया एवं 2014 के मध्य से इसने काम करना शुरू कर दिया।
- प्री-2020 एम्बिशन गैप को खत्म करना : सरकारों ने एम्बिशन गैप को खत्म करने हेतु उपायों को मज़बूती प्रदान करने पर विचार किया।
- उत्तरदायित्व में प्रगति : विकासशील देशों द्वारा कटौती प्रयासों के मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन हेतु तैयार फ्रेमवर्क अब पूरी तरह सक्रिय हो गया। इसके द्वारा देशों की संपोषणीयता प्रयासों को अब अच्छी तरह मापा जा सकेगा।
- जलवायु परिवर्तन पर कार्य हेतु तकनीकी को बढ़ावा : CTCN अब पूरी तरह सक्रिय चरण की तरफ बढ़ चुका है, जिससे विकासशील देशों के कार्यों को मदद मिल सकेगी। CTCN द्वारा विकासशील देशों की तरफ से तकनीकी विकास एवं तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दों पर मदद मिलने के अनुरोध को अब सहायता मिल सकेगी।
UNFCCC के अंतर्गत COP-17 सम्मेलन का आयोजन डरबन में 2011 में संपन्न हुआ। यह अपने किस्म का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने काफी संतुलित तरीके से प्रगति की,जिसमें कन्वेंशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल, बाली एक्शन प्लान एवं कानकुन समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।
इसके मुख्य परिणामों में पार्टीज द्वारा लिया गया एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सम्मिलित है जिसमें 2015 के पहले तक, जल्द-से-जल्द जलवायु परिवर्तन पर एक सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात कही गई। साथ ही इस कानूनी समझौते को 2020 तक स्थापित करने की बात भी कही गई। इस समझौते के अनुसार GHG के उत्सर्जन में कटौती के लिये सभी विकसित एवं विकासशील देश अपने दायित्वों को निभाएंगे। इस कानूनी उपकरण के विकास हेतु इस अधिवेशन में ADP (Ad-hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action) की स्थापना की गई।
एडीपी-[ADP (Ad-hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action)]
यह एक सहायक निकाय है जिसकी स्थापना COP-17 में दिसम्बर 2011 में हुई थी। इस ADP को एक प्रोटोकॉल का विकास करना था जो कि एक अन्य कानूनी उपकरण या कन्वेंशन के अंतर्गत कानूनी बाध्यता युक्त एक सहमतिपूर्ण परिणाम था। इसे सभी पार्टियों के लिये उपयुक्त होना ज़रूरी था। इसका विकास 2015 के पहले तक पूरा कर लेना था ताकि COP-21 (2015) तक इसे अपना लिया जाए। जिससे यह 2020 से प्रभावी एवं क्रियान्वित हो सके।
यह 2012 के प्रथम मध्य हेतु अपने कार्यों की योजना बनाएगा जिसमें शमन, अनुकूलन, योजना, तकनीकी विकास एवं हस्तांतरण, कार्यों की पारदर्शिता एवं समर्थन तथा क्षमता-विकास, पार्टियों द्वारा प्रस्तुतीकरण करवाना एवं प्रासंगिक तकनीकी, सामाजिक तथा आर्थिक सूचनाएँ सम्मिलित हैं।
- 1 जनवरी, 2013 को प्रारंभ होने वाली ‘क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि’ की स्थापना पर सहमति इस सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि में 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की आठ वर्षों की अवधि में औद्योगीकृत व विकसित देशों द्वारा 1990 के स्तर से कम-से-कम 18% की कटौती की बात कही गई।
- इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया।
- भारत UNFCCC के CBDR (समान लेकिन विभेदी ज़िम्मेदारी) अर्थात् समानता के सिद्धांत के अनुपालन की अपनी मांग पर दृढ़ रहा। जिसमें भविष्य की वार्ताओं अर्थात् आगे किसी भी नए जलवायु व्यवस्था में समानता के सिद्धांत को शामिल करना निहित था।
- कानकुन करार के अंतर्गत प्रावधानित, GCF (Green Climate Fund) की वास्तविक स्थापना इसी सम्मेलन द्वारा की गई। साथ ही इसके निर्माण कार्य में प्रगति हेतु एक प्रबंधन ढाँचा को अपनाया गया।
ओज़ोन परत, समतापमंडल (स्ट्रेटोस्फीयर) में मुख्यत: 15 से 30 किमी. की उँचाई पर अवस्थित है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (अल्ट्रा-वायलेट) किरणों को अवशोषित कर जीव समुदायों, विशेषकर: मनुष्यों को त्वचा कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से बचाती है। किंतु ओज़ोन परत का दिनों-दिन क्षरण होता जा रहा है।
- क्लोरो-फ्लोरोकार्बन(CFC) ओज़ोन परत के क्षरण के लिये प्रमुख उत्तरदायी गैस है। इसका प्रयोग रेफ्रीजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे आदि में होता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, हैलोन्स आदि रसायन भी ओज़ोन परत के क्षरण हेतु ज़िम्मेदार हैं।
- 1987 में निर्मित तथा 1989 से प्रभावी ‘मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल’ ओज़ोन परत संरक्षण से संबंधित है।
- विश्व ओज़ोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है।
- समतापमंडल के अतिरिक्त वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात् क्षोभमंडल में भी ओज़ोन पाई जाती है। पर्यावरणीय दृष्टि से समतापमंडल की ओज़ोन लाभदायक है, जबकि क्षोभमंडल की ओज़ोन हानिकारक है, क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करती है एवं स्मॉग का निर्माण करती है, जो श्वसन के लिये हानिकारक होता है।
अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर सर्वाधिक ओज़ोन क्षरण के तीन कारण हैं-
- ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल (PSCs)
- ध्रुवीय भँवर (Polar Vortex)
- सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव (Active Chlorine Effect)
- ओज़ोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है, जहाँ पर ओज़ोन गैस उपस्थित रहती हो, बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर समतापमंडल में ओज़ोन अपघटित क्षेत्र है, जो दक्षिणी गोलार्द्ध में बसंत ऋतु (अगस्त-अक्तूबर) के आरंभ होने पर घटित होता है।
- वायुमंडल में ओज़ोन का सांद्रण करीब 300 डॉबसन यूनिट है। कोई क्षेत्र जहाँ का सांद्रण 220 डॉबसन यूनिट से नीचे गिर जाता है, वह ओज़ोन छिद्र का भाग माना जाता है।
- भारत ने ओज़ोन परत के संरक्षण हेतु 1991 में वियना कन्वेंशन पर तथा ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में 1992 में मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये।
जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होती है। मौसमी प्रतिरूप में लंबे समय के परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन सामान्यत: तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है, जो कई वर्षों में होता है। जलवायु परिवर्तन के भयंकर दुष्परिणामों से बचने के लिये विश्व के सभी देशों में यह सहमति बनी है वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2०C से नीचे और तापमान की वृद्धि को 1.5०C तक सीमित रखा जाए।
जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Climate Change)
जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। औद्योगीकरण से पहले इस प्रक्रिया में मानवीय कारकों की भूमिका कम थी। औद्योगीकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया तथा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक तापन व प्रदूषण के रूप में गंभीर समस्या सामने आई। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारक निम्नलिखित हैं-
- प्राकृतिक कारक (Natural Factors)
- वायुमंडल सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है, जिस कारण मौसम एवं जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ में अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन परिवर्तन होते रहते हैं। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन हज़ारों वर्षों तक स्थायी रहते हैं एवं अत्यंत धीमी गति से घटते हैं। सौर विकिरण में विभिन्नता, सौरकलंक चक्र, ज्वालामुखीय उद्भेदन, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं।
- मानवजनित कारक (Anthropogenic Factors)
- वर्तमान जलवायु परिवर्तन मानव जनित समस्या है। मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से पर्यवरण को प्रभावित करता है। मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्यों एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है। इस तरह की समस्याएँ पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं। मानवजनित कारक और उनका जलवायु परिवर्तन में योगदान-
- संसाधनों का दुरुपयोग
- नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगीकरण
- जीवाश्म ईंधन का प्रयोग
- भूमि-उपयोग में बड़े पैमाने पर बदलाव
- जलवाष्प, CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों (CH4, N2O, CFC) में वृद्धि
- समतापमंडल में ओज़ोन का ह्रास
- तापमान में वृद्धि
2009 में COP का 15वाँ अधिवेशन कोपेनहेगन में संपन्न हुआ। साथ ही यह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत Annex-1 पार्टीज के लिये आगे की प्रतिबद्धता हेतु एड-हॉक वर्किंग ग्रुप (AWG-KP) का 10वाँ सम्मेलन था एवं AWG-LCA का 8वाँ अधिवेशन था। कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ने जलवायु परिवर्तन नीति को उच्चतम राजनैतिक स्तर तक बढ़ाया।
- समझौते के प्रमुख बिंदु
- इस सम्मेलन ने प्रभावशाली वैश्विक जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण हेतु बातचीत को आगे बढ़ाया जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के CDM का संवर्द्धन भी सम्मिलित था।
- इसने कोपेनहेगन एकार्ड (Copenhagen Accord) को जन्म दिया, जिसने (लघु एवं दीर्घ अवधि में) कार्बन कटौती एवं जलवायु परिवर्तन जवाबदेही हेतु एक स्पष्ट राजनैतिक इरादे को व्यक्त किया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा बेसिक देशों (BASIC Countries- Brazil, South Africa, India, China) के बीच GHG के उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु ऐतिहासिक अर्थपूर्ण समझौता था।
- इस कोपेनहेगन एकार्ड की प्रकृति गैर बाध्यकारी थी क्योंकि विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य असामंजस्य होने की वजह से COP-15 एक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौते (Legally Binding Agreement) का रूप नहीं ले सका।
- इस समझौते के तहत महत्तम वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि, पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2ºC से ज़्यादा न हो, इसकी बात की गई। इसे सीमित करने हेतु एक दीर्घ अवधि लक्ष्य की स्थापना हो, जिसका 2015 में पुनर्निरीक्षण हो। साथ ही इसमें एनेक्स-1 देशों (विकसित देश) को 2020 तक हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिये एक निश्चित लक्ष्य तैयार करना था। विकासशील देशों को राष्ट्रीय स्तर पर GHG के उत्सर्जन दर में कमी लाने के लिये कुछ कटौती संबंधी ऐच्छिक प्रयास करने थे परंतु वे इस कटौती हेतु शर्तों से बंधे नहीं थे। हालाँकि इसे व्यवहारिक रूप में कैसे संपादित किया जाए इस पर कोई सहमति नहीं बनी। इसमें एक और मांग जोड़ी गई कि महत्तम तापमान वृद्धि को 1.5ºC से नीचे रखा जाए। यह मांग सुभेद्य विकाशील राष्ट्रों द्वारा की गई थी।
- 4 नए निकायों की स्थापना-
- REDD+ पर एक तंत्र का विकास
- COP के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय पैनल जो वित्तीय प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन करे
- कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund)
- एक प्रौद्योगिकी तंत्र (Technology Mechanism)
इस सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक उनके हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु एक लक्ष्य को तय करने पर सहमति जताई। विकासशील देशों ने उनके उत्सर्जन में कमी हेतु राष्ट्रीय रूप से उचित कटौती रणनीतियों (Mitigation Strategies) के अनुकरण करने को स्वीकारा लेकिन कार्बन उत्सर्जन की कमी हेतु प्रतिबद्धता की ज़रूरत को नहीं स्वीकार किया।
भारत में लुप्त हो रहे महत्त्वपूर्ण जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिये 1973 में जीव संरक्षण के प्रयास शुरू किये गए। इसके अंतर्गत तेज़ी से लुप्त हो रही प्रजातियों के लिये संरक्षित क्षेत्र बनाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है। लुप्त हो रहे महत्त्वपूर्ण जीवों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं-
- प्रोजेक्ट टाइगर : 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ (जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है) के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। इसी के अंतर्गत टाइगर रिज़र्व की स्थापना की गई, जो फिलहाल 55 हैं।
- प्रोजेक्ट एलीफेंट : 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करना था।
- हाथियों को उनके बृहद् पर्यावास से जोड़ने वाला सँकरा रास्ता हाथी गलियारा (Elephant Corridor) कहलाता है।
- हाथियों की अवैध हत्या को रोकने हेतु दक्षिण एशिया में 2003 में साइट्स द्वारा माइक (MIKE) कार्यक्रम शुरू किया गया। The Ministry of Environment and Forests (MoEF) एवं Wildlife Trust of India (WTI) द्वारा 2011 में ‘हाथी मेरे साथी’ अभियान शुरू किया गया।
- गंगा डॉल्फिन : इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना आदि नदी तंत्र में पाई जाती है। यह मीठे जल की प्रजाति है।
- हंगुल परियोजना : इसे ‘कश्मीर स्टैग’ भी कहते हैं, जो केवल कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। इसे जम्मू और कश्मीर IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया।
- मगरमच्छ संरक्षण परियोजना : मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1975 में इसे बनाया गया।
- गैंडा परियोजना : इसे 1987 में शुरू किया गया एवं 2005 में ‘इंडियन राइनो विजन 2020’ प्रारंभ किया। एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं।
- गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट : गिद्धों के संरक्षण हेतु 2011 में SAVE (Saving India’s Vulture Extinction) प्रारंभ किया गया।
- लाल पांडा परियोजना-1996 : पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु
- हिम तेंदुआ योजना-2009 : हिमालयी राज्यों में तेंदुआ संरक्षण
विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जिसे ‘हॉटस्पॉट क्षेत्र’ कहते हैं। हॉटस्पॉट की संकल्पना को पर्यावरणविद् नार्मन मायर्स ने 1988 में विकसित किया। किसी स्थान को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड-
- इस क्षेत्र में विश्व की कम-से-कम 0.5% या 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिये।
- इस क्षेत्र की प्राथमिक वनस्पतियों का कम-से-कम 70% नष्ट हो चुका हो।
उपर्युक्त कारकों को सम्मिलित करते हुए विश्व के जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है, वे अत्यधिक हॉटस्पॉट (Hottest Hotspots) क्षेत्र कहलाते हैं। इनके विनाश का भी खतरा अधिक है। इस वर्ग में विश्व के 8 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को रखा जाता है-
1. मेडागास्कर, 2. फिलीपीन्स, 3. सुंडालैंड, 4. ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र, 5. कैरेबियन, 6. इंडो-बर्मा, 7. पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, 8. तंजानिया/केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र।
भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र (India's Leading Hotspots)
भारत के चार क्षेत्र विश्व के जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं-
- हिमालयी क्षेत्र : एक सींग वाला गैंडा, एशियाई जंगली भैंसा, सुनहरा लंगूर, हिमालय का ताहर, गंगा की डॉल्फिन, नामदफा उड़ने वाली गिलहरी।
- इंडो-बर्मा क्षेत्र : बंदर, लंगूर, गिब्बन आदि कपियों का आवास क्षेत्र। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र, म्याँमार, थाइलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं दक्षिणी चीन आता है।
- पश्चिमी घाट और श्रीलंका : दक्षिण-पश्चिमी भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिम के उच्च भूमि क्षेत्र तक फैला हुआ है। एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर, शेर पूँछ वाला बंदर (मकाक) आदि कुछ विशेष प्रजातियाँ हैं।
- सुंडालैंड क्षेत्र : दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित इंडो-मलाया द्वीप समूह के पश्चिमी भाग तक फैला है। भारत का निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आता है। प्रवाल, व्हेल, समुद्री गाय (ड्यूगॉन्ग) आदि विशेष प्रजातियाँ हैं।
होप स्पॉट (Hope Spot)
‘होप स्पॉट’ सागरों के ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्र जैव-विविधता से समृद्ध होने के अलावा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा किसी समुदाय के लिये आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में ‘मिशन ब्लू’ के अंतर्गत डॉ. साल्विया अर्ल ने किया तथा इसे IUCN के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। भारत के दो क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप को 2013 में इसके अंतर्गत नामित किया गया है।
यह जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था। 1992 के सम्मेलन से संबंधित देश UNFCCC में शामिल हो गए ताकि साथ मिलकर औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोका जा सके एवं उसके प्रभावों का मुकाबला किया जा सके। यह कन्वेशन 21 मार्च, 1994 से कार्य करने लगा। वर्तमान में इसकी (सदस्यता) सार्वभौमिक के करीब है। जिन 197 देशों ने कन्वेंशन को सत्यापित (Ratified) किया है, वे पार्टीज़ टू द कन्वेंशन (Parties to the Convention) कहलाते हैं जबकि 165 देश इस फ्रेमवर्क के हस्ताक्षरकर्त्ता बने।
सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें
- समस्या के अस्तित्व का पहचाना जाना : जब 1994 में UNFCCC कार्यशील हुआ था तो आज की अपेक्षा उस समय मानव जनित जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी कम वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद थे। इस स्थिति पर इसने मांट्रियल प्रोटोकॉल को आदर्श बनाते हुए (वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद मानव हित में कार्य करने हेतु) कुछ निश्चित नियम रूप को अपनाया।
- विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण : इस कन्वेंशन का अंतिम उद्देश्य हरितगृह गैसों की सांद्रता को स्थिर करना एवं इसे इस स्तर पर रखना जिससे जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके।
- लक्ष्य के रोडमैप का नेतृत्व करने हेतु विकसित देशों पर दायित्व : चूँकि अतीत एवं वर्तमान के अधिकांश हरितगृह गैसों के उत्सर्जन स्रोत विकसित औद्योगिक देश रहे हैं, अत: अपने घरेलू क्षेत्र में ज़्यादातर उत्सर्जन कटौती की अपेक्षा उन्हीं से की जाती हैं। ये एनेक्स-1 के देश कहलाए एवं वे OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) से संबंधित थे।
- विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन क्रियाओं हेतु वित्तीय सहायता का निर्देश : इस कन्वेंशन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन क्रियाविधि को समर्थन देने हेतु औद्योगीकृत देश राजी हुए।
- सचिवालय (Secretariat) : UNFCCC एवं क्योटो प्रोटोकॉल को सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है एवं इसे जलवायु परिवर्तन सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है। UNFCCC का सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते में सम्मिलित सभी संस्थानों को समर्थन देता है (खासकर कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) को)। कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग ऑफ पार्टीज (CMP) की तरह कार्य करती है। यह सहायक निकायों (जो COP/CMP को सलाह देता है) एवं COP/CMP ब्यूरो (जो COP/CMP से उत्पन्न संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक मुद्दों को मुख्यत: देखता है) को भी समर्थन देता है। ‘‘मोमेंटम फॉर चेंज : क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ’’ पहल भी इसके द्वारा प्रवर्तित की गई है।
- प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणुओं, परजीवियों एवं कृमियों के कारण संक्रमणजन्य रोगों, जैसे- पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब होने आदि का खतरा रहता है। संक्रमित जल पीने, नहाने, खाना बनाने आदि के लिये अनुपयुक्त होता है।
- पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है जिसमें अस्थियाँ व दाँत कमज़ोर हो जाते हैं।
- पेयजल में क्रोमियम की मात्रा उचित से अधिक होने पर यकृत तथा गुर्दा संबंधी रोग होते हैं।
- भारी धातुओं से युक्त जल के प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। पारायुक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से 1956 में जापान में मिनामाटा महामारी से अनेक लोगों की मौत हो गई थी। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अत्यधिक विषैले पदार्थ मिथाइल पारा (Methyl Mercury) में बदल जाता है जिससे अंगों, होंठ, जीभ आदि में संवेदनशून्यता; बहरापन, आँखों का धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन हो जाता है।
- कैडमियम प्रदूषण से ‘इटाई-इटाई’ रोग हो जाता है जिससे अस्थियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है तथा यकृत एवं फेफड़े का कैंसर हो जाता है।
- सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमज़ोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं।
- एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस (फेफड़े के कैंसर का एक रूप) रोग हो जाता है।
जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (Measures to Control Water Pollution)
जल प्रदूषण को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है-
- घरेलू सीवेज : घरेलू सीवेज में 99.9% जल एवं 0.1% प्रदूषक होते हैं। शहरी क्षेत्रों के घरेलू सीवेज के 90% से अधिक प्रदूषकों को केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हटाया जा सकता है।
- औद्योगिक अपशिष्ट जल : कुछ उद्योगों द्वारा सामान्य विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन किया जाता है जिनका निपटान नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है किंतु कुछ प्रदूषकों, जैसे- तेल, ग्रीस, भारी धातुओं आदि का निपटान विशेष निपटान संयंत्रों द्वारा किया जाना चाहिये। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे कारखानों से निकले अपशिष्टों को बिना शोधित किये नदियों, झीलों एवं तालाबों में विसर्जित न करें।
- कृषि अपशिष्ट जल : मानवोत्पत्ति संबद्ध गतिविधियों में केवल कृषि ही दो-तिहाई से अधिक वैश्विक जल-उपयोग हेतु उत्तरदायी है। कृषि क्षेत्र में अनेक अपरदन नियंत्रण प्रणालियों द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है। किसान उर्वरकों एवं कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग न कर तथा जैव-उर्वरकों एवं जैव-कीटनाशकों का प्रयोग कर जल की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। कीटनाशक का प्रयोग कैंसर का कारक भी है।
- आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिये एवं जल प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न कुप्रभावों से अवगत कराना चाहिये।
- सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिये प्रभावी कानून बनाना चाहिये। यद्यपि सरकार ने जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 लागू किया है लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- जल जीवों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है एवं यह जैवमंडल में पोषक तत्त्वों के संचरण एवं चक्रण में सहायक है। औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है एवं गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है।
- जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानवजनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन या ह्रास जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदायों के लिये अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है।
- जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्राचल (Parameter) हैं- कुल विघटित ठोस पदार्थ, कॉलिफॉर्म काउंट, विघटित ऑक्सीजन।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुओं (पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि) को पेयजल प्रदूषण के लिये उत्तरदायी माना है।
- जलीय पारितंत्र में सुपोषण, जैव आवर्धन आदि प्रक्रिया तेज़ हो जाती है।
- पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस (TDS) पदार्थ के सांद्रण की अधिकतम सीमा 500 mg/L मानी गई है। जल प्रदूषण में द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण इस सीमा से कहीं अधिक हो जाता है।
- प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ति पर भी पड़ता है, इससे प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोतरी होती है।
जल प्रदूषण के स्रोत (Sources of Water Pollution)
- उत्पत्ति के आधार पर जल प्रदूषकों के स्रोतों को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
- बिंदु स्रोत प्रदूषण (Point Source Pollution) : इसके अंतर्गत ऐसा प्रदूषण आता है जिसमें प्रदूषक, जल के निश्चित स्रोत से आते हैं। जैसे- नगरपालिका क्षेत्र का सीवेज स्थल एवं फैक्ट्रियों का बहि:स्राव स्थल।
- अबिंदु स्रोत प्रदूषण (Non-Point Source Pollution) : इसके अंतर्गत ऐसे प्रदूषण को शामिल किया जाता है जिसमें प्रदूषकों का बहि:स्राव किसी पृथक् स्रोत से नहीं होता है। इसमें प्रदूषक एक विस्तृत क्षेत्र से आते हैं। उदाहरण के लिये शहर के वर्षा जल का बहाव, कृषि क्षेत्र का बहाव, धोबी घाट, खुले में शौच, पशुओं के शव इत्यादि।
- बिंदु स्रोत प्रदूषण को उपयुक्त तकनीक का प्रयोग कर नियंत्रित किया जा सकता है किंतु अबिंदु स्रोत प्रदूषण को नियंत्रित करना कठिन है।
जल प्रदूषण के कारण (Causes of Water Pollution)
- घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोतों में मिलना,
- कृषि में प्रयुक्त उर्वरक एवं खरपतवार युक्त जल का नदी में मिलना,
- तेल अधिप्लाव,
- रेडियोसक्रिय तत्त्वों से युक्त रसायन का जलीय तंत्र तक पहुँचना,
- विद्युत ऊर्जा केंद्र से निकले उच्च तापयुक्त जल का जल स्रोत में निकास,
- नहाने व कपड़े धोने के लिये नदी जल का प्रयोग
वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस (ध्वनि व रेडियोधर्मी विकिरण भी) का इस मात्रा में मिल जाना कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव समेत अन्य जीवधारियों को हानि पहुँचाए, ‘वायु प्रदूषण’ कहलाता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%), ऑर्गन (0.9%), कार्बन डाइऑक्साइड (0.038%) इत्यादि गैसें पाई जाती हैं।
वायु प्रदूषकों के प्रकार (Types of Air Pollutants)
- प्रदूषकों की उत्पत्ति के आधार पर
- प्राकृतिक प्रदूषक (Natural Pollutants)- ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। कुछ उदाहरण हैं : पौधों के परागकण और पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों के सड़ने-गलने से निकलने वाली गैसें, जैसे- SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) आदि।
- मानवजनित प्रदूषक (Manmade Pollutants)- इसमें कारखानों, रसोईघरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक शामिल हैं।
- प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर
- गैसीय प्रदूषक (Gaseous Pollutants)- इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है-
- जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि।
- एरोसॉल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निस्सृत क्लोरो-फ्लोरोकार्बन।
- सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से निस्सृत सल्फर के यौगिक, जैसे- SO2, SO3 आदि। SO2 श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है।
- अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों से निस्सृत नाइट्रोजन के यौगिक, जैसे- नाइट्रस ऑक्साइड (N2O), नाइट्रिक ऑक्साइड (NO), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड (NO3)
- सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन।
- कणिकीय प्रदूषक (Particulate Pollutants)- कणिकीय प्रदूषकों के मुख्य स्रोत हैं- गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ, ताप संयंत्र, तेलशोधन कारखाना, निर्माण कार्य आदि। इन प्रदूषकों के कारण धुंध (Haze) फैल जाता है तथा दृश्यता प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही ये प्रदूषक पेफड़े व श्वसन प्रक्रिया को भी दुष्प्रभावित करते हैं। फ्लाई ऐश और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण हैं।
- गैसीय प्रदूषक (Gaseous Pollutants)- इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है-
- प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के आधार पर
- प्राथमिक प्रदूषक (Primary Pollutants)- ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। इनके उदाहरण हैं- ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएँ।
- द्वितीयक प्रदूषक (Secondary Pollutants)- सूर्य के विद्युतचुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणामस्वरूप द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिये प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड (SO3) बनाती है जो एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर एक और द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल (H2SO4) बनाती है जो कि अम्ल वर्षा का घटक है। NO2 के दो अन्य द्वितीयक प्रदूषक परॉक्सीएसिटिल नाइट्रेट (PAN) तथा नाइट्रिक अम्ल (HNO3) हैं। धूम-कोहरा (SMOG) धुएँ और कोहरे का मिश्रण होता है
इनके अतिरिक्त एरोसॉल, प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरा, फ्लाई ऐश, निलंबित कणिकीय पदार्थ तथा घरेलू वायु प्रदूषण भी वायु प्रदूषण के कारक हैं।
हमारे पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में किसी प्रकार के अवांछनीय परिवर्तन जो वायु, जल और मृदा में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव या अन्य जातियों तथा हमारे जीवमंडल में जीवन को आश्रय देने वाली व्यवस्थाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं या करेंगे, को प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया, जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है, ‘प्रदूषण’ कहलाती है तथा वह पदार्थ जिसे किसी संसाधन में मिलाने से संसाधन की उपयोगिता कम हो जाती है, प्रदूषक कहलाता है।
- वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जिस रूप में उत्पादित होते हैं, उसी स्वरूप में बने रहते हैं। जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि।
- वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंत:क्रिया के कारण निर्मित होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे- ओज़ोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, परॉक्सीएसिटिल नाइट्रेट (PAN), धूम (Smog) इत्यादि।
- प्रदूषकों के निवारण के आधार पर इसे जैव-निम्नीकृत (Bio-degradable) प्रदूषक तथा जैव-अनिम्नीकृत (Non-Biodegradable) प्रदूषक में बाँटा जाता है।
- वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्मजीवीय गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं, उन्हें जैव-निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं। जैसे- कागज़, सब्ज़ी, फल इत्यादि।
- वैसे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता, जैव-अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। ये लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं। जैसे- प्लास्टिक, रेडियोसक्रिय तत्त्व, सीसा इत्यादि। आहार शृंखलाओं में से गुज़रते हुए इसका अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। अत: जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि ही जैव-आवर्धन है।
- पर्यावरण पर मानवोद्भविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ़यता एवं संसाधनों के दोहन में प्रयुक्त तकनीकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक हैं।
- प्रदूषण के प्रमुख प्रकार- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, ताप प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण आदि हैं।
देश की शासन प्रणाली अथवा शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली का शिक्षण के स्वरूप पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली में शिक्षण दिया जाता है, यह उसी प्रकार का रूप धारण कर लेता है। शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं-
निरंकुश शिक्षण (Autocratic Teaching) : शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन होता है। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक केंद्रबिंदु होता है एवं शिक्षक का स्थान प्रधान होता है और विद्यार्थियों का स्थान गौण होता है। इसमें शिक्षक की विचारधारा को वरीयता दी जाती है और विद्यार्थियों को उसके आदेशों का बिना किसी किंतु-परंतु के पालन करना होता है। जैसे- प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन।
लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण (Democratic Teaching) : इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो कि व्यावहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। वस्तुतः इस पद्धति में विद्यार्थी केंद्र में और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। इसमें अनुशासनहीनता की स्थिति की संभावना बनी रहती है।
हस्तक्षेप रहित शिक्षण (Laisses Faire Teaching) : शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिये स्वतंत्र होता है। इसमें विद्यार्थी दबाव एवं बाधामुक्त होकर सीखता है। जैसे- भारतीय शिक्षा पद्धति।
व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ (Meaning of Individual Difference)
भिन्नता प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में कोई भी दो प्राणी पूरी तरह एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वे मनुष्य हों या कोई अन्य प्राणी। अलग-अलग व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है।
व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा (Definition of Individual Difference)
- स्किनर के अनुसार : व्यक्तित्व के वे सभी पहलू जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं।
- जेम्स ड्रेवर के अनुसार : कोई व्यक्ति अपने समूह से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भिन्नता रखता है, उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है।
- टायलर के अनुसार : शरीर के रंग-रूप, आकार-प्रकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में मौजूद भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं।
व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार (The Basis of Individual Differences)
मनुष्य के अलावा सभी प्राणियों में केवल शारीरिक बनावट एवं शारीरिक क्षमता के आधार पर भिन्नताएँ पाई जाती हैं। लेकिन मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कई आधार होते हैं। अपनी पुस्तक ‘साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिफरेंसेज’ में टायलर ने लिखा है, ‘‘एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है।’’ व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर का आधार भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता हो सकती है।
मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया है-
- जाति के आधार पर : समाज में जाति एवं नस्ल संबंधित भिन्नताएँ पाई जाती हैं। विभिन्न जातियों के रहन-सहन, खान-पान तथा उनकी संस्कृति आदि में अंतर होता है। कोई जाति विद्या अर्जन के लिये प्रसिद्ध होती है तो किसी को युद्ध लड़ने के लिये जाना जाता है।
- धर्म के आधार पर : धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरण को निर्धारित करता है। संसार में अनेक धर्म हैं जिनके रहन-सहन, खान-पान, आचार-व्यवहार तथा उनकी मान्यताओं में अंतर होता है। यही अंतर व्यक्ति की भिन्नता को दर्शाता है।
- अभिवृत्ति के आधार पर : किसी भी दो व्यक्ति की अभिवृत्ति एक समान नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृत्ति एवं रुचि अलग-अलग होती है।
- भाषा के आधार पर : प्रत्येक भाषा समुदाय की अपनी पहचान होती है चाहे वह अंचल के आधार पर हो अथवा राष्ट्र के आधार पर। दो भिन्न भाषाओं से जुड़े व्यक्तियों में भिन्नताएँ स्पष्ट हो जाती हैं।
- लिंग के आधार पर : आज किसी-न-किसी रूप में विश्व के प्रत्येक देश या क्षेत्र में नारियों को दोयम दर्जे पर रखा जाता है, जो न सिर्प रूढ़िवादिता के कारण है बल्कि अमानवीय भी है।
- समुदाय के आधार पर : आज पूरी दुनिया छोटे-छोटे और बड़े-बड़े कितने ही समुदायों में विभक्त है। पश्चिमी देशों के लोग स्वयं को पूर्वी लोगों की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं।
- विश्वसनीयता (Credibility) : शिक्षक किसी विद्यार्थी की उत्तर-पुस्तिका की जाँच करता है और जाँच के बाद अंक देता है तो यदि उसी उत्तर-पुस्तिका की पुन: कितनी ही बार जाँच क्यों न की जाए, पहले आए अंकों में और दुबारा दिये गए अकों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिये।
- वैधता (Validity) : इसके अंतर्गत दो विशेषताओं को शामिल किया गया है-
-
- मूल्यांकन पत्र निर्धारित किये गए पाठ्यक्रमों के आधार पर ही बनाया जाना चाहिये।
- परीक्षा जिस विषय की हो, उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिये।
- विभेदीकरण (Differentiation) : मूल्यांकन पत्र (पेपर) का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि पेपर तीनों स्तरों (प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि) के विद्यार्थियों के अनूकल हों। साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिये यानी मूल्यांकन में न्याय संगतता की विशेषता भी होनी चाहिये।
- समग्रता (Totality) : प्रश्न-पत्र के लिये जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके संपूर्ण भागों से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। तभी विद्यार्थियों की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है।
- उद्देश्यनिष्ठता (Purposefulness) : प्रश्न-पत्र तैयार करते समय निश्चित उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिये, जिससे कि विद्यार्थी और प्रश्न-पत्र तैयार करने वाली टीम/संस्था दोनों ही अपने-अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। उदाहरण- CTET के पेपर से विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, दूसरी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुशल विद्यार्थियों का चयन करके अपना उद्देश्य पूरा करता है।
- वस्तुनिष्ठता (Objectivity)
-
- प्रश्न-पत्र में बहुवैकल्पिक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिये।
- उत्तर-पुस्तिका की जाँच करते समय शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों व पूर्वाग्रह का प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर-पुस्तिका पर नहीं पड़ना चाहिये।
- मानकता (Standardization) : प्रश्न-पत्र एक निश्चित मानक पर आधारित हो। जैसे- उत्तीर्ण (पास) होने के लिये 33% अंकों की तथा प्रथम श्रेणी के लिये 60% अंकों की अनिवार्यता।
- व्यावहारिकता (Practicality) : मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक व व्यावहारिक होनी चाहिये। प्रश्न-पत्र ऐसे हों, जिनमें समय व धन की बचत हो, साथ ही प्रश्न-पत्र की गुणवत्ता (कागज़ स्वरूप) का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार मूल्यांकन में मितव्ययिता को भी महत्त्व देना चाहिये।
शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात् सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियाँ अधिक उपयोगी हैं। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक ‘The Conditions of Learning’ में अधिगम की निम्न आठ दशाओं/भेदों के बारे में लिखा है। ये दशाएँ कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर बढ़ता जाता है।
- संकेत अधिगम (Signal Learning) : यह पावलव की शास्त्रीय अनुबंध क्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएँ करना सीखता है।
- उद्दीपन-अनुक्रिया अधिगम (Stimulus-Response Learning) : यह थार्नडाइक के ‘संबंधवाद’ तथा स्किनर के ‘सक्रिय अधिगम’ का रूप है। गेने ने इस अधिगम के अंतर्गत थार्नडाइक के ‘प्रयास एवं भूल अधिगम’ तथा स्किनर के ‘कार्य अनुबंधन अधिगम’ को रखा है।
- शृंखला अधिगम (Chain Learning) : इस अधिगम में दो या दो से अधिक उद्दीपन-अनुक्रियाएँ आपसी समन्वय से एक शृंखला अधिगम का निर्माण करती हैं।
- शाब्दिक साहचर्य अधिगम (Verbal Association Learning) : यह शृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। जब यह शृंखला शाब्दिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाती है तो उसे शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं, जैसे- शब्दावली सीखना, कहानी याद करना इत्यादि इस अधिगम के उदाहरण हैं।
- विभेदन अधिगम (Discrimination Learning) : विभेदन अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न-भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न-भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता है। एक जैसे दिखने वाले उद्दीपनों में विभेद करने की क्षमता आ जाती है और बच्चा विभेदी उद्दीपन के अनुरूप अनुक्रिया करने में समर्थ हो जाता है, जैसे- बालक पुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीख जाता है।
- संप्रत्यय अधिगम (Concept Learning) : जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें ‘संप्रत्यय अधिगम’ कहते हैं। सर्वप्रथम केंडलर ने इसका उल्लेख किया था।
- नियम अधिगम (Rule Learning) : नियम अथवा सिद्धांत अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। इस अधिगम में दो या अधिक संप्रत्ययों को शृंखलाबद्ध किया जाता है, जिससे एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है, जैसे- ‘पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है।’
- समस्या-समाधान अधिगम (Problem Solving Learning) : समस्या-समाधान अधिगम में नियम अधिगम का ही प्राकृतिक विस्तार होता है। नियम अधिगम के साथ-साथ विद्यार्थियों को अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुँचते हैं। इस अधिगम में चिंतन की सामग्री निहित होती है।
भारत ने हमेशा से उच्चतर शिक्षा को महत्त्व दिया है। प्राचीन भारत में विकसित हुई शिक्षा को वैदिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इनका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति थी, ताकि सांसारिक बंधनों से परे किसी अमूर्त सत्ता का सान्निध्य प्राप्त कर सकें।
भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास का क्रम :
- दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय 700 ई.पू. में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना चौथी शताब्दी में हुई थी।
- गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने अध्यापक केंद्रित प्रणाली स्थापित की, जिसमें विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन और अपने शिक्षक के प्रति कुछ दायित्वों के अधीन रहना होता था।
- वर्तमान विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत औपनिवेशिक भारत से होती है। भारत में अंग्रेज़ी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता में सन् 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुई। भारत में यूरोपीय शैली पर आधारित यह पहला शिक्षण संस्थान था।
- सन् 1823 के माउंटस्टुआर्ट एलिफिंस्टन व 1835 के लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में वर्तमान भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों की जडे़ं मिलती हैं। इन रिपोर्टों में सुझाव था कि भारत में यूरोपीय साहित्य व विज्ञान की पढ़ाई के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हो और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का उपयोग किया जाए।
- लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार 1854 में आए चार्ल्स वुड डिस्पैच में किया गया, जिसे भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का ‘मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है। इसके तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय स्थापित किये गए।
- सन् 1943 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 12 और कॉलेजों की संख्या 75 थी। सन् 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के संदर्भ में पहला प्रयास थी।
- वर्ष 1950 में भारत में 20 विश्वविद्यालय थे, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2 लाख थी।
- औपनिवेशिक भारत में उच्चतर शिक्षा तक पहुँच केवल शहरी उच्च वर्ग के पुरुषों के पास थी, जिसमें ऊँची जातियों के पुरुषों की संख्या अधिक थी जबकि महिलाओं की संख्या भी बहुत कम थी। इस तरह से बडे़ शहरों तक सीमित उच्चतर शिक्षा व्यवस्था से शहर, कस्बे, गाँव और अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे।
- सन् 1948 में सभी विश्वविद्यालयों के लिये अनुदान संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने व उनकी देख-रेख करने के लिये डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई।
आज भारत अपने समाज और बाहरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए ज्ञान के नए क्षेत्रों का सृजन कर रहा है और उन्हें उच्चतर शिक्षा से जोड़ रहा है। इस प्रकार शुरुआत से लेकर अब तक की उच्चतर शिक्षा अपने स्वरूप में काफी बदल चुकी है। पाठ्यक्रम के अनुसार हम वर्तमान भारत में उच्चतर शिक्षा की संरचना और स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे।
सतत् प्रक्रिया (Continuous Process): शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है। अत: यह ज्ञात करने के लिये कि विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त हुए हैं या नहीं, मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है।
- व्यापक प्रक्रिया (Comprehensive Process): व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों-ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है।
- सामाजिक प्रक्रिया (Social Process): शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा, आदर्श एवं आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिये मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया है।
- उद्देश्यनिष्ठता (Purposefulness): पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है और जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, उसका स्तर कैसा है? आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर निर्भर करता है।
- निर्माणात्मक/रचनात्मक प्रक्रिया (Formative Process): मूल्यांकन ही शिक्षण विधियों, शिक्षक द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों की प्राप्ति व विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रभावशीलता आदि के विषय में हमें सही निर्णय लेने योग्य बनाता है। मूल्यांकन एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है।
- विद्यार्थी केंद्रित (Student Centred): मूल्यांकन द्वारा ही यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसलिये मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है।
- सहकारी/सहभागी निर्णय (Interactive Decision): पहले शिक्षक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करके कोई निर्णय लेता था, जो विश्वनीय नहीं था, किंतु अब मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक के अतिरिक्त विद्यार्थी के मित्र, अभिभावक व अन्य शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी के मूल्यांकन में उसके सभी पक्षों पर बातचीत करके ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वाग्रह से मुक्त होती है।
ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। इसके विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। पिछले तीन दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किये हैं। इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन-पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है।
- आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्टबोर्ड ने ले ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन ने चॉक का स्थान ले लिया है।
- इंगित करने के लिये इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेजर पॉइंटर ने ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं।
- शिक्षा में दृश्य-श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिये टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर-तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और शिक्षा अब तेजी से ई-शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है।
ई-शिक्षा के प्रकार
- समकालिक (Synchronous) शैक्षिक व्यवस्था- इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि ‘एक ही समय में’ अर्थात् विद्यार्थी और शिक्षक अलग-अलग स्थानों से एक-दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसलिये इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई-लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से विद्यार्थियों को स्टडी मटीरियल उपलब्ध कराया जाता है। समकालिक ई-शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षो में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
- असमकालिक (Asynchronous) शैक्षिक व्यवस्था- इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि ‘एक समय में नहीं’ अर्थात् यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकरी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिये वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्युटोरिअल्स, ई-बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई-शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय, जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों को एक्सेस(पहुँच) कर सकते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग असमकालिक शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है।




