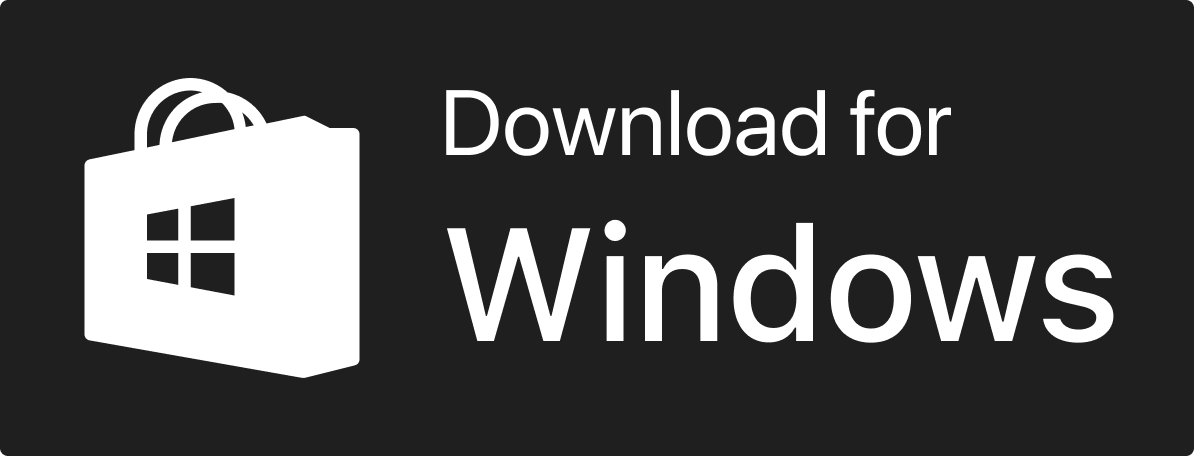प्रैक्टिस क्विज़
नया क्या है (View All)
- 16-Oct-25
[September 2020]: Hindi
- 16-Oct-25
[September 2020]: Home Science
- 16-Oct-25
[September 2020]: History
- 16-Oct-25
[September 2020]: Library and Information Science
- 16-Oct-25
[September 2020]: Geography
- 31-Jan-26
[CTET Paper-II (सामाजिक अध्ययन)]: पेपर -2 (31-01-2026)
- 31-Jan-26
[NVS PGT]: NVS TGT (31-01-2026)
- 31-Jan-26
[KVS TGT]: KVS TGT (31-01-2026)
- 31-Jan-26
[माध्यमिक विद्यालय अध्यापक]: माध्यमिक विद्यालय अध्यापक (31-01-2026)
- 31-Jan-26
[NTA UGC-NET इतिहास]: इतिहास ( 31-01-2026)
नोटिफिकेशन (View All)
- 31-Jan-26
UPPSC 2026 | Examination Calendar
Official Notification
- 29-Jan-26
SUPER TET 2026 | Syllabus
Official Notification
- 29-Jan-26
UPTET 2026 | Upper Primary Level (6 to 8) | Exam Pattern & Updated Syllabus
Official Notification
- 29-Jan-26
UPTET 2026 | Primary Level (1 to 5) | Exam Pattern & Updated Syllabus
Official Notification
- 21-Jan-26
UPESSC 2026 | Exam Calendar | UPTET & More
Official Notification
- 21-Jan-26
KVS-NVS 2025 | Tier-II Detailed Updated Syllabus
Official Notification
- 14-Jan-26
BPSC AEDO Exam 2025 | Revised Exam Date
Official Notification
- 12-Jan-26
DSSSB 2026 | Examination Schedule | Feb to May
Official Notification
- 07-Jan-26
EMRS 2025 | Tier-I | Provision to Download OMR & Answer Key
Official Notification
- 07-Jan-26
JPSC 2026 Exam Calendar | JET Exam Date Announced!
Official Notification
- 07-Jan-26
BPSC Special Education Teacher Recruitment 2025 | Examination Schedule
Official Notification
- 07-Jan-26
UP LT Grade Exam 2025 | Admit Card Released
Official Notification
- 06-Jan-26
EMRS 2025 | PGT Tier-I | Provisional Answer Key Released
Official Notification
- 06-Jan-26
EMRS 2025 | TGT Tier-I | Provisional Answer Key Released
Official Notification
- 06-Jan-26
KVS–NVS 2025 | Compensatory Time for PwBD Candidates
Official Notification
- 31-Dec-25
MP SET 2025 | Revised Exam Date Announced!
Official Notification
- 31-Dec-25
UKPSC Lecturer 2025 | Detailed Syllabus!
Official Notification
- 31-Dec-25
UKPSC Lecturer 2025 | Advertisement!
Official Notification
- 31-Dec-25
UKPSC Lecturer 2025 | Detailed Notification!
Official Notification
- 30-Dec-25
BPSC AEDO 2025 | Exam Postponed!
Official Notification
- 30-Dec-25
RSSB REET Mains Level-1 & 2 | Examination Schedule Released!
Official Notification
- 29-Dec-25
KVS/NVS 2025 | Tier-I Examination Schedule Out!
Official Notification
- 29-Dec-25
RPSC 2026 | Examination Calendar Released!
Official Notification
- 26-Dec-25
CTET-2026 | Form Completion Date Extended
Official Notification
- 26-Dec-25
DSSSB- 2025-26 | PRT-TGT-PGT Examination Dates Released
Official Notification
- 25-Dec-25
HTET 2025 | Detailed Notification Released!
Official Notification
- 24-Dec-25
BPSC AEDO 2025 | Examination Schedule!
Official Notification
- 18-Dec-25
MP SET 2025 | Postponed!
Official Notification
- 18-Dec-25
UGC-NET December 2025 | Subject-Wise Examination Schedule Released!
Official Notification
- 18-Dec-25
EMRS 2025 | Tier II | Detailed TGT Syllabus
Notification
- 18-Dec-25
EMRS 2025 | Tier II | Detailed PGT Syllabus
Notification
- 12-Dec-25
KVS/NVS Recruitment 2025 | Vacancy Revision Notification
Official Notification
- 12-Dec-25
UP LT Grade Exam 2025 | Pre Answer Key Released | Hindi
Official Notification
- 12-Dec-25
UP LT Grade Exam 2025 | Pre Answer Key Released | Mathematics
Official Notification
- 12-Dec-25
UP LT Grade Exam 2025 | Pre Answer Key Released | Science
Official Notification
- 02-Dec-25
CTET 2026 | Examination City Allotment Notice
Notification
- 27-Nov-25
CTET 2026 | Detailed Notification Out!
Official Notification
- 26-Nov-25
EMRS 2025 | Tier-I Examination Schedule
Notification
- 25-Nov-25
KVS-NVS 2025 | Tier-II Detailed Syllabus
Notification
- 24-Nov-25
KVS/NVS 2025 Tier-I Exam Date Announced | Official Update
Notification
- 24-Nov-25
Dadra & Nagar Haveli + Daman & Diu Primary and Upper Primary Teacher Recruitment 2025 | Detailed Advt.
Notification
- 24-Nov-25
Bihar STET 2025 Provisional Answer Key Out | Challenge Window Open
Notification
- 24-Nov-25
WB Primary Teacher Vacancy 2025 | Detailed Advertisement Released
Notification
- 19-Nov-25
UP TGT Exam (Advt. 01/2022) Postponement Notice
Notification
- 14-Nov-25
NVS–KVS Recruitment 2025 | Joint Detailed Notification Released | Teaching & Non Teaching Vacancies
Notification
- 14-Nov-25
Chhattisgarh TET 2026 | Notification Released!
Notification
- 13-Nov-25
KVS & NVS 2025 | Short Notification | Teaching & Non Teaching Vacancies
Notification
- 10-Nov-25
RPSC Assistant Professor 2025 | Exam Schedule
Notification
- 10-Nov-25
RSSB REET Mains Level-1 (Primary Teacher) | Detailed Advt 08/2025
Notification
- 10-Nov-25
RSSB REET Mains Level-2 (Upper Primary Teacher) | Detailed Advt 09/2025
Notification
- 10-Nov-25
WBSSC 2nd SLST (Asst. Teacher) Written Exam Result 2025 Out!
Notification
- 27-Oct-25
UP LT Grade Exam 2025 | Date Sheet
Notification
- 24-Oct-25
EMRS Recruitment 2025 | Last Date to Apply Extended
Notification
- 24-Oct-25
CTET 2025 | Exam Schedule Announced
Notification
- 16-Oct-25
MP SET 2025 Detailed Notification | Eligibility, Syllabus & Exam Date
Notification
- 13-Oct-25
UGC-NET December 2025 | Exam Schedule
Notification
- 10-Oct-25
EMRS Recruitment 2025 | Exam Dates Declared
Official Notification
- 08-Oct-25
UGC-NET December 2025 | Official Notification
Notification
- 03-Oct-25
DSSSB TGT 2025 Advertisement | Official Notification
Notification
- 01-Oct-25
MP SET 2025 | Complete Subject List
Notification
- 30-Sep-25
UP PGT Exam (Advt. 02/2022) Postponement Notice
Official Notification
- 22-Sep-25
UP LT Grade Exam 2025 : Date Sheet
Official Notification
- 22-Sep-25
EMRS Detailed Notification for Teaching & Non-Teaching Posts 2025
Official Notification
- 19-Sep-25
Bihar STET 2025 Application Form Released – Apply Online
Official Notification
- 11-Sep-25
DSSSB PRT Recruitment 2025 - Detailed Advertisement
Notification
- 10-Sep-25
BPSC AEDO 2025 - Detailed Advertisement
Notification
- 10-Sep-25
Himachal Pradesh TET 2025 Official Notification
Notification
- 10-Sep-25
Jharkhand Eligibility Test (JET) 2025 - Detailed Notification
Notification
- 10-Sep-25
Bihar STET 2025 - Short Notification
Notification
- 04-Sep-25
UPPSC Assistant Professor 2025 (Govt. Degree College) Abridged Advertisement
notification
- 04-Sep-25
BPSC TRE 4.0 Exam Date Announced – Official Update!
notification
- 04-Sep-25
UPPSC सहायक आचार्य परीक्षा 2025 - विस्तृत विज्ञापन
notification
- 01-Sep-25
RPSC Senior Teacher (TGT) 2024 Exam Date – Check Official Schedule
notification
- 29-Aug-25
RPSC School Lecturer (PGT) Agriculture 2025 – Detailed Notification
notification
- 21-Aug-25
DSSSB TGT CS Vacancies Out | RTI Update
notification
- 19-Aug-25
EMRS Raigarh (CG) Part-Time Guest Teacher Vacancy 2025
notification
- 12-Aug-25
UPPSC GIC Lecturer 2025 Short Advertisement
notification
- 12-Aug-25
UPPSC GIC Lecturer Detailed Notification 2025
notification
- 07-Aug-25
CTET Updated FAQs 2025
Official Notification
- 06-Aug-25
Marks released and e-dossier called for PGT (Economics)-Male, Post Code 80923, DOE & NDMC.
notification
- 04-Aug-25
DSSSB TGT Special Education Teacher Detailed Advertisement
notification
- 01-Aug-25
HTET Level-1 Provisional Answer Key 2024
notification
- 01-Aug-25
HTET Level-2 Provisional Answer Key 2024
notification
- 01-Aug-25
HTET Level-3 Provisional Answer Key 2024
notification
- 30-Jul-25
UP Aided Colleges TGT/PGT Vacancy Data Requested by Directorate
Official Notification
- 30-Jul-25
Samagra Shiksha, Chandigarh | JBT Advertisement 2025
Official Notification
- 28-Jul-25
EMRS Recruitment 2025 | Response to Parliamentary Question
Official Notification
- 28-Jul-25
UP LT Grade 2025 विस्तृत विज्ञापन
Official Notification
- 25-Jul-25
UP TGT Exam-UPTET Update
Official Notification
- 25-Jul-25
WBSSC Notifies Exam Dates for 2nd SLST 2025
Official Notification
- 24-Jul-25
KVS-NVS School Vacancies State-UT-Wise – Parliament Response
Official Notification
- 23-Jul-25
RPSC Grade-1 School Lecturer Detailed Notification 2025 Released
Official Notification
- 23-Jul-25
RPSC Grade-2 Senior Teacher Detailed Notification 2025 Released
Official Notification
- 22-Jul-25
Declaration of results of UGC-NET June 2025
Official Notification
- 21-Jul-25
UP LT Grade Short Advertisement 2025
Official Notification...
- 06-Jun-25
UGC-NET June 2025 Exam Schedule
UGC-NET June 2025 Exam Schedule
- 20-Dec-24
UGC-NET दिसंबर 2024 : परीक्षा कार्यक्रम
Official Notification
- 12-Dec-24
REET 2024 विज्ञापन
Official Notification
- 20-Nov-24
UGC-NET दिसंबर 2024 - ऑनलाइन आवेदन
Official Notification
- 17-Sep-24
CTET दिसंबर 2024 : सूचना बुलेटिन
CTET दिसंबर 2024 : सूचना बुलेटिन
- 12-Sep-24
UGC-NET जून 2024 - आंसर-की चैलेंज (27 अगस्त - 5 सितंबर)
Official Notification
- 09-Sep-24
UGC-NET जून 2024 - आंसर-की चैलेंज (21-23 अगस्त)
Official Notification
- 02-Aug-24
UGC-NET जून 2024 - परीक्षा कार्यक्रम
Official Notification
- 01-Aug-24
CTET जुलाई 2024 : परिणाम के संबंध में सार्वजनिक सूचना
Official Notification
- 01-Jul-24
UGC-NET जून 2024 की संशोधित तिथि
Official Notification
- 20-Jun-24
UGC-NET जून 2024 रद्द
Official Notification
- 07-Jun-24
UGC-NET जून 2024 : परीक्षा शहरों का आबंटन
UGC NET June 2024
- 07-Jun-24
CTET जुलाई 2024 : सूचना बुलेटिन
CTET
कॉन्सेप्ट कार्ड
मिश्रण (Mixture)
मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्त्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाकर प्राप्त होता है। मिश्रण के निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि अवयव अपने मूल गुणों को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि मिश्रण को अपेक्षाकृत सरल यांत्रिक विधियों जैसे- छनन (Filtration), वाष्पीकरण (Evaporation), आसवन (Distillation), अपकेंद्रण (Centrifugation) आदि द्वारा उसके मूल घटकों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, हवा एक सामान्य मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें सम्मिलित रहती हैं।
मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं – समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण।
समांग मिश्रण (Homogeneous Mixture)
जब मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में और इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि पूरे मिश्रण के सभी भागों में उनका वितरण एकसमान हो, तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में विभिन्न अवयवों को अलग-अलग पहचानना संभव नहीं होता क्योंकि वे अणु स्तर पर समान रूप से फैले रहते हैं।
मुख्य लक्षण :
- मिश्रण के प्रत्येक भाग में गुण-धर्म समान रहते हैं।
- अवयवों का पृथक्करण नग्न आँखों से या साधारण तरीकों से संभव नहीं होता।
- अक्सर इनका निर्माण घुलनशील पदार्थों के विलयन से होता है।
उदाहरण : चीनी का जलीय विलयन, नमक का घोल, हवा।
विषमांग मिश्रण (Heterogeneous Mixture)
जब मिश्रण के अवयव अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं और वे पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते, तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। इसमें प्रत्येक भाग की संरचना और गुण-धर्म अलग-अलग होते हैं। ऐसे मिश्रण में अवयवों को आसानी से पहचाना जा सकता है और साधारण विधियों द्वारा अलग भी किया जा सकता है।
मुख्य लक्षण :
- मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण और संघटन अलग-अलग होते हैं।
- विभिन्न अवयव नग्न आँखों से दिखाई देते हैं।
- इनका पृथक्करण अपेक्षाकृत सरल होता है।
उदाहरण : बारूद, कुहासा, दूध में घी की परत, मिट्टी और रेत का मिश्रण।
अतः मिश्रण रसायन विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है, जिसमें पदार्थों का मेल होता है लेकिन उनकी मूल पहचान बनी रहती है। समांग मिश्रण पूर्णतः एकसमान और समान गुणधर्म वाले होते हैं, जबकि विषमांग मिश्रण में विविधता और असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह भेद रसायन और दैनिक जीवन दोनों में मिश्रणों को समझने और उपयोग करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
हार्ड डिस्क
हार्ड डिस्क एक महत्त्वपूर्ण डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिये किया जाता है। हार्ड डिस्क को Hard Disk Drive (HDD) भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
हार्ड डिस्क एक Non-Volatile मेमोरी है, अर्थात् कंप्यूटर बंद होने या बिजली चले जाने पर भी इसमें संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता। इसी कारण इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन, वीडियो, ऑडियो, चित्र, दस्तावेज और अन्य फाइलों को स्टोर करने के लिये किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाये तो हार्ड डिस्क वह मेमोरी है जिसमें डेटा हमेशा के लिये सुरक्षित रहता है।
हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता काफी अधिक होती है। सामान्यतः हार्ड डिस्क 256 GB से लेकर 1 TB या उससे अधिक डेटा को स्टोर कर सकती है। इसी वजह से यह बड़ी फाइलों और भारी सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिये उपयुक्त मानी जाती है।
हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। इसके पीछे एक सर्किट बोर्ड लगा होता है, जो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के बीच संचार (communication) स्थापित करता है। हार्ड डिस्क एल्यूमीनियम और कांच से बनी होती है, जिसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। इसी चुंबकीय सतह पर डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है।
अन्य मेमोरी डिवाइस की तुलना में हार्ड डिस्क सस्ती होती है और बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है। हार्ड डिस्क का अविष्कार 13 सितंबर 1956 को IBM कंपनी की एक टीम द्वारा किया गया था, जिसने कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी।
हार्ड डिस्क के प्रकार
हार्ड डिस्क कंप्यूटर की एक महत्त्वपूर्ण सेकेंडरी मेमोरी है, जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिये किया जाता है। तकनीक के विकास के साथ-साथ हार्ड डिस्क के कई प्रकार विकसित हुए हैं। मुख्य रूप से हार्ड डिस्क के पाँच प्रकार माने जाते हैं — SATA, PATA, NVMe, SCSI और SSD।
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) आज के समय में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क तकनीक है। इसका उपयोग लगभग सभी आधुनिक डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटरों में किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटरों में 3.5 इंच की SATA हार्ड डिस्क और लैपटॉप में 2.5 इंच की SATA हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। SATA डेटा ट्रांसफर करने की तेज गति के लिये जानी जाती है, जिसकी स्पीड लगभग 150 MBps से 600 MBps तक होती है। इसे Serial ATA भी कहा जाता है और इसका आविष्कार वर्ष 2000 में किया गया था।
PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) पुराने समय में उपयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क तकनीक है। इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड कम होती थी, इसी कारण आज के समय में इसे SATA ने लगभग पूरी तरह से बदल दिया है।
NVMe (Non-Volatile Memory Express) एक आधुनिक और अत्यंत तेज तकनीक है, जिसका उपयोग हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर और लैपटॉप में किया जाता है। यह PCIe इंटरफेस पर आधारित होती है और बहुत तेज डेटा ट्रांसफर प्रदान करती है।
SCSI (Small Computer System Interface) का उपयोग मुख्य रूप से सर्वर और बड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। यह एक साथ कई डिवाइस को कनेक्ट करने में सक्षम होती है।
SSD (Solid State Drive) सबसे आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। यह बहुत तेज, हल्की और विश्वसनीय होती है, लेकिन इसकी कीमत सामान्य हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक होती है।
हार्ड डिस्क के भाग –
हार्ड डिस्क कंप्यूटर की एक महत्त्वपूर्ण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कई अलग-अलग भागों से मिलकर बनी होती है। इन सभी भागों का अपना-अपना विशेष कार्य होता है, जिनकी सहायता से हार्ड डिस्क डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करती है।
हार्ड डिस्क का सबसे प्रमुख भाग Platter (प्लैटर) होता है। यह एक गोल चकती होती है, जिस पर चुम्बकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। इसी प्लैटर पर डेटा को चुम्बकीय रूप में स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक या एक से अधिक प्लैटर हो सकते हैं।
Read Write Head (रीड राइट हेड) हार्ड डिस्क का वह भाग है जो डेटा को पढ़ने और लिखने का कार्य करता है। यह एक छोटा-सा चुम्बक होता है, जो प्लैटर की सतह के ऊपर बहुत तेजी से दायें-बायें खिसकता है।
रीड राइट हेड को पकड़ने वाला भाग Read Write Arm (रीड राइट आर्म) कहलाता है। यह आर्म हेड को सही स्थान पर ले जाकर डेटा को पढ़ने या लिखने में मदद करता है।
Actuator (एक्टूएटर) वह भाग होता है, जिसकी सहायता से रीड राइट आर्म घूमता और हिलता है। यह रीड राइट हेड की मूवमेंट को नियंत्रित करता है।
Spindle (स्पिंडल) एक मोटर होती है, जो प्लैटर के बीच में स्थित रहती है। इसकी मदद से प्लैटर बहुत तेज गति से घूमता है।
हार्ड डिस्क में Logic Board (लॉजिक बोर्ड) भी होता है, जो इनपुट और आउटपुट डेटा को कंट्रोल करता है। इसके अलावा Circuit Board (सर्किट बोर्ड) हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करता है।
Connector (कनेक्टर) डेटा को सर्किट बोर्ड से रीड राइट हेड और प्लैटर तक पहुँचाने का कार्य करता है। अंत में HSA (Head Stack Assembly) रीड राइट आर्म का पार्किंग एरिया होता है, जहाँ कंप्यूटर बंद होने पर हेड सुरक्षित स्थिति में रहता है।
हार्ड डिस्क की विशेषताएँ
हार्ड डिस्क कंप्यूटर की एक महत्त्वपूर्ण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिये किया जाता है। इसकी कई विशेषताएँ होती हैं, जिनके कारण यह कंप्यूटर सिस्टम का एक आवश्यक भाग बन जाती है।
हार्ड डिस्क की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह Non-Volatile मेमोरी होती है। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर बंद होने या बिजली चले जाने पर भी इसमें संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो और अन्य आवश्यक फाइलें हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहती हैं।
हार्ड डिस्क की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी High Capacity (उच्च भंडारण क्षमता) है। यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। आधुनिक हार्ड डिस्क 256 GB से लेकर कई टेराबाइट (TB) तक डेटा स्टोर कर सकती है, जिससे बड़े आकार की वीडियो फाइलें, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है।
हालाँकि हार्ड डिस्क की एक सीमा यह है कि इसकी Speed (गति) RAM की तुलना में धीमी होती है। RAM की अपेक्षा हार्ड डिस्क डेटा को एक्सेस करने में अधिक समय लेती है, इसी कारण कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर इसका प्रभाव पड़ता है।
हार्ड डिस्क में Mechanical Parts (मैकेनिकल भाग) होते हैं, जैसे घूमने वाली प्लेट्स और रीड-राइट हेड। ये भाग मजबूत होते हैं और सामान्य उपयोग में जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन झटके या गिरने से नुकसान हो सकता है।
इसके अतिरिक्त हार्ड डिस्क के पीछे एक Circuit Board (सर्किट बोर्ड) लगा होता है, जो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बीच संचार स्थापित करता है। यही सर्किट बोर्ड डेटा के सही तरीके से ट्रांसफर होने में मदद करता है। इन सभी विशेषताओं के कारण हार्ड डिस्क कंप्यूटर की एक अनिवार्य स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है।