SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना एक नई केंद्र-सरकार की योजना है जो हाशिये पर रहने वाले व्यक्तियों को, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को, व्यापक कल्याण और पुनर्वास के उपाय प्रदान करती है। यह योजना दो मौजूदा उप-योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है, जिसका उद्देश्य इन समुदायों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है।
मुख्य उद्देश्य और विशेषताएँ
- समग्र पुनर्वास : SMILE का मुख्य उद्देश्य इन समुदायों के लिये बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएँ, परामर्श और बुनियादी दस्तावेज़ीकरण की सुविधा प्रदान करना है।
- शिक्षा और कौशल विकास :
- यह कक्षा 9वीं और उससे ऊपर के ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
- PM-DAKSH योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका के अवसर प्रदान किये जाते हैं।
- स्वास्थ्य और आवास :
- PM-JAY के सहयोग से, यह योजना लिंग-पुष्टि सर्जरी (gender-reaffirmation surgery) का समर्थन करने वाले अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्रदान करती है।
- 'गरिमा गृह' के रूप में आवास सुविधा प्रदान की जाती है, जो भोजन, कपड़े, मनोरंजन और चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करती है।
- संरक्षण और समर्थन : प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल स्थापित किये गए हैं ताकि अपराधों की निगरानी और समय पर जाँच सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन भी उपलब्ध है।
यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से लागू की जाएगी। यह अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें गरिमा और सशक्तिकरण के साथ जीवन जीने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं महिला सुरक्षा सूचकांक (NARI 2025) के अनुसार, जयपुर को महिला सुरक्षा के मामले में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले शहरों में शामिल किया गया है।
- NARI सूचकांक क्या है?
- प्रस्तुतकर्ता : पीवैल्यू एनालिटिक्स
- प्रकाशन : राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा दिल्ली में जारी
- कवरेज : भारत के 31 प्रमुख शहर
- मापदंड :
- महिलाओं की समग्र सुरक्षा की भावना
- उत्पीड़न के अनुभव (शारीरिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक आदि)
- दिन और रात की सुरक्षा में अंतर
- बुनियादी ढाँचा एवं प्रशासन पर विश्वास
- जयपुर का प्रदर्शन (NARI 2025 रिपोर्ट के अनुसार)
- कुल अंक : 59.1% (राष्ट्रीय औसत 64.6% से कम)
- स्थान : 25वाँ / 31 (सबसे निचले समूह में, पटना, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और राँची के साथ)।
- सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष
- उत्पीड़न का अनुभव :
- 8% महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना किया (राष्ट्रीय औसत: 7%)
- सुरक्षा का अनुभव (Day vs Night) :
- दिन : 31% महिलाओं ने शहर को “अत्यधिक सुरक्षित” माना।
- रात : केवल 10% महिलाओं ने इसे “अत्यधिक सुरक्षित” माना।
- बुनियादी ढाँचे पर विश्वास :
- 17% – “अत्यधिक सुरक्षित”
- 11% – “सुरक्षित”
- प्रशासन पर विश्वास :
- 24% – “अत्यधिक सुरक्षित”
- 12% – “अत्यधिक असुरक्षित”
- उत्पीड़न का अनुभव :
- शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता शहर
- कोहिमा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर
- इन शहरों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा।
- यहाँ महिलाओं ने दिन और रात दोनों समय सुरक्षा की उच्च अनुभूति दर्ज की।
- कोहिमा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर
- समग्र विश्लेषण
- जयपुर, अपनी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक महत्त्व के बावजूद, महिला सुरक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है।
- खासकर रात्रिकालीन असुरक्षा, उत्पीड़न की उच्च दर और प्रशासन पर विश्वास की कमी गंभीर चुनौतियाँ हैं।
- रिपोर्ट इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि केवल बुनियादी ढाँचे में सुधार नहीं, बल्कि प्रभावी कानून-व्यवस्था, संवेदनशील प्रशासन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव भी ज़रूरी है।
द्वितीय बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन 14–15 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम (भारत) में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय था – “भविष्य की दिशा में: ब्लू इकॉनमी, नवाचार और सतत साझेदारी।” इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के समुद्री सहयोग, नवाचार और सतत विकास पर व्यापक चर्चा हुई।
भारत के लिये प्रमुख महत्त्व
- समुद्री नेतृत्व व क्षेत्रीय एकीकरण
भारत द्वारा सम्मेलन की मेजबानी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री सहयोग में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत किया। यह भारत की सागरमाला परियोजना के लक्ष्यों के साथ भी पूरी तरह मेल खाता है, जो बंदरगाह आधारित विकास और बेहतर संपर्क (Connectivity) पर बल देती है।
- मुख्य पहल और रणनीतिक परिणाम
- बिम्सटेक समुद्री परिवहन सहयोग समझौते (AMTC) को शीघ्र लागू करने पर जोर दिया गया, जिससे क्षेत्रीय समुद्री व्यापार, बंदरगाह-आधारित विकास और संपर्क को प्रोत्साहन मिलेगा।
- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) को पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार व बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाले महत्त्वपूर्ण गलियारे के रूप में रेखांकित किया गया। यह परियोजना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव घटाकर संपर्क को सरल बनाएगी।
- भारत ने मुंबई में बिम्सटेक सतत समुद्री परिवहन केंद्र (Sustainable Maritime Transport Centre) स्थापित करने की घोषणा की, जो हरित नौवहन (Green Shipping), नीति समन्वय और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा।
- इको-फ्रेंडली क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया, जिससे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र एक टिकाऊ पर्यटन गलियारा बन सके।
- भारत की इंडो-पैसिफिक भूमिका को सशक्त करना : यह सम्मेलन भारत की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है। विशेषकर बिम्सटेक देशों के साथ संबंधों को गहरा करके भारत अपने समुद्री प्रभाव और आर्थिक पहुँच को विस्तारित करता है।
बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 भारत की समुद्री नवाचार, सतत विकास और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करता है, बल्कि बंगाल की खाड़ी को वैश्विक व्यापार और सतत साझेदारी का केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम है।
सड़क सुरक्षा और सुचारु यातायात के लिये पैदल यात्रियों और वाहन चालकों दोनों को कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिये।
पैदल यात्रियों के लिये नियम-
- फुटपाथ का प्रयोग करें- हमेशा फुटपाथ पर चलें। यदि न हो, तो सड़क के बाएं कोने में यातायात की दिशा की ओर देख कर चलें।
- ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें- सड़क पार करने के लिये ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फुटओवर ब्रिज या अंडरपास का प्रयोग करें।
- सिग्नल का पालन करें- पैदल यात्री सिग्नल का ध्यानपूर्वक पालन करें और संकेत मिलने पर ही सड़क पार करें।
- अचानक सड़क पार न करें- खड़े वाहनों के बीच से या तेज़ यातायात में सड़क पार न करें।
- सतर्क रहें- मोबाइल फोन या ईयरफोन का उपयोग सड़क पर चलते समय न करें।
- बच्चों और बुजुर्गों को सहारा दें- सड़क पार कराते समय इन पर विशेष ध्यान दें।
वाहन चालकों के लिये नियम-
- गति सीमा का पालन करें- क्षेत्र के अनुसार निर्धारित गति सीमा का पालन करें (स्कूल, रिहायशी क्षेत्र, हाईवे आदि)।
- सड़क संकेतों और सिग्नल का पालन करें- ट्रैफिक लाइट, स्टॉप साइन आदि का सम्मान करें।
- पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दें- ज़ेब्रा क्रॉसिंग या बिना सिग्नल वाली जगहों पर पैदल यात्रियों को पहले रास्ता दें।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में ओवरटेक न करें- स्कूल, अस्पताल आदि के पास ओवरटेक करना मना है।
- इंडिकेटर का प्रयोग करें- मुड़ने या लेन बदलने से पहले संकेत दें।
- नशे में या लापरवाही से वाहन न चलाएं- यह कानूनन अपराध है और खतरनाक भी।
- दस्तावेज़ रखें- ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र हमेशा साथ रखें।
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मेहरानगढ़ किले (जोधपुर) में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान आवां पंचायत (टोंक) के सरपंच दिव्यांश एम. भारद्वाज को उनके अभिनव नेतृत्व और सामुदायिक पहल के लिये राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच के पुरस्कार से सम्मानित किया। वे राजस्थान के 41 जिलों की 11,341 पंचायतों में से एकमात्र पुरस्कार विजेता हैं।
- मुख्य उपलब्धियाँ (आवां पंचायत मॉडल)
- सहायक बुनियादी ढाँचा
- लड़कों और लड़कियों हेतु अलग-अलग वातानुकूलित पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधा सहित।
- दो श्मशान घाट और एक हेरिटेज पंचायत भवन का निर्माण।
- राजकालेश्वर तीर्थ पर घाट, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल व ड्रेसिंग रूम का विकास।
- क्षमता निर्माण एवं नवाचार
- शैक्षिक उद्देश्यों हेतु छात्रों की हवाई यात्रा प्रायोजित की।
- बालिका दिवस पर एक छात्रा को प्रतीकात्मक सरपंच नियुक्त कर महिला नेतृत्व को बढ़ावा।
- आदर्श मॉडल
- दिव्यांश की पहल ने आवां को उत्कृष्टता का मॉडल बनाया।
- इसका अनुकरण महाराष्ट्र में करने पर विचार।
- सहायक बुनियादी ढाँचा
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025
-
- प्रदानकर्ता : प्रधानमंत्री
- अवसर : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल, मधुबनी, बिहार)
- उद्देश्य : पंचायतों को 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़े 9 स्थानीय विकास लक्ष्यों (LSDGs) पर आधारित प्रदर्शन के लिये सम्मानित करना।
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की विशेष श्रेणियाँ :
- जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (CASPA): जलवायु के प्रति संवेदनशील पंचायतों के लिये।
- आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (ANPSA): स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये।
- पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (PKNSSP): पंचायती राज प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिये।
-
भारत अपनी भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों के लिये विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ विशाल पर्वत, विस्तृत वन, लंबी नदियाँ, अद्भुत स्थापत्य और अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहरें मौजूद हैं। यह सूची भारत के उन प्रमुख "सबसे बड़े", "सबसे लम्बे" और "सबसे ऊँचे" स्थलों व विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जो न केवल सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
|
क्रम |
श्रेणी |
स्थान / नाम |
अतिरिक्त जानकारी / राज्य |
|
1 |
सबसे लंबा सड़क पुल |
महात्मा गांधी सेतु |
पटना, बिहार – गंगा नदी पर, लंबाई लगभग 5.75 किमी |
|
2 |
सबसे बड़ा पशु मेला |
सोनपुर मेला |
बिहार – हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित |
|
3 |
सबसे ऊँची मीनार |
कुतुब मीनार |
दिल्ली – ऊँचाई 72.5 मीटर, 12वीं शताब्दी में निर्मित |
|
4 |
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील |
वूलर झील |
जम्मू-कश्मीर |
|
5 |
सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बाँध |
भाखड़ा नांगल बाँध |
पंजाब – सतलुज नदी पर, ऊँचाई 226 मीटर |
|
6 |
सबसे बड़ा रेगिस्तान |
थार रेगिस्तान |
राजस्थान |
|
7 |
सबसे बड़ा गुफा मंदिर |
कैलाशनाथ मंदिर |
एलोरा, महाराष्ट्र – 8वीं शताब्दी |
|
8 |
सबसे बड़ा चिड़ियाघर |
अलीपुर ज़ूलॉजिकल गार्डन |
कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
|
9 |
सबसे बड़ी मस्जिद |
जामा मस्जिद |
दिल्ली – निर्माण 1656 ई. में शाहजहाँ द्वारा |
|
10 |
सबसे ऊँची पर्वत चोटी |
गॉडविन ऑस्टिन (K-2) |
काराकोरम श्रृंखला, ऊँचाई 8,611 मीटर |
|
11 |
सबसे लंबी सड़क सुरंग |
जवाहर सुरंग |
जम्मू-कश्मीर – लंबाई 2.85 किमी |
|
12 |
सबसे बड़ा डेल्टा |
सुंदरबन डेल्टा |
पश्चिम बंगाल – गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का संगम |
|
13 |
सबसे अधिक वनों वाला राज्य |
मध्य प्रदेश |
कुल वन क्षेत्रफल लगभग 77,493 वर्ग किमी (भारत में सबसे अधिक) |
|
14 |
सबसे लंबा मंदिर गलियारा |
रामेश्वरम मंदिर |
तमिलनाडु – लंबाई लगभग 1,200 मीटर |
|
15 |
सबसे ऊँचा झरना |
जोग फॉल्स |
कर्नाटक – ऊँचाई लगभग 253 मीटर |
|
16 |
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग |
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH-44) |
लंबाई लगभग 3,745 किमी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक |
|
17 |
सबसे ऊँचा द्वार |
बुलंद दरवाजा |
फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश – ऊँचाई लगभग 54 मीटर |
|
18 |
सबसे लंबी नदी |
गंगा नदी |
कुल लंबाई 2,525 किमी (भारत में लगभग 2,510 किमी) |
|
19 |
सबसे बड़ा संग्रहालय |
भारतीय संग्रहालय |
कोलकाता, पश्चिम बंगाल – स्थापना 1814 |
|
20 |
सबसे बड़ा गुम्बद |
गोल गुम्बद |
बीजापुर, कर्नाटक – व्यास लगभग 44 मीटर |
हाल ही में केरल और तमिलनाडु द्वारा संयुक्त रूप से किये गए एक व्यापक सर्वेक्षण में कुल 2,668 नीलगिरी तहर (Nilgiritragus hylocrius) दर्ज किये गए :
- केरल : 1,365
- तमिलनाडु : 1,303
यह आँकड़ा देश की स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण में हुई प्रगति को दर्शाता है और साथ ही नीलगिरी तहर जैसे संवेदनशील जीवों की रक्षा के लिये जारी प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- नीलगिरी तहर : परिचय और विशेषताएँ
- सामान्य नाम : वरयाडू या नीलगिरी आइबेक्स
- वैज्ञानिक नाम : Nilgiritragus hylocrius
- परिवार : Caprinae (कप्रीन खुरधारी स्तनधारी)
- स्थानिकता : केवल पश्चिमी घाट तक सीमित
- राज्य पशु : तमिलनाडु
यह प्रजाति 1,200 से 2,600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित पर्वतीय घास के मैदानों (Montane Grasslands) और शोला वनों में निवास करती है। यह मुख्यतः चट्टानी ढलानों और ऊँचे घास वाले क्षेत्रों में सक्रिय रहती है।
- मुख्य वितरण क्षेत्र
- केरल :
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (ENP) – सर्वाधिक संख्या
- तमिलनाडु :
- पलानी हिल्स
- श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिज़र्व
- अगस्त्यमलाई क्षेत्र
- केरल :
- व्यवहार और जीवन चक्र
- प्रकृति : दिवाचर (दिन में सक्रिय)
- औसत जीवनकाल : 3 – 3.5 वर्ष
- अनुकूल परिस्थिति में जीवनकाल : 9 वर्ष तक
- सामाजिक संरचना : झुंडों में रहना पसंद करती है; नर और मादा अलग-अलग समूहों में भी देखे जा सकते हैं।
- प्रमुख खतरे
नीलगिरी तहर की संख्या में गिरावट के पीछे कई पारिस्थितिक और मानवजनित कारण हैं :- आवासीय क्षरण :
- वनों की कटाई
- जलविद्युत परियोजनाएँ
- एकल प्रजाति वृक्षारोपण (Monoculture Plantation)
- पालतू पशुओं के साथ चरागाह की प्रतिस्पर्धा
- अवैध शिकार
- स्थानीय विलुप्ति : विशेषकर कर्नाटक की पहाड़ी श्रृंखलाओं से
- आवासीय क्षरण :
- पारिस्थितिक महत्त्व
- यह प्रजाति पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक संतुलन में अहम भूमिका निभाती है।
- यह बाघ और तेंदुए के लिये एक प्रमुख शिकार प्रजाति है।
- नीलगिरी लंगूर और लायन-टेल्ड मकाक जैसी अन्य स्थानिक प्रजातियों के साथ सह-अस्तित्व में रहती है।
- इसकी उपस्थिति किसी क्षेत्र के पर्वतीय घासभूमि के स्वास्थ्य का संकेतक मानी जाती है।
- संरक्षण स्थिति
|
मंच / कानून |
स्थिति |
|
IUCN रेड लिस्ट |
संकटग्रस्त (Endangered) |
|
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 |
अनुसूची-I (सर्वोच्च संरक्षण) |
- नेत्रदान चाक्षुष-विकृति युक्त कॉर्निया-अंधता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये अमूल्य दान है।
- नेत्रदान किसी भी लिंग, आयु अथवा सामाजिक स्तर का व्यक्ति चाहे वह चश्मा क्यों न लगाए, कर सकता है।
- एड्स, हेपेटाइटिस B या C, जलभीति (Rabies), ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, मस्तिष्क शोध से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं।
- नेत्रदान मृत्यु के 4-6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर या अस्पताल में किया जाता है। इसके लिये इच्छुक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर नेत्र धरोहर के रूप में रखने होते हैं, जिसकी जानकारी निकट संबंधियों को दे देनी चाहिये। कोई व्यक्ति ब्रेल किट भी दान कर सकता है।
प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन्स (मुख्यतः मीथेन) का मिश्रण है जिसे भूमि से प्राप्त करते हैं, परंतु यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इसे उच्च दाब पर संपीडित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas-CNG) के रूप में भंडारित कर इससे ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। कम प्रदूषणकारी होने के कारण अब इसे परिवहन साधनों के ईंधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा है। पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक परिवहन होने से यह आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है।
- आज पाइपों द्वारा घरों एवं कारखानों में CNG की आपूर्ति होने से अधिक-से-अधिक लोगों तक इसका सीधा लाभ पहुँचाया जा रहा है।
- अनेक रसायनों एवं उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में प्राकृतिक गैस प्रारंभिक पदार्थ के तौर पर उपयोग में लाई जाती है। उदाहरणार्थ प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है।
- भारत में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त पदार्थ पेट्रोरसायन (Petrochemicals) कहे जाते हैं जिनका उपयोग अपमार्जक, रेशे (पोलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक आदि), पॉलिथीन एवं अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है।
यह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ईंधन है, जिसका उपयोग स्कूटर, मोटर साइकिल, कार आदि हल्के वाहनों के संचालन में पेट्रोल (Petrol) के रूप में; जबकि ट्रेक्टर, बस, ट्रक जैसे भारी वाहनों में डीज़ल (Diesel) के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम शब्द पेट्रा (चट्टान) एवं ओलियम (तेल) के मेल से बना है जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पेट्रोलियम भूमि के नीचे स्थित चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है।
- मृत समुद्री जीवों के शरीर के सागर की निचली सतह में जमने और ऊपर से रेत-मिट्टी की मोटी परतों से ढक जाने के पश्चात् ये लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप-दाब पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं। किंतु अत्यंत धीमी प्रक्रिया और निर्माण की जटिल परिस्थितियों के कारण इसका निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। तेल और गैस के जल से हल्के होने के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सतहें जल की सतह से ऊपर होती हैं।
- 1859 में विश्व का प्रथम तेल कुआं अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में ड्रिल किया गया था। 1867 में असम के माकुम में तेल के होने का पता चला। आज गुजरात, बॉम्बे हाई समेत गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बेसिन में भी तेल कुएं हैं।
- अत्यधिक व्यावसायिक महत्त्व के कारण पेट्रोलियम को ‘काला सोना’ (Black Gold) भी कहते हैं।
पेट्रोलियम का परिष्करण
पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीज़ल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, कैरोसिन तेल, बिटुमेन आदि संघटकों से निर्मित अप्रिय गंध वाला गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। इसके विभिन्न संघटकों/प्रभाजों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है जिसका संपादन पेट्रोलियम परिष्करणी (Petroleum Refinery) में किया जाता है।
- फायर मूंगे, मूंगा (Coral) प्रजाति के ऐसे जंतु हैं जो मूंगे से ज़्यादा जेलीफिश (Jelly Fish) के गुण रखते हैं। स्पर्श होने पर वैसी ही चुभन होती है जैसी जेलीफिश के स्पर्श होने पर होती है।
- इनका वैज्ञानिक नाम मिलीपोरा (Millepora) है। इनके शरीर की ऊपरी सतह पर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं।
- ये पीले या भूरे रंग के होते हैं। मिलीपोरा जंतु समुद्र से नदी क्षेत्र में आने वाले गंदे पानी में एवं समुद्र के अपतटीय भाग में पाए जाते हैं।
- संभवतः ये प्रजातियाँ भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर और थाईलैंड से खत्म हो चुकी हैं।
- सजावट के रूप में एवं ज्वैलरी व्यापार में इनका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अधिक तापमान में ये प्रजाति जीवित नहीं रह पाती।
- बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग एवं ब्लीचिंग प्रभाव के कारण यह अति संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में आता है।
- जल निकायों का संरक्षण (Conservation of Water Bodies)- भारत की अधिकतर नदियाँ तथा झीलें प्रदूषण की शिकार हैं तथा इनका जल पीने योग्य नहीं रह गया है। यहाँ की नदियों एवं तालाबों के जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत असंसाधित मल-जल प्रवाह है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय’ का कार्य केंद्र प्रायोजित स्कीमों ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)’ एवं ‘जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना’ (NPCA) के तहत नदियों, झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan–GAP)- देश की प्रमुख नदियों में से एक तथा स्वयं का निर्मलीकरण (गंगा में पाए जाने वाले वायरस जैसे Bacteriophage वगैरह जीवाणुओं को खा जाते हैं।) करने वाली गंगा आज लगभग अपने अपवाह के आधे भाग में प्रदूषित हो गई है। वर्तमान में लगभग 50,000 से अधिक आबादी वाले 100 से अधिक शहरों का असंसाधित मल-अपशिष्ट गंगा में अपवाहित किया जाता है तथा हज़ारों की संख्या में लाशों व जले हुए अवशेषों को इसमें प्रवाहित किया जाता है। गंगा बेसिन में भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ‘केंद्रीय गंगा प्राधिकरण’ (CGA) का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान (GAP) की शुरुआत की गई।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan)- 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण (CGA) का नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण’ (NRCA) कर दिया गया था। गंगा कार्य योजना का विलय NRCP के साथ कर दिया गया।
- नमामि गंगे कार्यक्रम (Namami Gange Project)- केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिये 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को खत्म करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य स्तंभ हैं-
- सीवरेज ट्रीटमेंट
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
- वनीकरण
- जैव विविधता का विकास
- जन-जागरूकता
- गंगा ग्राम योजना
- नदी सतह की सफाई
- औद्योगिक प्रवाह निगरानी
उदयपुर के संस्थापक एवं मेवाड़ के शासक
प्रारंभिक जीवन
- महाराणा उदय सिंह का जन्म 1522 ई. में हुआ था। ये राणा सांगा के पुत्र थे।
- पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता फैल गई थी।
- महाराणा उदय सिंह को बचपन में बनवीर के षड्यंत्र से पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचाया था।
राजगद्दी और शासनकाल
- वर्ष 1540 में महाराणा उदय सिंह बनवीर को पराजित कर मेवाड़ के शासक बने।
- अपने शासन काल में अफगानों और मुगलों के कई हमलों का सामना किया।
- उन्होंने युद्ध से अधिक राजपूत विरासत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
उदयपुर की स्थापना (1559)
- 1567-68 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
- उदय सिंह ने प्रत्यक्ष युद्ध न करके राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
- उदयपुर की स्थापना की, जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा और पिछोला झील के किनारे स्थित था।
- यह स्थान प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और बाद में एक समृद्ध राजधानी बना।
निर्णय का महत्त्व
- कुछ लोग इसे पलायन मानते हैं, लेकिन यह एक रणनीतिक निर्णय था जिससे मेवाड़ की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
- उनके पुत्र महाराणा प्रताप को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करने का अवसर मिला।
- वे राजपूत संस्कृति और गौरव की रक्षा करने वाले शासक माने जाते हैं।
मृत्यु और विरासत
- 1572 में निधन हुआ।
- उदयपुर के संस्थापक के रूप में स्मरणीय।
- उनकी दूरदर्शिता से मेवाड़ का अस्तित्व सुरक्षित रहा।
- आज उदयपुर "झीलों की नगरी" के नाम से प्रसिद्ध है और राजपूत वीरता का प्रतीक है।
- शाखा बैंकिंग- प्रधान शाखा के निर्देशन में बैंक की छोटी शाखाओं द्वारा बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना शाखा बैंकिंग कहलाता है।
- नेट बैंकिंग- इंटरनेट तथा कंप्यूटर की सहायता से उपभोक्ता द्वारा अपने बैंकिंग खातों का स्वयं संचालन व भुगतान, हस्तांतरण करना नेट बैंकिंग कहलाता है।
- कोर बैंकिंग- कोर बैंकिंग में किसी वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएँ इंटरनेट के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसमें कोई भी शाखा दूसरी शाखा के खाते का विवरण देखने, जमा अथवा निकासी करने में सक्षम होती है।
- NEFT प्रणाली- यह एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसके ज़रिये धन राशि के हस्तांतरण में कुछ समय लगता है अर्थात् यह एक रियल टाइम प्रणाली नहीं है।
- RTGS प्रणाली- इसके तहत धन का हस्तांतरण वास्तविक समय में होता है जिसकी अधिकतम अवधि 30 मिनट है। इस प्रणाली से न्यूनतम 2 लाख या इससे अधिक राशि एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित की जा सकती है। अधिकतम धन हस्तांतरण की सीमा बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है। NEFT तथा RTGS का प्रबंधन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है।
- ECS प्रणाली- ‘इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग स्कीम’ के माध्यम से बैंक अपने खाता धारक की लिखित अनुमति के बिना किंतु उसकी सहमति से अन्य संस्था को नियमित रूप से धन हस्तांतरण करता है। जैसे- ब्याज, वेतन, पेंशन, लाभांश आदि।
- IFSC कोड- Indian Financial System Code, 11 अंकीय कोड होता है जो प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा रहता है। इसके पहले के चार अक्षरों में बैंक का नाम, अगला अंक शून्य तथा अंतिम 6 अंकों में बैंक ब्रांच से संबंधित विवरण होता है।
- तनावमूलक बल के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इस प्रकार से निर्मित घाटी को ‘भ्रंश घाटी’ कहते हैं।
- बलार्ड की परिकल्पना रिफ्ट (भ्रंश) घाटी की उत्पत्ति से संबंधित है।
- यह कई किलोमीटर तक विस्तृत हो सकती है। विस्थापन का स्वरूप क्षैतिज, तिर्यक या लंबवत हो सकता है। जर्मन भाषा में इसे ‘ग्राबेन’ कहा जाता है।
- भ्रंश घाटी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-
- भारत की नर्मदा एवं ताप्ती तथा ऊपरी दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं।
- मृत सागर बेसिन;
- दक्षिण कैलिफोर्निया की मृत घाटी (Death Valley);
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी;
- यूरोप में राइन नदी घाटी;
- नील नदी की घाटी;
- विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीका की ‘महान भ्रंश घाटी’ (Great African Rift Valley) है। इसी भ्रंश में न्यासा, रुडोल्फ (तुर्काना), तांगान्यीका आदि झीलें स्थित हैं।
- बैकाल झील तथा लाल सागर भी भ्रंश घाटियाँ हैं।
- लाल सागर का निर्माण भ्रंश घाटी के अक्षीय द्रोणी के फलस्वरूप हुआ है।
- विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वार बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ने पर विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है और बल्ब दीप्त हो उठता है।
- विद्युत परिपथ, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के मध्य विद्युत प्रवाह (विद्युत धारा) के संपूर्ण पथ को दर्शाता है।
- बल्ब के दीप्त होने के लिये परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होना आवश्यक है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है।
- किन्हीं कारणों से बल्ब के तंतु के टूट जाने यानी बल्ब के फ्यूज हो जाने पर परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है और बल्ब दीप्तिमान नहीं हो पाता।
- विद्युत धारा में मान और दिशा दोनों होते हैं; किंतु सदिशों के योग के नियम का अनुकरण नहीं करने के कारण यह अदिश राशि है।
- किसी प्रकाश स्रोत से निकले प्रकाश के रास्ते में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उस प्रकाश अवरोधक वस्तु के दूसरी ओर उसी के जैसी काली आकृति बनती है, जिसे ‘छाया’ कहते हैं।
- छाया देखने के लिये एक प्रकाश स्रोत, प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु तथा अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक परदे का होना आवश्यक है। दैनिक जीवन में दिखने वाली छायाओं के लिये ज़मीन, दीवार, इमारत या ऐसी ही अन्य सतहें परदे का कार्य करती हैं।
- कई बार तो छायाओं को देखकर हमें वस्तु की आकृति की जानकारी भी प्राप्त होती है, किंतु कई बार छायाएँ भ्रम भी उत्पन्न करती हैं। हम अपने हाथों की मुद्राओं से विविध जंतुओं की छाया होने के भ्रम पैदा कर सकते हैं।
- किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा छाया बनाने से यह साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसी कारण, हम सीधे पाइप से उस पार की वस्तुएँ देख सकते हैं पर मुड़े हुए पाइप से उस पार की वस्तुएँ नहीं देख सकते।
- पतली झिर्री या छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते देखना, मोटर वाहनों के अग्रदीपों से आते किरण पुंजों को देखना, टॉर्च के प्रकाश के किरण पुंज को देखना या विमानपत्तन के टॉवर की सर्चलाइट के किरण पुंज को देखना भी प्रकाश के सरल रेखा में गमन को दर्शाता है।
- रामकिंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला कला का जनक कहा जाता है।
- इनका जन्म 25 मई, 1906 को पश्चिम बंगाल के बाँकुड़ा ज़िले में हुआ था।
- इन्होंने शांतिनिकेतन में नंदलाल बोस के सान्निध्य में कला की शिक्षा ली।
- ये प्रथम भारतीय मूर्तिकार हैं जिन्होंने सीमेंट व कंकरीट माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर मूर्तियों की रचना की।
- भारतीय कला में इनके अतुलनीय योगदान के लिये वर्ष 1970 में भारत सरकार ने इन्हें ‘पद्मविभूषण’ से सम्मानित किया।
- शांतिनिकेतन में इन्हें ‘किंकर दा’ के नाम से जाना जाता था।
- रामकिंकर बैज मुख्यतः मूर्तिकार थे, लेकिन चित्रकार के रूप में भी इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
- इन्होंने अपनी चित्रकला का प्रारंभ लघु चित्रों से किया। लेकिन बाद में ‘तैल रंगों’ में भी चित्रकारी करने लगे।
- इन्होंने तैल माध्यम में व्यक्ति चित्र तथा विशाल अमूर्त चित्र बनाए, जिसके उदाहरण हैं- सुजाता, कन्या और कुत्ता, अनाज की ओसाई, माँ-बेटा, कृष्ण-जन्म, शीतकालीन मैदान आदि।
- इनके चित्रों में यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है।
- भारतीय कला में सबसे पहले आधुनिकतावादियों में से एक रामकिंकर बैज ने यूरोपीय आधुनिक दृश्य भाषा की शैली को आत्मसात किया।
- इन्होंने आलंकारिक शैली एवं भावनात्मक शैली में अपनी कला को प्रदर्शित किया।
- उनकी थीम मानवतावाद की गहरी समझ और मनुष्य एवं प्रकृति के बीच पारस्परिक निर्भरता वाले संबंधों की सहज समझ से जुड़ी होती थी।
- प्रतिमाओं को सहज और सुंदर बनाने के लिये इन्होंने सीमेंट, लेटराइट एवं गारे का उपयोग किया।
- इनकी कला में हमें आधुनिक पश्चिमी एवं पूर्व भारतीय शास्त्रीय मूर्तिकला मूल्यों का समावेश मिलता है।
- इन्हें वर्ष 1976 में विश्व भारती द्वारा मानद डॉक्टरल उपाधि ‘देशोत्तम’ से सम्मानित किया गया।
- बैज की कला का मुख्य विषय सामान्य जन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और परिवेश से प्रेरित रहा।
- रामकिंकर बैज अमूर्तन और एक्सप्रेसेनिस्ट शैली में काम करने वाले भारत के प्रथम मूर्तिकार थे।
- रामकिंकर बैज ने आधुनिक कला की सभी प्रवृत्तियों, जैसे- यथार्थवाद, घनवाद से लेकर अतियथार्थवाद आदि को सहज रूप में अपनाया।
- रामकिंकर बैज के व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रभावित होकर बांग्ला के चर्चित उपन्यासकार ‘समरेशु बसु’ ने ‘देखी नाई फिरे’ नाम से उनके ऊपर किताब लिखी।
- रामकिंकर बैज की कुछ प्रमुख मूर्तिशिल्प
- ‘यक्ष-यक्षिणी’ की पाषाण मूर्ति जो 24 फीट ऊंची है तथा वर्तमान में यह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में स्थापित है।
- प्रसिद्ध मूर्ति ‘दोपहर की विश्रांति में श्रमिक’ मेहनतकश मजदूरों तथा किसानों के जीवन को दर्शाती है।
- इनके द्वारा निर्मित प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध ‘पार्श्व’ है।
- ‘मिलकॉल’, ‘महात्मा बुद्ध’ तथा ‘संथाल परिवार’ आदि इनके अन्य प्रमुख मूर्तिशिल्प हैं।
|
नाम |
क्षेत्र |
|
मसोले |
कांगो-जायरे नदी बेसिन |
|
फैंग |
अफ्रीका में (विषुवतरेखीय प्रदेशों में) |
|
मिल्पा |
ग्वाटेमाला एवं यूकाटन |
|
लोगन |
पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में |
|
इचाली |
ग्वाडेलूप |
|
कोनूल/कोमिले |
मेक्सिको |
|
मिल्पा |
मध्य अमेरिकी देश में एवं मेक्सिको |
|
कोनूको |
वेनेजुएला |
|
रोका |
ब्राज़ील |
|
कैंगिन |
फिलीपींस |
|
तुंग्या/टांग्या |
म्यांमार |
|
चेन्ना |
श्रीलंका |
|
लेदांग |
जावा एवं मलेशिया |
|
रे |
लाओस एवं वियतनाम |
|
टावी |
मालागासी |
|
हुमा |
इंडोनेशिया एवं जावा |
|
देश |
गुप्तचर संस्थाएँ |
|
चीन |
Ministry of State Security – MSS (पूर्व में सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट) |
|
रूस |
के.जी.बी./जी.आर.यू. |
|
दक्षिण अफ्रीका |
State Security Agency- SSA (पूर्व में ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्यूरिटी) |
|
यू.के. |
एम.आई. (मिलिट्री इंटेलीजेंस)- 5 एवं 6, ज्वाइंट इंटेलीजेंस आर्गेनाइजेशन |
|
पाकिस्तान |
इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आई.एस.आई.) |
|
भारत |
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW), इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) |
|
यू.एस.ए. |
सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (CIA), फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) |
|
इज़राइल |
मोसाद |
|
मिस्र |
जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट (मुखबरात) |
|
जापान |
नाइचो |
|
ईरान |
सावाक |
|
इराक |
अल मुखबरात |
माइक्रोवेव ओवन एक रसोईघर उपकरण है, जो कि खाना पकाने और खाना गर्म करने के काम आता है।
सिद्धांत (Principle)
- माइक्रोवेव गैर-आयनित विकिरण होता है, जो विद्युत-चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन नाम की एक वैक्यूम ट्यूब होती है। इस ट्यूब से लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज (GHz) आवृत्ति की माइक्रोवेव निकलती हैं।
- जब माइक्रोवेव्स किसी पोलर मॉलीक्यूल (जैसे- जल, वसा या शुगर) के संपर्क में आती हैं तो अणुओं में घूर्णन होता है, जिस कारण वे एक-दूसरे से टकराते हैं। चूँकि तापमान गतिज ऊर्जा से संबंधित है इसलिये उसमें वृद्धि होती है। अतः माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने या गर्म करने हेतु इन पोलर मॉलीक्यूल का होना आवश्यक है।
माइक्रोवेव ओवन के लाभ (Advantages of Microwave Oven)
- माइक्रोवेव ओवन केवल खाने को ही गर्म करता है, कंटेनर और आस-पास की हवा को नहीं।
- माइक्रोवेव एक गैस स्टोव की तुलना में खाना गर्म करने के लिये बहुत कम समय लेता है।
- अमेरिकी ऊर्जा दक्षता एजेंसी ने एक शोध में पाया है कि माइक्रोवेव ओवन गैस स्टोव की तुलना में ऊर्जा का प्रयोग करने में तो निश्चित रूप से बेहतर होते हैं, हालाँकि इलेक्ट्रिक हीटिंग या इंडक्शन कुकिंग की तुलना में यह उतने कुशल नहीं हैं।
समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के आधार पर इसके महत्त्पूर्ण मॉडल निम्नलिखित हैं-
- सांख्यिकीय मॉडल (Statistical Models) : व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण इस मॉडल की उत्त्पति हुई है । व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बच्चों तथा व्यक्तियों में अंतर पाए जाते हैं। उनमे पाया जाने वाला यह अंतर ही बच्चों की विशिष्टता के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कभी भी दो बच्चे एक समान नहीं होते हैं, उनमें प्राय: कुछ-न-कुछ विभिन्नता ज़रूर होती है।
- मौखिक संचार मॉडल (Oral Communication Model) : इस प्रकार के मॉडल में भिन्न बच्चे मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं। जिनका उल्लेख निम्नलिखित है-
- कथन क्षतियुक्त बच्चे : कथन क्षतियुक्त बच्चों में हकलाना, स्वरदोष जैसे बोलने के दोष होते हैं।
- भाषायी दिव्यांग बच्चे : ऐसे बच्चे हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जो कि उनके वातावरण अर्थात् घर, स्कूल, बाज़ार में बोली जा रही है। ऐसे बच्चे मातृभाषा ठीक ढंग से नहीं बोल पाते हैं। इस प्रकार के बच्चों के मौखिक संचार में भिन्नता पाई जाती है। अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुँचा पाना इनकी प्रमुख समस्या होती है। इसके कारण संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित, सीखने में मंद गति, व्यक्तित्व संबंधी दोष, पिछड़ापन जैसे परिणाम सामने आते हैं।
- चिकित्सीय अथवा जीव-विधा मॉडल (Medical or Biological Model) : इस प्रकार के मॉडल के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे शामिल होते हैं। बच्चों में इस प्रकार की शारीरिक भिन्नता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है-
- आनुवंशिक कारणों की वजह से भी कई बार शारीरिक अक्षमता आ जाती है।
- जन्म के पश्चात् किसी प्रकार से चोट लगने के कारण भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है।
- जन्म के समय होने वाली किसी प्रकार क्षति के कारण भी कई बार शारीरिक अक्षमता आ जाती है।
- जन्म-पूर्व क्षति अर्थात् जन्म से पूर्व यदि गर्भवती महिला किसी दवा का सेवन कर ले अथवा अन्य कोई ऐसे कार्य कर ले जिनमें गर्भ समस्या उत्पन्न हो जाए तो बच्चों में शारीरिक अक्षमता आ सकती है।
- सांस्कृतिक मॉडल (Cultural Model) : इस प्रकार के मॉडल में मुख्यत: सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बच्चों को शामिल किया जाता है। ऐसे बच्चों को वे सुविधाएँ नहीं प्राप्त होती हैं जो प्राय: सामान्य बच्चों को प्राप्त हो जाती हैं। अत: इनका अधिगम स्तर गिर जाता है। यही कारण है कि इनके लिये सामान्य शिक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त शैक्षिक प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है।
- मनोसामाजिक मॉडल (Psychosocial Model) : इस मॉडल में मनोसामाजिक रूप से अलग-अलग प्रवृति वाले बच्चे आते हैं। संवेगात्मक रूप से परेशान बच्चे को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे भावनाओं का प्रबंधन सही ढंग से नहीं कर पाते, अत: वे संवेगात्मक असंतुलन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ऐसे बच्चे अपने लिये और अन्य लोगों के लिये कठिनाई उत्पन्न करते हैं।
संविधान प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मानवता की प्रगति के लिये समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शिक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पहुँचे। इसे पूरा करने के लिये समावेशी शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। इस दृष्टि से हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
- आवश्यकता-
- सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है।
- बच्चों में उनकी सीखने की क्षमता और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भेदभाव मिटाने के लिये समावेशी शिक्षा आवश्यक है।
- बच्चों के शैक्षणिक और सामाजिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये।
- सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा विशेष बच्चों को समाज व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये।
- बच्चों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा स्थापित करने के लिये।
- बच्चों में भय को कम करने, दोस्ती का निर्माण व आत्मविश्वास की क्षमता के लिये।
- समूह में सुरक्षा और सुरक्षित भावना के विकास तथा विविधता के बीच व्यक्तिगत क्षमतानुसार आत्मविश्वास के लिये।
- महत्त्व-
- समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिये उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
- यह अन्य विद्यार्थियों को अपनी उम्र के साथ कक्षा में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिये अभिप्रेरित करती है।
- समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।
- यह सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिये भी अवसर प्रदान करती है।
- समावेशी शिक्षा गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। साथ ही यह बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के साथ रहने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिये स्कूल का माहौल बेहतर हो सकता है।
- यह प्रथा भेदभाव को दूर करने में मदद कर सकती है जो समाज के हर क्षेत्र में व्यापक है।
- यह राष्ट्र के विकास के लिये व्यक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ावा देती है।
विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है-
- विकास का प्रतिरूप- विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं, मस्तकाधोमुखी दिशा तथा निकट से दूर दिशा में होता है। प्रथम प्रकार की दिशा में शारीरिक विकास ‘सिर से पैर की ओर’ होता था। वहीं दूसरे प्रकार की दिशा में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है उसके पश्चात् केंद्र से दूर के भागों में होता है।
- विकास की दिशा- विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। कोई भी बालक विकासक्रम में पहले सामान्य क्रियाएँ संपादित करता है उसके बाद विशेष क्रियाओं की तरफ जाता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है।
- विकास अवस्थाओं का पालन- विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। बालक को सामान्य रूप से देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि उसका विकास रुक-रुक कर हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के रूप में जब बालक के दूध के दाँत निकलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि दाँत एकाएक निकल आए, परंतु इसकी नींव गर्भावस्था के पाँचवे महीने में पड़ जाती है और ये जन्म के बाद 5-6 महीने में आते हैं।
- विकास में व्यक्तिगत विभेद- विकास में व्यक्तिगत विभेद हमेशा स्थिर होते हैं। जिस बालक में शारीरिक क्रियाएँ जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेज़ी से होता है। इसके उलट जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति धीमी होती है उनमें मानसिक और अन्य प्रकार का विकास भी विलंब से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं।
- विकास की गति में विभिन्नता- विकास की गति में तीव्रता और मंदता विद्यमान होती है। व्यक्ति का विकास सदैव एक ही गति से नहीं होता बल्कि उसमें निरंतर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उदाहरण के लिये विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है उसके पश्चात् मंद पड़ जाती है।
- परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम- बालक का विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। परिपक्वता का अर्थ व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के अंदर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप उसके शारीरिक अंग अपने-आप परिपक्व हो जाते हैं। उसके लिये उसे वातावरण से मदद नहीं लेनी पड़ती है। वहीं शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में मदद प्रदान करते हैं। ये सीखने के लिये परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं।
- विकास की प्रक्रिया- विकास एक अविराम प्रक्रिया है। यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के रूप में शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक चलता रहता है, लेकिन कालांतर में वह उठने-बैठने, चलने-फिरने और दौड़ने-भागने की क्रियाएँ करने लगता है।
- श्री अरबिंदो घोष का जन्म 1872 ई. में कलकत्ता में हुआ था। जिस परिवार में श्री अरबिंदो का जन्म हुआ वहां शिक्षा का विशेष महत्त्व था।
- परिवार के अनेक व्यक्ति विद्वता में परिपूर्ण थे तथा शिक्षा की महत्त्व से पूर्ण परिचित थे। यही कारण है कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें पढ़ाई के लिये इंग्लैंड भेज दिया गया था जहाँ उन्होंने 14 वर्ष तक विशुद्ध पाश्चात्य तरीके से पढ़ाई की। वहां की संस्कृति, लेखक एवं रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ने के लिये ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का अध्ययन किया।
- 1890 ई. में श्री घोष भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए परंतु घुड़सवारी परीक्षण में असफल होने के कारण उन्हें अकादमी से निकाल दिया गया था।
- 1893 ई. में वे भारत लौट आए। भारत आने के बाद 13 वर्षों तक बड़ौदा के गायकवाड़ के यहाँ नौकरी की।
- 1905 ई. में बंगाल विभाजन आंदोलन के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए।
- वर्ष 1910 में राजनीति त्यागकर वे आजीवन पुदुच्चेरी में स्थायी रूप से बस गए तथा वहीं पर उन्होंने अरबिंदो आश्रम की स्थापना की जो आज भी विश्वविख्यात है।
- वर्ष 1950 में इस महान दार्शनिक, उच्चकोटि के शिक्षाशास्त्री एवं समाज सुधारक का निधन हो गया।
- शेल गैस प्राकृतिक गैस का एक गैर-परंपरागत रूप है। हालाँकि यह नवीकरणीय नहीं है।
- यह चट्टानी संस्तरों के मध्य फंसी हुई (Trapped) पाई जाती है। इसके निष्कर्षण के लिये चट्टानों में ड्रिलिंग कर तेज़ दबाव से पानी की धार छोड़ी जाती है, जिससे चट्टानों में फंसे हाइड्रेट के अणु मुक्त हो जाते हैं।
- यह एक महंगी एवं उच्च प्रौद्योगिकीय पद्धति है।
- तुलनात्मक रूप से कम पर्यावरणीय नुकसान के चलते इसे पेट्रोलियम व कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत में शेल गैस के मुख्य क्षेत्र कैंबे, गोंडवाना क्रम की शैलें, कृष्णा-गोदावरी बेसिन तथा कावेरी क्षेत्र में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त गंगाघाटी, असम-अराकान, झरिया, बोकारो, उत्तरी करनपुरा, रानीगंज, सोहागपुर आदि क्षेत्रों में भी इसके पाए जाने की संभावना है।
नोट- चीन में इसका सर्वाधिक भंडार है, जबकि अमेरिका इसका तेज़ी से विकास कर रहा है।
श्वसन प्रक्रम में हम सर्वप्रथम साँस लेते हुए पर्यावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं जिसे प्रश्वास या अंतःश्वसन (Inhalation) कहते हैं। फिर हम साँस छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइडन से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं जिसे उच्छ्वसन (Exhalation) कहते हैं। इस प्रकार श्वासोच्छवास (सामान्य शब्दों में साँस लेना) प्राणी के शरीर (फेफड़ों) और उसके बाह्य पर्यावरण के मध्य गैसीय विनिमय या गैसों का परिवहन (Transportation of Gases) है जो सभी जीवों में जीवन पर्यंत चलने वाला अर्थात् सतत प्रक्रम है।
- एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन मिलकर एक श्वास या साँस की रचना करते हैं। कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वास (अंतःश्वसन और उच्छ्वसन) लेता है, उसे उसकी ‘श्वासोच्छवास दर’ (Breathing Rate) कहते हैं। श्वासोच्छ्वास दर को प्रायः श्वसन दर से भी प्रकट किया जाता है।
- एक वयस्क व्यक्ति की विश्रामावस्था में श्वासोच्छ्वास दर प्रति मिनट 15-18 होती है जबकि व्यायाम के दौरान यह दर बढ़कर 25 बार प्रति मिनट तक हो जाती है।
- अधिक श्रम करने के दौरान हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति के लिये हम तेज़ी से श्वास लेते हैं। तेज़ी से श्वास लेने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से भोजन के विखंडन की दर बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यही कारण है कि हमें शारीरिक श्रम करने के बाद भूख लग जाती है।
- सोने के दौरान हमारी श्वासोच्छ्वास दर अपेक्षाकृत कम हो जाती है क्योंकि सोने के क्रम में फेफड़ों को कम ऑक्सीजन मिल पाती है। यही कारण है कि नींद या झपकी आने पर हम जम्हाई लेते हैं जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और हमें जागते रहने में मदद मिलती है।
- ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करने वाले जीवों के लिये ऑक्सीजन विषाक्त होती है। मानव या अन्य जीवों पर लंबे समय तक अशुद्ध ऑक्सीजन का भी दुष्प्रभाव पड़ता है।
पत्थर जैसे कठोर काले रंग के इस पदार्थ का उपयोग खाना पकाने के ईंधन, रेल इंजनों को चलाने के लिये भाप उत्पादन, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन और विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
- बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व वन, मृदा के नीचे दब गए और अधिक मृदा के भार से संपीडित (Compressed) हो गए। पृथ्वी की गहराई में जाकर वन के पेड़-पौधे मृत होकर धीरे-धीरे कोयले में रूपांतरित हो गए। कोयले में मुख्यतः कार्बन के होने तथा मंद प्रक्रम द्वारा मृत वनस्पतियों का कोयले में रूपांतरण कार्बनीकरण (Carbonisation) कहलाया।
- वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है।
- कोयले के औद्योगिक प्रक्रमण (Industrial Processing) द्वारा कोक, कोलतार एवं कोयला गैस जैसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं-
- कोक (Coke) : यह कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण में उपयोगी है।
- कोलतार (Coal Tar) : यह लगभग दो सौ पदार्थों के मिश्रण से बना अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है जिसका संश्लेषित रंग, औषधि, सुगंध, विस्फोटक, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, सड़क एवं छत निर्माण सामग्री इत्यादि में होता है। आज-कल कोलतार की जगह सड़क निर्माण में बिटुमेन जैसे पेट्रोलियम उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं। मॉथ एवं अन्य कीटों को भगाने में प्रयुक्त नैफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं।
- कोयला गैस (Coal Gas) : कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय प्राप्त होने वाली कोयला गैस का उपयोग कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। लंदन में 1810 में एवं न्यूयॉर्क में 1820 के आस-पास इसका उपयोग पहली बार सड़कों को प्रकाशित करने के लिये किया गया था किंतु आज यह ऊष्मा के स्रोत के रूप में ज़्यादा प्रयुक्त है।
सी.टी. स्कैन (Computerized Tomography Scan) का प्रयोग बीमारी के सटीक निदान हेतु किया जाता है। इसके तहत X-किरणों का उपयोग करते हुए शरीर के भीतरी हिस्सों का अलग-अलग स्तर पर अनेक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है तथा उन्हें कंप्यूटर की सहायता से इस प्रकार मिलाया जाता है जिससे शरीर के विशेष अंग की बहुआयामी छवि प्राप्त हो जाती है जिसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इसके प्रयोग से बीमारी की आरंभ अवस्था में पता लगाकर उपचार आरंभ करना संभव है।
उपयोग
- मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का पता लगाने में।
- मस्तिष्क के अंदर खून जमा होने का पता लगाने में।
- दुर्घटना संबंधित सिर पर चोट लगने एवं गंभीर चोटों का पता लगाने में।
- कैंसर की जाँच में।
- फेफड़े, लीवर आदि के कैंसर की जाँच में।
- रीढ़ की हड्डी संबंधित बीमारियों का पता लगाने में।
- हृदय, गुर्दे और रक्त वाहिकाओं की जन्मजात विकृतियों का पता लगाने में।
- मूर्छा या बेहोशी में।
- पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा-सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिये उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौमजल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, तब भौमजल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिये उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है।
- जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत-से नगरों में जल भरने के लिये लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत-से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिये यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ न हो।
वर्षा जल का संग्रहण-
- वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूलमंत्र यह है कि ‘‘जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिये।’’
- वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है अत: इस जल को घरों में वापस लाने के लिये हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
- वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली का यहाँ उल्लेख किया गया है-
- छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण- इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा ज़मीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है जहाँ से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौमजल की पुन: पूर्ति करेगा।
- एक दूसरा विकल्प यह है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुँचने दिया जाए।
जल का भौगोलिक वितरण-
- अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वे जल से समृद्ध हैं। इसके विपरीत रेगिस्तान हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है।
- भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एकसमान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्राय: बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अत: हमारे देश में एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है।
- यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ वर्षा तो पर्याप्त होती है, फिर भी जल की कमी रहती है। यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है।
जल प्रबंधन-
- अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं, तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुँच पाए। आपने संभवत: जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए।
- कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दाँतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोंटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुन: पूर्ति करने के लिये किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षाजल संग्रहण कहते हैं।
- हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुन: पूर्ति करने के लिये बावड़ी बनाने की प्रथाओं (पारंपरिक) का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका है। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे-धीरे गाद जमा होती गई। तथापि, जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुन: विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुन: बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुन: उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भाँति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुँचाती है।
- जल एक सार्वभौमिक विलायक है।
- प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये ही प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं।
- पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिये, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ढाई बाल्टी जल के बराबर है।
- कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिये लंबी कतारें आदि मुद्दे देखने को मिलते हैं।
- निकट भविष्य में विश्व की एक-तिहाई से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा।
- एक शोध के अनुसार वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया गया था जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके।
जल की अवस्थाएँ (States of Water)-
- जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात् ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ़ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर (बर्फ़ छत्रक), बर्फ़ से ढके पर्वतों और हिमनदों (ग्लेशियर) में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों और नदियों के अतिरिक्त भू-तल के नीचे (भौमजल) भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आस-पास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है।
- जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत् चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं।
- अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आस-पास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिये जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं।
- हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिये जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है।
- पत्थर और लकड़ी से बने घर- ये घर पहाड़ी इलाकों में अच्छी मात्रा में वर्षा और बर्फबारी के साथ पाए जाते हैं। ये घर पत्थर और लकड़ी की ईंटों से बने हैं। यहाँ की छतें ढालयुत्त तरीके से दोनों तरफ लकड़ी की बनी हैं। ये घर अधिकांश: मनाली (हिमाचल प्रदेश) और कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों में पाए जाते हैं। श्रीनगर में छत, दरवाज़े और खिड़कियों पर मेहराब के साथ लकड़ी की सुंदर नक्काशी (मेहराब के रूप में जानी जाती है) की जाती है। श्रीनगर के पुराने घरों में डब के नाम से जानी जाने वाली एक विशेष खिड़की पाई जाती है।
- हाउसबोट- एक हाउसबोट पानी में पाई जाती है और इसे लकड़ी से बनाया जा सकता है। हाउसबोट कश्मीर और केरल में पाई जाती हैं। नाव में एक सुंदर लकड़ी की नक्काशी पाई गई जिसे खटामबंद (लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर) के नाम से जाना जाता है। ये घर 80 फीट तक लंबे और 8-9 फीट चौड़े हो सकते हैं।
- ऊँची इमारतें- ये इमारतें मैदानी इलाकों के बड़े या मेट्रो शहरों में पाई जाती हैं। ये ईंट, सीमेंट, लोहा, स्टील आदि से बनी होती हैं।
- डोंगा- डोंगा नाव पर मौजूद घर कश्मीर की डल झील में पाए जाते हैं।
- टेंट हाउस- ये घर प्लास्टिक या कपड़ों से बने होते हैं। आमतौर पर पर्वतारोही इन घरों का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख की चांगपा जनजाति, रेबो नामक शंकु के आकार का तंबू (टेंट) बनाने के लिये याक के बालों की बुनी हुई पट्टी का उपयोग करती है। लेह एवं लद्दाख में टेंट के बने लेखा का उपयोग जानवरों के आश्रय के रूप में किया जाता है।
- इग्लू- ये घर बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बर्फ की चादरों से बने होते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। ये घर बहुत छोटे प्रवेश द्वार के साथ अंडाकार आकृति के होते हैं।
यह एक ऐसा निवास स्थान है जहाँ मनुष्य रहते हैं। मानव आश्रय गृह/मकान कहलाता है। गृह/मकान दो प्रकार के हो सकते हैं-
- कच्चा घर- ये आवास लकड़ी, मिट्टी, पुआल आदि से बने होते हैं, उदाहरण के लिये- झोपड़ी / मिट्टी के घर।
- पक्का घर- ये आवास कंक्रीट, ईंटों, लोहे, लकड़ी आदि से बने होते हैं, उदाहरण के लिये- फ्लैट, बंगला आदि।
विशिष्ट क्षेत्र के लिये विशिष्ट घर-
विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट जलवायु या रहने की स्थिति होती है जो उस क्षेत्र के आधार पर होती है जहाँ मानव अपना घर बनाता है। वे इस प्रकार हैं-
- मिट्टी के बने घर- ये घर मिट्टी, चारे, झाड़ियों, बबूल की लकड़ी, घास आदि के बने होते हैं।
- ये घर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक गर्म जलवायु होती है या गाँवों में।
- ये घर आमतौर पर राजस्थान के गाँवों में पाए जाते हैं ताकि गर्मी में भी तापमान अनुकूल हो सके।
- इन घरों को कीड़ों से बचाने के लिये आमतौर पर गाय के गोबर और मिट्टी से लेपन या रंगा जाता है।
- इनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं।
- लकड़ी और बाँस से बने घर- ये घर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये घर आमतौर पर बाँस और लकड़ी से बने होते हैं। ये घर ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर (3 से 3.5 मी.) हैं ताकि इन्हें बाढ़ से बचाया जा सके। इनकी छते ढालू प्रकार की होती हैं। ये घर असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- पत्थर के घर- लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पत्थर के घर पाए जाते हैं। ये घर दो मंज़िलों वाले पत्थरों से बने हैं। ये घर मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढके हुए हैं। इस प्रकार के घरों में लकड़ी का उपयोग फर्श या छत बनाने में किया जाता है। यहाँ के भूतल में आमतौर पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। यहाँ के लोग पहली मंज़िल पर रहते हैं और कभी-कभी भीषण ठंड के दौरान भूतल पर चले जाते हैं और छत पर सब्ज़ियाँ एवं फल सुखाने के लिये रखे जाते हैं।
जल संसाधन-
जल एक महत्त्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का तीन-चौथाई भाग जल से ढका है इसीलिये इसे ‘जल ग्रह’ कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के दो-तिहाई भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों एवं जंतुओं की सहायता करते हैं।
- पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों, सागरों एवं खाड़ियों के अंतर्गत आता है जिसे समग्र रूप में ‘जलमंडल’ कहा जाता है।
- पृथ्वी पर स्थानिक तौर पर जल का वितरण समान नहीं है। उत्तरी गोलार्द्ध में जहाँ स्थल की तुलनात्मक रूप से अधिकता है, वहीं दक्षिणी गोलार्द्ध में जल की।
- पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97% जल महासागरों में है जो खारा है अथवा पीने योग्य नहीं है।
- शेष लगभग 3% जल, जो ताज़ा एवं पीने योग्य है, हिमानियों (लगभग 2%), भौम जल, झीलों, नदियों आदि के अंतर्गत आता है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में जल की अधिकता है। उत्तरी गोलार्द्ध के कुल क्षेत्रफल के 60.7% भाग और दक्षिणी गोलार्द्ध के 80.9% भाग पर जल है। पृथ्वी के कुल जलीय धरातल का 43% उत्तरी गोलार्द्ध में तथा 57% दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित है।
जलीय चक्र-
- जल का इसके विभिन्न भौतिक रूपों (तरल, गैस एवं ठोस) में स्थलमंडल एवं जलमंडल, महाद्वीपों एवं महासागरों, धरातल एवं भूमिगत, वायुमंडल एवं जैवमंडल आदि के मध्य निरंतर प्रवाह एवं आदान-प्रदान को ‘जलीय चक्र’ कहते हैं।
- जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है अर्थात् प्राकृतिक रूप से इसकी प्रकृति इस तरह की है कि इसे प्रयोग एवं पुन: प्रयोग किया जा सकता है।
- यह पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल के विकास से लेकर कभी न समाप्त होने वाली व्यवस्था है। यह जैवमंडल का महत्त्वपूर्ण घटक है।
- जल चक्र यह उद्घाटित करता है कि जिस मात्रा एवं अनुपात में जल का वाष्पन (Evaporation) एवं वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) होता है, उसी मात्रा एवं अनुपात में ‘वर्षण’ (Precipitation) होता है। अर्थात् पृथ्वी पर नियमित कई भौगोलिक संतुलनकारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जल चक्र एक अतिमहत्त्वपूर्ण संतुलनकारी प्रक्रिया है।
- पृथ्वी पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, उपभोग वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास एवं ताज़े सीमित जलीय संसाधनों की कमी से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिये उपयुक्त है। यह भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है।
- मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन् उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जलस्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन एवं फसलों की बढ़ती मांग, नगरीकरण आदि हैं।
सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनियमन करने वाले संवादात्मक (Interactive) तंत्र होते हैं जो बाह्य उद्दीपनों (Stimuli) के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है-
- कोशिकीय संगठन (Cellular Organisation)- सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका (Cell) है। यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है।
- उपापचय (Metabolism)- जीवन को पूर्ण करने के लिये सजीवों में होने वाली सभी जैव-रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएँ कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं-
- उपचयन (Anabolism)- इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे- वृद्धि (Growth) क्रिया।
- अपचयन (Catabolism)- इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। जैसे- श्वसन (Respiration) क्रिया।
- वृद्धि (Growth)- इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
- प्रजनन (Reproduction)- सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। यह जीवों का मुख्य गुण है।
- चेतना (Consciousness)- यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता (Sensitivity) आती है अर्थात् सभी सजीवों में अनुभूति करने एवं प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व व रासायनिक पदार्थों आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता (उद्दीपन शक्ति) होती है।
उपर्युक्त के अलावा गति (Movement), पोषण (Nutrition) एवं उत्सर्जन (Excretion) भी सजीवों के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। इन लक्षणों से स्पष्ट है कि पौधे तथा जंतु दोनों ही सजीव हैं।
- सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य देश की उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण एवं विकास करना है। इस संगठन को देश की सीमाओं की सुरक्षा की दिशा में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और इसके विभिन्न घटकों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में सड़कों का निर्माण किया है।
- ‘ज़ोजिला-कारगिल’ और ‘मनाली-लेह’ जैसी दुर्गम सड़कों का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा इस संगठन को ‘पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर-उरी राष्ट्रीय राजमार्ग’ के रखरखाव का कार्य भी सौंपा गया है।
- वर्तमान समय में इसके अंतर्गत सड़क निर्माण से संबंधित अनेक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं; जैसे-
- प्रोजेक्ट हीरक (Project Hirak): इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित ज़िलों; जैसे- भंडारा, गढ़चिरौली आदि में सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट बीकन (Project Beacon): इसके तहत सोनमर्ग-कारगिल-लेह मार्ग व लेह-उपसी-सरचू मार्ग का विकास कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट बीकन को ‘जम्मू-कश्मीर की जीवन रेखा’ भी कहते हैं।
- प्रोजेक्ट दंतक (Project Dantak): इसके अंतर्गत भूटान में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।
संविधान सभा (Constituent Assembly) में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं-
- अम्मु स्वामीनाथन
- दक्षयानी वेलायुदन
- बेगम एजाज़ रसूल
- दुर्गाबाई देशमुख
- हंसा मेहता
- कमला चौधरी
- लीला रॉय
- मालती चौधरी
- पूर्णिमा बनर्जी
- राजकुमारी अमृत कौर
- रेणुका रॉय
- सरोजिनी नायडू
- सुचेता कृपलानी
- विजयलक्ष्मी पंडित
- एनी मस्करीनी
औपचारिक और अनौपचारिक आकलन (Formal and Informal Assessment)
- मानकीकृत उपायों का प्रयोग करके परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का समर्थन करने के लिये औपचारिक आकलन के आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। इन आँकड़ों की गणितीय रूप से गणना की जाती है और उन्हें संक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार के आकलन के लिये प्रतिशत, अंक या मानक स्कोर आमतौर पर दिये जाते हैं।
- वहीं दूसरी ओर अनौपचारिक आकलन में आँकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि इसका संबंध सामग्री और प्रदर्शन से है। उदाहरण के लिये एक भाषा का शिक्षक एक विद्यार्थी-विशेष के उच्चारण का आकलन करते समय स्कोर का उपयोग करता है। जैसे कि 15 में से 10 शब्द सही ढंग से उच्चारण किये गए या रुब्रिक स्कोर, जैसे कि ठीक से उच्चारण न कर पाना, कुछ हद तक सही उच्चारण करना, सभी शब्दों का सही उच्चारण करना।
मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन (Quantitative and Qualitative Assessment)
- जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि मात्रात्मक आकलन आँकड़ों को इकट्ठा करने में मदद करता है जिसका विश्लेषण मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके किया जा सकता है। इसकी संख्यात्मक आँकड़ों या रेटिंग पर बहुत अधिक निर्भरता होती है। यह मूल्य आधारित होता है जो मानकीकृत प्रणाली पर आधारित उपकरण का प्रयोग करता है। इसकी प्रमुख सीमा यह है कि इसमें आँकड़ा संभावित प्रतिक्रियाओं के एक चयनित या पूर्व निर्धारित सेट से प्राप्त होता है। मात्रात्मक आकलन संख्याओं के आधार पर काम करता है।
- मात्रात्मक आकलन के विपरीत गुणात्मक आकलन स्कोर या संख्या पर नहीं बल्कि विवरण पर निर्भर करता है। यह स्थितियों या प्रदर्शन के विस्तृत विवरण के साथ मुख्य रूप से संबंधित है इसलिये यह बहुत अधिक व्यक्तिपरक हो सकता है। गुणात्मक आकलन मुख्य रूप से विद्यार्थी के व्यक्तित्व के गैर-शैक्षिक और ज़्यादातर सभी पहलुओं, जैसे- सामाजिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और नैतिक/नीतिपरक सहित का मूल्यांकन करने के बारे में है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आकलन (Direct and Indirect Assessment)
- उपर्युक्त के अलावा आकलन की अन्य विधियाँ भी हैं, जैसे- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आकलन की विधि। आकलन की प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थी को अपने सीखने का प्रदर्शन करने के लिये कहा जाता है। अप्रत्यक्ष विधि को विद्यार्थी को उनके सीखने पर चिंतन-मनन करने के लिये बनाया गया है। टेस्ट, निबंध, प्रस्तुतीकरण आदि आमतौर पर आकलन के प्रत्यक्ष तरीके हैं जबकि अप्रत्यक्ष विधि में सर्वेक्षण और साक्षात्कार शामिल किया जाता है।
आकलन के प्रकार को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है-
- रचनात्मक और संकलनात्मक आकलन
- औपचारिक और अनौपचारिक आकलन
- गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आकलन
रचनात्मक आकलन (Formative Assessment)
- ‘‘जब खाना पकाने वाला सूप का स्वाद लेता है तो यह रचनात्मक आकलन है, जब मेहमान सूप का स्वाद लेता है तो यह संकलनात्मक आकलन है।’’ रॉबर्ट स्टेक का यह लोकप्रिय उद्धरण आकलन के दो प्रकारों के बीच प्रमुख अंतर को दर्शाता है- रचनात्मक बनाम संकलनात्मक।
- रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों के सक्रिय विकास के साथ अनुदेशात्मक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षक के आकलन के अलावा स्वयं और हमउम्र आकलन के लिये गुंजाइश प्रदान करता है।
- सक्रिय भागीदारी से विद्यार्थियों की अधिगम की प्रेरणा बढ़ती है। आकलन की अनौपचारिक परिस्थिति और बेरोक तकनीक अधिगम को एक सुखद अनुभव बनाती है। इस प्रकार के आकलन पाठ्यक्रम के निर्देशन के दौरान किये जाते हैं और ये सत्र या पाठ्यक्रम के अंत तक सीमित नहीं होते हैं।
- इसके द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यह संव्यवहार प्रक्रियाओं और अधिगम की गतिविधियों में संशोधन या समायोजन की सुविधा प्रदान करता है।
संकलनात्मक आकलन (Summative Assessment)
- संकलनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित किया जाता है। यह विद्यार्थी के कार्यों के मूल्यांकन का सबसे पारंपरिक तरीका है। जैसा कि शब्द से पता चलता है, यह विद्यार्थी के अधिगम को मापता है कि उसने कितना पाठ्यक्रम/सेमेस्टर/यूनिट से सीखा है।
- यह निश्चित अंतराल पर किया जाता है अथवा अनुदेशन के बाद प्रत्येक सप्ताहों, महीनों, सेमेस्टर अथवा वर्ष में एक बार बोला या लिखा जाता है। यह तब घटित होता है जब उपलब्धि को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना होता है।
- इसे आमतौर पर ग्रेडेड टेस्ट के रूप में प्रतिवेदित किया जाता है और इसे ग्रेड के पैमाने या सेट के अनुसार चिह्नित किया जाता है। यह एक विशेष बिंदु पर समय के अंतर्गत कुछ मानकों के सापेक्ष सीखने वाले विद्यार्थी को मापने का एक साधन है।
- यह केवल एक निश्चित समय पर उपलब्धि के स्तर को बेहतर रूप से प्रमाणित करता है। इसलिये केवल संकलनात्मक मूल्यांकन पर निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि रचनात्मक आकलन सीखने में सुधार पर केंद्रित है जबकि संकलनात्मक आकलन सीखने का सारांश प्रस्तुत करता है। आदर्श तरीका यह है कि रचनात्मक और संकलनात्मक आकलन को संतुलित किया जाए ताकि एक विद्यार्थी के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर सामने आए।
- समाज में व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखने के लिये कुछ व्यवहारों को आवश्यक व्यवहार के रूप में सामाजिक मान्यता एवं स्वीकृति प्राप्त होती है, हँसी-मज़ाक का संबंध भी इसी प्रकार का एक मान्यता प्राप्त व्यवहार है। हँसी-मज़ाक के संबंध में दो संबंधियों के बीच एक प्रकार की समानता एवं पारस्परिकता का संबंध होता है। उदाहरण के लिये, एक पुरुष का अपनी पत्नी की छोटी बहन (जीजा-साली) एवं एक स्त्री का अपने पति के छोटे भाई के साथ के संबंध (भाभी-देवर) को हँसी-मज़ाक का संबंध कहा जाता है। कुछ कृषक जातियों में पति की असामयिक मृत्यु के बाद भाभी का देवर से विवाह उत्तर भारत में देखा गया है। पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद जीजा-साली का विवाह तो उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय प्रथा है।
- अन्य प्रकार के हँसी-मज़ाक के संबंध भी महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये, कुछ समुदायों में दादा-दादी के साथ और नाना-नानी के साथ भी बच्चों का हँसी-मज़ाक का संबंध होता है। यहाँ हँसी-मज़ाक के संबंध अनौपचारिकता, आत्मीयता एवं असीमित स्वतंत्रता के माहौल में बच्चों के विकास में मदद करते हैं।
- हँसी-मज़ाक के संबंध में एक प्रकार के निषेध का संबंध भी नातेदारी के बीच पाया जाता है। उदाहरण के लिये, एक स्त्री का अपने पति के बड़े भाई या पिता से निषेध का संबंध होता है। पति के पिता को श्वसुर (ससुर) एवं पति के बड़े भाई को जेठ या भसुर कहा जाता है।
- भारत के कई ग्रामीण समुदायों में टेकनोनामी (Teknonymy) की प्रथा काफी लोकप्रिय है। यह बच्चों के नाम के आधार पर माता-पिता के नामकरण की प्रथा है, जैसे- श्याम की माँ (या राधा के पिताजी) इस प्रथा का एक निहितार्थ यह है कि कई समुदायों में एक स्त्री अपने ससुराल में अपनी पहली संतान के बाद ही पूर्ण सदस्य बन पाती है। फलस्वरूप उसकी पहचान में (प्रथम) संतान का नाम जुड़ना स्वाभाविक बन जाता है।
- प्रसिद्ध मानवशास्त्री ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि नातेदारी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त एक निश्चित नातेदारी के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के वर्गीकरण की ओर संकेत करती है। उनके पहले एल.एच. मॉर्गन ने कहा था कि नातेदारी शब्दावली हमारे सामाजिक संबंधों के संदर्भ तथा मुहावरे प्रदान करती है। मॉर्गन ने नातेदारी में प्रयुक्त परिभाषित शब्दावलियों की दो व्यवस्थाओं की चर्चा की है- वर्गात्मक, वर्णनात्मक।
- वर्गात्मक व्यवस्था में नातेदारी में प्रयुक्त शब्दावली के अंतर्गत एक ही शब्द के द्वारा भिन्न प्रकार की नातेदारी को वर्गीकृत या संबोधित किया जाता है।
- वर्णनात्मक व्यवस्था में हर नातेदारी शब्द केवल एक खास नातेदार एवं एक खास संबंधी के लिये इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिये, माँ के भाई को मामा, पिता के भाई को चाचा तथा पिता की बहन के पति को फूफा कहा जाता है।
- ज़्यादातर समकालीन समाजों में दोनों प्रकार के (वर्गात्मक एवं वर्णनात्मक) शब्दों का उपयोग किया जाता है।
- नाभिकीय परिवार के अंदर माँ, पिताजी जैसे वर्णनात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है।
- उत्तर भारतीय नातेदारी शब्दावली तुलनात्मक रूप से वर्णनात्मक है और यह व्यक्ति के प्राथमिक संबंधों का वर्णन करती है।
- पितृपक्षीय वंशावली को परिभाषित करने के लिये ममेरे एवं मौसेरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे- भाई के पुत्र को भतीजा एवं बहन के पुत्र को भाँजा कहा जाता है।
- इसके विपरीत, दक्षिण भारतीय नातेदारी शब्दावली में तुलनात्मक रूप से वर्गात्मक शब्दावली पर ज़ोर दिया जाता है। यहाँ एक ही शब्द मामा के द्वारा माता का भाई, पत्नी के पिता एवं पिता की बहन का पति तीनों का बोध होता है।
बच्चे के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बच्चा उसका मित्र कहलाता है। यह आवश्यक नहीं कि समुदाय के सभी बच्चों के साथ उसके संबंध अच्छे हों। जिन बच्चों के साथ उसका संबंध अच्छा होता है एवं जिनके साथ वह रहना, कार्य करना एवं खेलना पसंद करता है उन्हें हम उसका मित्र (Friend) कहते हैं।
मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भाँति थोपा नहीं जा सकता। अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख-परखकर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक-दूसरे के लिये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मित्रों के बीच के आपसी संबंधों को मित्रता कहते हैं।
मित्रता का वर्गीकरण (Classification of Friendship)
अरस्तू ने मित्रता का वर्गीकरण तीन भागों में निम्नलिखित प्रकार से किया है-
- उपयोगिता की मित्रता- इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है।
- आनंद की मित्रता- इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बाँटते हैं।
- अच्छी मित्रता- इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक-दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिये नहीं होती है।
मित्रता का महत्त्व
मित्र व मित्रता का महत्त्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से मित्रता के कुछ महत्त्व निम्नलिखित हैं-
- एक मित्र बालक के खेल-कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है।
- एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। एक अच्छा मित्र ही सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र बच्चों को पाश्विक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है।
- बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।
परिवार के कार्यों की विवेचना निम्नलिखित दो श्रेणियों में की जा सकती है- मौलिक एवं परंपरागत कार्य
मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य (Basic and Universal Functions)- मौलिक कार्य विश्व के सभी देशों के परिवारों में पाए जाते हैं। इन्हें प्रत्येक परिवार के प्राणिशास्त्रीय कार्य (Biological Function) भी कह सकते हैं। ये कार्य निम्नांकित हैं-
- यौन इच्छाओं की पूर्ति का कार्य (Function of Satisfying Sexual Needs)- परिवार विवाह प्रथा के माध्यम से स्त्री व पुरुष को पत्नी व पति के रूप में यौन संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार यह उनकी प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता (यौन संतुष्टि) की पूर्ति करने में सहायता देता है। यदि कोई व्यक्ति विवाह न कर ऐसे संबंध स्थापित करता है तो ऐसा करना उचित नहीं समझा जाता है। विवाह के द्वारा ही समाज स्त्री-पुरुष के यौन-संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है।
- संतानोत्पत्ति (Reproduction)- समाज की निरंतरता के लिये यह आवश्यक है कि समाज में नए सदस्यों का जन्म हो। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को परिवार संतानोत्पत्ति द्वारा करता है।
- सुरक्षा (Safety)- मनुष्य समस्त जीवधारियों में एक ऐसा प्राणी है जिसे जन्म से लेकर काफी वर्षों तक दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। यदि उसे यह सहायता न मिले तो वह समाप्त हो जाएगा। यह सहायता परिवार अपने सदस्यों को सुरक्षा के रूप में देता है। परिवार निश्चित आयु तक उनका भरण-पोषण करके उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे भौगोलिक तथा सामाजिक पर्यावरण में रह सकें। सुरक्षा की प्रकृति मात्र प्राणिशास्त्रीय ही नहीं अपितु मानसिक भी होती है।
परिवार की कुछ कतिपय विशिष्ट विशेषताएँ निम्नांकित हैं-
- भावात्मक आधार (Formative Basis)- परिवार के सभी सदस्य भावनाओं में बंधे हुए हैं। ये संबंध भाई-बहन, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माँ-पुत्री या किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इस कारण व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रश्रय नहीं मिलता है। सभी सदस्यों के सामने पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा शक्ति का लक्ष्य रहता है। नि:स्वार्थ स्नेह, प्रेम एवं वात्सल्य केवल परिवार में ही पाया जाता है।
- रचनात्मक प्रभाव (Constructive Influence)- कूले (Cooley) ने परिवार को प्राथमिक समूह कहा है क्योंकि मानव का जन्म तथा विकास परिवार में ही होता है। परिवार द्वारा ही मानव के चरित्र, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार के ढंग आदि का निर्माण होता है। परिवार का लक्ष्य सभी सदस्यों को समान लाभ पहुँचाना है। यह व्यक्तित्व के विकास में अपना निर्माणात्मक प्रभाव डालता है तथा समाज के विचारों, विश्वासों एवं मूल्यों का विकास बच्चों में करता है।
- सदस्यों का उत्तरदायित्व (Responsibility of Members)- परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्थिति तथा भूमिका निश्चित होती है। परिवार के सभी सदस्य अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़े-से-बड़ा त्याग करने से नहीं हिचकते हैं। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति निजी स्वार्थ को कोई महत्त्व नहीं देता।
- सीमित आकार (Limited Size)- परिवार छोटा हो या बड़ा इसका आकार सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है। बर्गेस एवं लॉक (Burgess and Locke) के अनुसार परिवार की सदस्यता जन्म, विवाह तथा गोद लेने से ही मिलती है। इसी कारण परिवार का आकार छोटा होता है।
- सामाजिक नियमन (Social Regulation)- व्यक्ति साधारणत: परिवार की प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, संस्कारों आदि का उल्लंघन नहीं करता। परिवार अपने सदस्यों को समाज के अनुरूप बनाता है। वह उन्हें इस बात के लिये बाध्य करता है कि वे समाज के नियमों को मानें। मनुष्य को व्यवहार, शिक्षा, धर्म, कर्त्तव्य-बोध आदि अनेक सामाजिक तथ्यों का ज्ञान परिवार से ही होता है।
- स्थायी व अस्थायी प्रकृति (Permanent and Texporary Nature)- परिवार समिति भी है और संस्था भी। सदस्यों के आधार पर परिवार एक समिति है व अस्थायी है। नियमों तथा कार्यप्रणालियों के रूप में परिवार एक स्थायी संस्था है।
यद्यपि विभिन्न समाजों में परिवार की प्रकृति एवं स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है, परंतु निम्नलिखित कतिपय प्रमुख विशेषताएँ प्रत्येक प्रकार के परिवार में पाई जाती हैं-
परिवार की सामान्य विशेषताएँ अग्रांकित हैं-
- सार्वभौमिकता (Universality)- परिवार एक ऐसा समूह है जो सभी समाजों एवं सभी युगों में पाया जाता है। आज भी समाज चाहे सभ्य हो, चाहे आदिम, परिवार किसी-न-किसी रूप में अवश्य ही पाया जाता है। मरडॉक (Murdock) ने पूरे विश्व में 250 जनजातीय समाजों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया है कि परिवार विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है।
- वैवाहिक संबंध (Marital Relationships)- परिवार का उद्भव स्त्री-पुरुष के वैवाहिक संबंधों से होता है। अत: विवाह परिवार के निर्माण का प्रथम आधार है। मरडॉक ने विवाह द्वारा यौन व्यवहार पर नियंत्रण एवं प्रजनन को परिवार का मौलिक कार्य माना है।
- विभिन्न स्वरूप (Different Forms)- परिवार का स्वरूप एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह के रूप में संभव है। यह भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न होता है।
- वंश नाम या नामावली की व्यवस्था (System of Nomenclature)- प्रत्येक परिवार में वंश नाम की एक व्यवस्था पाई जाती है। वंश नाम मातृवंशीय अथवा पितृवंशीय हो सकता है।
- सामान्य निवास (Common Residence)- सामान्यत: परिवार का एक निश्चित निवास अथवा घर होता है अर्थात् परिवार के सदस्य एक साथ निवास करते हैं।
- सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति (Social Regulation)- समाज की संरचना परिवार पर ही निर्भर है। इसका कारण यह है कि परिवार ही नए सदस्यों के जन्म तथा उन्हें समाज के अनुसार सामाजिक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव किस सीमा तक समाज के ढंग, मान्यताओं या कार्यप्रणाली को अपनाएगा यह सभी परिवार पर ही निर्भर करता है।
परिवार की एक संक्षिप्त, स्पष्ट व समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। कुछ विद्वानों ने परिवार को एक समूह के रूप में, कुछ ने एक समिति के रूप में, कुछ ने एक संस्था के रूप में तथा कुछ अन्य विचारकों ने इसे सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वानों ने परिवार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है-
- बर्गेस एवं लॉक (Burgess and Locke) के अनुसार, ‘‘परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह, रक्त एवं गोद लेने वाले संबंधों से जुड़े होते हैं, जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जो पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री तथा भाई-बहन के रूप में अपनी-अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाते हुए एक-दूसरे से अंत:संचार तथा अंतर्क्रिया करते रहते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं।’’
- ऑगबर्न एवं निमकॉफ (Ogburn and Nimkoff) के अनुसार, ‘‘परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित, कम या अधिक स्थायी समिति है।’’
- मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार, ‘‘परिवार पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है, जो प्रजनन (बच्चों के जन्म) तथा बच्चों के पालन-पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है।’’
- इलियट एवं मैरिल (Elliott and Merrill) के अनुसार, ‘‘परिवार को पति-पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिवार एक सामाजिक संस्था भी है और समाज द्वारा मान्य एक ऐसा संगठन भी है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।’’
परिवार की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सदस्य विवाह, रक्त या विधिवत गोद लिये जाने के द्वारा मान्य संबंधों के परिणामस्वरूप परस्पर जुड़े होते हैं। उनमें परस्पर स्नेह, सहानुभूति, सेवा और त्याग की भावना पाई जाती है। वस्तुत: परिवार को तीन परिप्रेक्ष्यों द्वारा देखा गया है-
- संरचनावादी (Structuralist) विद्वान परिवार को ऐसे संबंधों की संरचना के रूप में देखते हैं जिसमें अंतर्संबंधित प्रस्थितियों व भूमिकाओं तथा सदस्यों के बीच सुव्यवस्थित अधिकारों व उत्तरदायित्वों की व्यवस्था पाई जाती है।
- प्रकार्यवादी (Functionalist) परिवार को एक ऐसी इकाई मानते हैं जिसके सदस्यों में प्रकार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं तथा यह देखने का प्रयास करते हैं कि परिवार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या योगदान देता है।
- अंतर्क्रियावादी (Interactionist) परिवार को सदस्यों के बीच पाई जाने वाली परस्पर अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया की व्यवस्था के रूप में देखते हैं तथा परिवार की संरचना एवं भूमिकाओं की विविधताओं को समझने का प्रयास करते हैं।
|
भारतीय राज्य |
संलग्न देशों की संख्या |
संलग्न देशों के नाम |
|
सिक्किम |
3 |
नेपाल, भूटान, चीन |
|
अरुणाचल प्रदेश |
3 |
चीन, भूटान, म्यांमार |
|
नागालैंड |
1 |
म्यांमार |
|
मणिपुर |
1 |
म्यांमार |
|
मिज़ोरम |
2 |
बांग्लादेश, म्यांमार |
|
त्रिपुरा |
1 |
बांग्लादेश |
|
मेघालय |
1 |
बांग्लादेश |
|
असम |
2 |
भूटान, बांग्लादेश |
|
पश्चिम बंगाल |
3 |
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान |
|
बिहार |
1 |
नेपाल |
|
उत्तर प्रदेश |
1 |
नेपाल |
|
उत्तराखंड |
2 |
नेपाल, चीन |
|
हिमाचल प्रदेश |
1 |
चीन |
|
पंजाब |
1 |
पाकिस्तान |
|
राजस्थान |
1 |
पाकिस्तान |
|
गुजरात |
1 |
पाकिस्तान |
|
जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य-क्षेत्र) |
1 |
पाकिस्तान |
|
लद्दाख (संघ राज्य-क्षेत्र) |
3 |
चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान |
|
दर्रा |
अवस्थिति |
|
वाखजीर दर्रा |
अफगानिस्तान-चीन |
|
सलांग दर्रा |
अफगानिस्तान |
|
बुच्नान दर्रा |
यू.एस.ए. |
|
ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा |
स्विट्ज़रलैंड |
|
थर्मोपली दर्रा |
यूनान |
|
स्नेक दर्रा |
इंग्लैंड |
|
हल्फाया दर्रा |
मिस्र |
|
बोलन दर्रा |
पाकिस्तान |
|
अर्लबर्ग दर्रा |
ऑस्ट्रिया |
- परिवार एक प्राथमिक समूह है जो मानव समाज की पूर्णत: मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। रॉल्फ लिंटन (Ralph Linton) के अनुसार माता-पिता और बच्चे का प्राचीन त्रित्व (Trinity) किसी अन्य मानव संबंध की अपेक्षा अधिकाधिक उतार-चढ़ावों के बावजूद विद्यमान रहा है। यह समस्त अन्य संरचनाओं का आधार स्तंभ है। मनुष्य की आवश्यकताओं को दो प्रमुख वर्गों में बाँटा जा सकता है- प्रथम, प्राथमिक आवश्यकताएँ अर्थात् ऐसी आवश्यकताएँ जो उसके जीवनयापन के लिये प्रमुख हैं तथा द्वितीय, द्वितीयक आवश्यकताएँ अर्थात् वे आवश्यकताएँ जो उसके जीवन के लिये प्रमुख तो नहीं परंतु वे भी अपना महत्त्व रखती हैं। परिवार इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसीलिये मानव समाज में परिवार की स्थिति केंद्रीय होती है। सभी समाजों में परिवार की भाँति नातेदारी एवं विवाह सामाजिक जीवन के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं।
- समूहों या सदस्यों के संबंध में परिवार एक समिति है। परिवार को जब नियमों या कार्यपद्धतियों के संबंध में देखा जाता है तो यह एक संस्था है। परिवार को समिति के दृष्टिकोण से देखें या संस्था के, पर इस तथ्य पर दो मत नहीं हो सकते हैं कि परिवार समाज की महत्त्वपूर्ण मौलिक एवं सार्वभौम इकाई है। परंतु सभी समाजों में परिवार का एक ही रूप प्रचलित नहीं है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी समाजों में एकाकी परिवार या दाम्पत्य परिवार (Conjugal Family) की प्रधानता है, जबकि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार की। सामाजिक जीवन को बनाने एवं समाजीकरण में परिवार की विशेष भूमिका है। इसी कारण चार्ल्स कूले ने परिवार को एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिक समूह माना है।
परिवार का अर्थ
- व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द ‘परिवार’, आंग्ल भाषा के ‘फैमिली’ (Family) शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह लैटिन भाषा के ‘फैमुलस’ (Famulus) शब्द से बना है। ‘फैमुलस’ का लैटिन भाषा में अर्थ है- एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य (अर्थात् माता-पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर तथा गुलाम इत्यादि) आ जाते हैं। जैविक दृष्टि से परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री एवं पुरुष को पति एवं पत्नी के रूप में यौन संबंध की स्थापना एवं प्रजनन (संतान उत्पत्ति) हेतु समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार को स्त्री एवं पुरुष का एक ऐसा समूह कहा जा सकता है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तथा एक ‘घर’ के रूप में पहचाने जाते हैं।
- जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग-अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों यह एटलस से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-
- भौतिक मानचित्र- पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे- पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है।
- राजनीतिक मानचित्र- राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों एवं विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है।
- थीमैटिक मानचित्र- कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे- सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है।
समुद्र (Oceans)-
- मछलियों की आकृति में कुछ समानताएँ दिखाई देती हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं।
- मछली के पंख एवं पूँछ चपटे होते हैं जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली में श्वसन के लिये गिल (क्लोम) होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएँ उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचनाएँ उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं।
- दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा-रेखीय होता है जिससे वे जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा-रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में, तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा-रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिये इनमें गिल (क्लोम) होते हैं।
- डॉलफिन एवं ह्वेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात-छिद्रों (Blowholes) द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिये रह सकते हैं। ये समय-समय पर समुद्री सतह (जल से बाहर) पर आकर श्वसन-छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं।
तालाब एवं झील (Ponds and Lakes)-
- कुछ जलीय पौधे जल की सतह पर प्लवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों का उगना सामान्य घटना है। इन पौधों की पत्तियाँ, तने और जड़ें काफी व्यवस्थित होती हैं।
- इनमें से कुछ पौधों की जडे़ं जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्त्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है।
- इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियाँ एवं फूल जल की सतह पर प्लवन (तैरते) करते रहते हैं।
- कुछ जलीय पौधे जल में पूर्णरूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियाँ संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियाँ बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती।
- मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मज़बूत होते हैं जो इसकी छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसे पश्चपाद में जालयुक्त पादांगुलियाँ होती हैं जो इसे तैरने में सहायता करती हैं।
पर्वतीय क्षेत्र (Mountain Regions)-
- ये आवास क्षेत्र सामान्यत: बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- वृक्ष सामान्यत: शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएँ तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिये इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है।
- पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं । उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणत: शरीर को गरम रखने के लिये याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होती है। पहाड़ी बकरी के मज़बूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिये अनुकूलित बनाते हैं। जैसे-जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊँचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है।
घासस्थल (Grasslands)-
- शेर वन में अथवा घासस्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें खा जाता है। यह मटमैले (हल्के भूरे) रंग का होता है। शेर के अगले पैर के नख (नाख़ून) लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। उसका मटमैला (हल्का भूरा) रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं।
- एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घासस्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिये इसके मज़बूत दाँत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी (शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं) की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आँखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज़ गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती हैं।
- शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत-सी विशिष्ट संरचनाएँ होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं।
कुछ स्थलीय आवासों का विवरण निम्नलिखित है-
मरुस्थल (Deserts)-
- मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गरम एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिये आस-पास की वायु का उपयोग करते हैं।
- समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय पारितंत्र में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गरमी से दूर रहता है। ऊँट में मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ऊँटों को पसीना (स्वेद) भी नहीं आता इसलिये शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है और वे जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं।
- मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं साँप के ऊँट की भाँति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज़ गरमी से बचने के लिये वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं।
- मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियाँ काँटों (शूल) का रूप ले लेती हैं जिससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश-संश्लेषण सामान्यत: तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल-संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिये मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं।
किसी जीव-जंतु का वह परिवेश जिसमें वह निवास करता है आश्रय या आवास कहलाता है। दूसरे शब्दों में, आश्रय से तात्पर्य उस स्थान-विशेष से है जो प्राणीमात्र को प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का शाब्दिक अर्थ ‘वास का स्थान’ होता है। जानवरों का आश्रय ज़्यादातर अस्थायी रूप से हो सकता है, लेकिन मनुष्यों के लिये यह आमतौर पर स्थायी रूप से होता है। कुछ मानव अपने व्यवसाय, अध्ययन आदि के आधार पर आश्रय बदलते हैं। आश्रय न केवल गोपनीयता प्रदान करता है बल्कि हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भंडारण भी करता है।
आश्रयों के प्रकार (Types of Shelters)
ध्यातव्य है कि आश्रय भोजन, पानी और संगति की भावना के साथ-साथ बुनियादी मानवीय ज़रूरतों में से एक है। यह एक ऐसी संरचना है जो हमें बारिश, खराब मौसम, अधिक गर्मी, ठंड, बर्फीली हवाओं आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एक आश्रय को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है- स्थायी तथा अस्थायी आश्रय
स्थायी आश्रय- यह मनुष्यों और जीव-जंतुओं का निवास स्थान है, जहाँ वे बहुत लंबे समय तक निवास करते हैं, जैसे- घर, घोंसले, गुफाएँ आदि। इन आश्रयों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है।
अस्थायी आश्रय- ये ऐसे आवास हैं जहाँ मनुष्य और जीव-जंतु बहुत कम अवधि या किसी विशिष्ट कारण या उद्देश्य के लिये निवास करते हैं। उदाहरण - छात्रावास, आश्रयगृह, प्रवासी पक्षियों के घोंसले, हाउसबोट आदि। इन आश्रय स्थलों को समय-समय पर एक-स्थान से दूसरे-स्थान पर ले जाया या स्थानांतरित किया जा सकता है।
- विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं।
- स्थल (ज़मीन) पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं।
- जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएँ हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिये भी सत्य है।
- किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएँ आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं।
- FICCI भारत में सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक पुराना शीर्षस्थ संगठन है जो देश की आर्थिक नीतियों व उद्योगपतियों के हितों के संरक्षण हेतु कानून बनाने व उन्हें लागू करने हेतु सरकार पर दबाव डालता है।
- इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। यह देश में उद्योग और वाणिज्य के विकास में उपयोगी आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देता है।
- यह व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन करता है, निवेश व व्यापार समझौतों के प्रभावों पर अपनी राय व्यक्त करता है।
- इसके महत्त्व का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके वार्षिक अधिवेशनों में भारतीय प्रधानमंत्री व विविध अवसरों पर वित्तमंत्री उपस्थित रहते हैं।
- अगस्त 2014 में FICCI द्वारा आयोजित कराए गए वार्षिक एग्रोकेम सम्मेलन में भारत के कृषि मंत्री ने प्रकृति व जैव-विविधता के लिये खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की।
- उमंग ऐप अर्थात् यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया।
- इस ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने तैयार किया है तथा इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- डिजिटल इंडिया पहल की दिशा में और सरकार की सारी सुविधाओं को एक जगह लाने हेतु यह एक बड़ी शुरुआत है क्योंकि इस ऐप पर केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सेवाएँ मिलेंगी।
- वर्तमान में इस ऐप पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की 163 सेवाएँ उपलब्ध हैं लेकिन और भी सुविधाओं को लगातार इस ऐप से जोड़ा जा रहा है।
- अभी उपलब्ध प्रमुख सेवाओं में पैन कार्ड निर्माण, गैस बुकिंग, आधार कार्ड डाउनलोडिंग, बिल पेमेंट तथा टैक्स पे करना आदि शामिल हैं।
- यह ऐप अंग्रेज़ी सहित 12 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा।
- जी. जैकब के अनुसार, ‘‘ सहयोगी अधिगम समूह में काम करने के मूल्य को बढ़ावा देने वाली अवधारणा एवं तकनीक है।’’
- सहयोगी अधिगम शिक्षकों को निम्नलिखित के लिये प्रोत्साहित करते हैं-
- ‘मूल्य’ सीखने-सिखाने की पारंपरिक आदर्श सोच से निकलने के लिये।
- बच्चों को सहयोग की भावना समझाने में सहायता करने के लिये।
- यह समझने के लिये कि व्यक्तियों में अंतर होते हैं तथा भिन्नताएँ लोकतंत्र हेतु आवश्यक हैं।
- बच्चों के सामाजिक संदर्भ का महत्त्व समझने के लिये।
सहयोगी अधिगम के नियम-
सहयोगी अधिगम के तीन अति महत्त्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं-
- सकारात्मक रूप से एक-दूसरे पर निर्भरता : इसमें शामिल हैं- समूह का एक साझा उद्देश्य हो, सभी के संसाधन साझा हों, एक समूह की एक पहचान बनाई जाए। इसके द्वारा सकारात्मक भावनाओं एवं मनोवृत्तियों पर ज़ोर दिया जाता है।
- व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी : यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे को कुछ-न-कुछ काम दिया जाए तथा कुछ कार्य समूह के सभी सदस्य इकट्ठा होकर करें।
- समान स्तर पर सहक्रियाएँ : समूह के सदस्यों के बीच समान स्तर पर सहक्रियाएँ समूह के सहज कार्य हेतु आवश्यक होती हैं। शिक्षक का कार्य होगा कि शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कुछ सहक्रियाओं के लिये आवश्यक है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को जानता हो।
सहयोगी अधिगम के उपयोग-
- सहयोगी अधिगम बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण एवं विचारों को समझने की योग्यता को बढ़ाता है।
- बच्चों में एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने के कौशल को विकसित करने में सहायता करता है।
- समस्याओं को सुलझाने के लिये फैसले लेने के कौशल का विकास करता है।
- सहयोगी अधिगम बच्चों को अलग प्रकार से लेकिन परिस्थिति के अनुसार उचित प्रक्रिया करने में योग्य बनाता है।
- सहयोगी अधिगम बच्चों को इस प्रकार के अवसर देता है कि वे बहुआयामी विचारों की छानबीन कर सकें तथा परिणामों का अंदाज़ा लगा सकें और साथ ही उन पर तर्क-वितर्क कर सकें।
- पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम विश्लेषणात्मक सोच तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। सहयोगी अधिगम काफी हद तक शिक्षार्थियों में इन कौशलों का विकास करने में सहायता कर सकता है।
3. कार्य का मूल्यांकन (Evaluation)- एक अध्यापक को कार्य का मूल्यांकन भी करना होता है ताकि यह पता चल सके कि जिन शैक्षिक उद्देश्यों को क्रिया के द्वारा प्राप्त कराने का प्रयास किया गया उनकी प्राप्ति हो पाई या नहीं। जब विद्यार्थी क्रिया कर रहे होते हैं, उस दौरान उनका ध्यान से अवलोकन किया जाना चाहिये। प्रगति की जाँच निर्माणात्मक मूल्यांकन द्वारा की जानी चाहिये। अंत में क्रिया संकलित मूल्यांकन करना चाहिये ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की क्रिया में भागीदारी का मूल्यांकन हो सके।
4. प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना (Reconsider the Activity)- इस बात पर भी विचार करना ज़रूरी है कि क्या अच्छा रहा और क्या नहीं तथा क्यों? पुन: विचार भविष्य में किसी भी क्रिया को बेहतर रूपरेखा देने, योजना बनाने एवं क्रिया में आवश्यक सुधार करने में सहायता करेंगे।
क्रिया आधारित अधिगम उपागम के उपयोग-
- अमूर्त अवधारणाओं को प्रयोगात्मक अनुभव या निदर्शन द्वारा स्पष्ट करने में सहायता करते हैं।
- बहु ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे कि देखना, सुनना, छूना, सूंघना एवं स्वाद इत्यादि। इस प्रकार जो सीखा जाता है, अधिक समय तक बना रहता है।
- विषयवस्तु सिखाने के अलावा कई जीवन कौशल सिखाए जाते हैं।
- बच्चों के दृष्टिकोण से सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है न कि बड़ों के दृष्टिकोण से।
- समस्याएँ एवं समाधानों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है जिससे आत्मसम्मान का विकास होता है।
- विज्ञान, गणित इत्यादि के नियमों को बच्चों की परीक्षित परिस्थितियों से जोड़कर अच्छी समझ विकसित करने में सहायता करते हैं।
- इसमें सृजनात्मकता तथा लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है।
- बच्चे को शारीरिक एवं मानसिक दोनों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है।
- पर्यावरण अध्ययन को विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर इसलिये रखा गया है ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरण की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु सुग्राही एवं संवेदनशील लगाव को विकसित किया जा सके। इसीलिये अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को उनके आसपास के परिवेश से घुलने-मिलने के अवसर प्रदान करें। क्रिया आधारित उपागम विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान के निर्माण तथा पुन: निर्माण में व्यस्त करता है।
- इस उपागम के अनुसार एक शैक्षिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिये-
- पर्यावरण अध्ययन के अधिगम उद्देश्य को स्पष्टता से विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिये।
- वास्तविक जीवन पर आधारित अवधारणा को विद्यार्थियों के समक्ष रखना चाहिये जो बच्चों के लिये सुखद या आनंददायक हो।
- किसी भी अवधारणा को पूरा करने में अधिक समय न लगे। लंबी क्रिया को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जा सके।
- अवधारणा की प्रकृति विद्यार्थियों की आयु के अनुसार होनी चाहिये।
- अवधारणा ऐसी हो जो विद्यार्थियों में रुचि एवं जिज्ञासा जगाए तथा सार्थक सूचना प्रदान करे।
क्रिया आधारित शिक्षण-अधिगम का आयोजन
क्रिया आधारित अधिगम हेतु चार चरण होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है-
-
- नियोजन (Planning)- अधिगम के उन उद्देश्यों की पहचान कर ली जाए जिन्हें नियोजित क्रिया रा प्राप्त किया जाना है। क्रिया के पश्चात संक्षिप्त चर्चा की योजना भी बनाई जानी चाहिये। इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिये कि विद्यार्थियों का किस प्रकार मूल्यांकन किया जाना है।
- क्रिया को संचालित करना (Operate the Activity)- विद्यार्थियों को क्रिया से अवगत कराया जाना चाहिये तथा उसके अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में बताना चाहिये। उनकी भूमिका के बारे में, कितना समय लगेगा, मूल्यांकन कैसे होगा यह भी बताना चाहिये। क्रिया शुरू होने के बाद देखें कि विद्यार्थी क्रिया करने में सार्थक रूप से योग्य है या नहीं। इस प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
अवधारणा की विशेषताएँ (Features of Concept)-
- पूर्वोल्लिखित परिभाषाओं के आधार पर अवधारणा की निम्नलिखित विशेषताओं का निर्धारण किया जा सकता है-
- अवधारणा के एक वर्ग या समूह की एक ऐसी संक्षिप्त परिभाषा होती है जिसे मात्र कुछ शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है।
- अवधारणा किसी घटना या व्यवहार प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या न होकर उसका एक संकेत मात्र होती है।
- अवधारणा का एक तार्किक आधार होता है जिसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, वास्तविक निरीक्षण एवं यथार्थ अनुभव के आधार पर होता है।
- अवधारणा स्वयं में अर्थयुक्त होती है क्योंकि यह तथ्यों के एक निश्चित समूह या वर्ग में पाई जाने वाली विलक्षणताओं की द्योतक होती है।
- अवधारणा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी होता रहता है। नए ज्ञान का संचय होने, वैज्ञानिक विशेष के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने अथवा तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का कोई नया स्वरूप प्रकट होने पर अवधारणाओं में परिवर्तन हो जाता है।
- अवधारणा स्वयं सिद्धांत का लघु स्वरूप नहीं होता बल्कि तथ्यों के एक वर्ग की विशेषताओं को संक्षेप में बताने वाला होता है।
अवधारणा का महत्त्व (Importance of Concept)-
- अवधारणा का महत्त्व इस बात से स्पष्ट होता है कि यह तथ्यों के एक वर्ग या समूह की संक्षिप्त परिभाषा का प्रतिनिधित्व करती है। अवधारणा के माध्यम से किसी घटना व प्रक्रिया को कुछ ही शब्दों में आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिये यदि किसी विद्यालय के एक वर्ग में कक्षा से विद्यार्थियों के भाग जाने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है तो इस संपूर्ण स्थिति को कक्षा पलायन की अवधारणा द्वारा समझाया जा सकता है।
- अवधारणा के महत्त्व के स्पष्टीकरण में गुडे तथा हाट ने लिखा है, ‘‘अवधारणा को विकसित करने वाली प्रक्रिया इंद्रियजनित बोध को प्राप्त करने व उससे निष्कर्ष निकालने में सहायक सिद्ध होती है।’’ इस प्रकार तथ्यों के एक वर्ग या समूह के गुणों को समझना, उनका अध्ययन करना और उन्हें व्यवस्थित करना या क्रमबद्ध व पृथक करना संभव होता है। अत: विचारों को आगे बढ़ाने के लिये अवधारणाओं का निर्माण ज़रूरी हो जाता है।
अवधारणा का अर्थ (Meaning of Concept)-
- अवधारणा से तात्पर्य भाषा दर्शन के उस शब्द से है जो तत्त्वमीमांसा, संज्ञानात्मक विकास और मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है।
- ध्यातव्य है कि जब कोई शोधकर्त्ता तथ्यों में अंतर्संबंधों को देखता है अथवा एक निश्चित घटना या व्यवहार प्रतिमान को पृथक करने में सफल होता है तो वह संपूर्ण स्थिति को बहुत ही संक्षेप में व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। इस संक्षिप्त अभिव्यक्ति को ही वैज्ञानिक अध्ययन में ‘अवधारणा’ के नाम से जाना जाता है। तत्त्व एवं सिद्धांत की भाँति वैज्ञानिक अध्ययन में भी अवधारणा का अपना विशिष्ट महत्त्व व उपयोगिता है।
अवधारणा की परिभाषाएँ (Definitions of Concept)-
विभिन्न विद्वानों द्वारा अवधारणा की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
- गुडे तथा हाट के अनुसार, ‘‘अवधारणा अमूर्त स्वरूप की होती है और वास्तविकता के कुछ ही विशेष पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है।’’
- मिचेल के अनुसार, ‘‘अवधारणा एक विवरणात्मक गुण या संबंध की ओर संकेत करने वाला एक पद है।’’
- पी.वी. यंग के अनुसार, ‘‘सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में अन्य तथ्यों से पृथक किये गए तथ्यों के एक वर्ग को अवधारणा का नाम दिया जा सकता है।’’
- सेरिंग के अनुसार, ‘‘अवधारणा वे शब्द या संकेत होते हैं जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं और उसकी विषयवस्तु को बतलाते हैं।’’
- फेयरचाइल्ड के अनुसार, ‘‘अवधारणाएँ वे विशिष्ट मौखिक संकेत हैं जो वैज्ञानिक निरीक्षण व चिंतन के आधार पर निकाले गए ‘सामान्यीकृत’ विचारों को दिये जाते हैं।’’
अम्ल- वे पदार्थ, जो खट्टे होते हैं अथवा जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जिनमें अम्ल (Acid) की उपस्थिति होती है। ये छूने में चिकने नहीं होते हैं। ये लिटमस पत्र को नीले से लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है।
|
अम्ल |
पदार्थ/स्रोत |
|
साइट्रिक अम्ल |
नींबू, संतरा आदि |
|
एसीटिक अम्ल |
सिरका |
|
कार्बनिक अम्ल |
कोल्ड ड्रिंक्स |
|
ऑक्सैलिक अम्ल |
टमाटर |
|
लैक्टिक अम्ल |
खट्टा दूध/दही |
|
यूरिक अम्ल |
मूत्र |
|
फॉर्मिक अम्ल |
लाल चींटी का डंक |
क्षार- वे पदार्थ, जो कड़वे होते हैं अथवा जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जिनमें क्षार (Base) की उपस्थिति होती है। ये छूने में चिकने होते हैं। ये लिटमस पत्र को लाल से नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण- सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया तथा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड आदि।
|
क्षार |
स्रोत |
|
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, |
चूने का पानी |
|
सोडियम हाइड्रॉक्साइड |
साबुन |
|
पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड |
साबुन |
|
मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड |
दूधिया मैग्नीशियम |
|
अमोनियम हाइड्रॉक्साइड |
खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिये उपयुक्त मार्जक |
- क्रियाशीलता के सिद्धांत की अपर्याप्तता (Lack of Principle of Self Activity)- ज्ञात है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत की अपर्याप्तता पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। यहाँ क्रियाशीलता से तात्पर्य क्रिया के माध्यम से प्रयोग द्वारा करके सीखने से है। स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है, फलस्वरूप अधिगम और बेहतर होता है। अत: पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से विकसित करने की आवश्यकता है।
- मनोरंजन का अभाव (Lack of Entertainment)- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मनोरंजक तत्त्वों का अभाव होना एक गंभीर समस्या है। इस कारण कुछ शिक्षार्थियों द्वारा इसके पाठ्यक्रम को बोझिल समझा जाता है। इस विसंगति को दूर करने के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। यह सर्वविदित है कि शिक्षण को रुचिकर बनाने के बाद ही अधिगम को प्रभावकारी बनाया जा सकता है और ऐसा करने के लिये शिक्षण प्रक्रिया मनोरंजक होनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी ऊबने लगते हैं एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते।
- अनुशासन की समस्या (Problem of Discipline)- ध्यातव्य है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है लेकिन कुछ शिक्षार्थी गतिविधि को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते जिससे कक्षा में अनुशासनहीनता का माहौल बनता है। अनुशासन के अभाव में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण सुचारु रूप से नहीं हो पाता। अत: शिक्षक को इस प्रकार की समस्या से सही ढंग से निपटना चाहिये और ऐसे विद्यार्थियों के साथ परिस्थितिजन्य व्यवहार करना चाहिये तथा उन्हें पर्यावरण अध्ययन की गंभीरता से परिचित कराना चाहिये।
- गृहकार्य में रुचि न लेना (Lack of Interest in Home work)- ध्यातव्य है कि पर्यावरण अध्ययन को अधिकतर शिक्षार्थी बहुत सरल मानते हैं और जब शिक्षक द्वारा इस विषय से संबंधित कोई गृहकार्य दिया जाता है तो वे इस विषय के गृहकार्य में विशेष रुचि नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिये अगर शिक्षक द्वारा दस पालतू और दस जंगली जानवरों की सूची बनाने का गृहकार्य दिया जाता है तो शिक्षार्थी इसे बेहद आसान मानकर इसे करने में रुचि नहीं लेते हैं। शिक्षक भी इस दिशा में कोई नवाचार नहीं कर पाते। इस प्रकार यह पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिये एक समस्या बन जाता है।
- तकनीक की कमी (Lack of Technique)- पर्यावरण अध्ययन में परंपरागत रूप से विषयसामग्री को प्रस्तुत करने के लिये व्याख्यान पद्धति का प्रयोग होता रहा है। यह बिना तकनीकी के भी संचालित हो सकती है लेकिन वर्तमान में यह पद्धति अपनी प्रासंगिकता खो रही है। पर्यावरण अध्ययन में कभी-कभी खुले मैदान में व्याख्यान की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में संचार के आधुनिक साधन महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान में संचार साधनों का रूप काफी विकसित हो चुका है लेकिन इन तकनीकों का प्रयोग पर्यावरण अध्ययन में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति एक समस्या के रूप में सामने आई है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक को पठनीय बनाकर तथा नवाचार का प्रयोग कर उसे रुचिकर एवं अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है।
- निजी अनुभवों का प्रयोग न होना (Lack of use of Personal Experience)- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षकों द्वारा निजी अनुभवों का प्रयोग न किया जाना एक गंभीर समस्या है। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में हर किसी के पास कोई न कोई निजी अनुभव ज़रूर होता है। अगर इन अनुभवों का प्रयोग शिक्षण में किया जाए तो यह लाभदायक सिद्ध होगा। अध्यापकों के लिये आवश्यक है कि वे अपने निजी अनुभवों का प्रयोग छात्रों के बीच करें और उन्हें यथासंभव पाठ्य-सामग्री का हिस्सा बना लें। ऐसा करने से छात्रों के मन में पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि जाग्रत होगी।
- प्रेरणा में कमी (Lack of Motivation)- विदित है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य-सामग्री में शिक्षार्थियों की रुचि पैदा करने के लिये प्रेरणा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारक है। प्रेरणा का तात्पर्य शिक्षार्थियों में किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिये रुचि उत्पन्न करना है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रेरणा छात्रों के अधिगम को अधिक स्थायी बनाने में सक्षम होती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रेरणा इसके लिये बेहद आवश्यक तत्त्व है। इसकी कमी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिये एक समस्या है।
- शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव (Lack of Teaching Aids)- पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण मुख्य रूप से प्रायोगिक क्रियाकलापों पर आधारित होता है और किसी भी प्रायोगिक कार्य के लिये अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी सामग्रियाँ शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। अगर विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण निश्चित रूप से बाधित होगा। जैसे अगर कोई शिक्षक कक्षा में महासागरों की अवस्थिति के संबंध में विद्यार्थियों को बताना चाहता है तो उसे ग्लोब की आवश्यकता होगी, ग्लोब के अभाव में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण बाधित होगा।
- सामुदायिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग न होना (Community Resources not being used in Required Quantity)- यह सर्वविदित है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कक्षा से अधिक कक्षा के बाहर कारगर सिद्ध होता है। यह कक्षा-कक्ष में पढ़ने और पढ़ाने से ही पूर्ण नहीं हो पाता है बल्कि इसके लिये ऐसे विभिन्न सामुदायिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है जहाँ भ्रमण करके शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कुछ महत्त्वपूर्ण सामुदायिक संसाधन हैं- पन-बिजलीघर, संग्रहालय, चिड़ियाघर, ऐतिहासिक इमारत, सरकारी भवन, पार्क, रेलवे स्टेशन आदि। पर्याप्त मात्रा में इन संसाधनों का प्रयोग न किया जाना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की प्रमुख समस्या है। कई बार कुछ सामुदायिक संसाधनों की यात्रा अत्यधिक खर्चीली हो जाती है, इसलिये इनका पर्याप्त प्रयोग नहीं हो पाता है।
- प्रायोगिक कार्य का अभाव (Lack of Experimental Work)- पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति विज्ञान की तरह है। जिस प्रकार विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्यों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण काफी हद तक प्रायोगिक कार्यों पर निर्भर करता है। प्रायोगिक कार्य के अभाव में पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान दोनों का शिक्षण संभव नहीं हो पाता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान प्रायोगिक कार्यों की अधिकता न होना इसके शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है।
- प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव (Lack of Trained Teacher)- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित शिक्षक प्रयोग के माध्यम बड़ी से बड़ी संकल्पनाओं को आसानी से समझा सकते हैं। इनकी कमी होने से शिक्षण की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो पाती है। वर्तमान समय में अधिकांश विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है जो पर्यावरण अध्ययन में एक समस्या के रूप के सामने आई है।
सर्वविदित है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान कक्षा के अंदर तथा बाहर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिये क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का संबंध किसी एक विशिष्ट विषय से न होकर अनेक विषयों से है। साथ ही इसकी विषयवस्तु बहुत जटिल और विविधताओं से भरी हुई है। इसके शिक्षण के दौरान सामने आने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याओं का विवरण निम्नलिखित है-
- वैयक्तिक विभिन्नताएँ (Individual Differences)- ध्यातव्य है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में वैयक्तिक विभिन्नता एक विकट समस्या है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ‘‘कोई व्यक्ति अपने समूह से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है।’’ उदाहरण- किसी विद्यालय के एक ही कक्षा-कक्ष में विभिन्न वैयक्तिक विभिन्नताओं वाले विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं लेकिन उनकी अधिग्रहण क्षमता, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि एक-दूसरे से भिन्न होती है जिस कारण कक्षा-कक्ष में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का कार्य कठिन हो जाता है। ज्ञात हो, पर्यावरण अध्ययन में प्रायोगिक ज्ञान अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये कई तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं लेकिन कक्षा-कक्ष में वैयक्तिक विभिन्नता के कारण सभी के लिये अलग-अलग प्रयोग आयोजित करना काफी खर्चीला हो जाता है जो एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आता है।
- पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएँ (Problems Related to Curriculum)- सर्वज्ञात है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर निर्मित नहीं किया गया है। यह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एक विकट समस्या है फलत: शिक्षार्थियों में पर्यावरण अध्ययन को सीखने की क्षमता का विकास धीरे-धीरे तथा क्रमबद्ध रूप से नहीं हो पाता है। ज्ञात हो कि पर्यावरण अध्ययन बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है और यदि इसका पाठ्यक्रम सही तरीके से विकसित नहीं किया गया तो यह अधिगम के लिये समस्या पैदा कर सकता है। शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध का पता लगाना और समझना महत्त्वपूर्ण है लेकिन इसके पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुसार प्रबंधित नहीं किया गया है। इसमें बच्चों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता को ठीक से संप्रेषित नहीं किया गया है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम बच्चों की आयु एवं सामान्य बुद्धि क्षमता के अनुरूप होना चाहिये। अगर पाठ्यक्रम इसके विपरीत होता है तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में समस्याएँ आना स्वाभाविक है।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिये आपको प्राय: शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की बहि:शालीय गतिविधियों के लिये कक्षा से बाहर ले जाना पड़ता है। कक्षा से बाहर के क्रियाकलापों के आयोजन में आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिये पर्याप्त पूर्व आयोजना की आवश्यकता होगी। अंत:शालीय (कक्षा के भीतर के) गतिविधियों के वर्णित सभी बिंदु बहि:शालीय गतिविधियों पर भी लागू होते हैं। तथापि इस सूची में निम्नलिखित बिंदु और जोड़े जा सकते हैं-
- उस स्थान का चयन पहले से कर लेना चाहिये जहाँ आपको बच्चों को ले जाना है।
- उस स्थान को पहले से जाकर देखना उपयोगी होगा। स्थान की संभावनाओं की जाँच कर लें। उदाहरण के लिये, यदि विद्यालय परिसर में पेड़ों का अध्ययन करना है तो यह देखना होगा कि वहाँ पर्याप्त संख्या में पेड़ मौजूद हैं भी या नहीं। इसी प्रकार जल-पक्षियों के अध्ययन के लिये आपको बच्चों को पास के ऐसे तालाब पर ले जाना होगा जहाँ काफी संख्या में विभिन्न प्रकार के जल-पक्षी उपलब्ध हों।
- बाहर जाने से पहले कक्षा में चर्चा का आयोजन अपेक्षाओं के बोध में सहायता करता है और की जाने वाली गतिविधियों से परिचित कराता है। यदि संभव हो तो प्रत्येक टोली के लिये लिखित रूप में गतिविधि संबंधी जानकारी पत्रक बनाकर टोली के मुखिया को दे दें। उसमें सरल भाषा में यह बताएँ कि उन्हें क्या करना, देखना या एकत्रित करना होगा।
- प्रत्येक बालक द्वारा लाई जाने वाली सामग्री की सूची बनाएँ। उदाहरण के लिये, प्रत्येक बालक के पास एक कॉपी, पेंसिल आदि होनी चाहिये। उन्हें जिन अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उनकी भी सूची बनाएँ। जैसे- मापने वाला फीता, सामान रखने वाले थैले, जार अथवा बोतल, पुराने अखबार आदि।
- टोली के मुखिया को उसका उत्तरदायित्व समझाएँ। प्रत्येक टोली के लिये विशिष्ट कार्य निश्चित कर दें।
- बाहर की जाने वाली गतिविधियों का आयोजन इस प्रकार करें कि बाद में कक्षा में किये जाने वाले अनुवर्ती (फोलोअप) क्रियाकलापों के लिये आपके पास पर्याप्त समय उपलब्ध हो। अत: बच्चों को खाली समय में स्वतंत्र प्रेक्षण के लिये प्रोत्साहित करें जिसके आधार पर बाद में कक्षा में चर्चा का आयोजन किया जा सके।
- सुरक्षा के सभी उपाय करें और बच्चों को संभावित खतरों/संकटों एवं उनसे बचने के उपायों को स्पष्टत: समझा दें।
कक्षा से बाहर की यात्रा के उपरांत जायज़ा लें कि बच्चों ने किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किये हैं। कक्षा में चर्चा आयोजित करें और भविष्य में किये जाने वाले क्रियाकलापों की योजना बनाएँ। एक लघु प्रदर्शनी का आयोजन करें जिसमें बच्चे अपना कार्य प्रदर्शित कर सकें। इससे उनके ज्ञान का विस्तार तो होगा ही, उन्हें भविष्य में कार्य करने के लिये अभिप्रेरणा भी प्राप्त होगी। गतिविधि की आयोजना करते समय आपको इस प्रकार के समाकलन को ध्यान में रखना चाहिये। बच्चों द्वारा सोचे/लाए गए विचारों का उपयोग करें। आप इन विचारों का परिष्करण, रूपांतरण और प्रबलन कर सकते हैं।
प्रभावी अधिगम और विभिन्न प्रक्रियात्मक कौशलों के विकास की दृष्टि से बच्चों की सहायता करने के लिये आप समूह गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। समूह गतिविधि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावी बनाती है क्योंकि बच्चे इसमें सक्रिय भागीदार होते हैं। वे प्राय: स्वयं कार्य करते हैं और स्व-अनुभव से सीखते हैं। इसलिये ऐसा अधिगम स्थायी, रोचक और लाभप्रद सिद्ध होता है। समूह के सदस्यों के बीच पर्याप्त अंत:क्रिया होती है। इससे सम-समूह अंत:क्रिया को बढ़ावा मिलता है और बच्चों में मिल-जुलकर कार्य करने की आदत विकसित होती है। यह स्व-अधिगम को भी बढ़ाता है। समूह गतिविधि द्वारा बच्चे अपने कार्यों के लिये अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार करना सीखते हैं। इसे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का एक प्रभावी उपकरण बनाने के लिये निम्नलिखित बातें उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं-
- किसी समूह में पाँच अथवा छह से अधिक बच्चे न हों।
- समूह के प्रत्येक सदस्य को कोई विशिष्ट भूमिका दें। उदाहरण के लिये, एक बच्चे को प्रयोग करने के लिये कहा जाए, दूसरा आँकड़ों एवं तथ्यों का अभिलेखन (रिकॉर्ड) करे और तीसरा परिणाम प्रस्तुत करे।
- किसी क्रियाकलाप को सुचारु रूप से चलाने के लिये समूह का एक नेतृत्वकर्त्ता होना चाहिये और सभी सदस्यों को उसके नेतृत्व में कार्य करना चाहिये।
- समूह के विभिन्न सदस्यों की भूमिकाओं में परस्पर परिवर्तन करते रहें ताकि प्रत्येक बच्चे को विभिन्न भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व निभाने का अवसर प्राप्त हो।
- निश्चित समूह न बनाएँ। समूहों के संघटन को बदलते रहें ताकि बच्चों में होने वाली अंत:क्रियाओं में वृद्धि हो और पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित हो।
- विभिन्न समूह अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करते रहें। यह सुनिश्चित करें कि सभी गतिविधियाँ पाठ विषय/प्रकरण से संबंधित हों।
- बच्चों को विभिन्न रूपों/माध्यमों में अभिव्यक्ति के लिये प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिये, लिखित रिपोर्ट के माध्यम से, आरेखन या चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त करना।
- प्रत्येक क्रियाकलाप की समाप्ति पर कक्षा में चर्चा करें ताकि शंकाओं का निवारण हो सके और प्रेक्षण तथा संकलित आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकें।
- बच्चों के कार्यों को कक्षा में प्रदर्शित करें।
- रियासती शासक
|
क्रम संख्या |
रियासत |
शासक |
|
1. |
कोटा |
राम सिंह |
|
2. |
जोधपुर |
तख़्त सिंह |
|
3. |
भरतपुर |
जसवंत सिंह |
|
4. |
उदयपुर |
स्वरूप सिंह |
|
5. |
सिरोही |
शिव सिंह |
|
6. |
धौलपुर |
भगवंत सिंह |
|
7. |
बीकानेर |
सरदार सिंह |
|
8. |
करौली |
मदनपाल |
|
9. |
टोंक |
नवाब वजीरुद्दौला |
|
10. |
बूंदी |
राम सिंह |
|
11. |
अलवर |
विनय सिंह |
|
12. |
जैसलमेर |
रणजीत सिंह |
|
13. |
झालावाड़ |
पृथ्वी सिंह |
|
14. |
प्रतापगढ़ |
दलपत सिंह |
|
15. |
बांसवाडा |
लक्ष्मण सिंह |
|
16. |
डूंगरपुर |
उदय सिंह |
|
17. |
जयपुर |
राम सिंह द्वितीय |
- ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट
- कोटा- मेजर बर्टन
- जोधपुर- मैकमेसन
- भरतपुर- मोर्रिसन
- जयपुर- ईडन
- उदयपुर- शावर्स ऑर
- सिरोही- जे.डी. हॉल
1. जयपुर (पिंक सिटी)
- हवा महल- अपने अनोखे डिजाइन और कई खिड़कियों के लिये प्रसिद्ध महल।
- अंबर का किला- शानदार किला जो अद्भुत वास्तुकला और दृश्यों के लिये जाना जाता है।
- सिटी पैलेस- राजस्थानी और मुग़ल वास्तुकला का एक मिश्रण।
- जंतर मंतर- एक खगोलीय वेधशाला है।
2. उदयपुर (झीलों का शहर)
- पिछोला झील- नाव की सवारी और सुरम्य दृश्यों के लिये प्रसिद्ध यह एक शांत झील है।
- सिटी पैलेस- एक भव्य महल जिसमें सुंदर वास्तुकला कार्य और एक संग्रहालय है।
- जगदीश मंदिर- भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर।
- फतेह सागर झील- जलीय खेलों और घूमने के लिये लोकप्रिय।
3. जैसलमेर (गोल्डन सिटी)
- जैसलमेर किला- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो अपने शानदार बलुआ पत्थर की वास्तुकला के लिये जाना जाता है।
- सैम सैंड ड्यून्स (रेत के टीले)- ऊंट की सवारी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिये एक शानदार स्थान।
- पटवों की हवेली- अद्भुत वास्तुकला और शिल्प कौशल का अद्वितीय उदाहरण।
4. पुष्कर
- पुष्कर झील- मंदिरों और घाटों से घिरी पवित्र झील जो आध्यात्मिक अनुभव के लिये आदर्श स्थान है।
- ब्रह्माजी का मंदिर- देश में भगवान ब्रह्मा को समर्पित कुछ ही मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।
- पुष्कर ऊंट मेला- एक वार्षिक सांस्कृतिक मेला जो राजस्थान की ग्राम्य परंपराओं को दर्शाता है।
5. अजमेर
- अजमेर शरीफ दरगाह- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल।
- अना सागर झील- एक खुबसूरत और सुरम्य झील है।
राजस्थान का समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और अद्भुत परिदृश्य इसे एक शीर्ष पर्यटन स्थल बनाते हैं, जहाँ प्रत्येक शहर में आपको अद्वितीय अनुभव मिलते हैं।
- यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है।
- शरीर की आवश्यकता की 50%-70% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से ही होती है।
- कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है।
- कार्बोहाइड्रेट्स तीन प्रकार के होते हैं- मोनो-सैक्राइड्स, डाइ-सैक्राइड्स तथा पॉली-सैक्राइड्स।
- ग्लूकोज मुख्य रूप से अंगूर तथा शहद में मिलता है तथा यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है।
- सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज डाइ-सैक्राइड्स के उदाहरण हैं।
- पॉली-सैक्राइड्स का निर्माण अनेक मोनो-सैक्राइड्स अणुओं के मिलने से होता है। पॉली-सैक्राइड्स मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है तथा यह जल में अघुलनशील होता है।
- सेल्यूलोज, मंड या स्टार्च, काइटिन एवं ग्लाइकोजेन मुख्य रूप से पॉली-सैक्राइड्स के उदाहरण हैं।
- अंगूर, गन्ना, शहद एवं मीठे फल में मुख्य रूप से शर्करा पाई जाती है।
- फल एवं सब्ज़ियों में सेल्यूलोज पाया जाता है।
- गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, जौ, केला, साबूदाना में श्वेतसार पाया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्य
- ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है।
- यह मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है।
- यह वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करता है।
- कार्बोहाइड्रेट्स RNA तथा DNA का घटक होता है।
- यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिये ईंधन का काम करता है।
- गणित एक प्रजातांत्रिक और समस्या केंद्रित तकनीक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से एक समस्या हल करने के लिये दी जाती है। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों में समस्या को हल करने की क्रियात्मकता को बढाती है।
- इस विधि के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान के उच्च क्रम को प्राप्त कर सकने में सक्षम होते हैं। इसके माध्यम से भावात्मक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। मस्तिष्क उद्वेलन गणित के लाभ निम्नलिखित हैं-
- गणित की शिक्षण विधि में ब्रेन-स्टॉर्मिंग आव्यूह रचना का विशेष महत्त्व है।
- इसके द्वारा विद्यार्थियों में सामूहिक रूप से सोचने तथा कार्य करने की आदत का विकास होता है।
- इसे शिक्षण की एक प्रजातांत्रिक प्रविधि कहा जाता है।
- यह विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक, उत्साहवर्धक, आत्मविश्वास, वास्तविकता, सृजनात्मकता तथा तर्क-वितर्क करने की क्षमताओं को बढ़ाता है।
- यह विद्यार्थियों के विचार, भाव और उद्देश्यों को व्यवस्थित करता है।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में विद्यमान समस्याओं को निम्नलिखित उपायों से दूर किया जा सकता है-
- शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना (Generate Interest Among Learners)- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षार्थियों की रुचि पैदा करके समस्याओं को दूर किया जा सकता है। रुचि पैदा करने के लिये पाठ्यक्रम को रोचक ढंग से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन कर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षार्थियों की रुचि पैदा की जा सकती है।
- पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना (Linking Curriculum to Life)-पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण पाठ्यक्रम को अगर आम जनजीवन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाए तो इसके अध्ययन से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, अगर शिक्षार्थियों को पशुपालन के संबंध में पढ़ाना है तो नज़दीक के किसी तबेले का भ्रमण कर शिक्षण कार्य किया जा सकता है।
- रोचक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना (Using Interesting Teaching Aids)- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में रोचक शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके समस्या को दूर किया जा सकता है। रोचक सामग्री के अंतर्गत ग्लोब, मानचित्र, डिजिटल बोर्ड, मार्कर, फूल के गमलों आदि को शामिल किया जा सकता है। इन सबका प्रयोग कर पर्यावरण अध्ययन को आसानी से कक्षा तथा कक्षा के बाहर समझाया जा सकता है।
- कविता और कहानियों का प्रयोग (Use of Poetry and Stories)-कविताएँ और कहानियाँ पढ़ना या सुनना बच्चों को अच्छा लगता है। अगर इनका प्रयोग पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में किया जाए तो यह काफी लाभदायक साबित होगा। इनके माध्यम से जटिल से जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझाया जा सकता है।
- करके सीखने पर बल (Emphasis on Learning by Doing)- पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिये। शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग करेंगे तो उन्हें अधिक सीखने को मिलेगा। पर्यावरण अध्ययन प्रायोगिक कार्यों पर अधिक निर्भर होता है। अगर प्रयोग स्वयं किये जाएँ तो बेहतर परिणाम की कल्पना की जा सकती है।
- शिक्षक का प्रशिक्षण (Teacher Training)- शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान न दिये जाने के कारण पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो सका है। शिक्षकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिये सरकार को आवश्यक तंत्र विकसित करना चाहिये, साथ ही आर्थिक सहयोग देना चाहिये है ताकि शिक्षकों के विषय संबंधी ज्ञान को अद्यतन किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न विषयों की शिक्षक-पुस्तिका के प्रयोग को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
कक्षा में प्रश्न पूछने के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं-
- विद्यार्थियों में उत्सुकता बढ़ाना ताकि वे अधिगम में अधिक रुचि ले सकें तथा चिंतन की प्रवृत्ति का विकास कर सक्रिय रूप से अधिगम के भागीदार बन सकें।
- विद्यार्थियों के ध्यान को किसी विशिष्ट बिंदु पर आकर्षित करने के लिये शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जा सकता है।
- स्व-शिक्षण में प्रश्न महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके माध्यम से शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है।
- प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों में संप्रेषण एवं अभिव्यक्ति का विकास सुनिश्चित होता है। विद्यार्थी प्रश्न का जवाब देते समय अपने विचारों को तर्कपूर्ण तथा आसान भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इससे विद्यार्थी में भाषा कौशल का विकास होता है।
- विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किये गए ज्ञान का आकलन एवं मूल्यांकन करने में प्रश्न सहायता प्रदान करते हैं। इससे विद्यार्थियों में परीक्षण और जाँच की क्षमता का विकास होता है।
- शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंत:क्रिया की वृद्धि में प्रश्न का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्राप्त होता है।
- शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी सही दिशा में अधिगम कर रहे हैं या नहीं।
- विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु व पाठ की ओर उन्मुख करना तथा पूर्वज्ञान का केंद्रीकरण व नवीन ज्ञानोन्मुख बनाना भी प्रश्न का उद्देश्य होता है।
- विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया इसका पूर्ण अनुमान लगाकर अग्रिम के लिये व्यवस्था करना तथा उनमें विचारशक्ति, कल्पना एवं तर्कशक्ति का विकास करना भी प्रश्न का उद्देश्य होता है।
- विद्यार्थी के मस्तिष्क की क्रियाशीलता एवं मानसिकता का विकास करना तथा उनकी आकांक्षा, अभिलाषा, आवश्यकता, महत्त्वाकांक्षा का ध्यान रखना प्रश्न के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।
- विद्यार्थियों के पूर्वज्ञान को जानने के लिये तथा उनमें विषयवस्तु के प्रति अवधान, रुचि एवं जिज्ञासा बनाए रखने के लिये प्रश्न आवश्यक होते हैं।
- विद्यार्थियों को सैद्धांतिक व व्यावहारिक रूप से तैयार करने के लिये तथा उनकी प्रगति एवं तर्कशक्ति का विकास करने हेतु प्रश्न ज़रूरी हैं।
शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएँ
शिक्षण में उपयोगी सहायक सामग्री की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
- सहायक सामग्री स्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायता प्रदान करती है। यह अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है।
- इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। वे अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को सुगमता से आत्मसात कर लेते हैं।
- इससे समय की बचत तथा रुचि में वृद्धि होती है। यह मौखिक बातों की अल्पता होती है। इससे शिक्षक को अच्छे शिक्षण में मदद मिलती है।
- वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिलता है। साथ ही, प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिलता है।
- विद्यार्थियों को उपकरण प्रयोग करने की विधि का ज्ञान होता है,साथ ही उनमें विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति उत्सुकता जाग्रत होती है।
- सहायक सामग्री सूक्ष्म बातों को सरलता से समझा देती है। यह विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति का विकास करती है।
शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के समय सावधानियाँ (Precautions While Using Teaching Aids)-
- विद्यार्थियों के अनुभव, आवश्यकता, समझ, आयु तथा विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार ही शिक्षण सामग्री होनी चाहिये।
- शिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिये जो कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो।
- शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों के परिवेश के अनुसार होनी चाहिये ताकि प्रकरण के सभी बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त हो सके।
- ऐसी शिक्षण सामग्री का चयन किया जाना चाहिये जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करे और उन्हें जिज्ञासु बना सके।
- शिक्षण सामग्री की जितनी देर आवश्यकता हो, उतनी ही देर तक प्रयोग में लाया जाना चाहिये।
- शिक्षण सामग्री सही हालत तथा शिक्षणात्मक मूल्यों से युक्त होनी चाहिये।
- जिस पाठ में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना हो उसके विषय में पहले से ही योजना बना ली जानी चाहिये।
- उपयुक्त स्थल पर ही शिक्षण सहायता सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिये।
- शिक्षण सामग्री पर्याप्त स्पष्ट हो जिससे विद्यार्थी उसे सरलता से देख और समझ सकें।
शिक्षण सहायक सामग्री/संसाधन का अर्थ (Meaning of Teaching Material/Resources)-
- ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर शब्दकोष के अनुसार, “वह चीज़ जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाई जाती है उसे सामग्री या संसाधन कहा जाता है।” पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एक अध्यापक के लिये शब्दकोष, नक्शा, ग्लोब, विद्यालय का बगीचा, वीडियो फिल्म इत्यादि सहायक सामग्री का कार्य करते हैं।
- एक शिक्षक जो पौधों के बारे में पढ़ाना चाहता है, वह विद्यालय के बगीचे को एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है। एक शिक्षक नदी तथा तालाब की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिये नदी या तालाब के पास भ्रमण की व्यवस्था कर सकता है या उनकी फिल्म/वीडियो क्लिप इत्यादि दिखा सकता है। ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य करते हैं। अत: शिक्षण सहायक सामग्री वह साधन है जिससे शिक्षार्थी का सीखना अत्यंत सहज हो जाता है।
शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषाएँ (Definitions of Teaching Aids)-
शिक्षण सहायक सामग्री को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है-
- एलविन स्ट्राँग के मतानुसार, ‘‘शिक्षण सहायक सामग्री के तहत वे सभी साधन सम्मिलित किये जाते हैं जिनकी सहायता से विद्यार्थियों की पठन रुचि बनी रहती है और वे पाठ को सुगमतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं।’’
- डेंड के मतानुसार, ‘‘शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या मौखिक पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है।’’
- कार्टर ए. गुड के मतानुसार, ‘‘जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रज्वलित किया जा सके या श्रवणेन्द्रिय संवेदनाओं द्वारा उसे आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है।’’
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में सहायक सामग्री की महत्ता (Importance of Aids in Teaching Environmental Studies)-
- पर्यावरण अध्ययन शिक्षण-अधिगम हेतु शैक्षिक संसाधनों का प्रयोग अति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन मूल्यों को पहचानने एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है ताकि मनुष्यों, संस्कृति तथा जैविक-भौतिक वातावरण के बीच सहसंबंधों को समझने और महसूस करने के लिये आवश्यक कौशल एवं मनोवृत्तियों का विकास किया जा सके।
- पर्यावरण अध्ययन में कक्षा से बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रियाएँ काफी प्रभावशाली होती हैं।
- पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित वास्तविक जीवन के अनुभव उपयुक्त होते हैं। स्थानीय संसाधन एवं सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं।
- पर्यावरण अध्ययन विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक योग्यता, सक्षमता तथा उपायकुशलता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। साथ ही उसे सामाजिक घटनाएँ, जो परिवार से शुरू होकर विस्तृत होती जाती हैं, के लिये जिज्ञासु बनाता है। अधिगम के संसाधनों का रचनात्मक उपयोग करके इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
जब किसी शंका/समस्या के समाधान के लिये या किसी जानकारी या सूचना की प्राप्ति के लिये किसी व्यक्ति द्वारा कुछ भाषायी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या, क्यों, कौन, कैसे, किसका, कौन-सा, कब, कहाँ ये ऐसे प्रश्न सूचक शब्द हैं, जिनके उत्तर उपलब्ध हों या इन प्रश्नों के उत्तरों की अभिलाषा की जाए, ऐसे शब्दों को प्रश्न कहते हैं।
- सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिये जो कुछ भी कहा या लिखा जाता है, उसे उस प्रश्न का उत्तर कहते हैं।
- बासिंग के अनुसार, ‘‘प्रश्न करने की कला का महत्त्व स्वीकार किये बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती।’’
- रमन बिहारी लाल के अनुसार, ‘‘अगर हम कहें कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण क्रिया ही नहीं होगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।’’
प्रश्नों का निर्माण (Formation of Questions)
- ब्रिटिश शिक्षाविद थॉमस रेमाउण्ट ने वर्ष 1904 में प्रकाशित अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन’ में लिखा है, ‘‘अच्छी प्रश्न कला की तकनीक को जानना एक नए युवा शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक उद्देश्य होना चाहिये।’’
- प्रश्न निर्माण अध्ययन-अध्यापन का एक आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह प्रक्रिया पूर्व से ही प्रचलित रही है। प्रश्न निर्माण के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाने तथा विद्यार्थियों के मूल्यांकन में मदद मिलती है।
- कक्षा की जीवंतता बनाए रखने में भी प्रश्न निर्माण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- प्रश्न के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद की ऐसी प्रक्रिया का निर्माण होता है जिससे पूरी कक्षा की क्रियाशीलता बनी रहती है तथा चिंतन की प्रक्रिया का निर्माण होता है।
- अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना- उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहन एवं प्रलोभन प्रदान करता है। एक प्रकार से परीक्षाएँ विद्यार्थियों को प्रेरणा भी प्रदान करती हैं।
- शिक्षण विधि में सुधार- शिक्षक तथा विद्यार्थीं दोनों ही परीक्षा परिणामों के आधार पर शिक्षण विधि की सफलता की मात्रा जान सकते हैं और आवश्यक होने पर उसमें सुधार के प्रयत्न कर सकते हैं। परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के आधार पर अध्यापक अपने द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि की सफलताओं का ज्ञान कर सकता है।
- मान्यता प्रदान करने में सहायक- परीक्षा परिणामों के आधार पर कहीं-कहीं विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती है और इन्हीं के आधार पर उनके लिये अनुदान की मात्रा निर्धारित की जाती है।
- शिक्षण में सुधार- प्रतिवर्ष परीक्षाओं के लिये शिक्षक को परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करना पड़ता है, परिणामस्वरूप अध्यापक के ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। अपने वर्द्धित ज्ञान के आधार पर अध्यापक सहज ही शिक्षण में सुधार कर लेता है।
- अध्यापक तथा विभागों का मूल्यांकन- परीक्षा परिणामों के आधार पर ही शिक्षक विद्यालय तथा विभिन्न विभागों का मूल्यांकन करने के भी काम आते हैं। विभिन्न विद्यालय तथा विभागों में अध्यापन की स्थिति, प्रभावशीलता तथा कुशलता का ज्ञान हो सकता है। इसके द्वारा इनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।
- शैक्षिक निर्देशन में सहायक- परीक्षाओं द्वारा न केवल बालक को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में काफी सहायता होती है बल्कि परीक्षाएँ विद्यार्थीं के संबंध में अनेक उपयोगी सूचनाएँ प्रदान करती हैं। परिणामों के आधार पर विद्यार्थीं की विषय संबंधी उपलब्धियों, अभियोग्यताओं, अभिरुचियों, योग्यताओं आदि का सहज ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी शैक्षिक निर्देशन के लिये अत्यंत आवश्यकता होती है।
- अन्वेषण के लिये आवश्यक- शिक्षा में अनुसंधान तथा शोधकार्य करने के लिये परीक्षाएँ आवश्यक सामग्री जुटाती हैं। अनेक परीक्षा परिणाम तथा विद्यार्थियों की निष्पत्तियाँ विभिन्न प्रकार के शोधकार्यों में आधारभूत तथ्यों का काम करती हैं।
मूर्धन्य विद्वानों का पिछले अनेक वर्षों से यह अटल विश्वास है कि परंपरागत शिक्षण-प्रविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जबरदस्ती ज्ञान को भरने से उनका स्वाभाविक विकास संभव नहीं है। तब इन परंपरागत शिक्षण विधियों के विरोधस्वरूप एक नई शिक्षण विधि का जन्म हुआ, जिसे स्वाध्ययन प्रविधि के नाम से जाना गया। परंपरागत शिक्षण विधि, विद्यार्थियों को ऊपर से ज्ञान प्रदान करती है, कहकर इसकी आलोचना की जाती रही है।
स्वाध्ययन प्रविधि की विशेषताएँ-
- स्वाध्याय विद्यार्थियों में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होता है।
- स्वाध्याय के माध्यम से खाली समय का सदुपयोग किया जाता है और विद्यार्थी को अध्ययन के लिये प्रेरित किया जाता है।
- अपने प्रयत्नों द्वारा समस्याओं को हल करने तथा स्वयं पढ़ते रहने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है।
- स्वाध्ययन से गणित के अध्ययन में विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि विकसित होती है।
अध्यापक की पूर्ण देख-रेख या पर्यवेक्षण (Supervision) में विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला अध्ययन पर्यवेक्षित-अध्ययन कहलाता है। इस प्रकार का अध्ययन स्वाध्याय अथवा समूह अध्ययन किसी भी रूप में संपन्न किया जा सकता है। शिक्षक यहाँ एक वास्तविक पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है तथा उसे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से विद्यार्थियों को उनकी अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के आधार पर कठिनाइयों का समाधान ढूँढना पड़ता है।
पर्यवेक्षण अध्ययन की विशेषताएँ-
- अध्यापक विद्यार्थियों की प्रगति से परिचित होते हैं।
- विद्यार्थियों को उचित समय पर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन मिलता रहता है।
- इसमें विद्यार्थियों को पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि में अधिक कार्य करने का अवसर दिया जाता है तथा इसमें गृह-कार्य भी दिया जाता है।
- पर्यवेक्षण अध्ययन का मूल उद्देश्य अनेक संबंधों के आधार पर सामान्यीकरण कराना होता है जिससे विद्यार्थी पाठ्यवस्तु का गहनता से अध्ययन कर सकें।
- पर्यवेक्षण अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक प्रधानता दी जाती है।
सीमाएँ-
- यह उच्च कक्षाओं के लिये अधिक उपयोगी है बजाय प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के।
- इसमें विद्यार्थियों के चारित्रिक विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि पाठ्यवस्तु के अध्ययन को ही प्रमुखता दी जाती है।
- इसमें विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशन पर ही निर्भर रहते हैं तथा प्रत्येक समस्या का समाधान अध्यापक से पूछते हैं। विद्यार्थी स्वयं समस्याओं का समाधान नहीं खोजते हैं।
गृह-कार्य को अधिगम अनुभवों का एक साधन माना जाता है। गृह-कार्य की रचना इस प्रकार तय की जाती है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अनेक शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर उत्पन्न अधिगम अनुभवों को संगठित करने के लिये गृह-कार्य देना अत्यावश्यक है। इस प्रकार गृह-कार्य अनुभवों के अभ्यास तथा पुनर्बलन का कार्य करता है। अध्यापकीय कक्षा-शिक्षण अधिगम में कठिनाइयों में विद्यार्थी जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने ढ़ंग से सीखने और स्थायी बनाने के दृष्टिकोण से गृह-कार्य का गणित में विशेष महत्त्व होता है। अतः गृह-कार्य वह साधन है जो विद्यार्थियों को स्वयं अभ्यास करके सीखने का मौका प्रदान करता है। यह अधिगम अनुभवों का एक प्रमुख अंग है। गृह-कार्य उस कार्य को कहते हैं जिसे विद्यार्थी शिक्षण के उपरांत घर पर पूरा करता है। इससे उसके द्वारा कक्षा में अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों की पुष्टि भी हो जाती है।
लारेन फॉक्स ने गृह-कार्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “गृह-कार्य विद्यार्थियों के लिये चुनौतीपूर्ण होना चाहिये।“
गृह-कार्य का महत्त्व
- इसके द्वारा विद्यार्थियों को समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान किये जाते हैं।
- गृह-कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन तथा कार्य करने की आदत का विकास होता है।
- गृह-कार्य के द्वारा विद्यार्थियों को गणित के किसी प्रकरण, सूत्र या नियम को सीखने में मदद मिलती है।
- गृह-कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में गणित के प्रति सकारात्मक रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है।
- गृह-कार्य को यदि वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर दिया जाए तो यह अधिक गतिशील हो सकता है।
गणित में अभ्यास कार्य अत्यावश्यक है। अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामिति की प्रक्रियाओं का स्पष्ट अवबोधन अभ्यास कार्य से ही संभव है। प्रारंभिक स्तर के गणित से लेकर उच्च स्तर के गणित को सीखने के लिये अभ्यास कार्य बहुत आवश्यक है। जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग की सही क्रियाओं को उचित ढ़ंग से हल करने की क्षमता तथा योग्यता विद्यार्थियों में तभी पैदा होगी जब वे इन क्रियाओं का व्यवस्थित ढ़ंग से अभ्यास करें, जब तक अभ्यास कार्य नियमित तथा व्यवस्थित ढ़ंग से नहीं किया जाता है तब तक उनके द्वारा विद्यार्थियों में वांछनीय क्षमता का विकास संभव नहीं होता है।
जिस प्रकार शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में कुशलता एवं निपुणता पाने के लिये अभ्यास कार्य आवश्यक एवं उपयोगी है उसी प्रकार गणित में दक्षता प्राप्त करने के लिये अभ्यास कार्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बिना अभ्यास के विद्यार्थी या व्यक्ति अपने क्षेत्र में पारंगत नहीं हो सकता है।
अभ्यास कार्य का महत्त्व
शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार, गणितीय सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का अवबोधन समुचित अभ्यास कार्य के बिना नहीं हो सकता है। समुचित अभ्यास कार्य का अर्थ यह नहीं है कि गणित के सूत्रों को रटकर उनका प्रयोग किया जाए, बल्कि अभ्यास कार्य गणितीय प्रत्ययों, नियमों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों आदि का उचित अवबोधन में सहायता करता है।
- सीखे हुए सिद्धांतों, नियमों, प्रक्रियाओं, प्रत्ययों आदि का प्रयोग अभ्यास के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। अन्यथा नियमों, सिद्धांतों, आदि का ज्ञान विद्यार्थियों के लिये बोझ बनकर रह जाएगा।
- अभ्यास कार्य के द्वारा विद्यार्थियों में गणना संबंधी कुशलताओं में विकास किया जा सकता है।
- गणित के अभ्यास कार्य के अभाव में, इसे एक नीरस तथा कठिन विषय माना जा सकता है जो असत्य है।
- अनेक सिद्धांतों एवं प्रत्ययों के बारे में अस्पष्टता के कारण ही नए विद्यार्थी उप-विषयों को सीखने में असमर्थ होते हैं तथा गणित उनको नीरस तथा कठिन विषय लगने लगता है।
- ऊँट महोत्सव - बीकानेर
- अवधि- 2 दिन (जनवरी)
- विशेष आकर्षण- राजस्थानी संगीत और नृत्य के साथ ऊंटों की दौड़ तथा सौंदर्य प्रतियोगिता।
- ब्रज होली महोत्सव - भरतपुर
- अवधि- 2 दिन (फरवरी-मार्च)
- विशेष आकर्षण- रासलीला, भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित संगीत एवं नृत्य तथा लट्ठमार होली।
- हाथी महोत्सव - जयपुर
- अवधि- 1 दिन (मार्च)
- विशेष आकर्षण- सजे हुए हाथियों की परेड और हाथी-मानव रस्साकशी का खेल।
- गणगौर महोत्सव - जयपुर
- अवधि- 18 दिन (मार्च-अप्रैल)
- विशेष आकर्षण- गौरी की मूर्तियों के साथ महिलाओं की शोभायात्रा, संगीत, नृत्य और देवी पार्वती के पारंपरिक अनुष्ठान।
- कार्तिक महोत्सव - अजमेर
- अवधि- 7 दिन (नवंबर)
- विशेष आकर्षण- पुष्कर झील के किनारे धार्मिक अनुष्ठान, पशु मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- बेणेश्वर महोत्सव - डूंगरपुर
- अवधि- 5 दिन (जनवरी-फरवरी)
- विशेष आकर्षण- आदिवासी सांस्कृति का प्रदर्शन, नदियों के संगम पर पूजा और पारंपरिक गीत-नृत्य आदि।
- पतंग महोत्सव - जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर
- अवधि- 1 दिन (14 जनवरी - मकर संक्रांति)
- विशेष आकर्षण- पतंग प्रतियोगिताएं और मकर संक्रांति का उत्सव।
- मेवाड़ महोत्सव - उदयपुर
- अवधि- 3 दिन (मार्च-अप्रैल)
- विशेष आकर्षण- देवी गौरी की शोभायात्रा, लोक-संगीत और नृत्य तथा आतिशबाजी।
- ग्रीष्म महोत्सव - माउंट आबू
- अवधि- 3 दिन (अप्रैल-मई)
- विशेष आकर्षण- लोक एवं शास्त्रीय संगीत, नक्की झील पर नाव-दौड़ और आतिशबाजी।
- मत्स्य महोत्सव - अलवर
- अवधि- 1 दिन (नवंबर)
- विशेष आकर्षण- विभिन्न मछलियों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मछली पकड़ने की प्रतियोगिताएँ।
- अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव - जैसलमेर
- अवधि- 3 दिन (जनवरी-फरवरी)
- विशेष आकर्षण- लोक-संगीत, ऊँट दौड़, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव - बाड़मेर
- अवधि- 4 दिन (फरवरी)
- विशेष आकर्षण- हस्त-शिल्प प्रदर्शनी और थार रेगिस्तान की संस्कृति का उत्सव।
- तीज महोत्सव - जयपुर
- अवधि- 2 दिन (जुलाई-अगस्त)
- विशेष आकर्षण- शोभायात्रा, हरे कपड़े पहनें महिलाएँ, झूले और लोक संगीत-नृत्य आदि।
- कजली तीज - बूंदी
- अवधि- 3 दिन (जुलाई-अगस्त)
- विशेष आकर्षण- लोकगीत-संगीत और नृत्य।
- बैलून महोत्सव - बाड़मेर
- अवधि- 2 दिन (फरवरी)
- विशेष आकर्षण- हॉट एयर बैलून की सवारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- शरदकालीन महोत्सव - माउंट आबू
- अवधि- 3 दिन (दिसंबर)
- विशेष आकर्षण- सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक संगीत-नृत्य और स्थानीय संस्कृति का उत्सव।
- शेखावाटी महोत्सव - सीकर, झुन्झुनू
- अवधि- 4 दिन (फरवरी)
- विशेष आकर्षण- सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा शेखावाटी की कला और वास्तुकला की प्रदर्शनी।
- जौहर मेला - चित्तौड़गढ़
- अवधि- 1 दिन (फरवरी)
- विशेष आकर्षण- राजपूत महिलाओं की वीरता का स्मरण और सांस्कृतिक प्रदर्शन।
- धुलंडी महोत्सव - जयपुर
- अवधि- 1 दिन (मार्च - होली)
- विशेष आकर्षण- होली का रंग-बिरंगा उत्सव, संगीत, नृत्य और हर्षोल्लास।
- राजस्थान समारोह - जयपुर
- अवधि- 3 दिन (मार्च)
- विशेष आकर्षण- भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य और राजस्थान की विरासत की प्रदर्शनी।
- आभानेरी महोत्सव - दौसा
- अवधि- 2 दिन (सितंबर-अक्टूबर)
- विशेष आकर्षण- आभानेरी बावड़ी की सुंदर पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक प्रदर्शनी तथा पारंपरिक शिल्प-कला का प्रदर्शन।
- राकेश शर्मा- भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री
- परिचय- भारतीय वायु सेना के पायलट राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने।
- मिशन- उन्होंने सोवियत अंतरिक्ष यान सोयुज टी-11 में इंटरकॉसमोस कार्यक्रम के तहत उड़ान भरी थी।
- उपलब्धि- सैल्यूट 7 (Salyut 7) अंतरिक्ष स्टेशन पर आठ दिन के मिशन के दौरान उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किये। इंदिरा गांधी के सवाल "अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है?" पर उनका उत्तर, "सारे जहां से अच्छा" बहुत प्रसिद्ध हुआ था।
- कल्पना चावला- भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री
- परिचय- हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता ली और NASA में शामिल हुईं।
- मिशन- चावला ने 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया (STS-87) में अपना पहला मिशन पूरा किया। उनका दूसरा मिशन STS-107 दुखद रूप से उनका आखिरी मिशन साबित हुआ।
- विरासत- 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। चावला को महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिये एक पथप्रदर्शक एवं प्रेरणा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
- सुनीता विलियम्स- रिकॉर्ड बनाने वाली अंतरिक्ष यात्री
- परिचय- ओहियो में एक भारतीय पिता और स्लोवेनियाई मां के घर जन्मी सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी और NASA की अंतरिक्ष यात्री हैं।
- मिशन- विलियम्स ने 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी (STS-116) और 2012 में रूसी सोयुज (Soyuz) अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी।
- उपलब्धि- उन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने (195 दिन) और सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में चलने (7 बार) का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। भविष्य में गगनयान आदि मिशन अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करेंगे।
राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विविधता एवं शुष्क जलवायु के लिये जाना जाता है। राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर को चार प्रमुख प्रतीक व्यक्त करते हैं- राज्य का पुष्प, वृक्ष, पक्षी एवं पशु।
- राज्य पुष्प- राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिडा (Tecomella undulata) है। थार मरुस्थल में पाए जाने के कारण इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। यह राजस्थान की गर्म तथा शुष्क जलवायु के अनुकूल होता है। रोहिडा गर्मियों में पीले रंग के सुंदर फूल देता है। इसे राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था।
- राज्य वृक्ष- खेजड़ी (Prosopis cineraria) राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे रेगिस्तान का गौरव अथवा थार का कल्पवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राज्य में खेजड़ी वृक्षों के प्रति जागरूकता हेतु खेजडली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बीज और पत्ते पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों में उपयोग किये जाते हैं।
- राज्य पक्षी- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान सरकार द्वारा इसे वर्ष 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया। यह एक शर्मीला पक्षी तथा स्थानीय लोग इसे सोन पक्षी के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके आवास में कमी और शिकार के कारण इसकी संख्या में काफी गिरावट आई है तथापि इसके संरक्षण के लिए प्रयास चल रहे हैं।
- राज्य पशु- राजस्थान के दो राज्य पशु हैं- चिंकारा और ऊँट। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1981 में चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया था। यह ‘एंटीलोप’ प्रजाति का मुख्य जीव है, जिसे छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2014 में राज्य सरकार द्वारा ऊँट (Camelus dromedarius) के संरक्षण हेतु ऊँट को भी राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया। इसे "रेगिस्तान का जहाज" कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तानी पर्यावरण के लिये पूरी तरह से उपयुक्त है। ऊंट राजस्थान के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो परिवहन, कृषि और दूध के लिये उपयोग होता है। यह पारंपरिक रेगिस्तानी जीवनशैली और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है।
ये प्रतीक राजस्थान की वनस्पति और जीवों की सहनशीलता एवं अनुकूलता को दर्शाते हैं तथा राज्य के अनूठे पर्यावरण व सांस्कृतिक परिदृश्य को व्यक्त करते हैं।
- लिखित गणित और मौखिक गणित एक-दूसरे के पूरक हैं। मौखिक गणित की अपनी सीमाएँ हैं। जब प्रश्न कठिन होते हैं तो उनकी संक्रियाएँ मौखिक रूप से करना असंभव हो जाता है तब लिखित गणित की मदद से उन्हें हल किया जाता है। जब विद्यार्थी समस्याओं को कागज, पेन या पेंसिल के माध्यम से लिखकर हल करता है तो हम उसे लिखित गणित कहते हैं। लिखित गणित को हल करने से मस्तिष्क को कम परिश्रम करना पड़ता है तथा समस्या का हल शीघ्रता से निकाला जा सकता है।
- सीखे हुए नियमों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों, संबंधों, प्रक्रियाओं तथा तथ्यों का अभ्यास करने के लिये लिखित गणित आवश्यक है। लिखित गणित का अभ्यास तभी करना चाहिये जब विद्यार्थियों को आधारभूत सिद्धांतों का स्पष्टीकरण भलीभांति हो जाए। लिखित गणित करने में मानसिक तथा मौखिक गणित का उपयोग आवश्यक होता है। प्रत्येक साधारण बात को लिखकर करने से लिखित गणित का महत्त्व नहीं रह जाता है। लिखित गणित करते समय विद्यार्थियों को सावधानीपूर्वक एकाग्रचित्त होकर व्यक्तिगत कोशिश करने के अवसर प्राप्त होते हैं। समस्याओं के सही हल ज्ञात करने से विद्यार्थी में आत्मविश्वास का विकास होता है और विद्यार्थी कठिनतम समस्याओं का हल आसानी से निकालने लगते हैं।
लिखित गणित के लाभ
- लिखित गणित में विद्यार्थी अपनी तर्कशक्ति एवं रचनात्मक कल्पना का अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं।
- लिखित गणित द्वारा विद्यार्थियों में गति के साथ शुद्धता से काम करने की भावना का विकास होता है।
- किसी समय को निर्धारित समय में करने की क्षमता लिखित गणित के द्वारा ही विकसित हो सकती है।
- लिखित गणित से विद्यार्थियों में विषय-सामग्री प्रस्तुत करने की शैली का विकास होता है।
- गृह-कार्य कराने का उपयोगी माध्यम लिखित गणित ही है।
- लिखित गणित द्वारा विद्यार्थियों के विचारों में क्रमबद्धता तथा तर्क का सही रूप प्रत्यक्ष में आता है।
- लंबी तथा बड़ी गणना के लिये लिखित कार्य आवश्यक है। लिखित कार्य में विद्यार्थियों को सूत्रों, विधियों आदि के प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं।
- लिखित गणित के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकता है।
मौखिक गणित
गणित में मौखित कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं परंतु अफ़सोस की बात यह है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति में मौखिक गणित तथा मौखिक कार्य को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। ज्यादातर विद्यार्थियों का गणित में कमज़ोर होने का कारण मौखिक गणित का उचित प्रयोग भी न करना है। मौखिक गणित को गणित के अध्यापन में गौण स्थान दिया जाता है लेकिन मौखिक गणित न करने से गणित के लिखित कार्यों में भी त्रुटियाँ होती हैं।
मौखिक गणित के लाभ
मौखिक गणित के महत्त्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं-
- सामूहिक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये मौखिक गणित का उपयोग लाभकारी होता है।
- मौखिक गणित से विद्यार्थियों की योग्यता आसानी से जांची-परखी जा सकती है।
- मौखिक गणित का उपयोग गणित के आधारभूत सिद्धांतों, नियमों आदि के अभ्यास में अत्यंत सहायक होता है।
- मौखिक गणित की सहायता से पाठ की पुनरावृत्ति शीघ्रता से की जा सकती है।
- मौखिक गणित से विद्यार्थियों में गणना प्रक्रियाओं में परिशुद्धता आती है।
- मौखिक गणित द्वारा विद्यार्थियों के सोचने के तरीकों में संकोच या घबराहट को दूर किया जा सकता है।
- मौखिक गणित के उपयोग से गणना करने में समय की बचत होती है तथा विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की जाँच कर स्वयं ही ठीक करते हैं।
- मौखिक गणित से विद्यार्थियों में समस्याओं को हल करने के लिये आवश्यक यांत्रिक कुशलता का विकास होता है।
- गणित के सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं को मौखिक गणित द्वारा समझाकर धारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है।
- प्रमुख भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं लेखक चॉमस्की का जन्म 7 दिसंबर, 1928 को अमेरिका में हुआ था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के सम्मानित प्रोफेसर और मैसाच्युसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं।
- चॉमस्कीय भाषा विज्ञान का आरंभ उनकी पुस्तक Syntactic Structures से माना जाता है जो उनके पीएचडी शोध, The Logical Structure of Linguistic Theory, का परिष्कृत रूप था।
- इस पुस्तक के द्वारा चॉमस्की ने पूर्व स्थापित संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों की मान्यताओं को चुनौती देकर Transformational Grammar की बुनियाद रखी।
- इस व्याकरण ने स्थापित किया कि शब्दों के समुच्चय का अपना व्याकरण होता है, जिसे औपचारिक व्याकरण द्वारा निरुपित किया जा सकता है।
- चॉमस्की ने अपने Principles and Parameters का मॉडल अपने पीसा के व्याख्यान के बाद विकसित किया जो बाद में Lectures on Government and Binding के नाम से प्रकाशित हुई।
- इसमें चॉमस्की ने सार्वभौम व्याकरण के बारे में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किये हैं।
चॉमस्की के अधिगम संबंधित सिद्धांत से जुड़े महत्त्वपूर्ण तथ्य को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है-
- उन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात (आनुवंशिक रूप से) खाका होता है जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई।
- मानव भाषा का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू सृजनात्मकता है।
- चॉमस्की के अनुसार एक साधारण या औसत स्तर का बच्चा भी भाषा के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकता है।
- कोई बच्चा सिर्फ भाषा को वाणी द्वारा सीमित मात्रा में ही सुनता है और उनमें से कुछ वाक्यांश भलीभांति संरचित भी नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी बच्चे के अंदर असीमित वाक्यों के निर्माण की संरचना विकसित हो जाती है।
- मनुष्य के अंदर भाषा का विकास पूर्ण रूप से उसकी आनुवंशिक पूँजी का ही प्रतिफलन होता है।
- मनुष्य मस्तिष्क जन्म के समय एक कोरे स्लेट की भांति नहीं होता है बल्कि मनुष्य की आनुवंशिक पूंजी बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करके भाषा तथा अन्य विकास को गति प्रदान करती है।
- चॉमस्की के अनुसार हम उन सही वाक्यों का असीमित निर्माण कर सकते हैं जिनका निर्माण अभी तक नहीं हुआ हो।
इस प्रकार एक शिक्षक के लिये अपने विद्यार्थी की भाषा के विकास के लिये चॉमस्की का भाषा अधिगम सिद्धांत को समझना अत्यावश्यक है।
- जलमार्ग किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात परिवहन है। भारत में आंतरिक एवं सामुद्रिक दोनों प्रकार का जल परिवहन किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीनकाल से ही नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता है।
- भारत में नदियों, नहरों, बांधों तथा सँकरी खाड़ियों के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक विस्तारित नेटवर्क है। 20236 किमी. की कुल नौचालनीय लंबाई में से नदियों का 17980 किमी. तथा नहरों का 2256 किमी. यांत्रिक जहाज़ों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत देश में कुल 106 जलमार्गों को नए राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इस अधिनियम के कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 हो जाएगी।
- इस समय गंगा-हुगली नदी के कुछ हिस्सों, ब्रह्मपुत्र-बराक नदी, गोवा की नदियाँ, केरल के अप्रवाही जल और गोदावरी-कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों तक नौ-संचालन सीमित है।
- यांत्रिक जहाज़ों की संगठित माल ढुलाई के अतिरिक्त विभिन्न क्षमता वाली देशी नौकाएँ भी विभिन्न नदियों व नहरों से माल ढुलाई कर रही हैं।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 में की गई एवं इसे राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रख-रखाव और नियमन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
आंतरिक जलमार्गों के प्रमुख लाभ-
- आंतरिक जलमार्ग ईंधन प्रभावी, लागत प्रभावी तथा पर्यावरण हितैषी के रूप में परिवहन के एक साधन के रूप में है।
- आंतरिक जलमार्ग परिवहन के सस्ते साधन को उपलब्ध कराने के साथ यातायात के दबाव को कम करेगा तथा रेल व सड़क परिवहन की भीड़भाड़ को कम करेगा।
- आंतरिक जलमार्ग वस्तुओं की परिवहन लागत में कमी करने के साथ बाज़ार में वस्तुओं की कीमत कम करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।
आंतरिक जलमार्गों की प्रमुख समस्याएँ-
- ग्रीष्मकाल में नदियों में जल की मात्रा कम होने से जहाज़ या स्टीमर चलाने के लिये प्रतिकूल स्थिति होती है।
- प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पठारी व ऊबड़-खाबड़ भूमि होने के कारण परिवहन योग्य नहीं होती हैं।
- अंतर्राज्यीय जल विवाद भी एक समस्या है।
भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी यात्रियों के यात्रा-वृत्तांतों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और इसके विषय में विवरण दिया। ऐसे ही कुछ यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है-
- मेगस्थनीज : यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। इसने ‘इंडिका’ नामक पुस्तक की रचना थी जिसमें इन्होंने भारतीय समाज के विषय में बताया है। मेगस्थनीज यूनानी यात्री था।
- फाहियान : यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के दरबार में आया तथा यह एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। फाहियान ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया था।
- ह्वेनसांग : यह 7वीं सदी में हर्षवर्द्धन के समय में आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया। यह चीनी मूल का बौद्ध भिक्षुक था। इसकी पुस्तक का नाम सी-यू-की है। इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है।
- अलबरूनी : यह 11वीं सदी में महमूद गज़नवी के साथ भारत आया तथा यह मूल रूप से उज्बेकिस्तान का निवासी था। इसकी प्रमुख कृति में तहकीक-ए-हिंद/किताब-उल-हिंद सम्मिलित हैं। अपनी पुस्तक में इन्होंने भारत के तालाबों के विषय में विशेष रूप से बताया है।
- इब्न बतूता : यह मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। इसे तुगलक ने दिल्ली के काज़ी के पद पर नियुक्त किया। इसके द्वारा लिखा गया यात्र-वृत्तांत ‘रेहला’ सर्वप्रमुख है जो अरबी भाषा में रचित है। इसमें भारतीयों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है।
- वास्को-डी-गामा : यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 ई. में भारत की धरती पर नए समुद्री मार्ग के द्वारा कदम रखा।
पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ (Meaning of Environmental Education)-
- पर्यावरणीय शिक्षा का सरल अर्थ है वह शिक्षा, जो हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन और सुधार की शिक्षा प्रदान करती है। मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने की बजाय उसका संरक्षण करे, यही संचेतना हमें पर्यावरणीय शिक्षा से मिलती है। पर्यावरणीय शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध कराती है और भविष्य में सावधान रहने के लिये मानव को तैयार करती है। पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है।
- इसमें पर्यावरण के विभिन्न पक्षों व घटकों का मानव के साथ अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा में जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले घटकों की भी जानकारी मिलती है।
पर्यावरणीय शिक्षा के प्रकार (Types of Environmental Education)-
- औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा- औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा में प्रशिक्षण के पात्र विद्यार्थी, कार्यरत कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरण के प्रति अभिरुचि रखने वाले पढ़े-लिखे लोग होते हैं।
- अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा- अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा मुख्यत: अनपढ़ लोगों को प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों के अतिरिक्त कम पढ़े-लिखे और काम-धंधों में लगे लोगों को भी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ग के लिये विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनपढ़ होने के कारण इन्हें ऐसे तरीकों से शिक्षित किया जाता है ताकि वे पर्यावरण के विविध पक्षों को समझ सकें।
पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Environmental Education)-
पर्यावरणीय शिक्षा का मूल उद्देश्य ऐसे समाज की रचना है जो प्रकृति और जीवों के अंतर्संबंधों की सही जानकारी रखता है तथा अपने आचरण को प्राकृतिक नियमों के अनुसार समायोजित कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके लिये पर्यावरण को संपूर्ण रूप में देखते हुए निर्णय लेने की क्षमता पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। इसलिये पर्यावरणीय शिक्षा से जागरूकता, सज्ञानता, अभिवृद्धि, कौशल, मूल्यांकन, कुशलता और सहभागिता की भावना विकसित होती है।
तरुण भारत संघ सतत् विकास उपायों के माध्यम से राष्ट्र के एक निराश्रित वर्ग के जीवन में गरिमा और समृद्धि लाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति, जाति या धर्म की परवाह किये बिना पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिये है। यह प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय-संचालित-विकेंद्रीकृत-प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
- तरुण भारत संघ (TBS) भारत का एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है। इसकी स्थापना 30 मई, 1975 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय राजस्थान के अलवर के भीकमपुरा में है।
- यह संगठन लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिये पारिस्थितिक अनुसंधान और भूमि विकास करने के लिये जाना जाता है।
- वे पुरानी झीलों और जोहड़ों का पुनर्निर्माण करते हैं तथा नई बावड़ियों को बनाने का कार्य करते हैं।
- इसके संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं जिन्हें ‘जल पुरुष’ के नाम से भी जाना जाता है।
उद्देश्य-
यह संस्था समुदायों के सशक्तिकरण के लिये काम कर रही है; ध्येयवाक्य : ग्राम स्वराज्य- ग्राम स्वशासन में विश्वास
- कल्याणकारी कार्यों में उदाहरण स्थापित करके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विस्तार या बहाली करना।
- मानव और प्राकृतिक संसाधन विकास के बीच संतुलन ढूंढ़ना।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- समाज में शिक्षा के स्तर में सुधार।
- स्वस्थ बनाने के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करना।
- मूल्य-आधारित कार्य के लिये ऊर्जा का दोहन करने के लिये मानव शक्ति, विशेष रूप से युवा शक्ति को सक्रिय करना।
वायु परिवहन, परिवहन का नवीनतम एवं सर्वाधिक तीव्र साधन है। भारत जैसे विशाल देश में वायु परिवहन का काफी महत्त्व है। भारत के आर्थिक विकास में मदद के अलावा इससे युद्ध काल में शत्रुओं से सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों तक शीघ्र सहायता पहुँचाने में सुविधा होती है।
- स्वतंत्रता के बाद भारत में 21 वायु परिवहन कंपनियाँ स्थापित हो चुकी हैं।
- भारत में वायु परिवहन के विकास का इतिहास 1911 ई. से प्रारंभ होता है, जब इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा प्रारंभ हुई। वर्ष 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज़ की स्थापना हुई।
- हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये DGCA ने मंज़ूरी प्रदान की है। इस प्रकार कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है।
- पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा वर्ष 1933 में कराची एवं लाहौर के बीच इंडियन नेशनल एयरवेज़ ने प्रारंभ की।
- 1935 में टाटा एयरवेज़ द्वारा मुंबई-तिरुवनंतपुरम (तत्कालीन त्रिवेंद्रम) तथा 1937 में मुंबई-दिल्ली मार्ग पर विमान सेवा की शुरुआत हुई।
- वर्ष 1953 में सभी विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन कर दिया गया।
- राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन दो निगमों- एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएँ देनी शुरू कर दी हैं।
- विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला अमेरिका करता है।
- भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 में की गई, जब भाप के इंजन द्वारा मुंबई से थाणे के मध्य पहली रेल चलाई गई थी।
- वर्तमान में भारत में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है।
- भारतीय रेल के पास 9213 रेल इंजन, 53220 यात्री गाड़ियाँ, 6493 अन्य सवारी गाड़ियाँ और 219381 रेल डिब्बे हैं।
- रेलवे ने 160 वर्षों की अवधि में असाधारण प्रगति की है।
- भारतीय रेलवे ने देश के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारतीय रेलवे एक मल्टी गेज प्रणाली है।
- भारतीय रेल की आय के दो मुख्य खंड हैं- माल भाड़ा और यात्री भाड़ा।
- माल भाड़ा खंड लगभग दो-तिहाई राजस्व जुटाता है जबकि शेष यात्री भाड़े से आता है। माल भाड़ा खंड के भीतर थोक यातायात का योगदान लगभग 95% से अधिक कोयले से आता है।
भारत का रेलवे प्रबंधन : ज़ोन (Railway Management of India : Zones)
- प्रशासनिक सुविधा एवं रेलों के परिवहन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय रेल को 17 ज़ोनों में बाँटा गया है।
- भारतीय रेल नेटवर्क का नियंत्रण इसके 17 ज़ोनल कार्यालयों द्वारा किया जाता है।
|
रेलवे मंडल और संभाग |
||
|
रेलवे मंडल का नाम |
मुख्यालय |
संभाग |
|
मध्य रेलवे |
मुंबई |
मुंबई, नागपुर, भुसावल, पुणे, शोलापुर |
|
पूर्वी रेलवे |
कोलकाता |
हावड़ा-I, हावड़ा-II, सियालदह, मालदा, आसनसोल, चितरंजन |
|
पूर्व-मध्य रेलवे |
हाजीपुर |
दानापुर,पं. दीन दयाल उपाध्याय (मुगलसराय), धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर |
|
पूर्व-तटीय रेलवे |
भुवनेश्वर |
खुर्दा रोड, वाल्टेयर, संबलपुर |
|
उत्तरी रेलवे |
नई दिल्ली |
दिल्ली-I, दिल्ली-II, अंबाला, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोज़पुर |
|
उत्तर-मध्य रेलवे |
इलाहाबाद (प्रयागराज) |
इलाहाबाद (प्रयागराज), झाँसी, आगरा |
|
उत्तर-पूर्वी रेलवे |
गोरखपुर |
इज़्ज़तनगर, लखनऊ, वाराणसी |
|
उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे |
मालीगाँव (गुवाहाटी) |
कटिहार, अलीपुरदुआर, रंगिया, लुमडिंग, तिनसुकिया |
|
उत्तर-पश्चिमी रेलवे |
जयपुर |
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर |
|
दक्षिणी रेलवे |
चेन्नई |
चेन्नई, मदुरै, पालघाट, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली |
|
दक्षिण-मध्य रेलवे |
सिकंदराबाद |
सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंतकल, विजयवाड़ा, नांदेड़ |
|
दक्षिण-पूर्वी रेलवे |
कोलकाता |
खड़गपुर, आद्रा, चक्रधरपुर, राँची, शालीमार |
|
दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे |
बिलासपुर |
बिलासपुर, नागपुर, रायपुर |
|
दक्षिण-पश्चिमी रेलवे |
हुबली |
बंगलूरू, मैसूर, हुबली |
|
पश्चिमी रेलवे |
मुंबई |
मुंबई सेंट्रल, वड़ोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, भावनगर |
|
पश्चिमी-मध्य रेलवे |
जबलपुर |
जबलपुर, भोपाल, कोटा |
|
कोलकाता मेट्रो रेलवे |
कोलकाता |
- |
दुनिया भर में विभिन्न स्थानों की यात्रा करके लोगों को दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाज़ों और परंपराओं के बारे में पता चला। उन्होंने बातचीत के दौरान कई चीज़ों का आदान-प्रदान भी किया, जैसे-
- भाषा- लोगों ने एक-दूसरे से भाषा सीखी और इस प्रक्रिया के दौरान एक नई भाषा का जन्म हुआ।
- संस्कृति- एक यात्री यात्रा करते समय अपने रीति-रिवाज़ को दूसरी जगह ले जाता है और यही कारण है कि आपको दुनिया के विभिन्न रीति-रिवाज़ों में कुछ समानताएँ एवं विभिन्नताएँ मिलेंगी।
- नए विचार- जब हम नए लोगों से मिलते हैं और विचारों पर चर्चा करते हैं तो नए विचार पैदा होते हैं। ये नए विचार आविष्कारों की नींव थे और इन विचारों ने मानव के विकास में मदद की।
- परिवहन के मुख्य रूप से तीन प्रकार के साधन हैं- भूमि, जल और वायु परिवहन।
- भूमि परिवहन- इसमें सभी भूमि-आधारित परिवहन प्रणालियाँ शामिल हैं जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिये उपयोग की जाती हैं। यह आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। इसके मुख्य दो प्रकार हैं- सड़क परिवहन और रेल परिवहन।
- वायु परिवहन- यह परिवहन का सबसे नवीनतम एवं सर्वाधिक तीव्र संसाधन है। भारत जैसे विशाल देश में वायु परिवहन का काफी महत्त्व है। इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है।
- जल-मार्ग परिवहन- यह किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात परिवहन है। प्राचीन काल से ही मनुष्य जल परिवहन की दृष्टि से नदियों के माध्यम से यातायात करता रहा है। भारी एवं वृहत् सामानों के परिवहन हेतु यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन है।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में विद्यमान समस्याओं को निम्नलिखित उपायों से दूर किया जा सकता है-
- शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना (Generate Interest Among Learners)- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षार्थियों की रुचि पैदा करके समस्याओं को दूर किया जा सकता है। रुचि पैदा करने के लिये पाठ्यक्रम को रोचक ढंग से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन कर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षार्थियों की रुचि पैदा की जा सकती है।
- पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना (Linking Curriculum to Life)- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण पाठ्यक्रम को अगर आम जनजीवन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाए तो इसके अध्ययन से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, अगर शिक्षार्थियों को पशुपालन के संबंध में पढ़ाना है तो नज़दीक के किसी तबेले का भ्रमण कर शिक्षण कार्य किया जा सकता है।
- रोचक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना (Using Interesting Teaching Aids)- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में रोचक शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके समस्या को दूर किया जा सकता है। रोचक सामग्री के अंतर्गत ग्लोब, मानचित्र, डिजिटल बोर्ड, मार्कर, फूल के गमलों आदि को शामिल किया जा सकता है। इन सबका प्रयोग कर पर्यावरण अध्ययन को आसानी से कक्षा तथा कक्षा के बाहर समझाया जा सकता है।
- कविता और कहानियों का प्रयोग (Use of Poetry and Stories)- कविताएँ और कहानियाँ पढ़ना या सुनना बच्चों को अच्छा लगता है। अगर इनका प्रयोग पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में किया जाए तो यह काफी लाभदायक साबित होगा। इनके माध्यम से जटिल से जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझाया जा सकता है।
- करके सीखने पर बल (Emphasis on Learning by Doing)- पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिये। शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग करेंगे तो उन्हें अधिक सीखने को मिलेगा। पर्यावरण अध्ययन प्रायोगिक कार्यों पर अधिक निर्भर होता है। अगर प्रयोग स्वयं किये जाएँ तो बेहतर परिणाम की कल्पना की जा सकती है।
- शिक्षक का प्रशिक्षण (Teacher Training)- शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान न दिये जाने के कारण पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो सका है। शिक्षकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिये सरकार को आवश्यक तंत्र विकसित करना चाहिये, साथ ही आर्थिक सहयोग देना चाहिये है ताकि शिक्षकों के विषय संबंधी ज्ञान को अद्यतन किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न विषयों की शिक्षक-पुस्तिका के प्रयोग को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक समाज नातेदारी या संबंधों का आधारभूत ढाँचा प्रस्तुत करता है। अपने नाभिकीय (Nuclear) परिवार के बाहर व्यक्ति के द्वितीयक एवं तृतीयक संबंध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी/नातेदार तो उसी नाभिकीय परिवार में पाए जाते हैं। नातेदारी संस्कृति का वह हिस्सा है जो जन्म और विवाह के आधार पर बने संबंधों एवं संबंध की अवधारणाओं और विचारों से संबंधित होता है। नातेदारी संगठन व्यक्तियों के उस समूह को इंगित करता है जो या तो एक-दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं या वैवाहिक संबंधी होते हैं।
- जी. इंकन मिचेल के अनुसार, “जब हम नातेदारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों को संदर्भित कर रहे हैं।” रक्त संबंधियों में सामान्यत: उन्हें शमिल किया जाता है जिनके बीच सामूहिक रूप से तथाकथित रक्त संबंध पाया जाता है।
- रक्त संबंधी संबंध का आशय यह है कि जिसका या तो उस परिवार में जन्म हुआ है या उसे परिवार द्वारा गोद लिया गया है। जबकि विवाह संबंधी उसे कहते हैं जिसके संबंध का माध्यम विवाह हो। उदाहरण के लिये, पिता-पुत्र संबंध एक रक्त संबंध है, जबकि पति-पत्नी संबंध एक विवाह संबंध है।
- नातेदारी दो महत्त्वपूर्ण एवं संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करता है-
- यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रस्थिति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति के हस्तांतरण को संभव बनाता है।
- कुछ समाजों में यह प्रभावी सामाजिक समूह के निर्माण को कायम रखने में प्रभावी होता है।
- नातेदारी व्यवस्था परिवार एवं विवाह जैसी दो जुड़ी संस्थाओं का प्रतिफल है और यह जन्म, मृत्यु एवं पुरुष-स्त्री के शारीरिक संबंध से जुड़े सामाजिक व्यवहार का नियमन करता है।
- नातेदारी एक-दूसरे के प्रति अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में और एक-दूसरे की अभिरुचियों एवं अपेक्षाओं के बारे में बतलाता है।
- ज़्यादातर समाजों में जहाँ नातेदारी संबंध महत्त्वपूर्ण होते हैं वहाँ वंशावली तय करने के स्पष्ट नियम होते हैं और वंश कई पीढ़ियों के लोगों को जोड़ता है।
- वंशावली के आधार पर यह बतलाया जा सकता है कि किस व्यक्ति की उत्पत्ति किस व्यक्ति से हुई है। वंशावली तय करने के कई तरीके हैं-
- एकपक्षीय वंश- माता-पिता में से जब केवल एक पक्ष को ही वंशावली में गिनने की प्रथा हो तो उसे एकपक्षीय वंश कहते हैं। इसके भी दो रूप हैं-
- पितृवंशीय- इसमें वंश का निर्धारण केवल पिता या दादा जैसे पुरुष संबंधियों से संबंध स्थापित करके किया जाता है। ध्यातव्य है कि पितृवंश में पुत्रों के साथ-साथ पुत्रियों की गिनती भी की जाती है और वंश पिता या दादा के नाम से जाना जाता है।
- मातृवंशीय- इसमें वंश का निर्धारण माँ या नानी जैसी स्त्री संबंधियों के साथ संबध स्थापित करके किया जाता है मातृवंश में पुत्रियों के साथ पुत्र की गिनती भी की जाती है वंश माता या नानी के नाम से जाना जाता है।
- द्विवंशीय- यह भी एकपक्षीय वंश का ही एक रूप है जिसमें मातृवंशीय एवं पितृवंशीय के गुण मिले रहते हैं। वंशावली का निर्धारण पिता या माता के एक ही पक्ष के आधार पर किया जाता है, परंतु अलग-अलग उद्देश्यों के लिये अलग-अलग वंशावली तैयार की जाती है। उदाहरण के लिये, अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिये एक पक्ष (पिता) एवं चल संपत्ति के हस्तांतरण के लिये दूसरे पक्ष (माता) के साथ संबंध स्थापित कर वंशावली तैयार की जाती है।
- एकपक्षीय वंश- माता-पिता में से जब केवल एक पक्ष को ही वंशावली में गिनने की प्रथा हो तो उसे एकपक्षीय वंश कहते हैं। इसके भी दो रूप हैं-
- द्विपक्षीय वंश- यह एकपक्षीय वंश नहीं होकर द्विपक्षीय वंश होता है। इसमें एक ही साथ माता और पिता, पुरुष पूर्वज एवं स्त्री पूर्वज दोनों की तरफ से (एक साथ, एक ही उद्देश्य के लिये) वंशावली तैयार की जाती है।
- भारत में सामान्यत: पितृवंशीय एवं मातृवंशीय दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं।
- उत्तर भारत में पितृवंशीय व्यवस्था ज़्यादा पाई जाती है।
- जनजातियों में संथाल एवं मुंडा जैसी जनजातियाँ पितृवंशीय हैं। बहुपति विवाह के रिवाज़ को मानने वाले टोडा लोग भी पितृवंशीय हैं।
- जनजातियों में उत्तर-पूर्व के खासी तथा गारो लोग मातृवंशीय व्यवस्था मानते हैं।
- केरल की नायर जाति मातृवंशीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है।
- एकपक्षीय वंश समूह को गोत्र या कुल कहा जाता है।
- गोत्र या वंश नातेदारों का ऐसा समूह है, जिसमें सभी पूर्वजों के साथ सात कड़ियों के आधार पर वंशानुगत संबंध स्थापित किया जाता है।
- एक कुल कई वंशों के मिलने से बनता है।
- कुल नातेदारों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामूहिक रूप से एक साझे पूर्वज से अपने को जोड़ते हैं, परंतु वे ज्ञात वंशावली के आधार पर उस पूर्वज से संबंध नहीं जोड़ पाते।
- एकपक्षीय वंश समूह के सदस्य सामान्यत: कर्मकाण्ड तथा आनुष्ठानिक उत्सवों के अवसर पर साथ-साथ उपस्थित होते हैं।
- उत्तराधिकार के नियम अधिकांशत: वंशावली द्वारा नियमित होते हैं।
- भारत के अधिकांश भाग में अभी हाल तक ज़मीन एवं घर जैसी अचल संपत्ति नज़दीकी पुरुष संबंधियों को हस्तांतरित होती थी।
- हालिया कानूनी विधेयकों ने पिता की संपत्ति में पुत्री को भी अधिकार प्रदान किया है।
- ज्ञात है कि शुरुआती वर्षों में पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के आधार के रूप में देखा गया। इस दौरान इसके पाठ्यक्रम में आगे आने वाले वर्षों/कक्षाओं की विषयवस्तु व अवधारणाओं की आधारभूत समझ को बनाने का उद्देश्य प्रस्तावित था।
- इस पाठ्यक्रम व इसके आधार पर बनी पाठ्यपुस्तकों से ये अपेक्षाएँ थीं कि वे आगे आने वाली कक्षाओं की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं को सरलीकृत रूप में प्राथमिक कक्षाओं में प्रस्तुत करें ताकि बच्चे आगे जाकर इनकी गहरी समझ विकसित कर पाएँ।
- विभिन्न शोधों से यह बात सामने आई है कि इन अवधारणाओं को समझने के लिये प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे संज्ञानात्मक स्तर पर तैयार नहीं होते हैं। साथ ही, केवल परिभाषाएँ या नामों का ज़िक्र कर देने से उस अवधारणा की समझ बन जाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा करने से बच्चे उन नामों को तो जानते हैं पर उनसे जुड़ी अवधारणाओं को समझ नहीं पाते हैं। यह तरीका बच्चों के लिये बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हो पाया है।
- पर्यावरण अध्ययन को घटकों में बाँटकर देखने की अप्रोच को दरकिनार कर एकीकृत स्वरूप को अपनाने का आधार ‘‘बाल केंद्रित दृष्टिकोण’’ है। अर्थात् पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में बाँटकर देखने का नज़रिया विषय-विशेषज्ञों की सोच से प्रभावित है।
- यदि हम बच्चों के दुनिया को देखने के नज़रिये की बात करें तो वह बिल्कुल अलग है। हम पाते हैं कि वे अपने आसपास की दुनिया को समग्र रूप में देखते हैं न कि विषयों की सीमाओं में तोड़कर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं।
- वर्तमान में NCF 2005 की सोच से प्रभावित होकर प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत स्वरूप को अपनाया गया है। अत: इनमें अवधारणाओं के नामों की सूची की बजाय प्रकरण को प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि यात्रा, आवास, भोजन, परिवार एवं मित्र आदि। प्रकरण एक समग्र समझ को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत विषयों की पारंपरिक सीमाओं को नज़रअंदाज़ कर साझे रूप में बच्चे के लिये प्राथमिकताओं को तय किया जाता है।
बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु व खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। वे निरंतर अपने आसपास की दुनिया से अंत:क्रिया करते रहते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका सोचने का दायरा व्यापक होता जाता है और उनके अनुभवों में गहराई आती है। अत: एक शिक्षक का यह दायित्व बन जाता है कि वह बच्चों के इन अनुभवों को और विस्तार प्रदान करे ताकि बच्चे अपनी वर्तमान समझ को व्यवस्थित कर पाएँ। उचित मार्गदर्शन की सहायता से समझ के दायरे को बढ़ाकर दुनिया में अपना अस्तित्व बना पाएँ। इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं-
- बच्चों को दक्ष बनाना ताकि वे प्राकृतिक व सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के बीच के अंतर्संबंध को समझ पाएँ। इसके साथ ही अपने शब्दों में इन अंतर्संबंधों की व्याख्या भी कर पाएँ।
- अमूर्त उदाहरणों की बजाय दैनिक जीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक व जीव जगत से जुड़े अनुभवों के अवलोकन और चित्रण की सहायता से बच्चों में समझ विकसित करना।
- प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी बच्चों की जिज्ञासा व सृजनात्मकता का पोषण करना। यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मनुष्य व मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएँ भी शामिल हैं।
- बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और संरक्षण के प्रति सजग बनाना तथा पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना।
- बच्चों को हाथ से की जाने वाली व विश्लेषणात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना ताकि उनमें मूलभूत संज्ञानात्मक व मनोगत्यात्मक कौशलों, यथा- वर्गीकरण, अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, तुलना आदि का विकास हो सके।
- बच्चों में खोजी एवं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना।
- राष्ट्रीय प्रतीकों, संस्थानों और संस्कृति के प्रति आदर का भाव विकसित करना।
- संसाधनयुक्त व संज्ञानात्मक क्षमता के विकास के लिये माहौल तैयार करना ताकि बच्चों को सामाजिक परिघटनाओं के लिये उत्सुक बनाया जा सके। उदाहरणार्थ, पहले बच्चे परिवार के बारे में जानें व समझें, फिर इस सामाजिक समझ का दायरा और व्यापक किया जाए।
- पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। विगत वर्षों में इसका विकास विज्ञान के विषय के रूप में हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों के विषय समाहित हैं।
- पर्यावरण सभी स्तर के जीवधारियों से मिलकर बनता है। हम सभी अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिये अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर हैं। यही कारण है कि पर्यावरणीय मुद्दों, जैसे- ग्लोबल वार्मिंग, ओज़ोन परत का ह्रास, घटते जंगल, ऊर्जा संसाधनों की कमी, वैश्विक जैव-विविधता का नुकसान आदि से हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जल, वायु, भूमि, मिट्टी और जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह हमें सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिये मानक स्थापित करने में मदद करता है। यह अन्य मुद्दों, जैसे- स्वच्छ पेयजल, रहने की आदर्श स्थिति, स्वच्छ एवं ताज़ी हवा, उर्वर भूमि और विकास आदि के विषय में जागरूकता उत्पन्न करता है।
- वास्तव में हमारा पर्यावरण कई अलग-अलग वातावरणों से बना है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, मानव निर्मित और सांस्कृतिक वातावरण शामिल हैं। यही कारण है कि पर्यावरण को एक जटिल संरचना माना जाता है।
- पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान, भू-विज्ञान, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों का एक अंतरानुशासनिक संयोग है जो प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभावों का अध्ययन करता है। यह विषय अध्येताओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की जटिलताओं को समझने में मदद करता है।
- जैसे यदि हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वायु प्रदूषण की अभिक्रिया एवं उसकी प्रकृति रसायन विज्ञान तथा रासायनिक अभियांत्रिकी (केमिकल इंजीनियरिंग) से संबंधित है। मानवों तथा अन्य जीवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है।
- पदार्थों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। मौसम पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन मौसम विज्ञान, भूगोल तथा ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण से निपटने वाले यंत्रों का अध्ययन भौतिक, अभियांत्रिकी तथा रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
- वायु प्रदूषण के इतिहास का अध्ययन इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण के आर्थिक तथा सामाजिक दुष्प्रभावों का अध्ययन क्रमश: अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में किया जाता है। वायु प्रदूषण से निपटने की नीतियों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
अर्थ (Meaning)-
- पर्यावरण अध्ययन प्रकृति पर मानवीय अंत:क्रिया के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के चारों ओर के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक घेरे में संपन्न होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं, परिवर्तनों, अंत:क्रियाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन कहलाता है।
- ध्यातव्य है कि पर्यावरण अध्ययन का विकास विभिन्न विषयों के समेकित रूप से हुआ है। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के समेकित रूप को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा जाता है।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 के अनुसार, ‘‘विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में समाहित करना चाहिये, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इतना ही नहीं, यह विषय तो भाषा, गणित, कला आदि का भी कुछ पुट लिये रहता है।’’
- वस्तुत: पर्यावरण अध्ययन विषयगत सीमांकन से लगभग मुक्त विषय है। परिवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव तथा परिवेश को समझे जाने वाले तरीकों का अध्ययन इसकी मुख्य विषयवस्तु है।
- बाल्यावस्था से ही बच्चे अपने परिवेश के प्रति सचेत होते हैं। वे चीज़ों व घटनाओं को अलग-अलग या टुकड़ों में देखने के विपरीत संपूर्णता के साथ देखते व महसूस करते हैं। उनके अपने बोध में उनका संपूर्ण परिवेश होता है। अतएव प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के विषयगत द्वंद्व में उलझे बिना समेकित रूप से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण पर बल दिया जाता है।
- पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बच्चे अपने पर्यावरण को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही उन कौशलों को भी सीखते हैं जिनसे पर्यावरण को जाना-समझा जा सके।
परिभाषाएँ (Definitions)-
- स्वान के अनुसार, ‘‘पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा यह है कि ऐसी सद्नागरिकता का विकास किया जाए जो पर्यावरण एवं उससे जुड़ी हुई समस्याओं से परिचित हो। इन समस्याओं के समाधान के लिये अपनी भागीदारी के अवसरों की जानकारी रखती हो तथा इसके लिये आत्मप्रेरित भी हो। अर्थात् पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण अध्ययन है।’’
- ए.बी. सक्सेना के अनुसार, ‘‘पर्यावरण अध्ययन वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में हमें संचेतना, ज्ञान और समझ देती है, इसके बारे में अनुकूल दृष्टिकोण का विकास करती है और साथ ही इसके संरक्षण तथा सुधार की दिशा में हमें प्रतिबद्ध करती है।’’
- चौबर डिक्शनरी के अनुसार, ‘‘पारिस्थितिकी एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों तथा मनुष्य-समुदायों के अपने वातावरण के साथ अंतर्संबंधों को व्याख्यायित किया जाता है। पर्यावरण के साथ जीवधारियों का जो भी आदान-प्रदान होता है, जो भी अंत: क्रियाएँ होती हैं तथा अंतर्संबंध बनते हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही पर्यावरण अध्ययन है।’’
एक शिक्षक के रूप में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है। वैसे भी उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति का निर्धारण और मूल्यांकन किया ही जाना चाहिये। मूल्यांकन से अभिप्राय विद्यार्थी के संपूर्ण मूल्यांकन से होता है, जिसमें व्यक्ति की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का मूल्यांकन भी निहित होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं-
- शारीरिक विकास का मूल्यांकन : शारीरिक विकास से अर्थ विद्यार्थी के स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन से है। अत: विद्यार्थी के उचित मानसिक विकास के लिये उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिये। शारीरिक विकास के मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी का समय-समय पर अच्छे चिकित्सक द्वारा परीक्षण भी होना चाहिये और किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष को दूर करने हेतु सही समय पर चिकित्सक की राय लेनी चाहिये। अगर किसी विद्यार्थी में कोई असामान्यता हो तो उसके अभिभावक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिये जिससे माता-पिता अपने बच्चे का उचित समय पर उपचार करा सकते हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन : मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मस्तिष्क को स्वस्थ तथा निरोग रखने से है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करके उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन के लिये समर्थ बनाता है। अत: शिक्षक को विद्यार्थियों में भय, चिंता, निराशा, कुंठा तथा अन्य मानसिक विकृतियों को दूर कर उनके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिये।
- सामाजिक विकास का मूल्यांकन : विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षकों तथा अनेक अन्य विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं और अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी में सहभागिता, सहानुभूति, सहयोग तथा अनुशासन जैसी क्षमताओं का विकास होता है, जो उन्हें एक कुशल सामाजिक प्राणी बनाता है। अत: विद्यालय का यह कार्य भी है कि वह विद्यार्थियों में इन क्षमताओं के विकास के साथ उनका मूल्यांकन भी करे जिससे यह विदित हो कि विद्यार्थियों में किस प्रकार के सामाजिक विकास वांछनीय हैं।
- व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन : व्यक्तित्व के अंतर्गत बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, चरित्र, सृजनात्मकता और स्वभाव जैसे मनोवैज्ञानिक गुण तथा शारीरिक गठन, वेशभूषा और वाणी जैसे शारीरिक गुण समाहित होते हैं। विद्यालय का यह प्रयास होता है कि वह विद्यार्थी में सम्यक् गुणों का विकास कर एक अच्छे व्यक्तित्व को विकसित करे। विद्यालय में समय-समय पर व्यक्तित्व परीक्षणों की सहायता से व्यक्ति संबंधी विशेषताओं व समस्याओं का पता करके उनके निवारण का प्रयास करना चाहिये।
- शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन : शैक्षिक उपलब्धियों से तात्पर्य है- विषयगत दक्षता या योग्यता का मापन। विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं जिसका समय-समय पर मूल्यांकन या जाँच की जाती है जिससे उनकी शिक्षण-अधिगम संबंधी समस्याओं का निवारण कर उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके।
- नैदानिक मूल्यांकन : नैदानिक मूल्यांकन आमतौर पर एक विद्यार्थी द्वारा सामना की गई चुनौतियों/कठिनाइयों का निदान करने के लिये किया जाता है। विद्यार्थी को पाठ्यक्रम आरंभ से पहले और पाठ्यक्रम की समाप्ति पर एक समरूप पूर्व और पश्च परीक्षण दिया जाता है। यह विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों को पूर्व एवं पश्च परीक्षणों के परिणामों की तुलना करके उनकी सीखने की प्रगति को दर्शाने की अनुमति देती है।
सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्त्व निम्नलिखित है-
- सतत् मूल्यांकन से विद्यार्थिंयों की प्रगति योग्यता एवं उपलब्धि की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है।
- सतत् मूल्यांकन से कमज़ोरियों का निदान किया जा सकता है और इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक अलग-अलग विद्यार्थी की शक्ति, कमज़ोरियाँ और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं। इससे शिक्षक को तात्कालिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है जो इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि क्या किसी इकाई विशेष का पूरी कक्षा में पुन: शिक्षण किया जाए अथवा क्या कुछ विद्यार्थियों को उपचारी अनुदेश दिया जाना चाहिये।
- इससे शिक्षक को प्रभावी शिक्षा कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलती है।
- बहुधा कुछ व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक समस्याओं से या समायोजन संबंधी समस्याओं के कारण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह होने लगते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आने लगती है जिनसे जाँचने के लिये सतत् व्यापक मूल्यांकन का विशेष महत्त्व है।
- सतत् मूल्यांकन से विद्यार्थियों को अपनी शक्ति और कमज़ोरियों की जानकारी मिलती है। इससे विद्यार्थी को उसके अध्ययन के संबंध में स्पष्ट वास्तविक जानकारी मिलती है। इससे विद्यार्थी को अपनी अच्छी अध्ययन आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने तथा अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रेरणा मिलती है।
- सतत् और व्यापक मूल्यांकन अभिक्षमता व अभिरुचि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है।
- इससे भविष्य के लिये अध्ययन क्षेत्रों, पाठ्यक्रमों और व्यवसाय के चयन के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- यह शैक्षिक और गैर-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति संबंधी सूचना/रिपोर्ट उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी की भावी सफलता का अनुमान लगाने में सहायता देता है।
- यह अधिगमकर्त्ताओं की अभिप्रेरणा बढ़ाने, उनकी अध्ययन की आदतों को सुधारने तथा उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुँचाने में मदद करता है।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के प्रतिभाग के स्तर को समुन्नत बनाने में मदद मिलती है जिससे उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे विद्यार्थी न केवल संज्ञानात्मक और शैक्षणिक अनुक्षेत्र में प्रगति बल्कि उसके संज्ञानेतर एवं व्यक्तित्व के विविध पक्षों, यथा- रुचि, अभिवृत्ति, आदतों, मूल्य एवं चरित्र में होने वाले रूपांतरण का भी आकलन मिल जाता है।
बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उन्हें समग्र रूप से विकसित होने के लिये यह ज़रूरी है कि उनकी सीखने की प्रगति के बारे में सी.सी.ई. द्वारा पता किया जाए जिससे निम्नलिखित बिंदुओं में विशेष सहायता मिल सकेगी-
- बच्चे के अधिगम और विकास में हुए परिवर्तनों का पता लगाना और उनकी सही-सही पहचान करना।
- हर बच्चे को सीखने के लिये कहाँ और कैसी मदद की ज़रूरत है, इसकी पहचान करना।
- बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने-सिखाने की योजना बनाना जिससे उनका बेहतर अधिगम और विकास हो।
- स्व-आकलन के अवसर देते हुए बच्चों में अपने काम की समीक्षा करके अधिगम को बेहतर करने की क्षमता का विकास करना।
- यह पता लगाना कि पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है।
- बच्चों के अधिगम और विकास की कमियों को पूरा करने के लिये कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना।
- माता-पिता, अभिभावकों एवं अन्य पण धारकों को बच्चों की प्रगति के बारे में साक्ष्य-आधारित फीडबैक देना और उन्हें बच्चे के अधिगम तथा विकास में रचनात्मक रूप से शामिल करना।
- आकलन के भय को दूर करते हुए हर बच्चे को सीखने हेतु लगातार प्रोत्साहित करना एवं उनमें आत्मविश्वास जगाना।
- प्रत्येक बच्चे विशिष्टताओं अथवा विषमताओं के संदर्भ में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं जिससे उनमें सीखने और कौशल ग्रहण करने के स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। बच्चों में इन विभिन्नताओं के कई कारक तत्त्व उत्तरदायी होते हैं। अत: शिक्षण अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट विद्यार्थी के रूप में समझना चाहिये न कि सामान्य रूप में।
- विशिष्टताओं अथवा विषमताओं के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को कुछ प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-
शारीरिक विषमताओं वाले बच्चे
- शारीरिक विषमताओं वाले विद्यार्थियों की श्रेणी में उन विद्यार्थियों को रखा जा सकता है जिनमें शारीरिक अशक्तता या अंगों के संचालन एवं समन्वय में समस्याएँ पाई जाती हैं। ऐसे शारीरिक दोष वाले व्यक्तियों में मांसपेशियों और शरीर के जोड़ों में विकार के कारण अंगों का संचालन प्रभावित होता है जो कि उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक समायोजन में चुनौती प्रस्तुत करता है।
- ऐसे विद्यार्थी शिक्षण अधिगम में सामान्य विद्यार्थियों के समान होते हैं लेकिन शारीरिक क्रियाकलापों वाले शैक्षणिक गतिविधियों में इन्हें कठिनाई होती है। उदाहरण के लिये हाथों की कठोर मांसपेशियों के कारण लिखने में समस्या, उठने-बैठने एवं चलने फिरने में समस्या, शीघ्र थक जाना आदि।
दृष्टि बाधित बच्चे
- दृष्टि दोष वाले बच्चे किसी वस्तु को सही तरह से देखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। दृष्टि दोष से संबंधित बच्चों को दो श्रेणियों पूर्ण दृष्टि बाधित (Blind) और अल्प दृष्टि (Low Vision) बाधित में विभाजित किया जाता है।
- विकलांगता अधिनियम, 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों को ऐसे बच्चों की श्रेणी में शामिल किया जाता है जो निम्नलिखित दृष्टि दोष में से किसी एक से ग्रस्त होते हैं-
- दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
- दृष्टि को सुधारने वाले लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20@200 (स्नेलन) से अधिक न हो,
- 20 डिग्री या इससे कम की दृष्टि क्षेत्र सीमा
- अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति की श्रेणी में दृष्टि क्षमता ह्रास वाले ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो दृष्टि सुधार युक्तियों या उपकरणों की सहायता से दृष्टि का उपयोग करते हुए अपने कार्यों के निष्पादन में सक्षम होते हैं।
श्रवण दोष वाले बच्चे
- श्रवण दोष वाले बच्चों में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जिनकी सुनने की क्षमता कम होती है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार- ‘‘श्रवण अक्षमता से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि।’’
- आंशिक श्रवण दोष वाले बच्चों की श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है और ऐसे बच्चे 5 फीट की दूरी पर हो रहे वार्तालाप को सुन पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
वाणी दोष वाले बच्चे
- साधारणत: बचपन से गंभीर श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। ऐसे बच्चों की बोल-चाल की शैली सामान्य बच्चों से भिन्न होती है। उदाहरण के लिये संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होना, बोलने समय काफी एकाग्रता की आवश्यकता, अस्पष्ट भाषा, धाराप्रवाह बोलने में समस्या आदि। ऐसे बच्चों में श्वसन क्रिया असामान्य होने के साथ-साथ इनकी आवाज़ हल्की और कर्कश होती हैं।
मानसिक मंदता वाले बच्चे
- मानसिक मंदता वाले बच्चों में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जिनमें सामान्य बच्चों की तुलना में कम मानसिक योग्यता पाई जाती है। कम मानसिक योग्यता के कारण ऐसे बच्चों में सीखने की गति मंद होती है जिस कारण से सीखने और शिक्षण प्रक्रिया में इनका निष्पादन कम हो जाता है।
- विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार मानसिक मंदता किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था को दर्शाती है जो विशेष रूप से बुद्धि की अवसामान्यता से अभिलक्षित होती है।
- ऐसे बच्चों का बुद्धि स्तर और सोचने-समझने की क्षमता बहुत सीमित होती है जिस कारण से ये समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं।
- उपर्युक्त के अलावा विशेष आवश्यकता वाले वर्ग में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों (लड़कों एवं लड़कियों) को भी शामिल किया जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी शैक्षणिक प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
उपलब्धि परीक्षण स्कूल से विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थीं ने कितनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है।
उपलब्धि परीक्षण के अर्थ और भाव को और अधिक स्पष्ट करने के लिये विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-
- इबेल : ‘‘उपलब्धि परीक्षण वह है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किये हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है।’’
- गैरीसन तथा अन्य : ‘‘उपलब्धि परीक्षण, बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है।’’
- फ्रीमैन : ‘‘शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्त्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करता है।’’
- थॉर्नडाइक और हेगन : ‘‘जब हम संप्राप्ति परीक्षण को प्रयोग करते हैं, तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है?’’
- प्रेसी, रॉबिनस और होरोक : ‘‘संप्राप्ति परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से विद्यार्थियों के सीखने के स्वरूप और सीमा का मापन करने के लिये किया जाता है।’’
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वे हैं, जिनकी सहायता से स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाए जाने वाले कौशलों में विद्यार्थियों की सफलता अथवा उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
उपलब्धि परीक्षण का महत्व (Significance of Achievement Test)
शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण प्रणाली के कामकाज और विकास के लिये उपलब्धि परीक्षणों को एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना है
थॉर्नडाइक और हेगन ने स्कूल की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण के महत्त्व का प्रतिपादन निम्नलिखित शब्दों में किया है-
- विद्यार्थियों का वर्गीकरण : उपलब्धि परीक्षणों से विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त होते हैं, उससे उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो सकता है। इसलिये उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान : इन परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता चल जाता है। कठिनाई जान लेने पर उसके निवारण के उपाय किये जा सकते हैं। इस दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रगति में योगदान किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों को प्रेरणा : अनुभव से पता चलता है कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने में भी इन परीक्षाओं को सफलता मिली है। जब विद्यार्थियों को इस बात का पता चलता है कि उनके अर्जित ज्ञान की जाँच हो रही है, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है।
- व्यक्तिगत सहायता : उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा सरलता से मंदबुद्धि, कुशाग्र बुद्धि तथा विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों को पता लगाकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता की जा सकती है।
- शिक्षा-निर्देशन : इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किये हैं तथा उनके पूर्व के और अभी के अंकों को देखकर उन्हें समुचित निर्देशन दिया जा सकता है कि उन्हें कौन-से विषय लेने चाहिये आदि।
- विद्यार्थियों को परामर्श : उपलब्धि परीक्षाओं से हमें पता चलता है कि विद्यार्थियों की रुचियाँ क्या हैं? उनकी अभियोग्यताएँ और कार्य-क्षमताएँ क्या हैं? इसके आधार पर उन्हें आगामी अध्ययन के लिये परामर्श दिया जा सकता है।
समायोजन दो शब्दों को मिलाकर बना है सम और आयोजन। सम का अर्थ है-अच्छी तरह या समान रूप से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था अर्थात् अच्छी तरह व्यवस्था करना। समायोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ और मानसिक द्वंद्व न उत्पन्न होने पाए।
- समायोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए गेट्स एवं अन्य विद्वानों ने लिखा है कि ‘समायोजन’ शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं और पर्यावरण के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध रखने के लिये अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। दूसरे अर्थ में समायोजन एक संतुलित दशा है, जिस पर पहुँचने पर हम उस व्यक्ति को सुसमायोजित कहते हैं।
समायोजन की प्रमुख परिभाषाएँ
- बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वैल्ड के अनुसार, ‘‘समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है।’’
- लोरेंस एफ. शैफर के अनुसार, ‘‘समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं : प्रथम, शारीरिक आवश्यकताएँ तथा द्वितीय सामाजिक आवश्यकताएँ। भूख, त्याग, नींद, काम वासना, मल-मूत्र त्याग आदि शारीरिक आवश्यकताएँ हैं, जबकि सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि सामाजिक आवश्यकताएँ हैं। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति बैचेन हो जाता है और उसमें तनाव पैदा हो जाता है।
- गेट्स व अन्य के अनुसार, ‘‘समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिये अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है।’’
समायोजन की आवश्यकता (Need of Adjustment)
सर्वांगीण विकास के लिये उसका वातावरण के साथ समायोजन अत्यंत आवश्यक है। इस आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है :
- मानसिक कष्ट और व्याधियों से अपने को दूर रखने के लिये।
- अपने मन और मस्तिष्क को व्यर्थ के चिंतन से दूर रखने के लिये।
- ध्यान की एकाग्रता बनाए रखने के लिये।
- विभिन्न गतिविधियों और कार्यकलापों में सक्रिय एवं उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिये।
- पलायन करना, चुनौती देना जैसी कुप्रवृत्तियों को न पनपने देने के लिये।
- जीवन में शौक पैदा करने के लिये।
- अपने काम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने के लिये।
- जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करने के लिये।
वर्तमान समय में आकलन शब्द का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जो सिखाया जाता है उसका आकलन विविध उपकरणों का प्रयोग करके किया जाता है। आकलन का यह प्रारूप सीखने और सिखाने के प्रारूप को प्रभावित करता है।
- आँकना ‘assess’ शब्द लैटिन भाषा के शब्द ‘assidere’ से लिया गया है जिसका अर्थ है- ‘साथ बैठना’ (to sit with)। इसका तात्पर्य यह है कि यह कुछ इस प्रकार है जिसको हम विद्यार्थियों के साथ और विद्यार्थियों के लिये करते हैं। आकलन के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता है।
- आकलन शिक्षक और शिक्षण दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह अधिगम को समृद्ध करता है, शिक्षार्थियों की प्रेरणा को बढ़ाता है और साथ ही शिक्षकों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों/रणनीतियों पर चिंतन-मनन करने और यदि आवश्यक हो तो संशोधन करने में सक्षम बनाता है।
- फ्रीमैन और लेविस (1998) के अनुसार आकलन के पाँच मुख्य उद्देश्य हैं- चयन करना, प्रमाणित करना, वर्णन करना, अधिगम में सहायता करना और शिक्षण में सुधार करना, जो सार्वजनिक निर्णय और व्यक्तिगत विकास को एक संतुलन देते हैं।
- सामान्य शब्दों में आकलन का आशय है- सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया।
- विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन (Assessment) कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके।
आकलन की परिभाषाएँ (Definitions of Assessment)
- हुबा एवं फ्रीड के अनुसार- ‘‘आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है या नहीं। यह समझने में मदद करता है कि बच्चे क्या जानते हैं और क्या जान सकते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी अधिगम में वृद्धि होती है।’’
- इरविन के अनुसार- ‘‘आकलन विद्यार्थियों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर विद्यार्थी विकास और अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है।’’
आकलन अभ्यास के लाभ
आकलन अभ्यास के निम्नलिखित लाभ हैं:
- यह विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित विस्तृत एवं गहन आँकड़ा प्रदान करता है।
- यह समझने में मदद करता है कि बच्चे क्या जानते हैं और क्या जान सकते हैं।
- यह विद्यार्थियों की प्रबलताओं और दुर्बलताओं की पहचान करके उनके अधिगम को समझने के लिये एक लेंस के रूप में कार्य करता है।
- यह शिक्षकों, माता-पिता और परिवार के सदस्यों को एक बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का निर्धारण करता है ताकि उनको उससे संबंधित अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सके।
- विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर उनके लिये निर्दिष्ट विशिष्ट रणनीति की योजना बनाने में शिक्षकों की मदद करता है।
- अधिगम के परिणामों में सुधार करने और अधिगम को बढ़ावा देने में योगदान करता है।
- एक कार्यक्रम की प्रबलताओं और दुर्बलताओं को पहचान करने में मदद करता है।
- इसके माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को संशोधित करने और शैक्षणिक दृष्टिकोण में सुधार करने के लिये प्राप्त जानकारी का उपयोग करने की सुविधा होती है।
- विद्यार्थी का समर्थन करने के लिये माता-पिता, शिक्षकों और शिक्षकों के बीच सहयोग की सुविधा होती है।
अत: यह कहा जा सकता है कि आकलन का उद्देश्य विद्यार्थी के सीखने के बारे में मान्य, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी एकत्र करना है, जिसका उपयोग अधिगम के परिणामों के संबंध में विद्यार्थी की प्रगति और उपलब्धि की निगरानी के लिये किया जा सकता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों को निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने के लिये उचित उपाय करने के लिये भी किया जाता है।
शिक्षण संस्थानों की व्यावहारिक एवं तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु एस.एम. कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान विधि को विकसित किया।
- क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं बल्कि व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है।
- इस अनुसंधान के द्वारा विद्यालय की क्रिया प्रणाली में सुधार, औद्योगिक समस्याओं का समाधान तथा सामाजिक समस्याओं के बेहतर निराकरण को संभव माना गया है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही तात्कालिक अनुप्रयुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है।
- एस.एम. कोरे- ‘‘क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक व्यवसायी अपने निर्णय में निर्देशित होने के लिये, सुधार लाने के लिये एवं मूल्यांकन के लिये अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है।’’
क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ (Characteristics of Action Research)
- इसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है।
- यह अनुसंधान व्यावहारिक पक्ष (Practical Aspect) पर अधिक बल देता है।
- इस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान के वर्ग में रखा गया है।
- इससे व्यवसायी अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं।
- यह नैदानिक (Diagnostic) कार्यों के लिये वैयक्तिक अनुसंधान है।
- यह अनुसंधान किसी विशेष संस्था, समुदाय तक ही सीमित होता है।
- यह अनुसंधान तात्कालिक समस्याओं के समाधान से ही संबंधित है।
- इस अनुसंधान के अंतर्गत Research-Action-Research-Action-Research की क्रिया सतत रूप से चलती है।
क्रियात्मक अनुसंधान के चरण (Steps of Action Research)
क्रियात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण हैं-
- समस्या का चयन
- समस्या का कथन एवं मूल्यांकन
- परिकल्पनाओं का निर्माण
- प्रदत्त संकलन
- उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर परिकल्पनाओं का परीक्षण
- परिणाम, निष्कर्ष एवं सुझाव
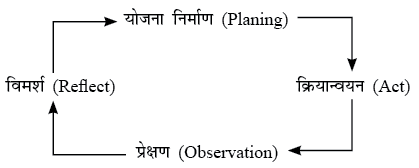
क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य (Objectives of Action Research)
- विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये विद्यालय प्रणाली (School System) में परिवर्तन करके स्वस्थ वातावरण को विकसित करना।
- विद्यार्थियों व शिक्षकों में समस्याओं के समाधान के लिये वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करना।
- विद्यालय कर्मचारियों को अपने निष्पादन में उत्कर्षता स्तर (Level of Excellence) लाने के लिये प्रेरित करना।
- विद्यालयों अथवा संस्था की कार्य दशाओं में सुधार लाना।
- विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर को उच्च करने में सहायता करना।
किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व लाने का कार्य अभिप्रेरणा के द्वारा ही होता है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है।
अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित शिक्षाविदों की परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं-
फ्रेंडसन- “सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं।”
गुड – “किसी कार्य को आरंभ करने, ज़ारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं।”
थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा का महत्त्व- “अभिप्रेरणा एक कला है। इसके द्वारा उन विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है जिनमें इस प्रकार की रुचि का अभाव पाया जाता है तथा जहाँ पर विद्यार्थियों की अधिगम में रुचि तो है परंतु वे उसका अनुभव नहीं करते हैं, वहाँ प्रेरणा के द्वारा उन्हें यह अनुभव कराया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट पाठ्यचर्याओं के प्रति भी विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न की जाती है।”
- अभिप्रेरणा के दो रूप होते हैं, जो शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगी हैं-
- बाह्य अभिप्रेरणा (External Motivation)
- आंतरिक अभिप्रेरणा (Internal Motivation)
छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होती है, जबकि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएँ कार्य करती हैं। व्यवहार परिवर्तन में वातावरण की भूमिका भी प्रभावी सिद्ध होती है। अत: शिक्षण के दौरान कक्षा का वातावरण इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिये कि विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रियाएँ संपन्न करने के साथ-साथ अपने उद्देश्य हेतु प्रतिबद्ध भी हों।
मनोविज्ञान के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। इसलिये शिक्षण कार्य कराते समय आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिये।
अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्त्व (Educational Importance of Motivation)
- अधिगम के लिये प्रोत्साहन हेतु
- व्यवहार में परिवर्तन हेतु
- अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु
- अनुशासन विकसित करने हेतु
- मार्गदर्शन हेतु
- सामाजिक व चारित्रिक गुणों हेतु
- उच्च आकांक्षा हेतु






