हार्ड डिस्क कंप्यूटर की एक महत्त्वपूर्ण सेकेंडरी मेमोरी है, जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिये किया जाता है। तकनीक के विकास के साथ-साथ हार्ड डिस्क के कई प्रकार विकसित हुए हैं। मुख्य रूप से हार्ड डिस्क के पाँच प्रकार माने जाते हैं — SATA, PATA, NVMe, SCSI और SSD।
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) आज के समय में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क तकनीक है। इसका उपयोग लगभग सभी आधुनिक डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटरों में किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटरों में 3.5 इंच की SATA हार्ड डिस्क और लैपटॉप में 2.5 इंच की SATA हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। SATA डेटा ट्रांसफर करने की तेज गति के लिये जानी जाती है, जिसकी स्पीड लगभग 150 MBps से 600 MBps तक होती है। इसे Serial ATA भी कहा जाता है और इसका आविष्कार वर्ष 2000 में किया गया था।
PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) पुराने समय में उपयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क तकनीक है। इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड कम होती थी, इसी कारण आज के समय में इसे SATA ने लगभग पूरी तरह से बदल दिया है।
NVMe (Non-Volatile Memory Express) एक आधुनिक और अत्यंत तेज तकनीक है, जिसका उपयोग हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर और लैपटॉप में किया जाता है। यह PCIe इंटरफेस पर आधारित होती है और बहुत तेज डेटा ट्रांसफर प्रदान करती है।
SCSI (Small Computer System Interface) का उपयोग मुख्य रूप से सर्वर और बड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। यह एक साथ कई डिवाइस को कनेक्ट करने में सक्षम होती है।
SSD (Solid State Drive) सबसे आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। यह बहुत तेज, हल्की और विश्वसनीय होती है, लेकिन इसकी कीमत सामान्य हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक होती है।
क्वॉड कोर प्रोसेसर एक आधुनिक और शक्तिशाली प्रोसेसर होता है, जिसमें चार स्वतंत्र कोर (Core) होते हैं। कोर प्रोसेसर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर को दिये गये निर्देशों को प्रोसेस करता है। जब एक प्रोसेसर में चार कोर होते हैं, तो वह एक समय में कई कार्यों को समानांतर रूप से करने में सक्षम हो जाता है। इसी कारण क्वॉड कोर प्रोसेसर को मल्टीटास्किंग के लिये बहुत उपयोगी माना जाता है।
क्वॉड कोर प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाना और कार्यों को तेजी से पूरा करना होता है। उदाहरण के लिये, यदि कोई उपयोगकर्ता एक साथ वीडियो देख रहा है, इंटरनेट ब्राउज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है और कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो क्वॉड कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कार्य अलग-अलग कोर द्वारा संभाला जा सकता है। इससे सिस्टम पर लोड कम पड़ता है और कंप्यूटर स्मूद तरीके से कार्य करता है।
सिंगल और ड्यूल कोर प्रोसेसर की तुलना में क्वॉड कोर प्रोसेसर अधिक तेज, अधिक कुशल और अधिक शक्तिशाली होते हैं। इन प्रोसेसर का उपयोग विशेष रूप से गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रोफेशनल कार्यों के लिये किया जाता है, जहाँ अधिक प्रोसेसिंग क्षमता की आवश्यकता होती है। आज के समय में अधिकांश लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्ट डिवाइस में क्वॉड कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हालाँकि क्वॉड कोर प्रोसेसर के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। यह प्रोसेसर अधिक बिजली का उपयोग करते हैं और ज्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, इनकी कीमत भी अधिक होती है। फिर भी, तेज गति, बेहतर प्रदर्शन और मल्टीटास्किंग क्षमता के कारण क्वॉड कोर प्रोसेसर आधुनिक कंप्यूटिंग के लिये एक महत्त्वपूर्ण विकल्प माना जाता है।
CU का पूरा नाम Control Unit (कंट्रोल यूनिट) है। यह CPU (Central Processing Unit) का एक महत्त्वपूर्ण भाग होता है, जो कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित (control) करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंट्रोल यूनिट, CPU का वह हिस्सा है जो कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसों, जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच समन्वय स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य सही क्रम में पूरे हों।
कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश देना और उन्हें नियंत्रित करना होता है। यह स्वयं कोई गणना नहीं करती, बल्कि अन्य इकाइयों को यह बताती है कि कब, कैसे और कौन-सा कार्य करना है। जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है, तब कंट्रोल यूनिट मुख्य मेमोरी से निर्देश (instructions) प्राप्त करती है, उन्हें डिकोड करती है और फिर उन्हें execute करने के लिये ALU (Arithmetic Logic Unit) को भेज देती है। ALU जब गणना पूरी कर लेता है, तो परिणाम वापस CU को भेज देता है।
Control Unit इनपुट/आउटपुट डिवाइसों और मुख्य मेमोरी के साथ लगातार कम्युनिकेशन करती रहती है। यह डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और यह तय करती है कि कौन-सा डेटा कब और कहाँ भेजा जाएगा। इसी कारण कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है।
कंट्रोल यूनिट CPU और GPU दोनों में उपयोग की जाती है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं—
- Program Counter (PC): इसका कार्य मेमोरी से निर्देशों को क्रमवार लोड करना और यह बताना होता है कि अगला निर्देश कौन-सा execute होगा।
- Instruction Register (IR): इसमें वर्तमान निर्देश को रखा जाता है, जिसे डिकोड करके CPU के लिये कमांड में बदला जाता है।
इस प्रकार, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को सही दिशा और गति प्रदान करती है।
Digitizer (डीजीटाइज़र) एक प्रकार की input device है, जिसका उपयोग drawings, graphics, images और signatures को डिजिटल रूप में बदलने के लिये किया जाता है। इस डिवाइस में एक सपाट सतह (flat surface) होती है, जिस पर एक विशेष pen या stylus की सहायता से कार्य किया जाता है। जब यूजर इस सतह पर कुछ भी लिखता, बनाता या स्केच करता है, तो वह तुरंत monitor या screen पर दिखाई देता है।
डीजीटाइज़र का मुख्य कार्य एनालॉग जानकारी को डिजिटल डेटा में बदलना होता है। यही कारण है कि इसका उपयोग signatures, images, maps और technical drawings को capture करने के लिये व्यापक रूप से किया जाता है। आज के समय में इसका प्रयोग शिक्षा, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।
डीजीटाइज़र का उपयोग विशेष रूप से CAD (Computer-Aided Design) एप्लीकेशन और AutoCAD जैसे सॉफ़्टवेयर के साथ किया जाता है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट इसका उपयोग accurate designs और blueprints तैयार करने के लिये करते हैं। इसके अलावा graphic designers भी डीजीटाइज़र की मदद से अधिक सटीक और professional डिज़ाइन बना पाते हैं।
touchscreen की तुलना में डीजीटाइज़र अधिक precision और control प्रदान करता है। इसमें pen की sensitivity अधिक होती है, जिससे बारीक से बारीक रेखाएँ भी आसानी से बनाई जा सकती हैं। यही कारण है कि जहाँ उच्च गुणवत्ता और शुद्धता की आवश्यकता होती है, वहाँ डीजीटाइज़र को प्राथमिकता दी जाती है।
Features of Digitizer in Hindi – डीजीटाइज़र की विशेषताएँ
- इसमें एक pen होता है, जो drawing, writing और inserting जैसे कार्यों को आसान बनाता है।
- touchscreen की तुलना में यूजर इस डिवाइस पर बेहतर control और accuracy के साथ काम कर सकता है।
Keyboard (कीबोर्ड) एक basic input device है, जिसका उपयोग यूजर कंप्यूटर को निर्देश (commands) देने के लिये करता है। कीबोर्ड की सहायता से यूजर letters, numbers, symbols, characters और functions को कंप्यूटर में इनपुट करता है। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच संवाद का एक प्रमुख माध्यम है।
कीबोर्ड में अलग–अलग प्रकार की keys होती हैं, जैसे alphabet keys, numeric keys, function keys और special keys। इन keys को दबाकर यूजर कंप्यूटर को बताता है कि उसे कौन-सा कार्य करना है। आज के समय में कीबोर्ड को USB और Bluetooth दोनों माध्यमों से कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़ा जा सकता है, जिससे इसका उपयोग और भी आसान हो गया है।
कीबोर्ड का उपयोग केवल टाइपिंग के लिये ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर को control करने, शॉर्टकट कमांड देने और कई बार माउस के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। इसलिए कीबोर्ड को कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्त्वपूर्ण इनपुट डिवाइस माना जाता है।
Types of Keyboard in Hindi – कीबोर्ड के प्रकार
कीबोर्ड मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं—
- QWERTY Keyboard
यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला और आधुनिक कीबोर्ड है। आज के समय में लगभग सभी देशों में इसी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। - AZERTY Keyboard
यह कीबोर्ड QWERTY लेआउट के आधार पर डिज़ाइन किया गया है और इसे French Keyboard भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फ्रांस और कुछ यूरोपीय देशों में किया जाता है। - DVORAK Keyboard
इस प्रकार के कीबोर्ड को टाइपिंग की गति (Typing Speed) बढ़ाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।
Features of Keyboard in Hindi – कीबोर्ड की विशेषताएँ
- कीबोर्ड का उपयोग कई बार mouse के स्थान पर भी किया जा सकता है।
- कीबोर्ड के चार प्रमुख भाग होते हैं— Main Keyboard, Cursor Keys, Numeric Keypad और Function Keys।
- कीबोर्ड सामान्यतः कम कीमत (less expensive) का इनपुट डिवाइस होता है।
RAM (Random Access Memory) कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण हार्डवेयर डिवाइस होता है। RAM का पूरा नाम Random Access Memory (रैंडम एक्सेस मेमोरी) है। यह कंप्यूटर में डेटा को temporarily (अस्थायी रूप से) स्टोर करने का कार्य करती है, अर्थात इसमें डेटा केवल कुछ समय के लिये ही सुरक्षित रहता है। जब कंप्यूटर चालू रहता है, तभी RAM सक्रिय रहती है।
RAM को Main Memory, Primary Memory या System Memory भी कहा जाता है। इसे कई बार Read-Write Memory भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को पढ़ा (read) और लिखा (write) दोनों जा सकता है। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फाइल्स इस समय उपयोग में होती हैं, वे सभी RAM में ही लोड रहती हैं।
RAM की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह डेटा को randomly access करती है। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर किसी भी डेटा को सीधे एक्सेस कर सकता है, जिससे कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत तेज हो जाती है। इसके विपरीत, CD और Hard Disk में डेटा क्रम (sequence) में एक्सेस होता है, जिस कारण वे अपेक्षाकृत धीमी होती हैं।
RAM एक volatile memory है, यानी इसमें मौजूद डेटा को सुरक्षित रखने के लिये लगातार power की आवश्यकता होती है। यदि कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए, तो RAM में मौजूद सारा डेटा lost (समाप्त) हो जाता है। इसी कारण, कंप्यूटर को दोबारा चालू या reboot करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य आवश्यक फाइल्स को हार्ड डिस्क से फिर से RAM में load किया जाता है।
RAM मदरबोर्ड पर स्थित होती है और यह एक ही समय में read और write दोनों कार्य कर सकती है। इसकी read और write करने की गति अन्य स्टोरेज डिवाइसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। RAM की क्षमता को bytes में मापा जाता है, जैसे MB (Megabyte) और GB (Gigabyte)। अधिक RAM होने से कंप्यूटर की performance बेहतर होती है और वह तेज गति से कार्य करता है।
गहन कृषि उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है जिसमें सीमित भूमि क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये पूँजी, श्रम और आधुनिक तकनीकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यह कृषि पद्धति मुख्यतः उन क्षेत्रों में विकसित हुई है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों में किसान बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं—जैसे जुताई, बुआई, कटाई और थ्रेसिंग—में मशीनों का प्रयोग कर कृषि का मशीनीकरण किया जाता है।
गहन कृषि को औद्योगिक कृषि भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भूमि को परती नहीं छोड़ा जाता, बल्कि वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में इनपुट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे—उर्वरक, बीज, सिंचाई, श्रम और पूँजी। यह पारंपरिक कृषि से भिन्न है, जहाँ प्रति इकाई भूमि पर इनपुट अपेक्षाकृत कम होते हैं और उत्पादन भी सीमित रहता है।
भारत में गहन कृषि को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा गहन कृषि विकास कार्यक्रम (Intensive Agriculture Development Programme – IADP) की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 1961 में आरंभ हुआ और इसे भारतीय कृषि क्षेत्र में सरकार का पहला बड़ा प्रयोग माना जाता है। इसे “पैकेज कार्यक्रम” भी कहा गया, क्योंकि इसमें किसानों को एक साथ बीज, उर्वरक, सिंचाई, ऋण और तकनीकी सहायता का पैकेज उपलब्ध कराया गया।
इस कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घटती लोकप्रियता के बाद की गई थी। IADP का मुख्य उद्देश्य किसानों को बीज और उर्वरक के लिये ऋण सुविधा प्रदान करना था, ताकि उत्पादन में तीव्र वृद्धि की जा सके। इस कार्यक्रम को फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से लागू किया गया।
बाद में IADP का विस्तार किया गया और विशेष फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agricultural Area Programme – IAAP) शुरू किया गया। इन प्रयासों ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने और हरित क्रांति की नींव रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पीट या दलदली मिट्टी भारत की एक विशिष्ट प्रकार की मृदा है, जो मुख्य रूप से अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लंबे समय तक जलभराव की स्थिति में वनस्पतियों के सड़ने-गलने से होता है। जल की अधिकता के कारण कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण अपघटन नहीं हो पाता, जिससे इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है।
पीट मिट्टी में जैविक पदार्थों एवं लवणों की मात्रा लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक पाई जाती है, जो इसे अन्य मृदाओं से अलग बनाती है। हालाँकि, इसमें पोटाश तथा फास्फोरस की कमी होती है, जिसके कारण यह सामान्य कृषि के लिये अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह मिट्टी सामान्यतः अम्लीय स्वभाव की होती है और इसकी संरचना काली या गहरे भूरे रंग की होती है।
भारत में पीट या दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत के डेल्टाई क्षेत्रों तथा हिमालय की तराई प्रदेश में भी यह मिट्टी बहुलता से मिलती है। जलभराव वाले इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से दलदली परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, जो इस मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं।
इस मिट्टी पर मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ये पौधे जलमग्न एवं लवणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। सुंदरवन जैसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति पीट मिट्टी का ही उदाहरण है।
कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी सीमित उपयोगी है, किंतु उचित जल निकास, उर्वरकों तथा मृदा सुधार उपायों द्वारा इसमें धान एवं कुछ अन्य फसलों की खेती की जा सकती है। इस प्रकार, पीट या दलदली मिट्टी पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।
लाल मिट्टी भारत में पाई जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण मृदा है। यह मिट्टी भारत के कुल भू-भाग का लगभग 18.6 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत की दूसरी सबसे विस्तृत मृदा मानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर तथा परिवर्तित आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अपक्षय और विघटन से हुआ है।
लाल मिट्टी का विस्तार भारत के कई भागों में पाया जाता है। यह विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान तथा छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई है। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। जहाँ लोहे का ऑक्साइड जलयोजित अवस्था में पाया जाता है, वहाँ यह मिट्टी पीले रंग की दिखाई देती है।
लाल मिट्टी सामान्यतः अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें लोहे, एलुमिनियम तथा चूने की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, जबकि मृतिका (ह्यूमस), नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की कमी होती है। इसी कारण यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से अधिक उपजाऊ नहीं होती।
हालाँकि, उचित सिंचाई, उर्वरकों तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से लाल मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसमें कपास, मूँगफली और बाजरा की खेती भी सफलतापूर्वक की जाती है। भारतीय कृषि में लाल मिट्टी का विशेष महत्त्व है।
उष्णकटिबंधीय मानसूनी अथवा पतझड़ वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत में पाए जाने वाले वनों में यह सबसे व्यापक प्रकार है। इन वनों के वृक्ष गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाती है। इसी कारण इन्हें मानसूनी वन या पतझड़ वन कहा जाता है।
ये वन भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा पश्चिमी घाट के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। मानसूनी जलवायु इन वनों के विकास के लिये अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।
इन वनों में आम, जामुन, नीम, महुआ, शहतूत, शीशम, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों से प्राप्त लकड़ी आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। यह लकड़ी सामान्यतः मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर, कृषि उपकरणों, भवन निर्माण तथा लघु उद्योगों में किया जाता है।
मानसूनी वनों की विशेषताएँ
- ये वन सदाबहार वनों की तुलना में कम घने होते हैं।
- इन वनों में वृक्षों की ऊँचाई औसत होती है।
- वृक्षों की प्रजातियों में अपेक्षाकृत समानता पाई जाती है।
- इन वनों का आर्थिक महत्त्व बहुत अधिक होता है।
- भारत में सबसे अधिक इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं।
- इन वनों से लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिये कच्चा माल प्राप्त होता है।
बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2023 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8.0 प्रतिशत है। यह प्रतिशत भारत के औसत वनाच्छादन (21.76 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। राज्यों में जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम (85.34 प्रतिशत) में पाया जाता है, वहीं हरियाणा में यह सबसे कम (3.63 प्रतिशत) है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार के वन क्षेत्र में 151.66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो लगभग 2.01 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।
भौगोलिक दृष्टि से बिहार उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। राज्य में प्राकृतिक वन मुख्यतः पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, मुंगेर, बाँका तथा जमुई जिलों में फैले हुए हैं। उत्तर बिहार का अधिकांश भाग प्राकृतिक वनों से रहित है, केवल पश्चिम चंपारण जिला इसका अपवाद है। शिवालिक श्रेणी के तराई क्षेत्र में स्थित पश्चिम चंपारण में प्राकृतिक साल के वन पाए जाते हैं।
दक्षिण बिहार के पठारी एवं पहाड़ी भागों—विशेषकर कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और बाँका जिलों—में भी साल के वन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती वनों की प्रधानता है। वर्षा की असमानता के कारण यहाँ आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं।
वनों के प्रकार के आधार पर बिहार में वनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—
1. आर्द्र पर्णपाती वन
2. शुष्क पर्णपाती वन
3. झाड़ीदार एवं विरल वन
कुल मिलाकर, सीमित वन क्षेत्र होने के बावजूद बिहार में वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से वन क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
बूढ़ी गंडक नदी उत्तर बिहार की एक महत्त्वपूर्ण नदी है, जिसे सामान्यतः गंडक नदी की परित्यक्त (Abandoned) धारा माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह नदी गंडक के पुराने प्रवाह पथ का प्रतिनिधित्व करती है, जो कालांतर में अपना मार्ग बदलने के कारण स्वतंत्र नदी के रूप में विकसित हो गई।
बूढ़ी गंडक नदी की उत्पत्ति चउतरवा चौर (विश्रामपुर), पश्चिमी चंपारण से मानी जाती है। यह नदी बिहार के मैदानी भागों में अपेक्षाकृत धीमी गति से बहती है और अधिक गाद वहन करती है, जिसके कारण इसके तटवर्ती क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
यह नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय तथा खगड़िया जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई अंततः गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार यह गंगा नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक को उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो क्षेत्रीय जल निकासी व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है।
बूढ़ी गंडक की अनेक सहायक नदियाँ हैं, जिनमें मसान, बालोर, पंडई, डंडा, सिकटा, तिऊर, धनौत, कोहरा, तिलावे तथा अंजानकोटे प्रमुख हैं। इनमें से बागमती नदी इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है, जो इसके जलप्रवाह और बाढ़ की तीव्रता को प्रभावित करती है।
मानसून के समय बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे इसके किनारे बसे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बावजूद यह नदी कृषि, विशेषकर धान, गेहूँ और गन्ने की खेती के लिये अत्यंत उपयोगी है।
इस प्रकार बूढ़ी गंडक नदी उत्तर बिहार की कृषि, जल संसाधन और भौगोलिक संरचना में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।
गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, जहाँ इसे प्रारंभ में भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग (उत्तराखंड) में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है।
भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसका प्रवाह लगभग 445 किलोमीटर लंबा है। बिहार में यह नदी चौसा (बक्सर) के पास प्रवेश करती है और आगे चलकर कटिहार (बिहार) एवं साहेबगंज (झारखंड) के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है।
बिहार में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और मुख्यतः बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार जिलों से होकर गुजरती है।
पटना जिला गंगा नदी का बिहार में सबसे लंबा प्रवाह क्षेत्र है, जहाँ इसकी लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है।
बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ
बाई ओर (उत्तर दिशा) से मिलने वाली नदियाँ—
घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला तथा महानंदा।
दाई ओर (दक्षिण दिशा) से मिलने वाली नदियाँ—
सोन, कर्मनाशा, पुनपुन तथा किऊल।
महत्त्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts)
- गंगा बिहार की कृषि, परिवहन एवं संस्कृति की जीवनरेखा है।
- गंगा के मैदान बिहार में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के लिये प्रसिद्ध हैं।
- पटना, मुंगेर और भागलपुर जैसे नगर गंगा के तट पर विकसित हुए।
प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का एक विश्वप्रसिद्ध केंद्र रहा है। इस काल में नालंदा, ओदंतपुरी तथा विक्रमशिला जैसे महाविहार उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ देश-विदेश से विद्यार्थी अध्ययन के लिये आते थे। ये संस्थान बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों के लिये प्रसिद्ध थे।
मध्यकाल में भी बिहार की शैक्षणिक परंपरा जीवित रही। इस काल में पटना, बिहारशरीफ और भागलपुर शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केंद्र बने। नगरों और गाँवों में प्राथमिक पाठशालाओं के साथ-साथ संस्कृत और फारसी में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय भी स्थापित किये गए। उस समय शिक्षा का विकास मुख्यतः राजाओं, जमींदारों और समाज के धनाड्य वर्ग द्वारा दिये गए दान पर निर्भर करता था।
अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद अपनाई गई औपनिवेशिक नीतियों के कारण पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गहरा आघात पहुँचा। स्थायी बंदोवस्त जैसी नीतियों से राजाओं और जमींदारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, जिससे शिक्षा को मिलने वाली आर्थिक सहायता में भारी कमी आई।
आधुनिक भारत में शिक्षा के इतिहास में 1813 ई. का चार्टर एक्ट अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल को भारत में शिक्षा के विकास के लिये प्रति वर्ष एक लाख रुपए व्यय करने का अधिकार दिया गया, किंतु व्यावहारिक स्तर पर इसका प्रभाव सीमित रहा।
इसके बाद 1835 ई. में लॉर्ड विलियम बैंटिक के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की औपचारिक शुरुआत हुई। इसी के साथ बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ 1835 ई. में हुआ, जब मैकाले प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। यहीं से बिहार में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी।
बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। 16वीं सदी में जब पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री व्यापार पर अपना प्रभाव स्थापित किया, तब वे धीरे-धीरे आंतरिक भू-भागों की ओर भी बढ़े। बिहार में उनका प्रवेश मुख्यतः बंगाल के हुगली (Hooghly) में स्थापित उनके व्यापारिक केंद्र के माध्यम से हुआ। पुर्तगाली व्यापारी नावों द्वारा गंगा नदी के रास्ते हुगली से पटना आया-जाया करते थे।
उस समय पटना बिहार का प्रमुख व्यापारिक नगर था और गंगा नदी के कारण यह एक महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन चुका था। पुर्तगाली व्यापारियों ने बिहार में स्थायी शासन स्थापित नहीं किया, बल्कि उनका उद्देश्य केवल व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। वे स्थानीय शासकों से अनुमति लेकर व्यापार करते थे।
पुर्तगालियों द्वारा बिहार से मुख्य रूप से सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े तथा अन्य वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। उस समय बिहार का सूती और रेशमी कपड़ा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अत्यधिक माँग में था। इसके बदले में पुर्तगाली व्यापारी चीनीमिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के मसाले, मदिरा और अन्य विदेशी वस्तुएँ बिहार में लाते थे।
पुर्तगाली व्यापारियों का बिहार की अर्थव्यवस्था पर सीमित किंतु प्रारंभिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने बिहार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से जोड़ा और यूरोपीय शक्तियों के लिये यहाँ के आर्थिक महत्त्व को उजागर किया। बाद में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया।
यद्यपि पुर्तगाली आगे चलकर अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सके, फिर भी बिहार में यूरोपीय व्यापार की नींव रखने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। उनके आगमन से बिहार में आधुनिक काल की व्यापारिक गतिविधियों का आरंभ माना जाता है।
कालामुख संप्रदाय शैव धर्म का एक अत्यंत उग्र, तांत्रिक तथा रहस्यमय संप्रदाय था। यह संप्रदाय अपने स्वरूप, साधना पद्धति और आचार-विचार में कापालिक संप्रदाय से काफी मिलता-जुलता था, किंतु इसकी प्रवृत्तियाँ कापालिकों की तुलना में अधिक भयावह और कठोर मानी जाती थीं।
‘कालामुख’ शब्द का अर्थ है — काले मुख वाले। इस नाम से ही इस संप्रदाय की उग्रता और तामसी स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी शिव के भैरव स्वरूप की उपासना करते थे और तंत्र-मंत्र आधारित साधनाओं पर विशेष बल देते थे।
इनके धार्मिक आचरण सामान्य सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से पूर्णतः भिन्न थे। ये लोग नरकपाल (मानव खोपड़ी) में भोजन करते थे, अपने शरीर पर श्मशान की भस्म मलते थे और मदिरा सेवन को साधना का अनिवार्य अंग मानते थे। इनका विश्वास था कि भय, मृत्यु और निषिद्ध कर्मों को स्वीकार कर ही आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति संभव है।
कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कठोर तपस्या और तथाकथित ‘महाव्रत’ का पालन करते थे। इसी कारण शिव पुराण में इन्हें ‘महाव्रतघर’ कहा गया है। ये लोग श्मशानों और एकांत स्थानों में निवास करते थे तथा सामाजिक नियमों और नैतिक बंधनों को तोड़ना आध्यात्मिक उन्नति का साधन मानते थे।
हालाँकि समय के साथ इस संप्रदाय की अत्यधिक उग्र, असामाजिक और तामसी गतिविधियों के कारण समाज में इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। वैदिक और भक्ति परंपराओं के उदय के साथ-साथ कालामुख संप्रदाय का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता चला गया और अंततः यह संप्रदाय लुप्त हो गया।
इस प्रकार कालामुख संप्रदाय प्राचीन भारत में शैव धर्म के तांत्रिक और उग्र स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय धार्मिक विविधता को समझने में सहायक है।
प्राचीन भारत में जिस बौद्ध धर्म ने एक समय व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की थी, वही धीरे-धीरे अपने मूल स्वरूप को खो बैठा और उसका पतन होने लगा। इसके पीछे अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे।
सबसे प्रमुख कारण यह था कि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया। ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर उन्हें वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म की स्वतंत्र और विशिष्ट पहचान कमजोर पड़ गई।
बौद्ध धर्म, जो प्रारंभ में कर्मकांड-विरोधी था, उसमें धीरे-धीरे अनुष्ठान, विधान और कर्मकांडों का प्रवेश होने लगा। इससे वह धर्म भी जटिल बन गया, जिससे सामान्य जनता पहले ही वैदिक धर्म से दूर हो चुकी थी।
एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण बौद्ध भिक्षुओं का आम जनजीवन से दूर हो जाना था। भिक्षु विहारों और मठों तक सीमित रह गए और जनसंपर्क कमजोर पड़ गया। इसके साथ ही पालि भाषा को त्यागकर संस्कृत अपनाना भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना, क्योंकि संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं थी।
समय के साथ बौद्ध मठ और विहार कुरीतियों तथा विलासिता के केंद्र बन गए। भिक्षुओं में अनुशासनहीनता बढ़ी और संघ की नैतिक शक्ति कमजोर हुई। इसके अतिरिक्त, बौद्ध संस्थाओं में अत्यधिक धन संचय हो गया, जिससे वे विदेशी आक्रमणकारियों के आसान लक्ष्य बन गए।
राजकीय संरक्षण का समाप्त होना भी बौद्ध धर्म के पतन का एक बड़ा कारण था। शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन तथा गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, न कि बौद्ध धर्म को। फलस्वरूप बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म न रह सका।
अंततः शैव धर्म से प्रतिस्पर्धा और बंगाल के शासक शशांक द्वारा बोधगया के बोधि वृक्ष को कटवाया जाना बौद्ध धर्म के पतन को और तेज करने वाले कारण बने।
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात् आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में बौद्ध शिक्षाओं को संकलित किया गया, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक धर्मग्रंथ माने जाते हैं। ये तीन भागों में विभाजित हैं— सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक। इनमें सुत्तपिटक का विशेष महत्त्व है क्योंकि इसमें बुद्ध के उपदेशों का विस्तृत संकलन मिलता है।
‘सुत्त’ शब्द का शाब्दिक अर्थ उपदेश या प्रवचन होता है। सुत्तपिटक में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, नैतिक शिक्षाओं तथा दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। इस पिटक की रचना बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद द्वारा की गई मानी जाती है।
सुत्तपिटक को पाँच निकायों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घ निकाय, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम काल, अंतिम उपदेशों, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन मिलता है। दूसरा है मज्झिम निकाय, जिसमें बुद्ध को कहीं साधारण मानव तो कहीं अलौकिक शक्तियों से युक्त दिव्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
तीसरा संयुक्त निकाय है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। इसमें अनेक संयुक्तों का संकलन है तथा मध्यम मार्ग और आष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। चौथा अंगुत्तर निकाय है, जिसमें बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को दिये गए उपदेशों का विवरण मिलता है। इसमें छठी शताब्दी ई.पू. के सोलह महाजनपदों का उल्लेख भी किया गया है।
पाँचवाँ और अंतिम निकाय खुद्दक निकाय है, जो आकार में लघु किंतु विषयवस्तु में अत्यंत व्यापक है। यह भाषा और विषय की दृष्टि से अन्य निकायों से भिन्न है। इस प्रकार सुत्तपिटक बौद्ध धर्म के नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक स्वरूप को स्पष्ट करता है।
बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण में बौद्ध संघ की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित यह संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठित समुदाय था, जिसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना तथा अनुशासित धार्मिक जीवन का पालन करना था।
संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को ‘उपसंपदा’ कहा जाता था। प्रारंभ में संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को ‘श्रमण’ की संज्ञा दी जाती थी। लगभग 10 वर्षों के कठोर अनुशासन और प्रशिक्षण के पश्चात्, जब उसकी योग्यता स्वीकार कर ली जाती थी, तब उसे पूर्ण रूप से ‘भिक्षु’ का दर्जा प्राप्त होता था। इस प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि संघ में प्रवेश सरल नहीं, बल्कि अनुशासन-प्रधान था।
बौद्ध संघ में कुछ व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। इनमें अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, दास तथा गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति सम्मिलित थे। इसका उद्देश्य संघ की पवित्रता, अनुशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना था।
संघ की संरचना गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। इसमें किसी एक व्यक्ति का निरंकुश अधिकार नहीं था, बल्कि सभी निर्णय सामूहिक सहमति से लिये जाते थे। संघ का द्वार सभी जातियों और वर्गों के लिये खुला था, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिये एक क्रांतिकारी कदम था।
संघ की सभा में प्रस्ताव को ‘नत्ति’ कहा जाता था तथा प्रस्ताव के औपचारिक पाठ को ‘अनुसावन’ कहा जाता था। किसी भी सभा की वैध कार्यवाही के लिये न्यूनतम 20 भिक्षुओं की उपस्थिति (कोरम) आवश्यक थी।
इस प्रकार बौद्ध संघ न केवल धार्मिक संस्था था, बल्कि एक सुसंगठित, लोकतांत्रिक और अनुशासित संगठन भी था, जिसने बौद्ध धर्म को दीर्घकाल तक जीवित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्राचीन भारत में जैन धर्म एक सशक्त धार्मिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, किंतु कालांतर में विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रभाव धीरे-धीरे कम होता चला गया। जैन धर्म के पतन के अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक कारण माने जाते हैं।
जैन धर्म में आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं अत्यधिक तपस्या पर विशेष बल दिया गया। संलेखना, उपवास, नग्नता (दिगंबर परंपरा) तथा कठिन आचार-विधानों को सामान्य जन के लिये अपनाना कठिन था। इसके अतिरिक्त, जैन धर्म ने जाति व्यवस्था के दर्शन को पूर्णतः नकारा नहीं, जिससे यह समाज में व्यापक सुधार आंदोलन का रूप नहीं ले सका।
जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। कृषि कार्य में हिंसा की संभावना तथा युद्ध में भाग लेने पर रोक के कारण कृषक और क्षत्रिय वर्ग इससे दूर होता चला गया। परिणामस्वरूप जैन धर्म मुख्यतः व्यापारियों और तपस्वियों तक सीमित रह गया।
जैन दर्शन की दार्शनिक जटिलता भी इसके पतन का एक प्रमुख कारण थी। स्याद्वाद, अनेकांतवाद, कर्म-सिद्धांत और द्वैतवादी तत्त्वज्ञान जैसे गूढ़ सिद्धांत सामान्य जनता के लिये सहज नहीं थे। इससे जैन धर्म जन-आंदोलन बनने के स्थान पर विद्वानों और साधुओं तक ही सीमित रह गया।
प्रारंभ में जैन धर्म एक संगठित आंदोलन था, किंतु बाद में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। फलस्वरूप जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर—दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिये अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और इसकी एकता को कमजोर कर गया।
इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था, जो जनसाधारण की भाषा थी। किंतु बाद में जब जैन ग्रंथों की रचना संस्कृत में होने लगी, तब आम जनता के लिये उन्हें समझना कठिन हो गया। इस भाषायी दूरी ने भी जैन धर्म के प्रसार को सीमित कर दिया। इन सभी कारणों से जैन धर्म धीरे-धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ।
तुलसीदास कामत गोवा मुक्ति आंदोलन के उन साहसी क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने पुर्तगाली अत्याचारों के सामने कभी अपने साहस और देशभक्ति को कम नहीं होने दिया। उनका जन्म गोवा के वोलवोई स्थान पर सन् 1934 में हुआ था। उनके पिता श्री काशीनाथ कामत डाक विभाग में पोस्टमैन थे, जिनसे तुलसीदास ने कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के संस्कार प्राप्त किये। बचपन से ही उनमें साहसिक कार्यों में रुचि थी और युवावस्था तक आते-आते उनमें गोवा को स्वतंत्र देखने की तीव्र चाह बढ़ गयी।
गोवा में स्वतंत्रता संघर्ष दो स्तरों पर चल रहा था—एक ओर खुला राजनीतिक मंच गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस था और दूसरी ओर गोमांतक दल जैसा भूमिगत क्रांतिकारी संगठन। तुलसीदास कामत इसी गोमांतक दल के सक्रिय सदस्य बने। यह दल पुर्तगाली शासन को अस्थिर करने हेतु गुप्त गतिविधियाँ, तोड़-फोड़ और निरंतर प्रतिरोध करता था।
जुलाई 1955 में जब गोमांतक दल की एक टुकड़ी ने सुरले माईस पर साहसिक आक्रमण की योजना बनाई, तो इसका नेतृत्व तुलसीदास कामत को सौंपा गया। इस अभियान में उन्होंने अद्भुत बहादुरी दिखाई, परन्तु संघर्ष के दौरान वे पुर्तगाली सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये।
गिरफ्तारी के बाद जेल में उनसे गोमांतक दल के प्रमुख नेता मोहन रानाडे के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये अत्यधिक यातनाएँ दी गयीं। गंभीर यातनाओं के बावजूद तुलसीदास कामत ने अपने नेता और संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। उनके इस अटल साहस और गोवा की स्वतंत्रता के प्रति समर्पण ने उन्हें सच्चे अर्थों में शहीद बना दिया। यातनाओं की वजह से जेल में ही उनकी मृत्यु हो गयी।
तुलसीदास कामत आज भी गोवा मुक्ति आंदोलन के उन वीरों में गिने जाते हैं जिनकी कुर्बानी ने स्वतंत्र गोवा की नींव को मजबूत किया।
बबला पारब गोवा के उन साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं जिन्होंने गोवा की मुक्ति के लिये निडरता के साथ संघर्ष किया। बबला पारब के पिता का नाम श्री धोंधो पारब था। वे बचपन से ही साहसी कार्यों में रूचि लेते थे और कठिन परिस्थितियों से सामना करने का आत्मविश्वास रखते थे। यही साहस और निडरता आगे चलकर उन्हें गोवा मुक्ति आंदोलन की ओर ले गयी।
जब गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ जनआक्रोश बढ़ा और क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज़ हुईं, तब बबला पारब भी इस संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने आंदोलनों, गुप्त संदेशों और संगठनात्मक गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान अनेक युवा देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर क्रांतिकारी संगठन ‘गोमांतक दल’ और अन्य प्रतिरोध समूहों से जुड़े। बबला पारब भी इन्हीं बहादुर युवाओं में से एक थे।
पुर्तगालियों को बबला पारब की बढ़ती गतिविधियाँ असह्य लगने लगीं। परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए भी उनकी देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिये समर्पण में कोई कमी नहीं आयी। वे अपने साथियों को प्रेरित करते रहे और पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे।
अंततः अगस्त 1956 में पुर्तगाली सैनिक बबला पारब को मोम नामक स्थान पर ले गये। वहाँ बिना किसी मुकदमे, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उन्हें गोलियों से भून डाला गया। उनकी यह निर्मम हत्या पुर्तगाली शासन की बर्बरता को दर्शाती है।
बबला पारब का बलिदान गोवा की स्वतंत्रता के इतिहास में एक अमर अध्याय है। उनका साहस, त्याग और देशप्रेम आज भी गोवा के लोगों को प्रेरणा देता है। वे उन वीर बलिदानियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया।
अर्जुन पिरानकर गोवा के उन साहसी क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने पुर्तगाल की दासता से गोवा को मुक्त कराने के लिये अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनका जन्म सन् 1917 में गोवा के खरपाल गाँव में हुआ था। उनके पिता श्री दाखू पिरानकर एक सामान्य कृषक थे, किन्तु परिवार का वातावरण राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ था। इसी वातावरण ने अर्जुन के भीतर बचपन से ही स्वतंत्रता की चाह और अत्याचार के विरोध की भावना को दृढ़ बना दिया।
युवावस्था में ही उन्होंने पुर्तगाली अत्याचारों को निकट से देखा। गोवा के सामान्य लोगों पर होने वाले जुल्मों ने उनके हृदय को आंदोलित कर दिया। वे अक्सर यह सोचा करते थे कि कब तक गोवा के लोग इस विदेशी शासन को सहन करेंगे। धीरे-धीरे वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गये और गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। अर्जुन पिरानकर अत्यन्त साहसी, चतुर और निडर क्रांतिकारी थे। वे अपने क्षेत्र में पुर्तगाली सैनिकों की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखते थे।
अपने अनेक दिनों के निरीक्षण के बाद उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पुर्तगाली रक्षक दल प्रतिदिन एक ही समय पर एक निश्चित सड़क से होकर गुजरता है। यह सूचना उनके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे किसी दिन बम प्रहार कर उस रक्षक दल पर हमला करेंगे। यह योजना अत्यन्त जोखिमपूर्ण थी, किन्तु अर्जुन पिरानकर ने अपने प्राणों की परवाह किये बिना इसे पूरा करने का संकल्प कर लिया।
19 फरवरी, 1957 को वे एक बम लेकर उस निर्धारित स्थान पर पहुँचे। जैसे ही वे बम को सड़क के किनारे पत्थरों के नीचे छिपा रहे थे, अचानक बम फट गया। इस विस्फोट में घटनास्थल पर ही उनका बलिदान हो गया। अर्जुन पिरानकर का यह बलिदान गोवा की स्वतंत्रता यात्रा में सदा स्मरणीय रहेगा।
रावजी राने गोवा के साहसी और दृढ़निश्चयी स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी स्थान रखते हैं। उनका जन्म गोवा के जुवेम ग्राम में हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर अन्याय और दमन के विरुद्ध विद्रोह की भावना थी। यही कारण था कि आगे चलकर वे गोवा के प्रख्यात क्रांतिकारी नेता दादा राने के अत्यन्त विश्वसनीय सहयोगी बने। दादा राने ने जब पुर्तगाली शासन के विरुद्ध एक संगठित क्रांतिकारी फौज का निर्माण किया, तो रावजी राने को उसका जनरल नियुक्त किया गया। यह पद उनके साहस, नेतृत्व क्षमता और युद्ध-कौशल का प्रमाण था।
जनरल के रूप में रावजी राने ने कई बार पुर्तगाली फौज के खिलाफ साहसिक युद्ध अभियान चलाये। हर अभियान में उन्होंने पुर्तगाली सेना को भारी क्षति पहुँचाई और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रबल किया। उनकी सूझ-बूझ, तेज निर्णय क्षमता और युद्धनीति के कारण गोवा के क्रांतिकारी आंदोलन को अपार प्रेरणा मिली। स्थानीय जनता उन्हें अत्यन्त सम्मान और प्रेम से देखती थी, क्योंकि वह केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि लोगों के रक्षक भी थे।
किन्तु पुर्तगाली शासन इस प्रतिरोध को अधिक समय तक सहन नहीं कर सका। एक दिन जब रावजी राने अकेले नगर की ओर जा रहे थे, तभी पुर्तगाली पुलिस के एक अधिकारी ने उन पर अचानक गोली चला दी। इस विश्वासघाती हमले में रावजी राने शहीद हो गये। उनकी मृत्यु ने सम्पूर्ण गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन को हिला दिया और लोगों के मन में गहरा रोष उत्पन्न कर दिया।
रावजी राने के बलिदान का बदला लेने के लिये उनके साथी क्रांतिकारियों तथा सैनिकों ने उस पुर्तगाली अफसर की हत्या कर दी और उसका घर जला दिया। यह घटना गोवा के संघर्ष को और अधिक उग्र और संगठित बना गई।
रावजी राने की शहादत आज भी साहस, निष्ठा और मातृभूमि के लिये समर्पण का प्रतीक मानी जाती है।
बाला मापारी गोवा के साहसी एवं समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 8 जनवरी, 1929 को गोवा के अस्सोनोरा गाँव में हुआ था। उनके पिता श्रीराम मापारी एक कृषक थे, जिनसे बाला को मेहनत, सादगी और मातृभूमि के प्रति प्रेम की प्रेरणा मिली। जिस समय गोवा पुर्तगाल के दमनकारी शासन में था, तब वहाँ के युवाओं में स्वतंत्रता की तीव्र चाह जाग उठी थी। इसी वातावरण में गोवा के क्रांतिकारियों ने “गोमांतक दल” नामक एक गुप्त संगठन बनाया, जो पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंकने के लिये निरंतर संघर्ष करता था। बाला मापारी इस दल के सक्रिय एवं निष्ठावान सदस्य थे।
गोमांतक दल ने एक साहसिक योजना के तहत अस्सोनोरा पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया। इस आक्रमण में क्रांतिकारियों ने न केवल चौकी पर अधिकार कर लिया, बल्कि वहाँ के विशाल शस्त्रागार पर भी कब्जा कर लिया। यह घटना पुर्तगाली शासन के लिये अत्यधिक अपमानजनक थी। परिणामस्वरूप, भारी संख्या में पुलिस बल भेजकर क्रांतिकारियों पर हमला कराया गया। इसी दौरान बाला मापारी गिरफ्तार कर लिये गये।
गिरफ्तारी के पश्चात् पुर्तगाली पुलिस ने उनसे उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के नाम और ठिकाने बताने का दबाव बनाया; परन्तु बाला मापारी ने अटूट साहस दिखाते हुए कुछ भी बताने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। उन पर अमानवीय अत्याचार किये गये, कठोर यातनाएँ दी गयीं, पर उनकी दृढ़ता और देशभक्ति नहीं डगमगायी। अंततः 18 फरवरी, 1955 को इन अत्याचारों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।
बाला मापारी उन वीर योद्धाओं में से थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर गोवा की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। उनका बलिदान हमेशा गोवा और भारत की स्वतंत्रता-गाथा में उज्ज्वल अक्षरों में अंकित रहेगा।
16वीं सदी के उत्तरार्ध में जब समुद्री अन्वेषणों का युग तेज़ी से बढ़ रहा था, तब यूरोपीय राष्ट्र भारत और पूर्वी द्वीपों के मसालों के व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिस्पर्द्धा में लग गये। इन्हीं देशों में हालैण्ड (डच) भी शामिल था। मसाले—विशेषकर लौंग, जायफल, दालचीनी और काली मिर्च—उस समय यूरोप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते थे और इन्हें सुनहरे व्यापार का प्रतीक समझा जाता था।
भारतीय उपमहाद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीपों की समृद्धि के बारे में सुनकर 1595 ई. में कॉर्नेलिस डी हॉउटमैन एशिया पहुँचा। यही वह यात्रा थी जिसने डचों को एशिया में सक्रिय व्यापारिक शक्ति बनने की दिशा में प्रेरित किया। इसके बाद डच व्यापारियों ने संगठित रूप से व्यापार करने के लिये एक बड़ी कम्पनी बनाने का निश्चय किया।
1602 ई. में डच ईस्ट इंडिया कम्पनी (VOC – Vereenigde Oost-Indische Compagnie) की स्थापना हुई। यह कम्पनी उस समय की सबसे शक्तिशाली व्यापारिक कम्पनियों में से एक बन गयी। इसे एशिया में व्यापार करने, किले बनाने, सैनिक रखने और स्थानीय शासकों से संधि करने का अधिकार दिया गया था।
NCERT के अनुसार डचों का मुख्य उद्देश्य “पूर्वी द्वीपों और भारत में मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना” था। डचों ने भारत के कई तटीय क्षेत्रों में अपने व्यापारिक केंद्र (कारखाने) बनाये। इनमें सूरत, मासुलीपट्टनम, पुलिकट तथा नागपट्टिनम प्रमुख थे। दक्षिण भारत में विशेष रूप से उनकी गतिविधि बहुत तीव्र थी क्योंकि मसालों का बड़ा भाग वहीं से व्यापार होता था।
डचों ने प्रारम्भिक वर्षों में पुर्तग़ालियों को चुनौती दी और मसाला व्यापार पर काफ़ी हद तक नियन्त्रण स्थापित कर लिया। हालाँकि, समय के साथ भारत में उनका प्रभाव कमजोर होता गया और 18वीं सदी के मध्य तक वे धीरे-धीरे ब्रिटिश शक्ति के बढ़ते प्रभाव के सामने पीछे हटने लगे। फिर भी भारतीय व्यापारिक इतिहास में डचों का आगमन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत में यूरोपीय प्रतियोगिता को नया रूप दिया।
बटुकेश्वर दत्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन साहसी क्रांतिकारियों में से थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिये अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म नवम्बर 1908 में कलकत्ता में एक मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद ही उनके मन में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध संघर्ष की चिंगारी प्रज्वलित होने लगी। सन् 1925 में हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गये और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ कार्य करने लगे।
8 अप्रैल 1929 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। इसी दिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधान सभा, दिल्ली में बम फेंककर अंग्रेज़ी शासन को यह संदेश दिया कि भारतवासी अब दमन को सहने वाले नहीं हैं। उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुँचाना नहीं बल्कि ‘बहरों को सुनाने के लिये’ एक शक्तिशाली चेतावनी देना था। घटना के बाद दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और गिरफ्तार कर लिये गये। बाद में उन पर लाहौर षड्यन्त्र मामले में भी आरोप लगाया गया, परंतु सबूतों के अभाव तथा भगत सिंह की टिप्पणी के आधार पर बटुकेश्वर दत्त को रिहा कर दिया गया।
1930 से 1937 तक उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में कठोर यातनाएँ झेली। 1938 में गांधीजी के हस्तक्षेप से उनके खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिहा किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वे जीवन भर संघर्षरत रहे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बटुकेश्वर दत्त ने शांत जीवन व्यतीत किया, परंतु स्वास्थ्य समस्याएँ उन्हें लगातार परेशान करती रहीं। जुलाई 1965 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यद्यपि उनका जीवन अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अमिट और अविस्मरणीय है।
प्रफुल्ल चाकी भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उनका जन्म 10 दिसम्बर 1888 को उत्तरी बंगाल के बोगरा ज़िले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। वे एक मध्यमवर्गीय हिन्दू कायस्थ परिवार से थे। उनके पिता राज नारायण तथा माता स्वर्णमयी अत्यन्त सरल और संस्कारशील व्यक्ति थे। जब प्रफ्फुल केवल 9 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहान्त हो गया। इस कठिन समय में उनकी माता ने अनेक संघर्षों के बीच उनका पालन-पोषण किया और उन्हें शिक्षा दिलाने का हर सम्भव प्रयास किया।
प्रफ्फुल चाकी ने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल होने लगी। कलकत्ता में रहते हुए वे ‘जगंतर’ क्रांतिकारी समूह से प्रभावित हुए और आगे चलकर बिरेन्द्र कुमार घोष जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आये। इस समूह ने ब्रिटिश शासन के अन्याय और क्रूरता के विरोध में सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया था।
उसी समय बिहार के मुज़फ्फरपुर में सेशन जज किंग्सफोर्ड अपने कठोर और दमनकारी आदेशों के लिये कुख्यात था। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि उसकी हत्या करके अंग्रेजी शासन को चेतावनी दी जाये। इस कार्य के लिये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। दोनों ने कई दिनों तक किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर नज़र रखी। परन्तु जानकारी में भ्रम के कारण उन्होंने जिस बग्गी को निशाना बनाया, उसमें किंग्सफोर्ड की जगह दो अन्य अंग्रेज महिलाएँ मौजूद थीं। विस्फोट हुआ और वे मारी गयीं।
इस घटना के बाद पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी। खुदीराम बोस पकड़े गये, परन्तु प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने हेतु स्वयं को गोली मार ली। वे मातृभूमि के लिये शहीद हो गये और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गये।
कर्नल किशन सिंह राठौड़ राजस्थान के उन वीर सपूतों में से एक थे, जिन्होंने अपने साहस, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से भारतीय सेना में विशिष्ट स्थान बनाया। चूरू जिले के घड़सीसर (वर्तमान सरदारशहर) के साधारण से परिवार में जन्मे किशन सिंह राठौड़ बचपन से ही पराक्रम, ईमानदारी और राष्ट्रसेवा की भावना से प्रेरित थे। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने 1 राजपूत/4 गार्ड्स जैसी प्रतिष्ठित इकाइयों में सेवाएँ दीं, जहाँ उनका अनुशासन और नेतृत्व क्षमताएँ जल्दी ही सबके सामने उजागर हो गयीं।
1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में कर्नल राठौड़ ने अदम्य साहस का परिचय दिया। कठिन परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और जोखिमभरी सैन्य चुनौतियों के बीच भी उन्होंने अपने साथियों का मनोबल ऊँचा रखा और दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला किया। युद्धभूमि में उनका नेतृत्व न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण था बल्कि सैनिकों के लिये प्रेरणास्रोत भी बन गया। इसी अद्वितीय वीरता के लिये उन्हें महावीर चक्र जैसे उच्च gallantry award से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी सैन्य क्षमता, राष्ट्रभक्ति और असाधारण साहस का प्रमाण है।
सेना में निरंतर उत्कृष्ट सेवा के फलस्वरूप कर्नल किशन सिंह राठौड़ को 20 अगस्त 1969 को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया। यह पदोन्नति उनके समर्पण, अनुभव और नेतृत्व का स्वाभाविक परिणाम थी। उन्होंने अपने सैनिक जीवन में अनुशासन, टीम भावना और राष्ट्रसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके कार्यों और सिद्धांतों ने कई युवा सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें एक आदर्श सैन्य अधिकारी के रूप में स्थापित किया।
राजस्थान और पूरे देश के लिये कर्नल राठौड़ का योगदान अमूल्य है। वे उन वीरों में शामिल हैं जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से राष्ट्र की रक्षा की और आने वाली पीढ़ियों के लिये प्रेरणा का स्रोत बने। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची वीरता कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण से जन्म लेती है।
पुली थेवर दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती और अत्यन्त साहसी विरोधियों में से एक थे। वे तिरुनेलवेली क्षेत्र के नेल्कातुमसेवल के पोलिगर (स्थानीय सरदार) थे और अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता की अटूट भावना के लिये प्रसिद्ध थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में जब ब्रिटिश शक्ति दक्षिण भारत में फैलने लगी, तब पुली थेवर उन गिने-चुने नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती दखलअंदाजी को खुलकर चुनौती दी।
उनका प्रमुख संघर्ष अर्कोट के नवाब से था, जिसे अंग्रेजों का पूरा समर्थन प्राप्त था। नवाब और कंपनी दोनों ही दक्षिण भारत के पोलिगर सरदारों की स्वायत्तता को समाप्त करना चाहते थे। परन्तु पुली थेवर ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अनेक बार अंग्रेजों तथा नवाबी सेना को युद्धभूमि में कड़ी चुनौती दी।
पुली थेवर की संघर्ष-गाथा में मरुधनायगम (बाद में यूसुफ खान) के साथ उनका टकराव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रारम्भ में मरुधनायगम अंग्रेजों की ओर से दबाव डालने भेजा गया था, परन्तु पुली थेवर की रणनीति, जनसमर्थन और निर्णायक युद्धकौशल ने उसे भी कठोर चुनौती दी। बाद में मरुधनायगम स्वयं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जो उस समय के राजनीतिक संघर्षों की जटिलता को दर्शाता है।
नेल्कातुमसेवल पुली थेवर का मुख्यालय था और यहीं से उन्होंने अपनी प्रतिरोध नीति को संचालित किया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे भारत में अंग्रेजों का संगठित रूप से विरोध करने वाले पहले प्रमुख सरदार थे। उनकी लड़ाई ने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की चेतना को प्रारम्भिक रूप में जागृत किया और आने वाले दशकों में हुए पोलिगर युद्धों की नींव भी रखी।
पुली थेवर का जीवन साहस, स्वाभिमान और विदेशी शासन के विरुद्ध अडिग प्रतिरोध का प्रतीक है। वे भारतीय स्वतंत्रता के उन प्रारम्भिक नायकों में से हैं, जिनके संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिये प्रेरित किया।
सरोजिनी नायडू, जिन्हें प्रेम से “भारत की कोकिला” कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी नेताओं में से एक थीं। उनका जन्म 13 फ़रवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक शिक्षाविद् थे और माता वरदा सुन्दरी कवयित्री थीं। साहित्यिक वातावरण में पली-बढ़ी सरोजिनी बचपन से ही कविता लिखने लगी थीं, और आगे चलकर उन्होंने भारतीय अंग्रेज़ी काव्य को एक विशिष्ट पहचान दिलायी।
सन् 1893 में उन्होंने डॉ. गोविंदराजुलु नायडू से विवाह किया। यह विवाह आपसी सहमति पर आधारित एक आदर्श आधुनिक वैवाहिक उदाहरण माना जाता है। विवाह के बाद भी उन्होंने अपने साहित्यिक और राष्ट्रीय कार्यों को समान रूप से आगे बढ़ाया।
गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन ने उनके राजनीतिक जीवन को दिशा दी। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली अग्रणी महिलाओं में शामिल थीं। राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ती गयी और वे पहली भारतीय महिला बनीं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राजनीतिक दायित्व दिये गये।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 के दांडी मार्च में उनका योगदान उल्लेखनीय था। गांधीजी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भी उन्होंने ही संभाला। सन् 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता का सम्मान मिला, जिससे वह इस पद पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
स्वाधीनता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया। यह पद उन्होंने अपनी मृत्यु (2 मार्च 1949) तक संभाला।
कवयित्री के रूप में उनकी रचनाएँ आज भी भारतीय अंग्रेज़ी साहित्य की महत्त्वपूर्ण धरोहर मानी जाती हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में The Golden Threshold (1905), The Bird of Time (1912), The Broken Wing (1917) और The Feather of the Dawn शामिल हैं।
सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय आंदोलन, महिला सशक्तिकरण और साहित्य—तीनों क्षेत्रों में एक अमिट प्रेरणा बनकर आज भी स्मरण की जाती हैं।
नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव प्राप्त है। वे ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेज़ी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों और स्थानीय शासकों के अधिकारों में हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध किया। कुँवर चैन सिंह का जन्म नरसिंहगढ़ के राजपरिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, धनुर्विद्या और शस्त्र-चालन की शिक्षा प्राप्त की। तेजस्वी व्यक्तित्व और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण वे आम जनता में भी अत्यन्त लोकप्रिय थे।
अंग्रेज़ी सत्ता ने उस समय मध्य भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिये कई रियासतों पर दबाव बनाना आरम्भ कर दिया था। नरसिंहगढ़ भी इस हस्तक्षेप से अछूता नहीं था। अंग्रेज़ों की यही दमनकारी नीति कुँवर चैन सिंह को नागवार गुज़री। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अंग्रेज़ों के आदेशों को मानने से इंकार कर दिया। इससे अंग्रेज़ी शासन को यह आशंका हुई कि यदि एक राजकुमार ने विद्रोह का मार्ग चुना तो अन्य रियासतें भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी हो सकती हैं।
स्थिति बिगड़ने पर उन्हें पकड़ने का आदेश जारी हुआ। कुँवर चैन सिंह ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंग्रेज़ी अत्याचार का प्रतिरोध चुनना उचित समझा। अन्ततः जून 1824 में सिहोर के दशहराबाग मैदान में उन्हें तोप के मुँह पर बाँधकर उड़ा दिया गया। मात्र तीस वर्ष की आयु में उन्होंने देश की स्वतन्त्रता और स्वाभिमान के लिये प्राणों की आहुति दे दी।
कुँवर चैन सिंह की शहादत अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध मध्य भारत में उभरती प्रतिरोध भावना का प्रारम्भिक और अत्यन्त प्रभावशाली उदाहरण है। 1857 से बहुत पहले, 1824 में दिया गया उनका बलिदान यह प्रमाणित करता है कि भारतीयों में परतन्त्रता के प्रति अस्वीकार व स्वतंत्रता की चाह पहले से ही सशक्त रूप ले चुकी थी। आज भी उन्हें मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद के रूप में सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है।
चन्द्रशेखर आज़ाद भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। उनका जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भावरा गाँव में हुआ था। बचपन से ही उनमें अन्याय के प्रति असहमति और देशभक्ति की प्रबल भावना थी। काशी में पढ़ाई के दौरान वे राष्ट्रवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए और यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई।
असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब अदालत में उन्होंने निर्भीक होकर अपना नाम “आज़ाद”, पिता का नाम “स्वतन्त्र” और निवास “जेल” बताया। उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी अंग्रेजों के हाथों जीवित नहीं पकड़े जायेंगे।
वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के प्रमुख सदस्यों में से थे। एचएसआरए का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना था। आज़ाद ने इसी संगठन के माध्यम से कई महत्त्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। 1925 की काकोरी कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने अंग्रेजी शासन को हिला दिया और उन्हें क्रांतिकारी नेतृत्व में एक कठोर, साहसी और रणनीतिक योद्धा के रूप में स्थापित किया।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य अनेक युवा क्रांतिकारी आज़ाद को अपना आदर्श मानते थे। वे उत्कृष्ट निशानेबाज़, तेज़ बुद्धि और अदम्य साहस के प्रतीक थे।
27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। आख़िरी गोली तक लड़ने के बाद उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपने वचन को निभाया—कि वे “आज़ाद” ही मरेंगे।
चन्द्रशेखर आज़ाद का जीवन भारतीय युवाओं के लिये प्रेरणा का स्रोत है। उनका साहस, त्याग और मातृभूमि के लिये समर्पण सदैव भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 19 जुलाई 1827 को जन्मे मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। देशभक्ति, स्वाभिमान और अन्याय के प्रति असहमति उनके स्वभाव का महत्त्वपूर्ण भाग था।
सन् 1857 में कम्पनी ने नई एनफील्ड राइफलें सैनिकों को दीं। इन राइफलों के कारतूस मुँह से काटकर खोलने पड़ते थे और कहा जाता था कि इन्हें चिकना करने के लिये गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। यह बात हिन्दू और मुस्लिम—दोनों धर्मों के लिये आस्था का प्रश्न थी। बेहरामपुर में हुए विरोध और साथियों की चिंताओं ने मंगल पांडे के भीतर विद्रोह की ज्वाला तेज कर दी।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए खुलेआम विद्रोह कर दिया। उन्होंने सैनिकों को अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। इस साहसिक कदम से ब्रिटिश अफसर भयभीत हो उठे और उन्हें रोकने का प्रयास किया। घिर जाने पर मंगल पांडे ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया, परन्तु वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।
इसके बाद उन पर त्वरित कोर्ट मार्शल चलाया गया। 6 अप्रैल 1857 को मुकदमा पूरा किया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में ही उन्हें फाँसी दे दी गयी। उनकी शहादत ने पूरे उत्तर भारत में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी और 1857 का व्यापक विद्रोह भड़क उठा। मंगल पांडे का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनकर हमेशा इतिहास में अमर रहेगा।
डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद ज़िले के पोईअवा गाँव में हुआ था। वे प्रारम्भ से ही अत्यंत मेधावी, सत्यनिष्ठ और देशभक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया और बिहार के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
महात्मा गांधी और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के साथ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभायी। यह आंदोलन किसानों के शोषण के विरुद्ध था और डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह ने किसानों की समस्याओं को समझकर उनके अधिकारों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य किया। वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों — असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि — में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री बने (1946–1957)। उन्होंने बिहार के आर्थिक और शैक्षिक विकास में ठोस सुधार किये। उनके नेतृत्व में कृषि, सिंचाई, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में अनेक योजनाएँ लागू की गईं, जिनसे बिहार की प्रगति की नींव रखी गयी। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले नेता थे, जिन्हें जनता “बिहार विभूति” कहकर सम्मान देती थी।
डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह ने अपने जीवन में हमेशा सत्य, निष्ठा और सेवा के आदर्शों का पालन किया। 5 जुलाई 1957 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी नीतियाँ और कार्य आज भी बिहार के विकास का आधार मानी जाती हैं।
निर्भया आंदोलन भारत में महिला सुरक्षा और न्याय के लिये हुए सबसे बड़े जनआंदोलनों में से एक था। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार और बर्बर हिंसा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना ने भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गहरा आक्रोश पैदा किया।
घटना के बाद देशभर के लोग – विशेष रूप से युवा वर्ग – दिल्ली की सड़कों पर उतर आये। इंडिया गेट और जंतर-मंतर जैसे स्थलों पर लाखों लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किये और दोषियों के लिये फाँसी की माँग की। यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त रूप से सोशल मीडिया और जनसमर्थन के ज़रिये पूरे देश में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के लिये सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, सशक्त कानूनी प्रावधान, और तेज़ न्याय प्रणाली की माँग की।
इस जनदबाव का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने ‘क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2013’ पारित किया, जिसके तहत बलात्कार के लिये सज़ाओं को और कड़ा किया गया तथा नए अपराधों जैसे पीछा करना (stalking), अमर्यादित स्पर्श (sexual harassment) आदि को भी परिभाषित किया गया। इसके अतिरिक्त, न्याय प्रणाली में त्वरित अदालतों (Fast Track Courts) की स्थापना की गयी।
निर्भया आंदोलन ने न केवल भारतीय समाज में महिला सुरक्षा पर संवाद शुरू किया, बल्कि यह देश में लैंगिक समानता की दिशा में एक नयी चेतना लेकर आया। इसने यह संदेश दिया कि समाज की संवेदनशीलता और एकजुटता से परिवर्तन संभव है।
साइलेंट वैली आंदोलन भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन केरल राज्य के पलक्कड़ ज़िले में स्थित साइलेंट वैली के सदाबहार वनों और वहाँ की जैव विविधता को बचाने के लिये शुरू किया गया था। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो दुर्लभ पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है।
1970 के दशक में केरल सरकार ने कुंठिपुझा नदी पर एक जलविद्युत परियोजना (Hydroelectric Project) की योजना बनाई थी। इस परियोजना से लगभग 8.3 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र डूबने की संभावना थी, जिससे अनेक वन्य प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती थीं। इसी के विरोध में स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर आंदोलन आरंभ किया।
इस आंदोलन में के. एन. शेषन, सुंदरलाल बहुगुणा, मधव गाडगिल, और अनेक स्थानीय संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाई। “केरल शास्त्र साहित्य परिषद (KSSP)” ने इस आंदोलन को जन-आंदोलन का रूप दिया। आंदोलनकारियों ने यह स्पष्ट किया कि बिजली परियोजना से पर्यावरण को स्थायी क्षति पहुँचेगी।
लगातार विरोध और वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना को स्थगित कर दिया। बाद में 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान (Silent Valley National Park) घोषित कर दिया गया।
हालाँकि, स्थानीय लोग आज भी सतर्क हैं क्योंकि समय-समय पर नयी परियोजनाओं की योजनाएँ बनती रही हैं। यह आंदोलन भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता का प्रतीक बन गया और इसे भारत के "चिपको आंदोलन" की तरह एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय सफलता माना जाता है।
देवबंद आंदोलन उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के मुसलमानों के धार्मिक पुनरुत्थान का एक प्रमुख आंदोलन था। इसकी स्थापना 1866 में मुहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के देवबंद नगर में की गयी। इसी वर्ष यहाँ दारुल उलूम देवबंद नामक एक मदरसा स्थापित किया गया, जिसने आगे चलकर इस आंदोलन का केंद्र रूप धारण किया।
देवबंद आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज को कुरान और हदीस की वास्तविक शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के लिये प्रेरित करना था। यह आंदोलन सूफी भक्ति प्रथाओं और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध करता था। देवबंदी विद्वानों का मानना था कि मुसलमानों को अपनी आस्था और नैतिकता को मज़बूत करते हुए, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से बचना चाहिये।
यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन (सर सैयद अहमद ख़ाँ द्वारा संचालित) के विचारों से भिन्न था। जहाँ अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक अंग्रेज़ी शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान पर बल देता था, वहीं देवबंद आंदोलन परम्परागत इस्लामी शिक्षा और नैतिक सुधार पर केंद्रित था।
राजनीतिक दृष्टि से भी देवबंदी नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्य भी है।
इस प्रकार, देवबंद आंदोलन न केवल एक धार्मिक पुनरुत्थान का प्रतीक था बल्कि यह भारत में इस्लामी शिक्षण और स्वतंत्रता की चेतना के प्रसार का भी केंद्र बन गया।
राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम महान नेता और भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव, मूर्तिपूजा, सामाजिक रूढ़ियों और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। वे पूर्वी और पश्चिमी विचारों के समन्वय के समर्थक थे और एकेश्वरवाद के प्रचारक थे। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं का केंद्र बनी। उन्होंने हिंदू कॉलेज (1817), इंग्लिश स्कूल और वेदांत कॉलेज (1825) की स्थापना में योगदान दिया, जिससे आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।
1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार और हिंदू धर्म का शुद्धिकरण था। इसने मूर्तिपूजा, सती प्रथा और सामाजिक अन्याय की आलोचना की तथा मानवता और तर्क को सर्वोच्च माना। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली अनुवाद कर एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रसारित किया। राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी थे। उनके संवाद कौमुदी (1821) और मिरात-उल-अखबार (1822) पत्रों ने सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन की आलोचना के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना को जगाया।
उनके सहयोगी डेविड हरे, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर और ताराचंद चक्रवर्ती थे। धर्म सभा जैसे रूढ़िवादी संगठनों ने उनका विरोध किया, किंतु उन्होंने समाज सुधार की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। बाद में देवेन्द्रनाथ टैगोर और केशवचंद्र सेन ने ब्रह्मो आंदोलन को आगे बढ़ाया। राजा राममोहन राय का योगदान भारतीय समाज में आधुनिकता, तर्कवाद, शिक्षा और धार्मिक सुधार की आधारशिला रखने वाला था, जिसके कारण उन्हें "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा जाता है।
मप्पिला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में ज़मींदारी-विरोधी और सरकार-विरोधी था, किन्तु बाद में इसने सांप्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख सहभागी मप्पिला मुसलमान किसान (मोपला) थे, जो अपने ज़मींदारों और ब्रिटिश प्रशासन दोनों से असंतुष्ट थे।
विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि नंबूदिरी ब्राह्मण ज़मींदारों द्वारा मप्पिला काश्तकारों का अत्यधिक शोषण किया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्नीसवीं सदी में लागू किये गये नये भूमि कानूनों ने ज़मींदारों को भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया, जिससे मोपला किसान अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित हो गये। यह अन्याय वर्षों तक उनके भीतर असंतोष को बढ़ाता गया।
1920 में मंजेरी में मालाबार जिला कांग्रेस समिति ने किरायेदार किसानों के अधिकारों का समर्थन किया और मकान मालिक-किरायेदार संबंधों को विनियमित करने के लिये कानून की मांग की। इससे मप्पिला किसानों में आंदोलन के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ।
अगस्त 1921 में एरनाड और वलुवनाड तालुकों में यह विद्रोह हिंसक रूप में भड़क उठा। बताया जाता है कि इस विद्रोह में लगभग 10,000 लोग मारे गये। कई स्थानों पर हिंदू जमींदारों और सामान्य हिंदू नागरिकों पर हमले हुए और धर्म परिवर्तन के लिये दबाव बनाया गया।
विद्रोह के दमन के दौरान एक दर्दनाक घटना घटी — जब मोपला कैदियों को पोदनूर के केंद्रीय कारागार ले जाया जा रहा था, तो बंद रेल डिब्बे में दम घुटने से सैकड़ों कैदियों की मौत हो गयी। यह घटना इतिहास में “वैगन त्रासदी (Wagon Tragedy)” के नाम से प्रसिद्ध हुई।
ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिये मार्शल लॉ लागू किया और मालाबार स्पेशल पुलिस नामक विशेष बल का गठन किया। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में किसान असंतोष, धार्मिक उग्रता और औपनिवेशिक दमन का मिश्रित प्रतीक बन गया।
दक्कन दंगे वर्ष 1875 में महाराष्ट्र के पूना, सतारा और अहमदनगर जिलों में हुए। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के अधीन किसानों द्वारा स्थानीय साहूकारों और प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध किया गया एक महत्त्वपूर्ण ग्रामीण आंदोलन था।
विद्रोह का कारण:
दक्कन दंगों का मूल कारण रैयतवारी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत किसान सीधे सरकार को भूमि-राजस्व चुकाते थे। परंतु समय के साथ यह व्यवस्था किसानों के लिये अत्यंत बोझिल साबित हुई। जब अकाल या फसल खराबी होती, तब भी उन्हें पूरा लगान देना पड़ता। इससे वे धीरे-धीरे साहूकारों (मुख्यतः वानियों) के ऋण पर निर्भर हो गये। अदालतों और नये कानूनों ने साहूकारों के पक्ष में निर्णय देना शुरू किया, जिससे किसानों और साहूकारों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक दूरी बढ़ती गयी।
विद्रोह का विकास:
1875 में कुनबी किसानों ने वानियों के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया। वे साप्ताहिक बाजारों में एकत्र होकर साहूकारों के घरों पर हमला करते, उनके बंधक बांड, ऋण पत्र और भूमि स्वामित्व के दस्तावेज जला देते थे। यह आंदोलन संगठित रूप में पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र में फैल गया।
ब्रिटिश प्रतिक्रिया और परिणाम:
ब्रिटिश सरकार ने पहले कठोर दमन किया, परंतु बाद में इस विद्रोह के गहरे आर्थिक कारणों को समझा। परिणामस्वरूप, किसानों की स्थिति सुधारने के लिये "दक्कन कृषक राहत अधिनियम" (Deccan Agriculturists’ Relief Act), 1879 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य किसानों को साहूकारों की मनमानी और शोषण से बचाना था।
निष्कर्ष:
दक्कन दंगे भारतीय किसान आंदोलनों का प्रारंभिक स्वरूप थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के खिलाफ ग्रामीण समाज की असंतोष भावना को उजागर किया। यह आंदोलन भविष्य के किसान संघर्षों की नींव बन गया।
रानी गाइदिन्ल्यू का नागा आंदोलन (1930 का दशक)
रानी गाइदिन्ल्यू का नागा आंदोलन उत्तर-पूर्व भारत के मणिपुर राज्य के ज़ेलियांगरोंग क्षेत्र में उभरा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति और नागा स्वशासन की स्थापना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक के अंत में हैपो जादोनांग ने की थी। जादोनांग के 1931 में ब्रिटिशों द्वारा फांसी दिए जाने के बाद, उनकी चचेरी बहन गाइदिन्ल्यू ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला।
1915 में मणिपुर के लुआंगकाओ गांव में जन्मी गाइदिन्ल्यू मात्र 13 वर्ष की आयु में हेराका आंदोलन से जुड़ीं, जो पारंपरिक नागा धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान पर केंद्रित था। उन्होंने ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों द्वारा नागाओं के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया। उनका आंदोलन नागा जनजातियों के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राजनीतिक आत्मनिर्णय का प्रतीक बन गया।
गाइदिन्ल्यू गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित थीं; उन्होंने ब्रिटिश करों का भुगतान करने से इनकार किया और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जन-आंदोलन चलाया। ब्रिटिश सरकार ने उनके आंदोलन को विद्रोह घोषित कर दिया और 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी।
1937 में जवाहरलाल नेहरू ने उनसे जेल में मुलाकात की और उन्हें "रानी गाइदिन्ल्यू" की उपाधि दी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें रिहा किया गया। रानी गाइदिन्ल्यू को स्वतंत्रता संग्राम की महान जननायिका और नागा स्वाभिमान की प्रतीक माना जाता है।
चुआर विद्रोह (1767-1802) छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानों के बीच के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा आदिवासी समुदायों की जमीनों पर कब्ज़ा करना और उनके पारंपरिक अधिकारों को छीनना था। आदिवासियों ने जब महसूस किया कि उनकी आज़ादी और जीविकोपार्जन के साधन खतरे में हैं, तो उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए।
विद्रोह की प्रकृति अत्यंत संघर्षपूर्ण और संगठित थी। आदिवासियों ने सीधा मुकाबला करने के बजाय गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने स्थानीय ज्ञान और जंगलों का उपयोग करते हुए अंग्रेजों की सेनाओं पर अचानक हमले किए और फिर गायब हो जाते थे। यह युद्ध केवल भौतिक संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बचाने की लड़ाई भी शामिल थी।
1798 तक यह विद्रोह अपने चरम पर पहुँच गया। आदिवासियों की दृढ़ता और साहस के कारण अंग्रेजों को कई क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चुआर विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति आदिवासियों की असंतोष और उनकी स्वतंत्रता की इच्छा को स्पष्ट रूप से दिखाया। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरणों में एक महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है, जिसने बाद में अन्य क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिरोध और विद्रोहों को प्रेरित किया।
यह विद्रोह आदिवासियों की भूमि, आज़ादी और जीवनशैली के संरक्षण के लिये उनकी साहसपूर्ण लड़ाई का प्रतीक है।
अभिरुचि मानव व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को विशेष कार्यों, विषयों या गतिविधियों की ओर आकर्षित करती है। अभिरुचि व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालती है, चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत विकास हो।
मानव जीवन में अभिरुचियों का विकास जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह अनुभव, परिवेश, शिक्षा और संस्कारों से विकसित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को आनंद और उत्साह के साथ करता है, तो यह उसकी अभिरुचि का परिणाम होता है। उदाहरण के लिये, किसी को संगीत में रुचि होती है, तो किसी को खेल, पठन-पाठन, विज्ञान या चित्रकला में।
अभिरुचियाँ न केवल व्यक्ति को कार्य में प्रेरणा देती हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और संतोष भी प्रदान करती हैं। यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने और सही दिशा में प्रयत्न करने में सहायता करती हैं। यदि किसी व्यक्ति की अभिरुचि और उसका कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से मेल खाते हैं, तो वह सफलता और संतुष्टि दोनों प्राप्त करता है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी अभिरुचियों का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों की अभिरुचि को पहचानकर उन्हें उचित मार्गदर्शन देना शिक्षक का कर्तव्य है। इस प्रकार, अभिरुचियाँ मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक और आनंदमय बनाती हैं। यह कहा जा सकता है कि अभिरुचि ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिये प्रेरित करती है।
- नेपाल का प्राचीन राज्य गंडक तथा कोसी नदियों के बीच में स्थित था।
- नेपाल पर सर्वप्रथम गोपालक वंश ने शासन किया था, जिसमें 8 राजा हुए थे। इसके बाद यहाँ आभीर वंश ने शासन किया। आभीरों के बाद शासन सत्ता किरातों के हाथों में आई और यहाँ 29 किरात राजाओं के शासन करने का उल्लेख मिलता है।
- नेपाल में अंशुवर्मा ने ‘वैश्वठाकुरीवंश’ की स्थापना की थी।
- अंशुवर्मा लिच्छवि ‘शिवदेश प्रथम’ का सामंत था।
- उसने स्वतंत्र स्थिति प्राप्त कर ‘महाराजाधिराज’ की उपाधि धारण की थी।
- अंशुवर्मा ने संभवतः 643 ई. तक शासन किया था ह्वेनसांग उसे ‘हाल का राज’ बताता है।
- 9वीं सदी के अंत तक नेपाल एक स्वतंत्र राज्य हो गया और इसी समय (लगभग 879 ई.) में नेपाल संवत का शुभारंभ किया गया था।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Operation Blackboard) कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1987 में हुआ था।
यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देशभर के प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना था, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके।
मुख्य उद्देश्य:
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कक्षाएँ और आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।
- लड़कियों और लड़कों के लिये अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करना।
- कम से कम 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।
- बच्चों को निरंतर और समग्र मूल्यांकन के माध्यम से उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना।
इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री, जैसे चार्ट, मानचित्र, विज्ञान और गणित किट, आदि प्रदान किये । इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यालयों में बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिये भी सहायता दी गई।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जिसे छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहा जाता है, रोज़गार की वह स्थिति है जहाँ श्रमिक तो काम पर लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य या लगभग शून्य होती है।
सरल शब्दों में :
- यदि किसी काम से कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए, तो भी उत्पादन के कुल स्तर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- इसका अर्थ यह है कि उस काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं।
मुख्य विशेषताएँ
- उत्पादकता : इस प्रकार की बेरोज़गारी में, श्रमिकों का सीमांत योगदान (यानी एक अतिरिक्त श्रमिक का उत्पादन में योगदान) शून्य होता है।
- दिखावटी रोज़गार : श्रमिक सतह पर 'रोज़गार प्राप्त' दिखते हैं, लेकिन वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। यह अल्प-रोज़गार (Underemployment) का एक रूप है।
- सामान्य क्षेत्र : यह समस्या भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, जहाँ एक ही छोटे खेत पर परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, भले ही उतने लोगों की आवश्यकता न हो।
उदाहरण : एक खेत पर पाँच लोगों की ज़रूरत है, लेकिन परिवार के आठ सदस्य काम कर रहे हैं। यदि तीन लोगों को हटा दिया जाए, तो भी फसल का उत्पादन उतना ही रहेगा। ये तीन अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार माने जाएँगे।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके तहत कंपनियाँ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने व्यावसायिक संचालन और हितधारकों के साथ अपनी बातचीत में एकीकृत करती हैं। यह व्यापार के माध्यम से लाभ कमाने के साथ-साथ समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का एक स्वैच्छिक और अब कानूनी रूप से बाध्यकारी तरीका है।
भारत में कानूनी अनिवार्यता
भारत CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश है। यह अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 द्वारा शासित है।
लागू होने के मानदंड
CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जो किसी भी वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित तीन वित्तीय मानदंडों में से कोई भी एक पूरा करती हैं :
- शुद्ध संपत्ति (Net Worth) : ₹500 करोड़ या उससे अधिक, या
- वार्षिक कारोबार (Turnover) : ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक, या
- शुद्ध लाभ (Net Profit) : ₹5 करोड़ या उससे अधिक।
व्यय की बाध्यता (Spending Obligation) :
पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी इस राशि को खर्च करने में विफल रहती है, तो उसे इसका कारण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताना होता है।
प्रशासनिक संरचना और अनुमत गतिविधियाँ
- CSR समिति (CSR Committee) :
अधिनियम कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में एक CSR समिति गठित करने का निर्देश देता है। इस समिति का मुख्य कार्य है :- एक CSR नीति तैयार करना और उसे बोर्ड को अनुशंसित करना।
- समय-समय पर कंपनी की CSR गतिविधियों की निगरानी करना।
- CSR के तहत अनुमत गतिविधियाँ (अनुसूची VII) :
कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों की एक विस्तृत सूची दी गई है जहाँ CSR निधि का उपयोग किया जा सकता है। इन गतिविधियों में शामिल हैं :- सामाजिक विकास : चरम भुखमरी और निर्धनता का उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य : एचआईवी-एड्स और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना (स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना)।
- पर्यावरण : पर्यावरणीय संवहनीयता, पारिस्थितिक संतुलन और वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय कोष : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सहित केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत कोषों में योगदान करना।
इस कानूनी ढाँचे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियाँ केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि समावेशी विकास और सतत पर्यावरण के निर्माण में भी सक्रिय भागीदार बनें।
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (Goods and Services Tax Appellate Tribunal - GSTAT) एक वैधानिक निकाय है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया है। यह जीएसटी (GST) प्रणाली से संबंधित विवादों के लिये एक विशेष और स्वतंत्र अपीलीय मंच के रूप में कार्य करता है।
- GSTAT का उद्देश्य
GSTAT का मूल उद्देश्य करदाताओं को अपील करने के लिये एक विशेषीकृत और स्वतंत्र मंच प्रदान करके GST प्रणाली में व्यवस्था, विश्वसनीयता और पूर्वानुमेयता को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य पूरे भारत में जीएसटी विवादों के लिये एक एकीकृत अपीलीय मंच तैयार करना है। यह जीएसटी कानूनों की व्याख्या में कानूनी टकराव और अस्पष्टता को कम करने में मदद करता है। - कार्यप्रणालियाँ और संरचना
GSTAT को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच और सुसंगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिये एक विशिष्ट संरचना पर डिज़ाइन किया गया है :- संचालन का विस्तार : GSTAT का संचालन नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ (Principal Bench) और देशभर में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों (State Benches) के माध्यम से किया जाता है।
- पीठ की संरचना : प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक केंद्रीय तकनीकी सदस्य और एक राज्य तकनीकी सदस्य होते हैं। यह संयोजन न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञता का समन्वय करता है ताकि निष्पक्ष और सुसंगत निर्णय दिए जा सकें।
- तीन 'S' सिद्धांत : GSTAT को निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है :
- Structure (संरचना) : न्यायिक + तकनीकी विशेषज्ञता का मिश्रण।
- Scale (विस्तार) : राज्य पीठों और सरल मामलों के लिये एकल सदस्यीय पीठों के माध्यम से राष्ट्रीय पहुँच।
- Synergy (समन्वय) : प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और मानवीय विशेषज्ञता का उपयोग।
- डिजिटल पहुँच : GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल करदाताओं और प्रैक्टिशनरों के लिये ऑनलाइन दाखिला, मामले की ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है।
- लाभ और प्रभाव
GSTAT भारतीय कर प्रणाली में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है :- न्याय की गति : यह बड़े और छोटे दोनों प्रकार के करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे न्याय में अनावश्यक देरी नहीं होती।
- समानता और निश्चितता : यह कानूनों की व्याख्या में अस्पष्टता को कम करता है और पूरे भारत में समानता और सुसंगतता सुनिश्चित करता है।
- व्यावसायिक विश्वास : यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और MSMEs, निर्यातकों, स्टार्टअप्स तथा नागरिकों के लिये कर अनुपालन को सरल बनाता है।
भारत का चाय बाज़ार वैश्विक स्तर पर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जो उत्पादन, उपभोग और निर्यात तीनों क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी है।
उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र
भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक चाय आपूर्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। देश में कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% निम्नलिखित चार राज्यों से आता है: असम (असम घाटी और कछार सहित), पश्चिम बंगाल (दुआर, तराई और प्रसिद्ध दार्जिलिंग क्षेत्र), तमिलनाडु और केरल।
उपभोग और निर्यात की स्थिति
भारत न केवल एक बड़ा उत्पादक है, बल्कि यह चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जो अपने उत्पादन का लगभग 80% घरेलू स्तर पर उपयोग करता है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग 840 ग्राम है।
उपभोग में अग्रणी होने के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, जो केन्या (शीर्ष निर्यातक) और चीन से पीछे है। भारत अपनी चाय का निर्यात 25 से अधिक देशों में करता है, जिनमें प्रमुख आयातक रूस, ईरान, UAE, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन शामिल हैं।
भारत के चाय निर्यात का लगभग 96% ब्लैक टी (काली चाय) है। अन्य निर्यातित प्रकारों में रेगुलर टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी और लेमन टी शामिल हैं। यह संरचना दर्शाती है कि भारत का बाज़ार मुख्य रूप से विशाल घरेलू मांग द्वारा संचालित होता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण चाय के निर्यात में भी यह एक प्रमुख स्थान रखता है।
विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के रूप में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी घटाना और सतत समाधान अपनाकर साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है।
संरचना : पाँच प्रमुख स्तंभ
विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी साझेदारी है, जो मिलकर कार्य करते हैं:
- IBRD – International Bank for Reconstruction and Development मध्यम-आय वाले और ऋण-योग्य गरीब देशों को दीर्घकालिक ऋण और विश्लेषणात्मक सेवाएँ देता है।
- IDA – International Development Association दुनिया के सबसे गरीब देशों को ब्याज-मुक्त ऋण (क्रेडिट) और अनुदान प्रदान करता है।
- IFC – International Finance Corporation विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency निवेश को बढ़ावा देने के लिये राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा उपलब्ध कराता है।
- ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes निवेशक और राज्य के बीच विवादों का समाधान करता है। (नोट : भारत इसका सदस्य नहीं है।)
सदस्यता और वोटिंग अधिकार
विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। वोटिंग अधिकार सदस्य देशों की शेयरधारिता पर निर्भर करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है, जिसके पास 16.41% वोट हैं।
प्रमुख रिपोर्टें
विश्व बैंक कई प्रभावशाली रिपोर्टें प्रकाशित करता है जो वैश्विक विकास को ट्रैक करती हैं, जैसे:
- मानव पूंजी सूचकांक
- विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)
(पहले यह Ease of Doing Business Report भी प्रकाशित करता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है।)
मलक्का जलडमरूमध्य दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह अंडमान सागर (हिंद महासागर) को दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) से जोड़ता है। इसके पश्चिम में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप तथा पूर्व में प्रायद्वीपीय (पश्चिम) मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड स्थित हैं। जलडमरूमध्य की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसके सबसे संकरे भाग की चौड़ाई मात्र 2.8 किलोमीटर है। यह इसे वैश्विक समुद्री व्यापार के दृष्टिकोण से एक "स्ट्रेटेजिक चोकपॉइंट" बनाता है।
- सामरिक महत्त्व
- मलक्का जलडमरूमध्य को मध्य-पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग माना जाता है।
- यह मार्ग एशिया, मध्य-पूर्व और यूरोप के बीच परिवहन की लागत और समय दोनों को कम करता है।
- वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60 प्रतिशत मालवाहन इसी गलियारे से होकर गुजरता है।
- ऊर्जा के क्षेत्र में इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह चीन और जापान जैसे एशिया के बड़े उपभोक्ता देशों तक तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का प्रमुख माध्यम है।
- सामरिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार की अवरोधक स्थिति (Blockade) से वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
भारत के लिये यह जलडमरूमध्य सामरिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की व्यापारिक और सुरक्षा रणनीतियों में इसका प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से भारत ने वर्ष 2001 में अंडमान और निकोबार कमान (ANC) की स्थापना की। यह कमान भारत की पहली और एकमात्र त्रि-सेवा (Tri-Services) कमान है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और मलक्का जलडमरूमध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना और किसी भी संकट की स्थिति में सैन्य संपत्तियों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित करना है।
इस प्रकार, मलक्का जलडमरूमध्य केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और सामरिक संतुलन के लिहाज से भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
फिनटेक (FinTech), यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी, उन तकनीकी नवाचारों को कहते हैं जो वित्तीय सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाते हैं। भारत में यूपीआई (Unified Payments Interface) ने फिनटेक के इस परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे देश डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। यूपीआई ने लेन-देन को इतना सरल, तेज और सुरक्षित बना दिया है कि यह सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन गया है।
यूपीआई का प्रभाव और महत्त्व
- सरलता और सुगमता : यूपीआई ने स्मार्टफोन के माध्यम से तत्काल, 24x7 और सुरक्षित भुगतान को संभव बनाया है। क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर दर्ज करके, कोई भी व्यक्ति आसानी से पैसे भेज या प्राप्त कर सकता है।
- वित्तीय समावेशन : यूपीआई ने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, खासकर उन लोगों को जो पहले डिजिटल लेन-देन से दूर थे। इसने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है।
- नवाचार का केंद्र : यूपीआई ने कई नए फिनटेक स्टार्टअप्स को जन्म दिया है, जैसे कि PhonePe, Google Pay, और Paytm, जिन्होंने विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करके एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है।
- वैश्विक प्रभाव : भारत का यूपीआई मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिये एक प्रेरणा बन गया है। यह अन्य देशों को अपनी स्वयं की तेज़ और कम लागत वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है, जिससे भारत फिनटेक नवाचार में एक अग्रणी के रूप में स्थापित हो रहा है।
संक्षेप में, यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जिसने भारत के वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को गति दी है।
मैसनर प्रभाव एक ऐसी घटना है जो सुपरकंडक्टर्स (अतिचालकों) में देखी जाती है। जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान (critical temperature) से नीचे ठंडा किया जाता है, तो वह अपनी सुपरकंडक्टिंग अवस्था में पहुँच जाता है। इस अवस्था में, वह पदार्थ न केवल अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह खो देता है, बल्कि अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को भी पूरी तरह बाहर निकाल देता है।
मुख्य बिंदु
- आदर्श डायामैग्नेटिज्म : मैसनर प्रभाव के कारण, एक सुपरकंडक्टर एक आदर्श डायामैग्नेटिक (diamagnetic) पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। इसका अर्थ है कि वह अपने ऊपर लगाए गए किसी भी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से विकर्षित करता है।
- चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन : यह प्रभाव प्रतिरोध के शून्य होने से अलग है। भले ही पदार्थ में कोई विद्युत प्रतिरोध न हो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन केवल सुपरकंडक्टिंग अवस्था में ही होता है। यही कारण है कि यह प्रभाव सुपरकंडक्टर्स की एक परिभाषित विशेषता है।
- लेविटेशन (उत्प्लावन) : मैसनर प्रभाव का सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन मैग्नेटिक लेविटेशन (चुंबकीय उत्प्लावन) है। जब एक सुपरकंडक्टर को एक चुंबक के पास लाया जाता है, तो सुपरकंडक्टर अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर धकेल देता है, जिससे दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह बल इतना शक्तिशाली होता है कि चुंबक सुपरकंडक्टर के ऊपर हवा में तैरने लगता है।
मैसनर प्रभाव सुपरकंडक्टर्स के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण खोज थी, जिसने उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद की।
डॉक्ट्रिन ऑफ रिपगनेंसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 से संबंधित एक सिद्धांत है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब समवर्ती सूची (Concurrent List) में दिये गए किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में आपस में टकराव या विरोध (repugnancy) होता है।
सिद्धांत का उद्देश्य और कार्यप्रणाली
इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने की शक्तियों में समन्वय बना रहे। इसकी कार्यप्रणाली को दो मुख्य भागों में समझा जा सकता है-
- सामान्य नियम : यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद के किसी कानून से विरोध करता है, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक अमान्य हो जाएगा जहाँ तक वह केंद्रीय कानून का विरोध करता है।
- अपवाद : यदि किसी राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई हो, तो वह केंद्रीय कानून के बावजूद भी उस राज्य में लागू रह सकता है। हालाँकि, संसद अभी भी उसी विषय पर एक नया कानून बना सकती है जो राज्य के कानून को रद्द या संशोधित कर सकता है।
डॉक्ट्रिन ऑफ रिपगनेंसी भारत की संघीय संरचना को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में एक समान कानूनी ढाँचा बना रहे, विशेषकर उन विषयों पर जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता और केंद्र सरकार की विधायी शक्तियों को बनाए रखता है, जबकि राज्यों को भी कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करता है।
न्यूरल नेटवर्क सिद्धांत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक मूल आधार है जो मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके से प्रेरित है। इसमें कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बनाया जाता है जो आपस में जुड़े होते हैं। ये न्यूरॉन कई परतों के माध्यम से जानकारी को प्रोसेस करते हैं।
न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है?
यह सिद्धांत एक सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है :
- इनपुट लेयर (Input Layer) : इस परत में डेटा या जानकारी इनपुट के रूप में प्रवेश करती है। यह परत बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करती है।
- हिडन लेयर्स (Hidden Layers) : इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में कई छिपी हुई परतें होती हैं। ये परतें इनपुट डेटा का विश्लेषण और प्रोसेसिंग करती हैं, जिससे जटिल पैटर्न को पहचाना जा सके।
- आउटपुट लेयर (Output Layer) : यह अंतिम परत है जो नेटवर्क के निष्कर्ष या निर्णय को प्रस्तुत करती है।
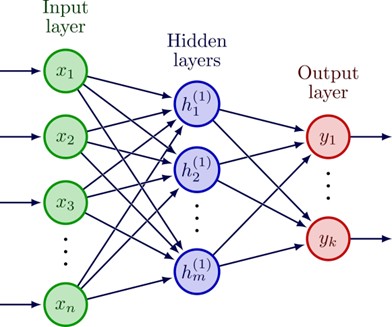
नेटवर्क इनपुट डेटा से सीखता है और धीरे-धीरे अपने कनेक्शनों को समायोजित करता है ताकि सबसे सटीक आउटपुट दिया जा सके।
न्यूरल नेटवर्क के अनुप्रयोग
यह सिद्धांत कई आधुनिक तकनीकों के लिये महत्त्वपूर्ण है :
- पैटर्न पहचान : इसका उपयोग चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट और हस्तलिखित अक्षरों को पहचानने में किया जाता है।
- चित्र और आवाज़ की समझ : यह Siri और Alexa जैसे वॉइस असिस्टेंट और गूगल फोटोज जैसे ऐप्स में चित्रों को समझने में मदद करता है।
- भविष्यवाणी और निर्णय लेना : वित्तीय बाज़ारों में स्टॉक की कीमतों का अनुमान लगाने या मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिये भी इसका उपयोग होता है।
- रोबोटिक्स और स्वचालन : रोबोट को सीखने और अपने पर्यावरण के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
न्यूरल नेटवर्क हमें जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, जिनके लिये पारंपरिक प्रोग्रामिंग विधियाँ अपर्याप्त होती हैं। यह AI को और अधिक बुद्धिमान और व्यावहारिक बनाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे "उत्सवों का उत्सव" (Festival of Festivals) भी कहा जाता है। 2000 में शुरू हुआ यह महोत्सव, राज्य की 17 जनजातियों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं को एक साथ लाता है।
क्यों खास है यह उत्सव?
इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह पक्षी नागाओं के लिये पवित्र और पूजनीय है, जो उनके लोकगीतों और लोककथाओं का हिस्सा है।
- जीवंत संस्कृति का प्रदर्शन : हॉर्नबिल महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि नागा संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ पारंपरिक योद्धा, अपनी पूरी पोशाक में, विजय, प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित नृत्य और युद्धघोष (war cries) करते हैं। उनकी पोशाक में हॉर्नबिल के पंख, सूअर के दाँत और रंगीन बुनी हुई पट्टियाँ होती हैं, जो उनकी पहचान और गर्व का प्रतीक हैं।
- पर्यटन का केंद्र : यह राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2023 में, 1.5 लाख से अधिक लोग इस उत्सव में शामिल हुए, जिनमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में थे।
हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की जनजातीय एकता और संस्कृति को दर्शाता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ नागा लोग अपनी पहचान और परंपराओं को गर्व के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह महोत्सव परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है, जो हर किसी को एक अविस्मरणीय अनुभव देता है।
कस्तूरी कॉटन भारत पहल कपड़ा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय कपास की ट्रेसबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग को बढ़ाना है। यह भारत सरकार (कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया), व्यापार निकायों और उद्योगों के बीच एक संयुक्त प्रयास है।
- पहल के मुख्य बिंदु
- उद्देश्य : इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय कपास की गुणवत्ता, पारदर्शिता और पहचान को सुनिश्चित करना है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग : एंड-टू-एंड ट्रेसबिलिटी और लेनदेन प्रमाणन के लिये एक माइक्रोसाइट विकसित की गई है, जिसमें क्यूआर कोड सत्यापन और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। यह तकनीक कपास की यात्रा को खेत से लेकर अंतिम उत्पाद तक ट्रैक करने में मदद करती है।
- प्रचार और फंडिंग : इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिये धन का आवंटन राज्य-विशिष्ट न होकर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।
- पंजीकृत इकाइयाँ : अब तक, लगभग 343 आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयाँ इस पहल के तहत पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से 15 इकाइयाँ आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश से लगभग 100 तरह की गाँठों को 'कस्तूरी कॉटन भारत' ब्रांड के तहत प्रमाणित किया गया है।
- कपास का महत्त्व : भारत में कपास एक महत्त्वपूर्ण फसल है, जो वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान देती है। इसे इसके आर्थिक मूल्य के कारण "व्हाइट-गोल्ड" भी कहा जाता है। कपास गर्म और धूप वाले मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता है, लेकिन यह जलभराव के प्रति संवेदनशील होता है।
यह पहल भारतीय कपास को वैश्विक बाज़ार में एक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
पोषण मानव शरीर के संचालन और स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण है। यह शरीर को आवश्यक ऊर्जा, विकास, मरम्मत, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पोषण की आवश्यकता को संतुलित आहार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पोषण की प्रमुख आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं :
- कार्बोहाइड्रेट्स :
- ऊर्जा का मुख्य स्रोत
- स्रोत : अनाज, फल, सब्जियाँ, दालें
- प्रोटीन :
- शरीर की वृद्धि, मरम्मत, एंजाइम व हार्मोन के उत्पादन में सहायक
- स्रोत : दालें, बीन्स, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद
- वसा :
- ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, शरीर के अंगों की सुरक्षा में सहायक
- स्रोत : तेल, घी, मक्खन, नट्स, बीज
- विटामिन्स :
- शरीर के विभिन्न कार्यों के लिये आवश्यक कार्बनिक यौगिक
- स्रोत : फल, सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, अनाज
- मिनरल्स :
- हड्डियों, दाँतों, और कोशिकाओं के सही संचालन के लिये आवश्यक
- स्रोत : डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मीट, अनाज
- पानी :
- शरीर के प्रत्येक कोशिका, ऊतक, और अंग के सही कार्य के लिये आवश्यक
- भूमिका : शरीर को हाइड्रेटेड रखना, जैविक प्रक्रियाओं में शामिल
- फाइबर :
- पाचन तंत्र के सही संचालन और कब्ज की समस्या को दूर करने में सहायक
- स्रोत : साबुत अनाज, फल, सब्जियाँ, दालें
संतुलित आहार के माध्यम से इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और सभी जैविक प्रक्रियाएँ सही ढंग से संचालित हो सकें। उचित पोषण से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होता है।
भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को “विधि के समक्ष समानता” और “विधि का समान संरक्षण” का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- “विधि के समक्ष समानता” की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है।
- “विधि का समान संरक्षण” का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है।
समानता संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल सिद्धांत है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 यह गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने या भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 14 की प्रमुख विशेषताएँ
- यह अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिक और गैर-नागरिक दोनों) को प्राप्त है।
- यह मनमानी (Arbitrariness) को असंवैधानिक घोषित करता है।
- यह मूल (Substantive) और प्रक्रियात्मक (Procedural) कानूनों दोनों पर लागू होता है।
- भारत में Rule of Law (कानून का शासन) की आधारशिला है।
- अनुच्छेद 14 के अपवाद
अनुच्छेद 14 के तहत समानता पूर्ण (Absolute) नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं :
-
- राजनयिकों और विदेशी शासकों को प्रतिरक्षा – अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत।
- युक्तिसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) – विधायिका कुछ उद्देश्यों हेतु व्यक्तियों, वस्तुओं या लेन-देन का वर्गीकरण कर सकती है।
- संवैधानिक वैधता की पूर्वधारणा – कानून तब तक वैध माना जाता है जब तक असंवैधानिक सिद्ध न हो।
- सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) – आरक्षण एवं विशेष प्रावधान सामाजिक न्याय हेतु मान्य हैं।
- युक्तिसंगत वर्गीकरण का सिद्धांत
अनुच्छेद 14 वर्ग-आधारित कानून (Class Legislation) को निषिद्ध करता है, लेकिन युक्तिसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) मामले में दो शर्तें निर्धारित की गईं :
-
- बोधगम्य विभेद (Intelligible Differentia) – वर्गीकरण किसी स्पष्ट भेद पर आधारित होना चाहिये जो समूह में शामिल व्यक्तियों को दूसरों से अलग करे।
- तर्कसंगत संबंध (Rational Nexus) – यह भेद अधिनियम के उद्देश्य से तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिये।
इस प्रकार, वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम या दिखावटी नहीं होना चाहिये।
अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो और असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार किया जाए। यह सिद्धांत औपचारिक समानता (Formal Equality) और वास्तविक न्याय (Substantive Justice) के बीच संतुलन स्थापित करता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक नींव का एक प्रमुख स्तंभ है।
मानव व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता (Heredity) वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण जीन (Genes) के द्वारा माता-पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, आनुवंशिकता वह सेतु है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है।
डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार : “वंशानुक्रम में व्यक्ति की सभी विशेषताएँ – उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक लक्षण, क्रियाशीलता एवं क्षमताएँ – सम्मिलित होती हैं, जिन्हें वह अपने माता-पिता, पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है।”
आनुवंशिकता के प्रमुख सिद्धांत
यद्यपि आनुवंशिकता का अध्ययन प्राचीन काल से होता आया है, किन्तु उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में वैज्ञानिक शोधों ने इसे ठोस आधार प्रदान किया। विभिन्न जीवविज्ञानियों और मनोविज्ञानियों ने इस विषय को समझाने के लिये अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किये। प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं:
1. समानता का सिद्धांत (Theory of Resemblance)
इस सिद्धांत के अनुसार, संतान अपने माता-पिता के समान होती है – “Like tends to beget like।”
उदाहरण : यदि माता-पिता लंबी कद-काठी के हैं, तो संभावना है कि बच्चे भी वैसे ही हों।
हालाँकि यह नियम सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि कभी-कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी देखी जाती हैं, जैसे साधारण बुद्धि वाले माता-पिता की संतान अत्यंत प्रतिभाशाली होना।
2. बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत (Continuity of Germplasm)
ऑगस्ट फ्रेडरिक वीज़मान (1843–1914) ने प्रतिपादित किया कि जीव का मूल बीजकोष (Germplasm) नष्ट नहीं होता। यह अण्डाणु और शुक्राणु के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता है। यही कारण है कि पूर्वजों के गुण कई पीढ़ियों बाद भी संतानों में प्रकट हो जाते हैं।
3. प्रत्यागमन का सिद्धांत (Theory of Regression)
इस सिद्धांत में कहा गया है कि संतान कभी-कभी माता-पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करती है।
उदाहरण :
- अत्यंत प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे अपेक्षाकृत साधारण हो सकते हैं।
- निम्न बुद्धि वाले माता-पिता के बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि पाई जा सकती है।
4. जीव-सांख्यिकी सिद्धांत (Biometric Theory)
फ्राँसिस गाल्टन ने अपने अध्ययनों को सांख्यिकीय आधार पर प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, संतान केवल माता-पिता के ही नहीं बल्कि दादा-दादी, नाना-नानी और कई पीढ़ियों पीछे के गुण भी ग्रहण करती है। इसमें पितृ और मातृ दोनों पक्षों का योगदान समान रूप से होता है।
5. अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत (Inheritance of Acquired Characters)
सामान्यतः यह माना जाता है कि जीवनकाल में अर्जित गुण संतानों में नहीं जाते। लेकिन लैमार्क ने इसे अस्वीकार कर कहा कि अर्जित गुण भी स्थानांतरित होते हैं।
उदाहरण : जिराफ़ की गर्दन शुरू में छोटी थी, परंतु ऊँची शाखाओं से पत्तियाँ खाने की आदत ने उसकी गर्दन को लंबा कर दिया, और यही गुण आने वाली पीढ़ियों में स्थायी हो गया।
6. विभिन्नता का नियम (Law of Variation)
इस सिद्धांत के अनुसार, संतान अपने माता-पिता से पूरी तरह समान नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ अंतर अवश्य पाये जाते हैं। एक ही माता-पिता के बच्चों में भी रंग, बुद्धि, व्यक्तित्व और स्वभाव में अंतर होना इसी नियम का प्रमाण है।
आनुवंशिकता मानव जीवन का मूल आधार है, जो यह सिद्ध करती है कि व्यक्ति का विकास केवल पर्यावरण पर नहीं, बल्कि वंशानुगत गुणों पर भी निर्भर करता है। विभिन्न सिद्धांत इस तथ्य को अलग-अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव व्यक्तित्व पूर्वजों के गुण और परिस्थितियों दोनों का संयुक्त परिणाम है।
मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्त्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाकर प्राप्त होता है। मिश्रण के निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि अवयव अपने मूल गुणों को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि मिश्रण को अपेक्षाकृत सरल यांत्रिक विधियों जैसे- छनन (Filtration), वाष्पीकरण (Evaporation), आसवन (Distillation), अपकेंद्रण (Centrifugation) आदि द्वारा उसके मूल घटकों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, हवा एक सामान्य मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें सम्मिलित रहती हैं।
मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं – समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण।
- समांग मिश्रण (Homogeneous Mixture)
जब मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में और इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि पूरे मिश्रण के सभी भागों में उनका वितरण एकसमान हो, तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में विभिन्न अवयवों को अलग-अलग पहचानना संभव नहीं होता क्योंकि वे अणु स्तर पर समान रूप से फैले रहते हैं।- मुख्य लक्षण :
- मिश्रण के प्रत्येक भाग में गुण-धर्म समान रहते हैं।
- अवयवों का पृथक्करण नग्न आँखों से या साधारण तरीकों से संभव नहीं होता।
- अक्सर इनका निर्माण घुलनशील पदार्थों के विलयन से होता है।
- उदाहरण : चीनी का जलीय विलयन, नमक का घोल, हवा।
- मुख्य लक्षण :
- विषमांग मिश्रण (Heterogeneous Mixture)
जब मिश्रण के अवयव अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं और वे पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते, तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। इसमें प्रत्येक भाग की संरचना और गुण-धर्म अलग-अलग होते हैं। ऐसे मिश्रण में अवयवों को आसानी से पहचाना जा सकता है और साधारण विधियों द्वारा अलग भी किया जा सकता है।- मुख्य लक्षण :
- मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण और संघटन अलग-अलग होते हैं।
- विभिन्न अवयव नग्न आँखों से दिखाई देते हैं।
- इनका पृथक्करण अपेक्षाकृत सरल होता है।
- उदाहरण : बारूद, कुहासा, दूध में घी की परत, मिट्टी और रेत का मिश्रण।
अतः मिश्रण रसायन विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है, जिसमें पदार्थों का मेल होता है लेकिन उनकी मूल पहचान बनी रहती है। समांग मिश्रण पूर्णतः एकसमान और समान गुणधर्म वाले होते हैं, जबकि विषमांग मिश्रण में विविधता और असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह भेद रसायन और दैनिक जीवन दोनों में मिश्रणों को समझने और उपयोग करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
बीसवीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ा। इस काल में कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जन-जन तक पहुँचाया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष का वातावरण बनाया।
- महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएँ
|
क्रम |
संस्था / संगठन |
स्थापना वर्ष |
संस्थापक / प्रमुख व्यक्ति |
|
01 |
गदर पार्टी |
1913 |
लाला हरदयाल, काशी राम |
|
02 |
हिन्दू महासभा |
1915 |
मदन मोहन मालवीय |
|
03 |
होमरूल लीग |
1916 |
बाल गंगाधर तिलक एवं ऐनी बेसेन्ट |
|
04 |
वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन |
1917 |
लेडी सदाशिव अय्यर |
|
05 |
खिलाफत आन्दोलन |
1919 |
अली बन्धु |
|
06 |
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस |
1920 |
एन. एम. जोशी |
|
07 |
स्वराज पार्टी |
1923 |
मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास |
|
08 |
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) |
1924 |
सचिंद्र नाथ सान्याल |
|
09 |
बहिष्कृत हितकारिणी सभा |
1924 |
डॉ. भीमराव अंबेडकर |
|
10 |
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) |
1925 |
डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार |
|
11 |
नौजवान भारत सभा |
1926 |
भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल |
|
12 |
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) |
1928 |
भगत सिंह |
|
13 |
खुदाई खिदमतगार |
1930 |
अब्दुल गफ्फार खाँ |
|
14 |
हरिजन सेवक संघ (पुणे) |
1932 |
महात्मा गाँधी |
|
15 |
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी |
1936 |
डॉ. भीमराव अंबेडकर |
|
16 |
फॉरवर्ड ब्लॉक |
1939 |
सुभाष चन्द्र बोस |
|
17 |
आज़ाद हिंद फ़ौज (INA) |
1942 |
रास बिहारी बोस |
|
18 |
आज़ाद हिंद सरकार |
1943 |
सुभाष चन्द्र बोस |
इन संगठनों ने स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया। गदर पार्टी से लेकर आज़ाद हिंद फ़ौज और आज़ाद हिंद सरकार तक, सभी ने भारत की आज़ादी के लिये अपने-अपने स्तर पर क्रांतिकारी योगदान दिया।
भारत एक नदी-प्रधान देश है जहाँ परिवहन और व्यापार की दृष्टि से नदियों और नहरों का विशेष महत्त्व रहा है। समुद्री मार्गों के साथ-साथ आंतरिक जल परिवहन (Inland Water Transport) भी किफायती, पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-सक्षम साधन है। इसी उद्देश्य से विभिन्न नदियों, नहरों और खाड़ी क्षेत्रों को राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways - NW) के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये जलमार्ग न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (विशेषकर बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग) को भी मजबूत करते हैं।
|
क्रमांक |
राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) |
नदी/नहर/जलमार्ग |
विस्तृत स्थान / राज्य |
|
NW-1 |
गंगा-भागीरथी-हुगली नदी तंत्र (हल्दिया से प्रयागराज/इलाहाबाद तक) |
गंगा नदी प्रणाली |
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल |
|
NW-3 |
वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपकारा और उद्योगमंडल नहरें |
नहर तंत्र |
केरल |
|
NW-4 |
कृष्णा नदी (मुक्तियाला से विजयवाड़ा) |
कृष्णा नदी |
आंध्र प्रदेश |
|
NW-10 |
अंबा नदी |
अंबा नदी |
महाराष्ट्र |
|
NW-68 |
मांडवी नदी (उसगाँव ब्रिज से अरब सागर तक) |
मांडवी नदी |
गोवा |
|
NW-73 |
नर्मदा नदी |
नर्मदा नदी |
गुजरात, महाराष्ट्र |
|
NW-100 |
तापी नदी |
तापी नदी |
गुजरात, महाराष्ट्र |
|
NW-97 |
सुंदरबन जलमार्ग (भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से जुड़ा) |
नदी व खाड़ी क्षेत्र |
पश्चिम बंगाल |
- भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग
भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग न केवल सस्ती और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था प्रदान करते हैं, बल्कि निर्यात-आयात, आंतरिक व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को भी मजबूत बनाते हैं। इनमें से गंगा पर आधारित NW-1 सबसे लंबा और महत्त्वपूर्ण जलमार्ग है, जबकि सुंदरबन क्षेत्र का NW-97 भारत-बांग्लादेश संबंधों और व्यापार के लिहाज़ से अहम है। भविष्य में इन जलमार्गों का और अधिक विकास देश की आर्थिक प्रगति और सतत परिवहन प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्राचीन भारत का इतिहास केवल भारतीय स्रोतों पर आधारित नहीं है, बल्कि विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विशेषकर चीनी बौद्ध यात्री, जो बौद्ध धर्म के अध्ययन, ग्रंथ-संग्रह और भारत की संस्कृति को समझने हेतु यहाँ आए, उन्होंने अपने यात्रा-वृत्तांतों में तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म और शिक्षा का चित्रण किया। इन विवरणों ने भारतीय इतिहास को और भी स्पष्ट बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
(i) फाहियान (Fa-Hien)
- समय : गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के शासनकाल में भारत आया।
- उद्देश्य : बौद्ध ग्रंथों व अवशेषों की खोज।
- विवरण :
- मध्यप्रदेश के समाज और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया।
- जनता को सुखी और समृद्ध बताया।
(ii) संयुन / सॉन्ग-युन (Song-Yun)
- आगमन : 518 ई. में भारत पहुँचा।
- प्रवास : लगभग 3 वर्ष रहा।
- उद्देश्य : बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों और परंपराओं का अध्ययन।
- विवरण : इसके लेखन से तत्कालीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का ज्ञान मिलता है।
(iii) ह्वेनसांग (Hsuan-Tsang / Xuanzang)
- आगमन : 629 ई. में चीन से प्रस्थान कर भारत पहुँचा।
- भारत प्रवास : लगभग 15 वर्ष (630–645 ई.)।
- शासक : हर्षवर्धन के शासनकाल में आया।
- उद्देश्य : बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और संग्रह; विशेषकर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण।
- विवरण :
- यात्रा-वृत्तांत “सी-यू-की (Si-Yu-Ki)” में 138 देशों का उल्लेख।
- हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का सजीव चित्रण।
- उल्लेख : सिंध का राजा शूद्र था।
- उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे।
(iv) इत्सिंग (I-Tsing / Yijing)
- आगमन : 7वीं शताब्दी के अंत में भारत पहुँचा।
- उद्देश्य : बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन और बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद।
- विवरण :
- नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विस्तार से वर्णन।
- अपने समय के भारत की शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक जीवन का उल्लेख।
इन चीनी यात्रियों के वृत्तांत भारतीय इतिहास के बहुमूल्य स्रोत हैं। इनके लेखन से हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की प्रामाणिक झलक मिलती है। विशेषकर फाहियान ने गुप्तकाल, संयुन ने बौद्ध धर्म की प्रगति, ह्वेनसांग ने हर्षकालीन भारत और इत्सिंग ने विश्वविद्यालयों व शिक्षा प्रणाली का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया। इस प्रकार, इनके विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति समझने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस (2025) पर प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक पहलों की घोषणा की। ये घोषणाएँ भारत के आर्थिक, सामरिक, तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में उठाए गए ठोस कदम मानी जा रही हैं।
- प्रमुख पहलें
- PM विकसित भारत रोज़गार योजना
- लक्ष्य : अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना।
- नए रोजगार प्राप्त युवाओं को ₹15,000 की वित्तीय सहायता।
- इससे लगभग 3 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
- यह पहल “स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत” की दिशा में मील का पत्थर है।
- मिशन सुदर्शन चक्र
- वर्ष 2035 तक स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना।
- उद्देश्य : सामरिक व नागरिक स्थलों की सुरक्षा, दुश्मन हमलों की रोकथाम और जवाबी क्षमता में वृद्धि।
- सेमीकंडक्टर क्रांति
- भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली Made-in-India सेमीकंडक्टर चिप प्रस्तुत करेगा।
- यह डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
- नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन (समुद्र मंथन)
- अपतटीय (Offshore) तेल, गैस और खनिज संसाधनों का मिशन मोड में अन्वेषण।
- ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन विविधीकरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण।
- GST एवं रिफॉर्म टास्क फोर्स
- अक्टूबर 2025 से GST सुधार लागू होंगे।
- आवश्यक वस्तुओं का पुनरीक्षण, MSMEs व उपभोक्ताओं को राहत।
- एक समर्पित Reform Task Force के जरिये लालफीताशाही में कमी और शासन को अधिक अनुकूल बनाने का लक्ष्य।
- उद्देश्य : वर्ष 2047 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना।
- हाई पावर डेमोग्राफी मिशन
- सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासन से उत्पन्न जनसांख्यिकीय असंतुलन का समाधान।
- राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और नागरिक अधिकारों की रक्षा पर बल।
- परमाणु ऊर्जा विस्तार
- वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य।
- इसके लिये 10 नए परमाणु रिएक्टरों का विकास किया जा रहा है।
- स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति
- भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 2030 की समयसीमा से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया।
- यह भारत की ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका का प्रमाण है।
79वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषित ये पहलें भारत के लिये केवल योजनाएँ नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की रूपरेखा है। रोज़गार, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और आर्थिक सुधारों में यह घोषणाएँ भारत को वैश्विक महाशक्ति की ओर अग्रसर करने में निर्णायक साबित होंगी।
- PM विकसित भारत रोज़गार योजना
किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिये जिस मानक परिभाषित परिमाण को अपनाया जाता है, उसे मात्रक (Unit) कहते हैं। मात्रक का प्रयोग मापन में एकरूपता (uniformity), सटीकता (accuracy) और सुव्यवस्था (consistency) लाने के लिये किया जाता है।
- मात्रकों के मुख्य प्रकार
- मूल मात्रक (Fundamental Units)
- ये ऐसे मात्रक हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते।
- उदाहरण : मीटर (m), किलोग्राम (kg), सेकंड (s) इत्यादि।
- व्युत्पन्न मात्रक (Derived Units)
- ये मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं।
- उदाहरण : वेग (m/s), बल (kg·m/s²), दाब (N/m²) आदि।
- मूल मात्रक (Fundamental Units)
- S.I. पद्धति (SI System)
- पूरा नाम : Système International d’Unités (अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली)
- स्वीकृति वर्ष : 1960 (अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप सम्मेलन द्वारा)
- विशेषताएँ :
- विश्वभर में मान्य
- माप में सरलता और एकरूपता
- सभी विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उपयोग
- S.I. के 7 मूल मात्रक
|
क्रम |
भौतिक राशि |
मात्रक (हिंदी) |
मात्रक (अंग्रेज़ी) |
संकेत |
|
1 |
लंबाई |
मीटर |
metre |
m |
|
2 |
द्रव्यमान |
किलोग्राम |
kilogram |
kg |
|
3 |
समय |
सेकण्ड |
second |
s |
|
4 |
तापमान |
केल्विन |
kelvin |
K |
|
5 |
विद्युत धारा |
ऐम्पियर |
ampere |
A |
|
6 |
ज्योति-तीव्रता |
कैण्डेला |
candela |
cd |
|
7 |
पदार्थ का परिमाण |
मोल |
mole |
mol |
- पूरक मात्रक (Supplementary Units)
|
भौतिक राशि |
मात्रक |
संकेत |
|
समतल कोण |
रेडियन |
rad |
|
घन कोण |
स्टेरेडियन |
sr |
- पुराने मात्रकों के नए नाम (S.I. पद्धति में)
|
भौतिक राशि |
पुराना नाम / संकेत |
नया नाम / संकेत |
|
तापमान |
डिग्री सेण्टीग्रेड (°C) |
डिग्री सेल्सियस (°C) |
|
आवृत्ति |
कंपन प्रति सेकण्ड (cps) |
हर्ट्ज़ (Hz) |
|
ज्योति-तीव्रता |
कैण्डिल शक्ति (C.P.) |
कैण्डेला (cd) |
26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ भारतीय संविधान विश्व के सबसे व्यापक और विस्तृत संविधानों में गिना जाता है। यह न केवल भारत की विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है, बल्कि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों और शासन प्रणालियों से प्रेरित अनेक प्रावधान भी सम्मिलित हैं। संविधान निर्माताओं ने विश्वभर के श्रेष्ठ संवैधानिक तत्वों को चुनकर उन्हें भारतीय आवश्यकताओं और संस्कृति के अनुरूप रूपांतरित किया। नीचे प्रमुख देशों और उनसे लिये गए प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत है।
- विदेशी स्रोत एवं अपनाए गए प्रावधान
|
देश |
अपनाए गए प्रावधान |
|
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) |
मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल |
|
ब्रिटेन (UK) |
संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया |
|
आयरलैंड |
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विशिष्ट क्षेत्रों (साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा) के विशेषज्ञों का नामांकन |
|
ऑस्ट्रेलिया |
प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केन्द्र–राज्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार |
|
जर्मनी (वाइमर गणराज्य) |
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित करने की शक्ति |
|
कनाडा |
संघात्मक ढाँचे में मज़बूत केन्द्र, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया |
|
दक्षिण अफ्रीका |
संविधान संशोधन की प्रक्रिया |
|
रूस (USSR) |
मौलिक कर्तव्य |
|
जापान |
"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की अवधारणा |
भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का पड़ा। मूल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे इसी अधिनियम से लिये गए हैं या मामूली संशोधन के साथ अपनाए गए हैं, जिससे यह संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत बन गया।
भारतीय संविधान को अक्सर “उधारों की थैली” कहा जाता है, किंतु यह मात्र नकल नहीं है, बल्कि एक गहन चिंतन-मनन के बाद तैयार किया गया दस्तावेज़ है। इसमें विश्वभर के श्रेष्ठ प्रावधानों को भारतीय संदर्भ में ढालकर लोकतंत्र, संघवाद और सामाजिक न्याय के बीच एक अद्वितीय संतुलन स्थापित किया गया है। यही संतुलन इसे समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदान करता है।
Verb (क्रिया) क्या होती है?
क्रिया(verb) वह शब्द होता है जो किसी कार्य, घटना या अवस्था को दर्शाता है। इसीलिये इसे “Action word” (करने वाला शब्द) या “state word” (स्थिति दर्शाने वाला) कहा जाता है।
- Action word → shows what is being done
- State word → shows condition or existence
Examples:
run, jump, eat, sleep, is, are, was, have, must, can, should
Types of Verbs
1. Main Verb(मुख्य क्रिया)
- यह वाक्य में मुख्य कार्य या स्थिति को दर्शाती है। इसे अकेले (alone) या सहायक क्रिया (helping verbs) के साथ प्रयोग किया जा सकता है।
Example:
She sings beautifully. → → यहाँ ‘sings’ मुख्य क्रिया (main verb) है, जो उसके गायन की क्रिया को दर्शा रहा है।
2. Auxiliary Verb (सहायक क्रिया)
ये क्रियाएँ मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य का काल (tense), भाव (mood), या वाच्य (voice) बनाती हैं।
- Auxiliary Verbs के प्रकार :
A. Primary Auxiliary (प्राथमिक सहायक क्रियाएँ)
Forms: be (am, is, are, was, were), do (do, does, did), have (has, have, had)
ये क्रियाएँ वाक्य में दो तरीकों से प्रयोग होती हैं :
- Main Verb (मुख्य क्रिया) की तरह
- Helping Verb (सहायक क्रिया) की तरह
Examples:
They are dancing. → → यहाँ are एक helping verb है जो dancing को support कर रहा है।
He has a laptop. → यहाँ has एक main verb है जो possession (स्वामित्व) दिखा रहा है।
B. Modal Auxiliary (मॉडल सहायक क्रियाएँ)
Always used with a main verb इनका प्रयोग क्षमता (ability), संभावना (possibility), अनुमति (permission), ज़रूरत (necessity) आदि को व्यक्त करने के लिये होता है। ये क्रियाएँ केवल सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होती हैं।
Common Modals:
can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to
Example:
You should complete your homework. à यहाँ "should" सलाह देने के लिये प्रयोग हुआ है।
C. Marginal Auxiliary (सीमांत सहायक क्रियाएँ)
ये क्रियाएँ कभी-कभी सहायक (modals) और कभी मुख्य क्रिया (main verbs) की तरह व्यवहार करती हैं।
Common Marginal Auxiliary:
need, dare, used to
Examples:
We need to talk. → यहाँ "need" मुख्य क्रिया है (Main Verb).
You need not worry. → यहाँ "need" सहायक क्रिया की तरह (Helping Verb) प्रयोग हुई है।
She used to sing. → used to" एक modal की तरह व्यवहार कर रहा है — past habit को दर्शाता है।
- मुख्य बिंदु (Key Points on Verbs)
- Verb दो प्रकार की होती हैं –
Main (मुख्य क्रिया) और Auxiliary (सहायक क्रिया)। - Modal Verbs के बिना वाक्य अधूरा होता है –
जैसे : "You must study." यहाँ “must” जरूरी है भाव व्यक्त करने के लिये। - Marginal Auxiliary लचीले होते हैं –
ये कभी main verb की तरह, तो कभी helping verb की तरह काम कर सकते हैं।
उदाहरण : "She used to dance." / "You need to try." - Verb की अच्छी समझ से भाषा के कई भागों में मदद मिलती है, जैसे :
- Tense (काल) पहचानना
- Voice (Active/Passive) बदलना
- Spotting Error में सही/गलत पहचानना
- Translation (अनुवाद) में अर्थ सही पकड़ना
- Verb दो प्रकार की होती हैं –
किसी पदार्थ पर विद्युत धारा प्रवाहित करके वांछित धातु की परत निक्षेपित करना विद्युत लेपन कहलाता है। उद्योग जगत में एक धातु की वस्तु पर अन्य धातु की परत चढ़ाकर उसे सुरक्षा और सुंदरता प्रदान की जाती है। जैसे- साइकिल-मोटरसाइकिल के हैंडिल, पहियों के रिम, नल की टोंटी, गैस बर्नर, वाहनों के भागों इत्यादि पर क्रोमियम लेपन कर उन्हें मज़बूत और चमकदार बनाया जाता है। संक्षारित नहीं होने से क्रोमियम खरोंच से बचाता है, किंतु महंगा होने के कारण समूची वस्तु को इससे न बनाकर उस पर केवल इसकी परत चढ़ा दी जाती है।
- लोहे से निर्मित वाहनों एवं पुलों को जंग से बचाने के लिये उन पर ज़िंक की परत चढ़ाई जाती है।
- खाद्य पदार्थों के भंडारण में प्रयुक्त लोहे के डिब्बों पर कम क्रियाशील टिन का लेपन किया जाता है।
- सोने या चांदी से प्रतीत होने वाले आभूषणों के निर्माण में सस्ती धातुओं पर सोने या चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है।
विद्युत लेपन की प्रक्रिया (Process of Electroplating)
250 मिली. आसुत जल से भरे एक बीकर में 10 सेमी. x 4 सेमी. की तांबे की दो प्लेटें इस प्रकार लटकाई जाती हैं कि तारों से जुड़े इनके ऊपरी सिरे जल से ऊपर हों। जल में दो छोटा चम्मच कॉपर सल्फेट घोला जाता है और चालकता बढ़ाने के लिये कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ बूँद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। अब बैटरी द्वारा प्लेट वाले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लगभग 15 मिनट पश्चात् हम पाते हैं कि बैटरी के ऋण सिरे वाले इलेक्ट्रोड पर कॉपर (तांबा) की परत चढ़ गई है तथा तांबे से निर्मित दूसरे इलेक्ट्रोड से समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल गया है जिससे विलयन में कॉपर कम नहीं पड़ता वस्तुतः कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाह करने पर विलयन कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। इलेक्ट्रोड़ों के धन और ऋण सिरों को परस्पर बदलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर भी विद्युत लेपन किया जा सकता है। कारखानों में विद्युत लेपन में प्रयुक्त विलयन के प्रदूषणकारी होने से इसके निबटारे के लिये विशिष्ट दिशा-निर्देश दिये गए हैं।
- यह योजना स्कूलों में मिड-डे मील योजना के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी।
- इसे पांच वर्ष (2021-22 से 2025-26) की शुरुआती अवधि के लिये लॉन्च किया गया है।
- कवरेज- यह योजना देश भर के 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में कक्षा I से VIII तक नामांकित 11.8 करोड़ विद्यार्थियों को कवर करेगी।
- प्राथमिक (1-5) और उच्च प्राथमिक (6-8) स्कूली बच्चे वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम और 150 ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं ताकि न्यूनतम 700 कैलोरी सुनिश्चित की जा सके।
- इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे प्री-प्राइमरी या बालवाटिका में पढ़ने में वाले विद्यार्थियों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- बालवाटिका एक प्रकार के प्री-स्कूल होते हैं जिनकी शुरुआत औपचारिक शिक्षा प्रणाली में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने के लिये वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों में की गई थी।
- पोषाहार उद्यान- इसके तहत सरकार स्कूलों में ‘पोषाहार उद्यानों’ को बढ़ावा देगी। विद्यार्थियों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्त्व प्रदान करने हेतु उद्यान स्थापित किये जाएंगे।
- पूरक पोषण- इस नई योजना में आकांक्षी ज़िलों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिये पूरक पोषण का भी प्रावधान है।
- यह गेहूँ, चावल, दाल और सब्ज़ियों के लिये धन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध और चुनौतियों को समाप्त करती है।
- वर्तमान में, यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है तो केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त लागत वहन नहीं की जाती है। इस नई योजना के तहत इससे संबंधित प्रतिबंध को हटा लिया गया है।
- तिथि भोजन- इस नई योजना के तहत तिथि भोजन (Tithi Bhojan) की अवधारणा प्रस्तुत की गई है जिसे व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।
- योजना के तहत निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को महीने में कम-से-कम एक बार स्वैच्छिक आधार पर हाशिये पर स्थित वर्गों के बच्चों के साथ अपना भोजन साझा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्यों को एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने के लिये भी कहा जाएगा जिसमें लोग बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)- केंद्र सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किये हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यक्रम में काम करने वाले रसोइयों तथा सहायकों को मानदेय प्रदान करने के लिये ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
- पोषण विशेषज्ञ- प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है जिसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बॉडी मास इंडेक्स (BMI), वज़न और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए।
- योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा- योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिये प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्कूल हेतु योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा को भी अनिवार्य किया गया है जो अब तक सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा था।
- शिक्षा मंत्रालय स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिये कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी शामिल करेगा।
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभिन्न समुद्री जीवों की खोज तथा उनका उपयोग कर मानव उपयोगी उत्पादों को विकसित करना शामिल है। दूसरे शब्दों में, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के तहत वे सभी प्रयास शामिल हैं, जिनमें जैविक समुद्री संसाधनों को जैव प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में मानव लाभ के लिये उपयोग किया जाता है।
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विविधता ने वैज्ञानिकों को समुद्री जीवों के विकास और उनसे जुड़े महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सुविधा प्रदान की है। चूँकि समुद्री जीव समुद्र के भीतर, प्रकाश की अनुपस्थिति, अधिक तापमान और दबाव में विकसित होते हैं, इसलिये वैज्ञानिकों ने इनकी मदद से विशिष्ट प्रकार की दवाओं और एंजाइमों को तैयार करने में सफलता हासिल की है।
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पर बढ़ते शोध ने बहुत-सी दवाओं के विकास को संभव बनाया है। कैरिबियाई समुद्री जीवों की मदद से बनाई गई एंटी-वायरल दवाएं, जैसे- Zovirax (Generic Name- Acyclovir), आदि पहले ही काफी सफल साबित हो चुकी हैं।
समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के कुछ अनुप्रयोग
- समुद्री जीवों (समुद्री शैवालों, अकशेरुकियों अर्थात् बिना रीढ़ वाले जीव) आदि ने बहुत-सी नई दवाओं के विकास को संभव बनाया है। इससे कैंसर के इलाज में भी कुछ सफलता मिली है।
- मछलियों और अन्य समुद्री जीवों से मिलने वाले एंजाइम खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले परंपरागत एंजाइमों से ज्यादा प्रभावी और फायदेमंद होते हैं। मछलियों से मिलने वाले Collagens और Gelatin प्रोटीन अपेक्षाकृत कम तापमान पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं।
- समुद्र में पाए जाने वाले अतिसूक्ष्म शैवालों से ऐसे बायोपॉलिमर्स का निर्माण संभव है, जो तेल निष्कर्षण की प्रक्रिया में मदद करते हैं।
- हिंद महासागर में पाया जाने वाला Dolastatin ब्रेस्ट कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में बहुत उपयोगी साबित हुआ है।
असम राइफल्स
इसकी स्थापना अर्द्धसैनिक बल के रूप में 1835 में कछार लेवी के नाम से की गई थी। भारत-म्यांमार तथा भारत-चीन पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। इसकी 46 बटालियनें हैं, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसका मुख्यालय शिलॉन्ग में है। इस बल को ‘पूर्वोत्तर का प्रहरी’ भी कहते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
NSG की स्थापना आतंकवाद का सामना करने के लिये 1984 ई. में की गई थी। NSG के कमांडो को ‘ब्लैक कैट’ कमांडो भी कहते हैं। इसकी ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है। इसके दो समूह हैं-
- स्पेशल एक्शन ग्रुप- इसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं।
- स्पेशल रेंजर ग्रुप- इसमें राज्य पुलिस बल के कर्मचारी होते हैं।
सशस्त्र सीमा बल (SSB)
यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1963 में भारत-चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में की गई थी। 2003 में इसे सशस्त्र सीमा बल का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, सीमा-पार अपराधों, तस्करी तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना है।
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)
इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। पहले इसे ‘क्राउन रिप्रेजेंटिटिव पुलिस’ कहा जाता था। 1949 में इसका नाम C.R.P.F. रखा गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दंगों से निपटने के लिये 1992 में स्थापित रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) CRPF का ही एक भाग है।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
इसका गठन चीन आक्रमण के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये अक्तूबर 1962 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह फोर्स वर्तमान में हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व सँभालने के साथ-साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा-संचार तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाता है।
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षा तथा भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बांग्लादेश सीमा उल्लंघन को रोकने हेतु 1965 ई. में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
केंद्र सरकार के अधीन औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों तथा वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु CISF का गठन 1969 ई. में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
नेशनल कैडेट कोर (NCC)
1948 में स्थापित इस निकाय का प्रमुख उद्देश्य भारत की रक्षा हेतु युवक-युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में तैयार करना है। इसका आदर्श वाक्य ‘एकता एवं अनुशासन’ है। इसमें स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर ऐच्छिक तौर पर भाग लिया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह जल, थल तथा वायुसेना तीनों ही स्तरों पर कार्य करता है।
न्यूक्लियर-फ्री ज़ोन उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ परमाणु हथियारों का विकास, स्वामित्व, परीक्षण और तैनाती पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। ऐसे क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से स्थापित किये जाते हैं, जिनका उद्देश्य शांति बनाए रखना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना होता है।
- टलाटेलोल्को की संधि, 1967 (Treaty of Tlatelolco) द्वारा लैटिन अमेरिका क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र रखने पर बल दिया गया।
- परमाणु अप्रसार संधि (1968) में भी परमाणु मुक्त क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था।
- रारोटोंगा संधि, 1985 (Treaty of Rarotonga) द्वारा दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया।
- पेलिंडाबा संधि, 1996 (Pelindaba Treaty) द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया।
- बैंकाक संधि, 1997 (Bangkok Treaty) द्वारा आसियान देशों ने इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र स्थापित किया गया।
इन सभी संधियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि दुनिया के कुछ संवेदनशील क्षेत्र परमाणु खतरे से मुक्त रहें, जिससे वैश्विक शांति, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले।
एक जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन कोश कहते हैं। वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। ये वे स्थान हैं जहाँ पर फसलों की महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ और स्थानिक जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कृषि पादप प्रजातियों एवं उष्णकटिबंधीय पौधों के जीन या आनुवंशिक पदार्थों को एकत्रित किया जाता है।
जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग है। आनुवंशिक पदार्थों का एकत्रीकरण कर जीन पूल केंद्रों में रखा जाता है, जो भविष्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जीन पूल केंद्र के अंतर्गत विश्व के महत्त्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
विश्व के प्रमुख जीन पूल केंद्र इस प्रकार हैं-
- दक्षिण एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो-चाइना एवं द्वीपीय क्षेत्र जो मलाया द्वीप को शमिल करता है।
- दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र, कॉकेशियन (Caucasian) मध्य-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम भारतीय क्षेत्र
- पूर्वी एशिया, चाइना एवं जापान क्षेत्र
- भूमध्यसागरीय क्षेत्र
- यूरोप क्षेत्र
- दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र
- मगरमच्छ संरक्षण के लिये 1974 ई. में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किये गए।
- ओडिशा का ‘भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान’ जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, के लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है।
- ‘केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान’ हैदराबाद में स्थित है।
- मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है।
- मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया।
- 1970 के दशक में शुरू की गई ‘भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना’ (पश्चिम बंगाल) का उद्देश्य खारे पानी में मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना था।
Polymer शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ‘पॉली’ अर्थात् अनेक और ‘मर’ अर्थात् इकाई अथवा भाग से हुई है। बहुलकों के बहुत वृहत् अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिनका द्रव्यमान अतिउच्च होता है। इन्हें बृहदणु भी कहा जाता है, जो कि पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों के बृहद् पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयाँ कुछ सरल और क्रियाशील अणुओं से प्राप्त होती हैं जो एकलक कहलाती हैं। यह इकाइयाँ एक-दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। बहुलकों के संबंधित एकलकों से विरचन के प्रक्रम को बहुलकन कहते हैं।
स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण
- प्राकृतिक बहुलक (Natural Polymers)- यह बहुलक पादपों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिये प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन और रबर।
- अर्द्ध-संश्लेषित बहुलक (Semi-Synthetic Polymers)- सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट (रेयॉन) और सेलुलोज नाइट्रेट आदि इस उपसंवर्ग के उदाहरण हैं।
- संश्लेषित बहुलक (Synthetic Polymers)- विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक जैसे- प्लास्टिक (पॉलिथीन), संश्लेषित रेशे (नाइलॉन 6,6) और संश्लेषित रबर (ब्यूना-S) मानवनिर्मित बहुलकों के उदाहरण हैं, जो विस्तृत रूप से दैनिक जीवन एवं उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं।
बहुलकों को उनकी संरचना, आणविक बलों अथवा बहुलकन की विधि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है।
- वर्ष 1919 में एक छोटे से सेल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में PIB के आठ क्षेत्रीय कार्यालय (चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, कोलकाता और भोपाल) तथा 34 शाखा कार्यालय स्थित हैं।
- पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संप्रेषित करने वाली एक नोडल एजेंसी है।
- पत्र सूचना कार्यालय विभिन्न संचार माध्यमों, जैसे- प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस विवरण, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, PIB की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस, ऑडियो-वीडियो क्लिपिंग्स आदि के ज़रिये सूचनाओं का प्रसार करता है।
- लगभग 8,400 अख़बारों और मीडिया संगठनों के ज़रिये अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना प्रकाशित की जाती है।
- PIB के अधिकारी न सिर्फ अपने संबद्ध मंत्रालयों को लगातार अपनी सेवाएँ देते हैं बल्कि मीडिया के माध्यम से उन मंत्रालयों के कामकाज का प्रचार भी करते हैं।
- PIB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मुखिया प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) हैं, जिनके साथ एक उपमहानिदेशक और आठ अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं।
- एक्स और यूट्यूब पर अपनी सेवा देने के पश्चात् पत्र सूचना कार्यालय ने नए प्लेटफार्म, जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाइन पर अपनी सुविधा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया।
- इस सेवा की मुख्य वेबसाइट हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू, तीनों भाषाओं में उपलब्ध है।
- पत्रकार कल्याणकारी योजना (Journalist Welfare Scheme)- पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ‘पत्रकार कल्याणकारी योजना’ लागू की गई है। इस संशोधित योजना में कहा गया है कि पत्रकार तथा उसके परिवार को जरूरत पड़ने पर एक समय के लिये अनुग्रहपूर्वक राहत देने के प्रावधान के साथ पांच लाख रुपये की धनराशि भी प्रदान की जाएगी। परिवार को राहत बहुत कठिनाई या आफत, जैसे- पत्रकार की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता जैसी स्थिति में ही दी जाएगी। खतरनाक बीमारी, जैसे- कैंसर, ब्रेन हेमरेज इत्यादि तथा दुर्घटना की स्थिति में भी राहत प्रदान की जा सकती है।
- 17 अगस्त, 1965 को इस संस्थान की स्थापना यूनेस्को की सहायता से हुई थी। यह भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है, जिसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इसे सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है।
- भारतीय जनसंचार संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय आइज़ोल (मिज़ोरम), अमरावती (महाराष्ट्र), ढेकनाल (ओडिशा), कोट्टायम (केरल) और जम्मू व कश्मीर में हैं।
- यह संस्थान अनुभवी एवं स्थायी संकाय सदस्यों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण देश का अग्रणी मीडिया स्कूल है। यहाँ संकाय और विद्यार्थी का अनुपात 1:8 है, जो किसी भी मीडिया स्कूल से बेहतर है।
- यह संस्थान प्रिंट मीडिया, फोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, संचार अनुसंधान, विज्ञापन और जन संपर्क सहित तमाम मीडिया विषयों पर प्रशिक्षण देता है।
- इसके द्वारा एक वर्ष के लिये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी तथा उड़िया भाषा में पत्रकारिता के साथ-साथ विज्ञापन व जन संपर्क, रेडियो व टीवी पत्रकारिता एवं फोटो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ-साथ यहाँ गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिये विकास पत्रकारिता के पाठयक्रम भी संचालित किये जाते हैं।
- यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भारत में कार्यरत एक संवाद समिति है।
- यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के समाचार ब्यूरो भारत के लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में तथा प्रमुख शहरों में विद्यमान हैं।
- U.N.I. का गठन कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत दिसंबर 1959 में हुआ। 21 मार्च, 1961 को इसने विधिवत् काम शुरू किया।
- 1 मई, 1982 को U.N.I. ने हिंदी सेवा ‘यूनीवार्त्ता’ की शुरुआत की तथा दस वर्ष पश्चात् 5 जून, 1992 को U.N.I. उर्दूसेवा तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई।
- U.N.I. की फोटो सेवा में प्रतिदिन लगभग 200 तस्वीरें वितरित की जाती हैं, जिनमें 60 अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें E.P.A., यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी तथा रॉयटर्स से ली जाती हैं। इसकी ग्राफिक्स सेवा प्रतिदिन 5 या 6 ग्राफिक्स वितरित करती है।
- U.N.I. ने ही सर्वप्रथम विश्व में उर्दू समाचारों की आपूर्ति की थी।
- इसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ है।
- U.N.I. संवाददाता वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, मास्को, दुबई, इस्लामाबाद, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, सिंगापुर, टोरंटो, सिडनी, बैंकाक और काबुल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
- U.N.I. ने ख़बरों के आदान-प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों से समझौते कर रखे हैं, जिनमें- चीन की शिन्हुआ, रूस की रिया नोवोस्ती, बांग्लादेश की यू.एन.बी., तुर्की की अनादोलू, संयुक्त अरब अमीरात की वाम, बहरीन की जी.एन.ए. और कुवैत की कुना इत्यादि शामिल हैं।
- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिये ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008’ संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर, 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे।
- ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे ‘न्यायाधिकारी’ कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है।
- ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देखता है। ऐसे मामलों की सूची ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम’ की अनुसूची में दी गई है।
- एक तरफ जहाँ यह 2 वर्षों की अधिकतम सज़ा वाले आपराधिक मामले को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह ‘न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948’, ‘सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955’, ‘बंधुआ मज़दूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976’, ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’ के अंतर्गत आने वाले मामले भी देखता है।
- इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है तो आपराधिक मामलों में ‘प्ली बार्गेनिंग’ (Plea Bargaining) के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है।
5 जुलाई, 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल निपुण भारत (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) का आरंभ किया गया।
- 29 जुलाई, 2020 को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के लिये उठाए गए कदमों की शृंखला के तहत निपुण भारत का शुभारंभ एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- निपुण भारत मिशन का विज़न शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार हो सके, जिससे प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 की पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई-लिखाई और अंकों के ज्ञान में ज़रूरी निपुणता हासिल कर सके।
- निपुण भारत को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा और केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक पांचस्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- नेत्रदान चाक्षुष-विकृति युक्त कॉर्निया-अंधता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये अमूल्य दान है।
- नेत्रदान किसी भी लिंग, आयु अथवा सामाजिक स्तर का व्यक्ति चाहे वह चश्मा क्यों न लगाए, कर सकता है।
- एड्स, हेपेटाइटिस B या C, जलभीति (Rabies), ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, मस्तिष्क शोध से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं।
- नेत्रदान मृत्यु के 4-6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर या अस्पताल में किया जाता है। इसके लिये इच्छुक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर नेत्र धरोहर के रूप में रखने होते हैं, जिसकी जानकारी निकट संबंधियों को दे देनी चाहिये। कोई व्यक्ति ब्रेल किट भी दान कर सकता है।
एक्स-रे उपकरण X-किरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदर मौजूद अस्थियों, ऊतकों एवं मांसपेशियों का चित्रण करता है। यह नियंत्रित X-किरणों के बीम का उत्पादन कर उस क्षेत्र में निर्देशित करता है जिसकी जांच की जानी है।
चिकित्सकीय उपयोग
- अस्थियों के टूटने का पता लगाने में।
- जोड़ों में चोट तथा संक्रमण का पता लगाने में।
- धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाने में।
- पेट में दर्द का पता लगाने में।
- कैंसर की जाँच करने में।
- अनियंत्रित रोगाणुओं की वृद्धि होने पर उन्हें शरीर से नष्ट करने में।
- शल्य कर्म में।
- धातु विज्ञान में।
- उद्योगों में।
हानिकारक प्रभाव
X-किरणें सजीव ऊतकों तथा जीवों को हानि पहुँचा सकती हैं। अत्यधिक X-किरणों के प्रयोग से जीवित कोशिकाएँ मृत हो जाती हैं एवं एक ही स्थान पर बार-बार X-किरणों के प्रयोग किये जाने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, अतः इसके अनावश्यक या अधिक एक्सपोज़र से बचना चाहिये।
- जब स्वतंत्र भारत में परमाणु ऊर्जा के संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुसंधान कार्य आरंभ करवाया, तब डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ‘परमाणु ऊर्जा आयोग’ (Atomic Energy Commission) के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रारंभ में परमाणु शक्ति के संबंध में ‘शांति के लिये परमाणु’ (Atoms for Peace) सिद्धांत को अपनाया गया अर्थात् केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति के विकास का लक्ष्य रखा गया।
- बांग्लादेश के संकट (वर्ष 1971) के पश्चात् जब यह स्पष्ट होने लगा कि चीन अपने मित्र पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के निर्माण में सहायता कर सकता है, तब भारत को गंभीरता से अपने परमाणु कार्यक्रम पर विचार करना पड़ा। इससे पूर्व ही वर्ष 1964 में चीन अपना प्रथम परमाणु विस्फोट करके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था।
- चीन और अमेरिका के मध्य बढ़ते राजनीतिक संबंधों को देखते हुए भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा : पोखरण-I) किया, परंतु विश्व समुदाय द्वारा इस विषय पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह उसका शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (Peaceful Nuclear Explosion- PNE) था।
- वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) पर हस्ताक्षर करने से भारत सदा इनकार करता रहा है। वास्तव में भारत इस संधि को भेदभाव पर आधारित मानता है क्योंकि इसमें केवल पांच देशों (ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन) को ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र (Nuclear Weapon States) स्वीकार किया गया है।
- वर्ष 1991-96 के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव गंभीरता से विचार करते रहे कि परमाणु परीक्षण किया जाए, परंतु उन्होंने परीक्षण के आदेश नहीं दिये।
- मई 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहसिक कदम उठाकर परमाणु परीक्षण (पोखरण-II) करवाए। परमाणु परीक्षण अत्यंत गोपनीय रूप से किये गए। फलस्वरूप भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र (Nuclear Weapon States) घोषित कर दिया।
- भारत ने न तो ‘परमाणु अप्रसार संधि’ (NPT) पर हस्ताक्षर किये हैं और न ही ‘व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि’ (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty- CTBT) को स्वीकृति दी है।
- भारत ने अपनी परमाणु नीति के तहत मुख्य रूप से तीन तत्त्वों को प्राथमिकता दी है- पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सुदृढ़ता; जो एक लोकतांत्रिक संप्रभु देश की भावना को प्रकट करता है।
भारत की परमाणु नीति के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं-- विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण एवं रखरखाव।
- परमाणु हथियारों से रहित किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना तथा परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों पर भी पहले आक्रमण नहीं करना।
- परमाणु आक्रमण होने पर जवाबी कार्यवाही इतनी सशक्त होगी कि दुश्मन की प्रतिक्रिया करने की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी।
- जवाबी परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार ‘परमाणु कमान प्राधिकरण’ (Nuclear Command Authority) के माध्यम से केवल राजनीतिक शक्ति होगा।
- भारत विश्व स्तर पर बिना भेदभाव वाले परमाणु नि:शस्त्रीकरण के द्वारा विश्व को परमाण्विक हथियारों से मुक्त कराने के अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहेगा।
- भारतीय सेना पर जैविक या परमाण्विक हथियारों से भारत पर या किसी स्थान पर हमले से नाभिकीय हथियारों के प्रयोग का विकल्प खुला रहेगा।
- भारत अपनी परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर सख्त नियंत्रण बनाए रखेगा।
‘प्रौद्योगिकी विज़न 2035’ का लक्ष्य सुरक्षा, समृद्धि में बढ़ोत्तरी और प्रत्येक भारतीय की अस्मिता को सुनिश्चित करना है। इसका उल्लेख संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के संबंध में दस्तावेज में ‘हमारी आकांक्षा’ या ‘विज़न वक्तव्य’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विज़न दस्तावेज में 12 विशेषाधिकारों (छः वैयक्तिक और छः सामूहिक) का उल्लेख भी किया गया है जो सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होंगे। ये इस प्रकार हैं-
वैयक्तिक विशेषाधिकार
- स्वच्छ वायु और पेयजल
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा और सार्वजनिक स्वच्छता
- 24 x 7 बिजली
- बेहतर आवास
- बेहतर शिक्षा, आजीविका और सर्जनात्मक अवसर
सामूहिक विशेषाधिकार
- सुरक्षित और तेज़ आवागमन
- सार्वजानिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा
- सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता
- पारदर्शी और प्रभावशाली शासन
- आपदा और जलवायु लोच
- प्राकृतिक संसाधनों का पारिस्थितिकीय अनुकूल संरक्षण
विज़न दस्तावेज के अनुसार ये विशेषाधिकार भारत के प्रौद्योगिकी विज़न के केंद्र में हैं। इन विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकियों का निर्धारण किया गया है-
- जिन्हें तेज़ी से तैनात किया जा सके;
- जिन्हें प्रयोगशाला से व्यवहार में लाया जा सके;
- जिनके लिये लक्ष्य अनुसंधान आवश्यक है, और
- जो कि अभी भी कल्पना में हैं।
प्रौद्योगिकियों के इन अंतिम वर्गों के संबंध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बायो प्रिंटिंग और रिजनरेटिव मेडिसिन जैसे उत्कृष्ट ‘ब्लू स्काई’ अनुसंधान उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा सटीक कृषि और रोबोट आधारित खेती, वर्टिकल खेती, इंटरेक्टिव फूड, ऑटोनोमस व्हीकल, बायोलूमिनेसंस, इमारतों की 3D प्रिंटिंग, भूकंप की भविष्यवाणी, मौसम प्रौद्योगिकियाँ, हरित खनन आदि ऐसी अन्य प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनसे मानव की वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी।
- यह छोटे समूह (5 सदस्यीय) के यात्रियों के लिये फीडर और शटल सेवा प्रदान करती है।
- यह बाधारहित परिवहन का अच्छा विकल्प है तथा मेट्रो से भी सस्ती सेवा होती है।
- यह ज़मीन से 5-10 मीटर ऊपर चलती है एवं वायरलेस, सेंसर और कमांड आधारित प्रणाली से संचालित होती है।
- एक तरफ यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी सहज होती है, वहीं यह सघन आबादी, संकरी सड़क एवं अन्य ज़मीनी यातायात के ऊपर से भी गुज़र सकती है।
- यह APM (Automated People Mover) पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ समय, धन व ईंधन की बचत में भी सहायक है।
- पॉड टैक्सी योजना को PRT (Personal Rapid Transit) भी कहा जाता है।
परियोजना के बारे में
- यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत DBFOT (डिज़ाइन, निर्माण, वित्तीयन, संचालन और हस्तांतरण) पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट है।
- 4000 करोड़ रुपये वाली यह परियोजना प्रारंभ में NH-8 के दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से राजीव चौक होते हुए गुरुग्राम तक 12.3 किमी. के लिये बनेगी।
- इस परियोजना को पूरा करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को दायित्व सौंपा गया है।
- प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस नगर-राज्य के एक कुलीन घराने में हुआ। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज (Aristocles) था, किंतु उसके शिक्षक (सुकरात) उसे प्लेटो कहा करते थे।
- लगभग 40 वर्ष की अवस्था में उसने एथेंस में अपने प्रसिद्ध स्कूल ‘अकादमी’ (Academy) की स्थापना की जिसमें वह अपनी आयु के अगले 40 वर्ष तक पढ़ाता रहा।
- ‘अकादमी’ में प्रवेश के लिये गणित का ज्ञान होना आवश्यक था।
- प्लेटो की ‘अकादमी’ में गणितशास्त्र के ज्ञान को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ‘अकादमी’ के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था- “गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है।” गणित के साथ ही वहां राजनीति, कानून एवं दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी।
- प्लेटो जब 70 वर्ष की आयु के लगभग पहुँच रहा था तब उसे अपने ‘आदर्श-राज्य’ के विचार को व्यवहार में लाने का अवसर प्राप्त हुआ।
- 361 ईसा पूर्व में उसने दियोनिसियस (Dionysius) नामक शासक के मार्गदर्शन में अपने मित्र डियोन की सहायता के लिये सिराक्यूज़ (Syracuse) की यात्रा की।
- प्लेटो ने शेष जीवन अपने अंतिम ग्रंथ ‘The Laws’ को लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की अपने एक शिष्य के विवाह समारोह में भाग लेने के दौरान मृत्यु हो गई
- प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं-
प्लेटो द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 38 के लगभग मानी जाती है किंतु उसके प्रामाणिक ग्रंथ केवल 28 हैं।
- The Republic (इसकी रचना करते हुए प्लेटो अत्यधिक उत्साहित प्रतीत होता है।)
- Statesman (इसकी रचना करते हुए प्लेटो के विचारों में निराशा दिखती है। सिराक्यूज़ में मिली असफलता ने उसे हतोत्साहित किया था।)
- The Laws
- The Symposium
- The Allegory of the Cave
- The Apology of Socrates (इसमें सुकरात की मौत की सज़ा का वर्णन है।)
- Meno
- Phaedo
- Gorgias
- Timaeus
- The Socratic Dialogue
- ‘बंगाल केमिकल्स’ के संस्थापक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को ‘भारतीय रसायनशास्त्र का पिता’ कहा जाता है।
- उनके उल्लेखनीय कार्यों में ‘हिंदू रसायनशास्त्र का इतिहास’ शामिल था। दो खंडों में प्रकाशित उनकी आत्मकथा ‘लाइफ एंड एक्सपीरियंसेज ऑफ ए बंगाली केमिस्ट’ उनके सर्वश्रेष्ठ कामों में शामिल है। यह आत्मकथा उनके जीवन और समय पर प्रकाश डालने के अलावा विशेषतः बंगाल और सामान्यतः भारत के बौद्धिक इतिहास को बताता है।
- वे गिलक्राइस्ट स्कॉलरशिप पाने वाले प्रारंभिक विद्यार्थियों में से थे। 1887 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाई।
- मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कई गुमनाम तत्त्वों को खोजने के लिये इंटरमीडिएट के रूप में जल में घुलनशील मरक्यूरस नाइट्रेट तैयार करने के दौरान उन्होंने अनेक दुर्लभ खनिजों का व्यवस्थित रासायनिक विश्लेषण किया। इसी दौरान उन्होंने 1896 में मरक्यूरस नाइट्राइट को खोजा और उसे वैज्ञानिक समुदाय के सामने लाए। उस समय इसे केवल एक यौगिक माना जाता था।
- उन्होंने बाद में लिखा भी कि मरक्यूरस नाइट्राइट की खोज ने मेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर दी। उनका एक और उल्लेखनीय योगदान अमोनियम नाइट्राइट का शुद्ध रूप में निर्माण रहा।
- 1911 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ‘नाइट’ की उपाधि से सम्मानित किया।
- 1933 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को डी.एस.सी. की मानद उपाधि से विभूषित किया।
- आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय महान वैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्री एवं आधुनिक भारत के मूर्धन्य शिल्पकारों में से थे।
- बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक एवं एक शक्तिशाली राजा था।
- 15 वर्ष में मगध साम्राज्य की बागड़ोर सँभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया।
- इसका अन्य नाम ‘श्रेणिक’ था (जैन साहित्य में)। हर्यक वंशी राजा श्रेणिक और क्षेत्रोजस उपाधि लगाते थे।
- इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। तब मगध की राजधानी राजगृह थी।
- बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसने तीन विवाह किये-
- प्रथम पत्नी महाकोशला देवी थी, जो कोशलराज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिससे एक लाख की वार्षिक आय होती थी।
- दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना (छलना) थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ।
- तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी।
- बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियाँ थीं।
- बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया था।
- बिंबिसार ने अवंति के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिये भेजा।
- बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ई.पू. में मगध की राजगद्दी पर बैठा।
- प्रमुख पदाधिकारी-
- सब्बत्थक महामात्र (सर्वाथक महामात्र)- सामान्य प्रशासन
- व्यावहारिक महामात्र- प्रधान न्यायाधीश
- सेनानायक महामात्र- सेना का प्रधान अधिकारी
- संघ में प्रविष्ट होने को ‘उपसंपदा’ कहा जाता था। संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले ‘श्रमण’ का दर्ज़ा मिलता था और 10 वर्षों बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी, तब उसे ‘भिक्षु’ का दर्जा मिलता था।
- संघ में अल्पवयस्क (15 वर्ष से कम आयु), चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था।
- आनंद के बहुत अनुनय-विनय के बाद बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को अनुमति दी थी।
- बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर जाति के लिये खुला था। अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया।
- संघ की सभा में प्रस्ताव (नत्ति) का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को ‘अनुसावन’ कहा जाता था। सभा की वैध कार्यवाही के लिये न्यूनतम संख्या (कोरम) 20 थी।
- अमावस्या, पूर्णिमा तथा दो चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में ‘उपोसथ’ (व्रत) कहा जाता है।
- पातिमोक्ख- भिक्षुओं की सभा में किये जाने वाले विधि-निषेधों का पाठ।
- इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों की समिति विचार करती थी और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी।
- वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह ‘पवरन’ कहलाता था।
- बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण दिन या त्योहार वैशाख की पूर्णिमा है, जिसे ‘बुद्ध पूर्णिमा’ भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई।
- बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में विभाजित थे- भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को ‘उपासक’ कहा जाता था।
- मानव सभ्यता के विकास में सूचना तकनीक को चौथी क्रांति माना जा रहा है, जिसका मूल आधार है- डिजिटल तकनीक। इस तकनीक में आंकड़ों को बाइनरी (0, 1) रूप में परिवर्तित कर सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली इसी तकनीक के आधार पर कार्य कर रही है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं-
- आंकड़ों, चित्रों व संदेशों की उच्च गुणवत्ता।
- सूचनाओं की संप्रेषण क्षमता एवं तीव्रता।
- त्रुटियों की संभावना एवं बाह्य हस्तक्षेप का नगण्य होना।
- डिजिटल तकनीक के द्वारा ग्लोबल विलेज (Global Village) की संकल्पना सार्थक होती दिख रही है क्योंकि किसी भी स्थान से किसी अन्य दूरस्थ स्थान को उपग्रहों के माध्यम से जोड़कर त्वरित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत जैसा विकासशील देश इस तकनीक के कारण विकास भी कर रहा है, किंतु इसी क्रम में एक तकनीकी समस्या ने भी जन्म लिया, जिसे ‘डिजिटल डिवाइड’ का नाम दिया गया है।
- यह एक ऐसी समस्या है जिसमें डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर रहे देशों के अंदर तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इसके उपयोग के आधार पर बड़ा आर्थिक अंतर उत्पन्न होता जा रहा है, जो सामाजिक समस्या को भी बढ़ा रहा है। इस प्रकार डिजिटल डिवाइड वह संकल्पना है जो डिजिटल तकनीक के उपयोग के आधार पर बढ़ रही आर्थिक-सामाजिक विषमता को व्याख्यायित करती है। इस समस्या के निवारण हेतु ‘डिजिटल कंवर्जेंस’ की अवधारणा अपनाई जा रही है। भारत सरकार ने इसके लिये दोहरी कार्यवाही को अपनाया है-
अवसंरचनात्मक विकास-
- इसके तहत वैसे क्षेत्रों में भी डिजिटल तकनीक से युक्त संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अभी तक पिछड़े हुए हैं। गुवाहाटी और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर पार्क व IIIT की स्थापना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- देश के पिछड़े क्षेत्रों को VSAT के माध्यम से बड़े सूचना केंद्रों से जोड़ा जा रहा है।
- देश के विभिन्न भागों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण के लिये नए शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
अनुप्रयोगात्मक प्रयास-
- ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे डिजिटल ज्ञान को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिये विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है।
- INSAT-3A द्वारा टेलीमेडिसिन तथा GSAT-3 द्वारा टेली एजुकेशन का प्रावधान कर सुदूर क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- गाँव व शहर के बीच आर्थिक विषमता को कम करने के लिये ‘GRAMSAT’ नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, जिसका उद्देश्य गाँवों के समुचित विकास को प्राप्त करना है। गाँवों में ज़मीन से जुड़े आंकड़ों की जानकारी के लिये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा नेटवर्किंग को विकसित किया जा रहा है, जिसमें SWAN (State Wide Area Network) उल्लेखनीय है।
DNA में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार (Nucleotide Bases) एडिनीन (A), थायमीन (T), साइटोसीन (C) तथा गुआनिन (G) को चरणबद्ध करने की क्रिया ही DNA अनुक्रमण कहलाती है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं-
- ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बड़ा उदाहरण है- DNA अनुक्रमण का।
- इसकी सहायता से विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों (Genetic Diseases), जैसे- अल्जाइमर (Alzheimer’s), सिस्टिक फाईब्रोसिस (Cystic Fibrosis), मायोटॉनिक डिस्ट्रोफी (Myotonic Dystrophy) और कैंसर (Cancer) आदि से निजात पाने में सहायता मिलेगी।
- जीन अनुक्रम (Gene Sequence) के माध्यम से पशुधन की वंशावलियों को जानने में मदद मिलेगी।
- इस प्रणाली की मदद से मानव जीन से संबंधित रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकेगा, परंतु सभी रोगों का ज्ञान केवल जीन अनुक्रमण से संभव नहीं है।
- पशुओं में रोगों से लड़ने वाली प्रजातियों का विकास किया जा सकेगा।
- यह प्रणाली रोगों के उपचार के लिये नई विधियों का पता लगाने में उपयोगी सिद्ध होगी।
- किसी भी व्यक्ति में रोग के लक्षण दिखने के पूर्व ही उसकी रोकथाम की जा सकेगी।
- ‘भुवन’ इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है, जिससे भारत के किसी भी क्षेत्र को इंटरनेट पर त्रि-विमीय (3D) रूप में देखा जा सकता है। ‘Google Earth’ तथा विकिमैपिया की तरह इसमें भू-भागों को अलग-अलग ऊँचाई से देखा जा सकता है।
- यह सॉफ्टवेयर अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल व तेलुगू भाषाओं में काम करता है।
- भुवन सॉफ्टवेयर पर भारत के 300 से अधिक शहरों की तस्वीरें उपलब्ध हैं।
- भुवन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी मददगार है।
- यह सॉफ्टवेयर पर्यावरण, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा नौवहन से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध करवाता है तथा पहचान हेतु मदद करता है।
- भुवन सॉफ्टवेयर की मदद भारत सरकार द्वारा संचालित ‘क्लीन गंगा’ जैसे अभियानों में ली जा रही है। ‘भुवन गंगा पोर्टल’ तथा ‘भुवन गंगा मोबाइल एप्लीकेशन’ इससे संबंधित हैं।
- ‘भुवन-गेल पोर्टल’ (Bhuvan-GAIL Portal) के माध्यम से गेल अपने पाइपलाइन की देख-रेख व सुरक्षा के लिये भुवन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।
- भुवन की कुछ सीमाएँ भी सामने आई हैं, जैसे- भुवन केवल ‘इंटरनेट एक्सप्लोरर’ में ही खुलता है। इसके अतिरिक्त धीमी रफ्तार, पंजीकरण आदि की भी समस्याएँ हैं।
- भारत में जब भी पुरा-वनस्पति विज्ञान की बात होती है तो प्रो. बीरबल साहनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने दुनिया के वैज्ञानिकों का परिचय भारत की अद्भुत वनस्पतियों से कराया।
- बीरबल साहनी को भारतीय पुरा-वनस्पति विज्ञान (इंडियन पैलियोबॉटनी) का जनक माना जाता है।
- प्रो. साहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति तथा पौधों के जीवाश्म पर महत्त्वपूर्ण खोज की। पौधों के जीवाश्म पर उनके शोध मुख्य रूप से जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर आधारित थे।
- प्रो. साहनी के योगदान का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि भारत में पुरा-वनस्पति विज्ञान का कोई भी पहलू उनसे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने वनस्पति विज्ञान पर अनेक पुस्तकों लिखीं और उनके अनेक शोध पत्र विभिन्न वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए।
- उल्लेखनीय है कि जीवाश्म वनस्पतियों पर अनुसंधान के लिये वर्ष 1919 में उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से ‘डॉक्टर ऑफ साइंस’ (D.Sc.) की उपाधि प्रदान की गई।
- प्रो. साहनी की पुरातत्त्व विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। भू-विज्ञान का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। प्राचीन भारत में सिक्कों की ढलाई की तकनीक पर उनके शोधकार्य ने भारत में पुरातात्त्विक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- प्रो. साहनी के कार्यों के महत्त्व को देखते हुए वर्ष 1936 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसायटी का सदस्य चुना गया।
- उनके द्वारा लखनऊ में जिस संस्थान की नींव रखी गई थी, उसे आज हम ‘बीरबल साहनी पुरा-वनस्पति विज्ञान संस्थान’ के नाम से जानते हैं। इस संस्थान का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1949 में किया था।
- प्रो. साहनी केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वे चित्रकला और संगीत के भी प्रेमी थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने उनके सम्मान में ‘बीरबल साहनी अवार्ड’ की स्थापना की है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को दिया जाता है।
- 19वीं सदी के यूरोप में जिस राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था उसकी अभिव्यक्ति इटली और जर्मनी के एकीकरण में हुई। वस्तुतः 19वीं सदी के आरंभ तक इटली कोई देश नहीं था। यह राजनीतिक दृष्टि से अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित था। यूरोप के विभिन्न राजवंश इटली के इन राज्यों पर अधिकार करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। यही कारण है कि मैटरनिक ने इटली को ‘एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र’ की संज्ञा दी थी। लेकिन उसका यह कथन सत्य प्रतीत नहीं लगता।
- यदि हम इटली की भौगोलिक स्थिति पर दृष्टिपात करें तो इसकी चौहद्दी को परिभाषित करने वाले तत्त्व वहाँ मौजूद थे। उत्तर में आल्प्स पर्वत तथा तीन तरफ समुद्र से घिरा यह प्रायद्वीप यूरोप के मध्य-दक्षिण में स्थित था। इसी तरह यहाँ इसे जोड़ने वाले तत्त्व भी विद्यमान थे, जैसे- रोमन साम्राज्य की याद यहाँ के लोगों में हमेशा बनी रहती थी, तत्कालीन यूरोप के साहित्य एवं धर्म की भाषा लैटिन थी जो कि इटली की ही भाषा थी। रोमन कैथोलिक धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में रोम इटली को धार्मिक एकता प्रदान करता था, साथ ही यहाँ एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता भी विद्यमान थी। इस तरह उपर्युक्त कारकों ने ही इटली के एकीकरण को प्रोत्साहन दिया।
- 1871 में जिस इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, वह कई चरणों और प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे निम्नलिखित चरणों में बाँटकर देखा जा सकता है-
- प्रथम चरण (1850 से पूर्व)- कर्बोनेरी एवं यंग इटली जैसी संस्थाओं के माध्यम से जनक्रांति के प्रयास। लेखकों के माध्यम से जागरूकता।
- द्वितीय चरण (1850-59)- सार्डिनीया ने आंतरिक सुधारों से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की एवं बाह्य स्तर पर काबूर के कूटनीतिक प्रयासों से इटली के एकीकरण को यूरोपीय स्तर पर प्रचारित किया। फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को 1859 में पराजित करके लोंबार्डी को प्राप्त किया।
- तृतीय चरण (1859-60)- ऑस्ट्रिया पर सार्डिनीया की विजय से उत्साहित परमा, मोडेना, टस्कनी का अंततः जनमत संग्रह से पीडमॉन्ट-सार्डिनीया में विलय।
- चतुर्थ चरण (1860-66)- नेपल्स एवं सिसली की प्राप्ति गैरीबाल्डी के सहयोग से।
- पांचवां चरण (1866-1871)- 1866 ई. में सेडोवा युद्ध में प्रशा के सहयोग से वेनेशिया की प्राप्ति एवं 1871 में रोम की प्राप्ति से एकीकरण पूर्ण।
परिचय
- रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर मठ (कोलकाता) में की थी।
- इसका नाम उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव और आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया था।
दर्शन एवं शिक्षाएँ
- मिशन वेदांत दर्शन और रामकृष्ण परमहंस की सार्वभौमिक शिक्षाओं पर आधारित है।
- इसका प्रमुख सिद्धांत है– “जीव ही शिव है”, अर्थात मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।
- यह आध्यात्मिक विकास को निष्काम कर्म (कर्म योग) के साथ जोड़ता है।
उद्देश्य और लक्ष्य
- व्यक्तियों व समाज का आध्यात्मिक उत्थान।
- बिना किसी भेदभाव के गरीबों, पीड़ितों और वंचितों की सेवा।
- सर्वधर्म समभाव और धार्मिक एकता को बढ़ावा देना।
- नैतिक, आध्यात्मिक व शैक्षणिक मूल्यों का प्रसार करना।
शैक्षिक एवं सामाजिक कार्य
- मिशन द्वारा देशभर में विद्यालय, महाविद्यालय एवं पुस्तकालय चलाए जाते हैं।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रावास और वृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण व आदिवासी कल्याण में भी मिशन सक्रिय है।
स्वास्थ्य सेवाएँ
- मिशन अस्पताल, औषधालय एवं मोबाइल क्लिनिक संचालित करता है।
- निःशुल्क चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
- आपदा राहत कार्यों में भी मिशन सक्रिय भूमिका निभाता है।
वैश्विक उपस्थिति
- मिशन की शाखाएँ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हैं।
- यह भारतीय दर्शन, योग और संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रचार करता है।
विरासत और प्रभाव
- रामकृष्ण मिशन ने आधुनिक भारतीय नवजागरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह आध्यात्मिकता और आधुनिकता के समन्वय पर बल देता है।
- स्वामी विवेकानंद का आह्वान – “युवा शक्ति के द्वारा राष्ट्र निर्माण”, आज भी प्रेरणा का स्रोत है।
यह एक ऐसी मशीन है जो ग्राहकों को बिना किसी बैंक शाखा या प्रतिनिधि की सहायता के संपूर्ण आधारिक लेन-देन, जैसे- बिना बैंक गए नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय लेन-देन के लिये अपने खाते तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करती है। भारत में सभी ATMs को जोड़ने वाले एटीएम नेटवर्क National Financial Switch का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है।
- बैंकों का स्वयं का एटीएम- यह बैंकों का स्वयं के स्वामित्व एवं संचालन वाला एटीएम होता है। बैंकों द्वारा स्वयं संचालित किये जाने से इसकी परिचालन लागत महंगी होती है। इसमें बैंक अपने लोगो का प्रयोग करते हैं।
- ब्राउन लेबल एटीएम (BLA)- तीसरे पक्ष द्वारा संचालित इस प्रकार के एटीएम में नकद की व्यवस्था तथा इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था संबंधित बैंक द्वारा की जाती है और अतिरिक्त सेवा (परिचालन एवं रख-रखाव) तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें भी बैंक अपने लोगो का प्रयोग करते हैं। संबंधित बैंक और संचालनकर्त्ता के मध्य एक समझौता होने के कारण रिज़र्व बैंक की इसमें प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है।
- व्हाइट लेबल एटीएम (WLA)- गैर-बैंकिंग इकाइयों के स्वामित्व में संचालित होने वाले एटीएम ‘व्हाइट लेबल एटीएम’ कहलाते हैं। इन पर किसी बैंक का लोगो नहीं होता है। 100 करोड़ रुपये के मूल्य की कोई भी गैर-बैंकिंग इकाई व्हाइट लेबल एटीएम के लिये आवेदन कर सकती है। एटीएम सुविधा को अत्यधिक तेज़ी तथा व्यापक रूप से फैलाने के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एटीएम परिचालित करने की अनुमति दी है। इन कंपनियों द्वारा दो-तिहाई एटीएम ग्रामीण इलाकों में लगाना अनिवार्य रखा गया है।
12 मार्च, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था है। समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत इस संस्था का पंजीकरण 7 जनवरी, 1956 को किया गया।
- अकादमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त चौबीस भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिये पुरस्कार प्रदान करती है। साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिये भी पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- इसका प्रमुख उद्देश्य प्रकाशन, अनुवाद, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं इत्यादि के माध्यम से भारतीय साहित्य के सतत् विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत देश भर में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और साहित्य सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।
- साहित्य अकादमी महान साहित्यकारों को साहित्य अकादमी ऑनरेरी फेलोशिप, आनंद फेलोशिप और प्रेमचंद फेलोशिप नामक सम्मानों से सम्मानित करती है।
- साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को जो सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया जाता है, वह उसे अपना फेलो चुनने के रूप में होता है।
- यह प्रतिवर्ष साहित्य के इतिहास एवं सौंदर्यशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर अनेक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं वार्षिक साहित्योत्सव का आयोजन करती है।
- साहित्य अकादमी तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है : इंडियन लिटरेचर (अंग्रेज़ी द्वैमासिक), समकालीन भारतीय साहित्य (हिंदी द्वैमासिक) और संस्कृत प्रतिभा (संस्कृत त्रैमासिक)
नोट- ‘साहित्य अकादमी’ की आधिकारिक वेबसाइट (sahityaakademi.gov.in) के अनुसार अकादमी की चार पत्रिकाएं इस प्रकार हैं- इंडियन लिटरेचर, समकालीन भारतीय साहित्य, संस्कृत प्रतिभा और आलोक (अर्द्धवार्षिक राजभाषा गृहपत्रिका)।
- पशुपालन कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा है, जिसके तहत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों, जैसे- भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है।
- भारत में पशुपालन का अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है एवं भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान भी रखता है।
- वर्ष 1919 से देश में पशुओं की गणना प्रारंभ हुई। आज़ादी के बाद प्रथम पशुधन गणना वर्ष 1951 में आयोजित की गई तथा उत्तरोत्तर हर पांचवें वर्ष यह गणना आयोजित की जाती है।
- पशुधन गणना के क्रम में वर्तमान पशुधन गणना के आंकड़े अक्तूबर 2019 में जारी किये गए थे, जो पशुधन गणना की 20वीं कड़ी है।
- पशुओं की प्रजातियों के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, खच्चर, गधे, ऊँट, मिथुन और याक को शामिल किया जाता है।
- 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, इसमें पशुधन गणना-2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि दर्ज़ की गई है।
- वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर-सरकारी निकाय (Inter-Governmental Body) है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में समूह-7 (G-7) के शिखर सम्मेलन में धन शोधन (Money Laundering) की समस्या के समाधान के लिये की गई थी। वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात् इसे आतंकी वित्तपोषण एवं संबंधित गतिविधियों की रोकथाम का अधिदेश प्रदान किया गया है।
- वर्तमान में FATF के कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग एवं खाड़ी सहयोग परिषद्) सदस्य हैं।
- FATF का मुख्यालय, जिसे ‘सचिवालय’ कहा जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के पेरिस स्थित मुख्यालय में है।
- धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता (Integrity) से संबंधित अन्य ख़तरों से निपटने के लिये मानकों का निर्धारण करना तथा वैधानिक, नियामकीय एवं परिचालन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देना वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) का मुख्य उद्देश्य है।
- भारत को वर्ष 2006 में कार्यबल के पर्यवेक्षक सदस्य का तथा वर्ष 2010 में पूर्ण सदस्य का दर्ज़ा प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका के लिये कार्यबल में भारत की सदस्यता बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह भारत को आतंकवाद से निपटने तथा आतंकी धन का पता लगाने, धन शोधन तथा आतंकी वित्त पोषण अपराधों की जाँच करने एवं मुकदमा चलाने में सहायक होगा।
- जीवन बीमा (Life Insurance)- जीवन बीमा मानव जीवन से जुड़ी आपात स्थितियों के लिये वित्तीय सुरक्षा देता है, जैसे- मृत्यु, दिव्यांगता, दुर्घटना इत्यादि। मानव जीवन प्राकृतिक और दुर्घटना के कारणों से मृत्यु और दिव्यांगता के जोखिमों के अधीन होता है। जब मानव जीवन का अंत होता है या व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से दिव्यांग होता है तो घर को आमदनी का नुकसान होता है। यद्यपि मानव जीवन का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भावी वर्षों में आय की हानि के आधार पर एक धनराशि निर्धारित की जा सकती है, इसलिये जीवन में आश्वासित राशि (या हानि के समय में अदा की जाने वाली गारंटीशुदा राशि) ‘लाभ’ के रूप में अदा की जाती है। जीवन बीमा उत्पाद पॉलिसी की अवधि के दौरान सीमित जीवन की मृत्यु के मामले में या दुर्घटना के कारण अपंग हो जाने पर एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)- स्वास्थ्य बीमा का संबंध बीमा के उस प्रकार से है जो प्रमुख रूप से आपके चिकित्सकीय खर्चों को कवर करता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बीमाकर्त्ता और व्यक्ति/समूह के बीच एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्त्ता विशिष्ट प्रीमियम पर निर्धारित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की सहमति देता है, जो पॉलिसी में वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन है।
- मोटर बीमा (Motor Insurance)- मोटर बीमा वाहन मालिक को अपने वाहन की क्षति के प्रति सुरक्षा देता है और वाहन के मालिक के प्रति कानून के अनुसार निर्धारित किसी तृतीय पक्ष की देयता के लिये भुगतान करता है। तृतीय पक्ष बीमा एक वैधानिक आवश्यकता है। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उपजे तीसरे पक्ष की ज़िंदगी या संपत्ति को क्षति या नुकसान के लिये वाहन का मालिक कानूनन जवाबदेह होता है।
- परिसंपत्ति बीमा (Asset Insurance)- परिसंपत्ति बीमा के के अंतर्गत इमारतों, मशीनरी, स्टॉक्स इत्यादि का आग और संबंधित ख़तरों तथा सेंध ख़तरे इत्यादि को बीमित किया जाता है। परिसंपत्ति बीमा साधारण बीमा की अत्यंत व्यापक श्रेणी है। समुद्र, वायु, रेलवे, रोड, कोरियर के ज़रिये सामानों के परिवहन को ‘मरीन कार्गो बीमा’ के तहत बीमित किया जा सकता है। इसके अलावा विमान और हेलीकॉप्टर्स का बीमा करने के लिये ‘एविएशन बीमा पॉलिसी’ जैसी विशेष पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं।
- यात्रा बीमा (Travel Insurance)- यात्रा बीमा आपके सफर के दौरान बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। यात्रा बीमा आप और आपके परिवार को यात्रा संबंधी दुर्घटनाओं, यात्रा के दौरान प्रत्याशित चिकित्सकीय खर्च, नुकसान जैसे कि सामान खोना, पासपोर्ट खोना इत्यादि और उड़ानों में बाधा या विलंब या सामान के विलंब से पहुँचने के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यात्रा बीमा देश के अंदर यात्रा या विदेश यात्रा या फिर दोनों से संबंधित होता है।
- मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म सहित आजीवक संप्रदाय का प्रचलन था। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, बिंदुसार आजीवक का तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
- सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था।
- मौर्य काल में भी वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था।
- जनसाधारण में नागपूजा का प्रचलन था। मूर्तिपूजा भी की जाती थी।
- पतंजलि के अनुसार, मौर्य काल में देवमूर्तियों को बेचा जाता था। देवमूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को ‘देवताकारू’ कहा जाता था।
- अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने कुछ गुफाएँ आजीवकों को दान में दी थीं।
- अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ।
- चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर जैन प्रथा ‘सल्लेखना’ के अनुसार प्राण त्याग दिये।
- मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः ‘शिव’ एवं ‘कृष्ण’ से की गई है।
- मेगस्थनीज ने मंडनिस एवं सिकंदर के बीच वार्तालाप का वृत्तांत दिया है।
- विश्वेश्वरैया योजना (Visvesvaraya Plan)- भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम. विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित ‘Planned Economy of India’ नामक पुस्तक में दिया गया है। यह योजना दस वर्षीय थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था-
- राष्ट्रीय आय को दोगुना करना;
- औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना;
- लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना।
- फिक्की का प्रस्ताव (The FICCI Proposal)- 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री’ (FICCI) ने राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के महत्त्व को समझा तथा इसका समर्थन भी किया। इसने नियोजन प्रक्रिया के समन्वय हेतु ‘राष्ट्रीय योजना आयोग’ की मांग की।
- कांग्रेस योजना (The Congress Plan)- वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिये ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ ने ‘राष्ट्रीय नियोजन समिति’ का गठन किया। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू थे।
- बॉम्बे प्लान (The Bombay Plan)- भारत के आठ प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसे ‘बॉम्बे प्लान’ के नाम से जाना है। इस आठ पूंजीपतियों में शामिल थे- पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, ए.डी. श्रॉफ, अर्देशिर दलाल तथा जॉन मथाई। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई। इसमें निम्न विषयों पर बल दिया गया-
- कृषि पुनर्संरचना;
- औद्योगीकरण पर बल एवं लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन;
- अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास;
- 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 65 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करना।
- गांधीवादी योजना (Gandhian Plan)- गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विस्तार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु, कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया।
- जन योजना (The People’s Plan)- एम.एन. रॉय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई।
- सर्वोदय योजना (The Sarvodaya Plan)- भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया।
- निवेश विवादों के समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिये समर्पित विश्व की अग्रणी संस्था है, जिसे निवेश विवादों के समाधान के संदर्भ में व्यापक अनुभव प्राप्त है।
- ICSID के सदस्य देशों ने विभिन्न संधियों, जैसे- द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) इत्यादि में तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में इसे निवेश विवाद समाधान मंच के रूप परिभाषित किया है।
- राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्र के नागरिकों के मध्य निवेश विवादों के समाधान पर कन्वेंशन, जिसे ICSID कन्वेंशन भी कहा जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत निवेश विवादों के समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना वर्ष 1966 में की गई। वर्तमान में इसमें हस्ताक्षरकर्त्ता (8) और अनुबंधित देशों (157) की कुल संख्या 165 है।
- ICSID कन्वेंशन विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित बहुपक्षीय संधि है, जो विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने में सहायक है।
- ICSID एक स्वतंत्र, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त तथा प्रभावी निवेश विवाद समाधान संस्था है। निवेशकों एवं राष्ट्रों के लिये इसकी उपलब्धता निवेश विवाद समाधान प्रक्रिया में भरोसा उत्पन्न करके अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने में सहायक है।
- ICSID की सुविधाएँ निवेश संधियों तथा मुक्त व्यापार समझौतों के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्र-राष्ट्र के मध्य विवादों के समाधान हेतु भी उपलब्ध हैं। यह सुलह (Conciliation), मध्यस्थता (Arbitration) तथा तथ्यान्वेषण (Fact Finding) के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रयास करते हैं।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार, “क्षेत्रीय व्यापार समझौते दो या दो से अधिक भागीदारों के बीच पारस्परिक व्यापार समझौतों के रूप में परिभाषित किये जाते हैं।”
क्षेत्रीय व्यापार समझौते के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार होते हैं-
- अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement)- यह राष्ट्रों के बीच एक प्रकार का व्यापार समझौता है जिसमें समझौते को स्वीकार करने वाले देशों को निश्चित उत्पादों हेतु प्रशुल्कों में कटौती की जाती है। इसके तहत सदस्य देश संघ में उत्पादित सामग्रियों पर निम्न व्यापार बाधाओं का प्रयोग करते हैं। उत्पादों की वह सूची जिस पर सदस्य देश प्रशुल्कों में कटौती हेतु सहमति प्रदान करते हैं, उसे सकारात्मक सूची कहते हैं। यह संघ में शामिल सभी सदस्य देशों को व्यापार बाधाओं में लचीलापन प्रदान करता है।
- मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement)- इस व्यापार समझौते के तहत मुख्यतः सदस्य देशों में उत्पादित वस्तुओं पर से प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क बाधाओं सहित सभी व्यापार बाधाएँ समाप्त कर दी जाती हैं; किंतु ज्यादातर समझौतों में संवेदनशील वस्तुओं की सूची को अलग रखा जाता है। इस समझौते के तहत सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को शामिल किया जाता है।
- सीमा शुल्क संघ (Customs Union)- एक सीमा शुल्क संघ के सदस्य (एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के विपरीत) आमतौर पर गैर-सदस्य देशों से आयात पर एक सामान्य बाह्य प्रशुल्क (Common External Tariff) अधिरोपित करते हैं, जबकि सदस्य देशों के मध्य शुल्क मुक्त व्यापार का निर्णय लेते हैं। इसमें सामान्यतः सदस्य देशों के मध्य पूँजी और श्रम का मुक्त संचलन नहीं होता है।
- साझा बाज़ार (Common Market)- इसके अंतर्गत सदस्य देश अपने बीच कुछ संस्थात्मक प्रावधानों, वाणिज्यिक एवं वित्तीय कानूनों तथा नियमनों के बीच समन्वय बैठाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन कारकों का मुक्त प्रवाह होता है। श्रम एवं पूँजी के मुक्त प्रवाह से भी नियंत्रण समाप्त किया जा सकता है। यूरोपियन साझा बाज़ार इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- आर्थिक संघ (Economic Union)- आर्थिक संघ एक साझा बाज़ार है जो राजकोषीय/मौद्रिक नीतियों के और अधिक समन्वय तथा साझे कार्यकारी, न्यायिक और विधायी संस्थाओं के माध्यम से विस्तारित है। आर्थिक संघ में सदस्य देश सामान्य नीतियों एवं नियमनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा संसाधनों के मुक्त संचलन की अनुमति प्रदान करते हैं। वे एकल मुदा भी अपना सकते हैं। यूरोपियन यूनियन इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात् नीति आयोग’ (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) का गठन किया गया। नीति आयोग, सरकार के थिंक-टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक-टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है एवं भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुवीक्षण करता है। यह संस्था राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है।
नीति आयोग के उद्देश्य
- राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना;
- सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना;
- ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचाना;
- आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना;
- अंतर-क्षेत्रीय एवं अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना;
- रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना।
नीति आयोग की संरचना
- नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष ‘भारत का प्रधानमंत्री’ होता है।
- गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो, को देखने के लिये क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिये बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती (Nominee) करेंगे।
- सचिवालय का गठन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- गिर नस्ल- यह मुख्य रूप से गुजरात (काठियावाड), महाराष्ट्र तथा आस-पास के क्षेत्रों में पाई जाती है एवं प्रतिदिन लगभग 15-20 लीटर दूध देती है।
- साहीवाल नस्ल- गायों की यह नस्ल अधिकतर उत्तर भारत में पाई जाती है तथा प्रतिदिन लगभग 20-25 लीटर दूध देती है। इस नस्ल की गाय के दूध में पर्याप्त मात्रा में वसा पाई जाती है।
- राठी नस्ल- यह नस्ल राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भागों में गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। यह प्रतिदिन लगभग 9-12 लीटर दूध देती है। यह रेगिस्तान में भारी-भरकम बोझ खींचकर चल सकती है।
- रेड सिंधी नस्ल- इस नस्ल की गाय का रंग लाल-बादामी होता है। इसका मुख्य स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत माना जाता है। यह प्रतिदिन लगभग 10-12 लीटर दूध देती है।
- हरियाणा नस्ल- दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाने वाली यह नस्ल उजले और हल्के धूसर रंग की होती है एवं प्रतिदिन लगभग 10-15 लीटर दूध देती है।
- इसके अतिरिक्त कांक्रेज, थारपारकर, मालवी, नागोरी, जर्सी, पोंवार, देवनी, निमाड़ी आदि गायों की नस्लें भारत में पाई जाती हैं।
- भारत में भैंसों की प्रमुख किस्मों में मुर्रा, भदावरी, नागपुरी, सुर्ती, मेहसाना, नीली-रावी तथा पढ़ारपुरी आदि प्रमुख हैं।
- पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व में चौथे एवं एशिया में दूसरे स्थान पर है। भारत से पहले क्रमशः चीन, अमेरिका तथा जर्मनी का स्थान है।
- भारत में पवन ऊर्जा का विकास वर्ष 1990 के दशक से प्रारंभ किया गया।
- पवन ऊर्जा के लिये राष्ट्रीय संस्थान (NIWE) 1998 में चेन्नई में स्थापित किया गया।
- पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को ‘पवन ऊर्जा’ कहते हैं।
- पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिये पवन चक्कियों को सामान्यतः उन स्थानों पर लगाया जाता है, जहाँ पवनें बिना किसी बाधा (अवरोध) के तेज़ गति से बहती रहती हैं। यही कारण है कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान आदि राज्यों के तटीय एवं मैदानी क्षेत्र पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- गुजरात के कच्छ में 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा की इकाई स्थापित की जा रही है। यह एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है।
- भारत विश्व में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है।
- भारत में राज्यवार सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश का स्थान है।
- महाद्वीपीय शेल्फ एवं गहरे समुद्री मैदान के मध्य के अत्यंत तीव्र ढाल वाले अर्थात् इन्हें जोड़ने वाले महासागरीय क्षेत्र को ‘महाद्वीपीय ढाल’ कहते हैं।
- यह क्षेत्र शेल्फ अवकाश से आरंभ होकर 2० से 5० की ढाल प्रवणता के साथ महासागरीय बेसिन तक विस्तृत होता है। सामान्यतया इसकी गहराई 200 मीटर से लेकर 3,000 मीटर तक होती है। इसी के अंतर्गत कैनियन (गहरी गर्त) एवं खाइयों जैसी समुद्री संरचनाएं भी पाई जाती हैं लेकिन इस क्षेत्र में निक्षेप नहीं पाए जाते हैं।
- यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर विस्तृत है।
- महाद्वीपीय ढाल की सीमा समाप्ति के क्षेत्र में जो कम ढाल वाला क्षेत्र होता है (जो कि अतितीव्र ढाल वाले महाद्वीपीय ढाल से अलग नज़र आता है) उसे ‘महाद्वीपीय उत्थान’ (Continental Rise) कहते हैं।
- गहराई बढ़ते हुए यह क्षेत्र समतल रूप में महासागरीय नितल में मिल जाता है।
राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण ‘पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय’ के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है जो वन्यजीव अधिनियम, 1972 (2006 में संशोधित) के तहत कार्य करता है। यह टाइगर रिज़र्व संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं-
- यह राज्यों द्वारा टाइगर संरक्षण के लिये बनाई गई योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें मंज़ूरी प्रदान करता है।
- यह भविष्य में संरक्षण के प्रयासों में गुणात्मक सुधार, आवास क्षेत्रों में सुधार आदि के लिये सूचनाएं प्रदान करता है।
- संरक्षण कार्यों में लगे हुए लोगों को अपने आपको सुरक्षित रखने के लिये प्रशिक्षण देता है एवं टाइगर रिज़र्व को बेहतर बनाने के लिये अधिकारियों के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाता है।
|
राजवंश |
संस्थापक |
राजधानी |
|
हर्यक वंश |
बिंबिसार |
राजगृह, पाटलिपुत्र |
|
शिशुनाग वंश |
शिशुनाग |
पाटलिपुत्र, वैशाली |
|
नंद वंश |
महापद्मनंद |
पाटलिपुत्र |
|
मौर्य वंश |
चंद्रगुप्त मौर्य |
पाटलिपुत्र |
|
शुंग वंश |
पुष्यमित्र शुंग |
पाटलिपुत्र |
|
कण्व वंश |
वासुदेव |
पाटलिपुत्र |
|
सातवाहन वंश |
सिमुक |
प्रतिष्ठान |
|
कुषाण वंश |
कुजुल कडफिसस प्रथम |
पुरुषपुर (पेशावर), मथुरा |
|
गुप्त वंश |
श्रीगुप्त |
पाटलिपुत्र |
|
पुष्यभूति वंश |
पुष्यभूति |
थानेश्वर, कन्नौज |
|
पल्लव वंश |
सिंहविष्णु |
कांचीपुरम् |
|
पाल वंश |
गोपाल |
मुंगेर |
|
गुर्जर प्रतिहार वंश |
हरिश्चंद्र |
कन्नौज |
|
सेन वंश |
सामंत सेन |
राढ़ |
|
गहड़वाल वंश |
चंद्रदेव |
कन्नौज |
|
चौहान वंश |
वासुदेव |
अजमेर |
|
चंदेल वंश |
नन्नुक |
खजुराहो |
|
गंग वंश |
वज्रहस्त पंचम |
पुरी |
|
उत्पल वंश |
अवंतिवर्मन |
कश्मीर |
|
परमार वंश |
उपेंद्र |
धार, उज्जैन |
|
सोलंकी वंश |
मूलराज प्रथम |
अन्हिलवाड़ |
|
चोल वंश |
विजयालय |
तंजावुर |
- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक वृहत् अंब्रेला स्कीम है। इसके द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ उन्हें तटीय राज्यों एवं उनके बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत गैर-प्रमुख पत्तनों (Non-major Ports) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से ‘भारतमाला परियोजना’ चलाई जा रही है। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
- परियोजना के प्रथम चरण, जिसकी अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है, के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों में शामिल हैं-
- राष्ट्रीय कॉरिडोर- 5,000 किमी.
- आर्थिक कॉरिडोर- 9,000 किमी.
- इंटर-कॉरिडोर एवं फीडर सड़कें- 6,000 किमी.
- तटवर्ती एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें- 2,000 किमी.
- सीमावर्ती संपर्क सड़कें- 2,000 किमी.
- हरित क्षेत्र एक्सप्रेस-वे- 800 किमी.
- अधूरे सड़क निर्माण कार्य- 10,000 किमी.
|
स्रोत |
विशेषताएँ |
|
भारत शासन अधिनियम, 1935 |
संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। |
|
ब्रिटेन का संविधान |
विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। |
|
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान |
मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। |
|
आयरलैंड का संविधान |
राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिये सदस्यों का नामांकन। |
|
कनाडा का संविधान |
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। |
|
ऑस्ट्रेलिया का संविधान |
समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। |
|
जर्मनी का वाइमर संविधान |
आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। |
|
सोवियत संघ (पूर्व) का संविधान |
मूल कर्त्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श। |
|
फ्रांस का संविधान |
गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। |
|
दक्षिण अफ्रीका का संविधान |
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। |
|
जापान का संविधान |
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। |
- बेरूबारी संघ मामले (1960) में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है क्योंकि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर-न्यायिक है अर्थात् इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- इसके पश्चात् सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले (1964) में, न्यायमूर्ति मधोलकर द्वारा प्रस्तावना के संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय पर विचार किये जाने की आवश्यकता पर ध्यानाकर्षित किया गया।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले (1967) में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है।
- अंततः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में, अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद-विवादों के पश्चात् प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया।
- प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं- उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता, जो ‘आधारभूत ढाँचे’ से संबंधित है।
- आनंद- ये महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे। इसका प्रमुख योगदान स्त्रियों को संघ के सदस्य के रूप में भिक्षुणी बनाना था। इसी के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी।
- सारिपुत्त- सारिपुत्त राजगृह का ब्राह्मण था। यह बुद्ध का अत्यंत प्रिय शिष्य था। इसकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जीवन काल में हुई थी। इसकी मृत्यु पर बुद्ध अत्यंत दुखी एवं शोक संतृप्त हुए थे।
- मोद्गलायन- यह भी राजगृह का ही निवासी था और सारिपुत्त के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। इसकी मृत्यु भी बुद्ध के जीवन काल में ही हुई थी।
- उपालि- उपालि भी बुद्ध का प्रिय शिष्य था। यह जापित का पुत्र था और इसका पिता शाक्य वंश में नाई का कार्य करता था।
- अनाथपिंडक- यह श्रावस्ती का प्रसिद्ध व्यापारी था। इसने चेतकुमार से जेतवन नामक विहार खरीदकर बुद्ध को दान दे दिया था।
- बिंबिसार- यह मगध का शासक था। इनकी पत्नी भी भिक्षुणी बन गई थी। कोशल के नरेश प्रसेनजित और मगध का शासक अजातशत्रु (बिंबिसार का पुत्र) भी बुद्ध के परम अनुयायी थे।
- महाकश्यप- बुद्ध का अनुयायी जिसका जन्म मगध के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति में यह संघ का अध्यक्ष था।
- जीवक- यह मगध नरेश बिंबिसार का राजवैद्य था। यह उच्चकोटि का आयुर्वेद का ज्ञाता था। इसकी माता सालबति राजगृह की गणिका थी।
- ब्रिटिश सरकार ने कैंपबेल आयोग की संस्तुतियों को गंभीरता से नहीं लिया था परिणामतः 1876-78 के दौरान मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिर से भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी थी। आर.सी. दत्त के अनुसार 50 लाख लोग कालग्रस्त हो गए। सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, “किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी शक्ति से परे है और करदाता और प्रभावित जनता दोनों के हित में नहीं है।“
- 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग का कार्य अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिये सुझाव देना था। आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की-
- लोगों को रोज़गार मिले और समय-समय पर मज़दूरी का पुनर्निर्धारण हो।
- अकाल संहिता का निर्माण हो।
- सिंचाई सुविधाएँ विकसित हों।
- अकाल के समय भू-राजस्व का संग्रहण रोक दिया जाए।
- अकाल कोष का गठन हो।
- अकाल सहायता का खर्च प्रांतीय सरकारों को वहन करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सहायता भी दी जाएगी।
- सरकार द्वारा इस आयोग की सिफारिशें कुछ हद तक स्वीकार कर ली गईं। अकाल कोष हेतु राजस्व के लिये अन्य स्रोतों को खोजने का प्रयत्न किया गया। 1883 की अकाल संहिता की तर्ज़ पर प्रांतीय अकाल संहिता का निर्माण किया गया।
- 1866 में भारत में कई हिस्सों में अकाल पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र ओडिशा था। इस अकाल की समीक्षा करने हेतु ‘जॉर्ज कैंपबेल आयोग’ गठित किया गया।
- आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अकाल जैसी घटनाओं के लिये सरकार ज़िम्मेदार है क्योंकि पूर्व सूचना देने के बावजूद सरकार द्वारा इसको नियंत्रित करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिकारी वर्ग मांग और पूर्ति के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए, मुक्त व्यापार की नीति पर चलते रहे।
- आयोग ने सुझाव दिया कि अकाल के दौरान राहत कार्यों की ज़िम्मेदारी का निर्वहन समाज सेवी संस्थाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिये। सरकार को रेलों और नहरों की स्थापना करनी चाहिये ताकि अकाल के प्रभाव को कम किया जा सके।
- ज़िलाधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक संभावित मृत्यु को रोका जाए।
- यद्यपि आयोग के सुझाव के अनुसार सरकार द्वारा राहत कार्य किये गए लेकिन उनकी मात्रा अत्यल्प थी।
- 19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। यह कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है।
- इस योजना का क्रियान्वयन सभी राज्य एवं केंद्रशासित सरकारों के कृषि विभागों के माध्यम से किया जाएगा।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्त्वों की स्थिति की सही जानकारी देना है और उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग और आवश्यक मृदा सुधारों के संबंध में भी सलाह देना है, ताकि लंबी अवधि के लिये मृदा स्वास्थ्य को कायम रखा जा सके।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है, जिसे किसान को उसकी प्रत्येक जोतों के लिये दिया जाएगा।
- इसमें 12 पैरामीटरों, जैसे- नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम (मुख्य पोषक तत्त्व), सल्फर (गौण पोषक तत्त्व), ज़िंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन (सूक्ष्म पोषक तत्त्व) और pH, EC, OC (भौतिक पैरामीटर) के संबंध में उनकी मृदा की स्थिति निहित होगी।
- मृदा की अम्लीयता, लवणीयता तथा क्षारीयता को जांचकर मृदा की गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में खेती के लिये अपेक्षित मृदा सुधार और उर्वरक सिफारिशों को भी दर्शाया जाएगा।
- इस प्रकार, मृदा में जिस तरह की समस्या हो, उसी तरह का निदान किया जाता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये देश में सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत प्रथम तीन वर्षों में 14 करोड़ किसानों को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना की टैग लाइन है- स्वस्थ धरा, खेत हरा।
- कहवा की खेती के लिये उष्ण-आर्द्र जलवायु, 16०C-28०C तापमान, 150-250 सेमी. वार्षिक वर्षा, गहरी व भुरभुरी (Friable) दोमट या लावा निर्मित मिट्टी व ढलानयुक्त भूमि की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी का प्रवर्द्धन कहवा के बीजों के द्वारा होता है।
- भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत ‘बाबा बूदान की पहाड़ियों’ से हुआ। वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरि पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में प्रमुख रूप से किया जा रहा है।
- कॉफ़ी की तीन किस्में- अरेबिका, रोबस्टा एवं लिबेरिका हैं।
- विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत में कहवा की दो किस्में ‘अरेबिका’ तथा ‘रोबस्टा’ उगाई जाती हैं। ‘रोबस्टा’ किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है।
- भारत में कॉफ़ी उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमशः कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु हैं।
- कॉफ़ी बोर्ड भारत के बंगलुरू में स्थित है।
- भारत विश्व में कॉफ़ी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक एवं पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
- जर्मनी यूरोपीय महाद्वीप का एक महत्त्वपूर्ण देश है, इसके उत्तर-पश्चिम में उत्तर सागर तथा उत्तर-पूर्व में बाल्टिक सागर स्थित है।
- जर्मनी के उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया तथा स्विट्ज़रलैंड, पश्चिम में फ्रांस, लक्जमबर्ग, बेल्जियम तथा नीदरलैंड स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन है जो सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- जर्मनी को भौतिक विशेषताओं के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है- उत्तरी मैदान और दक्षिणी उच्चभूमि व पर्वतीय क्षेत्र।
- उत्तरी मैदान यूरोप के विशाल मैदान का ही एक भाग है तथा दक्षिणी उच्चभूमियों में अनेक भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे- आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, ब्लैक फारेस्ट पठारी क्षेत्र, हार्ज़ पर्वत आदि।
- जर्मनी में पर्वत घाटियों से अनेक नदियों का उद्गम होता है जो न केवल कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है बल्कि खनिज संसाधनों की उपस्थिति के कारण जर्मनी में अनेक उद्योगों का विकास इन्हीं नदी घाटियों में हुआ है। जर्मनी की प्रमुख नदियाँ राइन, रूर, मैन, वेसर, एल्बे, ओडर और डेन्यूब हैं।
- राइन नदी फ्रांस व जर्मनी की सीमा बनाती है, वहीं ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारित करती है। रूर राइन की सहायक नदी है, जो बिटुमिनस कोयला के लिये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
- रूर बेसिन को ‘जर्मनी का काला प्रदेश’ तथा ‘औद्योगिक हृदय स्थल’ कहा जाता है। ‘राइन’ और ‘रूर’ के औद्योगिक क्षेत्रों में ही जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है।
- जर्मनी का ‘पिग-आयरन’ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
- राइन बेसिन में स्थित फ्रेंकफर्ट जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है।
- म्यूनिख इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार उद्योग के लिये, कोलोन मोटरवाहन उद्योग के लिये, एसेन लौह-इस्पात उद्योग के लिये प्रसिद्ध हैं।
|
क्रम संख्या |
जलधारा का नाम |
जलधारा की प्रकृति |
|
1. |
उत्तर विषुवतरेखीय धारा |
गर्म |
|
2. |
विपरीत विषुवतरेखीय धारा |
गर्म |
|
3. |
गिनी धारा |
गर्म |
|
4. |
एंटीलीज धारा |
गर्म |
|
5. |
फ्लोरिडा धारा |
गर्म |
|
6. |
गल्फस्ट्रीम धारा |
गर्म |
|
7. |
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह |
गर्म |
|
8. |
लैब्राडोर धारा |
ठंडी |
|
9. |
पूर्वी ग्रीनलैंड धारा |
ठंडी |
|
10. |
इरमिंजर धारा |
ठंडी |
|
11. |
नॉर्वे धारा |
गर्म |
|
12 |
रेनेल धारा |
ठंडी |
|
13. |
कनारी धारा |
ठंडी |
|
14. |
दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा |
गर्म |
|
15. |
ब्राज़ील धारा |
गर्म |
|
16 |
फ़ॉकलैंड धारा |
ठंडी |
|
17. |
बेंगुला धारा |
ठंडी |
|
18. |
अंटार्कटिक प्रवाह |
ठंडी |
आर्थिक अपराधों, जैसे- नकली सरकारी स्टांप या करेंसी बनाना, पर्याप्त धन न होने के कारण चेक का भुनाया न जाना, मनी लॉण्डरिंग और क्रेडिटर्स के साथ लेन-देन में धोखाधड़ी करना इत्यादि पर अंकुश लगाने के लिये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम- 2018 बनाया गया है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों पर नकेल कसना है जो आर्थिक अपराध करके देश से बाहर चले जाते हैं और वापस आने से इंकार कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-
- इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति 100 करोड़ या इससे अधिक राशि का आर्थिक अपराध करता है और मुकदमा नहीं लड़ता है/हों तथा देश छोड़कर चला जाता है एवं वापस आने से मना कर देता है, तो उसे आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जा सकता है।
- विशेष अदालत द्वारा धन शोधन (निवारण) अधिनियम- 2002 के अंतर्गत अपराधी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।
- विशेष अदालत द्वारा किसी आरोपी की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा सकता है।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसी सिविल दावे का बचाव करने के लिये अपात्र हो सकता है।
हाल ही में राज्यसभा में आम चुनावों में होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा हटाए जाने संबंधी गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा की गई थी।
प्रमुख बिंदु
- विधेयक को इस आधार पर पेश किया गया है कि चुनावों में खर्च की अधिकतम सीमा के कारण उम्मीदवार किये गए खर्च पर गलत आंकड़े पेश करते हैं।
- चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत लोकसभा के उम्मीदवार के अधिकतम खर्च की सीमा 70 लाख रुपये है, वहीं 28 लाख रुपये तक के अधिकतम खर्च की सीमा विधानसभा उम्मीदवारों के लिये निर्धारित की गई है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत, प्रत्येक उम्मीदवार नामांकन की तिथि और परिणाम की घोषणा की तिथि के बीच किये गए सभी व्यय का अलग एवं सही हिसाब रखेगा।
- सभी उम्मीदवारों को चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
- चुनाव में किये गए व्यय के गलत विवरण के आधार पर चुनाव आयोग उम्मीदवार को उम्मीदवार अधिनियम, 1951 की धारा 10A के तहत तीन साल तक के लिये अयोग्य घोषित कर सकता है।
- गौरतलब है कि किसी राजनीतिक पार्टी के खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जिसका अक्सर पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। हालाँकि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण चुनाव आयोग को सौंपना होगा।
विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के स्थान पर 16 दिसंबर, 2016 को संसद में दिव्यांग अधिकार विधेयक-2016 पारित किया गया जिसमें दिव्यांगता को एक उभरती और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगों के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-
- इस अधिनियम में विकलांगता के बहुआयामी स्वरूप को उजागर किया गया है।
- दिव्यांग अधिनियम में दिव्यांगजनों को 7 श्रेणियों से 21 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस अधिनियम के तहत सेरिब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया, मल्टीपल सक्लेरोसिस, ऑटिज्म और थैलेसीमिया को भी शामिल किया गया है।
- इस अधिनियम में एसिड हमले से पीड़ित भाषा से संबंधित विकलांगता को पहली बार शामिल किया गया है।
- सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है।
- पहली बार इस अधिनियम में दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों तथा अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान किये गए हैं।
- दिव्यांग समस्याओं के लिये स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया है ताकि त्वरित न्याय को सुनिश्चित किया जा सके।
रासायनिक खादों के लगातार व असंतुलित प्रयोग से हमारी कृषि भूमि एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मिट्टी में जीवांश की मात्रा घटने से उसकी उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप हमारे जलाशयों एवं भूमि के नीचे का जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसलिये कृषि भूमि में पोषक तत्त्वों की कमी को पूरा करने के लिये जैविक उर्वरकों, जैसे- गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद व जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिये। जैविक उर्वरक लाभकारी जीवाणुओं के वो उत्पाद हैं, जो मिट्टी एवं हवा से मुख्य पोषक तत्त्वों, जैसे- नाइट्रोजन व फॉस्फोरस का दोहन कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं।
जैविक उर्वरकों के उपयोग से लाभ
- जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में लगभग 10-15% की वृद्धि होती है।
- ये रासायनिक खादों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जरूरत का 20-25% तक पूरा करते हैं।
- इनके प्रयोग से अपेक्षाकृत अंकुरण शीघ्र होता है।
- जैविक उर्वरकों के द्वारा मृदा में कार्बनिक पदार्थ (ह्यूमस) की वृद्धि तथा मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार होता है।
- इनके प्रयोग से अच्छी उपज के अतिरिक्त गन्ने में शर्करा की, मक्का एवं आलू में स्टार्च तथा तिलहनों में तेल की मात्रा में वृद्धि होती है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारत सरकार द्वारा 1997 में किया गया।
- यह एक सांविधिक निकाय है तथा देश में दूरसंचार के कारोबार का एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है।
- दूरसंचार के क्षेत्र में उदारीकरण तथा निजी क्षेत्र का भागीदारी के विषय में इसके गठन को आवश्यक समझा गया था। इसके द्वारा सभी ऑपरेटरों के लिये Level Playing Field उपलब्ध कराया गया, जिसमें ट्राई के नियम, निर्देश एवं आदेश समाहित थे।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम में 2000 में कुछ संशोधनों द्वारा पूरे दूरसंचार नियामक ढाँचे तथा विवाद समाधान तंत्र को मज़बूत बनाया गया। ट्राई के कार्यों एवं भूमिका में स्पष्टता लाने के अलावा इसे कुछ अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए थे।
- विवादों के शीघ्र समाधान के लिये दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) नाम से एक अलग विवाद समाधान निकाय का गठन भी किया गया।
- ट्राई देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ट्राई दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाता है।
- ट्राई की विभिन्न शक्तियों और कार्यों में कुछ निम्नलिखित हैं-
- दूरसंचार सेवाओं में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- समय की अवधि निर्धारित करना एवं सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।
- दूरसंचार संचालन सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना।
- सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करना।
भारत में कृषि उत्पादों के बाज़ार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, 2003 के अधीन विनियमित किया जाता है। अप्रैल, 2017 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नए आदर्श APMC कानून की घोषणा की, जिसमें राज्य सरकारों को छूट है कि वे उसमें अपनी आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकती हैं। मॉडल APMC कानून के तहत निम्नलिखित व्यवस्था कि गई है-
- उपभोक्ताओं और किसानों के लिये बाज़ार निर्माण करना, जिसमें किसान प्रत्यक्ष रूप से अपने कृषि उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके;
- बाज़ार में मध्यवर्ती संस्थाओं के समान पंजीकरण की अनुमति देकर कृषि उत्पाद के बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना;
- किसान अपने कृषि उत्पादों को सीधे ठेके पर कृषि प्रायोजकों को बेच सकते हैं;
- बाज़ार क्षेत्र में बेचे जा रहे कृषि उत्पादों पर एक बाज़ार शुल्क की व्यवस्था करना;
- बाज़ार में कार्य कर रहे लोगों के लाइसेंस की जगह पंजीकरण की व्यवस्था करना, ताकि उन्हें एक या एक से अधिक बाज़ार में संचालन की अनुमति मिल सके;
- APMC के ज़रिये कमाए गए राजस्व से बाज़ार के आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना।
यह आदर्श कानून राज्य सरकारों को APMC बाज़ारों के गठन का अधिकार देता है। इनमें से बहुत सारे राज्यों ने आदर्श APMC कानून के प्रावधानों को आंशिक तौर पर अपनाया है और अपने APMC कानून में आवश्यक बदलाव भी किये हैं।
- केंद्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया था।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना, सिंचित भूमि क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाना था।
- इसके अंतर्गत खेतों में नालियों तथा अतिरिक्त पानी के निकास के लिये नाले बनाने का काम, भूमि का उचित आकार के भूखंडों में विभाजन, खेतों के लिये सड़क बनाना, चकबंदी की व्यवस्था करना, जोतों की सीमा का पुनर्निर्धारण, बारी-बारी पानी देने की बाड़ाबंदी प्रणाली लागू करना, मंडियों एवं गोदामों का निर्माण तथा कृषि संबंधित कार्यों के लिये भूमिगत जल के विकास के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।
- वर्ष 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके इसका नामकरण ‘कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम’ (Command Area Development and Water Management Programme- CADWM) कर दिया गया है।
6. बोमडी ला दर्रा
- यह अरुणाचल प्रदेश (उत्तर-पूर्वी) में अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है।
- बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है।
7. दिफू दर्रा
- दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में (उत्तर-पूर्वी हिमालय) भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है।
- अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले (म्यांमार) के बीच एक छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। भारत एवं म्यांमार के बीच यह एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिये पूरे वर्ष खुला रहता है।
8. काराकोरम दर्रा
- काराकोरम दर्रा, हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है जो भारत एवं चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है।
- भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान समय में आने-जाने के लिये बंद कर दिया गया है तथा चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे का अतिक्रमण कर लिया गया है।
- हिमालय पर्वत शृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित है।
9. रोहतांग दर्रा
- रोहतांग दर्रा हिमालय प्रदेश (लघु हिमालय) में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है।
- रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है क्योंकि अन्य समय बर्फीले तूफान तथा हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है।
- रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश के ‘लाहुल-स्पीति’ ज़िले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा ‘कुल्लू’ और ‘लाहुल-स्पीति’ को आपस में जोड़ता है।
- रोहतांग दर्रे (हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी) में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 9.02 किमी. लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किमी. तक कम करती है।
10. बुर्जि ला दर्रा
- बुर्जि ला वृहत् हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है।
- बुर्जि ला, कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में यह बंद हो जाता है।
- यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख से ‘देवसाई मैदान’ से जोड़ता है।
- बनिहाल दर्रा
- यह जम्मू-कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत शृंखला में स्थित है तथा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है।
- श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग ‘NH-44’ इसी दर्रे से गुजरता है।
- शीत ऋतु में यहाँ बर्फ का जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। अतः पूरे वर्ष आवागमन के लिये वर्ष 1956 में यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से ‘जवाहर सुरंग’ का निर्माण किया गया।
- लानक ला
- यह ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख एवं तिब्बत (भारत-चीन) के बीच संपर्क स्थापित करता है।
- वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानक ला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र ‘अक्साई चीन’ का हिस्सा है।
- अपने सामरिक महत्त्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिये सड़क मार्ग का निर्माण किया है।
- नाथू ला दर्रा
- यह सिक्किम के वृहत् हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं ल्हासा (भारत-चीन) के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु वर्ष 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया
- यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था।
- ज़ोजिला दर्रा
- यह जास्कर श्रेणी में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है।
- श्रीनगर-ज़ोजिला मार्ग के सामरिक महत्त्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग ‘NH-1’ घोषित किया गया है तथा इसके निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य Border Roads Organisation को सौंपा गया है।
- लिपुलेख दर्रा
- लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊँ श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है।
- मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है।
- लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिये स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है।
- यह भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है।
आयतनमंडल अथवा बहिर्मंडल
- यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर है, जिसका विस्तार आयनमंडल से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग में है।
- यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम हो जाता है, जिसके कारण यह निहारिका जैसा प्रतीत होता है।
- यहाँ पर तापमान लगभग 5,000०C से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया जा सकता है।
- आयनमंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को ‘बाह्य वायुमंडल’ भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आयतनमंडल एवं चुंबकमंडल को सम्मिलित किया जाता है।
- इस मंडल में Van Allen Radiation Belt की उपस्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी के ‘मैग्नेटिक फील्ड’ द्वारा पकडे गए आवेशित कण पाए जाते हैं।
- आयतनमंडल के पश्चात् वायुमंडल सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है।
- मध्य सीमा से ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को ‘तापमंडल’ कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊँचाई के साथ तापमान में तीव्रगति से वृद्धि होती है और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदाब न्यूनतम होता है।
- तापमंडल की विशिष्टताओं के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है-
- आयनमंडल (Ionosphere)
- आयतनमंडल अथवा बहिर्मंडल (Exosphere)
आयनमंडल
- मध्यमंडल के ऊपर आयनमंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 से 640 किमी. के मध्य पाया जाता है। अन्य कई स्रोतों में इसका विस्तार 400 किमी. तक ही माना जाता है।
- आयनमंडल में आयनों अर्थात् विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिये आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके ‘संचार व्यवस्था’ को संभव बनाता है।
- इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस व अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं जो एक प्रकार की सौर्यिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रान तरंग होती हैं।
- इस मंडल में ऊँचाई के साथ-साथ कई परतों का विकास होता है: D, E, F तथा G परतें।
- D परत- इसका विस्तार लगभग 80 से 99 किमी. के मध्य है। यह परत न्यून आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन करती है, परंतु उच्च एवं मध्यम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल्स को अवशोषित कर लेती है। यह परत सौर्यिक विकिरण से संबंधित है, इसलिये सूर्यास्त के साथ लुप्त होती है।
- E परत- इस परत को ‘केनली हैवीसाइड परत’ भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 99 से 150 किमी. के मध्य तक है। यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। इस परत का निर्माण सौर्यिक पराबैंगनी फोटॉन का नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने से होता है। यह परत भी सूर्यास्त के साथ ही विलुप्त हो जाती है।
- F परत- इस परत का निर्माण दो उप-परतों से हुआ है, F1 परत तथा F2 परत। इसको ‘एप्लीटन परत’ भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 150 से 380 किमी. के मध्य पाया जाता है। यह परत मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है।
- G परत- इसका विस्तार लगभग 400 किमी. से ऊपर पाया जाता है। यह लगभग 400 से 640 किमी. के मध्य उपस्थित रहती है।
- यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान का ग्रह है।
- इसके चारों ओर वलयों (छल्लों) का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसे छल्लेदार ग्रह भी कहते हैं।
- इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी. है जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है।
- शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है।
- लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिये लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे Ring Crossing की घटना कहते हैं।
- इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इसे ‘गैसों का गोला’ भी कहते हैं।
- शनि का घूर्णन काल 10 घंटा, 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष (कुछ स्रोतों में 29 वर्ष, 5 माह) का होता है।
- शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह Titan है।
- इसके 82 उपग्रह हैं, जिसमें ‘ऐंसेलेडस’ नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं।
- यह अंतिम ग्रह है जिसे आँखों से देखा जा सकता है।
- Titan शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है।
- ‘फ़ोबे उपग्रह’ शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है।
- यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था, परंतु अंग्रेज़ों के पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात् यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया।
- पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल (सियान साहिब) एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई।
- 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने ज़ोर पकड़ा।
- 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना इस विद्रोह का मूल उद्देश्य था।
- 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया जहाँ 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इस आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया गया।
- कूका आंदोलनकारी स्वयं के हाथों से बने वस्त्र पहनते थे। इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया। हम कह सकते हैं कि कूका आंदोलन में ‘असहयोग’ और ‘सविनय अवज्ञा’ आंदोलन के तत्त्व मौजूद थे।
- 24 दिसंबर, 2014 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कूका आंदोलनकारियों के वीरतापूर्ण कार्यों को सम्मान व पहचान देने हेतु एक संस्मरणीय स्टाम्प जारी किया गया।
नोट- बाबा राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन (12 अप्रैल, 1857) चलाया था, जिसमें मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था।
इस अधिनियम की विशेषताएँ अधोलिखित थीं-
- इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है।
- इस एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी लेकिन उसका भुगतान कंपनी करेगी।
- डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किये जाने थे।
- सरकारी नियुक्तियों के लिये प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। सिविल सेवाओं के लिये भी प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया।
- विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
- सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया।
- छः सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) का गठन किया गया तथा सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इसमें यह भी निर्दिष्ट था कि गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्य अनुबंधित सेवक (Covenanted Servant) ही होंगे।
- भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी चार के स्थान पर तीन सदस्यों वाली परिषद् के हाथ में दे दिया गया। यद्यपि उसे अभी भी बहुमत के आधार पर कार्य करना होता था।
- बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर, बंबई तथा मद्रास की परिषद् का गठन किया गया और बंगाल को उनके अधीक्षण का अधिकार भी दे दिया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा किसी को सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था।
गरीबी रेखा से संबद्ध वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरण प्रदान करने वाली ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में 1 अप्रैल, 2017 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरणों को शिविरों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ये सहायक उपकरण उच्च गुणवत्ता से युक्त होंगे और इन उपकरणों को भारत मानक ब्यूरो द्वारा तय मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय योजना है, जिसके लिये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- योग्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी दिव्यांगता/दुर्बलता के अनुरूप निशुल्क उपकरणों का वितरण किया जाएगा। एक ही व्यक्ति में अनेक दुर्बलता पाए जाने की स्थिति में, प्रत्येक दुर्बलता के लिये अलग-अलग उपकरण प्रदान किये जाएंगे।
- ये उपकरण वरिष्ठ नागरिकों को आयु संबंधी शारीरिक दिक्कतों से निपटने में मदद करेंगे और परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर उनकी निर्भरता को कम करते हुए उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देंगे।
- योजना को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) नामक एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा।
- भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम बुजुर्गों को दी जाने वाली इस सहायता एवं सामान्य जीवन जीने के लिये आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निशुल्क देख-रेख करेगा।
- प्रत्येक ज़िले में लाभार्थियों की पहचान राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उपायुक्त/जिलाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी के ज़रिये की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जहाँ तक संभव होगा, प्रत्येक ज़िले में 30% बुजुर्ग महिलाओं को लाभार्थी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- BPL श्रेणी के बुजुर्गों की पहचान करने के लिये राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या ज़िलास्तरीय कमेटी, NASP अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे BPL लाभार्थियों के आंकड़े एवं जानकारियों का उपयोग कर सकते हैं।
महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये की गई थी-
- महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना
- सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा
- शिकायतों के सुधार की सुविधा
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना
आयोग के सदस्य
- महिलाओं के हित के लिये समर्पित एक अध्यक्ष, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
- पांच सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य योग्य, एकीकृत और अस्थायी होंगे तथा कानून अथवा विधान, व्यापार संघ, महिलाओं के उद्यमिता प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव रखते हों; साथ ही यह भी ध्यान यह भी ध्यान रखा जाए कि इनमें से कम-से-कम एक सदस्य क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होगा।
- केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक सचिव स्तर का अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित हो।
- अनिवासी भारतीय के साथ होने वाले विवादों से निपटने के लिये सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को नामित किया गया है। आयोग का अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ अंतर्देशीय विवादों से संबंधित भारत या विदेशों से प्राप्त शिकायतों, जिनमें महिलाओं के साथ गंभीर अन्याय किया गया है, जैसे मामले देखता है।
बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में शुभारंभ किया गया।
- कार्य योजना के चार प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-
- अस्तित्व
- स्वास्थ्य एवं पोषण
- शिक्षा और विकास
- संरक्षण और भागीदारी
- कार्य योजना का महत्त्व
- बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना इन चार प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत प्रगति मापने के लिये उद्देश्य, उप-उद्देश्य, रणनीतियाँ, कार्यबिंदु और संकेतकों को परिभाषित करती है।
- यह योजना संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) पर ध्यान देगी एवं उन्हें प्राप्त करने हेतु रोडमैप प्रदान करेगी।
यह योजना बच्चों के लिये उभरती चिंताओं जैसे ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन आदि से प्रभावित बच्चों इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करती है। यह योजना बच्चों से संबंधित नए और उभरते मुद्दों के लिये यथा आवश्यक नए कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करने का भी सुझाव देती है।
वाणिज्यिक यौन शोषण एवं दुर्व्यापार से पीड़ित महिलाओं का बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्एकीकरण एवं दुर्व्यापार रोकथाम के लिये वर्ष 2007 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। ऐसे यौनकर्मी जो स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति के पेशे में हैं, यदि वे पुनर्वास के लिये इच्छुक हों तो वे भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पुनर्वास सुविधाओं का लाभ उठा सकती है।
कार्यान्वयन एजेंसी : कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य सरकारों के सामाजिक कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, महिला विकास नियम, महिला विकास केंद्र, शहरी स्थानीय संस्थाएँ, सार्वजनिक एवं निजी ट्रस्ट एवं स्वैच्छिक संगठन सम्मिलित हैं।
इस योजना का 5 घटक हैं-
- निवारण : सामुदायिक जागरूकता समूहों और किशोर समूहों का निर्माण। पुलिस और सामुदायिक नेताओं में सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री और कार्यशालाओं द्वारा जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना।
- बचाव : शोषण स्थल से पीड़ित को सुरक्षित निकालना।
- पुनर्वास : पीड़ितों के लिये सुरक्षित निवास जहाँ आधारभूत आवश्यकताओं, जैसे- भोजन, वस्त्र, परामर्श, चिकित्सकीय देखभाल, विधिक सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय उत्पादक गतिविधियों की आपूर्ति की जाती है।
- पुनः एकीकरण : पीड़ित का परिवार/समुदाय (केवल तभी जब वह चाहे) में पुनः एकीकरण करना और इसमें आने वाली लागत का भुगतान करना।
- स्वदेश वापसी : सीमा-पारीय पीड़िता को सुरक्षित स्वदेश लौटने में मदद करना।
नोट : ध्यातव्य है कि 1 मई, 2016 को शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ इस योजना से भिन्न है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना BPL कार्डधारकों के लिये LPG कनेक्शन मुहैया कराने से संबंधित है।
- 8 मार्च, 2010 (महिला दिवस के दिन) को भारत सरकार द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की शुरुआत की गई।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के सम्मिलन द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण करना है।
- इस मिशन के संस्थागत तंत्र का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध निदेशक और अपर सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय इकाई के गठन के माध्यम से किया जा रहा है।
- इस मिशन में एक कार्यकारी निदेशक तथा इसके सदस्यों में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और पोषण, जेंडर बजटिंग, महिलाओं के अधिकार और कानून कार्यान्वयन, हाशिये पर रहने वाली और कमज़ोर महिलाओं के सशक्तीकरण, मीडिया जागरूकता, जनसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।
राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं-
- बच्चों का घटता लिंगानुपात
- महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा
- बाल विवाह
- जेंडर बजटिंग और महिलाओं को मुख्यधारा में लाना
- शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल में लड़कियों कि दाखिला दिलाना
- शोषित और हाशिये पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को मुख्यधारा में लाना
- मानव तस्करी पर रोक लगाना
- NMEW महिला सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य भी करता है। इनमें लड़कियों में साक्षरता का स्तर, बच्चों के गिरते लिंगानुपात के बारे में संचार रणनीतियाँ और महिला संबंधी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन जैसे विषय शामिल हैं।
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के द्वारा मातृत्व अवकाश की अवधि, प्रासंगिकता और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होता है।
- इसके तहत प्रत्येक महिला 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हक़दार होगी।
- पुराने अधिनियम के तहत इस मातृत्व लाभ का उपयोग प्रसव की अपेक्षित तारीख से छः सप्ताह से पहले नहीं किया जाना चाहिये। अब यहाँ अवधि ‘आठ सप्ताह’ कर दी गई है।
- किसी महिला के दो बच्चे होने की स्थिति में मातृत्व लाभ 12 सप्ताह का दिया जाना ज़रुरी होगा।
- इसके अनुसार नियोक्ता अवकाश अवधि के दौरान घर से काम करने के लिये किसी महिला को अनुमति दे सकता है।
- मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन भी मिलेगा और तीन हज़ार रुपये का मातृत्व बोनस भी मिलेगा।
- पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसको ‘निम्न भू-भागों’ व ‘पठारों का देश’ कहते हैं।
- अफ्रीका में सर्वाधिक पाम ऑयल उत्पादन करने वाले देश नाइजीरिया को ‘तेलताड़’ की भी संज्ञा दी जाती है।
- मूंगफली यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है, जिसका नाइजीरिया निर्यात करता है; साथ-ही-साथ कोको का भी यहाँ वृहत् स्तर पर उत्पादन किया जाता है।
- नाइजीरिया के दक्षिणी भाग में विषुवत रेखीय जलवायु, मध्य क्षेत्र में सवाना तथा उत्तर में मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हुआ है।
- सवाना घास के मैदान में पशुपालन किया जाता है। वहीं विषुवत रेखीय जलवायवीय क्षेत्रों में वनों का विकास हुआ है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उत्तर-पूर्व दिशा से गर्म व धूल भरी हवाएँ चलती हैं, जिन्हें ‘हरमट्टन’ कहा जाता है।
- यहाँ के उत्तरी भाग में ‘जोस का पठार’ तथा मध्यवर्ती भाग में ‘अडामावा उच्चभूमि’ अवस्थित है। मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र टिन के भंडार से संपन्न है।
- इसके अतिरिक्त नाइजीरिया में लोहा, शीशा, जस्ता व मैंगनीज़ के भंडार भी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ कोयले का उत्पादन भी किया जाता है।
- यहाँ के मध्यवर्ती क्षेत्र से नाइजर नदी का प्रवाह होता है। नाइजर नदी के मुहाने पर नाइजीरिया का महत्त्वपूर्ण बंदरगाह ‘पोर्ट हारकोर्ट’ स्थित है जो पाम ऑयल व क्रूड ऑयल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। तेल ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है।
- नाइजर नदी पर ‘कैंजी बांध’ का निर्माण किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई व जलविद्युत उत्पादन करना है। नाइजर की प्रमुख सहायक नदी ‘बेन्यू’ है जो उससे पूर्व दिशा से आकर मिलती है।
- नाइजीरिया का ‘लागोस नगर’ जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है।
- हाउसा, फुलानी व योरुबा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। हाउसा व फुलानी ‘मुस्लिम धर्म’ का तथा योरुबा ‘ईसाई धर्म’ का पालन करती है। योरुबा यहाँ की समृद्ध जनजाति है, वहीं हाउसा कृषक तथा फुलानी पशुपालक जनजाति है।
- इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 के दशक में ‘आर्थर होम्स’ ने किया।
- होम्स के अनुसार पृथ्वी के मैंटल भाग में रेडियोएक्टिव तत्त्वों के विघटन से उत्पन्न तापीय भिन्नता के फलस्वरूप संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलकर लिथोस्फेयर से टकराती हैं तथा दो भागों में बंट जाती हैं।
- जहाँ पर ये संवहनीय धाराएँ टकराती हैं, वहाँ का भाग कमज़ोर हो जाता है तथा कालांतर में संवहनीय धाराएँ अपने प्रवाह के कारण लिथोस्फेयर को विखंडित कर देती हैं, जिससे महाद्वीपों का विखंडन होता है।
- होम्स ने स्पष्ट किया कि संवहन धाराएँ एक कोशिका के रूप में विकसित होती हैं, साथ ही पृथ्वी के मैंटल भाग में ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है। इससे स्थलखंडों में एक प्रकार का ‘प्रवाही बल’ कार्य करता है, जिसके सहारे ‘महाद्वीपीय संचलन’ की प्रक्रिया संपन्न होती है।
- सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को ‘समदाब रेखा’ कहते हैं।
- धरातलीय सतह पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है।
- समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, जिसे ‘दाब प्रवणता’ कहते हैं। जहाँ समदाब रेखाएँ पास-पास हों, वहाँ दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर-दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है।
- इस अंतर के कारण जो बल उत्पन्न होता है, वह हवा में क्षैतिज गति उत्पन्न करता है इसे वायुदाब प्रवणता बल कहते हैं। इसकी इकाई ‘मिलीबार’ होती है। इसको ‘बैरोमेट्रिक ढाल’ भी कहते हैं। वायुदाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, पवनों की गति उतनी ही अधिक होगी।
- सामान्य नियमानुसार वायु की दिशा समदाब रेखाओं के समकोण पर होनी चाहिये, क्योंकि वायुदाब प्रवणता की दिशा समदाब रेखाओं की लंबवत दिशाओं में होती है, परंतु वास्तविक स्थिति में अपेक्षित सैद्धांतिक दिशा से विचलन होता है।
- वायु की दिशा में यह विचलन पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न ‘विक्षेप बल’ या ‘कोरिऑलिस बल’ के कारण होता है। अतः हवाएँ समदाब रेखाओं को समकोण पर न काटकर न्यूनकोण पर काटती हैं।
- अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों की सघनता है, यहाँ अनेक प्रकार के वृक्षों और जीव-जंतुओं का विकास हुआ है।
- यहाँ के वृक्षों में महोगनी, आबनूस और शाल्मली जैसे वृक्षों की लकड़ियाँ आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
- अफ्रीका के ‘कांगो गणराज्य’ को ‘विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर’ कहते हैं, यहाँ के कांगो बेसिन में सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है।
- दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक क्षेत्र में जिराफ़ व ज़ेबरा जैसे प्रसिद्ध जानवर मिलते हैं, वहीं कालाहारी मरुस्थल ‘बस्टर्ड’ व ‘शुतुरमुर्ग’ जैसे पक्षियों का आवास स्थल है।
- अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में गोरिल्ला तथा चिम्पांजी पाए जाते हैं। अन्य जंतुओं में मगरमच्छ, सांप, बंदर, अजगर, दरियाई घोड़ा आदि महत्त्वपूर्ण हैं। वहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंटों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है।
- वन्यजीवों के संरक्षण हेतु अनेक राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों का विकास किया गया है। अफ्रीका के जंगल पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। केन्या का ‘मसाई मारा नेशनल पार्क’ इसके लिये बहुत प्रसिद्ध है।
- पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। इसके पश्चिम में ईरान, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण-पूर्व में भारत और दक्षिण में अरब सागर स्थित है।
- सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है तथा इसके द्वारा निर्मित मैदान को ‘सिंधु का मैदान’ कहते हैं। यह मैदान पाकिस्तान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से अनेक नहरों का निर्माण किया गया है, यही कारण है कि पाकिस्तान को ‘नहरों का देश’ कहते हैं।
- किरथर, हिंदुकुश एवं सुलेमान यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। हिंदुकुश पर्वत की चोटी ‘तिरिचमीर’ (7708 मी.) पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है।
- खैबर दर्रा ‘हिंदुकुश’ में, जबकि बोलन दर्रा ‘किरथर’ श्रेणी में स्थित है।
- पाकिस्तान के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में ‘स्वात घाटी’ स्थित है, जिसे ‘पाकिस्तान का स्वर्ग’ कहा जाता है।
- पाकिस्तान में ‘साल्टरेंज’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थल है जो सेंधा नमक, जिप्सम व चूना पत्थर के लिये महत्त्वपूर्ण है। यहाँ के मरुस्थलीय क्षेत्र में विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक ‘जैकोबाबाद’ स्थित है।
- पाकिस्तान के नगरीकृत देश है, जिससे यहाँ अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ ‘सुई’ व ‘मियाल’ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के लिये तथा ‘क्वेटा’ कोयले के लिये प्रसिद्ध है।
- ‘इस्लामाबाद’ पाकिस्तान की राजधानी है तथा ‘कराची’ यहाँ का सबसे बड़ा नगर है।
- पाकिस्तान के अधिकतर निवासी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तथा उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है।
- जापान एशिया की मुख्यभूमि से अलग प्रशांत महासागर ने स्थित एक द्वीपीय देश है।
- यहाँ की जलवायु कप उद्योग हेतु अनुकूल है। यहाँ सस्ते एवं कुशल श्रमिक उपलब्धता तथा पन-बिजली की सर्वाधिक संभावना है।
- इसे ‘सूर्योदय का देश’ (निप्पौन), ‘भूकंपों का देश’ और ‘पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन’ कहा जाता है।
- यह अनेक द्वीपों पर स्थित है किंतु इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में होंशू, होकैडो, क्यूशू, शिकोकू चार प्रमुख द्वीप हैं, जिन पर जापान की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है।
- जापान की मध्यवर्ती घाटी में स्थित ज्वालामुखियों की श्रृंखला को फोसा मैग्ना कहते हैं।
- होंशू द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान ‘क्वांटो’ व सुसुप्त ज्वालामुखी ‘फ्यूजीयामा’ स्थित हैं।
- होंशू द्वीप पर ही जापान की औद्योगिक पेटी का विकास हुआ है तथा इसी द्वीप पर जापान की राजधानी ‘टोक्यो’ स्थित है।
- ‘वीवा झील’ जापान की मीठे पानी की महत्त्वपूर्ण झील है। यह होंशू द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी ‘शिनानो’ है।
- जापान के दक्षिणी तट पर उष्णकटिबंधीय तूफ़ान आते हैं, जिसे ‘टायफून’ कहा जाता है।
- जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोशिवो जलधारा (गर्म) व ओयाशिवो जलधारा (ठंडी) आकर मिलती हैं, जिससे मछलियों के लिये अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि जापान के पूर्वी तट पर वृहद् स्तर पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।
- जापान का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने से यहाँ की कुल उपलब्ध भूमि (14%) पर कृषि की जाती है। साथ ही, पर्वतीय ढालों पर भी सीढ़ीदार कृषि की जाती है।
- ओसाका को ‘जापान का मैनचेस्टर’ तथा नगोया को ‘जापान का डेट्रॉयट’ एवं ‘जापान का ब्रेडफोर्ट’ कहा जाता है।
- जापान में औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण हैं- कुशल श्रम, औद्योगिकी, जल विद्युत आदि।
- यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं।
- जापान की व्यावसायिक फसलें चाय, तंबाकू, गन्ना हैं।
- जापान अधिकांश खनिज संसाधनों का आयात करता है किंतु मशीनरी उद्योग में उन्नत तकनीक का प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में यह प्रमुख निर्यातक देशों में से एक है।
- जापान मोटर वाहन, इस्पात, समुद्री जहाज़, विविध प्रकार की मशीनों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात करता है।
- जापान के प्रमुख बंदरगाह योकोहामा, कोबे, नगोया तथा ओसाका हैं।
- एशिया में सर्वाधिक जलविद्युत का विकास जापान में हुआ है।
- होंशू द्वीप पर ही हिरोशिमा, नगोया, योकोहामा, क्योटो तथा ओसाका शहर भी स्थित हैं।
- ‘क्योटो’ जापान की पुरानी राजधानी होने के साथ-साथ हस्तकला उद्योग के लिये भी प्रसिद्ध है।
- नागासाकी एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
- जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का विध्वंस भी झेला था।
- हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी भाग तथा प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है।
- इस मृदा के निर्माण पर पर्वतीय पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय पर्यावरण में परिवर्तन के अनुरूप मृदा की संरचना व संघटन में भी परिवर्तन होता है। घाटियों में प्रायः यह दुमटी तथा ऊपरी ढालों पर इनकी प्रकृति मोटे कणों वाली होती है; साथ ही ऊपरी ढालों की अपेक्षा निचली घाटियों में ये मृदाएँ अधिक उर्वर होती हैं।
- पर्वतीय मृदा का विकास सामान्यतः पर्वतों के ढालों पर होता है तथा मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होने के कारण यह पतली परतों के रूप में पाई जाती है। अतः साधारणतः यह अप्रौढ़ (Immature) मृदा है।
- पर्वतीय मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि यहाँ जीवाश्मों की अधिकता होने के बावजूद भी जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है। इसमें पोटाश, फॉस्फोरस एवं चूने की कमी होती है।
- इस मृदा में गहराई कम होती है तथा यह सरंध्रयुक्त होती है।
- पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण यह मृदा बागानी कृषि; जैसे- चाय, कहवा, मसालों एवं फलों की खेती के लिये बहुत उपयोगी होती है।
- यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है, जिसका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है, जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें (ग्रेनाइट तथा नीस) पाई जाती हैं।
- इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्रों, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों तथा मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी इस मृदा का विकास हुआ है।
- प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होने के कारण इस ‘मंडलीय मृदा’ भी कहते हैं।
- लोहे के ऑक्साइड (मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड) की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है।
- इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह स्वभाव से अम्लीय प्रकृति की होती है।
- महीन कण वाली लाल व पीली मृदाएँ सामान्यतः उर्वर होती हैं, जबकि मोटे कणों वाली मृदाएँ अनुर्वर होती हैं।
- लाल मृदा ऊँची भूमियों पर बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती के लिये उपयोगी है, जबकि निम्न भूमियों पर इसमें चावल, रागी, तंबाकू तथा सब्जियों आदि की खेती की जाती है।
- हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की परिघटना है जो भारत के उत्तर-पश्चिम हिस्सों में गर्मियों के मौसम के दौरान सामान्य तापमान से अधिक होती है। हीट वेव आमतौर पर मार्च और जून के बीच पाई जाती है और कुछ मामलों में इसका जुलाई तक विस्तार होता है।
- वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण दीर्घकालीन तथा प्रचंड उष्ण लहरों की आवृत्ति में वृद्धि हो गई है। भारत में मानव स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों का अनुभव किया जा रहा है। इसके कारण मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस हीट वेव का असर भारत के विभिन्न आय वर्गों पर अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। निम्न आय वर्ग को हीट वेव सर्वाधिक प्रभावित करती है।
- हीट वेव से निपटने के लिये NDMA ने निम्नलिखित रणनीति अपनाई है-
- पूर्वानुमानित उच्च और अत्यधिक तापमान पर निवासियों को चेतावनी देने के लिये पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) और अंतर-एजेंसी समन्वयन (Inter-Agency Co-ordination) की स्थापना करना।
- स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों (Health Care Professionals) के लिये क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और सूचना, शिक्षा और संचार सामग्रियों के माध्यम से हीट वेव से बचने के लिये सार्वजनिक जागरूकता सुनिश्चित करना।
- गैर-सरकारी संगठनों व नागरिकों का समाज के साथ सहयोग व समन्वय स्थापित करना।
उपर्युक्त रणनीतियों के माध्यम से हीट वेव एक्शन प्लान बनाकर इसके प्रभाव को कम करने की योजना बनाई गई है।
- यह दो शब्दों ‘रुपी’ यानी रुपया तथा ‘पेमेंट’ यानी भुगतान से मिलकर बना है। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई एक नई कार्ड भुगतान योजना है। इसे एक घरेलू, ओपन लूप, बहुपक्षीय प्रणाली प्रदान करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण को पूरा करने हेतु शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की इस प्रणाली में भाग लेने की अनुमति होगी।
- भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम के गठन का मूल उद्देश्य सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिये राष्ट्रव्यापी, एकसमान और मानक व्यापार प्रक्रिया में विभिन्न प्रणालियों के साथ अलग-अलग सेवा स्तरों को समेकित तथा एकीकृत करना था। रुपे भुगतान कार्ड की शुरुआत मार्च, 2012 में की गई तथा मई, 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। रुपे कार्ड भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क है। 2017 से रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई।
- रुपे कार्ड के माध्यम से प्रत्येक लेन-देन की लागत में कमी आएगी। इससे भारतीय उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके माध्यम से लेन-देन करने पर संबंधित डाटा भारत में ही रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जो बैंकिंग सेवाओं की पहुँच से लगातार बाहर हैं उन्हें भी रुपे कार्ड के ज़रिये बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाया जाएगा।
- वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को ‘एयरोसॉल’ कहा जाता है। इसके अंतर्गत धूलकण, राख, कालिख, परागकण, नमक, जैविक पदार्थ (बैक्टीरिया) इत्यादि आते हैं।
- यह एक परिवर्तनशील प्रकृति का तत्त्व है, जिसकी मात्रा विभिन्न कारणों से घटती-बढ़ती रहती है।
- इसकी मात्रा वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घटती जाती है।
- ऊपरी वायुमंडल में एयरोसॉल की उपस्थिति मुख्यतः उल्काओं के विघटन, ज्वालामुखी उद्भेदन तथा प्रचंड आँधियों इत्यादि के फलस्वरूप होती है।
- इसके कारण ही सूर्य से आने वाले प्रकाश का ‘वर्णात्मक प्रकीर्णन’ होता है, जिससे कई प्रकार के नयनाभिराम (Picturesque) आकाशीय रंगों का आविर्भाव होता है।
- एयरोसॉल अथवा धूलकण आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित एयरोसॉल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से हो जाता है तो ‘धूम कोहरे’ (Smog) का निर्माण होता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर, 2016 को ‘भीम ऐप’ (Bharat Interface for Money App) नामक एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया।
- भीम ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस ऐप द्वारा अन्य UPI खाता या पतों पर पैसा भेजा सकता है। जिन उपयोगकर्त्ताओं के पास UPI नहीं है उन्हें IFSC और मोबाइल मनी आइडेंटीफायर के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं।
- भीम ऐप एक UPI आधारित ऐप है जो सीधे बैंक खाते से जुड़ा होता है।
- भीम ऐप उपयोगकर्त्ताओं को मोबाइल नंबर या उनके नाम के आधार पर वास्तविक समय में भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- भीम ऐप में प्रमाणीकरण के लिये तीन घटकों का प्रयोग किया जाता है।
- पहले चरण में ऐप को मोबाइल डिवाइस आईडी और मोबाइल नंबर से जोड़ा जाता है।
- दूसरे चरण में प्रयोगकर्त्ता अपने बैंक खाते को भीम ऐप से जोड़ता है।
- तीसरे चरण में प्रयोगकर्त्ता को ट्रांजेक्शन करने के लिये एक UPI पिन बनाना पड़ता है।
- यह पेटीएम या मोबिक्विक की तरह एक मोबाइल वॉलेट नहीं है।
- आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)
- देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना वर्ष 1990 की जगह वर्ष 1992 से लागू की जा सकी।
- इसका प्रमुख उद्देश्य ‘सर्वांगीण मानव विकास’ था। इसी में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना की शुरुआत हुई।
- औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्त्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल दिये जाने की शुरुआत हुई।
- योजना ने अपने लक्ष्य से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की।
- नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
- इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता ‘सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास’ को दी गई।
- अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण योजना का आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।
- प्राथमिकता क्रम में सुधार के क्षेत्रों को चुना गया। ये थे- भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋणभार कम करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)
- इसका उद्देश्य ‘देश में गरीबी और बेरोज़गारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना’ था।
- इस योजना ने निर्धारित लक्ष्य 8% वार्षिक वृद्धि दर के करीब 7.6% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया तथा यह अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)
- योजना लक्ष्य ‘तीव्र एवं समावेशी विकास’ था।
- इसे भी सफल योजना में गिना जाता है। इस योजना में औसत संवृद्धि दर 8% रही।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)
- मुख्य उद्देश्य ‘तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास’ है।
- इस योजना में विकास दर 8%, कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10 % वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया।
- 5 करोड़ रोज़गार सृजन, गरीबी को कम-से-कम 10% बिंदु तक कम करना।
- योजना के अंत तक शिशु मृत्यु दर 25 तथा मृत्यु दर को 1 प्रति हज़ार जीवित जन्म तक लाने तथा 0-6 वर्षों के आयु वर्ग में लिंगानुपात 950 करने का लक्ष्य।
- योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य।
- सभी गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना तथा विद्युतीकरण करना।
- राजकोषीय घाटे को GDP के 3% के स्तर तक सीमित करना।
- इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के लिये रखी गई है।
- पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78)
- इस योजना का उद्देश्य ‘गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता’ की प्राप्ति थी। इसमें आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता दी गई।
- योजना में वर्ष 1975 में बीस सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया।
- इसमें ‘गरीबी निवारण’ कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इसी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974), काम के बदले अनाज़ तथा अंत्योदय योजना (1977-78) प्रारंभ हुई।
- इसमें पहली बार गरीबी तथा बेरोज़गारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- जनता पार्टी सरकार ने इसे एक वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त घोषित कर दिया।
- अनवरत योजना (1978-80)
- यह द्वितीय योजना अवकाश था।
- इस योजना (छठी योजना का प्रथम चरण) को जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) प्रारंभ की गई।
- अनवरत योजना की संकल्पना गुन्नार-मिर्डाल द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी।
- छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)
- योजना का उद्देश्य ‘गरीबी उन्मूलन और रोज़गार में वृद्धि’ था।
- ग्रामीण बेरोज़गारी उन्मूलन तथा गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। जैसे- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आदि।
- सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)
- योजना का उद्देश्य ‘उत्पादकता को बढ़ाना और रोज़गार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिये सुदृढ़ आधार’ तैयार करना था।
- ‘भोजन, काम और उत्पादन’ का नारा दिया गया।
- पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई।
- योजना अपने लक्ष्य से अधिक विकास दर हासिल करने में सफल रही।
- इस योजना में ‘मानव संसाधन विकास’ पर अधिक बल दिया गया था।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)
- हैरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित
- कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, योजना सफल रही तथा इसने लक्ष्य से ज़्यादा विकास दर हासिल की।
- इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजनाएँ, जैसे- भाखड़ा नांगल, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)
- यह पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी जिसका उद्देश्य ‘समाजवादी समाज’ की स्थापना करना था।
- इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई।
- इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई।
- तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)
- देश की ‘अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाने का लक्ष्य’ के साथ शुरू की गई यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित मानी जा सकती है।
- पुनः कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया।
- यह योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। जिसके प्रमुख कारण थे : भारत-चीन युद्ध 1962, भारत-पाक युद्ध 1965 तथा वर्ष 1965-66 का सूखा।
- योजना अवकाश (1966-69)
- यह प्रथम योजना अवकाश था।
- इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएँ क्रियान्वित की गईं।
- कृषि एवं उद्योगों को इस दौरान समान प्राथमिकता दी गई।
- योजना अवकाश के कारण भारत-पाक युद्ध, सूखा, मूल्य-वृद्धि तथा संसाधनों की कमी थे।
- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)
- इसका उद्देश्य ‘स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता’ की प्राप्ति थी।
- योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस. मान्ने द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी।
- इस योजना में कृषि तथा सिंचाई प्राथमिकता के क्षेत्र थे।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना की विशेषता थी।
- इसमें ‘समाजवादी समाज’ की स्थापना पर विशेष बल दिया गया तथा क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिये ‘विकास केंद्र उपागम’ की शुरुआत की गई।
- इसमें 14 बैकों का राष्ट्रीयकरण किया गया (1969), एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act-1969) तथा बफर स्टॉक की अवधारणा लागू की गई।
- रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसेनिक जहाज़ ‘एच.एम.आई.एस. तलवार’ के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी।
- सैनिकों की यह मांग भी थी कि नाविक बी.सी. दत्त को (जिसे जहाज़ की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।) रिहा किया जाए।
- नौसेना के इस विद्रोह को बंबई, कराची के नाविकों का पूरा सहयोग मिला।
- इस नौसेना विद्रोह में इंकलाब-ज़िंदाबाद, जय हिंद, हिंदू-मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, आदि नारे लगाए गए।
- इस विद्रोह के समर्थन में बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मज़दूरों ने हिस्सा लिया। उनके प्रदर्शनों में तीन झंडे एक साथ चलते थे- कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा।
- इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभभाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि, “हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं।”
- नौसेनिक विद्रोह भारत में अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक महत्त्वाकांक्षाओं की शव-पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ। वस्तुतः इस घटना से यह स्पष्ट हो गया था कि सैनिकों की स्वामीभक्ति, जो कि अंग्रेज़ी साम्राज्य की नींव थी, वह अब क्षीण हो चुकी थी। इसी कारण से इस घटना के 18 माह बाद भारत से ब्रिटिश राज का अंत हो गया।
- चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है तथा बाहर की ओर वायुदाब तेज़ी से क्रमशः बढ़ता जाता है, जिसके कारण वायु केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। वायु के प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में एंटी क्लॉक वाइज़ तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में क्लॉक वाइज़ होती है, जबकि प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है तथा बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है, जिसके कारण वायु केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत अर्थात् उत्तरी गोलार्द्ध में क्लॉक वाइज़ तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में एंटी क्लॉक वाइज़ होती है।
- चक्रवात में वायुदाब प्रवणता काफी तीव्र होती है, जिसके कारण पवनों का वेग प्रबल होता है। उष्ण चक्रवात में वायु की गति 120 किमी./घंटा से अधिक होती है। अतः ये विनाशकारी होते हैं, जबकि प्रतिचक्रवात में वायुदाब प्रवणता काफी मंद होती है। अतः पवन का वेग काफी मंद होता है।
- चक्रवात में धरातल के निकट वायु का अभिसरण तथा 10-12 किमी. ऊँचाई पर अपसरण होता है, जबकि प्रतिचक्रवात में ऊँचाई पर अभिसरण व धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है।
- चक्रवात में वायु ऊपर उठती है जिसके कारण वर्षा होती है, जबकि प्रतिचक्रवात में वायु का अवतलन होता है। अतः वर्षा का अभाव रहता है।
- चक्रवात का आधार अपेक्षाकृत छोटा होता है, जबकि प्रतिचक्रवात का आधार काफी बड़ा होता है।
- आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकार बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान उनका प्रसिद्ध नारा “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा” क्रांतिकारियों के लिये एक प्रेरणा स्रोत था।
- ब्रिटिश पत्रकार एवं नौकरशाह, वेलेंटाइन शिरोल ने जहाँ उन्हें ‘भारतीय अशांति का जनक’ कहा तो उनके अनुयायियों ने उन्हें ‘लोकमान्य’ की उपाधि दी।
- तिलक एक राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक प्रखर विद्वान थे। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने तिलक के बारे में कहा कि “संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है।”
- तिलक ने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत की तथा 1803 में ‘आर्कटिक होम इन द वेदास’ नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने 1877 में संस्कृत और गणित में पुणे के डेक्कन कॉलेज से स्नातक पूर्ण किया।
- तिलक ने 1884 में गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी और विष्णुशास्त्री चिपलूणकर एक साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। इस सोसाइटी ने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की।
- तिलक ने शैक्षणिक गतिविधियों के समानांतर लोगों में जागरूकता लाने के लिये दो समाचार पत्रों, मराठी में ‘केसरी’ और अंग्रेजी में ‘मराठा’ का संपादन किया।
- व्यक्तिगत रूप से बाल विवाह का विरोध करने के बावजूद तिलक ने 1891 ऐज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया, क्योंकि वह इसे विदेशी शासकों के हिंदू धर्म में हस्तक्षेप के रूप में देखते थे।
- तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1897 में 18 माह तथा 1908 में 6 वर्ष की सजा हुई। 1908 में तिलक को सजा काटने के लिये मांडले जेल (बर्मा) भेजा गया।
- 1 अगस्त, 1920 को मुंबई में तिलक की मृत्यु हो गई।
- गौरतलब है कि भारत इस समय जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है और देश में एक बड़ी आबादी कार्यकारी जनसंख्या की है। भारत के संदर्भ में गिग इकोनॉमी के विकास में एक बड़ी चिंता दक्ष कार्यशील आबादी की कमी है। गिग इकोनॉमी के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होना अनिवार्य होता है। कंपनियाँ अपने कार्य की आवश्यकतानुसार ही दक्ष लोगों को चुनती हैं। ऐसे में कार्य की प्रकृति एवं मांग को देखते हुए इतनी बड़ी कार्यशील जनसंख्या को प्रशिक्षित करना एक मुश्किल कार्य है।
- वर्तमान में देश में मौजूदा श्रम कानून स्पष्ट रूप से गिग इकोनॉमी को अपने दायरे में नहीं ला पाए हैं। जिसके कारण कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दे- यथा बोनस, बीमा, मातृत्व लाभ और यौन उत्पीड़न इत्यादि पर कानून की पकड़ नहीं होती है।
- गिग इकोनॉमी के अंतर्गत रोज़गार प्रदाता जॉब्स सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ नहीं देता है।
- गिग इकोनॉमी के अंतर्गत अस्थायी जॉब या कार्य के लिये कोई निश्चित वेतन अनुमानित नहीं होता है और देय वेतन या मेहनताने की राशि में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
- गिग इकोनॉमी के अंतर्गत कर्मचारियों को किसी प्रकार की जॉब्स सुरक्षा नहीं होती है, इसलिये कर्मचारियों को एक कार्य या प्रोजेक्ट के पूरा होने पर अगला कार्य या प्रोजेक्ट तलाशने का मानसिक तनाव झेलना पड़ता है।
- भारत में तेज़ी से बढ़ता डिजिटलीकरण गिग इकोनॉमी के विकास का मुख्य कारण है। गिग इकोनॉमी के चलन में देश में डिजिटली संचार में तेज़ी से हो रहे विकास की प्रमुख भूमिका है, जिसने जॉब्स के साथ-साथ काम को काफी फ्लेक्सिबल बना दिया है, इससे बिना किसी भौगोलिक बाधा के कहीं से भी कार्य किया जा सकता है।
- गिग इकोनॉमी को अपनाने से कंपनियों की ऑपरेशनल लागत कम हो जाती है, क्योंकि कंपनियाँ कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा देने के लिये बाध्य नहीं होती हैं। इसमें कंपनियाँ अपने कार्य की आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को हायर करती हैं।
- गिग इकोनॉमी के अंतर्गत श्रमिकों एवं पेशेवरों को जरूरी फ्लेक्सेबिलिटी उपलब्ध होती है। इससे पेशेवर एवं श्रमिक बार-बार नौकरी को बदल सकते हैं एवं अपनी पसंद का कार्य चुन सकते हैं। वर्तमान में गिग इकोनॉमी की जॉब्स को लोक तनावपूर्ण और स्थायी जॉब्स से बदलने के एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
- औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या में हो रही कमी ने भी गिग इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा दिया है। हाल ही में औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या में भारी कमी दर्ज की जा रही है तो दूसरी तरफ तेज़ी से बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में देश में नौकरियों की कमी ने भी ऐसी पार्टटाइम या फ्रीलांस नौकरियों की ज़रूरत या प्रचलन को बढ़ावा दिया है।
गिग इकोनॉमी रोज़गार प्रदात्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिये ही लाभदायक हो सकती है-
- इसके अंतर्गत कंपनियाँ कम लागत पर विशेषज्ञ पेशेवरों एवं कर्मचारियों को हायर कर उनसे अपना कार्य करा रही हैं।
- इसके अंतर्गत कंपनियों पर कर्मचारियों को पेंशन, इंसेंटिव या अन्य सुविधाएँ देने की बाध्यता नहीं है, जिसके कारण कंपनियों की ऑपरेशनल लागत भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है।
- गिग इकोनॉमी के अंतर्गत कंपनियाँ ज़्यादा-से-ज़्यादा नौकरियाँ उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित होती हैं, जिससे कार्यकारी जनसंख्या को अर्थव्यवस्था में योगदान देने का मौका प्राप्त होता है और उनके लिये रोज़गार की उपलब्धता बढ़ जाती है।
- गिग इकोनॉमी के अंतर्गत दक्ष पेशेवरों को उनकी पसंद का कार्य मिल जाता है और कर्मचारियों को अन्य कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है, वे कार्य के साथ-साथ या कार्य पूर्ण होने पर अन्य कार्य भी कर सकते हैं।
- भारत जैसे देश में जहाँ महिलाओं को कार्य करने में बहुत सी सामाजिक बंदिशों एवं ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, वहाँ गिग इकोनॉमी महिलाओं को कार्य करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। इससे महिलाओं को पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करने का विकल्प मिल जाता है।
- राष्ट्रीय श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग के सांकेतिक अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में, 77 लाख (7.7 मिलियन) श्रमिक गिग इकॉनमी में कार्यरत थे। वे गैर-कृषि कार्यबल का 2.6% या भारत में कुल कार्यबल का 1.5% थे। वर्तमान में डिजिटलाइजेशन बढ़ने के कारण रोज़गार और कार्य का स्वरूप धीरे-धीरे बदलता जा रहा है। गिग इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है। यह इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल है, जिसमें स्थायी कर्मचारियों के बजाय फ्रीलांसर्स, गैर-स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, इसके अंतर्गत अनुबंध आधारित स्थायी नौकरियाँ भी शामिल होती हैं, जिसमें कर्मचारियों की आय, उनके द्वारा किये गए कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। गिग इकोनॉमी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनियाँ अपनी ज़रूरतों के अनुसार काबिल एवं कुशल कर्मचारियों को लघु अवधि या किसी विशेष प्रोजेक्ट्स के लिये हायर करती है और उनके काम के लिये पूर्वनिर्धारित वेतन/मेहनताना देती है। हालाँकि काम खत्म होने के बाद कंपनी और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं रहता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष काम/क्षेत्र की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिये हायर किया जाता है।
- 2029-30 तक गिग कार्यबल के 2.35 करोड़ (23.5 मिलियन) तक बढ़ने की उम्मीद है। 2029-30 तक गिग वर्क के गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% या भारत में कुल आजीविका का 4.1% होने की उम्मीद है।
- गिग इकोनॉमी एक ऐसी मुक्त व्यवस्था है, जहाँ पूर्णकालिक रोज़गार की जगह अस्थायी रोज़गार का प्रचलन/विकल्प होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रोज़गाररत् व्यक्ति/श्रमिक एक बार काम/प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार दूसरे काम या प्रोजेक्ट को करने के लिये स्वतंत्र होते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत लोग अपनी सहूलियत के अनुसार काम कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी वर्कर्स को फ्लेक्सेबिलिटी, पसंदीदा काम व वर्क लाइफ बैलेंस और अच्छी कमाई जैसी कई सहूलियतें देती हैं। गिग इकोनॉमी में किसी व्यक्ति की सफलता उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर करती है। विषय एवं कार्य का अच्छा अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान व प्रचलित कौशल प्राप्त व्यक्ति की इस व्यवस्था में अच्छा कार्य एवं प्रदर्शन कर सकता है। भारत के संदर्भ में गिग इकोनॉमी अनौपचारिक श्रम क्षेत्र का ही विस्तार है। इसके अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को कोई सामाजिक सुरक्षा, बीमा इत्यादि की सुविधा नहीं मिलती है।
- उपयोग के आधार पर
- जड़ : गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम आदि।
- तना : आलू, अरबी, जिमीकंद, गांठगोभी, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन आदि।
- फल : खीरा, कद्दू, लौकी, मिर्च, भिंडी, बैंगन, टमाटर, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, फ्रेंच बीन आदि।
- बीज : सेम, मटर, लोबिया आदि।
- अपरिपक्व पुष्प : फूलगोभी, ब्रोकली आदि।
- कुल के आधार पर
- क्रूसीफेरी : फूलगोभी, गांठगोभी, मूली, शलजम, सरसों, ब्रोकली, पत्तागोभी, कैनोला
- कुकुरबिटेसी : लौकी, टिंडा, सीताफल, करेला, खीरा, धनिया, तोरई, तरबूज (इन्हें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, इनमें कड़वेपन का कारण ग्लूकोसाइड कुकुरबिटोसिन है।)
- एमेरिलीडेसी : लहसुन, प्याज
- लेग्यूमिनोसी : मटर, सेम, मेथी, राजमा, सोयाबीन
- अंबैलीफैरी : गाजर, धनिया
- मालवेसी : भिंडी
- सोलेनेसी : आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च
- पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ पकड़ने वाली तकनीक है, जिसमें आदमी के बातचीत के कई ग्राफ एक साथ बनते हैं और इसके हर संभावित झूठ को पकड़ने की कोशिश की जाती है।
- असल में जिस इंसान का टेस्ट होना है उसकी धड़कन, साँस और रक्तचाप के उतार-चढ़ाव को ग्राफ के रूप में दर्ज किया जाता है।
- शुरू में नाम, उम्र और पता पूछा जाता है और उसके बाद अचानक से उस विशेष दिन की घटना के बारे में पूछ लिया जाता है। इस अचानक सवाल से उस इंसान पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और ग्राफ में बदलाव दिखता है। अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। टेस्ट के दौरान संबंधित व्यक्ति से कुछेक सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 4 से 5 उस घटना से संबंधित होते हैं, जिन-जिन सवालों पर ग्राफ में बदलाव आता है, उनका विशेषज्ञ विश्लेषण करते हैं।
- सामान्यतः झूठ बोलते समय श्वसन की गति और लय बदल जाती है। इस दौरान ब्लड प्रेशर, पल्स, साँस की गति और शरीर से निकल रहे पसीने का आधार पर यह जानने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं।
- इस तरह के वैज्ञानिक तकनीक वाले टेस्ट में यह ज़रूरी नहीं कि आरोपी सच ही बोले, इसमें झूठ बोलने की भी पूरी आशंका होती है। यही कारण है कि कोर्ट इन्हें साक्ष्य के रूप में नहीं मानता। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस को इस टेस्ट से कोई मदद नहीं मिली।
- इस व्यवस्था में केंद्र को ही महत्त्व मिलता है, प्रांतों को नहीं।
- आमतौर पर छोटे देशों में, जहाँ केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है, एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है।
- ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता, न ही उनके पास निश्चित शक्तियाँ होती हैं; उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं।
- इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, उनके नाम बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसलिये, एकात्मक व्यवस्था (Unitary System) को ‘विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ’ (Indestructible Union of Destructible States) कहा जाता है।
- ब्रिटेन इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
- फ्राँस की राजनीतिक प्रणाली भी एकात्मक ढाँचे पर आधारित है।
एकात्मक प्रणाली की विशेषताएँ
- एकात्मक प्रणाली (Unitary System) के अंतर्गत पूरे देश के लिये एक ही सरकार काम करती है; कार्यपालिका या विधायिका के स्तर पर केंद्र और राज्यों में समानांतर ढाँचा नहीं पाया जाता।
- ऐसे देशों में छोटी प्रशासनिक इकाइयों को केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही काम करना होता है।
- केंद्र सरकार अपनी इच्छा से स्थानीय स्तर पर थोड़ा-बहुत राजनीतिक विकेंद्रीकरण (Political Decentralisation) कर सकती है, किंतु वह विकेंद्रीकरण भी स्थानीय इकाइयों का संवैधानिक अधिकार न होकर केंद्र सरकार की प्रशासनिक कार्य-योजना (Administrative Workplan) का परिणाम होता है।
- इंग्लैंड की शासन प्रणाली इसी ढाँचे पर आधारित है।
- इस प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर न तो संविधान का उतना महत्त्व होता है और न ही न्यायपालिका को वैसी सर्वोच्चता हासिल होती है, जैसी कि संघात्मक ढाँचे में।
लाभ-
- यदि समाज में जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वैविध्य हो तो उस वैविध्य के अनुसार राजनीतिक प्रणाली का गठन करना आसान हो जाता है।
- इनमें राष्ट्रीय एकता (National Unity) और स्थानीय स्वायत्तता (Local Autonomy) दोनों व्यवस्थाओं के लाभ एक साथ उपलब्ध होते हैं।
- केंद्रीय सरकार को बहुत सारे छोटे दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है और वह अपना पूरा ध्यान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर केंद्रित कर पाती है।
- यदि कभी कोई राजनीतिक प्रयोग करना हो तो पहले उसे कुछ प्रांतों के स्तर पर करके व उसके परिणामों की समीक्षा करके धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया में प्रयोगों की विफलता का खतरा काफी कम रह जाता है।
हानियाँ-
- इसमें दोहरे शासन तंत्र की वजह से न सिर्फ ज़्यादा खर्च आता है बल्कि प्रशासन का ढाँचा भी अत्यंत जटिल हो जाता है।
- केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जो देश की शासन प्रणाली के लिये नुकसानदेह सिद्ध होते हैं।
- जब किसी राज्य में किसी ऐसे दल की सरकार बनती है, जो केंद्र सरकार बनाने वाले दल का विरोधी होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है।
- कई बार राज्य सरकारें जानबूझकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी जनता को भड़काती हैं जिससे क्षेत्रवादी प्रवृत्तियाँ (Regional Tendencies) उभरती हैं तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता (National Unity and Integrity) खतरे में पड़ जाती है।
- कई बार केंद्र सरकार उन राज्यों के विकास पर ज़्यादा बल देने के लिये बाध्य हो जाती है, जहाँ उसके अपने दल या किसी सहयोगी दल की सरकार होती है, जबकि विरोधी दलों की सरकारों द्वारा शासित राज्य केंद्र के असहयोगी रवैये के कारण प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ जाते हैं। इसलिये संघात्मक शासन प्रणाली पर अक्सर असंतुलित विकास (Imbalanced Development) का आरोप लगाया जाता है।
- संघात्मक व्यवस्था कई स्वतंत्र राज्यों (Independent States) के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह अधिकार नहीं होता कि वे संघ से अलग हो सकें। इसलिये, संघात्मक व्यवस्था को ‘अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ’ (Indestructible Union of Indestructible States) कहा जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद (Federalism) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- ऐसे अन्य उदाहरणों में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड को रखा जा सकता है। ध्यातव्य है कि स्विट्ज़रलैंड का नाम तो ‘स्विस परिसंघ’ (Swiss Confederation) है, किंतु वास्तविक रूप में यह एक संघ (Federation) ही है, क्योंकि किसी भी कैंटन (Canton) को संघ (Federation) से अलग होने का अधिकार नहीं है।
संघात्मक प्रणाली की विशेषताएँ
- इसमें राज्यों या प्रांतों का अत्यधिक महत्त्व होता है, क्योंकि केंद्रीय शासन राज्यों की सहमति और समझौते के परिणामस्वरूप ही अस्तित्व में आता है।
- राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों एवं दायित्वों का वितरण स्पष्ट रूप में होता है, क्योंकि इसी के आधार पर राज्यों और केंद्र के मध्य समझौता होता है।
- संविधान की सर्वोच्चता परिसंघात्मक व संघात्मक प्रणालियों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि संघ की स्थापना संविधान रूपी लिखित दस्तावेज़ के आधार पर ही होती है। यदि इसे सर्वोच्चता हासिल न हो, तो संघ व इकाइयों के बीच का समझौता विश्वसनीय नहीं रह जाता।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Freedom of Judiciary) और संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता (Judicial Supremacy) का सिद्धांत इन प्रणालियों में अनिवार्यत: स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो संविधान केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण करता है, उसकी समुचित व्याख्या को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और उन विवादों के निपटारे के लिये न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मानना ज़रूरी हो जाता है।
- सर सैय्यद अहमद खां का जन्म दिल्ली के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में प्रवेश किया था।
- योग्यतम शिक्षकों द्वारा उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में सर सैय्यद अहमद खां ने भारतीय मुसलमानों के पुनरुद्धार एवं भलाई के लिये पहले अपने धर्म और समाज का अध्ययन किया, फिर इस्लाम के प्रति सुधारवादी रवैया अपनाया।
- वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से पूर्णरूपेण प्रभावित थे, जिस कारण वे जीवनपर्यंत इस्लाम में उदारवादी विचारधारा एवं आधुनिकता का समन्वय कराने में प्रयत्नशील रहे।
- उन्होंने धार्मिक कट्टरता, मानसिक संकीर्णता और अलगाववाद का भी विरोध किया और मुसलमानों को सहनशील व उदार होने को कहा।
- सर सैय्यद अहमद खां ने 1864 में ‘साइंटिफिक सोसाइटी’ की स्थापना की। इन्होंने मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिये 1870 में पत्रिका ‘तहज़ीब-उल-अख़लाक’ का प्रकाशन प्रारंभ किया।
- सर सैय्यद अहमद खां ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांफ्रेंस का गठन किया। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की।
सहकारी बैंक
- भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किये जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। ये बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तर पर किया गया है। राजकीय सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था है। इसके बाद केंद्रीय या ज़िला सहकारी बैंक ज़िला स्तर पर कार्य करते हैं एवं तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि के लिये ऋण उपलब्ध कराते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में स्वरोज़गार, लघु उद्योग तथा व्यक्तिगत वित्त के लिये साख उपलब्ध कराते हैं। राज्य सहकारी बैंक, कृषि सहकारी समितियाँ, शहरी सहकारी बैंक और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक आदि सहकारी बैंकों के प्रमुख उदाहरण हैं।
- आधुनिक आवर्त सारिणी में समूह-17 में रखे गए 5 तत्त्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन समूह के तत्त्व हैं- फ्लोरीन (F), क्लोरीन (Cl), ब्रोमीन (Br), आयोडीन (I), एस्टेटीन (At)
- हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है।
- फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्त्व है।
- क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) से क्रिया करके कार्बोनिल डाइक्लोराइड या फ़ॉस्जीन (COCl2) बनाती है।
- क्लोरीन का उपयोग विभिन्न तत्त्वों के क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफ़ॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड (CCl4) इत्यादि बनाने में किया जाता है।
- आयोडीन का पोटैशियम आयोडाइड एवं इथेनॉल में बना विलयन आयोडीन टिंक्चर कहलाता है। इसका प्रायोगिक एंटीसेप्टिक (रोगाणुरोधक) की तरह किया जाता है।
- रेडियोएक्टिव आयोडीन I-131 का प्रयोग थायरॉइड, कैंसर एवं ब्रेन-ट्यूमर का पता लगाने में होता है।
- सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिये किया जाता है।
- एस्टेटीन एक रेडियोएक्टिव, अत्यंत अस्थायी एवं पृथ्वी के भू-पर्पटी में पाया जाने वाला दुर्लभ तत्त्व है।
- परिसंघ (Confederation) का अर्थ होता है- वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र (Centre) का न तो महत्त्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। विभिन्न स्वतंत्र राज्य (States) या प्रांत (Provinces) मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों, जैसे- विदेश नीति (Foreign Policy), बाह्य सुरक्षा (External Security) तथा संचार (Communication) आदि का प्रशासन वे लोग मिलकर करेंगे और इसके लिये केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। इन प्रांतों या निर्माणक इकाइयों (Constituent Units) को यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि यदि वे चाहें तो परिसंघ (Confederation) से पुन: अलग हो सकते हैं।
- स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था में परिसंघ या केंद्रीय ढाँचा तो विनाशी (Destructible) होता है, किंतु जो प्रांत या राज्य मिलकर इसे बनाते हैं, वे अविनाशी (Indestructible) होते हैं। इसलिये इसे ‘अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन’ (Destructible Union of Indestructible States) भी कह दिया जाता है।
- भूतपूर्व सोवियत संघ सिद्धांतत: एक परिसंघ (Confederation) ही था, जो कई स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था। हालाँकि साम्यवादी शासन के दौरान व्यावहारिक तौर पर राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं थी।
- सोवियत संघ के टूटने के बाद उन सभी राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाना भी उसके परिसंघ होने का ही प्रमाण है।
- अब वे सभी स्वतंत्र राज्य ‘स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल’ (CIS-Commonwealth of Independent States) के रूप में जुड़े हैं। पर यह संगठन यूरोपियन यूनियन (European Union) की तरह एक ढीला-ढाला-सा संगठन है जिसे औपचारिक (Formal) दृष्टि से परिसंघ (Confederation) भी नहीं कहा जा सकता।
- इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का जब गठन हुआ था तो वह भी परिसंघ (Confederation) के रूप में ही विकसित हुआ था, किंतु आगे चलकर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्रांतिकारी निर्णयों से राज्यों का अलग होने का अधिकार खत्म हो गया। इसलिये अब अमेरिका परिसंघ (Confederation) न होकर संघ (Federation) बन गया है।
कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक, सीवेज का गंदा पानी, औद्योगिक कचरा इत्यादि किसी जलीय पारितंत्र में पहुंचकर पोषकों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। यह प्रक्रिया सुपोषण कहलाती है।
- जलीय पारितंत्र में पोषकों की मात्रा में अचानक हुई वृद्धि शैवालों की संख्या को अनियंत्रित रूप से बढ़ा देती है, जिससे जल सतह पर शैवालों की एक परत बन जाती है। इसे ही Algal Bloom कहते हैं। ये स्वच्छ जल (Fresh Water) और समुद्री जल (Marine Water) दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। ये जल का रंग परिवर्तित कर देते हैं (सामान्यतः नीला-हरा, पीला-भूरा या लाल)।
- ये सूक्ष्म शैवाल, यथा- डिनोफ्लैजिलेट्स एवं डायटम्स होते हैं। इसके अलावा सायनो बैक्टीरिया (नील-हरित शैवाल) भी एल्गल ब्लूम हेतु ज़िम्मेदार होते हैं।
- कुछ एल्गल ब्लूम टॉक्सिक होते हैं एवं कुछ नॉन-टॉक्सिक।
- हानिकारक एल्गल ब्लूम लोगों के स्वास्थ्य, समुद्री पारितंत्र, वन्य जीवन, पक्षियों, समुद्री स्तनधारियों, मछलियों एवं स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को ‘श्यानबल’ कहते हैं। तरलों के इस गुण को, जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है, ‘श्यानता’ कहते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता ‘शून्य’ होती है।
- श्यानता तरलों (द्रवों एवं गैसों) का गुण है। यह अणुओं के मध्य लगने वाले संजक बलों के कारण होती है। गैसों में द्रवों की तुलना में श्यानता बहुत कम होती है।
- ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है, परंतु गैसों की श्यानता बढ़ती है।
- किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक (Coefficient of Viscosity) द्वारा मापा जाता है।
- इसका मात्रक डेकाप्वांइज या प्वाइजली (PI) या पास्कल सेकेंड है।
- इसे प्रायः η (इटा) द्वारा दर्शाते हैं।
- कभी-कभी नवजात शिशुओं में सायनोटिक हृदय रोग (हृदय की संरचनात्मक गड़बड़ी, जैसे- फोरामेन ओवल का जन्मोपरांत भी बंद न होना आदि) के कारण उनके रक्त का पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण (ऑक्सीजन से युक्त होना) नहीं हो पाता, जिससे उनकी त्वचा, नाखून, होंठ आदि का रंग असामान्य रूप से नीला पड़ जाता है। इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम एवं ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहते हैं।
- अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण रंग का नीला पड़ जाना ‘सायनोसिस’ भी कहलाता है। कभी-कभी फेफड़े द्वारा रक्त को शुद्ध न कर पाना भी इसका एक कारण होता है।
- सायनोसिस का एक अन्य कारण मिथेमोग्लोबिनेमिया भी है। इसमें प्रदूषित भूमिगत जल से नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में पहंच जाता है जिससे उनके रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है एवं शरीर का रंग नीला पड़ जाता है।
- वस्तु व्यापार में वास्तविक भौतिक वस्तुओं, यथा-अनाज, चांदी, सोना, कच्चा तेल, धातुओं इत्यादि का व्यापार होता है।
- कमोडिटी बाज़ार एक ऐसा एक्सचेंज होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, कृषि उत्पादों तथा डेरिवेटिव्स उत्पादों का कारोबार किया जाता है।
- ये समझौते स्पॉट मूल्य, फ़ॉरवर्ड, फ्यूचर्स आदि हो सकते हैं।
- वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु वायदा कारोबार की भूमिका बढ़ रही है।
- कमोडिटी एक्सचेंज का प्रमुख उद्देश्य वस्तु में वायदा कारोबार की सुविधा प्रदान कर कीमतों में विपरीत संचलन से भागीदारों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- कमोडिटी एक्सचेंज सामान्यतः जिंसो (वस्तुओं) में वायदा समझौता करते हैं। उदाहरण के लिये, एक गेहूँ उत्पादक किसान अपने खेतों में खड़े गेहूँ को जो आगे कुछ महीनों में तैयार होगा, किसी आटा मिल को किसी भावी मूल्य पर बेचने का वायदा कर सकता है। ऐसे में गेहूँ की आपूर्ति तथा भुगतान भविष्य में किसी पूर्व निर्धारित तिथि पर होगा। इस प्रकार का वायदा समझौता विक्रेता किसान को अपनी फसल के संबंध में एक मूल्य सुनिश्चित करता है तथा साथ ही आटा मिल को भी गेहूँ की आपूर्ति को निश्चित मूल्य पर प्राप्त करना सुनिश्चित करता है।
- इस प्रकार वायदा बाज़ार का यह समझौता जहाँ उत्पादक किसान को मूल्य में गिरावट से संरक्षित करता है, वहीं आटा मिल को मूल्य की वृद्धि से संरक्षण प्रदान करता है।
कर्ज़ को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज़ को न लौटाने वाले ऋणी को इरादतन चूककर्त्ता कहते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार उन्हें इरादतन चूककर्त्ता कहते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं-
- कर्ज़ चुकौती के दायित्व को पूर्ण करने की क्षमता होने का बावजूद कर्ज़ का भुगतान नहीं कर रहा है।
- ऋण प्राप्तकर्त्ता ने जिस कार्य के लिये ऋण लिया है उस कार्य के लिये ऋण का इस्तेमाल न करके किसी दूसरे प्रयोजन में ऋण का प्रयोग किया हो।
- ऋण प्राप्तकर्त्ता ने उस संपत्ति का विक्रय कर दिया हो जिसके एवज़ में ऋण प्राप्त किया था।
- ऋण से प्राप्त धनराशि को किसी अन्य जगह ट्रांसफर कर दिया हो और अन्य आस्तियों के रूप में उक्त राशि उसके पास उपलब्ध न हो।
- ऋण प्राप्तकर्त्ता के भुगतान के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर तथा 25 लाख रुपये से अधिक ऋण का भुगतान न करने वाले चूककर्त्ताओं को ही इरादतन चूककर्त्ता की श्रेणी में रखा जाता है।
जानबूझकर कर्ज़ न चुकाने वालों पर शिकंजा कसने के लिये भारत सरकार ने ‘वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिमियम, 2002’ (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) पारित किया है जिसके तहत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में कार्यवाही करने के अधिकार दिये गए हैं। यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में बैंक गिरवी रखी प्रतिभूतियों को ज़ब्त कर ले और उन्हें संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को बेच दे या फिर उस संपत्ति को अपने प्रबंधन में ले ले।
- जब वायुमंडलीय आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु, जैसे- पत्थर, घास तथा पत्तियों आदि पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तो उसे ‘ओस’ कहते हैं।
- ओस का निर्माण तभी होता है, जब निम्नलिखित परिस्थितियां या अवस्थाएँ एक साथ मौजूद हों- आकाश साफ हो, हवा शांत हो, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो, ठंडी एवं लंबी रातें हों, ओसांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर हो।
- ओसांक बिंदु- जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है अर्थात् जिस तापमान पर एक निश्चित समय पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता तथा उसमें स्थित निरपेक्ष आर्द्रता बराबर हो जाए, उसे ‘ओसांक बिंदु’ कहते हैं।
- हिमांक बिंदु- वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिये, शुद्ध जल का हिमांक 0०C या 32०F होता है।
- जलवाष्प युक्त वायु जब ठंडे धरातल के संपर्क में आती है तो वायु का शीतलन होता है, जिससे वायु में उपस्थित जलकणों के कारण वायुमंडल की दृश्यता प्रभावित होती है, इसे ही ‘कोहरा’ कहते हैं।
- यह एक तरह का बादल होता है, जो धरातल के एकदम निकट होता है।
- सामान्यतः कोहरे की सघनता सूर्योदय के पश्चात् अधिक होती है और यह दोपहर तक या दोपहर पहले ही बिखर जाता है किंतु शीत ऋतु में यह कई दिनों तक उपस्थित रह सकता है। सामान्यतः इसकी दृश्यता लगभग 300 मीटर मानी जाती है।
- कोहरे को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है-
- कुहासा (Mist)- कुहासा वह वायुमंडलीय अवस्था है, जिसमें जल की सूक्ष्म बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। इसमें दृश्यता सीमा कोहरे की तुलना में अधिक होती है। इसमें दृश्यता लगभग 1-2 किमी. तक होती है।
- धुआंसा (Smog)- इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के बाद या औद्योगिक कारखानों वाले क्षेत्र में होता है, जहाँ अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है। धुआंसा कोहरे से पहले निर्मित होता है तथा उससे ज्यादा घना और लंबी अवधि का होता है। कोहरे तथा धुएं के मिश्रण को ‘स्मॉग’ कहते हैं। इसका लाखों लोगों की श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- संघनन जलवाष्प के छोटे-छोटे जल कणों या हिम कणों में बदलने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, जल के गैसीय रूप का पुनः जल में रूपांतरण होना ही ‘संघनन’ कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है।
- वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों के आस-पास की वायु के संतृप्त होने से संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। इन सूक्ष्म कणों को ‘आर्द्रताग्राही नाभिक’ कहते हैं क्योंकि इनमें आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता होती है।
- धूल के कण, धुएं की कालिख तथा समुद्री नमक के कण आदि अच्छे ‘आर्द्रताग्राही नाभिक’ के उदाहरण हैं, क्योंकि ये जल का अवशोषण करते हैं।
- वर्षण की उत्पत्ति के लिये संघनन एक आवश्यक प्रक्रिया है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प का ओस, तुषार, कोहरा और धुंध में परिवर्तन हो जाता है।
- अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य-प्रांत (वर्तमान मध्य प्रदेश) के महू में एक मराठी परिवार में हुआ था।
- अंबेडकर जाति व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिये अनेक प्रयास किये।
- 1926 में अंबेडकर बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किये गए।
- दलितों के उत्थान के उद्देश्य से अंबेडकर ने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता तथा प्रबुद्ध भारत आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया।
- अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर ने तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों में हिस्सा लिया।
- अंबेडकर वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। वे धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते थे।
- अंबेडकर ने अपनी पुस्तक ‘हू वर द शूद्राज़?’ में शूद्रों की उत्पत्ति के विषय में बताया, ‘‘शूद्र वह क्षत्रिय थे, जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था।’’
- महाराष्ट्र में प्रचलित ‘महार वतन प्रणाली’ तथा ‘खोट व्यवस्था’ का अंबेडकर ने विरोध किया।
- अंबेडकर ने गाँवों को ‘उदासीनता का अड्डा’ कहा।
- दलितों के उद्धार के लिये अंबेडकर ने उन्हें ‘बौद्ध-धर्म’ अपनाने को कहा। वर्ष 1956 में अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म अपना लिया था।
- दलित वर्गों के उत्थान के लिये अंबेडकर ने ‘इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी’ (1936) तथा ‘शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन’ (1942) जैसे संगठनों की स्थापना भी की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ही 1957 में अंबेडकर ने ‘रिपब्लिकन दल’ का नाम दिया।
- अंबेडकर ने संसदीय शासन पद्धति तथा कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया।
- दलितों के उत्थान की दृष्टि से अंबेडकर ने 1924 में ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ की स्थापना की। उन्होनें 1942 में ‘अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ’ की स्थापना की।
- अंबेडकर ने भारी उद्योगों, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा सहकारी कृषि का समर्थन किया।
- अंबेडकर गांधीवाद के कुछ पक्षों के आलोचक रहे हैं। उन्होंने ‘ट्रस्टीशिप’ के सिद्धांत को हास्यास्पद बताया।
- अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर ‘भारतीय संविधान के निर्माता’ हैं।
- अंबेडकर भारत के प्रथम ‘विधि मंत्री’ थे।
- 1951 में अंबेडकर ने ‘हिंदू कोड बिल’ पेश किया, जिसके पारित न होने पर उन्होंने नेहरू-मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।
- 1952 में अंबेडकर राज्यसभा के लिये मनोनीत हुए।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का गठन 1962 में हुआ था। यह भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सार्वजनिक और निजी विद्यालयों के लिये भारत में शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है।
- यह एक स्वायत्त निकाय है जो शिक्षा मंत्रालय के संरक्षण में कार्यरत है।
- सीबीएसई प्रत्येक वर्ष दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएँ आयोजित करता है। यह संबद्धता, शिक्षाविदों तथा परीक्षा संबंधी गतिविधियों से संबंधित है।
- बोर्ड का मूल उद्देश्य अपने संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिसमें विद्यार्थी-केंद्रित प्रतिमानों, शिक्षण परीक्षाओं में सुधार और मूल्यांकन प्रथाओं, कौशल सीखने आदि में सीबीएसई द्वारा शिक्षार्थी के समग्र विकास पर ज़ोर देने के साथ सतत् व्यापक मूल्यांकन पर अपना प्रमुख ध्यान केंद्रित रखा गया है।
- वर्तमान में, सीबीएसई से संबद्ध भारत में 29000 से अधिक विद्यालय और विदेशों में 240 विद्यालय हैं।
- सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रभावी ढंग से कार्यों को निष्पादित करने के लिये इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है, जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- NCERT और इसकी घटक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य है-
- स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना;
- पाठ्यपुस्तक, संवादपत्र और अन्य शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण करना और उन्हें प्रकाशित करना;
- शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी कई घटक इकाइयाँ देश के अन्य हिस्सों में स्थापित हैं।
- NCERT, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिये भी एक कार्यान्वयन एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय एवं वार्त्ता करता है और अन्य विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करता है।
- इस परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
- विद्यालय शिक्षा से सर्वेक्षण, शोध प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित कर संगठित करना।
- शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करना।
- उन्नतशील शैक्षिक विधियों और नवाचारों का प्रचार करना।
- केंद्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना।
- विद्यालय शिक्षा के संबंध में हर तरह की सूचनाएँ स्थापित करना।
- संपूर्ण देश में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाएँ स्थापित करना तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करने का प्रयास करना।
- अँधेरे में चमकने के कारण इसे ‘फॉस्फोरस’ नाम दिया गया है।
- सभी जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों में फॉस्फोरस पाया जाता है। जंतुओं की अस्थियों व दांतों में यह कैल्शियम फॉस्फेट व हाइड्रॉक्सीएपेटाइट के रूप में पाया जाता है।
- फॉस्फोरस को मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट या हड्डी के तत्त्व से दो विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है- 1. रियर्ड विधि, 2. विद्युत तापीय विधि।
- फॉस्फोरस के कई अपरूप पाए जाते हैं- सफेद फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, सिंदूरी फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस इत्यादि।
- सफेद फॉस्फोरस वायु में स्वतः जल उठता है।
- सेफ्टी माचिसों में लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है।
- समुद्री जहाज़ों पर संकेत इत्यादि के लिये होम्स सिग्नल बनाने में कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है।
- रोडेंटनाशी (Rodenticide) या चूहा विष में ज़िंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, जो फॉस्फोरस का यौगिक है। जंतुओं के शरीर का अम्ल ज़िंक फॉस्फाइड को फॉस्फीन में बदल देता है जो अत्यधिक जहरीली गैस है।
- स्मोक स्क्रीन (धूम्र पट) बनाने हेतु फास्फीन (PH3) का उपयोग किया जाता है।
यह एक विद्युत रासायनिक यंत्र है, जो हाइड्रोजन या अन्य ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर स्वच्छता एवं सक्षमतापूर्वक विद्युत का उत्पादन करता है।
अगर ईंधन सेल में हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो यह ‘हाइड्रोजन ईंधन सेल’ (Hydrogen Fuel Cell) कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर उप-उत्पाद के रूप में विद्युत, ताप एवं शुद्ध जल का उत्पादन करता है। सामान्यत: इसमें ऑक्सीजन को हवा से प्राप्त किया जाता है। इसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चूँकि यहाँ दहन (Combustion) की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। अत: कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता।
- एक सिंगल फ्यूल सेल (Single Fuel Cell) दिष्ट धारा (Direct Current) की छोटी मात्रा का उत्पादन करता है।
- हाइड्रोजन एवं फॉस्फोरिक एसिड बहुत ही सामान्य प्रकार के ईंधन सेल हैं।
- Alkaline Fuel Cell System का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है।
ईंधन सेल के अनुप्रयोग (Applications of Fuel Cell)
- हाथ में पकड़ने योग्य छोटे उपकरण, यथा- मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, कार से लेकर बस तक को विद्युत उपलब्ध कराने में।
- ऑफिस भवनों, अस्पतालों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक एवं संस्थागत सुविधाओं हेतु स्थिर विद्युत (Stationary Power) उपलब्ध कराने में।
- ये उन दूरस्थ स्थानों हेतु भी काफी उपयोगी है, जहाँ परंपरागत विद्युत आपूर्ति की पहुँच सीमित या संभव नहीं है।
- ईंधन सेल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोटर को विद्युत प्रदान करना अर्थात् शहर को प्रकाशित करने हेतु विद्युत-धारा का उत्पादन करना है। वर्तमान में ईंधन सेल को आकाश की उँचाइयों (अंतरिक्ष यान में) से लेकर समुद्र की गहराइयों तक (कुछ नवीनतम पनडुब्बियों में) प्रयोग में लाया जा सकता है।
लाभ (Advantages)
- इसके प्रचालन (Operation) में शोर नहीं होता। अत: इसे आवासीय क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है।
- यह प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करता।
- ये समय के साथ खराब नहीं होते एवं लीक नहीं होते।
सीमाएँ (Limitations)
- ईंधन सेल के सुचारु रूप से कार्य करने हेतु हाइड्रोजन के एक स्रोत का होना आवश्यक है।
- हाइड्रोजन को संगृहीत एवं वितरित करना मुश्किल है। अत: हाइड्रोजन गैस के स्टेशन उपलब्ध नहीं होते।
- यह अत्यधिक ख़र्चीला है।
- हम जानते हैं कि जब कोई धातु अपने आस-पास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है।
- संक्षारण के कारण कार के ढाँचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज़ तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है।
धातु संक्षारण की कुछ प्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं-
- सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी काली परत सिल्वर के ऊपर जमा हो जाती है।
- कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जिसकी हरी परत कॉपर पर जमा हो जाती है।
- लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं।
- वायु के संपर्क में आने पर एल्युमीनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमीनियम ऑक्साइड की यही परत एल्युमीनियम की और संक्षारण से सुरक्षा करती है। एल्युमीनियम की संक्षारण से सुरक्षा हेतु इस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं।
- एनोडीकरण- एनोडीकरण के लिये एल्युमीनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमीनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है।
संक्षारण से सुरक्षा- संक्षारण से धातुओं को सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं-
- धातु पर पेंट करके, तेल इत्यादि लगाकर
- यशदलेपन (Galvanisation)
- एनोडीकरण
- क्रोमियम लेपन
- मिश्रात्वन
घर्षण के उपयोग
- सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिये फिसलने लगते हैं।
- चिकनी सतह पर घर्षण कम होने के कारण चलने में परेशानी होती है। उदाहरण-
- बर्फ पर चलना कठिन होता है।
- कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती हैं।
- सड़क पर तेल आदि फैलने से साइकिल फिसल जाती है।
- घर्षण होने की वजह से विभिन्न वस्तुएँ अपनी सतह पर विरामावस्था में आसानी से बनी रहती हैं अन्यथा ज़रा-सा बल लगने पर वे गतिमान हो जातीं और दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता। उदाहरण-
- घर्षणहीन सतह पर रखी वस्तु वायु द्वारा गतिमान हो जाती है।
- घर्षणहीन सतह पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने पर विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है।
घर्षण से हानि
- घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है।
- मशीनों के कल पुर्जों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के ख़राब होने की संभावना रहती है।
2. गतिक घर्षण बल (Dynamic Frictional Force)
- गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को ‘गतिक घर्षण बल’ कहते हैं।
- गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है।
- यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने वाले बल का नाम F1 है एवं वस्तु को गतिशील बनाए रखने हेतु आवश्यक बल का मान F2 है तो,
F2 < F1
घर्षण बल के प्रकार
- सर्पी घर्षण बल (Sliding Frictional Force)- यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को ‘सर्पी घर्षण बल’ कहते हैं।
- लोटनिक घर्षण बल (Rolling Frictional Force)- जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाले बल को ‘लोटनिक घर्षण बल’ कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है।
घर्षण कोण (Angle of Friction)- सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहा जाता है।
विराम कोण (Angle of Repose)- आनत तल का क्षैतिज दिशा के साथ वह अधिकतम झुकाव कोण जिस पर वस्तु आनत तल पर ठीक संतुलन की अवस्था में बनी रहती है, विराम कोण कहलाता है।
घर्षण बल के गुण
- घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
- सतह चिकनी होने पर घर्षण कम होता है।
- सतह खुरदुरी होने पर घर्षण ज्यादा होता है।
- ठोस-ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण सर्वाधिक जबकि द्रव-ठोस सतह के मध्य उससे कम तथा वायु-ठोस के बीच घर्षण सबसे कम होता है।
- स्नेहक (Lubricants) के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है, क्योंकि द्रव-ठोस सतह के मध्य घर्षण कम होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है।
संतुलित बल (Balanced Force)
- यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हों और सभी बल परिमाण में एक-दूसरे के समान किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार लगे हों कि उनका परिणामी बल शून्य हो तो पिंड पर लगने वाले सभी बल ‘संतुलित बल’ कहलाते हैं।
- संतुलित बलों के कारण पिंड में कोई गति नहीं होती है।
असंतुलित बल (Unbalanced Force)
- यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल या कई बलों का परिणामी बल इस प्रकार कार्य करे कि पिंड बल की दिशा में गति करने लगे तो इस प्रकार के बलों को ‘असंतुलित बल’ कहा जाता है।
घर्षण बल (Friction)
- वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, ‘घर्षण बल’ कहलाता है।
- क्षैतिज तल पर रखी हुई वस्तु को यदि बल लगाकर गति दे दी जाए तो थोड़े समय के बाद वस्तु विरामावस्था में आ जाती है क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करते हुए तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु विरामावस्था में बल संतुलन को न प्राप्त कर ले।
- घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत होती है।
घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-
- स्थैतिक घर्षण बल
- गतिक घर्षण बल
1. स्थैतिक घर्षण बल (Static Frictional Force)
- किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल ‘स्थैतिक घर्षण बल’ कहलाता है।
- जब तक वस्तु गति की अवस्था में नहीं आती तब तक स्थैतिक घर्षण बल कार्यरत रहता है, जो बाह्य बल (F) के बराबर रहता है और उसे संतुलित करता है। जैसे-जैसे बाह्य बल बढ़ता है वैसे-वैसे स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता है।
सीमांत घर्षण बल (Limiting Frictional Force)
- किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिये जैसे-जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं, स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है परंतु एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ सकता। इस समय वस्तु गति करने ही वाली होती है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही ‘सीमांत घर्षण बल’ कहते हैं।
- उपर्युक्त व्याख्या से हम कह सकते हैं कि ‘सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ करने के लिये न्यूनतम बल के बराबर होता है।’
पाचक ग्रंथियाँ
यकृत (Liver)
- यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली (पित्ताशय) में सांद्रित एवं जमा होता है। यह विटामिन-A का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है।
- पित्त का लगातार स्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। यद्यपि पित्त में एंजाइम नहीं होते, फिर भी पित्त लवण भोजन, विशेषतः वसाओं के पाचन के लिये अत्यावश्यक होता है। पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है। लंबे समय तक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस B एवं C संक्रमण, विषाक्त धातुओं आदि के कारण यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यकृत के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं-
- बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण
- कार्बनिक पदार्थों का संग्रह
- एंजाइमों का स्रवण
- हिपैरिन का स्रवण
- लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिये आयरन को स्टोर करना
अग्न्याशय (Pancreas)
- अग्न्याशय U आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी, दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिर्स्रावी भाग से क्षारीय अग्न्याशयी रस निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है।
- अग्न्याशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिये उत्प्रेरक का कार्य करता है।
- SI पद्धति MKS पद्धति का संशोधित एवं परिवर्द्धित रूप है।
- वर्ष 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप-तौल अधिवेशन में SI पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। अब इसी पद्धति को मानक रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
- SI पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रकों तथा 2 संपूरक मात्रकों (Supplementary Units) को स्वीकार किया गया है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिये मात्रक ‘मोल’ को 1971 में मान्यता दी गई थी। तब से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 ही है।
|
SI पद्धति के सात मूल मात्रक |
|||
|
भौतिक राशि |
SI मात्रक |
प्रतीक |
विमा |
|
लंबाई |
मीटर (meter) |
m |
[L] |
|
द्रव्यमान |
किलोग्राम (kilogram) |
kg |
[M] |
|
समय |
सेकंड (second) |
s |
[T] |
|
विद्युत धारा |
एंपियर (ampere) |
A |
[A] |
|
ताप |
केल्विन (kelvin) |
K |
[K] |
|
ज्योति तीव्रता |
कैंडिला (candela) |
cd |
[cd] |
|
पदार्थ की मात्रा |
मोल (mole) |
mol |
[mol] |
- SI पद्धति के दो संपूरक मात्रक
|
1. |
समतल कोण (Plane Angle) |
रेडियन (Radian) |
rad |
|
2. |
ठोस कोण (Solid Angle) |
स्टेरेडियन (Steradian) |
sr |
- रेडियन (Radian)- वह कोण, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाता है, एक रेडियन कहलाता है।
- स्टेरेडियन (Steradian)- घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है।
- प्रोटीन बड़े, जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं जो पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ये मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु ज़रूरी होते हैं। ये शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक हैं।
- इन्हें पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पादप स्रोत- मटर, सोयाबीन, राजमा, चना एवं मूंग हैं तथा जंतु स्रोत- पनीर, मछली, मांस, अंडे एवं दूध इत्यादि हैं। सोयाबीन तथा पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जैसे-दूध, अंडा मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है तथा इन्हें संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एकमात्र गैर-पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
- प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्त्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के भी अंश पाए जाते हैं।
- प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें नहीं करतीं हैं।
- सामान्य क्रियाशील महिला हेतु प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा 45 ग्राम के करीब होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम के करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
- सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। जिसमें से 9 आवश्यक अमीनो अम्ल एवं 11 गैर-आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं।
- आवश्यक या तात्त्विक अमीनो अम्ल- मानव शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं हो सकता, अतः आहार के माध्यम से इन्हें लेना ज़रूरी होता है। उदाहरण- आइसोल्युसीन, हिस्टीडीन, ल्युसिन, मिथियोनीन, लाइसिन, वैलीन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनीन, फिनाइलएलानाइन।
- गैर-आवश्यक या अतात्त्विक अमीनो अम्ल- इसका उत्पादन मानव शरीर द्वारा संभव होता है, खासकर लिवर द्वारा। कुछ उदाहरण- ग्लूटामिन, प्रोलीन, ग्लाइसीन, आर्जिनीन, टाइरोसीन, सिस्टीन, एलानीन आदि।
(e) आँत (Intestine)
- मनुष्य की आँत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है।
- शाकाहारियों में आँत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र (Surface Area) मिल सके।
- मनुष्य की आँत को दो भागों में बाँटा जा सकता है-
छोटी आँत (Small Intestine)
- छोटी आँत तीन भागों में विभक्त होती है- ग्रहणी (Duodenum), अग्रक्षुद्रांत (Jejunum) तथा क्षुद्रांत (Ileum)
- आमाशय से निकलने के पश्चात् भोजन ‘अम्लान्न’ (Chyme) कहलाता है। यह काइम ग्रहणी में पहुँचता है जहाँ सबसे पहले यकृत से निकलकर पित्त रस इसमें मिलता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पित्त रस काइम को क्षारीय बना देता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशय रस आकर काइम में मिलता है। इसके पश्चात् यह इलियम में पहुँचता है, यहाँ आंत्र रस की क्रिया काइम पर होती है। छोटी आँत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत, उसका अवशोषण भी छोटी आँत में स्थित रसांकुर (Villi) द्वारा होता है। बिना पचा हुआ काइम बड़ी आँत में पहुँचता है जहाँ जल का अवशोषण होता है एवं शेष काइम मल के रूप में मलाशय में एकत्र होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
छोटी आँत में पाचन (Digestion in Small Intestine)
छोटी आँत में भोजन के आते ही इसमें तीन पाचक रस (पित्त रस, अग्न्याशय रस तथा आंत्र रस) मिला दिये जाते हैं।
- पित्त रस (Bile Juice)
- पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय (Gall Bladder) में संचित रहता है।
- पित्त रस गाढ़ा, हरे-पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है।
- मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली. पित्त रस स्रावित होता है।
- पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है।
- पित्त रस में पित्तवर्णक (Bile Pigment) जैसे- विलीरुबीन, बिली-वर्डिन आदि भी पाए जाते हैं।
- पित्त रस में उपस्थित दो लवण- सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा सोडियम टॉरोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी-छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं जिसे वसा का इमल्सीकरण (Emulsification of Fat) कहते हैं।
- वसा में घुलनशील विटामिन्स (K, E, D, A) के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- यदि किसी भी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है।
- अग्न्याशय रस (Pancreatic Juice)
- अग्न्याशय रस क्षारीय होता है जो अग्न्याशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है।
- इसमें 98% जल तथा शेष 2% एंजाइम व लवण (सोडियम बाइकार्बोनेट) होते हैं।
- इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिये पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अतः इसे ‘पूर्ण पाचक रस’ कहा जाता है।
- इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं।
- आंत्र रस (Intestinal Juice)
- यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है, जो आंत्र-ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है।
- मनुष्य में लगभग 2-3 लीटर आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है।
- आंत्र रस में निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं-
- माल्टेज- माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है।
- सुक्रेज- सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रेक्टोज में बदल देता है।
- लेक्टेज- लेक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है।
- इरेप्सिन- डाइ तथा ट्राइ पेप्टाइड (प्रोटीन के अवयव) को एमीनो अम्लों में तोड़ देता है।
इस प्रकार आँत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है।
बड़ी आँत (Large Intestine)
- बड़ी आँत, छोटी आँत की तुलना में अधिक चौड़ी, किंतु लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है।
- बड़ी आँत तीन भागों में विभक्त होती है-
- सीकम (Cecum)
- मलाशय (Rectum)
- कोलन (Colon)
- मनुष्य में सीकम से एक मुड़ी (Twisted) और कुंडलित (Coiled) लगभग 2 इंच लंबी रचना ‘वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स’ निकलती है। यह एक अवशेषी अंग है।
- बड़ी आँत कोई एंजाइम स्राव नहीं करती है। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिये संचित करना होता है। यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है।
(d) आमाशय (Stomach)-
- यह वक्षगुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है जो तीन भागों में बंटी रहती है- (i) अग्र भाग (कार्डियक), (ii) मध्य भाग (फंडिक), (iii) पश्च भाग (पाइलोरिक)
- आमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां (Gastric Glands) पाई जाती हैं।
आमाशय में पाचन (Digestion in Stomach)
- आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है।
- आमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित ‘जठर ग्रंथियाँ’ जठर रस स्रावित करती हैं, जो अत्यधिक अम्लीय (pH=1.8) होता है। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम्स, यथा- पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) एवं म्यूकस आते हैं।
- HCl की उपस्थिति में ‘पेप्सिनोजन’ सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं (पहले प्रोटिओज़ फिर पेप्टोंस) में तोड़ देता है। पेप्सिन का स्रवण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है।
- इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय ‘प्रोरेनिन’ सक्रिय ‘रेनिन’ में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है।
- आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम ‘गैस्ट्रिक लाइपेज’ वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है।
- म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर आमाशय की रक्षा करता है।
मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है- 1. आहार नाल तथा 2. सहायक पाचक ग्रंथियां
आहार नाल (Alimentary Canal or Gastrointestinal Tract)
यह एक लंबी व सतत् नलिका है हो मुख (Mouth) से गुदा (Anus) तक फैली हुई होती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है जो निम्नलिखित भागों में बंटी रहती है-
(a)मुखगुहा
(b)ग्रसनी
(c)ग्रासनली
(d)आमाशय
(e)आंत (छोटी आंत एवं बड़ी आंत)
(a) मुखगुहा (Oral Cavity or Buccal Cavity)-
- मुखगुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुखगुहा में जीभ तथा दांत होते हैं।
- स्वाद का अनुभव करने के लिये जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएँ (Taste Buds) पाई जाती हैं जो मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती हैं।
मुखगुहा में पाचन (Digestion in Mouth Cavity)
- पाचन का प्रारंभ मुखगुहा से ही हो जाता है जहाँ भोजन को ‘लार’ की सहायता से मथा जाता है।
- मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं।
- सभी लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं जिनमें 99% जल तथा 1% एंजाइम होते हैं। लार में मुख्यतः दो प्रकार के पाचक एंजाइम्स- टायलिन (Ptyalin) व लाइसोजाइम (Lysozyme) पाए जाते हैं।
- लार में टायलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैक्राइड माल्टोस में तोड़ देता है।
- लार में उपस्थित लाइसोजाइम व थायोसाइनेट आयन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं।
- भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड का पाचन मुखगुहा में ही हो जाता है।
(b) ग्रसनी (Pharynx)-
- मुखगुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है।
(c) ग्रासनली (Oesophagus)-
- मुखगुहा से लार युक्त भोजन ग्रासनली में पहुँचता है। यह एक लंबी नली है जो आ-माशय में खुलती है। इसकी क्रमाकुंचन (Peristalsis) क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है।
विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झाँसी, ग्वालियर और बिहार के आरा ज़िले शामिल थे।
- लखनऊ- यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हज़रत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया।
- कानपुर- विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था।
- झाँसी- 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उनके दत्तक पुत्र को झाँसी के सिंहासन पर बैठाने से इन्कार कर दिया।
- ग्वालियर- झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया।
- वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंतत: अंग्रेज़ों से हार गई।
- ग्वालियर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था।
- बिहार- विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर, बिहार के एक शाही घराने से थे।
दमन और विद्रोह
- 1857 का विद्रोह एक वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था।
- मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई, 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई।
विद्रोह के स्थान
भारतीय नेतृत्वकर्त्ता
विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी
दिल्ली
बहादुर शाह द्वितीय
जॉन निकोलसन
लखनऊ
बेगम हज़रत महल
हेनरी लॉरेंस
कानपुर
नाना साहेब
सर कॉलिन कैंपबेल
झाँसी एवं ग्वालियर
रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे
जनरल ह्यूरोज़
बरेली
खान बहादुर खान
सर कॉलिन कैंपबेल
इलाहाबाद (अब प्रयागराज) और बनारस
मौलवी लियाकत अली
कर्नल ऑनसेल
बिहार
कुँवर सिंह
विलियम टेलर
विद्रोह की असफलता के कारण
- सीमित प्रभाव- हालाँकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा।
- विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे- सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग।
- बड़ी रियासतें, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए।
- दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया।
- प्रभावी नेतृत्व नहीं- विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालाँकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके।
- सीमित संसाधन- सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेज़ों के अधीन थे। इसलिये विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी।
- मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं- अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और ज़मींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की।
विद्रोह का परिणाम
- कंपनी शासन का अंत- 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था।
- यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना।
- ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन- ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की ज़िम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली।
- इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी।
- भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा।
- भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिये बनाया गया था।
- धार्मिक सहिष्णुता- अंग्रेज़ों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति-रिवाज़ों और परंपराओं का सम्मान करेंगे।
- प्रशासनिक परिवर्तन- भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया।
- भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी।
- व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था।
- अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी।
- सैन्य पुनर्गठन- सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिये यह योजना बनाई गई थी।
इस प्रकार 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालाँकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिये।
हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव-
- हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए इनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का बाज़ारोन्मुख व गतिशील होना। हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भाँति मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन नहीं रही बल्कि यह अब ग्रामीण समाज के आय का मुख्य स्रोत बन गई है।
- किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ।
- इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्वकेंद्रण की भावना का विकास हुआ जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आई।
- हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई और इसने ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं, जैसे- जजमानी प्रथा, वस्तु-विनिमय (Barter) आदि, को समाप्त किया।
- हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिये अधिक लाभप्रद रही। इसका मुख्य कारण नई तकनीकी में लगने वाली अत्यधिक लागत थी जिसे छोटे किसानों द्वारा वहन करना संभव नहीं था।
- इसका परिणाम यह हुआ कि धनी व निर्धन किसानों के बीच असमानता बढ़ती गई। कुछ स्थानों पर इस असमानता की वजह से संघर्ष भी हुए।
- जहाँ हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज तथा संस्कृति में बदलाव किये, वहीं इससे कई नैतिक समस्याएँ भी पैदा हुईं। उत्तर भारत के इलाकों के किसानों जैसे- पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशा, शराब आदि के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ी।
- हरित क्रांति का महिलाओं के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पूर्व महिलाएँ बाहर खेतों में काम करके घर के पुरुष सदस्यों का हाथ बटाया करती थीं लेकिन किसानों की बढ़ती आय तथा मशीनों के बढ़ते प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं की स्वतंत्रता कम हुई।
हरित क्रांति के राजनीतिक प्रभाव-
- भारतीय राजनीति के क्षेत्र में हरित क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले। किसानों के नए वर्ग ने स्थानीय स्तर की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। पूर्व में राजनीति जहाँ समाज के उच्च जातियों तथा धनी वर्ग द्वारा ही नियंत्रित होती थी उसमें अब समाज के छोटे तबके के लोगों की भागीदारी बढ़ी।
- हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद ज़मींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार जैसे कदमों के चलते भारत में समतामूलक समाज के निर्माण को गति प्रदान की। इससे छोटे व मध्यम स्तर के किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इससे उनमें शिक्षा तथा राजनैतिक चेतना का विकास हुआ।
- किसान तथा उनसे संबंधित मुद्दों को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व दिया जाने लगा। इससे किसानों से संबंधित अनेक संगठनों का निर्माण हुआ तथा पूरे देश में उनकी भूमिका एक दबाव समूह की भाँति निर्मित हुई।
- किसान एवं उनसे संबंधित मुद्दे देश के मुख्य राजनीतिक दलों के लिये वोट बैंक बने तथा विभिन्न दलों ने किसानों के मुद्दों की वकालत करना प्रारंभ किया।
हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव-
- हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता दोनों में तीव्र वृद्धि हुई और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। वर्ष 1968 में गेहूँ का उत्पादन 170 लाख टन हो गया जो कि उस समय का रिकॉर्ड था तथा उसके बाद के वर्षों में यह उत्पादन लगातार बढ़ता गया।
- हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनों जैसे- ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ।
- कृषि के मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग होने वाली मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी तथा रासायनिक उर्वरकों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप देश में इससे संबंधित उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ।
- हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के विकास के लिये आवश्यक अवसंरचनाएँ जैसे- परिवहन सुविधा हेतु सड़कें, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, भंडारण केंद्रों और अनाज मंडियों का विकास होने लगा।
- विभिन्न फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) व अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना संभव हो सका। किसानों को दिये जाने वाले इस प्रोत्साहन मूल्य से वे नई कृषि तकनीकी अपनाने में सक्षम हुए।
- किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने लिये विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी बैंक तथा को-आपरेटिव सोसाइटी आदि के माध्यम से उन्हें ऋण सुविधाएँ दी जाने लगी। इसी कारण किसान कृषि में लगने वाली लागत को आसानी से इन संस्थाओं से प्राप्त कर सके।
- हरित क्रांति तथा मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर विकसित हुए। हरित क्रांति की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा ओडिशा से लाखों की संख्या में मज़दूर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोज़गार की तलाश में जाने लगे।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमज़ोर नीतियाँ थीं।
- उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और नाइट्रोजन- फास्फोरस- पोटैशियम (NPK) उर्वरकों का औसत इस्तेमाल एक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। गेहूँ और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी।
- वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी जो कि वर्तमान की जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई है लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था।
- रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही उपयोग करते थे। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं (1950-60) में सिंचित क्षेत्र के विस्तार व उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया लेकिन इन सबके बावजूद अनाज संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये शोध किये जा रहे थे तथा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। इसमें प्रोफेसर नार्मन बोरलाग प्रमुख हैं जिन्होंने गेहूँ की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है।
हरित क्रांति-
- वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई जब पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाए। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादकता किस्में (High Yielding Varieties- HYV) कहा जाता था।
- सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agriculture District Programme- IADP) नाम दिया गया। यह प्रयोग सफल रहा तथा वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया।
- मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिये प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
- पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVs के प्रयोग में सिंचाई के लिये अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अतः सरकार ने इनकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया तथा उर्वरकों आदि पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया।
- प्रारंभ में HYVs का प्रयोग गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया तथा गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई।
- आर्थिक कारण
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और ज़मींदार भूमि पर भारी-भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर-तरीकों से परेशान थे।
- अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिये गए कर्ज़ को चुकाने में असमर्थ थे जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीने हाथ से निकलती जा रही थी।
- बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार, गाँव को छोड़कर आए थे, इसलिये किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया।
- इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया।
- भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और ज़मींदार भूमि पर भारी-भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर-तरीकों से परेशान थे।
- सैन्य कारण
- 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ-
- भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था।
- एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था।
- उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी।
- वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है।
- 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ-
तात्कालिक कारण
- 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे।
- एक अफवाह यह फैल गई कि नई ‘एनफिल्ड’ राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है।
- सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुँह से खोलना पड़ता था।
- हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया।
- लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिये संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी।
- मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था।
- 8 अप्रैल, 1857 ई. को मंगल पांडे को फाँसी की सज़ा दे दी गई।
- 9 मई, 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को दस-दस वर्ष की सज़ा दी गई।
- ज्वालामुखी पृथ्वी की पर्पटी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट के दौरान गैसें, पिघली हुई चट्टानें (लावा), राख, भाप आदि बाहर की ओर उत्सर्जित होती हैं। ऐसे छिद्र पृथ्वी की पर्पटी के उन हिस्सों में होते हैं जहाँ चट्टानी स्तर अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं।
- ज्वालामुखी गतिविधि अंतर्जात प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी की विस्फोटक प्रकृति के आधार पर, अलग-अलग बहिर्वेधी भू-आकृतियाँ बन सकती हैं जैसे- पठार (यदि ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं है) या पहाड़ (यदि ज्वालामुखी विस्फोटक प्रकृति का है) या अंतर्वेधी भू-आकृतियाँ जैसे- बैकोलिथ, लैकोलिथ आदि।
- मैग्मा बनाम लावा-
- मैग्मा शब्द का प्रयोग पृथ्वी की आंतरिक पिघली हुई चट्टानों और संबंधित सामग्रियों को दर्शाने के लिये किया जाता है। मैंटल का एक कमज़ोर क्षेत्र जिसे दुर्बलतामंडल (Asthenosphere) कहा जाता है, आमतौर पर मैग्मा का स्रोत होता है।
- लावा और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह के ऊपर का मैग्मा है। एक बार जब यह मैग्मा ज्वालामुखी के छिद्र से पृथ्वी की सतह पर आया, तो इसे लावा कहा गया।
- ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्वानुमान हेतु उपकरण और तरीके-
- भूकंपीय डेटा- ज्वालामुखी विस्फोट के संभावित अग्रदूतों के रूप में भूकंप और झटकों की निगरानी करना।
- भूमि विरूपण- ज़मीन में बदलावों का अवलोकन करना, जो मैग्मा की गति का संकेत देता है।
- गैस उत्सर्जन और गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन- ज्वालामुखीय गैस उत्सर्जन, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विश्लेषण।
- पृथ्वी पर ज्वालामुखी का वितरण
- विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी तीन सु-परिभाषित बेल्ट में पाए जाते हैं-
- परि-प्रशांत मेखला
- मध्य-विश्व पर्वत बेल्ट
- अफ्रीकी रिफ्ट वैली बेल्ट
- विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी तीन सु-परिभाषित बेल्ट में पाए जाते हैं-
- मैग्मा बनाम लावा-
1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया।
विद्रोह
- यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी।
- यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली।
- विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है- सिपाही विद्रोह (ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा), भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह (भारतीय इतिहासकारों द्वारा), 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध (विनायक दामोदर सावरकर द्वारा)।
विद्रोह के कारण
- राजनीतिक कारण
- अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति- 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनैतिक कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था।
- बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारुढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया।
- रानी लक्ष्मी बाई के दत्तक पुत्र को झाँसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी।
- डलहौज़ी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झाँसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया।
- जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिये गए।
- लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया जिससे अभिजात वर्ग के हज़ारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोज़गार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य ‘अवध’ को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया।
- सामाजिक और धार्मिक कारण
- कंपनी शासन के विस्तार के साथ-साथ अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया।
- भारत में तेज़ी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था।
- अंग्रेज़ों के रहन-सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग-अविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था।
- 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया।
- ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी।
- भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था।
- इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज़ भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं।
- सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा-पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिये खतरा माना गया।
- शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे।
- यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया।
- आर्थिक प्रभाव
- उत्पादन में वृद्धि से वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी।
- उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि।
- स्वतंत्र कारीगर कारखानों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सके, फलत: कुटीर उद्योग समाप्त हो गए।
- बड़े-बड़े कृषि फार्मों की स्थापना के कारण छोटे किसानों को रोज़गार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर जाना पड़ा।
- औद्योगिक केंद्रों के आस-पास नवीन नगरों का विकास हुआ।
- अब शहर आर्थिक गतिविधियों का आधार बन गए।
- बाज़ारों की आवश्यकता ने सरकारों को उपनिवेश प्राप्ति के लिये प्रेरित किया।
- उत्पादक और उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया।
- औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ।
- सामाजिक प्रभाव
- औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ जैसे- मज़दूर एवं पूंजीपति।
- अब आर्थिक मापदंड संबंधों का मुख्य सूत्र बन गया।
- संबंधों का अर्थ आधारित होने से समाज में आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ गई।
- समाज में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ गया।
- श्रमिकों में सामाजिक चेतना का उदय।
- संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि।
- श्रमिकों के शोषण से वर्ग-संघर्ष की शुरुआत।
- औद्योगिक नगरों व केंद्रों की जनसंख्या बढ़ने से उनमें स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गईं।
- श्रमिकों को अमानुषिक एवं निराशाजनक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था।
- बाल श्रम की कुप्रथा व्यापक स्तर पर प्रचलित हो गई थी।
- चिकित्सा क्षेत्र में हुई महत्त्वपूर्ण खोजों के कारण मृत्यु दर में कमी आई।
- जनसंख्या वृद्धि से आवास समस्या बढ़ी और साथ ही बेरोज़गारी में वृद्धि हुई।
- महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में जनमत निर्मित हुआ।
- राजनीतिक प्रभाव
- औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राज्य के प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि हुई।
- उभरते मध्यवर्ग की संसदीय सुधार की मांग के कारण मताधिकार का विस्तार हुआ।
- राजनीतिक सत्ता भू-स्वामियों के हाथ से निकलकर उभरते मध्यवर्ग के हाथ में आ गई।
- विचारधारा पर प्रभाव
- नवीन अर्थशास्त्रियों ने पुरानी आर्थिक पद्धति के स्थान पर व्यापारिक स्वतंत्रता तथा उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर बल दिया।
- मज़दूरों की दशा सुधारने एवं जनकल्याण की भावना ने समाजवादी विधारधारा को जन्म दिया।
- ब्रिटेन का मानवतावदी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन आदर्शवादी समाजवाद का प्रणेत्ता था।
- कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स के विचारों और नेतृत्व में ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ ने जन्म लिया।
सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 124-147 (भाग-V के अध्याय 4) में, उच्च न्यायालयों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 214-232 (भाग-VI के अध्याय 5) में, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान अनुच्छेद 233-237 (भाग-VI के अध्याय 6) में, जबकि अधिकरणों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 323 (क) व 323 (ख) (भाग -XIV क), में हैं तथा आयोग, बोर्ड तथा फोरम आदि विभिन्न अधिनियम कार्यकारी आदेशों के आधार पर निर्मित किये जाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय
- न्यायाधीशों की नियुक्ति : राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से।
- न्यायाधीशों की अर्हताएँ :
- भारत का नागरिक हो।
- उच्च न्यायालय या न्यायालयों में न्यूनतम पाँच वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।
- उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर न्यूनतम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।
- शपथ : उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है।
- कार्यकाल : 65 वर्ष की आयु तक (संसद विधि द्वारा कार्यकाल निधारित करती है।)
- पद की रिक्ति : त्याग पत्र, कार्यकाल समाप्ति या महाभियोग [124(4)] द्वारा
- मूल या आरंभिक अधिकारिता :
- भारत सरकार बनाम राज्य सरकार/सरकारें
- दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद
- भारत सरकार + राज्य सरकार/सरकारें बनाम राज्य सरकार/सरकारें (अनुच्छेद-131)
- अपीलीय अधिकारिता :
- संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें (अनुच्छेद-132)
- सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें (अनुच्छेद-133)
- आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें (अनुच्छेद-134)
- विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें (अनुच्छेद-136)
- रिट अधिकारिता :
- पूरे देश में
- केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिये
- अभिलेख न्यायालय : अनुच्छेद-129 के तहत
- अधीक्षण संबंधी अधिकारिता : न्यायिक अधीक्षण अपने अधीनस्थ न्यायालयों का।
- सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अन्य प्रावधान : वर्तमान में ‘‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी।
ऊर्जा संसाधन शक्ति संसाधन कहे जाते हैं, जिन पर राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का विकास निर्भर करता है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों (सीमित मात्रा में उपलब्ध) के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम आदि एवं नवीकरणीय स्रोतों (असीमित मात्रा में उपलब्ध) के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, बायोमास आदि आते हैं। नवीकरणीय नि:शुल्क उपलब्ध संसाधनों के क्षय हेतु ‘आम व्यक्तियों की त्रासदी’ कहावत प्रयोग में लायी जाती है।
- भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, बायो ऊर्जा से 10 गीगावाट तथा लघु पनबिजली से 5 गीगावाट प्राप्त करना शामिल है।
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापन क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ने का लक्ष्य रखा है।
नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं-
- जल विद्युत ऊर्जा- भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ण करने वाला यह सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- पवन ऊर्जा- पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली हवाओं द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतघाटियों में, जहाँ प्रबल और लगातार हवाएँ चलती हैं, स्थापित किये जाते हैं।
- सौर ऊर्जा- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है और इसका दोहन अति मितव्ययिता के साथ किया जा सकता है। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान राज्य में है। भारत सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है जो नवीकरणीय ऊर्जा से कुल विद्युत उत्पादन का 57.1% है।
- भू-तापीय ऊर्जा- यह पृथ्वी के पर्पटी (Crust) में संचित ताप है, जिसे पृथ्वी के अंदर भंडारित यूरेनियम, थोरियम व पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण तथा पृथ्वी के क्रोड (Core) में मौजूद उच्च तापयुक्त तरल पदार्थ मैग्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये ऊर्जा ज्वालामुखी, उष्ण जल स्रोत आदि के रूप में पृथ्वी की सतह पर विद्यमान हैं।
- समुद्र ऊर्जा- समुद्र तरंग ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, समुद्री धाराएँ तथा तापीय ढाल के रूप में ऊर्जा के प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावित क्षमता 9000 मेगावाट है।
- बायोमास ऊर्जा- बायोमास के अंतर्गत जीवित या हाल-फिलहाल में मृत जीव, पौधे या जंतु आते हैं। बायोमास का प्रयोग नवीकरणीय विद्युत, थर्मल ऊर्जा या परिवहन ईंधन (जैव ईंधन-Biofuels) के उत्पादन हेतु किया जा सकता है। बायोमास ऊर्जा का आशय उन फसलों, अवशिष्टों एवं अन्य जैविक पदार्थों से है, जिनका उपयोग ऊर्जा या अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु, जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में किया जा सके।
- हाइड्रोजन ऊर्जा- भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को ही माना जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के लिये सर्वाधिक अनुकूल है। हाइड्रोजन का उपयोग विद्युत उत्पादन और परिवहन के लिये भी किया जा सकता है। यह सबसे सरल रासायनिक तत्त्व है (1 प्रोटॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन)। यह धरातल पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्त्वों में तीसरे स्थान पर आता है।
जलवायु परिवर्तन- जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होती है। मौसमी प्रतिरूप में लंबे समय के परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन सामान्यत: तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है, जो कई वर्षों में होता है। जलवायु परिवर्तन के भयंकर दुष्परिणामों से बचने के लिये विश्व के सभी देशों में यह सहमति बनी है वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2०C से नीचे और तापमान की वृद्धि को 1.5०C तक सीमित रखा जाए।
- जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक- जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। औद्योगीकरण से पहले इस प्रक्रिया में मानवीय कारकों की भूमिका कम थी। औद्योगीकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया तथा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक तापन व प्रदूषण के रूप में गंभीर समस्या सामने आई। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारक निम्नलिखित हैं-
- प्राकृतिक कारक (Natural Factors)- वायुमंडल सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है, जिस कारण मौसम एवं जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ में अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन परिवर्तन होते रहते हैं। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन हज़ारों वर्षों तक स्थायी रहते हैं एवं अत्यंत धीमी गति से घटते हैं। सौर विकिरण में विभिन्नता, सौरकलंक चक्र, ज्वालामुखीय उद्भेदन, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं।
- मानवजनित कारक (Anthropogenic Factors)- वर्तमान जलवायु परिवर्तन मानव जनित समस्या है। मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से पर्यवरण को प्रभावित करता है। मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्यों एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है। इस तरह की समस्याएँ पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं। मानवजनित कारक और उनका जलवायु परिवर्तन में योगदान-
- संसाधनों का दुरुपयोग
- नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगीकरण
- जीवाश्म ईंधन का प्रयोग
- भूमि-उपयोग में बड़े पैमाने पर बदलाव
- जलवाष्प, CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों (CH4, N2O, CFC) में वृद्धि
- समतापमंडल में ओज़ोन का ह्रास
- तापमान में वृद्धि
मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरा शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना ‘मृदा प्रदूषण’ कहलाता है। प्राय: जल भी भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। प्लास्टिक, कपड़ा, ग्लास, धातु और जैव पदार्थ, सीवेज, अपशिष्ट, औद्योगिक मलबा आदि मृदा प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। प्राकृतिक कारणों से भी मृदा की गुणवत्ता आदि में परिवर्तन होता है।
मृदा प्रदूषण के स्रोत (Sources of Soil Pollution)
- मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं- रसायनों का प्रयोग, भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन, मृदा अपरदन, उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक व नगरीय प्रदूषित अपशिष्ट, सिंचाई, हानिकारक सूक्ष्म जीव, डंपिंग आदि।
- रसायनों का प्रयोग- रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी कृषि के आवश्यक अंग हैं। रासायनिक उर्वरक फसलों के लिये आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करते हैं, परंतु इनके अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में भारी परिवर्तन आता है। जैवनाशी रसायन (कीटनाशी, रोगनाशी आदि), बैक्टीरिया सहित सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देते हैं।
- मृदा अपरदन- मृदा कणों का बाहरी कारकों, जैसे- वायु, जल या गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होकर बह जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन से कृषि क्षेत्र में कमी, बाढ़ आना, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आदि प्रभाव होते हैं।
- लवणीय जल- मृदा में उच्च लवणयुक्त जल के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। जल में उपस्थित लवण मृदा की ऊपरी परत पर जम जाता है। अम्लता की अधिक मात्रा का सांद्रण फसलों के लिये हानिकारक होता है।
- अन्य स्रोत- भूमिगत तथा रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, अम्ल वर्षा, विषैले पदार्थों का लीकेज, ठोस अपशिष्ट की डंपिंग, तेल अधिप्लाव तथा वनोन्मूलन, कृषि तकनीक व अकुशल सिंचाई, लैंडफिल, अतिचारण, शिफ्ट़िग कल्टीवेशन, सूक्ष्म जीव व बैक्टीरिया आदि भी मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। प्राकृतिक कारणों में कृषि की मात्रा व तीव्रता, तापमान व हवा, शैलिकीय कारक, मृदा की विशेषता आदि प्रमुख हैं।
मृदा प्रदूषण के प्रभाव (Effects of Soil Pollution)
- मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषित हो जाता है जिससे बहुत-सी बीमारियाँ होती हैं। लेड व आर्सेनिक की अधिक मात्रा से बच्चों का मानसिक विकास व शारीरिक विकास प्रभावित होता है। मल विसर्जन से भी विभिन्न रोग होते हैं, जैसे- एंथ्रेक्स (पशुओं में होने वाला), हुक वर्म, टिटनेस, आंत्र ज्वर, दस्त व पेचिस, सूजन आदि। इन सभी रोगों के लिये मृदा प्रदूषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार है।
- मृदा प्रदूषण से वनस्पति ह्रास व वनों में कमी होती है। इससे वैश्विक तापन के प्रभाव में भी वृद्धि होती है। मृदा अपरदन की समस्या, बाढ़, सूखा आदि अन्य बहुत से प्रभाव मृदा प्रदूषण के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। मृदा के माध्यम से प्रदूषक खाद्य शृंखला में पहुँच जाते हैं।
मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (Measures to Control Soil Pollution)
- उर्वरक, खरपतवार व कीटनाशी का सीमित प्रयोग करना चाहिये, इसकी अपेक्षा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिये।
- अपशिष्ट का उचित ढंग से निपटान करना चाहिये।
- डी.डी.टी. व अन्य हानिकारक रसायनों पर रोक लगा देनी चाहिये।
- राइज़ोबियम जैसे जैव उर्वरक का प्रयोग हो जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो सके।
- जैव उपचार तकनीक का प्रयोग।
- औद्योगिक कचरे का उचित निपटान, इसके लिये वेस्ट प्रबंधन तकनीक व पुनर्चक्रण प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिये।
- वृक्षारोपण व पशु खाद का प्रयोग।
- मृदा अपरदन को रोकने वाली तकनीक का प्रयोग।
‘74वें संविधान संशोधन’ द्वारा संविधान में भाग-9(क) जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है- ‘नगरपालिकाएँ’। इसमें अनुच्छेद-243P से अनुच्छेद- 243ZG तक शामिल हैं। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के लिये निर्दिष्ट 18 विषयों की सूची दी गई है।
अनुच्छेद- 243Q के अंतर्गत नगरपालिकाओं के तीन स्तरों की चर्चा की गई है-
- नगर पंचायत : यह संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है।
- नगरपालिका परिषद् : इन्हें छोटे शहरों में गठित किया जाता है।
- नगर निगम : इनका गठन बड़े शहरों या महानगरों में किया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है।
नगरपालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 243P : परिभाषाएँ
- अनुच्छेद 243Q : नगरपालिकाओं का गठन
- अनुच्छेद 243R : नगरपालिकाओं की संरचना
- अनुच्छेद 243S : वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
- अनुच्छेद 243T : स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 243U : नगरपालिकाओं की अवधि आदि
- अनुच्छेद 243V : सदस्यता के लिये निर्हताएँ
- अनुच्छेद 243W : नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
- अनुच्छेद 243X : नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उसकी निधियाँ
- अनुच्छेद 243Y : वित्त आयोग
- अनुच्छेद 243Z : नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
- अनुच्छेद 243ZA : नगरपालिकाओं के लिये निर्वाचन
- अनुच्छेद 243ZB : संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
- अनुच्छेद 243ZC : इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना
- अनुच्छेद 243ZD : ज़िला योजना के लिये समिति
- अनुच्छेद 243ZE : महानगर योजना के लिये समिति
- अनुच्छेद 243ZF : विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
- अनुच्छेद 243ZG : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप से संबंधित
- पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ‘आगमी सौर विकिरण’ या छोटे रूप में सूर्यातप (Insolation) कहते हैं।
- पृथ्वी भू-आभ है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है।
- पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी/प्रति वर्ग सेमी. प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है।
- वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोडा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है।
- सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात् 15 करोड़ 20 लाख किमी. दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर (Aphelion) कहा जाता है।
- 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात् 14 करोड़ 70 लाख किमी. दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर (Perihelion) कहा जाता है।
- इसलिये पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों, जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है।
- इसीलिये सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है।
पंचायतों का गठन, अनुच्छेद-243B
- प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। मध्यवर्ती पंचायत का गठन उन राज्यों में किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक हो।
पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद-243C
- राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संदर्भ में उपबंध कर सकता है।
|
स्तर |
संरचना |
अधिकारी |
निर्वाचन |
|
ग्राम स्तर |
ग्राम पंचायत |
प्रधान/मुखिया/सरपंच |
प्रत्यक्ष (राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया) |
|
खंड (ब्लॉक) स्तर |
क्षेत्र पंचायत |
प्रमुख |
अप्रत्यक्ष |
|
ज़िला स्तर |
ज़िला पंचायत |
अध्यक्ष/चेयरमैन |
अप्रत्यक्ष |
स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद-243D
- अनुच्छेद 243D में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं-
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है।
- पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है।
- महिलाओं के लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम-से-कम 1/3 स्थान आरक्षित हैं। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती।
- अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये जाएंगे। [उपर्युक्त तरह के आरक्षणों में स्थान चक्रानुक्रम (Rotation) पद्धति से आवंटित किये जाएंगे]
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों में से कम-से-कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।
- आरक्षण देने की उपर्युक्त व्यवस्था ग्राम तथा अन्य स्तर के लिये भी की जाएगी। पदों में आरक्षण के संदर्भ में राज्य की कुल जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा, जो कि स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में पंचायत स्तर की कुल जनसंख्या के आधार से अलग है।
अवधि अनुच्छेद- 243E
- प्रत्येक पंचायत, यदि किसी विधि के अधीन कार्यकाल से पूर्व विघटित नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुन: चुनाव करा लिया जाएगा।
राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद- 243I
- प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल, राज्य विधानमंडल में रखवाता है।
राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद- 243K
- पंचायतों के लिये कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त (राज्यपाल द्वारा नियुक्त) होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं रीति और आधार पर हटाया जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।
नोट: पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है।
जल निकायों का संरक्षण (Conservation of Water Bodies)- भारत की अधिकतर नदियाँ तथा झीलें प्रदूषण की शिकार हैं तथा इनका जल पीने योग्य नहीं रह गया है। यहाँ की नदियों एवं तालाबों के जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत असंसाधित मल-जल प्रवाह है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय’ का कार्य केंद्र प्रायोजित स्कीमों ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)’ एवं ‘जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना’ (NPCA) के तहत नदियों, झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan–GAP)- देश की प्रमुख नदियों में से एक तथा स्वयं का निर्मलीकरण (गंगा में पाए जाने वाले वायरस जैसे Bacteriophage वगैरह जीवाणुओं को खा जाते हैं।) करने वाली गंगा आज लगभग अपने अपवाह के आधे भाग में प्रदूषित हो गई है। वर्तमान में लगभग 50,000 से अधिक आबादी वाले 100 से अधिक शहरों का असंसाधित मल-अपशिष्ट गंगा में अपवाहित किया जाता है तथा हज़ारों की संख्या में लाशों व जले हुए अवशेषों को इसमें प्रवाहित किया जाता है। गंगा बेसिन में भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ‘केंद्रीय गंगा प्राधिकरण’ (CGA) का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान (GAP) की शुरुआत की गई।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan)- 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण (CGA) का नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण’ (NRCA) कर दिया गया था। गंगा कार्य योजना का विलय NRCP के साथ कर दिया गया।
नमामि गंगे कार्यक्रम (Namami Gange Project)- केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिये ` 20,000 करोड़ आवंटित किये गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को खत्म करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य स्तंभ हैं-
- सीवरेज ट्रीटमेंट
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
- वनीकरण
- जैव विविधता का विकास
- जन-जागरूकता
- गंगा ग्राम योजना
- नदी सतह की सफाई
- औद्योगिक प्रवाह निगरानी
19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक चिंतक कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की व्यापक आलोचना की और समाजवाद के नाम से एक वैकल्पिक प्रणाली प्रस्तावित की। उनके दर्शन, जिसे अक्सर मार्क्सवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है, ने राजनीतिक विचार के विकास को गहराई से प्रभावित किया और कई सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया।
ऐतिहासिक भौतिकवाद
- मूल विचार- भौतिक परिस्थितियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति होती हैं।
- उत्पादन के तरीके- समाज का विकास उत्पादन के तरीकों और उत्पादन संबंधों पर आधारित होता है।
- वर्ग संघर्ष- सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष के माध्यम से प्रगति होती है जो क्रांतिकारी परिवर्तनों की ओर ले जाती है।
वर्ग संघर्ष
- मुख्य संघर्ष- बुर्जुआ (पूंजीपति वर्ग) और सर्वहारा (मजदूर वर्ग) के बीच।
- शोषण- बुर्जुआ सर्वहारा का शोषण करते हैं और उनके श्रम से अधिशेष मूल्य निकालते हैं।
- अंतर्निहित तनाव- इन तनावों और पूंजीवाद के अंतर्विरोधों के कारण अंततः इसका पतन हो जाता है।
अलगाव का सिद्धांत
- प्रमुख अवधारणा- मजदूर अपने श्रम, अपने द्वारा निर्मित उत्पादों, अपने सहकर्मियों और अपनी मानव क्षमता से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार आवश्यकता का क्षेत्र उसके जीवन को काबू करता है और व्यक्ति स्वयं से कट जाता है।
- अलगाव का कारण- मजदूर उत्पादन के साधनों के मालिक नहीं होते और उन्हें मजदूरी के बदले अपना श्रम बेचना पड़ता है।
- प्रभाव- इससे नियंत्रण का नुकसान और अपने कार्य एवं स्वयं से अलगाव की भावना उत्पन्न होती है।
क्रांति और साम्यवाद
- सर्वहारा क्रांति- मजदूर वर्ग बुर्जुआ के खिलाफ उठेगा और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा।
- साम्यवाद की स्थापना- एक वर्गहीन एवं राज्यहीन समाज जहां उत्पादन के साधन सामूहिक स्वामित्व में होंगे।
- आवश्यकता पर आधारित वितरण- वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लाभ के बजाय आवश्यकता के आधार पर होगा।
- शोषण का अंत- साम्यवाद का उद्देश्य पूंजीवाद में पाए जाने वाले शोषण और अलगाव को समाप्त करना है।
प्रभाव और विरासत
- स्थायी प्रभाव- मार्क्स के विचारों ने राजनीतिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र और सामाजिक आंदोलनों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
- प्रमुख कार्य- "द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो" और "दास कैपिटल" अभी भी व्यापक रूप से अध्ययन किए जाते हैं।
- 20वीं और 21वीं सदी के आंदोलन- विभिन्न समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों ने मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरणा ली है।
- आधुनिक प्रासंगिकता- तमाम आलोचनाओं के बावजूद, पूंजीवाद का मार्क्स का विश्लेषण और एक समतावादी समाज की उनकी दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के बारे में महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।
संकट या खतरा (Hazard) उस घटना को कहते हैं जिसमें बड़े स्तर पर विनाश अर्थात् जीवन, संपत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचने की संभावना होती है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगली आग, सूखा इत्यादि प्राकृतिक संकट हैं जिनसे अत्यधिक विनाश की संभावना रहती है। किंतु यही संकट जब मानव आबादी वाले क्षेत्रों में अपना विध्वंसात्मक प्रभाव दिखाता है अर्थात् बड़े स्तर पर जान-माल की क्षति का कारण बनता है तब उसे आपदा (Disaster) कहा जाता है। अत: कहा जा सकता है कि संकट या खतरा तब आपदा का रूप ले लेता है जब वह मानव आबादी वाले क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाता है। संकट और आपदा प्राकृतिक और मानवनिर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा भू-स्खलन प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं, जबकि परमाणु विकिरण/विस्फोट, यातायात दुर्घटना, मानव आबादी वाले क्षेत्रों में लगी आग इत्यादि मानव निर्मित आपदाएँ हैं। कई बार तो मानवीय क्रियाकलाप, जैसे- भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास व निर्माण कार्य, परमाणु विखंडन आदि भी प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में प्रभावी कारक हो जाते हैं।
संकट या खतरों का वर्गीकरण (Classification of Hazards)
संकट और आपदा को विभिन्न प्रकारों में बाँटा गया है, जिनमें से प्रमुख हैं : भू-वैज्ञानिक संकट, जल-मौसमी संकट, पर्यावरणीय संकट, जैविक संकट, रासायनिक-औद्योगिक-परमाणविक संकट, दुर्घटनाजन्य संकट।
- भू-वैज्ञानिक संकट (Geological Hazards) : भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, भू-स्खलन, बांध टूटना, खदान में आग।
- जल व मौसमी संकट (Hydro-Meteorlogical Hazards) : तूफान, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बादल फटना, भू-स्खलन, बाढ़, सूखा, लू, पाला, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, ओला-वृष्टि, बर्फानी तूफान।
- पर्यावरणीय संकट (Environmental Hazards) : पर्यावरण प्रदूषण वनों की कटाई, बंजरीकरण, कीट संक्रमण (अप्रीका महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सर्वाधिक खतरा है।)
- जैविक संकट (Biological Hazards) : महामारी (मानव व पशुओं से संबद्ध), खाद्य विषाक्तता, जन विनाशक हथियारों का प्रयोग।
- रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणविक दुर्घटनाएँ (Chemical, Industrial and Nuclear Accidents) : रासायनिक संकट, औद्योगिक संकट, तेल रिसाव, तेल में आग, परमाणविक संकट।
- दुर्घटना संबंधित संकट (Accident Related Hazards) : ट्रेन/नाव/सड़क दुर्घटना, विमान दुर्घटना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगी आग, वन में आग, बम विस्फोट, भवन गिरना, खदान में पानी भरना, विद्युत दुर्घटना, समारोह में दुर्घटना।
फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक कारणों के संयोजन से उत्पन्न हुई थी, जिसने एक अस्थिर वातावरण पैदा किया जो क्रांति के लिये उपयुक्त था।
राजनीतिक कारण-
- निरंकुश राजतंत्र और अयोग्यता :
- बूर्बो राजवंश का राजा लुई XVI के निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। राजा की स्वेच्छाचारी शासन शैली एवं निरंकुशता ने अभिजात वर्ग तथा आम लोगों दोनों को अलग-थलग कर दिया।
- एस्टेट्स-जनरल, जो तीन एस्टेट्स (पादरी, कुलीन वर्ग और सामान्य लोग) का प्रतिनिधित्व करती थी, 1614 से उसकी बैठक नहीं बुलाई गई थी, जिससे शिकायतों के निवारण के लिये कोई मंच नहीं बचा था।
सामाजिक कारण-
- कठोर सामाजिक पदानुक्रम :
- फ्रांसीसी समाज को तीन एस्टेट्स में विभाजित था। प्रथम एस्टेट (पादरी) और द्वितीय एस्टेट (कुलीन वर्ग) को महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन्हें कई करों से छूट भी प्राप्त थी। जबकि तृतीय एस्टेट (सामान्य लोग) कर का मुख्य बोझ उठाते थे।
- मध्यम वर्ग, अपनी आर्थिक महत्ता के बावजूद, राजनीतिक शक्ति से वंचित था एवं राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व न प्राप्त होने से खिन्न था। यह वर्ग ऊपरी एस्टेट्स के विशेषाधिकारों से नफरत करता था। इसके अलावा किसान और शहरी श्रमिक खराब जीवन स्थितियों और सामंतों से पीड़ित थे।
आर्थिक कारण-
- वित्तीय संकट :
- महंगे युद्धों, जैसे कि अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की भागीदारी ने शाही खजाने को समाप्त कर दिया था। 1780 के दशक के अंत तक सरकार को गंभीर कर्ज का सामना करना पड़ा।
- राजा लुई XVI के कर प्रणाली में सुधार के प्रयासों को अभिजात वर्ग द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। उन्होंने करों से प्राप्त छूट को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे व्यापक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
- जीविका संकट :
- व्यापक गरीबी, बेरोज़गारी और अनाज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की दुर्दशा को बढ़ा दिया। 1780 के दशक के अंत में सूखे की वजह से फसल के मारे जाने से खाद्य पदार्थों की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे सार्वजनिक असंतोष बढ़ गया।
बौद्धिक कारण-
- प्रबोधन विचार :
- वाल्टेयर, रूसो तथा मोंटेस्क्यू जैसे प्रबोधन दार्शनिकों ने निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समर्थन किया।
- उनके लेखन ने मध्यम वर्ग और शिक्षित सामान्य लोगों को पारंपरिक अधिकार पर सवाल उठाने और राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारों की मांग करने के लिए प्रेरित किया।
फ्रांसीसी क्रांति लंबे समय से चली आ रही शिकायतों और तात्कालिक असंतोषजनक घटनाओं का परिणाम थी। असमान सामाजिक संरचना, आर्थिक संकट एवं तात्कालिक विचारकों के क्रांतिकारी विचारों ने उत्साह के लिये एक उपजाऊ जमीन तैयार की। वित्तीय संकट और राजतंत्र की प्रभावी सुधार लागू करने में विफलता ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिससे एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसने सत्ता और विशेषाधिकार की स्थापित प्रणालियों को बदल दिया। यह क्रांति प्राचीन शासन के अंत तथा फ्रांसीसी और विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनी।
भारत में जैव विविधता में बढ़ते ह्रास दर को देखते हुए सभी जीवित स्रोतों के संरक्षण को और अधिक प्रभावशाली तरीके से संरक्षित करने हेतु 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को परंपरागत संरक्षण के ज्ञान से जोड़कर जैवमंडल प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना तथा दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग के लिये समर्थ तंत्र का विकास करना है।
|
भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserves in India) |
|
|
नीलगिरि* |
|
|
नंदा देवी* |
|
|
नोकरेक* |
|
|
मानस |
|
|
सुंदरवन* |
|
|
मन्नार की खाड़ी* |
|
|
ग्रेट |
|
|
सिमलीपाल* |
|
|
डिब्रू साइखोवा |
|
|
दिहांग- दिबांग |
|
|
पंचमढ़ी* |
|
|
कंचनजंगा* |
|
|
अगस्त्यमाला* |
|
|
अचानकमार- अमरकंटक* |
|
|
कच्छ |
|
|
शीत मरुस्थल |
|
|
शेषाचलम |
|
|
पन्ना* |
|
|
नोट : *इन्हें यूनेस्को के Man And Biosphere (MAB) कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिज़र्व की विश्वतंत्र सूची में शामिल किया गया है। |
|
1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा के अनुसार- ‘‘जैव विविधता समस्त स्रोतों, यथा- अंतर्क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूहों जिनके ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विविधताएँ हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित हैं।’’
‘जैव विविधता’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया इस पर विवाद है। माना जाता है कि 1980 में ‘जैविक विविधता’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जैव विविधता ‘जैविक विविधता’ (Biological Diversity) का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता (Biodiversity) शब्द का प्रयोग वाल्टर जी. रोजेन द्वारा 1985 में किया गया।
जैव विविधता के प्रकार (Types of Biodiversity)
- आनुवंशिक विविधता : किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन आनुवंशिक विविधता है। उदाहरण: खरगोश की विभिन्न नस्लें।
- प्रजातीय विविधता : इसका आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव-जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है। उदाहरण: किसी समुदाय की विभिन्न प्रजातियाँ।
- सामुदायिक या पारितंत्र विविधता : एक समुदाय के जीव-जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव-जंतुओं व वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है।
जैव विविधता का मापन (Measurement of Biodiversity)
इसका आशय प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। इस हेतु 3 विधियाँ प्रचलन में हैं-
- α-विविधता (Alpha Diversity) : यह किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता है।
- β-विविधता (Beta Diversity) : इसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है।
- γ-विविधता (Gamma Diversity) : इसके द्वारा एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता का पता चलता है।
जैव विविधता की प्रवणता (Gradient of Biodiversity)
- अक्षांशों में प्राय: उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश (ध्रुवों से भूमध्य रेखा) की ओर परिस्थितियाँ अनुकूल होने के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर जाने पर एक किमी. के अंतराल पर तापमान में 6.5ºC की कमी होती है जो जैव विविधता का बड़ा कारण है।
जैव विविधता को खतरा (Biodiversity Under Threat)
- प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक है। अन्य कारण- कृषि क्षेत्रों का विस्तार, पशु-पक्षियों का अवैध शिकार, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी; प्राकृतिक कारण, यथा- बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन इत्यादि।
पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है, जिसमें इसकी जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टान्सले द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकीय पदचिह्न संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्पादक भूमि तथा जल के क्षेत्र को निरूपित करता है।
पारिस्थितिक तंत्र के संघटक (Components of An Ecosystem)
पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं- अजैविक संघटक, जैविक संघटक एवं ऊर्जा संघटक।
- अजैविक संघटक-
- ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किये हुए निर्जीव अवयव होते हैं, जो जीवों की उत्तरजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 मुख्य अजैविक कारक- प्रकाश/ताप, वायु, मृदा, जल/आर्द्रता।
- जैविक संघटक-
- ये जीवित अवयव होते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं।
- कार्यात्मक आधार पर जैविक संघटक के तीन भाग होते हैं- स्वपोषित संघटक, परपोषित संघटक एवं वियोजक।
- स्वपोषित संघटक (Autotrophs) : ये आहार शृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया क्रमश: प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इन्हें प्रथम पोषण स्तर (First Trophic Level) के अंतर्गत रखा जाता है।
- परपोषित संघटक (Heterotrophs) : इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिये पौधों, जंतुओं या दोनों पर निर्भर होते हैं।
आहार के स्रोत के आधार पर परपोषी के 3 प्रकार-
- शाकाहारी (Herbivores) : ये अपना भोजन मुख्यत: पौधों से प्राप्त करते है। अत: ये ‘प्राथमिक उपभोक्ता’ कहलाते हैं। ये पोषण स्तर-2 के अंतर्गत आते हैं।
- मांसाहारी (Carnivores) : ये स्वयं के पोषण हेतु शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इन्हें ‘द्वितीयक उपभोक्ता’ भी कहते हैं। ये पोषण स्तर-3 के अंतर्गत आते हैं।
- सर्वाहारी (Omnivores) : ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को आहार बनाते हैं। ये नीचे के तीनों पोषण स्तर से आहार प्राप्त करते हैं।
जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी के 3 प्रकार होते हैं- परजीवी (Parasites), मृतजीवी (Saprophytes) तथा प्राणीसमभोजी (Holozoic)
- वियोजक (Decomposers) : अपघटक या वियोजक जटिल जैविक पदार्थों (मृत पौधों तथा जंतुओं) का वियोजन कर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं और अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इन सरल रूपों को हरे पौधे ग्रहण करते हैं। ये हमेशा सूक्ष्म जीवी नहीं होते।
- वियोजक दो प्रकार के होते हैं- कवक/बैक्टीरिया तथा अपरदकारी (Detritivores)
- ऊर्जा संघटक-
- इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है।
- सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, अत: इसे ‘विद्युत चुंबकीय विकिरण’ भी कहा जाता है।
- सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें ‘फोटॉन’ कहते है।
- पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यातप या सौर विकिरण कहते हैं।
- पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुँचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं।
पर्यावरण का आशय जैविक तथा अजैविक घटकों एवं उनके आस-पास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। इसके अंतर्गत मानवजनित पर्यावरण, यथा-सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है।
पर्यावरण के निम्नलिखित 4 तत्त्व हैं-
स्थलमंडल (Lithosphere) : यह पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी भाग है, जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी मैंटल के सबसे ऊपरी भाग से बना है। क्रस्ट या भूपर्पटी को दो भागों में बांटा जा सकता है- महाद्वीपीय एवं महासागरीय भूपर्पटी। स्थलमंडल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। लेकिन यह महासागरों और महाद्वीपों के बीच भिन्न होती है। स्थलमंडल की मोटाई महासागरीय भाग में कुछ किलोमीटर से लेकर महाद्वीपों में लगभग 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह विभिन्न प्रकार के शैलों जैसे- आग्नेय (Igneous), अवसादी (Sedimentary) और रूपांतरित (Metamorphic) शैलों से बना है।
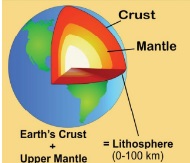
जलमंडल (Hydrosphere) : यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, धरातल के नीचे एवं हवा में पाए जाने वाले जल को सम्मिलित करते हैं। यह द्रव, वाष्प एवं हिम के रूप में हो सकता है। पृथ्वी की सतह में पाया जाने वाला जल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है-
- स्वच्छ जल (लगभग 3%- हिमनदों, झीलों, सरिताओं तथा भूजल के रूप में संग्रहीत)
- लवणीय जल (लगभग 97%- सागरों और महासागरों में भंडारित)।
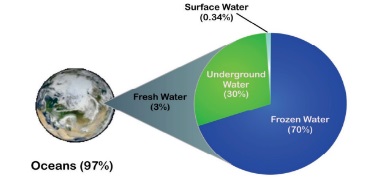
वायुमंडल (Atmosphere) : वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैस, जलवाष्प तथा धूलकणों का मिश्रण है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड महत्त्वपूर्ण हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों में क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल तथा बाह्यमंडल सम्मिलित हैं, जिनमें प्रथम दो परतें पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं।
जैवमंडल (Biosphere) : बायोम के समूह को ‘जैवमंडल’ कहते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल एवं जलमंडल आपस में मिलते हैं एवं वहाँ जीवन का कोई अंश ज़रूर मौजूद होता है। इस मंडल के बाहर जीवन नहीं पाया जाता है।
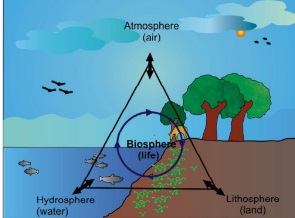
- पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी है। एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है। चट्टान कठोर या मुलायम साथ ही विभिन्न रंगों की हो सकती है। उदाहरण के लिये-
- ग्रेनाइट कठोर है, सोपस्टोन मुलायम है।
- गैब्रो काला है और क्वार्टजाइट दूधिया सफेद हो सकता है।
- चट्टानों में खनिज घटकों की निश्चित संरचना नहीं होती है। फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज चट्टानों में पाए जाने वाले सबसे आम खनिज हैं।
- विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिन्हें उनके निर्माण के तरीके के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है-
आग्नेय शैल- मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण- ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि।
आग्नेय शैलों की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- अवसादी चट्टानों की तुलना में आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी तथा प्रतिरोधी होती है। परंतु कभी-कभी अधिक समय तक खुले रहने के कारण कुछ आग्नेय चट्टानें मुलायम हो जाती हैं।
- इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है।
- ये चट्टानें रवेदार होती हैं तथा इनके रवों में काफी भिन्नता मिलती है।
- आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
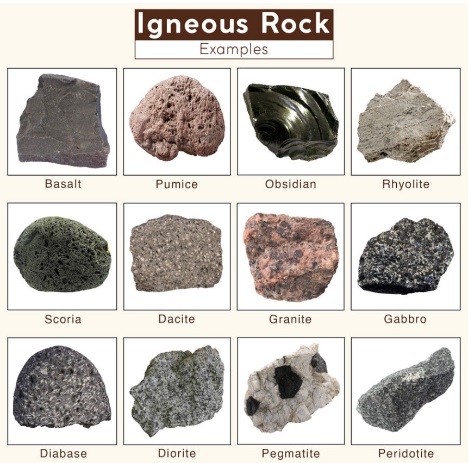
अवसादी शैल- अवसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम हैं। इसे द्वितीयक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे- बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि।
अवसादी शैलों की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
इनमें परतें पाई जाती हैं। ये परत निक्षेप धरातल के समानांतर तथा एक-दूसरे से रंग एवं कणों की बनावट में भिन्न होती हैं। परतों की वजह से ये स्लैब के टुकड़ों के समान उखड़ती है।
अवसादी शैलों में विभाजक तल मिलते हैं जिसको संस्तरणतल कहा जाता है।
आग्नेय शैलों की तुलना में ये मुलायम होती हैं और भू-धरातल के ठीक नीचे पाई जाती हैं।
इन शैलों में पौधों और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं।

अवसादी शैलों का रंग कार्बनिक पदार्थों तथा लोहे के ऑक्साइड के कारण भिन्न-भिन्न होता है।
रूपांतरित शैल- पहले से मौजूद चट्टानें, जो पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही हैं, रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। तृतीयक चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का दूसरा नाम हैं। जैसे- फायलाइट, शिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट और मार्बल आदि।
रूपांतरित शैलों की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
रूपांतरित चट्टानें विभिन्न उत्पत्ति की होती हैं क्योंकि इनका निर्माण अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों से होता है। यहाँ तक कि कभी-कभी इनका निर्माण रूपांतरित शैलों में पुनर्रूपांतरण से भी होता है।
ये वास्तविक अवसादी और आग्नेय चट्टानों की तुलना में ये चट्टानें अधिक कठोर एवं घनी होती हैं।
इन शैलों में पहले के चट्टान का गुण मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी।
रूपांतरित शैलों में बहुमूल्य धातुएं एवं खनिज पाए जाते हैं।
वास्तविक चट्टान की अपेक्षा अपरदन हेतु ये अधिक प्रतिरोधी होती हैं।
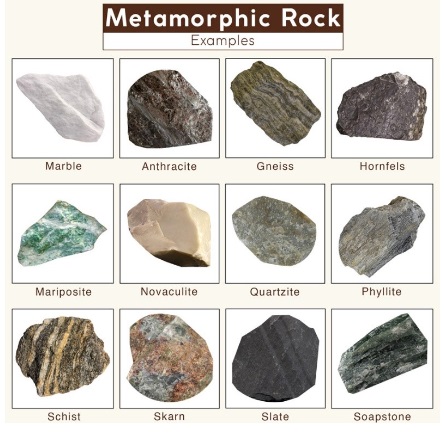
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23½° झुकी हुई है। इसका अक्ष अंडाकार कक्षतल के साथ 66½° का कोण बनाता है। पृथ्वी की दो प्रमुख गतियाँ हैं- घूर्णन गति (Rotation) और परिभ्रमण गति (Revolution)। पहली को दैनिक गति तथा दूसरे को वार्षिक गति भी कहते हैं। इन गतियों का पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
पृथ्वी का घूर्णन (Rotation of Earth)-
पृथ्वी का अपने ध्रुवीय अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसका अक्ष भूमध्यरेखीय तल के लम्बवत रहता है तथा केंद्र से होकर गुजरता है। इसके एक पूर्ण घूर्णन की अवधि लगभग 24 घंटे (23 घंटा, 56 मिनट, 4.09 सेकंड)है। यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है। इसीलिये इसे दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं-
- दिन एवं रात का होना
- सूर्योदय, दोपहर एवं सूर्यास्त का होना
- समय का निर्धारण
- दिशा का निर्धारण
- पवनों और समुद्री धाराओं में विक्षेपण
- दैनिक ज्वार-भाटा की स्थिति में परिवर्तन
- ध्रुवों पर चपटापन
- भूमध्य रेखा पर उभार
पृथ्वी का परिभ्रमण (Revolution of Earth)-
अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी का परिभ्रमण कक्ष पूर्ण वृत्ताकार न होकर अंडाकार (Elliptical) है। सूर्य के चतुर्दिक होने वाले पृथ्वी के भ्रमण को परिभ्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण पूरा करने में लगभग 365 ¼ दिन लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो इस दशा को अपसौर (Aphelion) कहा जाता है। यह दशा जुलाई में आती है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है तो इस दशा को उपसौर (Perihelion) कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं-
- ऋतुओं में परिवर्तन
- दिन एवं रात्रि की अवधि में भिन्नता
- ग्रीष्म एवं शीत ऋतु की गहनता में भिन्नता
- ध्रुव तारे का एक दिशा में दिखाई पड़ना
- पवनपेटियों का खिसकाव
- अक्षांशों का निर्धारण
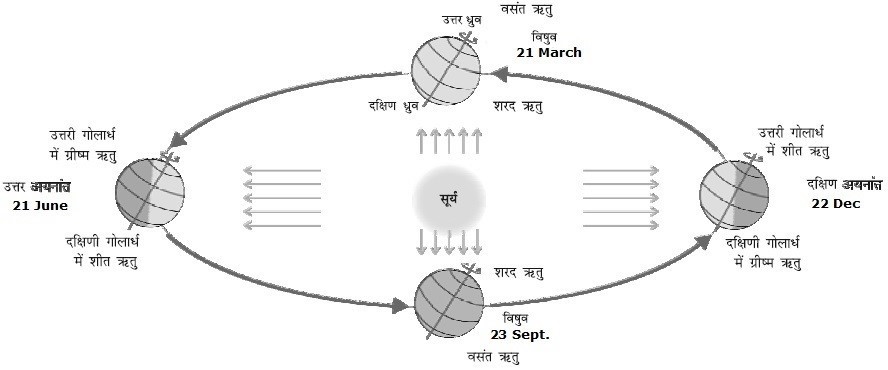
अन्य गतियाँ-
पृथ्वी की धुरी के झुकाव में धीरे-धीरे परिवर्तन होता है, जिसे अक्षीय पूर्वता (Axial Precession) कहते हैं। यह लगभग 26,000 वर्षों में एक चक्र पूरा करता है। इसके अलावा, पृथ्वी की कक्षा की दिशा और आकार में भी परिवर्तन होते हैं, जिन्हें कक्षीय अवशोषण (Orbital Eccentricity) और कक्षीय पूर्वता (Orbital Precession) कहते हैं। इन सबका संयुक्त प्रभाव दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन में दिखाई देता है
शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है-
- शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है (Teaching is a Tripolar Process)- शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्चा शिक्षण के तीन ध्रुव हैं। बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष- शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं।
- शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है (Teaching is a Science as well as an Art)- शिक्षा मनोवैज्ञानिक एन.एल. पेज के अनुसार शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण अनुभवों पर आधारित है इसलिये कला है। शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य इसके वैज्ञानिक पक्ष के महत्त्व को दर्शाता है।
- शिक्षण अंत:प्रक्रिया है (Teaching is an Inter-Active Process)- शिक्षण में सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है।
- शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है (Teaching is a Social and Professional Process)- शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है।
- शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है (Teaching is an Intentional Process)- किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।
- शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है (Teaching is a Process of Development)- शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है।
- शिक्षण औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है (Teaching is both Formal and Informal Process)- शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।
- शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है (Teaching is a Therapeutic Process)- शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- शिक्षण भाषायी प्रक्रिया है (Teaching is a Linguistic Process)- शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करती है।
- शिक्षण सतत् प्रक्रिया है (Teaching is a Continuous Process)- शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी जीवनभर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है।
- अध्येता का सामान्य अर्थ होता है- ‘अध्ययन करने वाला’।
- अध्येता को ‘अधिगमकर्त्ता’, ‘शिक्षार्थी’ या ‘विद्यार्थी’ भी कहते हैं।
- शिक्षण के केंद्रबिंदु में अध्येता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
- अध्येता शिक्षा ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही वह सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों को आत्मसात करता है तो वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है।
- विद्यालयी वातावरण अध्येता के मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव हमें सभी शिक्षक व साथी सहपाठियों के साथ अध्येता के मिलनसार व्यवहार में दिखाई देता है। विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो उसे जीवनपर्यंत बेहतर नागरिक बनने के लिये प्रेरित करता है।
अध्येता की विशेषताएँ (Characteristics of Learner)
एक अध्येता के सद्गुणों व विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख निम्नलिखित अवयवों/बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-
- मूल प्रवृत्तियाँ : प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी-मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं, इन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं।
- संवेग एवं स्थायी भाव : प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुख-दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। इन अनुभवों से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे मानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन भावों को मनोवैज्ञानिक भाषा में ‘संवेग’ कहते हैं। स्थायी भाव एक अर्जित संस्कार है। अर्जित संस्कार धीरे-धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप धारण कर लेते हैं, फलस्वरूप आचरण व व्यवहार नियंत्रित होने लगते हैं।
- अभिवृद्धि एवं विकास : किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को ‘अभिवृद्धि’ कहते हैं और किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है, उसे ‘विकास’ कहते हैं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण : बालक को अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों और पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएँ और गुण प्राप्त होते हैं, उन्हें ‘वंशानुक्रम’ के नाम से जाना जाता है। किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण अथवा घेरे को ही ‘वातावरण’ कहते हैं।
- खेल एवं खेल प्रणाली : अध्येता के विकास में खेलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है।
शिक्षण सहायक सामग्री/संसाधन का अर्थ (Meaning of Teaching Material/Resources)-
ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर शब्दकोष के अनुसार, “वह चीज़ जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाई जाती है उसे सामग्री या संसाधन कहा जाता है।” पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एक अध्यापक के लिये शब्दकोष, नक्शा, ग्लोब, विद्यालय का बगीचा, वीडियो फिल्म इत्यादि सहायक सामग्री का कार्य करते हैं।
एक शिक्षक जो पौधों के बारे में पढ़ाना चाहता है, वह विद्यालय के बगीचे को एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है। एक शिक्षक नदी तथा तालाब की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिये नदी या तालाब के पास भ्रमण की व्यवस्था कर सकता है या उनकी फिल्म/वीडियो क्लिप इत्यादि दिखा सकता है। ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य करते हैं। अत: शिक्षण सहायक सामग्री वह साधन है जिससे शिक्षार्थी का सीखना अत्यंत सहज हो जाता है।
शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषाएँ (Definitions of Teaching Aids)-
शिक्षण सहायक सामग्री को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है-
- डेंड के मतानुसार, ‘‘शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या मौखिक पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है।’’
- कार्टर ए. गुड के मतानुसार, ‘‘जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रज्वलित किया जा सके या श्रवणेन्द्रिय संवेदनाओं द्वारा उसे आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है।’’
शिक्षण सहायक सामग्री के भाग (Parts of Teaching Aids)-
इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को आमतौर पर निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जा सकता है-
- दृश्य-सहायक सामग्री (Visual Aids)- दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है, जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों (आँखों) का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपटे, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड इत्यादि शामिल हैं।
- श्रव्य-सहायक सामग्री (Audio Aids)- श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल श्रवणेंद्रियों (कानों) का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेपरिकॉर्डर इत्यादि शामिल हैं।
- दृश्य-श्रव्य सामग्री (Visual-Audio Aids)- दृश्य-श्रव्य सामग्री से तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है, जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तथा कठिन-से कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। एडगर डेल के मतानुसार, ‘‘दृश्य-श्रव्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण-प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का सम्प्रेषण किया जाता है। इन्हें बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है।’’




